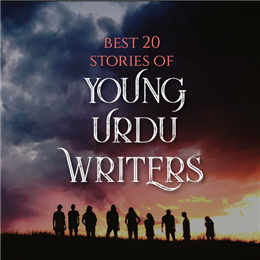आँख की पुतली का तमाशा
“मुझे उससे दस घंटे मुहब्बत हुई थी सिर्फ़ दस घंटे...
इसके बा’द मेरा दिल ख़ाली हो गया।”
वो ख़ाली नज़रों से दूर कहीं अनदेखे मंज़रों में खोई कह रही थी। मैंने कुछ हैरानी और क़द्रे दिलचस्पी से उसे देखा और बिना टोके उसे कहने दिया जो न जाने कब से वो कहना चाह रही थी।
“दिल की ज़मीन बिना किसी कशिश-ए-सक़ल के ख़ला बन गई जिसमें ये कम-‘उम्र मुहब्बत मु’अल्लक़ हो गई। उसका ज़र्रा-ज़र्रा दल के ख़ला में तैरने लगा।
पौ फटने से ज़रा पहले की सेहर-अंगेज़ रोशनी जैसी। तारीकी की चादर उतारकर रोशनी ओढ़ने तक का दौरानिया या फिर सूरज की मा’दूम होती बनफ़्शी शु’आ’ओं को निगलती शाम की सियाही जितना वक़्त...
मुख़्तसर मगर मुकम्मल और भरपूर।
ऐसी सरशारी कि जैसे जिस्म-ओ-जाँ हल्के-फुल्के हो कर आसमानों को चीरते ऊपर... और ऊपर उड़ते जा रहे हों। वो कैफ़ियत दसवें से ग्यारहवें घंटे में ख़त्म हो चुकी थी। और फिर कभी महसूस न हो सकी... उससे भी नहीं जिससे मुहब्बत हुई थी।
अब तो मैं सोचती हूँ कि अगर वो दस घंटे भी मेरी ज़िंदगी में न आए होते तो मैं क्या कर लेती।”, उसने मुस्कुराते हुए मगर उदास लहजे में मुझसे ताईद चाही। मैं महज़ उसकी सूरत देखकर रह गई।
“कभी-कभी तो मुझे लगता है उसका भी क़ुसूर नहीं था। वो तो जानता ही न था उन दस घंटों की मुहब्बत की बाबत...
और फिर मैं ख़ुद ही उस मुहब्बत के होने की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपने ही दिल के सामने खड़ी हो गई। और उसे ख़ाली कर दिया।
बल्कि दिल ने ख़ुद ही कह दिया... ख़ाली ही छोड़ दो।
और मैंने ऐसा ही किया। जैसे क़त्ल के बा’द पानी से सारे निशान धो दिए जाएँ।
मेरा दिल तो कोई क़दीम पत्थर था जिसे कुदाल से तोड़ा गया।
मा’बद-ख़ाने की घंटियों जैसी आवाज़ आती थी जब उस पर कुदाल की ज़र्ब पड़ती थी।”
उसका चेहरा पिछले कुछ मिनट्स से अब तक कई हज़ार कैफ़ियतों की ‘अक्कासी कर चुका था।
“मैं अपने शहर में आने वाले अंदोह-नाक ज़लज़ले से बच निकलने वाली उन इंसानों की बाक़ियात में से थी जिनका घर बचा था न घर वाले।”
वो सामान से भरा ट्रक लेकर वहाँ आया था और वापसी पर मुझे भर ले गया। उसके लिए ये सौदा ख़सारे का न था। वो कहता, “मुझे तुम्हारे हुस्न ने गंग कर दिया था। ऐसा जला कर राख कर देने वाला माहताबी हुस्न... कि मुझे कुछ याद न रहा।”
मुक़ामी बाशिंदों ने निकाह करके ट्रक में सामान की जगह लाद दिया।
निकाह से लेकर छः घंटे की मसाफ़त तक वो मेरे दिल का बिला-शिरकत-ए-ग़ैरे मालिक बना रहा। ट्रक के पिछले हिस्से में वो मेरे हुस्न के लम्स में बे-ख़ुद रहा और मैं जो घर वालों के बा’द तन्हाई और ख़ौफ़ का शिकार थी। दो बोलों के बा’द चादर और चार-दीवारी के एहसास की दुनिया में पाँव धरते ही उससे मुहब्बत करने लगी।
“उसने निकाह से एक घंटा पहले मुझसे बात की। उसकी निगाहों की वारफ़्तगी ने मुझसे मेरा मज़हब भी छुड़वाया और मेरा अपना आप भी।”
पहाड़ी लोग ऐसे ही होते हैं। ए’तिबार कर लिया तो कर लिया।
उसके मद्धम और मदहोश लहजे की सरगोशियाँ और निगाहों की वारफ़्तगी ने मुझे ख़ुद-सुपुर्दगी के उस मुक़ाम तक पहुँचा दिया जहाँ मन-ओ-तू की कोई दीवार न रही। मुझे ऐसे में दीवार ही नज़र न आई। पस-ए-दीवार क्या नज़र आता। मुझे तो आसमानों की तरफ़ उड़ाने वाली सरशारी ने मस्हूर कर रखा था।
निकाह से लेकर छः घंटे की मसाफ़त तक... मैंने मुहब्बत को अपने तन-मन पर किसी वही की तरह उतरते देखा। मैं भूल गई माँ के सर तक लिपटी ज़मीन... बाप की मेहनत से बनाए दर-ओ-दीवार के नीचे फँसी लाश, भाई और बहनों के साकित वजूद... सब ही कुछ भूल गई...”
“मुहब्बत कितना ताक़तवर जज़्बा है ना... कितनी शिद्दतों में जिस्म-ओ-जाँ को घुसेड़ देता है बिल्कुल वैसे जैसे जूस निकालने वाली मशीन में फल को...”
वो ताईद चाह रही थी। मैंने सर हिलाने पर इक्तिफ़ा किया। क्योंकि मुझे तो कभी इस जज़्बे से आश्नाई न रही थी। सीधे-सीधे अंदाज़ में ज़िंदगी गुज़ारते म’आशी तौर पर अपने से बेहतर शौहर ढूँडते और जब मिल गया तो हालात को मज़ीद बेहतर बनाने की सई’ में नौ से पाँच की मुलाज़िमत से थकन भरे वजूद पर मुहब्बत कहाँ से नाज़िल होती...
मैंने तअस्सुफ़ से सोचा।
“और कुछ के नसीब में तो दस घंटे की मुहब्बत भी नहीं होती...”, मैं उसे कहना चाहती थी मगर कह न पाई।
शाम के सात बजने वाले थे। ऑफ़िस ड्राईवर का फ़ोन आ रहा था। दूसरे दिन आने का वा’दा कर के मैंने जल्दी से रिकार्डर सँभाला और फ़ाइल और पर्स सँभालती, तंग-गलियों से तेज़-तेज़ गुज़रती बाहर क़द्रे चौड़ी सड़क पर खड़ी ऑफ़िस की गाड़ी में जा बैठी।
“मुहब्बत... दस दिन की मुहब्बत... काफ़ी है अगर हो जाए तो...”, मैंने ला-शु’ऊरी तौर पर अपना और उसका मुवाज़ना करते हुए तंज़ से सोचा।
बाहर निकलते ही तेज़ गाड़ियों का शोर, भागम-दौड़ , नफ़्सा-नफ़सी का ‘आलम... नए घर की ता’मीर के लिए उठाया क़र्ज़, पहली क़िस्त की अदायगी सर पर आन पहुँची थी। अभी घर की तज़ईन-ओ-आराइश का मसअला अलग था।
शादी को साल भर होने को था। हम दोनों मियाँ बीवी ने बाहमी रज़ा-मंदी से बा-क़ाएदा मंसूबा-बंदी करते हुए पहले घर और फिर बच्चों का सोच रखा था।
ज़मीन का क़र्ज़ उतारना मियाँ साहिब के ज़िम्मे था जबकि घर की ता’मीर के लिए बैंक का क़र्ज़ मुझे चुकाना था।
उफ़। किस क़दर थका देने वाले शब-ओ-रोज़ हैं।
मैंने सर सीट की पुश्त पर रखा और आँखें मूँद लीं।
दूसरे रोज़ मैं वहाँ पहुँची तो वो अभी सो कर उठी ही थी। नीम-ख़्वाबीदा आँखें और भी ख़ूबसूरत लग रही थीं।
“वो दस घंटे की मुहब्बत...”, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हज़ार बार की सुनी हुई कहानियों पर कोई सवाल क्या करूँ...
उसके सुनाने का अंदाज़ दिलचस्प था वर्ना कल ही ये इंटरव्यू ख़त्म हो चुका होता।
“फिर क्या होना था...?
वो कहता था मैंने आज तक इतनी हसीन लड़की को छुआ तक नहीं था। सिर्फ़ तुम्हें छूने की ख़्वाहिश इस क़दर ज़ोर-आवर थी कि मैं भूल गया... अपने बीवी बच्चे और मुश्किल से होती गुज़र-बसर...
और फिर उसने मुझे ट्रक से उतार कर इस छोटे से कमरे में मुंतक़िल किया जो उसके किसी यार-दोस्त का था।
उसके पास दोस्त को इस कमरे के लिए देने को कुछ न था सो उसने मुझे पेश कर दिया।
उसके दोस्त के हाथ लगाने से पहले मैंने आख़िरी बार उसकी तरफ़ मुहब्बत से देखना चाहा मगर मुहब्बत अपना वक़्त पूरा कर चुकी थी...
मुहब्बत... कई क़दम दूर जा खड़ी हुई और मेरा जिस्म निकाह वाला और बिना निकाह वाला झिंझोड़ते रहे।
ख़ाली दिल वाले को कोई कहीं भी फेंक दे... वो अपने अंदर लड़ने की ताक़त ही नहीं पाता।
मेरा हाल भी ऐसा ही था।
जब उसकी जिन्सी कशिश कम हुई तो वो मुझे यहाँ फेंक गया।
उसने क्या फेंकना था... मैंने भी ख़ुद को फेंक डाला। एक गिध नोचे या हज़ार... क्या फ़र्क़ पड़ता है।”, उसका लहजा बे-हिसी की आख़िरी हुदूद को छू रहा था।
“उधर तलाक़ का काग़ज़ मेरी हथेली पर रखा इधर चंद नोट दूसरे हाथ में भींचे वो यूँ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। हुस्न वाले का रस्ता बाज़ार-ए-हुस्न पर ख़त्म हो गया और मुहब्बत का रस्ता ना-रसाई के कर्ब पर।”
मैंने दुख से उसे देखा। वो आँसू पीने की नाकाम कोशिश करते हुए मुस्कुरा रही थी।
वो हीरा मंडी में नई-नई आई थी मगर उसकी आँखों की पुर-असरार ख़ामोश उदासी बताती थी कि वो लाई गई है। ख़ुद तो वो कहीं और रहती है। किसी ना मा’लूम जज़ीरे पर।
उस रोज़ अपने सुर्ख़ मेहंदी से सजी पोरों वाले नाज़ुक पाँव में झनझनाती पाज़ेब पहनते हुए मुझसे बोली, “तुमने कभी अपने पाँव देखे हैं मुक़द्दस पानियों में तैरते गुलाबियों में घुली शफ़्फ़ाफ़ पत्तियों जैसे।
मूसीक़ियत थिरकती है जब ये उठते और थमते हैं, अनछुए से, जिनके लम्स से चाँद खिल उठे।”
बनावट और ख़ूबसूरती में बिल्कुल मेरे पाँव जैसे। मगर बस एक ही फ़र्क़ है कि मेरे पाँव एक रक़्क़ासा के पाँव हैं। इनको देखकर एहसासात में वो पाकीज़गी नहीं आती, वो नर्मियाँ वो मुक़द्दस शफ़्फ़ाफ़ रोशनी नहीं आती बल्कि एक चीख़ता-चिंघाड़ता, नफ़स के तारों को छेड़ता, रंग-ओ-बू का भारीपन हवास पर तारी हो जाता है...
कैसा वजूद...? कैसी ज़ात...
ये सब आँख की पुतली से नहीं देखा जाता। नज़र सिर्फ़ वही आता है जो आँख की पुतली के पोशीदा पर्दे में छिपा होता है। जो तुम्हारे पाँव को मुक़द्दस ख़याल से छूने की जसारत करता है और मेरे पाँव पर कीचड़ डाल देता है...
वर्ना देखो न कोई फ़र्क़ है दोनों में...?”
मैंने ला-शु’ऊरी तौर पर पाँव को समेटा। ‘अजीब लड़की थी वो और उससे भी ‘अजीब उसकी बातें।
उसकी आख़िरी बात ने मुझे झिंझोड़ कर रख दिया था...
फ़र्क़...
मैं तो दस घंटे की मुहब्बत की सरशारी से भी महरूम थी।
हाँ वो रक़्क़ासा थी और सेक्स-वर्कर भी थी... वो जानती थी अपना काम भी और मुक़ाम भी...
मगर मैं...
मुझमें और उसमें कोई ख़ास फ़र्क़ था क्या...? मैंने दियानत-दारी से सोचा।
“कुछ ख़ास फ़र्क़ नहीं... मेरा भी निकाह वाला हर रात मेरा जिस्म किसी गिध के जैसा नोचता है... और... और... मेरी हर हफ़्ते की रात भी किसी ग़ैर-मर्द के साथ...”
मैंने ख़ुद से भी छुपाना चाहा।
और उसे अपने ख़सारे का भी दुख था... मगर मुझे...
सेल की मैसेज बीप ने मुझे चौंकाया...
और जिस ख़सारे का एहसास होने चला था उससे खींच बाहर किया।
“जल्दी चलो ड्राईवर... मुझे शाम में एक मीटिंग में जाना है। घर ड्राप करो मुझे...!”
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.