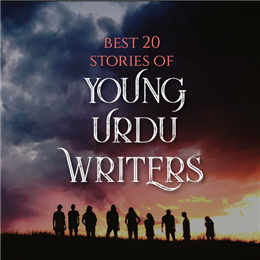कबाला
तो यूँ है कि वो एक फ़नकार की बाँहों में मर गई।
ये उन दिनों की बात है जब उसने एक नया हुक्म-नामा हासिल करने के लिए ‘अदालत से रुजू’ किया था। मैं ‘अदालत की बजाए ‘अदालत-ए-’आलिया का लफ़्ज़ इस्ति’माल करूँ तो ज़ियादा बेहतर होगा। उसे ‘अदालत-ए-’आलिया से बड़ी उम्मीदें थीं कि वो उसकी बात ज़रूर सुनेंगे और ऐसा क़ानून ज़रूर जारी करेंगे जिसके नफ़ाज़ की वो ख़्वाहाँ थी। ये जाने बग़ैर कि क्या आज़ाद और मुहज़्ज़ब मु’आशरों में इस तरह के किसी क़ानून की जगह भी है या नहीं। मुझे हैरत होती थी कि आख़िर वो अपने रूमानियत-ज़दा ख़्वाबों की तकमील के लिए क़ानून की राह क्यों अपनाना चाहती है। क्या समाज की नज़र में मु’अज़्ज़िज़ कहलाना इतना ही ज़रूरी है। अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर वो अपनी ख़्वाहिशात की तकमील चोर-रास्तों से भी तो कर सकती है, जैसे अज़ल से आदम-ओ-हव्वा की औलाद करती आई है और मु’अज़्ज़िज़ भी कहलाती रही है। मगर उसे वो तमाम आरज़ूएँ क़ानूनन जायज़ और मबनी-बर-हक़ हो कर पूरी करना थीं ताकि वो क़ाबिल-ए-तक़लीद बन सके और उसके बा’द आने वालियों को कोई मसअला न रहे। उसकी ये ख़्वाहिशात क्या थीं? आपको ज़रूर तजस्सुस ने घेर रखा होगा। ये ख़्वाहिशात थीं या महज़ कुछ सवाल थे। कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब हासिल करने के लिए तजरबा लाज़िम ठहरता है। मैं इन सबसे वाक़िफ़ हूँ।
मैं उसकी मुख़्तसर ज़िंदगी की तमाम जुज़इयात से वाक़िफ़ हूँ।
उस वक़्त से लेकर जब वो एक यहूदी रब्बी की कुश्ता-ए-तीर-ए-नज़र बनी... उस वक़्त तक जब उसने एक फ़नकार की बाँहों में आख़िरी हिचकी ली।
ताले कम रखो, चाबियाँ थोड़ी लगानी पड़ेंगी।
अगर तुम्हारे पास दो ताले हैं तो चाबियाँ भी दो ही होंगी। अगर पहली बार चाबी ग़लत लगी है तो अगली बार लाज़िमन दुरुस्त ही लगेगी। क्या इस में कोई शक है?
वो एक यहूदी ‘आलिम था जो बर्लिन के एक कम्यून के अंदर तालमूद की तशरीहात कर रहा था। कबाला की रौशन या फिर तारीक ज़िंदगी का आग़ाज़ (और यहाँ रौशन और तारीक का फ़ैसला क़ारी पर है कि वो क्या तय करता है) उस यहूदी ‘आलिम के ऊंचे क़द और दिलकश आवाज़ से हुआ। अपने सुनहरी बालों पे धुंदले नीले रंग का स्कार्फ़ जमाए वो वहीं बैठी-बैठी तहलील हो गई। उसका हाथ मेरे हाथ के ऊपर था। मैंने उसकी हथेली को गीली हो कर ठंडी पड़ते महसूस किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि तीर-ए-नज़र चल चुका है और फिर इसके बा’द कबाला की आरज़ूएँ, ख़्वाब या फिर वो सवाल शुरू’ हो गए जो आगे चल कर इस सारे अलमिए की बुनियाद बने।
वो सवाल उसने ‘अदालत में उठाने से क़ब्ल मुझसे ही किए थे।
इस सानिहे में हुक्म या’सूफ़ के साथ में भी घुन की तरह पिस गई थी। हुक्म या’सूफ़ पे मर मिटने का यारा मुझमें न था। क्योंकि मैं ज़रूरत से ज़ियादा ख़ूबसूरत और बा-इख़्तियार लोगों से ख़ौफ़ खाती हूँ। ये मेरा नफ़्सियाती मसअला है। ओ’ह्दा, ताक़त और हुस्न ख़ौफ़ में मुब्तिला करते हैं और जहाँ ख़ौफ़ हो वहाँ मुहब्बत नहीं होती। मैंने हुक्म या’सूफ़ की शानदार और वसी’ मर्दाना वजाहत के सामने ख़ुद को निहायत कम-तरीन महसूस किया और घुटने टेक दिए और वैसे भी अगर ये काम मैं करती तो फिर ये कहानी कौन लिखता? वक़्त... तारीख़ लिखने वालों को अंधे ‘इश्क़ से महरूम रखता है और ये महरूमी ही तो तारीख़ लिखवाती है। उसकी मर्दाना लोचदार आवाज़, उसकी गहरा तअस्सुर देती लबरेज़ आँखें और चौड़े कंधे किसी भी ‘औरत के पाताल में तस्मा डाल के बाहर खींच लेते थे।
जब मैं और कबाला कम्यून से बाहर निकलीं तो वो लड़खड़ा रही थी। उसका बदन बुख़ार में तप रहा था और उस पर कुछ ऐसी ख़ुमारी छा गई थी जैसे बहुत कुछ पी के आई हो। मैंने उसे सहारा दिया हुआ था। ख़यालात मेरे दिमाग़ में कीड़ों की तरह कुलबुला रहे थे। इससे क़ब्ल कि कोई सवाल मेरी नोक-ए-ज़बाँ पर आता दफ़’अतन उसने सवाल कर दिया। ये उसके सवाल-याफ़्ता दौर का पहला सवाल था।
क्या ये मुहब्बत है जो मैं महसूस कर रही हूँ?
हम बर्लिन के एक मुज़ाफ़ाती गाँव की एक सर-सब्ज़ शादाब सड़क के किनारे एक हरे-भरे दरख़्त के नीचे बैठ गईं। हम दोनों में से किसी में भी आगे चलने की सकत न थी। मैंने उसकी तरफ़ देखा। थकावट या फिर शिद्दत-ए-जज़्बात से उसकी नन्ही सी नाक सुर्ख़ पड़ गई थी और आँखें पानियों से लबरेज़ थीं।
“तुम क्या महसूस कर रही हो?”, मैंने पूछा।
“उसकी आँखें, उसकी भारी आवाज़, उसका ठहरा हुआ जानदार लहजा, मेरा जी चाहा कि मैं पूरी की पूरी उसके साथ लिपट जाऊँ। इसके अंदर समा जाऊँ। उसकी आवाज़ मेरी समा’अत को मतलूब है। मेरा जी चाहा कि उसके हुल्क़ूम के अंदर दाँत गाड़ के उसकी भारी मर्दाना आवाज़ का सारा रस पी जाऊँ...”
कबाला की आवाज़ लरज़ गई।
मेरा ज़हन इस वहशत-अंगेज़ ख़याल के साथ इत्तिफ़ाक़ न कर सका। हुल्क़ूम में दाँत गाड़ कर आवाज़ का रस पीने से उसकी क्या मुराद थी। क्या ये शिद्दत की इंतिहा नहीं। मेरा हक़ीक़त-पसंद दिमाग़ इस ख़याल की तौजीह तलाश करने से क़ासिर था। हो सकता है रूमानियत-ज़दा लोगों के पास इस ख़याल को सराहने की कोई वज्ह हो मगर मेरे पास नहीं थी। मैंने उसकी ज़ाहिरी हालत और लरज़ती आवाज़ को उसकी सेहत की ख़राबी पर महमूल किया। वो उस वक़्त बुख़ार-ज़दा थी और उस पर हैजानी कैफ़ियत तारी थी। मैंने एक घोड़ा-गाड़ी को रोका। कबाला को उस पर सवार किराया। ख़ुद भी साथ बैठी और टाउन वापिस चली गईं।
कुछ दिन के वक़्फ़े से हम दोनों ने फिर कम्यून का दौरा किया। इस उम्मीद के साथ कि अब वहाँ हुक्म या’सूफ़ के ‘इलावा किसी दूसरे रब्बी का लैक्चर होगा। मगर इसे ख़ुश-क़िस्मती कहिए या बद-बख़्ती कि सामने स्टेज पर वो अपनी वसी’ शख़्सियत के साथ बिराजमान था। इस दफ़ा’ भी वो उसी महवियत और पागलपन के साथ या’सूफ़ को घूरती रही। वापसी पर जब हम मुज़ाफ़ात की ख़ूबसूरत पथरीली सड़क पर चल रही थीं। उसने एक नया सवाल तराश लिया।
क्या मैं उस ख़ूबसूरत इंसान के बच्चे को जनम दे सकती हूँ?
उस लम्हे उसका हाथ मेरे हाथ में था। मैंने उसके बदन को बे-जान हो कर डूबते महसूस किया। इस जज़्बे का इज़हार शायद उसके लिए बेहद भारी था। मेरा बदन भी पसीने में भीग गया। हम दोनों वहीं बैठ गईं। वो एक मज़हबी ‘आलिम है। उसके बारे में ऐसा सोचा भी कैसे जा सकता है।
“बुरीदा! सोचो। अगर उस शख़्स का ख़लिय्या मेरे लहू से आमेज़ हो कर एक इंसान की तश्कील करे तो कैसा होगा...”
उसकी आवाज़ मद्धम सरगोशी जैसी थी।
सोचो वो भी इतनी शिद्दत और तलब में टूट कर बच्चा मेरे बदन के हवाले करे। जितनी शिद्दत और तलब मैं इस वक़्त महसूस कर रही हूँ तो उस बच्चे की नफ़्सियात कैसी होगी? वो बच्चा सीरत-ओ-किरदार के किस मे’राज पर होगा? मैं ये तजरबा करना चाहती हूँ बुरीदा!”
मेरे होंट ख़ुश्क थे और हल्क़ में कांटे उग आए थे। दिन ठहरा हुआ था। माहौल में उमस थी। वजूद के अंदर भी ऐसी ही गर्मी हो और बाहर भी वैसा ही मौसम हो तो अंदर बाहर के दोनों मौसम आमेज़ हो कर अजीब सी हैजानी कैफ़ियत पैदा करते हैं। मुझे लगा कि मेरे नथुने फड़क रहे हैं और मैं सिसकारी लेने लगी हूँ। तब मुझे महसूस हुआ कि कबाला जो कुछ भी महसूस कर रही है वो उसके बुतून की किन्हीं गहराइयों से निकल रहा है। वो इस मुआ’मले में बेबस और लाचार हो चुकी है। अगर वो ये तजरबा करना चाहती है तो इसमें क्या हर्ज है? मगर ये फ़ैसला मैं नहीं कर सकती थी। ये समाज का फ़ैसला था और समाज ऐसे तजरबों के दरमियान हाइल था।
मैं कुछ दिनों से बे-सम्ती और उलझाव की शिकार हूँ। मेरे अंदर भी कुछ सवाल हैं और ये सवाल मेरी शनाख़्त और शख़्सी आज़ादी के हैं। बर्लिन यूनीवर्सिटी में मेरे ख़लाई प्राजैक्ट का आख़िरी दौर चल रहा है। शो’बा कुछ लोगों को आस्ट्रेलिया भेज रहा है। उन मुम्किना लोगों में मैं भी शामिल हूँ। मुझे वहाँ सैटेलाइट से मिलने वाली तस्वीरों के ख़ुसूसी तज्ज़िये की क्लासेज़ लेनी हैं और ये कोर्स तीन हफ़्तों का है। हमने तन्हाई के ‘इवज़ आज़ादी का सौदा किया है और ये सौदा कुछ महंगा भी नहीं है। मैं शनाख़्त का सवाल उठाती हूँ। मैं जर्मन हूँ। ये मेरी शनाख़्त है और ये शनाख़्त मुझे इस पूरे ‘आलमी गाँव के अंदर मो’तबर बनाती है मगर सवाल तो वसाइल की फ़राहमी का है। मैं ये सोचे बग़ैर नहीं रह सकती कि क्या कबाला सीरत-ओ-किरदार की इंतिहा पर पनपने वाले एक ग़ैर-मा’मूली बच्चे को इस समाज के लिए जनम देना चाहती है जो एक दूसरे से वसाइल छीन लेने की तग-ओ-दव में बर-सर-ए-पैकार है?
दुनिया में कौन सा ऐसा मुआ’शरा है जो अख़्लाक़ी बरतरी की बुनियाद पर सुपर-पावर कहलाता हो? कोई भी नहीं। बल्कि मोहलिक असलहे की इफ़रात ही वो बुनियादी शर्त है जिसकी बिना पर सुपर-पावर का ख़िताब मिलता है। बरतरी और कमतरी, बुलंदी और पस्ती के ये मे’यारात सरमाये और मौत के साथ जुड़े हैं। एक तरफ़ सरमाया बढ़ता है दूसरी तरफ़ हयात घटती है। जो जिस्म-ओ-जाँ की तग-ओ-दव करता है उसे उतना ही मिलता है जिससे उसकी रूह उसके बदन के साथ बनी रहे। मैं कबाला को भी इसी तनाज़ुर में देखने लगी थी।
वो इस शख़्स के क़ुर्ब के लिए चौबीस घंटे अपने आसाब के साथ जंग लड़ती थी। उसका लहू उसके लम्स के लिए उबलता और फिर ठंडा पड़ता और इस जाँ-तोड़ आसाबी जंग के दौरान वो बदहाल हो जाती। उसकी रूह और उसके आसाब उस रिज़्क़ के लिए जाँ-तोड़ कोशिश कर रहे थे जो कभी उसका नसीब न बना और दूसरी तरफ़ वही शख़्स अपनी बीवी को बहुत आसानी और बग़ैर किसी मेहनत के मयस्सर था महज़ इसलिए कि वो उसकी मालिक थी। वो ‘औरत जो उसके हुसूल के लिए कोई रुहानी या जज़्बाती तग-ओ-दव भी नहीं करती उसे वो हासिल है। वो उसे अपने बोसे की हलावत और बदन की हरारत से फ़ैज़-याब करता है। इसके साथ पूरे का पूरा मुलव्वस है। ये इंसाफ़ नहीं था। क्या कबाला की तलब की शिद्दत और आसाब की शिकस्त-ओ-रेख़्त कोई मा’नी नहीं रखते थे। महज़ इसलिए कि वो मालिक नहीं थी बल्कि अपनी रूह की मज़दूर थी। क्या मिल्कियत के आगे मेहनत की कोई औक़ात नहीं?
मुझे अपने उलझन भरे इन सवालों के दरमियान ही आस्ट्रेलिया जाना पड़ा। मैं नहीं जानती थी कि मेरे बा’द कबाला ऐसी हिमाक़त करेगी कि तारीख़ भी जिसको कभी मिटा न पाएगी।
उन्हीं दिनों कबाला ने ‘अदालत-ए-’आलिया से रुजू’ किया। मुद्दआ’ ये था कि रब्बी या’सूफ़ को उसके साथ मिलाप की क़ानूनी इजाज़त दी जाए ताकि वो उसकी ऐ’लानिया वल्दियत के साथ उसका बच्चा पैदा कर सके। ‘अदालत ने उसकी इस दरख़्वास्त को मबनी-बर-हिमाक़त क़रार दिया और उसे सरज़निश की कि आइंदा वो हुक्म या’सूफ़ जैसे किसी मु’अज़्ज़िज़ रब्बी को बदनाम करने की साज़िश न करे और बेहतर है कि किसी नौजवान के साथ शादी कर के ख़ुश-बाश आ’इली ज़िंदगी गुज़ारे। एक बा-किरदार मज़हबी ‘आलिम के मुत’अल्लिक़ ऐसे परागंदा ख़याल रखना ही अव्वल तो जुर्म है और अगर उसने ये जुर्म कर ही लिया था तो यूँ ‘अदालत में आ के उसे एक मु’अज़्ज़िज़ ‘आलिम को बदनाम नहीं करना चाहिए था। मैं जब अपना प्राजैक्ट मुकम्मल कर के वापिस आई तो कबाला की ये हिमाक़त शहर का तब्सिरा बन चुकी थी। मैं अगर वहाँ होती तो उसे ऐसा कोई क़दम न उठाने देती। मगर अब तीर चल चुका था और अब हमें मुक़द्दर का खेल देखना था। ये दिन घुटन और बेचैनी के थे। कबाला को समझ नहीं आ रही थी कि उसके मुक़द्दमे में आख़िर ख़राबी क्या है? जिस तरह लोग अपने बाक़ी हुक़ूक़ के लिए अ’दालती जंग लड़ते हैं उसी तरह उसने भी महज़ अपने हुक़ूक़ के लिए एक फ़रियाद की है। इस में ग़लती क्या है और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं कबाला के दिमाग़ के इस ढीले पुर्ज़े तक कैसे पहुँचूँ जिसे कसने के बा’द उसका दिमाग़ ठीक हो सके। इन्ही हब्स-ज़दा दिनों के दौरान कबाला को एक चिट्ठी मौसूल हुई। ये चिट्ठी हुक्म या’सूफ़ की तरफ़ से थी। मत्न यहाँ दर्ज कर रही हूँ :
ख़ुदावंद लम-यज़ल के बर-गुज़ीदा बंदे मूसा पर सलामती हो
मैं तुमसे ‘उम्र में दोगुना बड़ा हूँ। तुम मा’सूम और पाकीज़ा हो। ख़ुदा तुम्हारी पाकीज़गी को सलामत रखे। मुझे मा’तूब मत करो। एक मज़हबी इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान जिन्स और ‘औरत है। तुमने या मेरे रब ने मुझे इस इम्तिहान में डाला है। तो निकालेगा भी वही। वो मुझे इस्तिक़ामत बख़्शे। मैं तुम्हें हम-कनार करूँ। तुम्हारे उबलते लहू की हिद्दत को अपने बदन की हरारत से ठंडा करूँ। मैं ऐसा सोच तो सकता हूँ मगर कर नहीं सकता। हम में से हर शख़्स समाज के क़ाइ’दे-क़वानीन और अपने ख़ुद-साख़्ता उसूलों का क़ैदी है। महरूमी सिर्फ़ तुम्हें ही नहीं मुझे भी है। इंसान अशरफ़-उल-मख़्लूक़ात है। मगर इस शरफ़ की सबसे भारी क़ीमत वो इस जिन्स के ज़िम्न में चुकाता है और कोई क़ुर्बानी इंसान और उसकी रूह पर इस क़दर भारी नहीं जितनी शहवत की क़ुर्बानी भारी है। और ये क़ुर्बानी देने वालों का दर्जा भी सबसे बुलंद है। तुम बादशाह सुलैमान के वालिद दाऊद नबी के हालात-ए-ज़िंदगी ज़रूर पढ़ो। ख़ुदा तुम पर अपना करम रखे।
अहक़र-उल-‘इबाद
या’सूफ़
कबाला ने इस रुक़ए को कई बार पढ़ा। कभी तैश और कभी मलामत के साथ। यही हाल मेरा था। चंद लाईनों में सिमटी इस तहरीर के अंदर जहाँ कबाला के लिए सरज़निश थी वहाँ उसके लिए एक उम्मीद का पैग़ाम भी था कि हुक्म या’सूफ़ और कुछ नहीं तो कम-अज़-कम कबाला के लिए हम-दर्दाना ख़यालात ज़रूर रखते हैं और उसके लिए कुछ सोचते भी हैं और कबाला की वज्ह से उनकी जो सुबकी हुई है उसकी तरफ़ भी उन्होंने कोई इशारा नहीं किया था। मेरे दिल में उनकी अ’ज़्मत कुछ और भी पुख़्ता हो गई थी।
मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि कबाला को साथ लेकर उनसे मिलने ज़रूर जाऊँगी कि उऩ्ही दिनों हुक्म या’सूफ़ का सानिहा-ए-इर्तिहाल हो गया। आह। वो कितना शदीद हादिसा था कि शिद्दत-ए-ग़म से पसलियाँ टूटने को आईं। छियालीस साल की ‘उम्र कोई मरने की ‘उम्र नहीं होती। सारे शहर की तोपों का रुख़ कबाला की तरफ़ हो गया था। हर शख़्स का यही ख़याल था कि एक नौ-‘उम्र जज़्बाती लड़की की अहमक़ाना मुहब्बत ने एक ‘आलिम की जान ले ली। हुक्म या’सूफ़ को दिल का दौरा पड़ा था। ये सच था या नहीं मगर अब सच बन गया था। या’सूफ़ का मरना उसी दिन लिखा था जिस दिन उन्हें मरना था मगर मौत का इल्ज़ाम कबाला पर आना भी मुम्किन है तक़दीर का ही कोई हिस्सा हो। अब तक तो मैं इन बातों को नहीं मानती थी मगर अब मुझे भी लगने लगा था कि कुछ वाक़ि’आत की तशकील में इंसानों का कोई अ’मल-दख़्ल या इरादा नहीं होता। वो महज़ तय हो चुके कुछ वाक़ि’आत का हिस्सा बना दिए जाते हैं। जैसे कबाला बन गई थी, जैसे हुक्म या’सूफ़ बन गए थे, या फिर जैसे कोई और भी बनने वाला था।
हुक्म या’सूफ़ ने मरने से कुछ अ’र्सा क़ब्ल कबाला को जो ख़त लिखा था उस में एक पैग़ाम या हुक्म भी था कि दाउद नबी के हालात-ए-ज़िंदगी को ज़रूर पढ़ो और यही हुक्म कबाला की ज़िंदगी में एक नया मोड़ ले आया। मैं भी अपने ख़लाई महारत के तवील और महंगे कोर्स को यकसर भुला कर उसके साथ लग गई थी। हमने मुक़ामी लाइब्रेरी से अंबिया के हालात-ए-ज़िंदगी के हवाले से कुछ किताबें ढूँढ निकालीं और उन्हें अपने नाम से जारी करा के साथ ले आईं। दाऊद नबी के हालात-ए-ज़िंदगी में ऐसा क्या था कि जिसकी तरफ़ हुक्म या’सूफ़ ने इशारा किया था। रातें ख़ुनक थीं मगर एक शानदार आदमी की याद में ग़मनाक भी थीं। वो आदमी जिसका मज़ार सिर्फ़ कबाला ही नहीं बल्कि मेरे दिल में भी बन गया था। इन तारीक ख़ुनक रातों में हमने अंबिया के हालात-ए-ज़िंदगी का मुताला’ जारी रखा कबाला की आँखें पहले से भी बड़ी और रौशन हो गई थीं जैसे उसके अंदर कोई लाईट हाऊस उग आया हो और फिर एक रात मुताले’ के दौरान हज़रत दाऊद के हालात-ए-ज़िंदगी पढ़ते हुए एक पैराग्राफ़ हमारे सामने आ गया और यूँ उभरा गोया हाई-लाइटर से उजाला गया हो। मत्न यहाँ दर्ज कर रही हूँ :
“और फिर एक शब दाऊद नबी बहुत बे-क़रार थे। मुशीर-ए-ख़ास ने बेचैनी को भाँप लिया और दस्त-बस्ता ‘अर्ज़ की कि क्या हुज़ूर को किसी बीवी या किसी ख़ास हरम की ज़रूरत है? मगर पैग़ंबर ने कोई जवाब न दिया। मुशीर-ए-ख़ास ने दुबारा ‘अर्ज़ गुज़ारी कि हुज़ूर सभी बीवियाँ नहा धो कर तैयार हैं। मगर पैग़ंबर ने मुशीर-ए-ख़ास को जाने का इशारा कर दिया। रात ढल रही थी और दाऊद नबी दरीचे में खड़े सामने शहर को देख रहे थे जब उनके मुशीर-ए-ख़ास अक्तीफ़ुल की पोती बिंत-ए-सबा ग़ुस्ल-ए-ज़रूरी करने कनीज़ के हमराह छत पर आई और उसने लिबास अलग किया और ग़ुस्ल शुरू’ किया। दाऊद ने बिंत-ए-सबा का नौ-ख़ेज़ हुस्न मुलाहिज़ा किया और फिर उसे अपने महल में बुलवा कर अपने वस्ल से शाद-काम किया। उस पर ख़ुदा नाराज़ हुआ और जिस हैकल का ख़्वाब दाऊद नबी ने देखा था उसको उनके बेटे शाह सुलैमान ने मुकम्मल किया।”
वहाँ ख़्वाब टूटने की बात थी मगर यहाँ तो ज़िंदगी ही टूट गई थी और ख़्वाब भी कहाँ बचे थे। दुख की बात तो ये थी कि कोई वस्ल भी नहीं हुआ, कुछ भी न हुआ और सब कुछ हो गया। उसने सारी ख़ल्क़ के ताने सुने और मलामत उठाई और तिश्ना-काम भी रही। क्या ही अच्छा होता वो भी आदम की दूसरी बेटियों की तरह चोर रास्ता अपनाती, ये ज़िल्लत तो न सहनी पड़ती, ये महरूमी का दुख तो न होता। आह कितनी ‘अज़ीम, कितनी अर्फ़ा’, कितनी शानदार थी वो और कितनी मा’तूब हो गई। उसकी ला-हासिल मुहब्बत, उसका ज़ब्त, उसकी तिश्ना-कामी और फिर उस पर होने वाली मलामत की मैं गवाह हूँ। क्या इतने बड़े इम्तिहान से गुज़रने वाले आदमी की अस्ल शनाख़्त के लिए एक गवाह का होना काफ़ी है? वो सारी रात रोया करती। कभी-कभी मुझे यूँ लगता कि उसकी रूह बड़े समंदर में ढल गई है जो हर वक़्त बहता रहता है। वो क़तार-अंदर-क़तार आँसू बहाती। इस आँसू बहाने में भी एक लज़्ज़त है। मुझे इस लज़्ज़त का तजरबा नहीं मगर मैंने इसे कबाला के बदन से फूटते देखा था। हम साथ रहा करतीं वो रात को सोते वक़्त मेरी तरफ़ पीठ फेर लेती और फिर उसका बदन हौले-हौले लरज़ने लगता। चंद लम्हों की मुहब्बत, जिसमें लम्स को पाने की ख़्वाहिश, वसी’ सीने में समा जाने की आरज़ू और जाने क्या-क्या था।
क्या हर्ज था अगर इस लरज़ते बदन को उस ख़ाक हो चुके जिस्म से कुछ थोड़ा सा असासा मिल जाता? क्या था जो इस मुज़्तरिब रूह को उस गुमशुदा रूह की कुछ परछाईं मिल जाती? इतनी शदीद तलब इल्क़ा कर के फ़ासले इतने ज़ियादा क्यों बढ़ा दिए गए।
आख़िर इससे क्या मक़सूद था?
कबाला की बर्दाश्त का दर्जा बढ़ता जा रहा था और मेरा घटता जा रहा था। पता नहीं क्यों मुझे ये वहम लाहिक़ हो गया था कि बर्दाश्त का दर्जा बढ़ने से आज़माइश के सिलसिले दराज़ होते चले जाते हैं। वो दिन को ख़ामोश और पुर-सुकून रहती थी और रात को मुतलातिम, ये कैफ़ियत उस पर ठहर गई थी। इस जुमूद को तोड़ने के लिए मैंने उसके साथ जा कर फ़िल्म देखने का इरादा किया। मुझे क्या मा’लूम था कि तक़दीर एक-बार फिर उसकी घात में है। इत्तिफ़ाक़ से ये फ़िल्म शाह सुलैमान के हालात-ए-ज़िंदगी पर मबनी थी और इस फ़िल्म में मर्कज़ी किरदार अदा कर रहा था “मा’रिब”
मा’रिब शक्ल से यहूदी लगता था, नज़रियाती हवाले से मुल्हिद और जिन्सी लिहाज़ से अ’रब। वही लोचदार मर्दाना आवाज़, गहरा तअस्सुर देती लबरेज़ आँखें और चौड़े कंधे, उसको कोई मज़हबी ख़ुत्बा सुनने से ज़ियादा कोई भी अच्छा सा खाना पेट भर कर खाने से दिलचस्पी थी। वो बहुत सलीक़े और नज़ाकत से खाता, और ये नफ़ासत उसके क़ुदरती मिज़ाज का हिस्सा न थी बल्कि उसे उसके पेशे ने सिखाई थी। तसन्नो’ और बनावट, हर मुआ’मले में और हर शख़्स के सामने बने रहो और तहज़ीब का मुज़ाहिरा करो। कौन जाने ये लोग अपनी तन्हाइयों में क्या और कैसे होते हैं। क्योंकि हम जैसे आ’म लोग तो उन्हें सिर्फ़ पर्दा स्क्रीन पर ही देखते हैं।
वही ऊंचा क़द, गहरा तअस्सुर देती लबरेज़ आँखें और चौड़े कंधे, ये ग़लती थी या तक़दीर का टकराव, मैं फिर कोई फ़ैसला करने से क़ासिर हूँ। हम हाल के अंदर जा कर कुर्सियों पर बैठ गईं। वो तब भी पुर-सुकून और ख़ामोश दिखाई दे रही थी। मेरा ज़हन दो तरफ़ बट गया। दिमाग़ की एक रौ मेरे अपने उस हाथ की तरफ़ थी जिसके ऊपर कबाला का हाथ रखा था और दूसरी रौ स्क्रीन पर थी। तक़दीर के इस खेल का तीसरा कोना ज़ुहूर-पज़ीर हो रहा था। अचानक कबाला का हाथ लरज़ा। शाह सुलैमान सामने खड़े थे। वजाहत, तमकनत, वक़ार और तुनतुने का पैकर-ए-आ’ज़म, हाथ में तलवार लिए जिन्नात को तह-ए-तेग़ करते सालार-ए-आ’ज़म।
‘अक़्ल-ए-ग़याब जुस्तजू, ‘इश्क़ हुज़ूर-ओ-इज़्तिराब
फ़िल्म के इख़्तिताम से पहले ही वो बेहोश हो चुकी थी।
कार्डियोलौजी केयर यूनिट में बेहोश पड़ी कबाला की ज़बान पर एक ही जुमला रवाँ था।
“मुझे शाह सुलैमान से मिलना है।”
मा’रिब के मुत’अल्लिक़ मा’लूमात लेने में मुझे काफ़ी दिक़्क़त का सामना करना पड़ा। वो तुर्की में पैदा हुआ और वहाँ के नाइट-क्लबों की एक मशहूर चेन के मालिक का इकलौता बेटा था। उसकी माँ जर्मन थी। तुर्की और जर्मनी उसके मुशतर्का ठिकाने थे। मा’रिब को ढ़ूँढने और राब्ता करने में कई महीने लग गए। इससे आगे की कहानी “मा’रिब” की ज़बानी सुनिए।
मुझे मेरे अस्सिटैंट ने बर्लिन से आने वाले एक पैग़ाम की बाबत बताया जो बार-बार आ रहा था कि वहाँ के मा’रूफ़ कार्डियोलौजी सैंटर में ज़ेर-ए-इ’लाज एक मरीज़ा मुझसे मिलना चाहती है। ये पैग़ाम हस्पताल की इंतिज़ामिया और वहाँ के एक मा’रूफ़ समाजी इदारे की तरफ़ से आ रहा था जो एस.ओ.एस. के साथ काम करता है। मैं इस तरह के पैग़ामात का आ’दी हूँ। हमारी ज़िंदगियों में इस तरह के वाक़ि’आत चलते रहते हैं। इसलिए ज़ियादा संजीदा होने की ज़रूरत नहीं होती। मगर इस पैग़ाम में कुछ अलग था और दूसरी बात ये कि इस संजीदा नौ’इय्यत के पैग़ाम को दो हस्सास इदारे नश्र कर रहे थे। लिहाज़ा मैंने अपनी मसरूफ़ियत में से इस काम के लिए एक दिन मुख़्तस किया और पैग़ाम भिजवा दिया कि मैं फ़्रैंकफ़र्ट में अपने प्राईवेट घर के अंदर एक दिन के लिए फ़ारिग़ हूँ और उस मरीज़ा से मिलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा खाना और हसीन ‘औरत मेरा शौक़ थीं मगर अब नहीं हैं। ये तब्दीली मुझमें उस मरीज़ा से मिलने के बा’द आई है।
मैं बेदिली के साथ उसका मुंतज़िर था जैसे ये भी कोई रोज़मर्रा का काम हो और उसे ख़त्म करने के बा’द ज़ाती तफ़रीह के लिए कहीं जाना हो। अभी मैं इसी कैफ़ियत में था कि अस्सिटैंट ने मुझे उसके आने की इत्तिला दी। मैं कमरा-ए-मुलाक़ात की तरफ़ बढ़ा। ये मुलाक़ात खु़फ़िया थी मगर उसके साथ कुछ और लोग भी थे। हस्पताल इंतिज़ामिया, समाजी इदारे या उसके ख़ानदान के लोग सभी के चेहरों पे संजीदगी और हैरत थी।
मैंने उसे देखा, वो दराज़-क़द, शहद रंग बालों और कुशादा रौशन आँखों वाली हसीन लड़की थी। उसके बदन पर सियाह लबादा था मगर उसके कंधे उ’र्यां थे। उसने सर को हल्के आसमानी रंग के स्कार्फ़ से ढक रखा था। मगर स्कार्फ़ के नीचे से घने लंबे बालों का आबशार बह कर दूर नीचे तक चला गया था। वो खड़ी हो गई थी और टकटकी बाँधे मुझे देख रही थी। मेरी कैफ़ियत भी कुछ मुख़्तलिफ़ नहीं थी। मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। फिर वो एक दम दीवार की तरफ़ मुड़ गई। घने लंबे शहद रंग बालों का आबशार अब मेरी नज़रों के सामने था कि वो चीख़ पड़ी।
नहीं। नहीं। ये वो नहीं हैं ये वो नहीं हैं। वो उन्हीं अल्फ़ाज़ को दोहरा रही थी। कमरे में मौजूद सब लोग हैरत-ज़दा थे कि उसे अचानक हुआ क्या था। सब हैरान थे कि दफ़’अतन उसकी दोस्त जो उसकी महरम -ए-राज़ भी थी मेरे क़रीब आई और मुझे किसी दूसरे कमरे में जाने की दरख़्वास्त की। मैं मा’ज़रत-ख़्वाह हूँ सर! क्या आप उसकी ज़िंदगी की ख़ातिर एक-बार बादशाह सुलैमान के गेट अप में उसके सामने आएँगे?
मैं हैरान रह गया। अच्छा तो ये बात थी। वो मा’रिब से नहीं शाह सुलैमान से मिलना चाहती है। कुछ सोचने के बा’द मैंने हाँ कह दी। फ़िल्म के प्रोड्यूसर से राब्ता करने कॉस्ट्यूम मंगवाने और तैयार होने में ख़ासा वक़्त लगा मगर ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अनोखा और अछूता तजरबा था। आज मैं लाखों, करोड़ों नाज़िरीन के लिए नहीं बल्कि सिर्फ़ एक, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हस्ती की ख़ातिर तैयार हो रहा था। ये चीज़ और ये एहसास मेरे अंदर ‘अजीब तलातुम पैदा कर रहे थे। मैंने अपनी रूह के अंदर ऐसी सरशारी और खलबली इससे क़ब्ल किसी भी फ़िल्म के सीन के लिए तैयार होते वक़्त कभी महसूस नहीं की थी। मगर आज कुछ ख़ास था। पैसे या शुहरत की ख़ातिर नहीं बल्कि एक ज़िंदगी की ख़ातिर, करोड़ों लोगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ़ एक लड़की की ख़ातिर। आह!
मैं कैसे बयान करूँ? जैसे में एक दूल्हा हूँ और दुल्हन ब्याहने जा रहा हूँ और फिर मैं शाह सुलैमान के गेट-अप में तैयार था।
मैंने क़दम उस कमरे की तरफ़ बढ़ाए जिसके अंदर वो थी तो मुझे लगा कि मेरा दिल उछल कर बदन से बाहर आ जाएगा। तेज़ शोर मचाती धक-धक से बचने के लिए मैंने क़दम मज़बूती से जमा लिए और फिर उसकी तरफ़ देखा। वो किसी ‘आमिल के मा’मूल की तरह उठी। बहुत आहिस्ता से चलती हुई मेरी तरफ़ बढ़ी। इस कारवाई के गाले ऐसा नर्म-ओ-नाज़ुक बदन मेरी बाँहों में था। वो अपने होंटों और साँसों से मेरी गर्दन, रुख़्सारों और सीने के बोसे ले रही थी। यकदम मैंने उसके बदन को ढीला पड़ते महसूस किया। मेरे दिल की धड़कन बेहद तेज़ हो गई थी। ताब न ला कर मैंने एक झटके से उसे बाज़ुओं से पकड़ कर ख़ुद से अलग किया। मैं उसके ईमान शिकन होंटों का बोसा लेना चाहता था।
जूँही मेरे होंट उसकी नाक के क़रीब गए मुझे लगा कि उसकी साँस रुक गई है। आह। बोसा अधूरा ही रहा। वो जा चुकी थी। वो मेरे बाज़ुओं में झूल गई थी।
अच्छा खाना और हसीन ‘औरत मेरा शौक़ थीं मगर अब नहीं हैं।
मेरे एक दोस्त का कहना है कि मुझ पर “कबाला” का असर है। (याद रहे कि यहूदी मज़हब में कबाला एक काले जादू का नाम है) मेरा ये दोस्त मेरी ज़िंदगी में दर आने वाले इस हादिसे से वाक़िफ़ नहीं। मैं उसे बताना भी नहीं चाहता कि वो एक अधूरा बोसा ही दर-अस्ल मेरी अब तक की सारी ज़िंदगी की ज़ाती शय है। वर्ना तो कितने ही बोसे हैं जिन्हें करोड़ों नाज़िरीन देख चुके हैं। वो तो सिर्फ़ अपनी कहता है और मैं उसकी बात को सच मानता हूँ कि वो भी झूट नहीं बोलता।
वो नहीं जानता कि उसका नाम भी “कबाला” था।
और मैं एक अधूरे बोसे के ला-मुख़्ततिम दायरे में ठहर गया हूँ।
“कबाला” भी तो यही है। एक ला-मुख़्ततिम दायरे का पुर-सुकून ठहराव।
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.