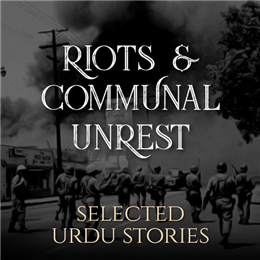रूह से लिपटी हुई आग
स्टोरीलाइन
कहानी मानवीय स्वभाव की उस सोच पर वार करती है जिसे फ़साद फैलाने और क़त्ल-ओ-ग़ारतगरी के लिए कोई बहाना चाहिए। ऐसी स्वभाव के लोगों के लिए एक छोटी सी अफ़वाह ही काफ़ी होती है। भीड़ भरे बाज़ार वीरान होने लगते हैं, लोग सड़कों से गायब हो जाते हैं और अपने घरों या किसी सुरक्षित जगह पनाह ले लेते हैं। दुकानें लूट ली जाती हैं और घरों को आग लगा दिया जाता है।
सूखी घास, नए नोटों के तरह कड़कड़ाते नारे जो सिक्का राइज-उल-वक़्त बने हुए हैं, हर चिंगारी को क़बूल करने और भड़कते हुए शोले में तबदील कर देने वाला दिमाग़... हर दूसरा शख़्स या चंद अश्ख़ास का गिरोह, जो मैं नहीं हूँ, या हम नहीं हैं, साज़िशें बनती हुई आँखें, मुस्कुराहटों को कुदूरतों, नफ़रतों और अदावतों में रंग देने वाले ज़ेहन से जुड़ी हुई दो आँखें। उनमें सचमुच आफ़त की चिंगारी अगर आज उड़ कर न आ पड़ी तो कल आ पड़ेगी, कल भी गुज़र गया तो परसों। चिंगारी के उड़कर गिरने, सुलगने, भड़क उठने और फिर राख का ढेर बन जाने के जहाँ इतने सारे सामान मौजूद हों, वहाँ कौन किसी का हाथ पकड़ेगा, कौन किसी मुस्कुराहट को क़त्ल का पैग़ाम बनने से रोक सकेगा।
रात के ग्यारह बजे तक जागने वाली सड़क सुबह छः बजे भी ऊँघ रही थी, चीनी और शीशे के बर्तनों के जले, अध जले टुकड़ों के ढेर, लुटी हुई दूकानों, राख हो जाने वाली लकड़ी की बड़ी टालों के दरमियान चाय का मग एक छनाके के साथ फ़र्श पर गिरकर चकना-चूर हो गया।
“अरे ख़ातून...” एक भारी लेकिन निस्वानी आवाज़ उभरी, “क्या ग़ज़ब करती है, रोज़ाना एक बर्तन तोड़ देती है, अभी पिछले हफ़्ते ही एक पिरिच तोड़ी थी।”
ख़ातून ने जो नीम पागल है, आएं बाएं शाएं की। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं लेकिन चेहरे पर ख़जालत की झिलमिलाती चिलमन, अलफ़ाज़ के आधे, चौथाई या उससे भी कम उगले हुए और उससे भी कम समझे हुए मअनी ने मिल-जुल कर अफ़सोस, नदामत, शर्मिंदगी का एक मजमूई तास्सुर पैदा कर दिया था। लेकिन यहाँ तो अफ़सोस का एक टूटा फूटा, लूला लंगड़ा लफ़्ज़ भी नहीं, चेहरे पर शर्मिंदगी का एक तास्सुर भी नहीं, आँखों में आँसू तो दूर की बात, नदामत की एक लकीर भी नहीं। हाँ कुछ लोग, या कुछ लोगों का गिरोह ज़रूर है जो सोचते एक तरह हैं, न हंसते एक तरह हैं, न रोते एक तरह हैं, दो हाथ हैं, दो आँखें और दो टांगें हैं। सांस लेने के दो नथुने हैं, प्यार करने के लिए दो होंट हैं, जो चलते फिरते बातें करते, चिराग़ां करते, सारे शहर को रोशनियों का शहर बना देते हैं और फिर उस रोशनी से अपने दिलों को तारीक करलेते हैं।
एक नज़र न आने वाली लकीर के दोनों तरफ़ इंसानों का ठाठें मारता हुआ समुंदर है, एक तरफ़ हंसी के फ़व्वारे छूटते हैं तो दूसरी तरफ़ आँसुओं के दरिया बह जाते हैं, एक तरफ़ कोई वाक़िआ ग़म-ओ-अंदोह की एक ठंडी लहर दौड़ा जाता है तो दूसरी तरफ़ ख़ुशी की एक लहर दिल-ओ-दिमाग़ को छू जाती है, लेकिन उस लकीर ही की तरह ये जम-ए-ग़फ़ीर, इंसानों का ये हुजूम है कहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं।
तो इससे क्या हुआ? आँखों को दिमाग़ ने झुठलाया। एक मकान छोड़कर दूसरे मकान में जो रहता है वो मैं हूँ। उससे पाँच मकान पहले और तीन मकान बाद जो रहता है वो भी मैं हूँ। वो सारा मुहल्ला मैं हूँ, वो सारी गली मैं हूँ और फ़ुलां मकान, फ़ुलां गली, फ़ुलां सड़क, फ़ुलां मुहल्ला, फ़ुलां दूकान, मैं नहीं बल्कि तुम हो। तुम भी नहीं ग़ैर हो, ग़ैर भी नहीं दुश्मन हो, मेरे दुश्मन, हम सबके दुश्मन।
टूटे बर्तनों के इस ढेर से एक टुकड़ा कुलबुलाया, उठा, दूसरे कोने से दूसरा टुकड़ा, एक तरफ़ से कंडा, एक जानिब से पेंदा और ज़रा सी देर में एक निहायत ख़ूबसूरत प्याली और तश्तरी आँखों के सामने थी।
फिर उस सड़क से आ मिलने वाली, एक पतली सड़क के छोटे लेकिन ख़ूबसूरत से मकान से जो पास के दूसरे मकानों के शोलों की ज़द में आकर ज़मीन बोस हो चुका था, जली, अध-जली स्याह ईंटों, ख़ाकिस्तर कपड़ों और दूसरे सामान के मलबे के अंदर से एक सुबुक सी मेज़ और दो कुर्सियाँ जिन पर लपकते शोलों का जैसे कोई असर ही नहीं हुआ था, उसी तबाह-ओ-बर्बाद मकान के एक ऐसे कमरे में जिस तक आग की एक भी लपट न पहुंची थी, ख़ुद बख़ुद बड़े सलीक़े से रख दी गईं। कमरे की सजाट मकीनों की ख़ुशज़ौक़ी की गवाही दे रही थी। हल्के सब्ज़-रंग के पर्दे जिन पर नाज़ुक नाज़ुक सुर्ख़ फूल छपे हुए थे, दरवाज़े पर टँगे थे। एक जदीद पेंटिंग बाएं दीवार पर टंगी थी, एक छोटी मेज़ पर रेडियो रखा हुआ था, अलमारी में कृष्ण, बेदी, मंटो के अफ़सानवी मजमुए, कुछ अदबी जरीदे, बा’ज़ रसाइल के ज़ख़ीम नंबर और अंग्रेज़ी की चंद किताबें बड़े सलीक़े से रखी हुई थीं।
यकायक दोनों दरवाज़ों के पर्दों में इर्तिआश पैदा हुआ। एक की लहरें तेज़ थीं, दूसरे की मद्धम, एक के पीछे से एक बेचैन, मुज़्तरिब, लेकिन निहायत ख़ुशसलीक़गी से बादामी रंग के सूट और धारीदार टाई में मलबूस एक नौजवान तेज़ तेज़ क़दम बढ़ाता हुआ एक कुर्सी पर जा बैठा। दूसरे दरवाज़ा के पर्दों के पीछे से साड़ी, गहरी सुर्ख़ लिपस्टिक, नाक में चमकती हुई छोटी सी कील और कान की लवों में धीरे धीरे हिलते हुए आवेज़ों की बैरूनी शनाख़्त के दरमियान जो हयूला उभरा, उसकी आँखों ने चोरी चोरी मेज़ और सामने कुर्सी पर बैठे हुए नौजवान का जाइज़ा लिया, लेकिन जैसे ही नज़रें टकराईं, उसकी आँखें गोया ज़मीन में गड़ गईं और फिर वो दूसरी तरफ़ की कुर्सी पर बैठ गई।
चार रोज़ क़ब्ल पुल पर जली बुझी लकड़ी की टाल की हरारत ने चाय बनाई, ख़ुलूस के अनदेखे हाथों ने उसे पहले केतली और फिर उन प्यालियों में उंडेला जो मुहब्बत की चाशनी से बेदाग़ जुड़ गई थी। दो आँखें मेज़ की एक जानिब से उठीं, दो दूसरी जानिब से, एक तरफ़ इश्तियाक़ की शिद्दत और उसका इज़हार था तो दूसरी तरफ़ इश्तियाक़ के बावजूद ख़ामोशी। फिर तक़रीबन एक साथ लबों को छूने के बाद जब प्यालियां तश्तरियों में वापस रखी जाने लगीं तो उनके कोने टकड़ाए और इस मामूली से टकराव से दोनों प्यालियां फिर टुकड़े टुकड़े हो गईं। तश्तरियां रखे ही रखे अपने पुराने ज़ख़्मों को याद करके चूर चूर हो गईं।
कुर्सीयों और मेज़ को नज़र न आने वाले हाथों ने फिर उसी जले हुए मकान के मलबे में ला पटका, दरवाज़ों और खिड़कियों के पर्दे भक् से जल गए, दीवार पर टंगी हुई तस्वीर का रंग-ओ-रोग़न पिघल कर टप टप गिरने लगा, फ्रे़म जल कर कोयला हो गया, रिसाले और किताबें, रेडियो, रेडियो पर रखा हुआ गुल-दान, गुलदान पर सजे हुए गुलाब के फूल, पहले स्याही माइल हुए, फिर स्याह, फिर बेरंग हो गए। बादामी रंग के सूट, धारीदार टाई और हल्के सब्ज़ रंग की साड़ी की जगह मामूली फटे पुराने कपड़ों में रहम की भीक मांगने वाली चार आँखों ने ले ली। चंद घंटों बल्कि चंद लम्हों ने उनकी उम्रों से कम से कम बीस बीस बरस छीन लिए। एक नस्ल जवान हो गई, एक नस्ल बूढ़ी हो गई, एक नस्ल क़ब्र की गोद में सो गई।
सुनसान सड़क, लुटी हुई दूकानें, बिखरे हुए, टूटे फूटे शीशे के बर्तन, हज़ारों मन लकड़ी जो कोयला, भई, न राख, फ़ायर ब्रिगेड, गश्त लगाती हुई पुलिस की टुकड़ियों के बूटों की आवाज़... अपनी ही सांस और हवा की सरसराहाट से चौंक पड़ने वाले बहादुर दिल, मुस्कुराहटों से नफ़रतें जगाने वाले चेहरे, नफ़रतों को मुस्कुराहटों से क़बूल करने वाली मस्लहतें।
एक दम भगदड़ मच गई। सामने सड़क पर बहुत से लोग एक तरफ़ से दौड़ते हुए आए और जिसका जहाँ सींग समाया घुस गया। दूकानों के शटर आन की आन में गिरा दिए गए, जो सवारी जिस तरफ़ गई लौट कर न आई, सब्ज़ी तरकारी फ़रोख़्त करने वाले ठेले तेज़ी से दौड़ते चले गए, मकानों के दरवाज़े, खिड़कियाँ बंद हो गईं और चंद ही मिनटों में सारे इलाक़े पर कर्फ़यू के सन्नाटे के एक बहुत बदसूरत, मुहीब और बड़े परिंदे ने आकर अपने पर फड़फड़ाए और जहाँ-जहाँ उसके परों की हवा पहुंची वहाँ वहाँ जो लोग सड़कों पर थे, मकानों में घुस गए। जो अपने आंगनों में थे कमरों में चले गए, जो कमरों में थे बिस्तरों में दुबक गए और जो पलंगों के नीचे थे, कोनों खद्दरों और बक्सों के पीछे, मई जून के महीनों के लिए पिछले साल की रखी हुई ख़स की टट्टियों के पीछे दुबक गए। हर तरफ़ सन्नाटा था, कोई आवाज़ न थी, सांस भी लोग आहिस्ता-आहिस्ता ले रहे थे।
फिर एक जीप आई जिस पर लाऊड स्पीकर लगा हुआ था। कुछ सिपाही पीछे बैठे थे, कंधों से बंदूक़ें लटकाए हुए, “शहर के किसी भाग में कोई दुर्घटना नहीं हुई है, कर्फ़यू लगने में अभी तीन घंटे बाक़ी हैं, आप लोग दूकानें खोलिए, सौदा सुल्फ़ ख़रीदिए, कोई दुर्घटना नहीं हुई है।”
लेकिन कोई दूकान नहीं खुली। सौदा सुल्फ़ ख़रीदने कोई घर से नहीं निकला।
“अब्बू, अब्बू”, मेरी बेटी ने दरवाज़े में दाख़िल होते हुए कहा, “गोली चली है बहुत से लोग मारे गए।”
“कहाँ?” मैं हंसा। उसके ज़ेहन से डर दूर करने के लिए मैंने कहा, “गोली तो कहीं नहीं चली।”
“नहीं अब्बू, आपको मालूम नहीं। रिक्शे वाला कह रहा था, कहीं गोली चली है।”
“नहीं बेटी, कहीं गोली नहीं चली।” मैंने कहा।
“नहीं अब्बू।” मेरी सात आठ साल की बच्ची को अपनी मालूमात सही होने पर इसरार था।
“वो बड़े ख़राब हैं।”
“वो कौन?” मैंने डरते हुए पूछा।
“वो...” उसने कंधे पर टंगा हुआ बस्ता उतारते हुए उन लोगों का मजमूई नाम लिया जिन्हें वो अपने से अलग, दूसरा और ग़ैर समझती थी, “वही जिन्होंने इतने बहुत से आदमियों को मार डाला। दूकानें जला दीं।”
अगले रोज़ अख़बार से मालूम हुआ कि कहीं गोली चली थी न झगड़ा हुआ था, एक मरखने बैल ने किसी को दौड़ाया, वो “बचाओ बचाओ” चिल्लाता हुआ भागा, फिर कुछ और लोग भागे, फिर सन्नाटे का मुहीब परिंदा आया और पर फ़ड़फ़ड़ाता रहा और फ़िज़ा में उसके परों से निकलने वाली हवा फैलती रही।
इस मरखने बैल की ख़बर तो अगले रोज़ अख़बारों में छप गई लेकिन इस दरमियान जो दिल हरकत करते करते चंद लम्हों के लिए रुक गए, उन्हें हाथ से निकल जानेवाले उन लम्हों में हरकत कौन देगा और इस आठ साला बच्ची के ऊपर सन्नाटे के मुहीब परिंदे के परों से निकलने वाली हवा से पैदा होने वाले ज़हर और ज़हर-आलूद सवालों का जवाब कौन देगा?
सूखी घास, नए नोटों की तरह कड़कड़ाते नारे जो सिक्का-ए-राइज-उल-वक़्त बने हुए हैं, हर चिंगारी को क़बूल करने और भड़कते हुए शोले में तबदील कर देने वाला दिमाग़... हर दूसरा शख़्स या चंद अश्ख़ास का गिरोह जो मैं नहीं हूँ, या हम नहीं हैं, साज़िशें बनती हुई आँखें, मुस्कुराहटों को कुदूरतों, नफ़रतों, अदावतों के रंग में रंग देने वाले ज़ेहन से जुड़ी हुई दो आँखें। उनमें सचमुच आफ़त की चिंगारी के उड़ कर गिरने, सुलगने, भड़क उठने और फिर राख का ढेर बन जाने के जहाँ इतने सारे सामान मौजूद हूँ, वहाँ कौन किसी का हाथ पकड़ेगा, कौन किसी मुस्कुराहट को क़त्ल का पैग़ाम बनने से रोक लेगा?
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.