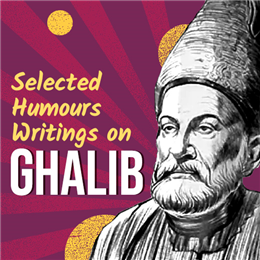ग़ालिब की महफ़िल
(मुक़ाम दिल्ली 1856 ईसवी)
रावी: 1850 ई. तक दिल्ली और लखनऊ की महफ़िलों पर बहार थी, हर तरफ़ शे’र-ओ-सुख़न का चर्चा था। इसमें कोई शक नहीं कि सियासी तौर पर आज़ाद के अलफ़ाज़ में दरख़्त-ए-इक़बाल को दीमक लग चुकी थी। लेकिन अभी बर्ग-ओ-बार की शगुफ़्तगी और ताज़गी को देखते हुए गुमान तक न होता था कि ये दरख़्त गिरा चाहता है। दिल्ली में मोमिन, ज़ौक़, ग़ालिब, शेफ़्ता, सालिक, मजरूह और आज़ुर्दा अपनी रंगीन तवानाइयों से पाबंद-ए-वज़्अ सामईन को मस्हूर कर रहे थे। उधर लखनऊ में 1847 ई. के बाद रंगीले पिया जान-ए-आलम ने दरबार सजाया था और ऐसा रंग जमाया था कि लोग अंदर के अखाड़े को भूल गए थे।
1850 ई. के बाद, शातिर फ़लक ने उस बिसात-ए-अदब के मोहरों को एक एक करके चुनना शुरू किया। 1851 ई. में मोमिन सिधारे, 1854 ई. में ज़ौक़ ने इस दुनिया से मुँह मोड़ा, 1856 ई. में रंगीले पिया जान-ए-आलम माज़ूल हुए और मटिया बुर्ज भेज दिए गए। कुछ परवाने उस बुझी हुई शम्मा का तवाफ़ करने के लिए वहां भी जा पहुंचे लेकिन सच पूछिए तो महफ़िल सूनी हो गई।
तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि 1856 ईसवी है। अगरचे बुझ चुकी है लेकिन ख़ाकस्तर में कुछ चिनगारियां बाक़ी हैं। बिसात उठाई जा रही है लेकिन अभी शे’र-ओ-सुख़न के कुछ मतवाले आँखें बंद किए हाल-ए-मस्त, महफ़िल में बैठे हैं। ये हालत है कि हम आपको दिल्ली क़ासिम जान की गली में लिए चलते हैं, जहां असदुल्लाह ख़ां ग़ालिब अल-मारूफ़ ब मिर्ज़ा नौशा हकीम मुहम्मद हसन ख़ां की हवेली में रहते हैं।
(क़दमों की चाप)
शेफ़्ता: (बुलंद आवाज़ से) कल्लू।
कल्लू: (दूर से) जी सरकार।
शेफ़्ता: क्यों भई मिर्ज़ा नौशा तशरीफ़ रखते हैं?
कल्लू: जी हुज़ूर, दीवानख़ाना में लेटे हैं। मीर मेह्दी मजरूह भी वहीं बैठे हैं।
(वक़फ़ा)
तशरीफ़ ले आइए, आइए नवाब साहिब तशरीफ़ लाइए, ख़्वाजा साहिब।
(चाप)
शेफ़्ता: हुज़ूर तस्लीमात अर्ज़ करता हूँ।
हाली: आदाब बजा लाता हूँ।
ग़ालिब: आहा... नवाब मुस्तफ़ा ख़ां और ख़्वाजा अलताफ़ हुसैन हाली भी साथ तशरीफ़ लाए हैं।
शेफ़्ता: हुज़ूर, ख़्वाजा अलताफ़ हुसैन तो ज़रूर तशरीफ़ लाए हैं लेकिन नवाब मुस्तफ़ा ख़ां कहां हैं?
ग़ालिब: (हंसकर) ईं, मीर मेह्दी, सुना तुमने। अरे भई मेरी बीनाई में इतना फ़ुतूर आ गया। ज़रा देखना ये नवाब मुस्तफ़ा ख़ां नहीं हैं।
मेह्दी मजरूह: हुज़ूर हैं तो नवाब मुस्तफ़ा ख़ां ही।
शेफ़्ता: (हंसकर) कौन, नवाब मुस्तफ़ा ख़ां, वाह मीर मेह्दी ये क्या बात हुई।
ग़ालिब: (हंसकर) अरे भई तो आख़िर तुम फिर कौन हो जो इस तरह बेबाकाना मुझ ख़ाकनशीं के घर घुसे चले आते हो।
शेफ़्ता: (हंसकर) हुज़ूर मैं तो आपका शेफ़्ता हूँ।
ग़ालिब: अख़ाह, ये बात है। सुना मीर मेह्दी। अच्छा भई शेफ़्ता ख़ुदा तुम्हें जज़ाए ख़ैर दे कि एक साठ बरस के बूढ़े पर शेफ़्ता हो।
हाली: हुज़ूर ही का शे’र है,
वफ़ादारी बशर्त-ए-उस्तुवारी अस्ल-ए-ईमाँ है
मरे बुतख़ाने में तो काबे में गाड़ो ब्रहमन को
ग़ालिब: (हंसकर) वाह भई हाली वाह, (वक़फ़ा) इधर आओ न शेफ़्ता मेरे पास।
शेफ़्ता: आज हुज़ूर मेरे हाँ मुशायरे में तशरीफ़ नहीं लाए।
ग़ालिब: ऐ मीर मेह्दी बोलते क्यों नहीं।
(वक़फ़ा)
अरे भई शेफ़्ता इस सय्यद ज़ादे की फ़रमाइशों से नाक में दम है।
शेफ़्ता: हुज़ूर क्या बात हुई?
ग़ालिब: जवाब दो न मीर मेह्दी, अब चुप क्यों साध ली।
मजरूह: नवाब साहिब क़िबला, हुआ ये कि मेरे मिलने वालों में से एक साहिब का लड़का बेचारा नागहां मर गया। वो मेरे सर हो गए कि मिर्ज़ा नौशा से तारीख़ कहलवा दो। ख़ुशी की तक़रीब की फ़र्माइश होती तो मैं टाल भी जाता। बात ऐसी थी कि कुछ कह भी न सकता था। आख़िर उन्हें लेकर हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। उन साहिब को वतन वापस जाने की जल्दी थी। ज़िद करने लगे कि अभी तारीख़ कह दो। बस इसी में उलझे रहे (वक़फ़ा) और फिर कुछ तबीयत भी हुज़ूर की नासाज़ थी।
हाली: ख़ैर बाशद।
ग़ालिब: भई परसों से पिंडलियों में और पांव में दर्द है।
मजरूह: मैं तो कह रहा हूँ कि हुज़ूर पांव दाब दूं। आप मानते ही नहीं।
ग़ालिब: ऐ मीर मेह्दी तुझे शर्म नहीं आती, तू सय्यद ज़ादा हो कर मेरे पांव दाबेगा। क्यों मुझे गुनहगार करता है।
मजरूह: तो आप उजरत दे दीजिएगा ना। आख़िर इसमें हर्ज ही क्या है। लीजिए ज़रा पांव फैलाइए।
ग़ालिब: ऐ मीर मेह्दी तू मानेगा थोड़ा ही, अच्छा जो तेरे जी में आए कर। (वक़फ़ा) हाँ भई शेफ़्ता, मुशायरा कैसा रहा?
शेफ़्ता: आपके बग़ैर मुशायरे में क्या ख़ाक लुत्फ़ आता।
ग़ालिब: शेफ़्ता, सच पूछो तो अब मुशायरों में ग़ज़ल पढ़ने को मेरा जी नहीं चाहता। मुशायरों की रौनक़ तो ज़ौक़ मरहूम और मोमिन मरहूम के दम से थी। हाय मोमिन की जामा ज़ीबी और बांकपन याद आता है तो कलेजे पर साँप लोट जाता है और ज़ौक़ मरहूम की ज़बान का लुत्फ़ ही नहीं भूलता।
शेफ़्ता: ये तो आपने दुरुस्त इरशाद फ़रमाया। हकीम मोमिन ख़ां की मौत ने महफ़िलों को सूना कर दिया।
मजरूह: (हंसकर) हुज़ूर आपने सुना, नवाब साहिब ने क्या इरशाद फ़रमाया।
ग़ालिब: (हंसकर) हाँ मीर मेह्दी सुना, तुम भी ख़ूब समझे। क्यों शेफ़्ता, हकीम मोमिन ख़ां की मौत ने तो महफ़िलों को सूना कर दिया और ज़ौक़ मरहूम का ज़िक्र ही नहीं।
शेफ़्ता: (हंसकर) मेरा ये मतलब ही नहीं था।
ग़ालिब: ख़ैर तुम कुछ ही कहो शेफ़्ता, बा’ज़ शे’र तो ज़ौक़ ने ऐसे कहे हैं कि आदमी पहरों सर धुना करे। (ज़ानू पर हाथ मार के) हाय:
अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे
मर के भी चैन न पाया तो किधर जाऐंगे
मजरूह: सुब्हान-अल्लाह क्या शे’र कहा है, और हुज़ूर ने पढ़ा भी क्या ख़ूब है।
ग़ालिब: और सुनो;
इस रू-ए-ताबनाक पे हर क़तरा अर्क़
गोया कि इक सितारा है सुब्ह-ए-बहार का
हाय हाय क्या अछूती तशबीह है। सितारा है सुब्ह-ए-बहार का।
शेफ़्ता: अच्छा शे’र है।
ग़ालिब: शुक्र है तुमने ज़ौक़ मरहूम के किसी शे’र को अच्छा तो कहा। (वक़फ़ा)
हाँ भई, मुशायरे वाली बात तो वहीं की वहीं रह गई। मिस्र ए तरह क्या था, हाँ याद आ गया;
रंज और रंज भी तन्हाई का।
हाँ तो फिर किस की ग़ज़ल हासिल-ए-मुशायरा रही।
शेफ़्ता: ग़ज़लें कुछ कमज़ोर थीं। (हंसकर) वर्ना कुछ शे’र मुझे ज़रूर याद रह जाते।(वक़फ़ा)
नवाब मिर्ज़ा दाग़ का एक मतला ख़ूब था
मजरूह: हाँ तो इरशाद फ़रमाईए न। क्या मतला था?
शेफ़्ता: मतला था;
जलवा देखा तिरी रानाई का
क्या कलेजा है तमाशाई का
मजरूह: सुब्हान-अल्लाह, सुब्हान-अल्लाह, क्या कलेजा है तमाशाई का।
ग़ालिब: ख़ूब कहा, देखना शेफ़्ता शागिर्द के हाँ उस्ताद से भी ज़्यादा तीखापन और घुलावट है। ज़ौक़ का नाम रोशन कर दिया दाग़ ने।
शेफ़्ता: जी इसमें क्या शक है, लेकिन सच पूछिए तो हमारे ख़्वाजा अलताफ़ हुसैन हाली की ग़ज़ल सबसे अच्छी थी।
ग़ालिब: (ताज्जुब से) हाँ बहुत ख़ूब। हाली, तुमने ग़ज़ल पढ़ी थी।
हाली: जी नहीं।
शेफ़्ता: हुज़ूर बात ये है कि ग़ज़ल उन्होंने कही थी पढ़ी नहीं। मैं समझा के थक रहा, माने ही नहीं। और क्या अर्ज़ करूँ, क्या ग़ज़ल लिखी है।
ग़ालिब: भई हाली, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम शे’र न कहोगे तो तबीयत पर बड़ा ज़ुल्म करोगे। अब शेफ़्ता ने भी क़रीब क़रीब वही बात दूसरे पैराए में बयान की। उनकी बात तो शे’र के मुआमले में बावन तोले पाओ रत्ती सच हुआ करती है। (हंसकर) मेरी बात सुनकर तुमने दिल में कहा होगा कि बूढ़ा सठिया गया है। अब क्या कहते हो।
हाली: हुज़ूर ये क्या इरशाद फ़रमाते हैं।
ग़ालिब: भई आख़िर फिर तुमने ग़ज़ल कही तो पढ़ी क्यों नहीं?
हाली: हुज़ूर...
शेफ़्ता: मैं अर्ज़ करता हूँ, कहते हैं कि हुज़ूर इस्लाह दें तो ग़ज़ल पढ़ता हूँ।
मजरूह: और कहते भी ठीक हैं।
शेफ़्ता: तो और क्या।
ग़ालिब: (हंसकर) तो यूं कहो कि खिचड़ी पकाकर आए हो तुम और हाली। (वक़फ़ा) भई हाली, सुनो बात ये है कि शे’र कहने का जौहर फ़ित्री और तबीई होता है जिसे ये नेअमत मब्दा-ए-फ़य्याज़ की तरफ़ से अता होती है उसका सोना मश्क़ से ख़ुदबख़ुद कसौटी पर चढ़ता चला जाता है। बाक़ी रहा इस्लाह का मुआमला, तो भई मैंने किसी से इस्लाह नहीं ली, मैं तुम्हें क्या इस्लाह दूँगा।
शेफ़्ता: ख़ैर, आज तो हुज़ूर, ख़्वाजा साहिब इस्लाह लिए बग़ैर न मानेंगे।
मजरूह: नवाब साहिब क़िबला, अब हुज़ूर इस्लाह देने से बहुत इजतिनाब करने लगे हैं। आप इसरार फ़रमाएं तो बात बनेगी, पिछले दिनों एक साहिब का ख़त आया कि अब आप मेरे अशआर पर इस्लाह क्यों नहीं देते। आपने बसबब ज़ौक़-ए-सुख़न के अशआर की इस्लाह मंज़ूर फ़रमाई थी, अब क्या बात वाक़े हुई कि आप तवज्जो नहीं फ़रमाते। अब हुज़ूर ही से पूछिए कि हुज़ूर ने क्या जवाब लिखा?
शेफ़्ता: क्या लिखा हुज़ूर ने जवाब में?
ग़ालिब: (हंसकर) जल कर लिखा था कि लाहौल वला क़ुव्वा, किस मलऊन ने बसबब ज़ौक़ शे’र के इस्लाह अशआर मंज़ूर की थी। अगर मैं शे’र से बेज़ार न हूँ तो मेरा ख़ुदा मुझसे बेज़ार। मैंने तो ब तरीक़ क़हर-ए-दरवेश बजान दरवेश लिखा था कि जैसे अच्छी जोरू बुरे ख़ाविंद के साथ मरना भरना क़बूल करती है। मेरा तुम्हारे साथ वो मुआमला है।
(तीनों मिलकर हंसते हैं)
मजरूह: अब आप ही फ़रमाईए नवाब साहिब कि इस्लाह के लिए कोई ग़ज़ल क्या पेश करे।
ग़ालिब: अरे भई हटाओ भी अब ये क़िस्सा। हाँ हाली सुनाओ अपनी ग़ज़ल।
शेफ़्ता: (हंसकर) हाय, क्या ग़ज़ल कही है हाली ने। हुज़ूर तक़सीर माफ़ हो। भई हाली, अगर हुज़ूर इस्लाह देने का वादा न फ़रमाएं तो ग़ज़ल न सुनाना।
हाली: बहुत ख़ूब पीर-ओ-मुर्शिद।
शेफ़्ता: (हंसकर) ख़ूब ग़ज़ल लिखी है हाली ने।
(मीर मेह्दी और हाली मिलकर हंसते हैं)
ग़ालिब: तुम तीनों जीते और मैं हारा। मुझ बूढ़े में अब दम कहां है कि तुम तीनों का मुक़ाबला करूँ। हाँ साहिब ग़ज़ल सुनूँगा और झक मार के इस्लाह भी दूँगा। (तीनों हंसते हैं) लो अब सुनाओ ग़ज़ल हाली।
हाली: मिस्र ए तरह पर गिरह लगा के मतला बना दिया है;
रंज और रंज भी तन्हाई का
वक़्त पहुंचा मिरी रुस्वाई का
मजरूह: वाह-वा, माशा अल्लाह, क्या गिरह लगाई है।
हाली: तस्लीमात। (वक़फ़ा)
उम्र शायद न करे आज वफ़ा
सामना है शब-ए-तन्हाई का
ग़ालिब: हाय क्या शे’र कहा है हाली, “उम्र शायद न करे आज वफ़ा” और दूसरा मिसरा यूं पढ़ो “काटना है शब-ए-तन्हाई का।”
शेफ़्ता: आहा हा, क्या बरजस्ता इस्लाह दी है। हुज़ूर ने क्या मौज़ूं लफ़्ज़ रखा है, “काटना।”
हाली: अपने शे’र का सही मतलब भी मेरी समझ में इस्लाह के बाद ही आया है।
ग़ालिब: हाँ हाली पढ़ो।
हाली: कुछ तो है क़दर तमाशाई की
है जो ये शौक़ ख़ुद-आराई का
यही अंजाम था ऐ फ़स्ले खिज़ाँ
गुल-ओ-बुलबुल की शनासाई का
मजरूह: बहुत ख़ूब, बहुत ख़ूब!
हाली: तस्लीम।
ग़ैर के घर भी न जी से उतरा
पूछना क्या तिरी रानाई का
ग़ालिब: वाह, क्या रानाई का सबूत दिया है। पहले मिसरे को यूं पढ़ो;
बज़्म-ए-दुश्मन में न जी से उतरा
पूछना क्या तिरी रानाई का
शेफ़्ता: ख़ूब इस्लाह दी हुज़ूर ने, ग़ैर का लफ़्ज़ कुछ कमज़ोर था। दुश्मन के लफ़्ज़ ने शे’र में जान डाल दी और फिर बज़्म-ए-दुश्मन, अब उनकी रानाई में किस काफ़िर को शक होगा कि दुश्मन की भरी महफ़िल में ख़ुद महफ़िल-ए-नज़ारा बने बैठे हैं और हाली के जी से नहीं उतरते।
हाली: तस्लीम, मक़ता अर्ज़ करता हूँ;
होंगे ‘हाली’ से बहुत आवारा
दूर है घर अभी रुस्वाई का
मजरूह: अहा, हा, क्या मक़ता है, क्या तमन्ना है। दर-ए-रुस्वाई तक पहुंचने की।
ग़ालिब: ख़ूब ग़ज़ल कही तुमने हाली।
हाली: सब आप ही का फ़ैज़ है।
ग़ालिब: ऐ मीर मेह्दी, मुझे ज़्यादा गुनहगार न कर, अब तू मेरे पांव न दाब।
मजरूह: बहुत अच्छा हुज़ूर, तो लाइए मेरी उजरत दिलवाइए।
ग़ालिब: (हंसकर) वाह, उजरत कैसी? तुमने मेरी पांव दाबे, मैंने तुम्हारी उजरत दाबी। हिसाब बराबर हुआ, उजरत का सवाल कहां है।
(तीनों हंसते हैं)
ग़ालिब: क्यों भई शेफ़्ता, मेरे दीवान की तबाअत का इंतज़ाम हो रहा है ना।
शेफ़्ता: जी हाँ, एक मतबा से बातचीत शुरू की है। तसहीह मैं ख़ुद करलूंगा।
ग़ालिब: तसहीह तो ख़ैर हो जाएगी। तुमने अशआर का इंतिख़ाब भी किया है या नहीं?
शेफ़्ता: ये हुज़ूर क्या इरशाद फ़रमाते हैं। हुज़ूर का कलाम तो सरापा इंतिख़ाब है। हाँ, आपके इरशाद के मुताबिक़ उन अशआर पर निशान लगा रहा हूँ जो ख़ास तौर पर मुझे पसंद हैं।
ग़ालिब: सुना मीर मेह्दी और सुन रहे हो हाली। हमारा कलाम सरापा इंतिख़ाब है (हंसकर) भई शेफ़्ता, अगर तुम्हारे ख़ुलूस पर एतिमाद न होता तो मैं समझता कि तुम मुझे बनाते हो।
शेफ़्ता: ये क्या फ़रमाते हैं आप।
ग़ालिब: सुनो हाली, इक्कीस बरस की उम्र में मैंने एक अच्छा-ख़ासा दीवान मुरत्तिब कर लिया था और उसके बाद उसमें कुछ और रतब दिया, बस मिला के एक नुस्ख़ा भोपाल भेज दिया था। अब जो उन पुरानी ग़ज़लों को पढ़ता हूँ तो ख़ुद हंसी आती है। सब मज़ामीन ख़्याली, बेहूदा जिगर कावी। बात ये है कि शुरू में बेदिल के कलाम पर मर-मिटा था। बड़ी जिगर कावी और अर्क़ रेज़ी से मज़मून तलाश करता था और ऐसी दूर की कौड़ी लाता था कि कभी शे’र का मतलब आधा, और कभी पूरा ख़ब्त हो जाता था और हमारे नवाब मुस्तफ़ा ख़ां कहते हैं कि आपका कलाम सरापा इंतिख़ाब है। अब तुम्हीं बताओ कि हमारी इस बज़्लासंजी का क्या जवाब है। (हाली और मीर मेह्दी हंसते हैं)
शेफ़्ता: हुज़ूर के रंग-ए-क़दीम के शे’र भी अच्छे हैं।
ग़ालिब: अच्छे तो क्या हैं, हाँ ये पता चलता है कि शायर पुराने ढर्रे पर नहीं चलता। (वक़फ़ा) बेदिल के ततब्बो ने जहां मुझे नुक़्सान पहुंचाया है वहां फ़ायदा भी ख़ास्सा हुआ है। पेश पाउफ़्तादा मज़ामीन से गुरेज़, पामाल ख़्यालात से इजतिनाब, मज़मून की जुस्तजू में जिगर कावी, अलफ़ाज़ की नशिस्त में अर्क़ रेज़ी बेदिल ही का फ़ैज़ान है। इख़तिरा तराकीब फ़ारसी का गुर, और इस्तिआरात-ओ-तशबीहात की तुर्फ़गी का सबक़ मैंने बेदिल ही से सीखा है।
शेफ़्ता: हुज़ूर की बा’ज़ तशबीहात और इस्तिआरात तो लाजवाब हैं, सुनो हाली;
ख़ूँ दर जिगर निहुफ़ता ब ज़र्दी रसीदा हूँ
ख़ुद आशियाने ताइर-ए-रंग पुरीदा हूँ
दौरान-ए-सर से गर्दिश-ए-साग़र है मुत्तसिल
ख़ुम ख़ाना-ए-जुनूँ में दिमाग-ए-रसीदा हूँ
मैं चश्म-ए-वा कुशादा-ओ-गुलशन नज़र फ़रेब
लेकिन अबस कि शबनम-ए-ख़ुरशीद दीदा हूँ
सर पर मिरे वबाल-ए-हज़ार आरज़ू रहा
या-रब मैं किस ग़रीब का बख़्त-ए-रसीदा हूँ
हूँ गर्मि-ए-निशात-ए-तसव्वुर नग़मा संज
मैं अंदलीब गुलशन-ए-ना-आफ़्रीदा हूँ
पानी से सग गज़ीदा डरे जिस तरह असद
डरता हूँ आईने से कि मर्दुम गज़ीदा हूँ
हाली: सुब्हान-अल्लाह, एक से एक बढ़कर तशबीयह है। सारी ग़ज़ल मुरस्सा है।
मजरूह: ऐसी तरकीबें और ऐसे तशबीहात-ओ-इस्तिआरात कि एक दरयाए-मआनी को मुख़्तसर से लफ़्ज़ों के कूज़े में बंद कर दें और कहाँ मिलेंगी।
ग़ालिब: (हंसकर) ऐब मै जुमला बगफ़ती हुनरशि नीज़ बगो, तुम तो क्यों बयान करोगे। मुझसे ख़ुद अपने इब्तिदाई दौर की बेहूदगियां सुनो। देखो ये शे’र भी मेरे ही हैं:
जुनूँ गर्म इंतज़ार-ओ-नाला बेताबी-ए-कमंद आया
सुवैदा ता ब-लब ज़ंजीर से दूद सिपंद आया
मह-ओ-अख़तर फ़िशां की बहर-ए-इस्तिक़बाल आँखों से
तमाशा किशवर-ए-आईना में आईना बंद आया
अदम है ख़ैर ख्वाह-ए-जलवा को ज़िंदान-ए-बेताबी
ख़िराम-ए-नाज़, बर्क़-ए-ख़िरमन-ए-सई पसंद आया
(हंसकर) क्यों जी हमारा कलाम सरापा इंतिख़ाब है ना?
(तीनों हंसते हैं, क़दमों की चाप)
कल्लू: हुज़ूर, बेगम साहिबा ज़नान ख़ाने में तशरीफ़ ले जाना चाहती हैं। मकान देखकर वापस तशरीफ़ लाई हैं।
ग़ालिब: अच्छा लीजिए, आप सब साहिब ज़रा इस साथ वाले कमरे में होजाएं।
(क़दमों की चाप, वक़फ़ा)
(क़दमों की चाप, ग़ालिब क़हक़हा लगाता है)
ग़ालिब: भई लतीफ़ा हो गया, इस वक़्त तो (फिर हँसता है) ।
शेफ़्ता: इरशाद, इरशाद।
ग़ालिब: भई बात ये है कि बरसात में इस मकान में बहुत तकलीफ़ होती है। ख़ुदा का क़हर है। मेंह घड़ी-भर बरसे तो छत घंटा भर बरसती है। आख़िर बेगम ने तक़ाज़ा किया कि मकान बदलो। मैं मरी। में दिल्ली आज नया मकान देखने गई थीं। अब जो वापस आईं तो मैंने पूछा कि मकान पसंद आया तो फ़रमाया कि मकान तो अच्छा है लेकिन लोग उसमें बला बताते हैं। ये सुनकर मैंने कहा कि दुनिया में आपसे बढ़कर भी कोई बला है।
(चारों हंसते हैं)
ग़ालिब: हाँ भई हाली, अगर बेदिल का रंग मुझ पर छाया रहता तो उर्दू में तर्ज़-ए-बेदिल न निभती। बस यूं समझ लो कि बेहूदा गो होकर रह जाता। वो तो यूं कहो कि मबदाए फ़य्याज़ ने मुझे गुमराह न होने दिया। मीर की सादगी ने चश्मनुमाई की। सहल मुम्तना कलाम ने मुझे मुतनब्बा किया। रफ़्ता-रफ़्ता मैं सीधे ढर्रे पर आगया। शेफ़्ता की सोहबत ने मेरे जौहर को और भी चमका दिया। अब देख लो ग़ज़ल का क्या रंग है।
शेफ़्ता: ये तो हुज़ूर की ज़र्रा नवाज़ी है। (हंसकर) परसों लतीफ़ा हुआ। मेरे मकान पर अहबाब जमा थे कि कोई साहिब हैं अफ़सोस तख़ल्लुस फ़रमाते हैं, वो तशरीफ़ ले आए। आपका ज़िक्र आगया तो उन्होंने आपकी ग़ज़ल उम्मीद बर नहीं आती, नज़र नहीं आती के कुछ शे’र पढ़े और फिर जब ये शे’र पढ़ा, आगे आती थी हाल-ए-दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, तो फ़रमाया कि इस शे’र में क्या बात है। पामाल मज़मून है और तर्ज़-ए-अदा में भी कोई जिद्दत नहीं। ताज्जुब है कि मिर्ज़ा नौशा ने ऐसा शे’र कहा, मैं तो समझता हूँ कि ये शे’र उनका है ही नहीं।
ग़ालिब: (हंसकर) सुख़न-फ़हमी आलम-ए-बाला मालूम शुद, फिर...
शेफ़्ता: मैंने मतानत से कहा कि क़िबला, शे’र तो ये मिर्ज़ा नौशा ही का है लेकिन माफ़ कीजिएगा, आप शे’र का हुलिया बिगाड़ के इस तरह पढ़ते हैं कि मिर्ज़ा नौशा का शे’र नहीं रहता।
ग़ालिब: बहुत ख़ूब।
शेफ़्ता: फिर मैंने शे’र पढ़के सुना दिया और मज़े की बात ये है कि शे’र का मतलब फिर भी न समझे। फिर जो अहबाब ने खोल के मतलब समझाया तो बहुत झेंपे और फ़ौरन उठकर चल दिए।
मजरूह: ज़रा पढ़ीएगा तो शे’र नवाब साहिब क़िबला, किस तरह शे’र पढ़ने से मतलब साफ़ होना चाहिए।
शेफ़्ता: सुनिए आगे आती थी हाल-ए-दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती (बात पर-ज़ोर देकर पढ़ा जाये।)
हाली: वाह, नवाब साहिब क्या पहलू बदला है शे’र के मज़मून ने। मतलब ये हुआ कि दीवानगी का सा आलम तो पहले भी था कि अपने दिल के हाल पर ख़ुद ही हंस लिया करते थे। यहां तक तो ख़ैरियत लेकिन अब तो ये आलम है कि हंसी किसी बात पर नहीं आती, बेवजह भी हंस देते हैं।
मजरूह: वाह, ख़्वाजा साहिब, आपने ख़ूब मतलब समझा शे’र का।
(दूर से एक मर्दाना आवाज़, जिसमें रस और सोज़ है, सुनाई देती है, ये गाती हुई, “मुद्दत हुई है यार को मेहमाँ किए हुए।” आवाज़ क़रीब आती जाती है।)
ग़ालिब: ज़रा सुनना शेफ़्ता।
शेफ़्ता: जी सुन रहा हूँ।
ग़ालिब: ये एक दरवेश सिफ़त आदमी है जिसे मेरे बहुत से शे’र याद हैं। पिछले दिनों उसने मेरी ग़ज़ल गाकर सुनाई थी। दिल-ए-नादाँ तुझे हुआ क्या है।
शेफ़्ता: तो दीवानख़ाने में बुला लें।
ग़ालिब: नहीं आएगा और लुत्फ़ ये है कि कुछ लेता भी नहीं। पिछली बार मैंने कुछ देना चाहा तो ख़फ़ा हो गया। बस चुप-चाप बैठे सुना करो। ग़ज़ल गाएगा और चला जाएगा।
(अब आवाज़ साफ़ आती है और ये ग़ज़ल गाई जाती है)
मुद्दत हुई है यार को मेहमाँ किए हुए
जोश-ए-क़दह से बज़्म-ए-चराग़ां किए हुए
फिर चाहता हूँ नाम-ए-दिलदार खोलना
जां नज़र दिलफ़रेबी-ए-उनवाँ किए हुए
मांगे है फिर किसी को लब-ए-बाम पर हवस
ज़ुल्फ़-ए-सियाह रुख़ पे परेशां किए हुए
चाहे है फिर किसी को मुक़ाबिल में आरज़ू
सुरमे से तेज़ दुशना-ए-मिज़्गाँ किए हुए
इक नौबहार-ए-नाज़ को ताके है फिर निगाह
चेहरा फ़रोग़-ए-मय से गुलिस्ताँ किए हुए
जी ढूंढता है फिर वही फ़ुर्सत कि रात-दिन
बैठे रहें तसव्वुर-ए-जानां किए हुए
ग़ालिब हमें न छेड़ कि फिर जोश-ए-अश्क से
बैठे हैं हम तहय्या-ए-तूफ़ाँ किए हुए
(आख़िरी शे’र के साथ आवाज़ दूर होती चली जाती है, ग़ज़ल के गाने के दौरान में शेफ़्ता, मजरूह और हाली मौक़ा ब मौक़ा दाद देते हैं।)
शेफ़्ता: क्या मुरस्सा ग़ज़ल है ये हुज़ूर की, हर शे’र लाजवाब है। (हंसकर) “हर चह अज़ दिल ख़ेज़द बर्दिल रेज़द” वाला मुआमला है।
ग़ालिब: तुम भी क्या बातें ले बैठे शेफ़्ता, बुढ़ापे में हमें ये तज़्किरे नापसंद हैं।
(वक़फ़ा)
लो मैं अभी आया।
(क़दमों की चाप)
शेफ़्ता: (सरगोशी में लेकिन इस तरह कि आवाज़ साफ़ सुनाई दे) मीर मेह्दी ये ग़ज़ल सुनकर मिर्ज़ा नौशा की नज़रों में अगले वक़्तों की तस्वीर फिर गई। इस वाक़िया की कसक अब तक उनके दिल से गई नहीं।
मजरूह: (उसी तरह सरगोशी में कि आवाज़ साफ़ सुनाई दे) आपकी मुराद है कि ये उसी का ज़िक्र है, जिसने (आवाज़ साफ़ सुनाई नहीं देती सिर्फ़ खुसर पिसर की आवाज़ आती है।)
शेफ़्ता: (सरगोशी में) अरे एक क़त्ताल-ए-आलम थी वो आफ़त का टुकड़ा। हई हई वो हुस्न वो रागदारी और फिर मिर्ज़ा नौशा ने।(आवाज़ सुनाई नहीं देती, खुसर फुसर की आवाज़ आती है।)
मजरूह: उसके मरने का बड़ा सदमा हुआ था उनको। मैं देखता था... (आवाज़ सुनाई नहीं देती)
शेफ़्ता: और उसका मर्सिया भी कैसा दर्दनाक लिखा है, मिर्ज़ा नौशा ने,
किस तरह काटे कोई शब हाय तार-ए-बर्शगाल
है नज़र ख़ू कर्द-ए-अख़्तर-शुमारी हाय हाय
गोश महजूर-ए-पयाम-ओ-चश्म महरूम-ए-जमाल
एक दल तिस-पे ये ना उम्मीदवारी हाय हाय
मजरूह: और मक़ता तो मुलाहिज़ा हो;
गर मुसीबत थी तो ग़ुर्बत में उठा लेते ‘असद’
मेरी दिल्ली ही में होनी थी ये ख़्वारी हाय हाय
शेफ़्ता: (हंसकर) जो दीवान छपने के लिए जा रहा है, उसमें मक़ता को यूं बदल दिया है;
इश्क़ ने पकड़ा न था ग़ालिब अभी उलफ़त का रंग
रह गया था दिल में जो कुछ ज़ौक़-ए-ख़्वारी हाय हाय
(क़दमों की चाप)
ग़ालिब: हाँ भई शेफ़्ता।
कल्लू: हुज़ूर, मतबा समर हिंद से, एक आदमी आया है। कहता है दीवान-ए-सुख़न देहलवी पर जो कुछ आपको लिखना था वो लिख लिया हो, तो इनायत फ़र्मा दीजिए।
ग़ालिब: भई उससे कह दो कि शाम तक वो काग़ज़ पहुंच जाएगा।
कल्लू: बेहतर हुज़ूर।
शेफ़्ता: सुख़न देहलवी अपना कलाम छपवा रहे हैं और आप तक़रीज़ लिख रहे हैं।
ग़ालिब: हाँ भई शेफ़्ता, मैंने तो बहतेरा उसे समझाया कि भाई मुझसे तक़रीज़ न लिखवाओ। एक तो मैं जो कुछ लिख के देता हूँ, लोग उससे ख़ुश नहीं होते, दूसरे मेरी तक़रीज़ और तारीफ़, किसी को रास नहीं आती। लेकिन वो मानता ही नहीं।
शेफ़्ता: जी हाँ, लोग ये शिकायत तो करते हैं कि आप मुसन्निफ़ की सताइश में मज़ाइक़ा करते हैं और तक़रीज़ में इधर उधर की बातें लिख कर टाल देते हैं।
ग़ालिब: सच है शेफ़्ता, कि मुझे हिंदुस्तानी फ़ारसी लिखने वालों की रविश नहीं आती, कि बिल्लकुल भाटों की तरह बकना शुरू कर दूं, मेरे क़सीदे उठाकर देख लो, तश्बीब के शे’र बेशतर, और मदह के कमतर पाओगे।
मजरूह: तो हुज़ूर ने इस तक़रीज़ में क्या लिखा है?
ग़ालिब: कुछ इधर उधर की बातें हैं, तारीफ़ में तो ये दो फ़िक़रे हैं कि “इस सेहरकार जादू निगार ने परीज़ादान-ए-मआनी को अलफ़ाज़ के शीशों में इस तरह उतारा है, जैसे आबगीन-ए-मय से रंग-ए-मय नज़र आए। लफ़्ज़ से जल्वा-ए-मअनी आश्कारा है, चश्म-ए-बद्दूर आग़ाज़-ए-जवानी और नौ-बहार बाग़ ज़िंदगानी है, उम्र के लिए दफ़्तर क़ज़ा-ओ-क़दर में हुक्म-ए-दवाम लिखा गया है।”
मजरूह: सुब्हान-अल्लाह, क्या मोती पिरोए हैं। हुज़ूर तो मजमा उलबहरीन हैं। नज़्म चश्म-ए-बद्दूर, नस्र नूरू अली नूर।
हाली: हज़रत सुख़न के अशआर हुज़ूर को याद हों तो सुनाइए।
ग़ालिब: मेरे हाफ़िज़े का हाल तो तुम जातने ही हो। शे’र किस मलऊन को याद रहता है।
शेफ़्ता: एक-आध शे’र शायद याद आजाए।
ग़ालिब: हूँ (वक़फ़ा) ख़ूब याद आया। एक ताज़ा ग़ज़ल के कुछ शे’र आज एक पुर्जे़ पर लिख कर दे गया था। वो शायद यहीं कहीं पड़ा होगा पुर्ज़ा, (वक़फ़ा) ये रहा। सुनो भई शेफ़्ता।
मिले न दर्द भी साक़ी शराब के बदले
जले न क्योंकर मिरा दिल कबाब के बदले
मजरूह: ख़ूब, बहुत ख़ूब।
ग़ालिब: नहीं भई, मतला मामूली है, जभी शेफ़्ता चुप रहे, अब दो शे’र और सुनो;
शबीह-ए-यार को बदलूँ शबीह-ए-यूसुफ़ से
वर्क़ ग़ुलाम का लूं आफ़ताब के बदले
सँभाला होश तो मरने लगे हसीनों पर
हमें तो मौत ही आई शबाब के बदले
शेफ़्ता: सुब्हान-अल्लाह, मौत का लफ़्ज़ क्या ज़ू मानी रखा है, अच्छा शे’र कहा है।
ग़ालिब: ख़्वाजा अलताफ़ हुसैन साहिब।
हाली: जी इरशाद।
ग़ालिब: अब आप कानों में उंगलियां दे लें ज़रा।
मजरूह: (हंसकर) वो क्यों?
ग़ालिब: ऐ मीर मेह्दी, ये ठेरे मौलवी। मुझे शे’र पढ़ना हैं शराब की तारीफ़ में, जो ये बिगड़ गए तो।
हाली: आप यूं मुझे शर्मसार करते हैं हुज़ूर।
ग़ालिब: तो सुनो भई।
वो बादाकश हूँ कि ग़फ़लत हुई तो साक़ी ने
दिया शराब का छींटा गुलाब के बदले
शेफ़्ता: सुब्हान-अल्लाह, शागिर्द का शे’र सुनकर उस्ताद का एक शे’र याद आ गया।
ग़ालिब: यानी मेरा?
शेफ़्ता: जी हाँ।
आसूदा बाद ख़ातिर-ए-ग़ालिब कि खूए ओस्त
आमेख़्तन ब बादा-ए-साफ़ी गुलाब रा
वाह वाह, रिन्दी के मज़ामीन बांधना ख़ास हुज़ूर का हिस्सा है, हाय।
फिर देखिए अंदाज़-ए-गुल अफ़शाई गुफ़्तार
रख दे कोई पैमाना-ए-सहबा मिरे आगे
शेफ़्ता: और वो शे’र;
जाँफ़िज़ा है बादा जिसके हाथ में जाम आ गया
सब लकीरें हाथ की गोया रग-ए-जां हो गईं
ग़ालिब: हंसकर भई मुझे तो अपना ये शे’र पसंद है;
कल के लिए कर आज न ख़िस्त शराब में
ये सूए ज़न है साक़ी-ए-कौसर के बाब में
हाली: ख़ूब, हुज़ूर ने क्या हीला-ए-शरई निकाला है।
(तीनों हंसते हैं)
ग़ालिब: सुना भई शेफ़्ता, नहीं चौके न मौलवी हाली, दाद भी फ़िक़हियों और मौलवियों की इस्तिलाह में दी।
शेफ़्ता: ये सब आपका फ़ैज़ है (वक़फ़ा) अब इजाज़त मर्हमत हो। आज वापस जाने का इरादा है।
हाली: मुझे भी इजाज़त मर्हमत हो।
ग़ालिब: भई जी तो नहीं चाहता कि तुम दोनों चले जाओ लेकिन अब मजबूरी है, हाँ भई अब दीवान की तबाअत का काम तुम्हारे ज़िम्मे है।
शेफ़्ता: आप इतमीनान रखें, मैं ख़ुद तसहीह करलूंगा। अच्छा, तस्लीमात।
हाली: ख़ुदा-हाफ़िज़।
ग़ालिब: फ़ी अमान अल्लाह।
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.