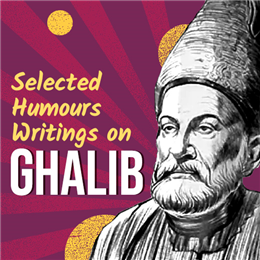तुझे हम वली समझते जो न बादा ख़्वार होता
रावी: यादगार-ए-ग़ालिब में हाली लिखते हैं,
“मरने से कई बरस पहले चलना फिरना मौक़ूफ़ हो गया था। अक्सर औक़ात पलंग पर पड़े रहते थे। ग़िज़ा कुछ ना रही थी। 1866 ई. में ख़्वाजा अज़ीज़ लखनवी लखनऊ से कश्मीर जाते वक़्त रास्ते में ग़ालिब से मिले थे, मिर्ज़ा साहिब के पुख़्ता मकान में एक बड़ा फाटक था, जिसकी बग़ल में एक कमरा और कमरे में एक चारपाई बिछी हुई थी। उस पर एक नहीफ़-उल-जुस्सा आदमी, गंदुमी रंग, अस्सी-बयासी साल के ज़ईफ़, लेटे हुए, एक मुजल्लद किताब सीने पर रखे, आँखें गड़ोए हुए पढ़ रहे थे। ये ग़ालिब थे, जो दीवान-ए-क़ाआनी मुलाहिज़ा फ़र्मा रहे थे।
ख़्वाजा अज़ीज़: आदाब बजा लाता हूँ (ज़ोर से) आदाब बजा लाता हूँ (वक़फ़ा)
ग़ालिब: तशरीफ़ रखिए। बंदा-परवर, ये क़लमदान और काग़ज़ है, आँखों से किसी क़दर सूझता भी है लेकिन कानों से बिल्कुल सुनाई नहीं देता। जो कुछ मैं पूछूँ उसका जवाब लिख दो। कहां से आए हो, क्या नाम है। (वक़फ़ा)
अज़ीज़ लखनवी, मुझसे मिलने आए हो तो ज़रूर कुछ न कुछ कहते होगे। कुछ अपना कलाम भी सुनाओ।
अज़ीज़: हम तो आपका कलाम आपकी ज़बान मुबारक से सुनने की ग़रज़ से आए थे।
ग़ालिब: भई कुछ तो सुनाओ।
अज़ीज़: एक मतला याद आया है, वो अर्ज़ किए देता हूँ। महज़ तामील-ए-इरशाद है,
मह-ए-मिस्र अस्त दाग़ अज़ रश्क-ए-महताबे कि मन दारम
ज़ुलेख़ा को रशद अज़ हसरत-ए-ख़्वाबे कि मन दारम
ग़ालिब: सुब्हान-अल्लाह क्या मज़े का मतला कहा है। भाई तुम तो ख़ूब कहते हो (शे’र दोहराते हैं),
अज़ीज़: अब आप भी कुछ इरशाद फ़रमाईए। मुद्दत से आरज़ू थी कि आपका कलाम आपकी ज़बान से सुनें।
ग़ालिब: क्या सुनाऊँ, मेरा हाल देख ही रहे हो। एक ग़ज़ल के चंद शे’र याद आगए। वही सुनाए देता हूँ,
हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी कि हर ख़ाहिश पे दम निकले
बहुत निकले मरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले
डरे क्यों मेरा क़ातिल क्या रहेगा उसकी गर्दन पर
वो ख़ूँ जो चश्म-ए-तर से उम्र भर यूं दम-ब-दम निकले
निकलना ख़ुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन
बहुत बे-आबरू हो कर तिरे कूचे से हम निकले
भरम खुल जाये ज़ालिम तेरी क़ामत की दराज़ी का
अगर इस तुर्रा-ए-पुरपेच-ओ-ख़म का पेच-ओ-ख़म निकले
हुई इस दौर में मंसूब मुझ से बादा आशामी
फिर आया वो ज़माना जो जहां में जाम-ए-जम निकले
हुई जिनसे तवक़्क़ो ख़स्तगी की दाद पाने की
वो हमसे भी ज़्यादा ख़स्ता-ए-तेग़-ए-सितम निकले
मुहब्बत में नहीं है फ़र्क़ जीने और मरने का
उसी को देखकर जीते हैं जिस काफ़िर प दम निकले
कहां मयख़ाने का दरवाज़ा ‘ग़ालिब’ और कहां वाइज़
पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले
अज़ीज़: हुज़ूर आपने बड़ा सरफ़राज़ किया। गुस्ताख़ी होती है मगर अभी सेरी नहीं हुई।
ग़ालिब: भाई, अब मैं थक गया। एक शे’र और सुन लो। आजकल अक्सर पढ़ता रहता हूँ,
ज़िंदगी अपनी जो इस शक्ल से गुज़री ‘ग़ालिब’
हम भी क्या याद करेंगे कि ख़ुदा रखते थे
ग़ालिब: (बा-आवाज़-ए-बुलंद) खाना लाओ।
अज़ीज़: हुज़ूर तकलीफ़ न कीजिए। हम सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए उतर पड़े थे। रेल का वक़्त बिल्कुल क़रीब है। बग्घी सराय में खड़ी है, अस्बाब बंधा हुआ रखा है। आपसे मिलने को आए थे, अब इजाज़त चाहते हैं।
ग़ालिब: आपकी ग़ायत इस तकलीफ़ से ये थी कि मेरी सूरत और कैफ़ियत मुलाहिज़ा फ़रमाएं, ज़ोफ़ की हालत देखी कि उठना बैठना दुशवार है। बसारत की हालत देखी कि आदमी को पहचानता तक नहीं हूँ। समाअत की कैफ़ियत मुलाहिज़ा की कि कोई कितना ही चीख़े, ख़बर नहीं होती। ग़ज़ल पढ़ने का अंदाज़ मुलाहिज़ा किया, कलाम सुना, अब एक बात रह गई है कि मैं क्या खाता हूँ, इसको भी मुलाहिज़ा करते जाइए। सुबह को सात बादाम का शीरा, क़ंद के शर्बत के साथ। दोपहर को टके भर गोश्त का गाढ़ा पानी, कभी दो-चार फुल्के। क़रीब शाम तीन तले हुए कबाब, कुछ घड़ी रात गए पाँच रुपये भर शराब, ज़िंदगी अज़ाब हो गई है। हाय, मेरा एक शे’र है,
याद थीं हमको भी रंगारंग बज़्म-आराइयाँ
लेकिन अब नक़्श-ओ-निगार ताक़-ए-निस्याँ हो गईं
(फिर ठहर ठहर कर गुनगुनाते हैं)
रावी: ग़ालिब आगरे में रौनक़ अफ़रोज़ हैं। दीवान सिंह राजा के यहां ग़ालिब के एज़ाज़ में एक मख़सूस ग़ैर तरही मुशायरा है। इफ़हाम उद्दीन साहिर, अहमद शेवन, ज़ैन-उल-आबदीन शोरिश, ग़ुलाम ग़ौस बेख़बर शरीक हैं। ग़ालिब बातें कर रहे हैं।
ग़ालिब: भई हमको इब्तदाए शबाब में एक मुर्शिद-ए-कामिल ने नसीहत की थी कि ज़ोह्द-ओ-वरा मंज़ूर नहीं। ताहम क़ानेअ फ़िस्क़-ओ-फ़ुजूर हैं। पियो, खाओ, मज़े उड़ाओ। मगर ये याद रहे कि मिस्री की मक्खी बनो, शहद की मक्खी न बनो। सो मेरा इस नसीहत पर अमल रहा है। मैं जब बहिश्त का तसव्वुर करता हूँ और सोचता हूँ कि अगर मग़फ़िरत हो गई और एक क़स्र मिला और एक हूर मिली। इक़ामत-ए-जाविदानी है और उसी एक नेक बख़्त के साथ ज़िंदगानी है। इस तसव्वुर से जी घबराता है और कलेजा मुँह को आता है। है है वो हूर अजीरन हो जाएगी। तबीयत क्यों न घबराएगी। वही ज़मुर्रदें काख़ और वही तूबा की एक शाख़, चश्म-ए-बद्दूर, वही एक हूर।
बे-ख़बर: हुज़ूर ज़रा इस हूर को भी देखिए।
ग़ालिब: कौन?
बे-ख़बर: ये दुर्गा बाई सनम हैं। वाह, क्या सज-धज है। क़श्क़े की आब-ओ-ताब और सब्ज़ दोशाले की आन बान तो देखिए।
सनम: आदाब बजा लाती हूँ। आपका अरसे से शुहरा सुना था, आज ज़ियारत हुई।
ग़ालिब: वाह, सियह चोटी, ज़रअफ़शाँ मांग, सब्बज़ उस पर दोशाला है
तमाशा है पर ताऊस में काले को पाला है
सनम: आपकी ज़र्रा नवाज़ी है।
ग़ालिब: आप ज़र्रा नहीं आफ़ताब हैं। हाँ साहिब, अब मुशायरा शुरू हो, सनम साहिबा आप ही शुरू कीजिए।
सनम: अर्ज़ करती हूँ,
कुछ दवा-ए-दिल-ओ-जिगर न हुई
मर गए तुम उन्हें ख़बर न हुई
दिल-ओ-जां हिज्र में गए ऐसे
एक को एक की ख़बर न हुई
रहें अब दैर ही में चल के ‘सनम’
अपनी काबे में तो बसर न हुई
ग़ालिब: सुब्हान-अल्लाह, शायरा और शे’र दोनों का जवाब नहीं। ख़ैर, अब चंद शे’र मेरे भी सुन लीजिए,
है बस-कि हर इक उनके इशारे में निशाँ और
करते हैं मुहब्बत तो गुज़रता है गुमाँ और
या-रब वो न समझे हैं न समझेंगे मरी बात
दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां और
है ख़ून-ए-जिगर जोश में दिल खोल के रोता
होते जो कई दीदा-ए-खू ना ब फ़िशां और
मरता हूँ हर इक वार पे हरचंद सर उड़ जाये
जल्लाद को लेकिन वो कहे जाएं कि हाँ और
हैं और भी दुनिया में सुख़नवर बहुत अच्छे
कहते हैं कि ‘ग़ालिब’ का है अंदाज़-ए-बयाँ और
बे-ख़बर: सच है, ग़ालिब का है अंदाज़ बयाँ और।
(हल्की मौसीक़ी)
रावी: मुफ़्ती सदर उद्दीन ख़ां आज़ुर्दा की अदालत है। ग़ालिब का मुक़द्दमा पेश होता है। इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने शराब क़र्ज़ ली और दाम न दे सके।
मुफ़्ती सदर उद्दीन आज़ुर्दा: कहिए मिर्ज़ा साहिब, आपको अपनी सफ़ाई में कुछ कहना है। इस्तिग़ासा के गवाहों के बयानात बिल्कुल वाज़ेह हैं।
ग़ालिब: पीर-ओ-मुर्शिद मुझे कुछ अर्ज़ करना नहीं, मेरा एक शे’र है। इस वक़्त याद आया, वो सुनाए देता हूँ,
क़र्ज़ की पीते थे मय लेकिन समझते थे कि हाँ
रंग लाएगी हमारी फ़ाका मस्ती एक दिन
मुफ़्ती साहिब: मिर्ज़ा साहिब क्या शे’र कहा है। आप जैसे शायर बेबदल के लिए अदालत में इस तरह खिचा खिचा फिरना आपकी तौहीन है, आप तशरीफ़ ले जाइए। जुर्माने की रक़म मैं अपने पास से अदा किए देता हूँ।
दरबारी के हल्के हल्के सुर आहिस्ता-आहिस्ता बुलंद होजाते हैं।
नक़ीब: निगाह-ए-रूबरू, आला हज़रत ख़िताब फ़रमाते हैं।
बहादुर शाह ज़फ़र: अब मिर्ज़ा नौशा की बारी है। मिर्ज़ा साहिब, अपनी ग़ज़ल सुनाइए। मगर रेख़्ता हो, फ़ारसी नहीं।
ग़ालिब: पीर-ओ-मुर्शिद,
फ़ारसी बीं ता-बीनी नक़्श हाय रंग रंग
बगुज़र अज़ मजमूआ-ए-उर्दू कि बेरंग मन अस्त
ज़फ़र: माबदौलत तो उर्दू में शे’र कहते हैं और उसी का शे’र पसंद करते हैं।
ग़ालिब: अर्ज़ करता हूँ,
ये न थी हमारी क़िस्मत कि विसाल-ए-यार होता
अगर और जीते रहते, यही इंतज़ार होता
तिरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना
कि ख़ुशी से मर न जाते अगर एतबार होता
कोई मेरे दिल से पूछे तिरे तीर नीम कश को
ये ख़लिश कहां से होती जो जिगर के पार होता
ग़म अगरचे जांगुसिल है प कहाँ बचें कि दिल है
ग़म-ए-इश्क़ गर न होता ग़म-ए-रोज़गार होता
उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता
जो दुई की बू भी होती तो कहीं दो-चार होता
ये मसाईल-ए-तसव्वुफ़ ये तिरा बयान ‘ग़ालिब’
तुझे हम वली समझते जो न बादा-ख़्वार होता
सुब्हान-अल्लाह, सुब्हान-अल्लाह।
ज़फ़र: भई, हम तो तब भी वली न समझते।
ग़ालिब: पीर-ओ-मुर्शिद तो अब भी ऐसा ही समझते हैं मगर ये इसलिए इरशाद हुआ कि मैं अपनी विलाएत पर कहीं मग़रूर न होजाऊं।
ज़फ़र: (हल्का क़हक़हा) मिर्ज़ा नौशा, ख़ुदा तुम्हें ज़िंदा रखे। बड़े ही दिलचस्प आदमी हो और भई पढ़ते तो ख़ूब हो।
रावी: 9 बजे सुबह का अमल है, ग़ालिब खाना खाने अंदर जाते हैं। चेहरे पर परेशानी के आसार हैं। एक तोता सर्दी की वजह से सिमटा सिमटाया परों में चोंच दबाए बैठा है।
ग़ालिब: मियां मिट्ठू, न तुम्हारे जोरू न बच्चे, तुम किस फ़िक्र में सर झुकाए बैठे हो।
उमराव बेगम: मैं कहती हूँ ये तुम्हें हो क्या गया है और कुछ न मिला तो इस तोते के पीछे पड़ गए।
ग़ालिब: तो क्या झूट कहता हूँ, मेरा एक फ़ारसी का क़तआ है,
ब आदम ज़न ब शैतान तौक़ लानत
सिपर दंदाज़ रह-ए-तकरीम-ओ-तज़लील
व लेकिन दर असीरी तौक़-ए-आदम
गिराँ-तर आमद अज़ तौक़-ए-अज़ाज़ील
उमराव: हाँ हाँ, तुम तो मुझे तौक़-ए-लानत समझते हो। मैं तो रोज़ ख़ुदा से दुआ माँगती हूँ कि मुझ गुनाहगार को इस दुनिया से उठा ले या तुम्हारी इस्लाह कर दे। बूढ़े होने को आए, क़ब्र में पैर लटकाए बैठे हो, मगर ये मुई शराब ऐसी मुँह से लगी है कि छूटती ही नहीं।
ग़ालिब: तुम्हें क्या, तुमने तो अपने खाने पीने के बर्तन अलग कर ही लिये।
उमराव: (तेज़ हो कर) क्यों न करती। हाँ, ख़ूब याद आया। तुमने मुझे उस मकान की महल सरा देखने को भेजा था। अभी देखकर आई हूँ। तुम कहते थे दीवानख़ाना बहुत अच्छा है। महल सरा भी बुरी नहीं, मेरा क्या है, मैं तो किराए के मकान में रहने की आदी हो चुकी हूँ, मगर मैंने सुना है उस मकान में कोई बला है।
ग़ालिब: क्या दुनिया में आपसे बढ़कर भी कोई बला है।
उमराव: यही तो तुम्हारी बातें मुझे पसंद नहीं, फिर छेड़खानी पर उतर आए।
ग़ालिब: मैं हूँ हंसोड़ और तू है मुक़त्ता, मेरा तेरा मेल नहीं।
उमराव: सुना है शहर में वबा फैल गई है, हैजे़ से बराबर मौतें हो रही हैं। तुम तो बाहर दोस्त अहबाब में दिल बहलाते रहते हो। मैं घर में पड़ी दहला करती हूँ।
ग़ालिब: कैसी वबा, जब एक सत्तर बरस के बुड्ढे और सत्तर बरस की बुढ़िया को न मार सके तो तुफ़ है, उस वबा पर। अच्छा, अब मैं बाहर जाता हूँ, तुम्हारे वज़ीफ़े को देर होती होगी। (मूसीक़ी)
रावी: शेफ़्ता के मकान पर मेहमान जमा हैं। मुफ़्ती सदर उद्दीन आज़ुर्दा, मौलवी फ़ज़ल हक़, मुस्तफ़ा ख़ां शेफ़्ता, उर्दू दीवान-ए-ग़ालिब का तज़्किरा कर रहे हैं।
आज़ुर्दा: मिर्ज़ा साहिब, बेदिल का रंग आपने ख़ुद ही तर्क कर दिया है। इंतिख़ाब में ऐसे अशआर सब निकाल दीजिए।
ग़ालिब: क्यों भई मुस्तफ़ा ख़ां, तुम्हारी क्या राय है। भई, तुम तो जानते हो तुम्हारी राय पर मुझे कितना एतिमाद है।
शेफ़्ता: पीर-ओ-मुर्शिद, ये आपकी मुहब्बत है कि मेरी नाचीज़ राय को इस क़दर वक़अत देते हैं। आप ख़ुद ही फ़ैसला कीजिए कि आपके रंग में पहले से तबदीली हुई है कि नहीं।
ग़ालिब: क्यों नहीं, मेरी तबीयत अगरचे इब्तिदा से नादिर ख़्यालात की जोया थी लेकिन आज़ादा रवी के सबब से ज़्यादातर उन लोगों की तक़लीद करता रहा जो सीधे रास्ते से हट गए थे। आख़िर जब उन लोगों ने जो इस राह में पेशरौ थे देखा कि मैं बावजूद इस के कि उनके हमराह चलने की क़ाबिलियत रखता हूँ और फिर भी बेराह सा भटकता फिरता हूँ, तो उनको मेरे हाल पर रहम आया और उन्होंने मुझ पर मुरब्बियाना नज़र डाली। शेख़ अली हज़ीं ने मुस्कुराकर मेरी बेराह रवी मुझको जताई। तालिब आमली और उर्फ़ी शीराज़ी की ग़ज़बआलूद निगाह ने आवारा फिरने का जो माद्दा मुझमें था, उसको फ़ना कर दिया। ज़ुहूरी ने मेरे बाज़ू पर तावीज़ और कमर पर ज़ाद-ए-राह बाँधा और नज़ीरी ने अपनी रविश-ए-ख़ास पर चलना मुझे सिखाया। अब मैंने वो रंग इख़्तियार किया है कि फ़ारसी को भी रेख़्ते पर रश्क आए।
आज़ुर्दा: मगर मिर्ज़ा साहिब, ये सच्ची बात तो है कि आप बहुत अर्से तक भटकते रहे हैं और अब भी सीधी राह पर नहीं आए हैं।
शेफ़्ता: मिर्ज़ा साहिब का ये शे’र आपने सुना है,
लाखों लगाव एक चुराना निगाह का
लाखों बनाव एक बिगड़ना इताब में
आज़ुर्दा: वाह क्या शे’र है। ये शायरी नहीं एजाज़ है, मगर मिर्ज़ा साहिब, ये तो आपका रंग नहीं, ख़ास हमारी तर्ज़ का शे’र है।
ग़ालिब: तो ऐ कि मह्व-ए-सुख़न गुस्तरान पेशीनी
मुबाश मुनकिर-ए-ग़ालिब कि दर ज़माना-ए-तस्त
फ़ज़ल हक़: मिर्ज़ा साहिब, आज़ुर्दा की राय सही है। आपको याद नहीं जब आप अकबराबाद से आए थे तो यहां के मुशायरों में आपकी मुश्किल-पसंदी पर किस क़दर तंज़-ओ-तअरीज़ होती थी। मुल्ला अब्दुलक़ादिर रामपुरी ने तो एक बेमानी शे’र आपसे मंसूब ही कर दिया था। अगर आप चाहें तो नमूने के तौर पर चंद शे’र बेदिल के रंग के रहने दें। वर्ना उर्दू दीवान में तो आपको मौजूदा रंग में ज़्यादा जलवागर होना चाहिए।
ग़ालिब: अच्छा भाई तुम और शेफ़्ता मिलकर मेरे रेख़्ते का इंतिख़ाब कर दो। फिर मैं उसे एक नज़र देख लूँगा और उसके बाद दीवान छापेखाने को दे दिया जाएगा। तुम दोनों की नुक्ता संजी और ज़ौक़-ए-सुख़न का मैं क़ाइल हूँ।
फ़ज़ल हक़: अभी नवाब साहिब ने आपका जो शे’र सुनाया था, उस ग़ज़ल के और शे’र याद हों तो सुनाइए। इस ज़मीन में मोमिन और ज़ौक़ की भी मशहूर ग़ज़लें हैं।
ग़ालिब: मेरा भी दोग़ज़ला है। मगर भाई, अब हाफ़िज़ा कमज़ोर हो गया है, चंद ही शे’र याद हैं, वो सुन लो,
मिलती है खू-ए-यार से नार इलतिहाब में
काफ़िर हूँ गर न मिलती हो राहत अज़ाब में
क़ासिद के आते आते ख़त इक और लिख रखूं
मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में
मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौर-ए-जाम
साक़ी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में
लाखों लगाव एक चुराना निगाह का
लाखों बनाव एक बिगड़ना इताब में
वो नाला-ए-दिल में ख़स के बराबर जगह न पाए
जिस नाले से शिगाफ़ पड़े आफ़ताब में
असल-ए-शुहूद-ओ-शाहिद-ओ-मशहूद एक हैं
हैरां हूँ फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में
हैं गैब गैब जिसको समझते है हम शुहूद
हैं ख़्वाब में हनूज़ जो जागे हैं ख़्वाब में
फ़ज़ल: क्या कहने हैं मिर्ज़ा साहिब, दरिया को कूज़े में बंद करना यही है।
रावी: ग़ुरूब-ए-आफ़ताब के वक़्त ग़ालिब खाना खा रहे हैं। हाली के साथ दूसरे शागिर्द भी मौजूद हैं, हाली रूमाल से मक्खियां झल रहे हैं।
ग़ालिब: आप नाहक़ तकलीफ़ फ़रमाते हैं। मैं इन कबाबों में से आपको कुछ भी न दूँगा। (हंसकर) भई आपने नवाब अब्दुल्लाह ख़ां का क़िस्सा सुना है। उनके दस्तरख़्वान पर सब के लिए हर क़िस्म के खाने होते थे। मगर ख़ास उनके लिए हमेशा एक ही चीज़ तैयार होती थी। एक दिन मुज़ाअफ़र उनके सामने आया। मुसाहिबों में से एक डोम बहुत मुँह लगा हुआ था। नवाब साहिब ने उसको खाना देने के लिए ख़ाली रकाबी मांगी। जिसके आने में कुछ देर हुई। नवाब खाते-जाते थे और ख़ाली रकाबी बार-बार मांगते थे। मुसाहिब नवाब के आगे रूमाल हिलाने लगा और कहा, “हुज़ूर और रकाबी किया कीजिएगा। अब यही ख़ाली हुई जाती है। नवाब ये फ़िक़रा सुनकर फड़क गए और वही रकाबी उसकी तरफ़ सरका दी। (थके हुए लहजे में) लो भई, अब मैं ज़रा आराम करना चाहता हूँ, पैर की टीस होश उड़ाए देती है (कराह कर) तुम लोग मेरे क़रीब आ जाओ बातें करने से तबीयत बहली रहेगी।
मजरूह: लाइए में आपके पांव दबा दूं।
ग़ालिब: भई तू सय्यद ज़ादा है, मुझे क्यों गुनहगार करता है।
मजरूह: ऐसा ही है तो मुझे कुछ उजरत दे दीजिएगा।
ग़ालिब: अच्छा यही सही।
हाली: वाह क्या ख़ुशगवार हवा है। आसमान को देखिए क्या निखरा हुआ है।
ग़ालिब: जो काम ख़ुदराई से किया जाता है, अक्सर बेढंगा होताहै। सितारों को देखिए किस अबतरी से बिखरे हुए हैं न तनासुब है न इंतज़ाम, न बेल है न बूटा। मगर बादशाह ख़ुद-मुख़्तार है कोई दम नहीं मार सकता। (हल्का क़हक़हा)
हाली: आपका एक शे’र मेरी समझ में नहीं आया।
ग़ालिब: तो क्या ताज्जुब है। मेरी ज़िंदगी भी तो तुम्हारी समझ में नहीं आई। अच्छा वो क्या शे’र है?
हाली: क़मरी कफ़-ए-ख़ाकसतर-ओ-बुलबुल क़फ़स-ए-रंग
ऐ नाला-ए-निशान-ए-जिगर सोख़्ता क्या है
ग़ालिब: अरे भाई, ऐ की जगह जुज़ पढ़ो मअनी ख़ुद समझ में आजाऐंगे।
हाली: अगर आप ऐ की जगह जुज़ का लफ़्ज़ रख देते या दूसरा मिसरा इस तरह कहते कि “ऐ नाला-ए-निशाँ तेरे सिवा इश्क़ का क्या है” तो क्या हर्ज था।
ग़ालिब: तुम ठीक कहते हो। मतलब तो वाज़ेह होजाता मगर मेरी इन्फ़िरादियत का ख़ून हो जाता। मैं शारेअ आम पर चलने से बचता हूँ। मैंने एक दफ़ा अपने मरने की तारीख़ कही थी। ग़ालिब मर्द। उसी साल शहर में वबा फैली। साल गुज़रने पर किसी ने कहा कि हज़रत आपने तो अपने मरने की तारीख़ भी कह ली थी। फिर ये क्या हुआ। मैंने उसे लिखा कि लिसान-उल-गैब की बात ग़लत नहीं हो सकती, मगर वबाए आम में मरना मेरी शान के ख़िलाफ़ था। मैं तर्ज़-ए-ख़्याल में जिद्दत और तुर्फ़गी देखता हूँ। शायरी को मअनी आफ़रीनी समझता हूँ, क़ाफ़िया-पैमाई नहीं। मैं ऐसी रिआयतों को जो हर शख़्स को सूझ जाएं मुब्तज़िल जानता हूँ। एक शख़्स ने एक दफ़ा एक शे’र की मेरे सामने बहुत तारीफ़ की। मैंने पूछा कि इरशाद तो हो वो कौन सा शे’र है, उसने मीर अमानी असद का ये शे’र सुनाया,
असद इस जफ़ा पर बुतों से वफ़ा की
मरे शेर शाबाश रहमत ख़ुदा की
मुझे उस पर बहुत ग़ुस्सा आया। बेसाख़्ता ज़बान से निकला कि हज़रत, अगर ये किसी और असद का शे’र है तो उस पर रहमत ख़ुदा की और अगर मुझ असद का शे’र है तो मुझ पर लानत ख़ुदा की। मेरे शेर और रहमत ख़ुदा की। ऐसे मुहावरे जो आमियों और सौकियों की ज़बान पर जारी हैं मेरे शे’र की शरीयत में हराम हैं। मैं तो जहां सल्ले-अला भी अपने किसी शागिर्द के यहां लिखा देखता हूँ उसे नाम-ए-ख़ुदा कर देता हूँ। मदह-ओ-सताइश की मुझे पर्वा नहीं तहसीन नाशनास का मैं क़ाइल नहीं,
न सताइश की तमन्ना न सिले की पर्वा
गर नहीं हैं मेरे अशआर मअनी न सही
अच्छा भई मीर मेह्दी अब तुम बस करो, थक गए होगे।
मजरूह: हुज़ूर मेरे पैर दाबने की उजरत।
ग़ालिब: भैया कैसी उजरत, तुमने मेरे पांव दाबे, मैंने तुम्हारे पैसे दाबे। हिसाब बराबर हुआ। (क़हक़हा)
रावी: 1860 ई.ग़दर का हंगामा फ़िरो हो चुका है, मगर दिल्ली पर हर-सू वीरानी छाई हुई है। लोग परेशान हैं, जान-ओ-माल, आबरू कुछ महफ़ूज़ नहीं। ग़ालिब ने मीर मेह्दी मजरूह को ख़त लिखा है। मजरूह अपने अहबाब को पढ़ कर सुना रहे हैं।
मजरूह: भाई क्या पूछते हो, क्या लिखूँ। दिल्ली की हस्ती मुनहसिर कई हंगामों पर है। क़िला, चाँदनी चौक, हर-रोज़ मजमा जामा मस्जिद का, हर हफ़्ते सैर जमुना के पुल की, हर साल मेला फूल वालों का, ये पांचों बातें अब नहीं। फिर कहो दिल्ली कहां। परसों मैं सवार हो कर कुओं का हाल दरयाफ़्त करने गया। मस्जिद जामे से राजघाट दरवाज़ा तक बिला मुबालग़ा एक सहरा लक़-ओ-दक़ है। ईंटों के ढेर जो पड़े हैं वो अगर उठ जाएं तो एक हू का आलम हो जाए। क़िस्सा मुख़्तसर शहर सहरा हो गया। अब जो कुँवें जाते रहे और पानी गौहर-ए-नायाब हो गया तो ये सहरा सहराए कर्बला हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, दिल्ली वाले अब तक यहां की ज़बान को अच्छा कहते हैं, वाह-रे हुस्न-ए-एतिक़ाद, बंदा-ए-ख़ुदा। उर्दू बाज़ार न रहा, उर्दू कहां, दिल्ली कहां। वल्लाह अब शहर नहीं है, कैंप है, छावनी है। न क़िला न शहर, न बाज़ार, न नहर।
मजरूह: हाय क्या था क्या हो गया।
हाली: तज़्किरा देहली-ए-मरहूम का ऐ दोस्त न छेड़, न सुना जाएगा हमसे ये फ़साना हरगिज़। ग़ालिब का आख़िरी ज़माना है, ज़ोफ़ बहुत बढ़ गया है। अक्सर पलंग पर लेटे लेटे गुज़रती है। इस वक़्त मुंशी हरगोपाल तफ्ता आए हुए हैं। उनसे बातें हो रही हैं।
ग़ालिब: मैं तो बनी आदम को मुसलमान हो या हिंदू, या नसरानी, अज़ीज़ रखता हूँ और अपना भाई गिनता हूँ। दूसरा माने या न माने। बाक़ी रही वो अज़ीज़दारी जिसको अह्ल-ए-दुनिया क़राबतदारी कहते हैं। उसको क़ौम और ज़ात और मज़हब और तरीक़त शर्त है और उसके मुरातिब-ओ-मदारिज हैं। दुनियादार नहीं हूँ, फ़क़ीर ख़ाकसार हूँ। क़लंदरी व आज़ादगी व ईसार-ओ-करम के जो दवाई मेरे ख़ालिक़ ने मुझमें भर दिए हैं बक़दर-ए-हज़ार एक भी ज़ुहूर में न आए। न वो ताक़त-ए-जिस्मानी कि लाठी हाथ में लूं और उस में शतरंजी और टीन का लोटा, सूत की रस्सी लटका लूं और पा पियादा चल दूं। कभी शीराज़ जा निकला, कभी मिस्र में जा ठेरा, कभी नजफ़ जा पहुंचा। न वो दस्तगाह कि एक आलम का मेज़बान बन जाऊं। अगर तमाम आलम में न हो सके न सही जिस शहर में रहूं उस शहर में तो नंगा भूका नज़र न आए।
तफ्ता: हुज़ूर वो मेरी ग़ज़ल पर अब तक इस्लाह न हुई। मैं चाहता था कि तीसरा दीवान जल्द मुरत्तब कर लेता।
ग़ालिब: मिर्ज़ा तफ्ता, तुम मश्क़-ए-सुख़न कर रहे हो और मैं मश्क़-ए-फ़ना में मुसतग़रिक़ हूँ। बूअली सेना के इल्म और नज़ीरी के शे’र को ज़ाए और बेफ़ायदा और मौहूम समझता हूँ। ज़ीस्त बसर करने को थोड़ी सी राहत दरकार है। बाक़ी हिक्मत और सलतनत और शायरी और साहिरी सब बेकार है। हिंदुओं में अगर कोई अवतार हुआ तो क्या और मुसलमानों में नबी बना तो क्या। दुनिया में नाम आवर हुए तो क्या और गुमनाम रहे तो क्या। कुछ मआश हो कुछ सेहत जिस्मानी, बाक़ी सब वहम है ए यार जानी। अच्छा भाई अब मैं थक गया।
रावी: ग़ालिब बिस्तर-ए-मर्ग पर हैं। बड़ी देर के बाद होश आया है, हाली और दूसरे अहबाब पास बैठे हैं। ग़ालिब एलाई के ख़त का जवाब लिखवा रहे हैं।
(नहीफ़ आवाज़ में और ठेर ठेर कर) जान-ए-ग़ालिब, तुम मेरा हाल क्या पूछते हो। दो-चार दिन में हमसायों से पूछना, हाय, हाय,
दम-ए-वापसीं बरसर-ए-राह है
अज़ीज़ो अब अल्लाह ही अल्लाह है
(हुज़्निया मूसीक़ी आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाती है)
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.