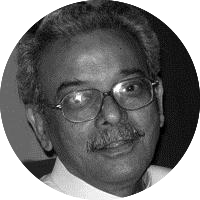कुछ उर्दू रस्म-उल-ख़त के बारे में
ये हमारी ज़बान की बद-नसीबी ही कही जाएगी कि इसका रस्म-उल-ख़त बदलने की तज्वीज़ें बार-बार उठती हैं, गोया रस्म-उल-ख़त न हुआ, ऐसा दाग़-ए-बदनामी हुआ कि इससे जल्द-अज़-जल्द छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी हो। कभी इसके लिए रोमन रस्म-ए-ख़त तजवीज़ होता है, कभी देवनागरी और अफ़सोस की बात ये है कि रस्म-ए-ख़त में तब्दीली की बात कहने वाले अक्सर ख़ुद अहल-ए-उर्दू ही होते हैं।
जब से अंग्रेज़ बहादुर की निगाह-ए-करम इस बात पर पड़ी, इसके दोस्त-नुमा दुश्मनों की ता'दाद बढ़ती ही गई है। अंग्रेज़ों ने पहले तो इसका नाम “हिन्दी” से बदल कर “हिन्दुस्तानी” रखना चाहा। जब वो न चला तो उनकी ख़ुश-क़िस्मती से लफ़्ज़ “उर्दू” उनके हाथ आ गया। अस्ल हक़ीक़त तो ये है कि अठारवीं सदी के अवाख़िर तक “ज़बान-ए-उर्दू-ए-मुअ'ल्ला” का ख़िताब फ़ारसी के लिए आ'म था और लफ़्ज़ “उर्दू” के मअ'नी थे “शाहजहाँबाद का शहर” या “क़िला-ए-मुअ'ल्ला शाहजहाँबाद।” जब दिल्ली (या'नी उर्दू ब-मअ'नी “दिल्ली शहर”) में हिन्दी (या'नी आज के मअ'नी में उर्दू) ज़बान आ'म हुई तो इसको (या'नी ''हिन्दी” को) “ज़बान उर्दू-ए-मुअ'ल्ला” कहा जाने लगा। फिर मुख़्तसर होते होते ये फ़िक़रा “ज़बान उर्दू“, या “उर्दू की ज़बान” और फिर सिर्फ़ “उर्दू” रह गया।
अंग्रेज़ों को भी ये बात मुवाफ़िक़ आती थी, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदुओं की कोई अलग ज़बान हो और वो “हिन्दी” कहलाए। लिहाज़ा उन्होंने “हिन्दी” का नाम हमारी ज़बान से छीन कर एक नई ज़बान को दे दिया, और हमारी ज़बान का नाम सिर्फ़ “उर्दू” रह गया। या'नी अंग्रेज़ों की मेहरबानी से हमारी ज़बान सारे हिन्दुस्तान की ज़बान के बजाए “उर्दू” या'नी “लश्कर बाज़ार” या “शाही कैंप और दरबार” की ज़बान ठहरी।
अंग्रेज़ों ने दूसरा सितम ये किया कि उन्होंने लफ़्ज़-ए-“उर्दू” के मअ'नी “लश्कर बाज़ार”, “शाही कैंप और दरबार” नहीं, बल्कि “फ़ौज, लश्कर” बयान किए। आहिस्ता-आहिस्ता ये बात इतनी मक़बूल हुई कि सब उर्दू वाले भी यही समझने लगे कि हमारी ज़बान दर-अस्ल एक फ़ौजी और लश्करी ज़बान है। अभी हाल ही में “हमारी ज़बान” में एक नज़्म छपी है जिसमें ये बात कम-ओ-बेश फ़ख़्रिया कही गई है कि उर्दू “लश्करी” ज़बान है।
अहसन मारहरवी ने 1910 में एक तवील नज़्म “उर्दू लश्कर” के नाम से लिखी और तबा’ कराई थी। मैंने उसका एक नुस्ख़ा निज़ामी बुक एजेंसी बदायूँ के यहाँ से बड़े इश्तियाक़ से मँगवाया कि देखें, आज से कोई सौ बरस पहले अहसन मारहरवी ने उर्दू ज़बान के नाम के बारे में शायद कोई दिलचस्प बात कही हो, या शायद ये बताना चाहा हो कि उर्दू दर-अस्ल “लश्करी” ज़बान नहीं है।
मुझे ये देखकर मायूसी हुई कि इस नज़्म में वही आ'म बात दुहराई गई है कि इस ज़बान की पैदाइश और तरक़्क़ी मुसलमानों के ज़माने में और उनकी फ़ौज वग़ैरह में हुई। लफ़्ज़ “उर्दू” के ग़लत लेकिन मक़बूल मअ'नी “लश्कर” की मुनासिबत से अहसन मरहूम ने अपनी नज़्म का नाम “उर्दू लश्कर” रख दिया, और वली दकनी से लेकर अपने ज़माने तक के बड़े अदीबों को “उर्दू लश्कर के सरदार” क़रार दिया।
इब्तिदा इसकी हुई है उस ज़माने में यहाँ
जब मुसलमानों का था हिंदुस्ताँ में ख़ूब राज
गो अदालत की ज़बाँ उर्दू न थी फिर भी बहुत
फ़ौज में बाज़ार में चलता था इससे काम काज
इस पर तुर्रा ये कि उर्दू को अंग्रेज़ों का एहसान-मंद ठहराया गया है। अहसन मारहरवी कहते हैं,
है गर्वनमैंट अपनी आ'दिल हमको है उससे उमीद
वो हमारे हाल पर फ़रमाएगी बे-शक करम
की हिमायत जिस क़दर उर्दू ज़बाँ की आज तक
वो नहीं कुछ कम जो आसानी से हो जाए रक़म
अ'द्ल पर इस सल्तनत के नाज़ करना चाहिए
ऐसे आ'दिल ऐसे मुंसिफ़ थे न कस्रा और जम
ऐसी सूरत में अगर गिलक्राइस्ट (Dr. John Gilchrist) को उर्दू का मोहसिन-ए-आ'ज़म क़रार दिया गया तो कुछ तअ'ज्जुब की बात नहीं। आपने कभी ग़ौर किया कि अगर हमारी ज़बान का अस्ल नाम, या'नी “हिन्दी” बर-क़रार रखा जाता तो ये अफ़साना घड़ना और राइज करना मुम्किन न था कि ये लश्करी ज़बान है।
भला कौन था जो तस्लीम करता कि जिस ज़बान का नाम “हिन्दी” हो, उसे लश्करियों और फ़ौजियों ने राइज किया था? मीर अम्मन ने जब “बाग़-ओ-बहार” में “उर्दू” (या'नी दिल्ली की ज़बान) की “तारीख़” अपने लफ़्ज़ों में बयान की तो उन्होंने सबसे बड़ी ना-इंसाफ़ी इस ज़बान के साथ ये की कि उन्होंने ये कहीं कहा ही नहीं कि ये ज़बान (जिसे वो “उर्दू” की ज़बान कह रहे हैं) दर-अस्ल “हिन्दी” के नाम से जानी जाती है। उन्होंने ये तो कहा कि इस ज़बान को “उर्दू” (या'नी दिल्ली) के सारे लोग बोलते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या औरतें, क्या मर्द, क्या बच्चे क्या बूढ़े, लेकिन उन्होंने ये बताने से गुरेज़ किया कि इस ज़बान का नाम “हिन्दी” है। जब ‘मीर’ कहते हैं,
क्या जाने लोग कहते हैं किसको सुरूर-ए-क़ल्ब
आया नहीं ये लफ़्ज़ तो हिन्दी ज़बाँ के बीच
तो उनकी मुराद जयशंकर प्रशाद और रामचन्द्र शुक्ल की हिन्दी से न थी, और न टी.वी. और आकाशवाणी की हिन्दी से थी। लफ़्ज़ “हिन्दी” से ‘मीर’ वही ज़बान मुराद ले रहे थे जिसमें वो शे'र कहते थे और जिसे हम आज “उर्दू” कहते हैं।
जब हमारी ज़बान का नाम “हिन्दी” से “उर्दू” बना दिया गया तो अंग्रेज़ों और अंग्रेज़ों के हिमायती “क़ौम-परस्त” हिंदुओं की तवज्जोह रस्म-ए-ख़त पर ज़ियादा ज़ोर-ओ-शोर से हुई। सब जानते हैं कि अपनी ख़ूबसूरती, कम जगह में ज़ियादा अल्फ़ाज़ खपा देने की सलाहियत, फ़नकाराना तनव्वो’ के इम्कानात और फ़ारसी, अ'रबी, संस्कृत से इसके रब्त के सबब से उर्दू का रस्म-उल-ख़त हिन्दुस्तानी तहज़ीब की शानों में एक शान है और उर्दू के मख़्सूस हालात को मद्द-ए-नज़र रखें तो इसे उर्दू ज़बान की जान कहा जा सकता है।
या'नी मौजूदा हालात में उर्दू का रस्म-उल-ख़त बदलने की तजवीज़ दर-हक़ीक़त उर्दू को मौत के घाट उतारने की तजवीज़ है। रंज की बात ये है कि उर्दू के मुख़ालिफ़ीन, और दोस्त-नुमा दुश्मन, मुद्दत-ए-दराज़ से इसके रस्म-उल-ख़त को अपनी दुश्मनी का हदफ़ बनाए हुए हैं।
उर्दू का रस्म-उल-ख़त बदल कर उसे रोमन में लिखने की तजवीज़ सबसे पहले हज़रत गिलक्राइस्ट (Gilchrist) ने रखी थी। अफ़सोस है कि हम में से अक्सर अब भी गिलक्राइस्ट को उर्दू ज़बान के मोहसिनीन में शुमार करते हैं, जब कि हक़ीक़त बर-अ'क्स है।
अपनी किताब The Oriental Fabulist मतबूआ’ 1803 में गिलक्राइस्ट ने ब-ख़याल ख़ुद ये “साबित” किया था कि उर्दू ही नहीं, बल्कि और भी कई हिन्दुस्तानी ज़बानों को रोमन रस्म-ए-ख़त में “आसानी और सेहत के साथ” लिखा जा सकता है।
इस मुआ'मले पर थोड़ी सी बहस मरहूम अतीक़ सिद्दीक़ी ने अपनी किताब Origins of Modern Hindustani Literature मतबूआ’ अ'लीगढ़ १९६३ में पेश की है। लेकिन गिलक्राइस्ट की तजवीज़ में जो सामराजी तकब्बुर और हाकिमाना तंग-नज़री पिन्हाँ है, उसकी तरफ़ अतीक़ सिद्दीक़ी ने ए'तिना नहीं किया। इस तजवीज़ पर ए'तिराज़ के बजाए सिद्दीक़ी मरहूम ने इसे “हिन्दुस्तान को मुत्तहिद करने की काबिल-ए-ता'रीफ़ कोशिश” का नाम दिया है।
गिलक्राइस्ट की बात पर उस वक़्त शायद ज़ियादा तवज्जोह न दी गई लेकिन जब अंग्रेज़ों के ज़ेर-ए-असर उर्दू और “हिन्दी” की तफ़रीक़ क़ाएम होने लगी और “हिन्दी” ज़बान को हिंदुओं के “क़ौमी तशख़्ख़ुस” की पहचान बनाया जाने लगा, तो मुल्क के एक तबक़े ने, जो अनजाने में अंग्रेज़ी सामराज का शिकार बन चुका था, उर्दू की मुख़ालिफ़त को भी “हिन्दी” के क़याम के लिए ज़रूरी जाना।
उर्दू की मुख़ालिफ़त जिन बुनियादों पर की जाने लगी, उनमें एक ये भी थी कि उर्दू का रस्म-ए-ख़त “नाक़िस है” या/और ग़ैर-मुल्की है। चुनाँचे राजिंदर लाल मित्रा ने 1864 में एक मज़्मून ब-ज़बान-ए-अंग्रेज़ी लिखा और अपने तईं साबित किया कि नागरी रस्म-उल-ख़त को उर्दू रस्म-उल-ख़त पर फ़ौक़ियत है।
उस ज़माने में उर्दू रस्म-ए-ख़त को रोमन कर देने की बात इतने ज़ोर शोर से उठाई जा रही थी कि गारसाँ द तासी ने ख़दशा ज़ाहिर किया कि कहीं सियासी मस्लेहत और दबाव के तहत अंग्रेज़ लोग उर्दू का रस्म-ए-ख़त रोमन कर ही न डालें। द तासी ने लिखा कि ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। इस मुआ'मले की तफ़्सील के लिए फ़रमान फ़त्हपूरी की किताब “उर्दू इमला और रस्म-उल-ख़त” मतबूआ’ इस्लामाबा'द मुलाहिज़ा हो।
राजिंदर लाल मित्रा ने अपने ज़माने के “हिंदू क़ौम-परस्त” हल्क़ों पर गहरा असर डाला था। भारतेंदु हरीशचंद्र से भी उनके मरासिम थे। कुछ अ'जब नहीं कि अगर भारतेंदु को उर्दू से नागरी रस्म-ए-ख़त वाली “हिन्दी” की तरफ़ राग़िब करने में “हिंदू क़ौम-परस्त” हल्क़ों का हाथ था, तो उन्हें उर्दू से मुतनफ़्फ़िर करने और उसके रस्म-उल-ख़त में कीड़े निकालने की तरफ़ राजिंदर लाल मित्रा ने मेहमेज़ किया हो।
वर्ना कोई वज्ह नहीं कि वही भारतेंदु हरीशचंद्र जिन्होंने 1871 में लिखा था कि मेरी और मेरे घराने की औरतों की ज़बान उर्दू है, दस साल बा'द एजूकेशन कमीशन के सामने ये कहते हुए पाए जाएँ कि उर्दू रस्म-उल-ख़त एक तरह से मुसलमानों की साज़िश है, कि इसमें “लिखिए कुछ और पढ़िए कुछ” की आसानी है। इस तरह आ'म सादा-लौह रिआ'या को धोका देने के लिए ये रस्म-ए-ख़त निहायत मौज़ूँ है।
इन मुआ'मलात की तफ़्सील के लिए वसूधा डालमिया की किताब मुलाहिज़ा हो जो 1997 में दिल्ली ऑक्सफ़ोर्ड यूनीवर्सिटी प्रैस से शाया’ हुई है। The Nationalization of Hindu Tradition Bharatendu Hirishchandra and Nineteenth Century Banaras इसके अ'लावा सागरी सेन गुप्ता की पी.एच.डी. थीसिस भी देखी जा सकती है। इसके अज्ज़ा Annual of Urdu Studies No.91 में शाया’ हुए हैं।
लुत्फ़ की बात ये है कि उर्दू पर “लिखें कुछ, पढ़ें कुछ” का इल्ज़ाम धरने वाले ये भूल जाते हैं कि ख़ुद देवनागरी इस ऐ'ब से ख़ाली नहीं। (अगर ये ऐ'ब है) अंग्रेज़ी वग़ैरह का तो पूछना क्या है, कि जहाँ मा'मूली आवाज़ों, मसलन च, श, फ़, वग़ैरह को बयान करने के आठ-आठ नौ-नौ तरीक़े हो सकते हैं। देवनागरी का हाल ये है कि यहाँ ख (Kha) और र-व (ra va) मैं कोई फ़र्क़ नहीं।
“रवाना” लिखिए और “खाना” पढ़िए। ध (dha) और घ (gha) में इतना कम फ़र्क़ है कि ज़रा सी लर्ज़िश-ए-क़लम से घर की जगह “धर”, “धान” की जगह “घान” हो जाता है। थ (tha) और य (ya) में भी इसी क़दर कम फ़र्क़ है कि “थान” को “यान” पढ़ लेने का पूरा पूरा इम्कान है। नून-ग़ुन्ना लिखने के लिए तरह-तरह के पापड़ बेले जाते हैं। इस एक ही आवाज़ को तीन-चार तरह लिखा जाता है। “चन्द्र बिंदू” कुछ है, “ङ” और तरह से है, सिर्फ़ “बिंदी” और तरह की है, और कहीं आधा ma (म) लगा देते हैं। इस रंग के उलझावे और भी हैं, लेकिन मिसाल के लिए इतने काफ़ी होंगे। फिर इस दा'वे के क्या मअ'नी कि देवनागरी में ग़लत पढ़ने की गुंजाइश नहीं।
खड़ी बोली के मुतअद्दिद अल्फ़ाज़ देवनागरी में लिखे ही नहीं जा सकते, मसलन मुंदरजा-ज़ेल अल्फ़ाज़ की लिखाई से देवनागरी क़ासिर है, कव्वा, लिए, गाँव, ड्योढा, बहन, किवाड़, कोई, ब-वज़्न-ए-फ़अ'ल (वतद-मजमूअ’) या ब-वज़्न-ए-फ़अ'ल (सबब-ए-सकील) वग़ैरह।
इसी तरह ये भी है कि अनगिनत अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जिनमें वस्ती या आख़िरी हर्फ़ साकिन है लेकिन देवनागरी उन्हें मुतहर्रिक लिखने पर मजबूर है। चुनाँचे, चलना (chalana), फ़ासला (fasala), चिकना (Chikana), घास (ghasa), जनता (janata) वग़ैरह लिखना और चलना, रास्ता, चिकना, घास, जनता वग़ैरह में मुतहर्रिक लिखे हुए हर्फ़ (लाम, स/स, काफ़, स, नून) को साकिन पढ़ना पड़ता है जो नागरी रस्म-ए-तहरीर की रूह के ख़िलाफ़ है।
मुंदरजा-बाला मिसालों से ये भी साबित होता है कि खड़ी बोली (या'नी उर्दू) और नागरी रस्म-ए-ख़त में कोई मुनासिबत नहीं। खड़ी बोली जो बा'द में उर्दू-हिन्दी या'नी उर्दू कहलाई, वो नागरी में लिखी जाने का तक़ाज़ा ही नहीं करती। देवनागरी रस्म-उल-ख़त और खड़ी बोली में बाहम मुनासिबत होती तो ये मुश्किलात भी न होतीं और ये अ'दम मुनासिबत न होती।
आ'म उर्दू वालों ने रस्म-ए-ख़त की तब्दीली या इमले में “इस्लाह” की तजावीज़ को कभी लाएक़-ए-तवज्जोह न जाना। ये उनकी सलामती-तबा’ की दलील है। लेकिन उर्दू के बा'ज़ “ख़ैर-ख़्वाह” हज़रात को ख़्वाह-मख़ाह ही कुरेद लगी रहती है कि इस बे-चारी ग़रीब की जोरू को अपनी भावज बनाकर छेड़ते रहें। आज़ादी के फ़ौरन बा'द तरक़्क़ी-पसंद हल्क़ों से आवाज़ उठाई गई कि इस ज़बान को ज़िंदा रहना है तो इसे अपना रस्म-उल-ख़त बदल कर देवनागरी कर लेना चाहिए।
जब इस बात पर किसी ने कान न धरे तो आज़ादी के दो दहाई बा'द फिर बा'ज़ लोगों ने, जिनमें कुछ बहुत बड़े तरक़्क़ी-पसंद नाम भी इन्फ़िरादी तौर पर शामिल थे, यही ना'रा बुलंद किया। इस बार एहतिशाम साहब जैसे जय्यद मुफ़क्किर और साइब-उल-राय तरक़्क़ी-पसंद अदीब ने भी इस आवाज़ को सख़्ती से दबा देने का मशवरा दिया लेकिन उर्दू की बेचारगी उसके “दोस्तों” को ऐसी दिलकश लगती है कि वो उसे बार-बार रुस्वा करने पर आमादा रहते हैं। उनकी देखा देखी सियासी लोगों को शौक़ चराता है कि उर्दू की “इस्लाह” फ़रमाने वालों में अपना भी नाम लिखवा लें।
चुनाँचे आज एक तरफ़ तो हमारे कुछ बहुत बड़े अदीब किसी न किसी उ'नवान से उर्दू के रस्म-उल-ख़त में तब्दीली लाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ़ मौलाना मुलाइम सिंह भी उर्दू वालों से कहते हैं कि रस्म-उल-ख़त बदल डालो, फ़ाएदे में रहोगे। (यही बात मोरारी-जी देसाई भी कहते थे) फ़ाएदा क्या होगा, उसका हिसाब तो आसान है, कि बहुत ही कम फ़ाएदा होगा। लेकिन नुक़्सान कितना होगा, उसका हिसाब ना-मुम्किन है, क्योंकि रस्म-उल-ख़त की तब्दीली किसी भी ज़बान के लिए ख़ुसरान-ए-अ'ज़ीम का बाइ'स होती है। उर्दू जैसी बत्तीस दाँतों में दबी हुई एक ज़बान बेचारी का तो पूछना ही कुछ नहीं कि रस्म-ए-ख़त खो कर वो किस क़दर मज़ल्लत में गिर जाएगी।
अहल-ए-उर्दू बराह-ए-करम अपने तारीख़ी सरमाये पर नज़र डालें, अंग्रेज़ों की सियासत को ख़याल में लाएँ। उर्दू के रस्म-ए-ख़त में तब्दीली की हर सिफ़ारिश के डांडे अंग्रेज़ों की उन साज़िशों से मिलते हैं जो उन्होंने उर्दू/हिन्दी का झगड़ा पैदा करके इस मुल्क के हिंदू-मुसलमान में तफ़र्रुक़ा डालने की ग़रज़ से रची थीं।
गिलक्राइस्ट ने अपनी किताब The Oriental Linguist मतबूआ’ 1802 (अव्वल ऐडिशन 1798) में लिखा है कि मैं जिस ज़बान (या'नी उर्दू) को “हिन्दुस्तानी” का नाम देना चाहता हूँ, उसका अस्ल नाम तो “हिन्दी” या “हिंदवी” है, लेकिन इससे हमारा ख़याल हिंदुओं की तरफ़ मुंतक़िल होता है। “हिन्दी/हिंदवी” वो ज़बान है जो हिन्दुस्तान में मुसलमानों के “हमलों” के पहले बोली जाती थी। [बहुत ख़ूब, इसी तहक़ीक़ के बलबूते पर हम अहल-ए-उर्दू मिस्टर गिलक्राइस्ट को अल्सिना-ए-हिंद का माहिर गरदानते हैं बहर-हाल आगे सुनिए]
गिलक्राइस्ट ने मज़ीद फ़रमाया कि ये बात तो है कि इस (या'नी जिस ज़बान का नाम मैं “हिन्दुस्तानी” रखना चाहता हूँ) ज़बान के बोलने वाले उसे “हिन्दी/हिंदवी” ही कहते हैं, लेकिन उससे क्या होता है? हिन्दुस्तानी बे-वक़ूफ़ लोग हैं, उन्हें इन बारीकियों की तरफ़ मुतवज्जह भी किया जाए तो वो ख़ाक न समझेंगे। ये नाम (“हिन्दी“) तो हिंदुओं की ज़बान का होना चाहिए। रफ़्ता-रफ़्ता “हिन्दी” का वो रूप भी नुमूदार होगा जिसमें संस्कृत और दीगर “हिन्दुस्तानी” अ'नासिर की कसरत होगी। मुसलमान “हिन्दुस्तानी” को, और हिंदू लोग “हिन्दी” को इख़्तियार कर लेंगे। ये दो तर्ज़ इस मुल्क में मक़बूल हो जाएँगे।
मुंदरजा-बाला बयानात की लग़्वियत की तरफ़ आपको मुतवज्जह करने की ज़रूरत नहीं। अफ़सोस इस बात का है कि इन बातों की तरदीद करने के बजाए ख़ुद हमने भी अपनी ही ज़बान की बुराइयाँ शुरू’ कर दीं। लेकिन एक बात यहाँ ज़रूर ज़हन-नशीन कर लेनी चाहिए।
गिलक्राइस्ट की बातों से साफ़ ज़ाहिर है कि उर्दू वालों ने कभी नहीं चाहा था कि वो फ़ारसी अ'रबी से भरी हुई ज़बान लिखें। बल्कि “हिन्दी” वालों को समझाया गया कि तुम संस्कृत भरी ज़बान लिखो। इस सिलसिले में डाक्टर ताराचंद की किताब The Problem of Hindustani (मतबूआ’ इलाहाबाद) का मुताला’ सूदमंद होगा।
अंग्रेज़ों की ख़ुशामद के बा-वजूद अहसन मारहरवी को क़ौमी यक-जहती का इस क़दर पास है कि उन्होंने अपनी तवील नज़्म “उर्दू लश्कर” (जिसका ज़िक्र ऊपर हुआ) में फ़ारसी अ'रबी लफ़्ज़ों को मा’-अत्फ़-ओ-इज़ाफ़त लिखने से गुरेज़ किया है और इंशा तो बहुत पहले “रानी केतकी की कहानी” लिख कर साबित कर चुके थे कि फ़ारसी अ'रबी अल्फ़ाज़ को बरते बग़ैर भी उर्दू लिखी जा सकती है। (और लुत्फ़ ये है कि आज हिन्दी वाले इस किताब को अपनी नस्र के शाहकारों में गिनते हैं।) अंग्रेज़ों की सियासत किस-किस तरह उर्दू ज़बान और इसके बोलने वालों पर कारगर हुई, उसको समझने के लिए आलोक राय की किताब Hindi Natioanalism मतबूआ’ Longmansसन 2001 मुलाहिज़ा हो। आलोक राय साहब फ़र्ज़ंद हैं अमृत राय के, लेकिन उन्होंने इस किताब में अमृत राय की बदनाम-ए-ज़माना किताब A House Divided के बयानात की क़लई’ खोल दी है।
उधर कुछ दिनों से वलाएत में रहने वाले बा'ज़ अहल-ए-उर्दू की तरफ़ से आवाज़ उठी है कि उर्दू का रस्म-ए-ख़त रोमन कर दिया जाए। वज्ह ये बयान की गई है कि इंग्लिस्तान में रहने वाले अहल-ए-उर्दू के बच्चे उर्दू बोल तो सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। लिहाज़ा अगर उर्दू का रस्म-उल-ख़त रोमन कर दिया जाए तो वो ब-ख़ूबी उर्दू पढ़ और लिख भी सकेंगे। मुम्किन है ये तजवीज़ किसी एक फ़र्द-ए-वाहिद को, या किसी गिरोह को अच्छी मा'लूम होती हो, लेकिन इसके पस-ए-पुश्त दर-अस्ल सहल-अंगारी और काहिली है, कि हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने की ज़हमत काहे मोल लें, क्यों न उर्दू को अंग्रेज़ी कर दें, हर्रे लगेगी न फिटकरी और रंग (उनके ख़याल में) चोखा आएगा।
मैं जानना चाहता हूँ कि अगर यूरोप और अमरीका के सैकड़ों मक़ामात में फैले हुए लेकिन मुट्ठी भर यहूदी अपनी ज़बान Yiddish को इतना फ़रोग़ दे सकते हैं कि उसमें बड़े-बड़े अदीब पैदा हों, और हर यहूदी, वो चाहे जहाँ भी रहता हो, यिडिश पढ़ और लिख लेता हो, तो उर्दू वाले जो सिर्फ़ इंग्लिस्तान में लाखों की ता'दाद में हैं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते।
जब बनारस और इलाहाबाद के बंगाली यहाँ चार सौ बरस से रहते रहने के बा-वजूद उर्दू के मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद-जमा’ में अब भी ग़लती करते हैं, क्योंकि बंगाली में मुज़क्कर-मुअन्नस नहीं है, और उर्दू के वाहिद-जमा’ के क़ाएदे बंगाली में नहीं चलते, तो उर्दू के लोग चंद ही बरसों में अपनी ज़बान से इतने दूर क्यों हो जाते हैं कि उन्हें इसे लिखना या पढ़ना दुशवार हो जाता है? फिर इलाहाबाद में तो मुतअद्दिद ऐसे बंगालियों से भी मेरी मुलाक़ात है जो उर्दू और बंगाली में मुकम्मल तौर पर ज़ू-लिसान हैं।
मुम्किन है वो उर्दू पढ़ न सकते हों, लेकिन उनका शीन क़ाफ़ उतना ही दुरुस्त है जितना किसी उर्दू वाले का हो सकता है और आपस में वो इस धड़ल्ले से बंगाली में बातचीत करते हैं कि हम लोग मुँह देखते रह जाते हैं। जो क़ौमें अपनी ज़बान और तहज़ीब पर इफ़्तिख़ार रखती हैं उनके यही तौर होते हैं। न मा'लूम हम लोग अपनी ज़बान के बारे में इस क़दर मुदाफ़आ'ना और ए'तिज़ारी रवैया क्यों अपनाए बैठे हैं।
ख़ैर, अब इन बातों से क़त’-ए-नज़र मुझे ये अ'र्ज़ करना है कि उर्दू का रस्म-उल-ख़त रोमन कर देने में कई तरह के नुक़्सानात-ए-अ'ज़ीम हैं। उनमें से चंद हस्ब-ए-ज़ेल हैं,
(1) उर्दू का रस्म-उल-ख़त बदलना उर्दू ज़बान और अदब दोनों के लिए नुक़्सान-देह है। बदला हुआ रस्म-ए-ख़त ख़्वाह रोमन हो या नागरी, इससे उर्दू ज़बान और अदब दोनों को ऐसा धक्का पहुँचेगा कि मुम्किन है कि वो जाँ-बर ही न हो सकें। वो गिराँ क़द्र अदबी सरमाया जो गुज़िश्ता पाँच छः सौ बरस से उर्दू के अपने रस्म-ए-ख़त में लिखा गया है, तक़रीबन सारे का सारा ज़ाए’ हो जाएगा।
हम अपने क्लासिकी मुतून, और क्लासिकी ही क्यों, गुज़िश्ता पाँच दहाई के बड़े मुतून के भी अच्छे ऐडिशनों के मुआ'मले में बहुत मुफ़लिस हैं। जो तहज़ीब और मुआ'शरा अपने बड़े अदीबों के अहम-तरीन मुतून को भी बाज़ार में दस्तयाब नहीं रखता, उससे तवक़्क़ो’ करना फ़ुज़ूल और ख़ाम-ख़याली है कि वो अपने सारे गुज़िश्ता सरमाये को नए रस्म-उल-ख़त में मुंतक़िल करके उसे आ'म और मुतदावल करेगा।
रस्म-उल-ख़त बदला गया तो दस बरस भी न गुज़़रेंगे कि ज़बान और अदब दोनों पर ख़ाक उड़ने लगेगी और उर्दू के दुश्मन दिल-ओ-जान से यही चाहते हैं। इस वक़्त तो ये आ'लम है कि न ‘मीर’ का कोई मो'तबर कुल्लियात बाज़ार में मिलता है, न ‘मीर’ अनीस का, न नुसरती या बाक़र आगाह का।
प्रेमचंद, नज़ीर अहमद, मंटो, राशिदुल-ख़ैरि, हसन निज़ामी, बेदी, अमजद हैदराबादी वग़ैरह का तो पूछना ही क्या है। लेकिन इनके पुराने ऐडिशन मौजूद हैं और पढ़ने वाले उन्हें पढ़ भी सकते हैं। जब उर्दू का रस्म-ए-ख़त रोमन या नागरी हो जाएगा तो आहिस्ता-आहिस्ता इनके पढ़ने वाले अ'न्क़ा हो जाएँगे। कुछ दिन बा'द उर्दू का पुराना सरमाया उर्दू में पढ़ने वाला कोई न होगा, हत्ता कि ये पुराने, गले-सड़े ऐडिशन भी कुछ लाइब्रेरियों और कुछ कबाड़ियों के अ'लावा कहीं और न मिलेंगे और रोमन या नागरी में ये मुतून दस्तयाब होंगे नहीं। फिर नतीजा ज़ाहिर है।
(2) फ़र्ज़ किया कोई सूरत ऐसी निकल आती है कि उर्दू का सारा अदब न सही, सारा आ'ला अदब पहले रोमन या नागरी में मुंतक़िल कर लिया जाए, फिर रस्म-उल-ख़त बदला जाए। अव्वल तो ये मुम्किन नहीं। इस काम के लिए रुपया ही इतना दरकार होगा कि एक पूरी हुकूमत का ख़र्च इससे चल जाएगा। लेकिन मान लिया ये मुम्किन हुआ भी तो हम जिस रस्म-ए-ख़त को इख़्तियार करेंगे, उसके अपने मसाइल हमारे सामने आएँगे और उनका अब तक कोई हल नहीं बहम हो सका है।
दूसरी मुश्किल ये होगी कि जब उर्दू रस्म-ए-ख़त ही में ऐसे ऐडिशन नहीं मिलते जिनको पूरी तरह सही नहीं तो कम-ओ-बेश लाएक़-ए-ए'तिमाद कहा जा सके, तो उर्दू से नागरी या रोमन में मुंतक़िल करने के लिए किस ऐडिशन को मो'तबर माना जाएगा? और बहुत सी अहम किताबें या अहम शो'रा के कुल्लियात तो अभी तबाअ'त-पज़ीर भी नहीं हुए। उनके किस नुस्खे़ को बुनियादी मत्न क़रार दिया जाए, और क्यों?
(3) रस्म-उल-ख़त बदलने से पहले सबसे बड़ा सवाल ये तय होना चाहिए कि नए रस्म-उल-ख़त में उर्दू अल्फ़ाज़ का महज़ तलफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर किया जाएगा, या इमला भी ज़ाहिर किया जाएगा? अगर सिर्फ़ तलफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर किया जाएगा तो नए रस्म-उल-ख़त में उर्दू के बहुत से हुरूफ़-ए-तहज्जी बाक़ी न रहेंगे। मसलन स(س), स(ص ), सबको एक ही अ'लामत के ज़रीए’ ज़ाहिर किया जाएगा। इसी तरह ऐ'न और अलिफ़ में एक क़ाएम रखा जाएगा, एक तर्क होगा।
(4) जिन लोगों ने ये तजवीज़ पेश की है कि उर्दू का रस्म-उल-ख़त रोमन कर दिया जाए, उनसे दरख़्वास्त है कि इस तजवीज़ में मुज़म्मिर ख़राबियों और इस पर अ'मल दर-आमद होने के ख़ास नुक़्सानात को ध्यान में कब लाएँगे। उनमें से बा'ज़ हस्ब-ए-ज़ेल हैं,
(5) उर्दू को रोमन रस्म-उल-ख़त में लिखने के लिए कोई ऐसा निज़ाम अभी तक नहीं है जिसे सब क़ुबूल करते हों। बहुत से लोग मन-मानी करते हैं, बहुत से लोग Library of Congress के निज़ाम पर अ'मल करते हैं। बहुत से लोग Library of Congress के निज़ाम में थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ करके उसे बरतते हैं। बहुत से लोग कम-ओ-बेश वो निज़ाम इस्ति'माल करते हैं जो अ'रबी से रोमन करने के लिए मुतदावल है। बहुत से लोग कोई और निज़ाम ब-कार लाते हैं। मिसाल के तौर पर, ख लिखने के लिए हस्ब-ए-ज़ेल मुख़्तलिफ़ तरीक़े मुस्ता'मल हैं,
छोटा ऐक्स (small x)
छोटा के और छोटा ऐच (kh)
छोटा के और छोटा ऐच, लेकिन दोनों हर्फ़ों के नीचे लकीर(kh)
बड़ा के (K)
लिहाज़ा सवाल ये है कि जब मुख़्तलिफ़ लोग एक ही हर्फ़ को रोमन रस्म-ए-ख़त में मुख़्तलिफ़ तरह अदा करेंगे, कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ तो बच्चे की ता'लीम किस तरह होगी? या फिर ये होगा कि कम-ओ-बेश हर घर में रोमन उर्दू अपनी ही तर्ज़ की होगी। किसी का किसी से मेल न होगा और इसका इम्कान ज़ियादा है कि हर बा-असर तब्क़ा अपने तौर पर अपने क़ाएदे इख़्तियार करेगा।
जिस ज़बान के बोलने वाले अभी तक इस बात पर मुत्तफ़िक़ न हो सके कि “दा'वा” (دعویٰ) लिखें या “दा'वा“ (دعوا ), “गुज़र” (گزر) लिखें या “गुज़र” (گذر), “तोता” (توتا) लिखें या “तोता” (طوطا), “वतीरा” (وطیرہ) लिखें या “वतीरा” (وتیرہ), “रहमान” (رحمٰن) लिखें या “रहमान” (رحمان), “तमग़ा” (تمغا) लिखें या “तमग़ा” (تمغہ), “मुअ'म्मा” (معمہ) लिखें या “मुअ'म्मा” (معما), “महीना” (مہینہ) लिखें या “महीना” (مہینا), “पैसा” (پیسہ) लिखें या “पैसा” (پیسا), “तमाशा” (تماشہ) लिखें या “तमाशा” (تماشا), “गए” (گئے) लिखें या “गए” (گیے) वग़ैरह सद-हा मिसालें हैं, उसके बारे में ये तवक़्क़ो’ करना ख़ाम-ख़याली है कि सब लोग कान दबाकर एक ही क़ाएदे पर इत्तिफ़ाक़ कर लेंगे और झगड़ा न करेंगे।
यहाँ तो अभी ये आ'लम है कि यही फ़ैसला करने में सर-फुटव्वल हो रही है कि “ख”, “भ” वग़ैरह मख़लूत आवाज़ों को उर्दू हुरूफ़-ए-तहज्जी माना जाए कि नहीं? और अगर माना जाए तो उन्हें कहाँ जगह दी जाए? “बे” के फ़ौरन बा'द ''भ” आए या “बड़ी ये” के बा'द? लुग़त में पहले “बेटा” का इंदिराज हो या “भारी” का?
अभी तो इसी पर तकरार है कि लुग़त लिखते वक़्त अलिफ़ मद (आ) वाले लफ़्ज़ पहले आएँगे कि ख़ाली अलिफ़ वाले? ब-ज़ाहिर तो ये बात ऐसी है कि इसमें किसी बहस या इख़्तिलाफ़ की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन अगर आप उर्दू के “मुस्तनद” लुग़ात मुलाहिज़ा करें तो आप को मा'लूम होगा कि इस बाब में “नूरुल-लुग़ात” का अ'मल कुछ है, “आसिफ़िया” का कुछ और है, फ़ेलुन का कुछ दूसरा ही है, और तरक़्क़ी उर्दू बोर्ड पाकिस्तान, के अज़ीमुश्शान “उर्दू लुग़त, तारीख़ी उसूल पर” के ख़यालात दीगर हैं। ऐसी सूरत में ये उम्मीद करना कि सब लोग तब्दील-ए-ख़त (Tranliteration) के एक ही उसूल पर इत्तिफ़ाक़ कर लेंगे, या जल्द इत्तिफ़ाक़ कर लेंगे, महज़ उम्मीद-परस्ती है।
(6) उर्दू में बहुत सी आवाज़ें ऐसी हैं जिन्हें रोमन रस्म-उल-ख़त अदा नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर, हस्ब-ए-ज़ेल अल्फ़ाज़ को रोमन में सही लिखना ग़ैर-मुम्किन है,
बहन, क़ाएदा, कहना, कव्वा, कुआँ, दो-धारी (ब-मअ'नी दो धारों वाली, मसलन दो-धारी तलवार), दुआ’ वग़ैरह। इन अल्फ़ाज़ में ज़ेर, ज़बर, पेश की जो आवाज़ें हैं, वो रोमन या नागरी में नहीं अदा हो सकतीं।
(7) अगर सिर्फ़ लफ़्ज़ को अदा करना है (और ब-ज़ाहिर मक़सद यही मा'लूम होता है) तो उर्दू के हज़ारों अल्फ़ाज़ का तलफ़्फ़ुज़ बिगाड़ कर रोमन में लिखना होगा। मसलन मुंदरजा-ज़ेल अल्फ़ाज़ को देखें,
पर्दा, अगर इसे parda लिखें तो लफ़्ज़ ग़लत हो जाता है। अगरpardah लिखें तो और भी ग़लत हो जाता है। अगर इसे pard लिखें तो कोई लफ़्ज़ ही नहीं बनता। (मलहूज़ रहे कि बाज़-औक़ात इसे अंग्रेज़ी लफ़्ज़ क़रार देते हैं तो इसे purdah लिखते हैं।)
गुनाह, इसे अगर gunah लिखें तो h की आवाज़ अंग्रेज़ी में ग़ाइब हो जाएगी, सिर्फ़ “गुना” सुनाई देगा। अंग्रेज़ी में कोई तरीक़ा ऐसा नहीं कि आख़िर में आने हवाली हा-ए-हव्वज़ की आवाज़ को मलहूज़ रख सकें। मजबूरन इसे gunaha लिखना पड़ेगा जो तलफ़्फ़ुज़ के क़तअ'न मुनाफ़ी है।
कारवाँ, अगर इसके नून-गुना के लिए कोई एक अ'लामत सब लोग मुक़र्रर कर भी लें तो रोमन में इस लफ़्ज़ को या तो karvan लिखेंगे, या karavan लिखेंगे। उर्दू के लिहाज़ से दोनों तलफ़्फ़ुज़ ग़लत हैं। उर्दू में “कारवाँ” की रा-ए-मोहमला साकिन है, लेकिन इस पर हल्का सा ज़बर भी है। रोमन में वस्ती सुकून ज़ाहिर करने का कोई तरीक़ा नहीं है और जिस तरह सुकून/हरकत “कारवाँ”, “फ़ैसला” जैसे बे-शुमार लफ़्ज़ों में है, इसके लिए रोमन में कुछ भी इंतिज़ाम नहीं।
मीर (या-ए-मा'रूफ़), दूर (वाव-ए-मा'रूफ़) जैसे कितने ही अल्फ़ाज़ हैं जो ब-ए'तिबार-ए-तलफ़्फ़ुज़ रोमन में अदा नहीं हो सकते। अंग्रेज़ी में miir का तलफ़्फ़ुज़ me’ar और duur का तलफ़्फ़ुज़ du’ar है, क्योंकि अंग्रेज़ी तलफ़्फ़ुज़ के ए'तिबार से आख़िरी R नहीं बोला जाता। अगर उसे बोलना है तो उसके पहले या बा'द हरकत देनी होगी, जो उर्दू तलफ़्फ़ुज़ के मुनाफ़ी है। उर्दू जानने वाले तमाम अंग्रेज़ और अमरीकन अपनी ज़बान की मजबूरी के बाइ'स “मीर” को mere बर-वज़्न fear बोलते हैं। एक मुद्दत हुई जब मैं (ज़ियादा-तर तालिब-ए-इ'ल्मी के दिनों में) अंग्रेज़ी में फिल्में देख लिया करता था। अब फ़िल्म का नाम याद नहीं रहा, लेकिन उसमें एक हिन्दुस्तानी किरदार “कबीर” नामी था। मुझे उसका तलफ़्फ़ुज़ kabi’ar सुनकर थोड़ी सी हैरत हुई।
बा'द में मग़रिबी ममालिक में हर जगह मैंने यही सूरत पाई। “कश्मीर” के पुराने हिज्जे इसी वज्ह से Cashmere थे और एक ख़ास तरह का ऊनी कपड़ा आज भी Cashmere कहलाता है। इसी तरह, एक ख़ास तरह के रेशमी कपड़े को Madras कहते हैं और चूँकि इस हिज्जे में दोनों A की क़ीमत ग़ैर-मा'लूम है, लिहाज़ा इस लफ़्ज़ को अंग्रेज़ी क़ाएदे के मुताबिक़ आज भी “मैडरस” (“मैड” बर-वज़्न sad और “रस” बर-वज़्न fuss) कहते हैं।
(8) अ'रबी फ़ारसी, ख़ासकर अ'रबी के अनगिनत अल्फ़ाज़ हैं, उर्दू में जिनके तलफ़्फ़ुज़ के बारे में इख़्तिलाफ़ है। बहुत से ऐसे हैं जिनके बारे में इख़्तिलाफ़ नहीं लेकिन उर्दू में उनका तलफ़्फ़ुज़ अ'रबी/फ़ारसी से मुख़्तलिफ़ है। ख़ैर, जहाँ इख़्तिलाफ़ नहीं, वहाँ तो मुम्किन है कि रोमन में भी उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ को अपना लिया जाए (हालाँकि बहुत से लोग न मानेंगे) लेकिन जहाँ इख़्तिलाफ़ है वहाँ क्या-किया जाए, मसलन,
rivayat लिखें कि ravayat?
murawatलिखें कि muruu’at?
hisabलिखें कि hesabया hasab?
Mihdi लिखें कि mahdiया mehdi? (ये ख़याल रहे कि अंग्रेज़ी में Mihdi/Mahdi/Mehdi जो भी लिखें, हर्फ़ h पढ़ने में न आएगा और बच्चे को ये सीखने में बहुत मुश्किल होगी कि यहाँ हर्फ़ h साफ़ साफ़ बोला जाएगा)
taqii’ah लिखें याt aqaiyah या taqayyiah?
Sayyid लिखें या sayyad या saiyad या syed लिखें?
janazaलिखें या janazah?
Zimam लिखा जाए कि zamam?
Qabool लिखना बेहतर है किqubool?
इसी तरह, sha’oor दुरुस्त माना जाए या shu’oor? या furogh अच्छा है कि farogh?
(9) एक मुश्किल इन लफ़्ज़ों में होगी और ऐसे लफ़्ज़ बहुत हैं और राइज भी हैं, जिनको शे'र में तो अस्ल तलफ़्फ़ुज़ के ए'तिबार से नज़्म किया जाता है लेकिन बोल-चाल में उनका तलफ़्फ़ुज़ कुछ और है। मसलन, शम्अ’, शक्ल, ज़ब्ह, शहद, हर्ज, तरह, इत्मीनान, हरकत, कलमा, सदक़ा, वग़ैरह।
(10) बहुत से ऐसे लफ़्ज़ हैं जो मौक़े’ या रिवाज के ए'तिबार से कई तरह बोले जाते हैं। उनका क्या होगा? मसलन ये अल्फ़ाज़ रोमन में किस तरह लिखे जाएँगे,
कि, इसके तीन तलफ़्फ़ुज़ हैं।
(1) क़ाफ़ के बा'द हल्की या-ए-मा'रूफ़
(2) क़ाफ़ के बा'द हल्की या-ए-मजहूल
(3) क़ाफ़ के बा'द लंबी या-ए-मजहूल।
और अगर ज़रूरत हो तो कभी-कभी क़ाफ़ के बा'द तवील या-ए-मा'रूफ़ भी बोली जाती है।
लैला, और इस क़िस्म के तमाम अल्फ़ाज़ जिनका तलफ़्फ़ुज़ कभी-कभी या-ए-मा'रूफ़ से करते हैं (बर-वज़्न “फैली” और कभी ख़ासकर इज़ाफ़त की हालत में अलिफ़ मकसूरा के साथ (बर-वज़्न “फैला”)
चियूंटी : इसके तीन तलफ़्फ़ुज़ हैं।
(१) चींउटी बर-वज़्न फ़ाइ'लुन,
(२) चूँटी बर-वज़्न फ़े'लुन
(3) च्यूँटी, या-ए-मख़लूत के साथ, बर-वज़्न फ़े'लुन
हद, ख़त, कफ़, हज और इस तरह के दूसरे अ'रबी लफ़्ज़ जिनके आख़िरी हर्फ़ पर तश्दीद है, लेकिन वो सिर्फ़ इज़ाफ़त की हालत में कभी-कभी बोली जाती है।
मुच्छर, चपरास वग़ैरह बहुत से लफ़्ज़ हैं जिन्हें दिल्ली वाले और बहुत से मशरिक़ी हिन्दुस्तान वाले, रा-ए-हिन्दी से बोलते हैं (मुच्छड़, चपड़ास और बाक़ी लोग सादा रा-ए-मोहमला से।)
(11) अब बा'ज़ बातें और देख लीजिए। अगर इमला नहीं ज़ाहिर करना है तो बहुत जगह तलफ़्फ़ुज़ भी ग़लत हो जाएगा। मसलन मुंदरजा-ज़ेल पर ग़ौर करें,
ज़ो'फ़, सई'द, मा'ज़ूर, मा'क़ूल
ज़िद की और बात है, लेकिन इन लफ़्ज़ों में ऐ'न का तलफ़्फ़ुज़ सरासर अलिफ़ या हमज़ा का नहीं। हस्ब-ए-ज़ेल से मुक़ाबला करें,
ज़ोर, लईक, माजूर, माकूल
साफ़ ज़ाहिर है कि ज़ो'फ़/ज़ोर, सई'द/लईक, मा'ज़ूर/माजूर और मा'क़ूल/माकूल के तलफ़्फ़ुज़ एक नहीं हैं। अव्वल-उल-ज़िक्र लफ़्ज़ों में थोड़ी सी आवाज़ ऐ'न की सुनाई देती है। रोमन उसे किस तरह अदा करेंगे।
जिन लफ़्ज़ों में वाव-ए-मा'दूला मा’ अलिफ़ है (ख़्वान, ख़्वाब) उनका तलफ़्फ़ुज़ उन लफ़्ज़ों से मुख़्तलिफ़ है जिनमें वाव-ए-मा'दूला बे-अलिफ़ है (ख़ुश, ख़ुद)। ऐसे अल्फ़ाज़ में इमला ज़ाहिर करें तो तलफ़्फ़ुज़ हाथ से जाता है और तलफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर करें तो इमला का ख़ून होता है।
रोमन में हमज़ा का मुतबादिल कुछ नहीं। रोमन रस्म-ए-ख़त में हमज़ा और ऐ'न और अलिफ़ सब एक हो जाएँगे। मसलन,
अ'क्स aks، तअस्सुफ़ tassuf، आलम alam
रोमन में पढ़ने वाला इन अल्फ़ाज़ में फ़तहा की आवाज़ का कुछ इम्तियाज़ न कर सकेगा। आहिस्ता-आहिस्ता इनका तलफ़्फ़ुज़ बदल जाएगा और फिर शाइ'री को मौज़ूँ पढ़ना तक़रीबन ना-मुम्किन हो जाएगा।
इस्तिदलाल अभी और भी हैं। लेकिन जो मानना चाहे उसके लिए इतने बहुत हैं और जो न मानना चाहे उसके लिए पूरी किताब भी काफ़ी न होगी। बहर-हाल, रस्म-उल-ख़त की तब्दीली के मुअय्यिदीन से मेरी दरख़्वास्त है कि वो मसऊ'द हसन रिज़वी अदीब की छोटी सी किताब “उर्दू ज़बान और इसका रस्म-उल-ख़त” पढ़ लें और अगर तौफ़ीक़ हो तो उसी मौज़ू पर मुहम्मद हसन अ'सकरी और एहतिशाम हुसैन के मज़ामीन भी देख जाएँ। शानुल-हक़ हक़्क़ी ने हाल में अच्छी बात कही है,
“रस्म-उल-ख़त अपनी ज़बान के लिए और ज़बान अपने बोलने वालों के लिए होती है। चंद ग़ैर-मुल्कियों की सहूलत के लिए अपनी ज़बान की काया पलट करना मज़हका-ख़ेज़ हरकत होगी। दुनिया को उर्दू की तरफ़ मुतवज्जह करना हो तो हमें इसके अंदर बेहतर से बेहतर अदीब पैदा करने की ज़रूरत है न कि इसकी दुुम में खटखटा बाँधने की।”
इस पर मैं सिर्फ़ इतना इज़ाफ़ा करूँगा कि उर्दू का रस्म-ए-ख़त अगर रोमन कर दिया जाए तो जितनी सहूलतें हासिल होंगी उनसे कहीं बढ़कर मुश्किलें पैदा होंगी। और ये बात भी ध्यान में रखने की है कि अगर एक-बार रस्म-ए-ख़त की तब्दीली पर हम राज़ी हो गए तो ये तक़ाज़ा बार-बार उठेगा। आज लोग देवनागरी या रोमन के लिए कह रहे हैं, कल को किसी और रस्म-उल-ख़त के लिए माँग होगी कि उर्दू लिखने के लिए उसे भी इस्ति'माल किया जाए।
ख़ुद हिन्दुस्तान में लोग कहेंगे कि देवनागरी क़ुबूल है तो बंगाली क्यों नहीं? बंगाली क़ुबूल है तो तमिल क्यों नहीं? फिर ये सिलसिला ख़त्म नहीं होने वाला।
जैसा कि मैंने ऊपर कहा, अपने रस्म-उल-ख़त या इमला में तब्दीली का तक़ाज़ा करने की बीमारी सिर्फ़ उर्दू वालों में है। अगर किसी और ज़बान वाले से कहिए कि “मियाँ तुम्हारा रस्म-ए-ख़त या इमला नाक़िस है, इसे बदल डालो” तो वो मरने-मारने पर आमादा हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मग़रिब में तीसरी दुनिया से आए हुए सिर्फ़ उर्दू के ही लोग बसते हों।
हिन्दुस्तान और अफ़्रीक़ा और एशिया की अक्सर ज़बानें बोलने वालों की कसीर ता'दाद मग़रिब में मुक़ीम है। उनमें से तो किसी की भी ज़बान से नहीं सुना गया कि हमारे बच्चों को अस्ल रस्म-ए-ख़त में दिक्कतें पेश होती हैं, क्यों न अपनी ज़बान मसलन मराठी, बंगाली, मलयालम, सिंघल, स्वाहिली, हौसा का रस्म-ए-ख़त बदल कर रोमन कर दिया जाए।
कुछ दिन हुए एक साहब की तजवीज़ नज़र से गुज़री कि उर्दू में हर्फ़ मिलाकर लिखे जाते हैं। इससे कम्पयूटर को बड़ी मुश्किल होती है। दुनिया की अक्सर ज़बानों की तरह उर्दू के हर्फ़ भी अलग-अलग लिखे जाएँ तो कम्पयूटर के मैदान में आसानी हो जाएगी।
अव्वल तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि अलग-अलग हर्फ़ लिखने से कम्पयूटर को कौन सी आसानी हो जाएगी? कम्पयूटर ग़रीब उर्दू का नक़्क़ाद तो है नहीं कि अ'क़्ल से आ'री हो। वो तो एक बहुत ही नाज़ुक और हस्सास मशीन है, जो सिखाएगा सीख लेगा। ऐसा नहीं है कि कम्पयूटर जब उर्दू फ़ारसी अ'रबी लिखता है तो उसे मा'लूम रहता है कि अंग्रेज़ी या फ़्रांसीसी नहीं है और इसमें मुझे बड़ी मुश्किल होना चाहिए। कम्पयूटर तो हुक्म का बंदा है। उसमें अक़दारी फ़ैसले की सलाहियत नहीं। लेकिन बुनियादी सवाल ये कि उर्दू में हर्फ़ों को अलग-अलग क्यों नहीं लिखा जाता, जब कि मसलन रोमन और नागरी में ऐसा मुम्किन है।
इस सवाल का जवाब ये है कि जिन ज़बानों में हर्फ़ अलग-अलग लिखे जाते हैं उनमें ए'राब-ए-बिल-हर्फ़ या ए'राब-ए-सरीह, या मौके़’-मौके़’ से दोनों का इल्तिज़ाम होता है। मुअख़्ख़र-उल-ज़िक्र को संस्कृत/हिन्दी में “मात्रा” कहते हैं। ए'राब-ए-बिल-हर्फ़ के लिए वहाँ शायद कोई इस्तिलाह नहीं है। इन दोनों इस्तेलाहों के अ'मल को यूँ वाज़ेह कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपने उर्दू में लिखा,
हम
अब आपसे कहा गया कि अच्छा इसके हर्फ़ अलग-अलग करके रोमन रस्म-ए-ख़त में लिखिए, जिस तरह अंग्रेज़ी लिखी जाती है। तो आपने लिखा,
HM
अब नातिक़ा सर-ब-गरीबाँ कि इसे क्या पढ़िए। ज़ाहिर है कि अंग्रेज़ी में कोई लफ़्ज़ उस क़िमाश का है ही नहीं जिसमें सिर्फ़ ये दो हर्फ़ हों। ला-मुहाला आप कहेंगे, “लफ़्ज़, 'हम के ए'राब क्या हैं?
ये मा'लूम हो तभी तो अंग्रेज़ी में लिखूँगा।”
आपकी बात वज़नी है, लिहाज़ा आपको बताया गया कि यहाँ हम में अव्वल मफ़्तूह है।
“बहुत ख़ूब, अभी लीजिए।”, आपने झट कहा और लिखा,
HAM
इस बात से क़त’-ए-नज़र कि लफ़्ज़ Ham के अंग्रेज़ी में कई मअ'नी हैं, और भी मअ'नी उर्दू लफ़्ज़ हम के मअ'नी से मुताबिक़त नहीं रखते, आप ये मुलाहिज़ा करें कि पढ़ने-सीखने वाले को कितनी मुश्किल होगी (और आपके कम्पयूटर ग़रीब को शायद कितनी मुश्किल होगी) जब ये लफ़्ज़ हम रोमन रस्म-ए-ख़त में, उर्दू रोमन तर्ज़ के मुताबिक़, हर्फ़ अलग-अलग करके लिखा जाएगा?
अगर आप ए'राब-ए-बिल-हर्फ़ न देंगे तो कोई पढ़ ही न सकेगा कि लिखा किया है? उर्दू में तो रस्म बन चुकी है, पढ़ने वाले को मा'लूम है कि शुरू’-शुरू’ की इक्का-दुक्का मनाज़िल के बा'द ए'राब-ए-सरीह (ज़ेर, ज़बर, पेश) मेरा साथ छोड़ देंगे। लिहाज़ा मुझे ख़ुद ही मा'लूम करना है कि मसलन हस्ब-ए-ज़ेल शे'र में अल्फ़ाज़ पर ए'राब क्या हैं,
कई गुज़रे सन तिरा कम था सिन जो लिए थे सुन तिरे घुंगरू
गया सीना छन गए होश छिन जो बजे थे छुन तिरे घुंगरू
चुनाँचे जब मेरा साबिक़ा उर्दू ज़बान और रस्म-ए-ख़त में लफ़्ज़ हम से पड़ा तो मैंने ये पुकार न लगाई कि अरे भाई इस पर ए'राब क्या हैं? मैंने ख़ुद को सिखा लिया है कि यहाँ अव्वल हर्फ़ पर तीन में से एक हरकत होगी और मुझे क़यास और तजुर्बे से काम लेकर मा'लूम कर लेना है कि इस वक़्त कौन सी हरकत है। अगर मुझे सिर्फ़ HM दिखाया जाएगा तो मैं मरते-मरते मर जाऊँगा लेकिन मुझे ए'राब न मिलेगा।
अच्छा अगर ये तय कर लें कि मियाँ जिस तरह उर्दू में अटकल से पढ़ते हो, उसी तरह रोमन में अटकल से पढ़ लो। जान लो इस ज़बान में ए'राब-ए-बिल-हर्फ़ नहीं हैं। इस पर इलतमस ये है कि क्या मअ'नी, उर्दू ज़बान में ए'राब-ए-बिल-हर्फ़ नहीं? तो फिर उसी लफ़्ज़ “नहीं” में हा-ए-हव्वज़ के बा'द क्या है? हर्फ़-ए-दुवुम यहाँ मकसूर है और हर्फ़-ए-सिवुम पर कोई हरकत नहीं, वो लंबी अलिफ़ की आवाज़ ज़ाहिर कर रहा है, कहने को छोटी ये है।
ये ए'राब-ए-सरीह है, या'नी किसी हर्फ़ को अ'लामत में बदल कर उससे ए'राब का काम लिया जा रहा है। यही छोटी ये जब लफ़्ज़ “ईधर” में आएगी तो और तरह लिखी जाएगी, जब लफ़्ज़ “पीली” में लिखी जाएगी तो और तरह लिखी जाएगी। अब ज़रा “बाँग-ए-दरा” का पहला मिसरा’ हर्फ़ों को अलग-अलग करके रोमन तर्ज़ में सिर्फ़ उर्दू के ए'राब के मुताबिक़ लिखिए,
अलिफ़ बड़ी ये छोटी हे मीम अलिफ़ लाम छोटी हे अलिफ़ बड़ी ये फ़े स्वाद छोटी ये लाम काफ़ शीन वाव रे छोटी नून दाल वाव सीन ते अलिफ़ नून ग़ुन्ना
मैंने लफ़्ज़ों के दरमियान फ़ासले रखे हैं, लेकिन कोई बंदा-ख़ुदा इस मिसरे को पहले से उर्दू में पढ़े बग़ैर पढ़ ही दे तो देखूँ, सही और मौज़ूँ पढ़ना तो दूर रहा। कहीं पर ए'राब ग़ाइब हैं, कहीं ए'राब-ए-सरीह है, लेकिन फिर भी मुबहम (मसलन पता नहीं चलता कि हिंदुस्ताँ मैं वाव-ए-मा'रूफ़ है कि मजहूल?)
मा'लूम हुआ उर्दू में कहीं-कहीं ए'राब-ए-सरीह है, ज़ियादा-तर फ़ुक़दान ए'राब है, और जहाँ ए'राब हैं वहाँ अक्सर मुबहम हैं। ऐसी ज़बान को आप अंग्रेज़ी की तरह अलग-अलग हर्फ़ों और इल्तिज़ाम ए'राब के साथ किस तरह लिखेंगे।
एक बात और भी है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ी में ए'राब-ए-बिल-हर्फ़ बिल्कुल नहीं है। और न ऐसा है कि ए'राब-ए-बिल-हर्फ़ की इमदाद से तलफ़्फ़ुज़ क़तई’ और वाज़ेह हो जाता है। अंग्रेज़ी में जहाँ-जहाँ (मसलन) हस्ब-ए-ज़ेल हर्फ़-ए-आख़िर लफ़्ज़ में साथ आते हैं, वहाँ ए'राब-ए-बिल-हुरूफ़ है,
BLE (aBLE) ; DLE (bunDLE); GLE (bunGLE); KLE (tacKLE)
मगर मुश्किल ये है कि इन तीनों में हर्फ़ और उसके मा-क़ब्ल के दरमियान हरकत यकसाँ नहीं है।
Table में bऔर L के बीच में हल्का सा ज़म्मा है।
Bundle में d और L के बीच में हल्का सा कस्रा है।
Bungleमें b औरL के बीच में कुछ नहीं है, फ़तहा मान सकते हैं लेकिन वो इस क़दर हल्का है कि होना न होना मुसावी समझिए।
Tackle में k और L के बीच में बहुत हल्का सा ज़म्मा है, ज़रा कस्रा की तरफ़ माइल।
लिहाज़ा वहाँ भी तलफ़्फ़ुज़ की मुश्किलें ए'राब के होने या न होने की बिना पर हैं, ख़्वाह हर्फ़ कितनी ही दूर-दूर क्यों न लिखे जाएँ। अंग्रेज़ी की नक़्ल करने से यहाँ उर्दू को कुछ न मिलेगा।
ख़लील धनतेजवी की ये बात बा-वज़्न है, “अगर ग़ैर-उर्दू-दाँ तब्क़ा भी उर्दू लिखना-पढ़ना सीख लेता है तो उर्दू की आबयारी करने वालों के बच्चों को (ये काम) क्यों नहीं सिखाया जा सकता?”
हम उर्दू वालों की ये अदा ख़ूब है कि जिस दरख़्त से फल हासिल करना मुश्किल नज़र आए, उस दरख़्त की जड़ ही काट देने पर तुल जाएँगे, ख़ुद थोड़ी सी मेहनत न बर्दाश्त करेंगे। इसी तरह, राम प्रकाश कपूर ने भी सच्ची बात कही है। ये और बात है कि हम लोगों को ख़ुद-बीनी से फ़ुर्सत ही नहीं कि इन अल्फ़ाज़ के आईने में अपनी सूरत देखें,
“उर्दू की लड़ाई ख़ुद उन लोगों से है जो उर्दू बोलते हैं, उर्दू के मुशाइ'रे पढ़ते हैं, उर्दू की मजालिस में शरीक होते हैं, उर्दू के नाम की रोटी खाते हैं, उर्दू के कारवाँ को चलाते हैं और कभी-कभी उर्दू को सरकारी ज़बान बना देने की माँग करके अ'वाम को गुमराह भी करते हैं। उर्दू में फिल्में लिख कर हिन्दी के नाम से बेचते हैं। उर्दू के गानों पर हिन्दी सर्टीफ़िकेट बर्दाश्त करते हैं। इन तमाम बड़े-बड़े उर्दू-दाँ हज़रात के बच्चे उर्दू नहीं पढ़ते, नहीं बोलते, नहीं लिखते, नहीं जानते। न ही ख़ुद ये लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे उर्दू जैसी ज़बान सीखें।”
गुज़िश्ता चालीस बरस से मैं उर्दू के बड़े-बड़े अदीबों और प्रोफ़ैसरों की ख़िदमत में हाज़िरी देता रहा हूँ और मैंने हत्तल-मक़दूर इस बात पर टोका भी है कि आपके बच्चे, पोते पोतिया, नवासे-नवासियाँ उर्दू नहीं पढ़ते। ये अच्छी बात नहीं, और कुछ नहीं तो ये ख़याल फ़रमाइए कि आपकी तहरीरों से आपके अख़्लाफ़ महरूम रहेंगे, ये मुंसफ़ी से आ'री है कि नहीं? लेकिन मुझे अफ़सोस है कि इक्का-दुक्का के सिवा किसी के कान पर जूँ न रेंगी। और यही लोग हैं जिनकी सदा-ए-मातम सबसे ज़ियादा बुलंद सुनाई देती है कि हाय उर्दू मर गई या मर रही है। और ऐसा क्यों न हो, उन्होंने अपने घर से उर्दू को बदर कर दिया है, इसलिए वो यही कहने में आ'फ़ियत समझते हैं कि उर्दू का ख़ात्मा हो गया, या होने वाला है।
हक़ीक़त, ज़ाहिर है कि इसके बिल्कुल बर-अ'क्स है। लेकिन उर्दू की बक़ा के लिए सबसे ज़ियादा तआ'वुन और क़ुर्बानियाँ ग़रीब-ग़ुर्बा की तरफ़ से या फिर उन इ'लाक़ों से आई हैं जिन्हें हम यू.पी. वाले उर्दू के इ'लाक़े नहीं समझते और वहाँ के उर्दू बोलने वालों को “अहल-ए-ज़बान” नहीं तसव्वुर करते।
उर्दू के लिए सई’ और जहद सबसे ज़ियादा बिहार में की गई और की जा रही है। फिर महाराष्ट्र में, जहाँ उर्दू मुख़ालिफ़ हुकूमतों के बा-वजूद उर्दू ज़रीया’-ए-ता'लीम की दर्सगाहें ख़ूब बर्ग-ओ-बार ला रही हैं और उर्दू मीडियम से ता'लीम पाए हुए बच्चे मुसलसल हाई स्कूल के इम्तिहान में सारे सूबे में पहली पोज़ीशन लाते हैं। यू.पी. वाले समझते हैं कि हमने उर्दू पढ़ना छोड़ दिया तो सबने छोड़ दिया। वो बिहार और महाराष्ट्र क्या, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, आंध्रा, हिमाचल प्देश जा के देखें तो उन्हें मा'लूम हो। यू.पी. वाले अपने गले में “अहल-ए-ज़बान” का तमग़ा लटकाए रहें और समझते रहें कि उर्दू का क़ुल हो चुका। दुनिया उन पर हँस रही है, अभी और हँसेंगी।
रामप्रकाश कपूर ने अपनी तहरीर मतबूआ’ “शाइ'र” मुंबई में हाशिम अ'ली अख़्तर साहब (साबिक़ वाइस चांसलर, उस्मानिया यूनीवर्सिटी, और फिर अ'लीगढ़ यूनीवर्सिटी) का हवाला दिया है कि उनके दोस्तों, रिश्तेदारों में “चालीस की उ'म्र से कम वाला एक भी फ़र्द उर्दू रस्म-उल-ख़त नहीं जानता।” लिहाज़ा हाशिम अ'ली साहब चाहते हैं कि उर्दू का रस्म-उल-ख़त बदल दिया जाए।
ये तो ऐसा ही हुआ कि अगर किसी मुआ'शरे में चालीस से कम उम्र वाले अफ़राद जाहिल हूँ तो हाशिम अ'ली साहब की मंतिक़ के मुताबिक़ उस मुआ'शरे में ख़वांदगी (Literacy) को मंसूख़ क़रार दिया जाए और उसको “ज़बानी” (Oral) मुआ'शरे की सत्ह पर क़ाएम किया जाए। और अगर किसी मुआ'शरे में चालीस से कम-उम्र वाले अफ़राद को कोई बीमारी है तो उस बीमारी का इ'लाज करने के बजाए उसे नॉर्मल हालत-ए-सेहत क़रार दिया जाए और सब लोगों के लिए उस बीमारी में मुब्तिला होना ज़रूरी क़रार दिया जाए।
मैं कई गुज़िश्ता तहरीरों में रोमन और नागरी रस्म-उल-ख़तों की कई और कमज़ोरियाँ तफ़्सील से बयान कर चुका हूँ, लिहाज़ा यहाँ इन बातों का इआ'दा नहीं करना। यहाँ आख़िरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत से मुराआ'त की भीक माँगने के बजाए हम उर्दू वालों को ख़ुद अपनी ज़बान के फ़रोग़ और इस्तिहकाम की कोशिश करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हुकूमतों ने जितना किया है और जो कर रही हैं, उससे ज़ियादा की उम्मीद आपको क्यों हो? ख़ुद हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है कि नहीं?
मोमयाई की गदाई से तो बेहतर है शिकस्त
मोर-ए-बे-पर हाजत-ए-पेश-ए-सुलैमाने मबर
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.