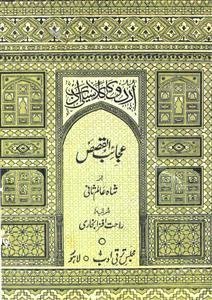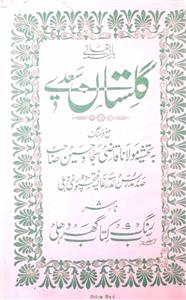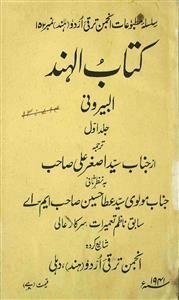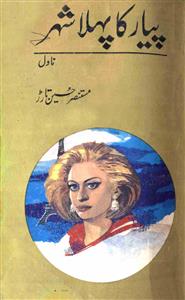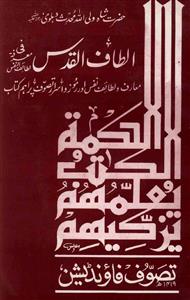For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org
For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org
लेखक: परिचय
शाह आलम सानी मुग़लिया सलतनत के ऐसे बादशाह थे जिनके बारे में ये कहना मुश्किल है कि वो ज़्यादा बदनसीब थे या ज़्यादा पीड़ित। अपने 48 साल की हुकूमत में बारह साल तक वो जान के ख़तरे की वजह से राजधानी दिल्ली में क़दम नहीं रख सके। दिल्ली आने के बाद सत्रह साल तक उन्होंने चौतरफ़ा विद्रोहों में घिरे रह कर अपनी आँखों से मुग़लिया सलतनत के पतन का तमाशा देखा जिसके बाद क़ुदरत को मंज़ूर न हुआ कि वो अपनी आँखों से और कुछ देखते। उनके अमीर-उल-उमरा ग़ुलाम क़ादिर रोहेला ने उनकी आँखें निकाल कर उन्हें अंधा कर दिया और ज़िंदगी के बाक़ी 19 साल उन्होंने उसी हालत में हुकूमत की। ये उनकी निजी ज़िंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी थी जिसका दूसरा पहलू ये था कि उसी विकलांगता ने उनको नस्र(गद्य) में “अजाइब-उल-क़सस” और नज़्म में “नादिरात-ए-शाही” इमला करवाने का मौक़ा दिया। “अजाइब-उल-क़सस” उत्तर भारत में उर्दू नस्र के प्रथम नमूनों में से एक और अपनी ज़बान के लिहाज़ से बिल्कुल अलग है। तज़किरा लेखकों ने उनके उर्दू दीवान का भी ज़िक्र किया है जो कहीं नहीं मिलता। उर्दू, हिन्दी और फ़ारसी के शायरी के नमूने उनकी किताब “नादिरात-ए-शाही” में मिलते हैं जो उर्दू के साथ साथ देवनागरी लिपि में है और जिससे हमें उनके मिज़ाज और उनकी दिलचस्पियों का अंदाज़ा होता है।
शाह आलम सानी, आलमगीर सानी के बेटे और वलीअहद थे। उनकी पैदाइश ऐसी हालत में हुई जब आलमगीर सानी लाल क़िले में ऩजरबंदी के दिन गुज़ार रहे थे। शाह आलम का असल नाम मिर्ज़ा अबदुल्लाह उर्फ़ आली गुहर (या अली गौहर) था और बचपन में लाल मियां और मिर्ज़ा बुलाकी भी कहे जाते थे। बादशाह बनने के बाद उन्होंने अबुल मुज़फ्फ़र जलाल उद्दीन मुहम्मद शाह आलम सानी का लक़ब इख़्तियार किया। क़ैद के बावजूद उनकी शिक्षा शाही रीति के अनुसार हुई। वो फ़ारसी, उर्दू और हिंदी के इलावा तुर्की ज़बान भी जानते थे। जवान हुए तो क़िस्मत ने पल्टा खाया और उनके वालिद को बादशाह बना दिया गया। उस वक़्त बादशाह क़िले के अमीरों के हाथ में कठपुतली बन चुका था। वो जिसे चाहते हुकूमत से अपदस्थ कर देते या क़त्ल करते और जिसे चाहते बादशाह बना देते थे। आलमगीर सानी बादशाह और हमारे मिर्ज़ा अबदुल्लाह वलीअहद ज़रूर थे लेकिन इमाद-उल-मुल्क हुकूमत में स्याह-ओ-सफ़ेद का मालिक था। वलीअहद इस घुटन, बेबसी और अविश्वास से मुक्ति पाना चाहते थे। बाप आलमगीर सानी ने भी बेटे की मुहब्बत में यही पसंद किया कि उनको एक जागीर देकर क़िले से दूर कर दिया जाए। लेकिन इमाद-उल-मुल्क ने इसमें अपने लिए ख़तरा महसूस किया। उसने आलमगीर को मजबूर किया कि वो बेटे को दिल्ली वापस बुलाएं। शाहआलम ख़तरे को भाँप गए और घेराबंदी के बावजूद अवध की तरफ़ फ़रार होने में कामयाब हो गए। अवध के नवाब शुजा उद्दौला ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कुछ अर्सा लखनऊ में रहने के बाद इलाहाबाद के हाकिम मुहम्मद क़ुली ख़ान ने उनको इलाहाबाद बुला लिया। वो बहुत दिनों से बंगाल पर हुकूमत करने का ख़्वाब देख रहा था। उसने शाह आलम को बिहार और बंगाल पर लश्कर कशी के लिए तैयार कर लिया, शुजा उद्दौला ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। लेकिन इस मुहिम में उन्हें कामयाबी नहीं मिली और मुहम्मद क़ुली ख़ान निराश दिल हो कर इलाहाबाद वापस चला गया। लेकिन वलीअहद इस नाकामी से निराश नहीं हुए और अक्तूबर 1759 ई. में दुबारा बिहार का रुख़ किया। जब वो बिहार के क़स्बा खतौली में थे उसी वक़्त उनको बाप के क़त्ल किए जाने की ख़बर मिली। उन्होंने वहीं अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। ताजपोशी की प्रक्रिया के बाद उन्होंने बिहार में आगे बढ़ना शुरू किया। राजा राम नरायन ने आगे बढ़कर मुक़ाबला किया लेकिन ज़ख़्मी हो कर पटना के क़िले में छुप गया। इतने में अंग्रेज़ी फ़ौज राजा की मदद को पहुंच गई और अत्यधिक रक्तपात के बाद बादशाह को शिकस्त हुई। अंग्रेज़ उन्हें लेकर पटना आ गए और क़िले में रखा। इसी अर्से में मीर जाफ़र के दामाद मीर क़ासिम जिसको उन्होंने मीर जाफ़र की जगह बंगाल का हाकिम बना रखा था, बादशाह के पास आया और 24 लाख रुपये के बदले बंगाल की निज़ामत की सनद हासिल कर ली। कुछ अर्सा बाद मीर क़ासिम की अंग्रेज़ों से बिगड़ गई और लड़ाई में उसे शिकस्त हुई। वो भाग कर इलाहाबाद आया और बादशाह को जो अंग्रेज़ों की क़ैद जैसी मेहमानदारी से तंग आकर इलाहाबाद शुजा उद्दौला के पास चला आया था, बंगाल पर फ़ौजकशी के लिए उभारा, शुजा उद्दौला ने उसका समर्थन किया। बादशाह मीर क़ासिम और शुजा उद्दौला के टिड्डी दल जैसे लश्कर ने बंगाल पर चढ़ाई की और अंग्रेज़ों की मुट्ठी भर फ़ौज से बक्सर में 23 अक्तूबर 1764 ई. को ऐसी शिकस्त खाई जो हिंदुस्तान की क़िस्मत का फ़ैसला कर गई। अंग्रेज़ जो अभी तक सिर्फ़ व्यापारी थे अब मुल्क पर हुक्मरानी की तरफ़ चल पड़े। उन्होंने बादशाह से बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी इख़्तियारात 26 लाख रुपये के इवज़ हासिल कर लिये। बादशाह को इलाहाबाद और कौड़ा जहानाबाद जागीर में दिए गए और हिफ़ाज़त पर अंग्रेज़ फ़ौज नियुक्त हुई। अर्थात अब बादशाह अंग्रेज़ों की क़ैद में थे। बादशाह अंग्रेज़ों की क़ैद से परेशान थे, दिल्ली जाना चाहते थे लेकिन वहां के हालात बहुत ख़राब थे। आख़िर मरहटों ने हिफ़ाज़त का वादा करके उन्हें दिल्ली बुला लिया और उन्हें अपने इशारों पर नचाने लगे। उनसे रूहेलखंड पर हमला कराया, जहां मरहटों ने ख़ूब लूट मचाई और बादशाह को कुछ न दिया। बादशाह रोहेला हाकिम ज़ाबता ख़ां(जो बादशाह के मुहसिन नजीब उद्दौला का बेटा था) के बाल बच्चों को पकड़ कर दिल्ली ले आए। इन ही लड़कों में ग़ुलाम क़ादिर रोहेला था जिसको बादशाह ने ख़स्सी करा दिया और ज़नाना कपड़े पहनने पर मजबूर किया। उसी ग़ुलाम क़ादिर ने आख़िर बादशाह की आँखें निकालीं। वो ख़ुद भी आख़िरकार मरहटों के हाथों बेदर्दी से मारा गया। अंधा होने के बाद भी मरहटों ने शाह आलम को बादशाहत पर बरक़रार रखा। आख़िर अंग्रेज़ों ने आकर उन्हें दिल्ली से भगाया। अब बादशाह एक लाख रुपये माहवार पर अंग्रेज़ों का वज़ीफ़ा-ख़्वार था। उस ज़माने का मशहूर कथन है; “सलतनत शाह आलम अज़ दिल्ली ता पालम।” उसी हालत में 19 नवंबर 1896 में उसकी मौत हुई।
बक्सर की जंग में शिकस्त के बाद बादशाह के पास अय्याशी के सिवा करने को कुछ नहीं था। दिल्ली में चौतरफ़ा विद्रोहों के बावजूद ये सिलसिला आँखों से महरूम होने तक जारी रहा। शायरी और संगीत से दिल बहलाते थे। फ़ारसी और उर्दू में आफ़ताब और भाषा में शाह आलम तख़ल्लुस करते थे। फ़ारसी में मिर्ज़ा मुहम्मद फ़ाखिर मकीं से मश्वरा करते थे। उर्दू में सौदा को उनका उस्ताद बताया जाता है जो क़रीन-ए-क़ियास नहीं, सौदा उनके दिल्ली आमद से पहले फ़र्रुखाबाद जा चुके थे। शाह आलम के दौर में सलतनत बिगड़ती जा रही थी मगर उर्दू ज़बान सँवर रही थी। मुहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं, “आलमगीर के अह्द में वली ने उस नज़्म का चराग़ रौशन किया जो मुहम्मद शाह के अह्द में आसमान पर सितारा बन के चमका और शाह-आलम के अह्द में सूरज बन कर शिखर पर आया। शाह आलम के मिज़ाज में यूं भी स्थायित्व की कमी थी फिर ऐश में तो जादू का सा असर है। दिन रात नाच-गाने और शे’र-ओ-शायरी में गुज़ारने लगे। उन ही के ज़माने में सय्यद इंशा दिल्ली आए और दरबार से सम्बद्ध हो गए। बादशाह को उनके बग़ैर चैन नहीं आता था। शाह आलम बड़े अभ्यस्त शायर थे। उनके अशआर में पेचदार ख़्यालात, मुश्किल वाक्यांश या शब्द और कोई दूरस्थ रूपक नहीं मिलते। जो कुछ दिल में होता सीधे शब्दों में बयान कर देते थे। उनके कलाम में शान-ओ-शौकत कम मगर असर ज़्यादा है।
शायरी से हट कर शाह आलम का एक अहम कारनामा उनकी गद्य रचना “अजाइब-उल-क़सस” है। ये दावा तो नहीं किया जाता कि ये हिंदुस्तान या उत्तर भारत में उर्दू गद्य की पहली रचना है लेकिन यह 18वीं सदी की गद्य रचनाओं में से एक ज़रूर है और इसकी ज़बान दूसरी रचनाओं के मुक़ाबले में ज़्यादा निखरी हुई है। अगर नस्री दास्तानों को तारीख़ी क्रम से देखा जाये तो “अजाइब-उल-क़सस”, क़िस्सा मेह्र अफ़रोज़ दिलबर (1759 ई.), नौ तर्ज़-ए- मुरस्सा(1775 ई.), नौ आईन-ए-हिन्दी क़िस्सा मलिक मुहम्मद और गेती अफ़रोज़ (1788 ई.) के बाद चौथी गद्य रचना है जो 1792 ई. में लिखी गई। ये एक ना-मुकम्मल दास्तान है लेकिन इससे उस दौर के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल होती हैं। शाह आलम के हिंदी कलाम पर जैसा कि उसका हक़ है अभी तक तवज्जो नहीं दी गई है।
 For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org
For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org
समीक्षा कीजिए
Jashn-e-Rekhta | 13-14-15 December 2024 - Jawaharlal Nehru Stadium , Gate No. 1, New Delhi
Get Tickets