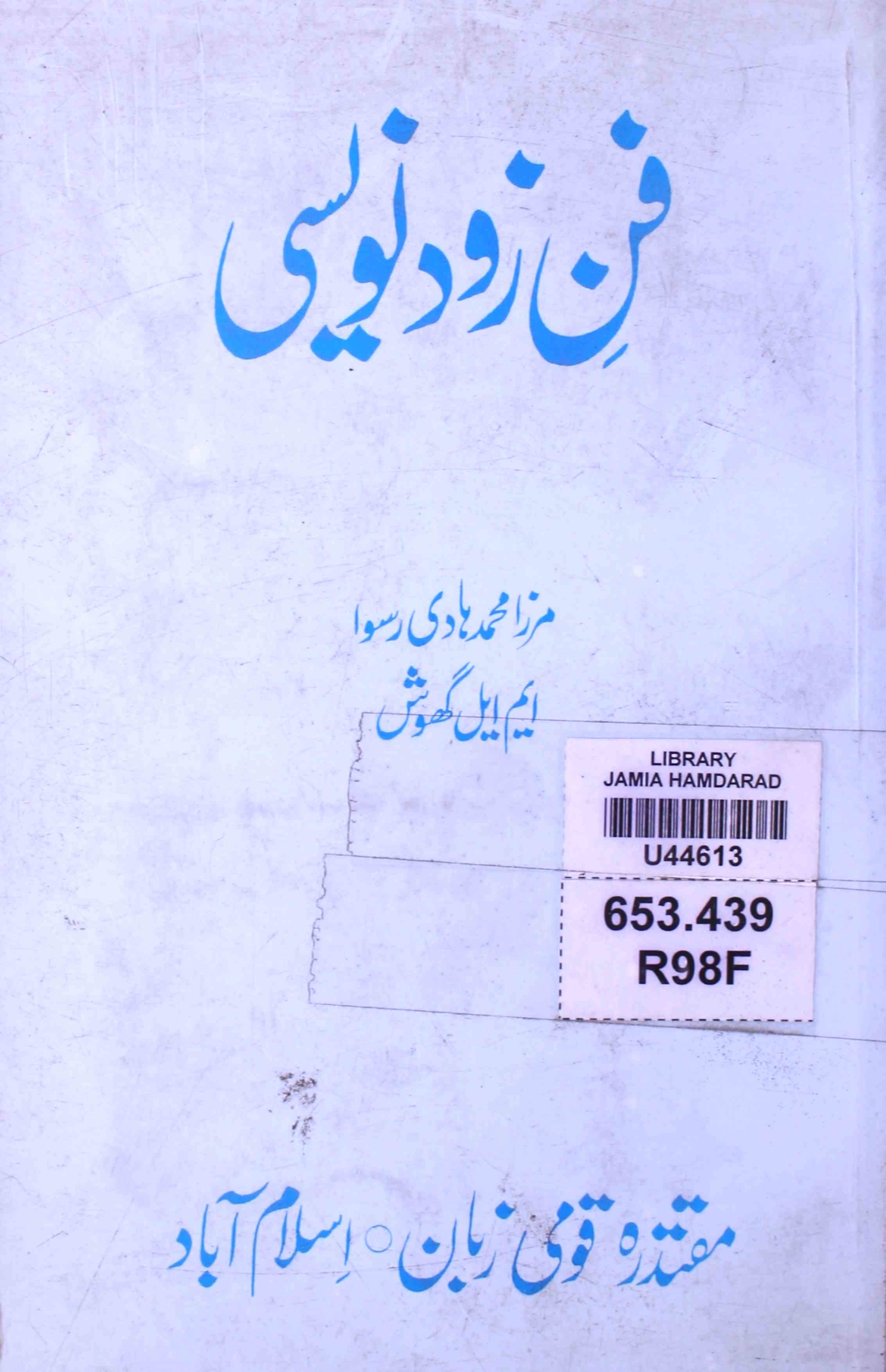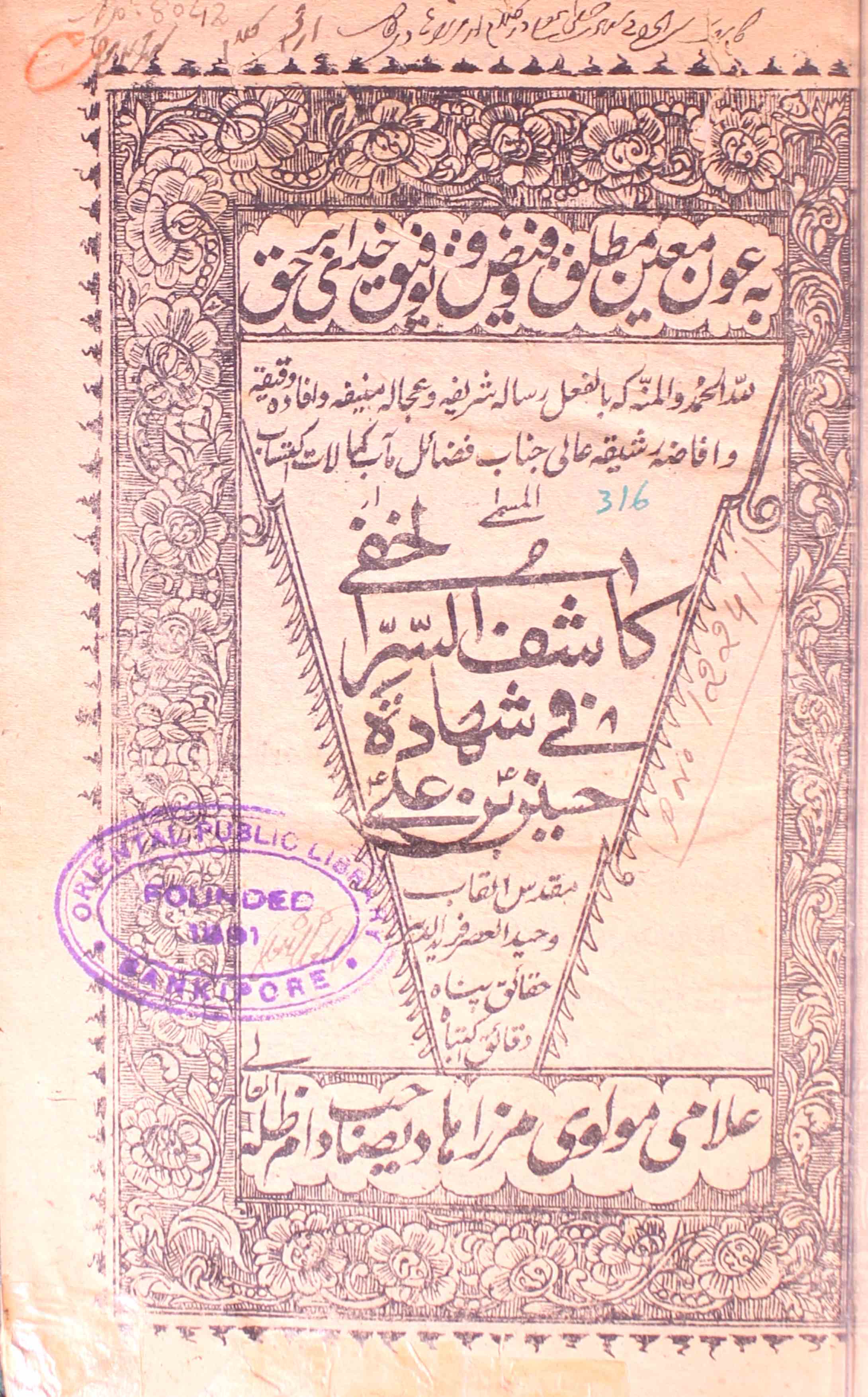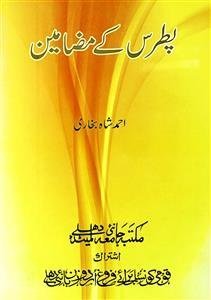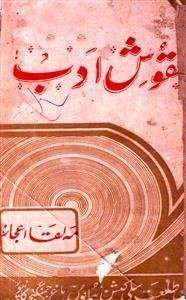For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org
For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org
पुस्तक: परिचय
مرزا ہادی رسوا ایک ایسے ناول نگار ہیں جنھوں نے اپنی جدت پسندی ،وسعت نظر،باریک بینی، فنی اوصاف اور قوت مشاہدہ سے اردو ناول نگاری کی نئی راہ ہموار کی۔ انھوں نے شعوری طور پر اردو ناول کوفنی اوصاف کا حامل بنانے کی بھی کوشش کی۔ مرزا ہادی علی رسوا نے لکھنؤ کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا، وہ اس ماحول میں پیدا ہوئے، وہاں ان کی پرورش ہوئی اور مختلف ملازمتیں کیں ،مختلف طبقوں سے سماجی رسم ورواج بڑھائے، چنانچہ ان کی نظروں میں سماج کا اعلی طبقہ اور نچلا طبقہ بھی رہا ،وہ ہر کسی کی عادات و اطوار سے واقف تھے اسی لیے انھوں نے اپنے ناولوں میں ،جس طبقے کی ترجمانی کی ،وہ ان کے سماجی و ثقافتی شعور کا پتہ ہمیں دیتا ہے۔ زیر نظر کتاب "انتخاب مرزا ہادی رسو" محمد حسن کی تصنیف ہے ،اس کتاب میں انھوں نے مرزا رسوا کی بعض تصانیف مثلا امراؤ جان ادا، شریف زادہ، ذات شریف ، مرقع لیلی مجنوں وغیرہ جیسی تصانیف کے ایسے اقتباسات یکجا کیے ہیں جن سے مرزا رسوا کے طرز فکر اور اسلوب بیان کا اندازہ ہوتا ہے۔
लेखक: परिचय
नाम मिर्ज़ा मुहम्मद हादी था, रुस्वा तख़ल्लुस करते थे। सन् 1858 में लखनऊ में पैदा हुए। उनका सम्बंध माझंदान से था। उनके पूर्वज मुग़ल काल में हिंदुस्तान आए और उनके परदादा ने अवध में निवास किया। मिर्ज़ा ने फ़ारसी, अरबी और दूसरे विषयों में ज्ञान प्राप्त किया। आरम्भ में उनके पिता ने ख़ुद शिक्षा दी। विशेष रूप से गणित का पाठ उन्हीं से लिया लेकिन जब रुस्वा सोलह वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। ख़ानदानी जायदाद से गुज़र बसर होने लगी। शिक्षा प्राप्ति की रूचि व लालसा बहुत अधिक थी। इसलिए अध्ययन में व्यस्त थे। सन् 1836 में पत्रकारिता से जुड़े लेकिन जल्द ही दूसरी मुलाज़मत भी शुरू की। लेकिन किसी काम में उनका मन कभी न लगा। एक ज़माने में रसायनशास्त्र की तरफ़ आकर्षित हुए तो फिर उसी के हो कर रह गए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में लखनऊ के एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। उसी ज़माने में प्राईवेट तौर पर कुछ परीक्षाएं भी पास कीं। सन् 1888 में रेड क्रिस्चियन कॉलेज में पढ़ाने लगे लेकिन 1901ई. में हैदराबाद चले गए और वहीं मुलाज़मत इख़्तियार की, लेकिन उनकी सेहत वहाँ अच्छी नहीं रही, इसलिए लखनऊ आगए। दुबारा 1919ई. में हैदराबाद गए और दारुलतर्जुमा से सम्बद्ध हो गए। कई किताबों के अनुवाद किए। दर्शनशास्त्र के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित एक किताब लिखी।
मिर्ज़ा हादी रुस्वा नाबिग़ा रोज़गार थे। विभिन्न विषयों तक उनकी पहुँच थी। दर्शन, तर्कशास्त्र, गणित, चिकित्सा, धर्मशास्त्र, रसायनशास्त्र, संगीत और खगोल विज्ञान के अलावा शायरी से उनकी दिलचस्पी साबित है। कहा जाता है कि उन्होंने शॉर्ट हैंड और टाइप का बोर्ड बनाया। उन्होंने बहुत कम समय में चार उपन्यास लिखे जिनमें “उमराव जान अदा” सबसे ज़्यादा मशहूर है और उसी उपन्यास के आधार पर उनकी शोहरत और महानता है। बहरहाल उनके उपन्यासों के नाम हैं “इफ़शा-ए-राज़”(1896ई.), “उमराव जान अदा”(1899ई.), “ज़ात शरीफ़”(1900ई.), “शरीफ़ ज़ादा”(1900ई.) और “अख़्तरी बेगम”(1924ई.)।
मिर्ज़ा रुस्वा उपन्यास के सन्दर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए “इफ़शा-ए-राज़” के प्रस्तावना में, “ज़ात शरीफ़” की भूमिका में और “उमराव जान अदा” में विभिन्न अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। “उमराव जान अदा” में मुंशी मुहम्मद हुसैन ने जो कुछ कहा है वो दरअसल उनके ज़ेहन व दिमाग़ की भी फ़िक्र है। जुमले हैं: “लखनऊ में चंद रोज़ रहने के बाद अह्ल-ए-ज़बान की असल बोल-चाल की ख़ूबी खुली। अक्सर नॉवेल नवीसों के बेतुके क़िस्से, मस्नूई ज़बान और तास्सुब आमेज़ बेहूदा जोश देने वाली तक़रीरें आपके दिल से उतर गईं।”
वास्तव में रुस्वा को ये एहसास था कि उपन्यास को अपने ज़माने के हालात को प्रतिबिम्बित करना चाहिए। चरित्र चित्रण मात्र अतिश्योक्ति पर आधारित न हो बल्कि इसमें कुछ तथ्य हों, उपन्यास कला के तक़ाज़े भी पूरा करे और उसकी भाषा चरित्र के अनुरूप हो। इन बातों को अगर ज़ेहन में रखें तो उनके अहम उपन्यास “उमराव जान अदा” की बहुत सी विशेषताएं स्वतः स्पष्ट होजाती हैं।
“उमराव जान अदा” पर टिप्पणी करते हुए अली अब्बास हुसैनी ने लिखा था कि ये रंडी की कहानी उसी की ज़बान है। लेकिन यह मत उपन्यास के तथ्यों को पेश करने से वंचित है। वेश्या की कहानी के पृष्ठभूमि में मिर्ज़ा रुस्वा ने अपने समय के लखनऊ का जो चित्रण किया है, वो उन्हीं का हिस्सा है। हैरत होती है कि कुछ लोग रंडी और रंडी बाज़ी के इर्दगिर्द ही इस उपन्यास का जायज़ा लेते हैं, हालाँकि मिर्ज़ा रुस्वा की चेतना उन सीमाओं में सीमित नहीं थी। यह उपन्यास लखनऊ की पतनशील सभ्यता का एक चित्रशाला है जिसके हवाले से बहुत सी तस्वीरें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। इस सम्बंध में ख़्वाजा मुहम्मद ज़करिया ने लिखा है:
“-۔ उपन्यास के आरम्भ में रुस्वा हमें अवध की एक ग़रीब बस्ती के समाज से परिचय कराते हैं, फिर दीर्घा के हवाले से नवाबों की संस्कृति को सामने लगाया गया है, फिर उमराव जान के दीर्घा से फ़रार के बाद उस ज़माने के असुरक्षित रास्तों, चोरों डाकूओं की कार्यवाईयों, राजनीतिक लापरवाही और फ़ौजों की बुज़दिलियों की तरफ़ स्पष्ट संकेत किए गए हैं। उपन्यास के आख़िरी हिस्से में अकबर अली ख़ां के हवाले से मध्यम वर्ग के घरों के नक़्शे बयान किए गए हैं, जो अब तक उपन्यासकार के क़ाबू में नहीं आसके थे। ग़रज़ उस युग के अवध के निम्न, मध्यम और उच्च सभी वर्गों के सामाजिक जीवन को इस उपन्यास का विषय बनाया गया है।
बहरहाल, चरित्र चित्रण, मनोवैज्ञानिक स्थिति और प्रतिक्रिया, संस्कृति और समाज की अभिव्यक्ति आदि के आधार पर इसकी गिनती उर्दू के सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में की जाती है। इस पर ख़ुरशीद उल-इस्लाम ने एक मूल्यवान लेख लिखा जो इस उपन्यास की विशेषताओं और महत्व को स्पष्ट कर देता है।
“शरीफ़ ज़ादा” और “ज़ात शरीफ़” में वो कैफ़-ओ-कम नहीं है जो “उमराव जान अदा” में है। “शरीफ़ ज़ादा” के बारे में कहा जाता है कि ये रुस्वा की अपनी जीवनी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रुस्वा ने जिस तरह ज़िन्दगी गुज़ारी है वो सबकी सब इसमें मौजूद है।
यहाँ इस बात की तरफ़ इशारा करता चलूँ कि एक उपन्यास “शाहिद-ए-राना” के बारे में कहा जाता है कि रुस्वा का उपन्यास इससे बहुत मिलता-जुलता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों में जिस तरह का फ़र्क़ है वो बहुत स्पष्ट है और ये तूफ़ानी बहस है, जिसे मैं यहाँ छेड़ना नहीं चाहता। बहरहाल, रुस्वा अपने वक़्त के एक ऐसे Genius थे कि उर्दू तारीख़ में उनका स्थान सुरक्षित है।
 For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org
For any query/comment related to this ebook, please contact us at haidar.ali@rekhta.org