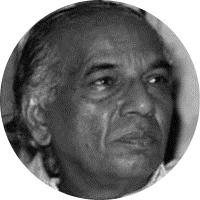मसऊद हसन रिज़्वी अदीब
मसऊद साहब मेरे उस्ताद थे, मेरे बुज़ुर्गों के दोस्त थे, बा’ज़ अदबी उमूर में रहनुमा थे, फिर भी मैं नहीं कह सकता कि मैं उनको बहुत क़रीब से जानता हूँ। मैं उनसे ज़्यादा उनके भाई आफ़ाक़ को जानता हूँ जिनसे मेरी मुलाक़ात मसऊद साहब ही के ज़रिए से हुई। दर अस्ल मसऊद साहब को बहुत क़रीब से जानना मुश्किल भी था। वो कम आमेज़ होने की हद तक गोशा नशीन थे। वक़्त का काफ़ी हिस्सा बहुत बड़ा हिस्सा, मुताला-ओ-तहक़ीक़ में सर्फ़ कर देते थे और घरवालों को भी उन मशाग़िल में दाख़िल और हारिज नहीं होने देते थे। ऐसा नहीं था कि वो “क़ुतुब अज़ जानमी जंबद” क़िस्म के लोगों में रहे हों। उनका अपना ज़ाती तांगा था उस पर सवार हो कर वो यूनीवर्सिटी भी जाते और दोस्तों के यहाँ भी, लेकिन ये आमद-ओ-रफ़्त न बहुत ज़्यादा थी न बहुत कम, कम आमेज़ी के बावजूद उनके दोस्त बहुत थे और कई तबक़ों में थे। फिर क़दीम-ओ-जदीद शागिर्दों का एक हलक़ा था लेकिन घरवाले क्या दोस्त, क्या शागिर्द, सब के फ़ासले और क़ुर्बतें मुतअय्यन थीं। वो हमेशा अपने को लिये दिये रहते और किसी को हदूद से तजावुज़ न करने देते थे। वज़ादारी, रिवायत और शराफ़त-ए-नफ़्स ने जो क़ुयूद आइद कर दिए थे उनसे वो ख़ुद भी मुनहरिफ़ थे।
वो बड़े रख-रखाव के इंसान थे और रख-रखाव को बेतर्तीबी, बेनज़्मी, बे एहतियाती, हिफ़्ज़-ए-मरातिब से बेपर्वाई या इफ़रात-ओ-तफ़रीत से लगाव नहीं। उनकी ज़िन्दगी एक नज़्म, एक तर्तीब, एक तवाज़ुन का नाम थी और उनका कमाल ये था कि उन्होंने अस्सी बरस से भी ज़्यादा तवील ज़िन्दगी में इस रब्त-ओ-तवाज़ुन को बिगड़ने न दिया। हिफ़्ज़-ए-मरातिब का ये हाल था कि अगर कोई मुलाक़ाती रोज़मर्रा के कामों से आता तो वो उससे अपने वसी मकान के बरामदे ही में मिल लेते। वहाँ एक हश्त पहल या गोल (मुझे ठीक से याद नहीं) मेज़ पर पड़ी रहती थी जिसके गिर्द दो तीन कुर्सियां होतीं, ये गोया उनका ऐवान-ए-आम था। यहाँ सरसरी समाअत और सरसरी फ़ैसले नहीं होते बल्कि हस्ब-ए-मर्तबा तफ़सीली गुफ़्तगू होती। हर आने वाले की हस्ब-ए-मर्तबा तवाज़ो होती। फ़र्माइश के बग़ैर ही चांदी के नक़्शी ख़ासदान में फ़ौरन पान की गिलोरियां पेश होतीं, चाय का वक़्त होता तो चाय भी आती या गर्मियों के ज़माने में ठंडा शर्बत। अगर किसी से बेतकल्लुफ़ी होती तो बेवक़्त भी चाय मंगा ली जाती। ये तवाज़ो हर कस-ओ-नाकस पर ज़ाए न की जाती। आख़िर उन्हें ये भी तो फ़ैसला करना होता था कि वो अपने नपे तुले वक़्त में से किसी को कितना दें। मामूली काम वाले अपना काम कर के बेताख़ीर वापस जाते लेकिन अगर कोई ऐसी हस्ती होती जिससे इल्मी या अदबी गुफ़्तगू की किसी सतह पर गुंजाइश होती तो उसके लिए वक़्त निकल आता। हद ये है कि अदबी कामों से दिलचस्पी रखने वाले शागिर्दों की पज़ीराई भी अच्छी तरह होती।
मैंने मसऊद साहब को सबसे पहले 1931ई. में अली अब्बास हुसैनी के यहाँ देखा था। उस वक़्त मैं सातवीं जमात में पढ़ता था मगर लिखने पढ़ने का चस्का उस वक़्त भी था और दो बरस पहले ही मेरे मज़ामीन और अशआर अख़बारात-ओ-रसाइल में शाए होने लगे थे। उस वक़्त मसऊद साहब पर इस मिसरे का इतलाक़ नहीं हो सकता था कि “चहल साल उम्र-ए-अज़ीज़त गुज़श्त” अड़तीस बरस का सिन ऐन जवानी कहिए। उसके बाद वो अधेड़ हुए, रीडर से प्रोफ़ेसर हो गए। पेंशन पा गए। यहाँ तक कि हमसे जुदा भी हो गए। लेकिन 1975ई. में इंतिक़ाल के वक़्त तक उनमें तब्दीली नहीं आने पाई। वही रख-रखाव, वही नोक पलक बाक़ी रही। उनके दोस्तों में कोई नया इज़ाफ़ा नहीं हुआ लेकिन जो पहले के दोस्त थे वो छूटे भी नहीं। वो वफ़ादारी बशर्त-ए-उस्तुवारी के क़ाइल थे।
मैं पढ़ने वालों को इस ग़लतफ़हमी में मुब्तला नहीं करना चाहता कि मसऊद साहब मर्दुमबेज़ार या मग़रूर थे। वो यार बाश नहीं थे लेकिन उनके दोस्तों का हलक़ा काफ़ी वसी था। उसमें लखनऊ के वो नवाब भी थे जो “चुनिया बेगम” के आशिक़ और “पाली” के मर्द-ए-मैदान थे। वो बांके भी थे जो क़दीम फ़ुनून हर्ब-ओ-ज़र्ब में ताक़ थे, वो दास्तानगो भी थे जिनकी लिसानी नींद उड़ा देती थी और वो ख़तीब भी थे जो सुनने वालों को महव-ए-हैरत कर देते थे। उनमें वो मुरक़्क़ा हाय इबरत भी थे जो साबिक़ ख़ानदान-ए-शाही के चश्म-ओ-चराग़ या अमली-ओ-अदबी ख़ानवादों की यादगार थे। अख़बारों के मुदीर और स्कूलों कॉलेजों के उस्ताद, मुज्तहिद, तबीब और डाक्टर मुग़न्नी और शायर, अफ़साना नवीस और नक़्द-निगार, तर्जुमे के माहिर और निसार, मर्सिया ख़्वाँ और मर्सिया गो, मज़ाह नवीस और नक़्द निगार, समाजी कारकुन और सियासत के अलमबरदार, ख़त्तात और मुसव्विर, ताजिर और साइंसदां भी थे। इस मुख्तलिफ़-उन-न्नौ और रंगारंग मज्मे में हर जगह मसऊद साहब की मख़सूस जगह थी और मसऊद साहब के हाँ उनकी मख़सूस पज़ीराई। उनमें से किसी मज्मे में भी वो न तो इस तरह घुल मिल जाते कि उसका तख़्मीरी हिस्सा बन जाएं और न बेगानावार तमाशाई मिसाल, किसी नामालूम गोशे ही में बैठे रहते। हर जगह अपनी संजीदा इन्फ़िरादियत को संभाले रहते लेकिन दूसरों पर इन्फ़िरादियत को वारिद न करते। अह्ल-ए-इल्म और बुज़ुर्गों का ख़ुद भी एहतिराम करते और बराबर वालों और दोस्तों को भी हद से बढ़ने की इजाज़त न देते। अपने छोटों की बात भी ख़मोशी से सुनते। लताइफ़-ओ-ज़राइफ़ का सिलसिला शुरू होता तो अपनी जानिब से भी कुछ संजीदा इज़ाफ़े करते। अदबी और इल्मी मुबाहिसों में अपनी बात पूरे ज़ोर-ओ-शोर से कहते। दूसरों की सुनते, जवाब-उल-जवाब देते लेकिन लोग जानते थे कि मसऊद साहब न इस हद के आगे जाएंगे न किसी और को जाने देंगे।
मैं ये कहने में फ़ख़्र महसूस करता हूँ कि मैं उनका शागिर्द हूँ। लेकिन मैं शागिर्द बाद में बना और नियाज़मंद पहले। मसऊद साहब को मैंने स्कूल के इब्तिदाई दर्जात ही से पढ़ना शुरू कर दिया था और उससे पहले शनासाई रसाइल के ज़रिए से हुई। ज़ियारत भी उसी ज़माने में हुसैनी साहब के यहाँ हुई। उस ज़माने में अली अब्बास हुसैनी जो दिल्ली कॉलेज में तारीख़ पढ़ाते और रूमानी अफ़साने लिखते थे। उनके क़रीब तरीन अदबी दोस्तों में अख़्तर अली तिलहरी, ख़्वाजा अतहर हुसैन और मसऊद साहब ही थे। ये लोग उनके यहाँ अक्सर आते। ख़्वाजा साहब और तिलहरी साहब तक़रीबन रोज़ाना और मसऊद साहब कभी कभी। उस वक़्त तक हुसैनी साहब से मेरी सिर्फ़ एक दूरी क़राबत थी। वो सय्यद आज़म हुसैन आज़म (साबिक़ मुदीर सरफ़राज़) और शमीम करहानी के हक़ीक़ी मामूं थे और आज़म हुसैन व शमीम मेरे मामूं के यक जद्दी भतीजे थे। ग़ालिबन तीन पुश्त ऊपर ये दोनों शाख़ें एक नुक़्ते पर मिल जाती थीं। मैं जब कभी लखनऊ जाता तो आज़म भाई से मिलने ज़रूर जाता। वो हुसैनी के साथ ही रहते थे और सह रोज़ा “सरफ़राज़”जो बाद में रोज़ाना हो गया था और अब सिर्फ़ हफ़्तावार भी नहीं रह गया, के नायब मुदीर भी थे और एक इल्मी और अदबी रिसाला “अदब” भी निकालते थे। “अदब”से हुसैनी, तिलहरी और ख़्वाजा अतहर (जिन्होंने एक ज़माने में रिंद के फ़र्ज़ी नाम से बहुत अच्छे मज़ाहिया मज़ामीन लिखे थे) ख़ास वाबस्तगी रखते थे। ये तीनों सरकारी मुलाज़िम थे और किसी अख़बार या रिसाले से वाबस्तगी सरकारी क़वाइद-ए-मुलाज़िमत के ख़िलाफ़ थी। लेकिन वाक़िफ़ान-ए-कार का कहना ये है कि ये तीनों हज़रात उसके बानियों में थे और ग़ालिबन मसऊद साहब को भी दामे और क़लमे उनके साथ थे। दोस्ती के अलावा अदब के इदारती उमूर में मश्वरत भी मसऊद साहब हुसैनी साहब के यहाँ खींच लाती थी। इसके अलावा आज़म, आरज़ू लखनवी के शागिर्द थे, और बा’ज़ ख़ानगी मजबूरियों की बिना पर आरज़ू को आज़म हुसैनी साहब के मकान ही पर बुला लाते थे। उनकी ज़बानदानी और शायरी दोनों ही जाज़िब-ए-तवज्जो थीं। उनकी वजह से भी मसऊद साहब अक्सर आने लगे थे। यूँ भी इन अस्हाब-ए-अर्बा (मसऊद तिलहरी, हुसैनी और अतहर) में बड़ी ज़ेहनी यगानगत थी। जब ये सब जमा होते तो इधर उधर की बातें होतीं, शायरी होती, अफ़साने और मज़ामीन सुनाए जाते, नक़्द-ओ-तब्सिरा होता, हल्की और क़ौमी मसाइल पर तबादला-ए-ख़्याल होता। उनमें, मैं भी दख़ल दर माक़ूलात करता और कोई माने या न माने अपनी सी कहता रहता। फिर 1935ई. से मुस्तक़िल तौर पर लखनऊ आ गया। अब ये मुलाक़ातें जल्द जल्द होने लगीं। उनकी ख़िदमत में ये चंद साल इस नियाज़मंदी के साथ गुज़रे कि मैं उनकी सुख़न शनाशी और दीदा-वरी का क़ाइल हो गया और अपने को उनके ख़ासा क़रीब पाने लगा। लेकिन याद दिलाता चलूँ कि ये क़ुरबत भी दूरी की क़ुरबत थी, मैंने उसी ज़माने में मसऊद साहब की “हमारी शायरी” पढ़ी। ये किताब दर अस्ल नक़्द-ए-अदब में उस मग़्रिबज़दगी के ख़िलाफ़ सदा-ए-एहतिजाज थी जो बीसवीं सदी के पहले रुबा में उर्दू शायरी के इक्तिसाबात के कुल्ली इनकार की शक्ल इख़्तियार करने लगी थी। मसऊद साहब ने उर्दू शायरी के बहुत से इसरार-ओ-अवारिज़ के चेहरे से नक़ाब उठा दी।
मसऊद साहब के दोस्तों में चंद हज़रात और थे। शेख़ मुमताज़ हुसैन उस्मानी (एडिटर “अवध पंच”) हकीम साहब आलम (मालिक दवाख़ाना “मोरन-उल-अदविया) मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी (मुसन्निफ़ “मन कीसतम” और मुतर्जिम “तारीख़-ए-अदब उर्दू” मुअल्लिफ़ा राम बाबू सक्सेना) सय्यद अली नक़ी सफ़ी और मौलाना ज़फ़र-उल-मलिक (मुदीर “अलनाज़िर”) ये सब के सब लखनऊ की अदबी अंजुमनों के सुतून थे। और ख़ुदा इन्हें बख़्शे, बड़े सिक़्क़ा और रुत्बा शनास लोग थे। शेख़ मुमताज़ हुसैन उस्मानी उस दौर के अदबी माहौल में क़ुतुब-उल-क़ुताब की हैसियत रखते थे। उनके यहाँ जाने वाले बहुत थे लेकिन वो शायद ही किसी के यहाँ जाते हों, अलबत्ता खरे दोस्त और खुले दिल से दुश्मन थे। वो मसऊद साहब को बहुत अज़ीज़ रखते थे। एक ज़माने में मसऊद साहब के एक हम वतन, बेख़ुद मोहानी ने “हमारी शायरी” के ख़िलाफ़ रिसाला बाज़ी शुरू की, पहले की छोटे छोटे रिसाले मसलन “आईना-ए-तहक़ीक़”लिखे और बाद में उन सबको यकजा करके “गंजीना-ए-तहक़ीक़”के नाम से तहक़ीक़ी किताब की सूरत में शाए करा दिया। इस पर मुमताज़ हुसैन उस्मानी ने “अवध पञ्च” में “गंजा-ए-ना तहक़ीक़” के नाम से वो ले दे की। बेचारे बेख़ुद तिलमिला उठे।
हकीम साहब आम लखनऊ के शुरफ़ा में थे। बहुत अच्छे तबीब, माक़ूल शायर और अच्छे अदब नवाज़ दोस्त थे। नख़ास में उनका मतब “मादन-उल-अदविया”था। कभी कभार मतब में मुलाक़ात हो जाती, कभी उनके बेहद बेतकल्लुफ़ और ख़ुश मज़ा दावतों में यकजाई हो जाती और कभी कभी उन मक़ासिदों में उन मुलाक़ातों के दौरान कभी आपस में मुस्कुराहटों और लतीफों का तबादला होता और कभी इल्मी, अदबी या सियासी मसले पर कुछ तबादला-ए-ख़यालात मगर बहुत नपा तुला और मुख़्तसर। हकीम साहब की तबाबत से भी कभी इस्तिफ़ादा करते लेकिन ग़ालिबन कशिश का एक सबब ये था कि हकीम साहब का ख़ानदान अवध के शाही तबीबों का ख़ानदान था।
अल्लामा सफ़ी लखनऊ से मुलाक़ातें ख़ालिस अदबी नौइयत की होतीं, कभी मुशायरों और मक़ासिदों में और कभी शिया कान्फ़्रेंस के इजलासों में, ये कान्फ़्रेंस एक समाजी इदारा था। अख़बार “सरफ़राज़” और “शिया यतीमख़ाना”दो इदारे उसके मातहत चलते थे। कई इस्लाही तहरीकें उस कान्फ़्रेंस ने चलाईं इसलिए उल्मा से इसका टकराव हुआ और वो उससे बिल्कुल किनारा-कश हो गए। ख़्याल ये था कि उल्मा की अलैहदगी के बाद कान्फ़्रेंस ख़त्म हो जाएगी। उस आलम में जिन लोगों ने उसको संभाला उनमें यही अर्बाब-ए-अर्बा थे।
मसऊद साहब बड़े ही मरन्जान मरंज क़िस्म के इंसान थे। वो अच्छे मुसलमान और अच्छे शिया थे लेकिन उनको तास्सुब और तंगनज़री की हवा नहीं लगी थी। दो एक बार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने किसी मुसलमान को हिंदू के मुक़ाबले में और शिया को सुन्नी के बारे में उसकी ग़लतियों पर टोक दिया है। यूनीवर्सिटी की सियासत में एक बार डाक्टर बीरबल साहनी और डाक्टर वली-उल-हक़ एक दूसरे के मुक़ाबिल सफ़-ए-आरा हो गए। मसऊद साहब ने डाक्टर साहनी का साथ न छोड़ा।
मज़हबी होने की वजह से उन्होंने “अंगारे”की इशाअत पर बड़ी रजामंदी का इज़हार किया। लेकिन उसके मुसन्निफ़ीन में सज्जाद ज़हीर उनकी यूनीवर्सिटी के तालिब इल्म रह चुके थे और अहमद अली उनके रफ़ीक़ थे। उनसे भी और डाक्टर रशीद जहाँ से भी उनके ताल्लुक़ात कभी नाख़ुशगवार न हुए। इख़्तिलाफ़ ख़्याल का एहतिराम करना और अपने ख़्याल को तर्क किए बग़ैर दूसरे की आज़ादी-ए-ख़्याल को हक़ बजानिब समझना इल्मी रवादारी का ख़ास्सा है और ये ख़ुसूसियत मसऊद साहब ने अपना ली थी।
मसऊद साहब की जवानी तक ऐसे कई असहाब थे जो अपने नामों के साथ “सुम्म-ए-लखनवी” लिखा करते थे। मसलन देहलवी सुम्म-ए-लखनवी, मतलब ये था कि पहले कहीं और जगह के रहने वाले थे बाद में सुकूनत तर्क कर दी और लखनवी हो गए उसमें एक तरफ़ तो उनके इस जज़्ब-ओ-ख़ुलूस-ओ-फ़ख़्र का इज़हार होता था जो अपने वतन के लिए उनके दिलों में घर किए हुए था। और दूसरी तरफ़ लखनवियत के फ़ख़्र का भी मुज़ाहरा होता था। बा’ज़ लोग जो ज़्यादा शदीद लहजा थे वो कहते कि ये असल में सुम्म-ए-इज़हार बरअत के तौर पर लिखते हैं कि हमें ख़ालिस लखनवी न समझ लिया जाए। मसऊद साहब भी सुम्म-ए-लखनवी थे ये क्योंकि उनका असली वतन उन्नाव के पास एक क़स्बा नेवतनी था। उन्नाव और लखनऊ में कुछ फ़ासिला ज़्यादा नहीं है। ग़ालिबन पच्चीस तीस मील का फ़ासिला होगा। उसका शुमार मुज़ाफ़ात-ए-लखनऊ में ही करना चाहिए। लेकिन कानपुर से क़ुरबत ज़्यादा होने की वजह से ज़ेहनों में उसका तसव्वुर लखनऊ से क़ुरबत का कम ही है। मसऊद साहब को लखनऊ से इश्क़ था। ये उसी इश्क़ का नतीजा था कि उन्होंने यहाँ मकान बना लिया और यहीं रह पड़े। इस मानी में वो सुम्म-ए-लखनवी हो गए। लेकिन मसऊद साहब को लखनऊ से जो गहरी वाबस्तगी थी उसके पेश-ए-नज़र उन्हें सुम्म-ए-लखनवी वाली सफ़ में शामिल करना ज़्यादती मालूम होती है। मरने से पहले वो सौ फ़ीसद लखनवी हो चुके थे।
वो लखनऊ के लिए “ताज़ा वारदान-ए-बिसात” की हैसियत रखते थे लेकिन लखनऊ की मुहब्बत में वो लखनऊ के क़दीम बाशिंदों से भी आगे थे। उन्हें लखनऊ के ज़र्रे ज़र्रे से मुहब्बत थी। अनीस और वाजिद अली शाह उनकी ज़िंदगीभर की अदबी और तख़्लीक़ी काविशों का मर्कज़ रहे। उनके अलावा लखनऊ उन पर फ़िदा हो या न हो, लेकिन वो फ़िदा-ए-लखनऊ ज़रूर थे। ये मुहब्बत अदबी और सक़ाफ़ती ज़्यादा थी और इलाक़ाई कम। यानी उन्हें लखनवी सक़ाफ़त और लखनऊ के मर्कज़-ए-अदब से दिलचस्पी थी। उन्होंने यहाँ की मसनवियाँ, यहाँ के क़सीदे, यहाँ के वासोख़्त, यहाँ की दास्तानें सब पढ़ डाली थीं, तारीख़-ए-अवध पर भी उनकी अच्छी नज़र थी। उनका अक़ीदा था कि वाजिद अली शाह के साथ इन्साफ़ नहीं किया गया, अंग्रेज़ों ने हुकूमत छीनने की ख़ातिर से बहुत सी रिवायतें गढ़ीं और गढ़वाईं। महल सराओं का माहौल और रंगरलियाँ भी ज़रूर थी, लेकिन ये सब मुद्दतों से लाज़िमा-ए-रियासत बन गई थीं। वाजिद अली शाह को रक़्स-ओ-सुरूद से दिलचस्पी ज़रूर थी लेकिन ये दिलचस्पी फ़न्नी थी। उसको लहू-ओ-लुअब से वाबस्ता करना दुरुस्त नहीं। ये और इस क़िस्म की बातें उनकी सुह्बत में अक्सर सुनने को मिलतीं और वो सब के लिए शहादत पास रखते थे। उन्होंने वाजिद अली शाह, अवध और लखनऊ पर उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी में बहुत सा मवाद जमा कर लिया था। वो लिखना भी चाहते थे लेकिन ज़ालिम वक़्त ने फ़ुर्सत न दी।
मसऊद साहब कोई तिरासी बरस पहले ख़ास मुहर्रम के महीने में पैदा हुए। उनको मर्सियों से जो ख़ास शग़फ़ था शायद उसमें अदबी लगाव के अलावा तारीख़-ए-पैदाइश को भी दख़ल रहा हो, मसऊद साहब ख़ुद न तो मर्सिया-गो थे न मर्सियाँ-ख़्वाँ, लेकिन मर्सिए की तारीख़-ओ-तफ़सीर-ओ-तन्क़ीद पर उनकी नज़र गहरी थी, अरबी मर्सिया हो या फ़ारसी मर्सिया उन्होंने सब कुछ छान लिया था। अरबी के आलिम नहीं थे मगर ख़ासी सलाहियत रखते थे, दूसरी ज़बानों के हज़ीना रिसाई और रज़मिया अदब का भी उन्होंने ख़ुसूसी मुताला किया था। दुनिया के सबसे बड़े मर्सिया निगार, मीर अनीस के हालात-ए ज़िन्दगी और कलाम का तो शायद ही कोई पहलू ऐसा रहा होगा जो उनकी हमागीर नज़र से बच रहा हो। अनीस के अलावा क़दीम-ओ-जदीद मर्सिया निगारों पर भी उन्होंने जम कर काम किया था और मरासी का एक नायाब ज़ख़ीरा जमा कर लिया था।
मसऊद साहब ने तहक़ीक़ के लिए मर्सिए का मौज़ू मुंतख़ब किया। ग़ालिबन अदब मज़हब और लखनऊ से लगाव भी मुहर्रिक रहे होंगे, अल्लामा शिबली ने “मवाज़ना अनीस-ओ-दबीर”लिख कर इस मौज़ू से दिलचस्पी बढ़ा दी थी। “मवाज़ना”की इशाअत के बाद अनीस-ओ-दबीर दोनों ही के तरफ़दारों ने अपने अपने ममदूहीन की सवानेह उमरियां लिखना शुरू कीं, कुछ लोगों ने “मवाज़ना”का जवाब भी लिखा। उनमें “अलमीज़ान”की सी मुतवाज़िन किताब भी थी और “रद्दुलमवाज़ना”जैसी ग़ैर मुतवाज़िन भी। नवलकिशोर प्रेस से मुख़्तलिफ़ मर्सिया निगारों के मरासी की बहुत सी जिल्दें शाए हुईं। बा’ज़ दूसरे मताबे ने भी उसमें हाथ बटाया। ज़मीर, दिलगीर, फ़सीह, ख़लीक़, दबीर, अनीस, मोनिस, रशीद, वहीद, ताश्शुक़ वग़ैरा का कलाम मतबूआ शक्ल में मिलने लगा था। लेकिन इस सिन्फ़ पर किसी ने जम कर काम नहीं किया था। तारीख़-ए-मर्सिया पर “दरबार-ए-हुसैन” ग़ालिबन वाहिद किताब थी लेकिन इस तस्नीफ़ पर सही मानों में तारीख़ का इतलाक़ नहीं होता कुछ जुज़्वी इशारे मवाज़ना वग़ैरा में भी थे। सवानेह बेहद तिश्ना और पाया-ए-एतिबार से साक़ित थे। मर्सियों और सलामों के मतन अग़्लात से पुर और अलहाक़ी कलाम की बिना पर मशकूक थे। मसऊद साहब ने उस काम में नज़्म-ओ-ज़ब्त लाने का बीड़ा ख़ुद उठाया और सारी ज़िन्दगी उस काम के लिए वक़्फ़ कर दी।
उन्होंने ईरानी मर्सिया-गोई पर हरावली काम किया है। अफ़सोस कि ये किताब अभी तक शाए नहीं हो सकी है, ममदूह को मरते दम तक उसकी इशाअत का ख़्याल था। ग़ालिबन अब उनके साहबज़ादे नय्यर मसऊद इस तरफ़ तवज्जो करें। हिंदुस्तानी मरासी के क़दीम नमूनों का पता न था। उन्होंने बड़ी कोशिश-ओ-काविश से क़ुदमा का कलाम जमा किया। उन्होंने अपने ज़ाती कुतुबख़ाने के लिए जो ज़ख़ीरा-ए-मरासी जमा किया था वो बेमिसाल था। बा’ज़ लोगों ने उनको तवज्जो दिलाई कि इस ज़ख़ीरे को किसी बुज़ुर्ग तर कुतुबख़ाने में महफ़ूज़ कर दिया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा शाइक़ीन-ए-अदब इससे फ़ायदा उठा सकें और इसकी मुनासिब देख-भाल हो सके। ये सवाल कई बार उठा लेकिन ग़ालिबन वो उस ज़ख़ीरे की जुदाई गवारा न कर सकते थे। इंतिक़ाल से कुछ दिन क़ब्ल उन्हें भी ये ख़्याल होने लगा कि इस ज़ख़ीरे को महफ़ूज़ कर देना चाहिए। ख़ुशक़िस्मती से आले अहमद सुरूर (साबिक़ सदर शोबा उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी) और डाक्टर मोहम्मद हसन (साबिक़ सदर शोबा उर्दू जम्मू-ओ-कश्मीर यूनीवर्सिटी) दोनों ही को यक वक़्त ये ख़्याल आया कि ये ज़ख़ीरा अपनी यूनीवर्सिटी के कुतुबख़ाने के लिए महफ़ूज़ कर दें।
मसऊद साहब ने इस सिलसिले में मुझसे राय मांगी क्योंकि उन्हें मालूम था कि अलीगढ़ से लगाव के अलावा मुझे रियासत-ए-जम्मू-ओ-कश्मीर से भी इलाक़ा ख़ास रहा है, दोनों ही ने एक ही रक़म तजवीज़ की थी। लेकिन डाक्टर मुहम्मद हसन ने तजवीज़ पहले पेश की थी। मुझे महसूस हुआ कि मसऊद साहब एक तरफ़ तजवीज़ की अव्वलियत और अपने शागिर्द की पेशकश और दूसरी तरफ़ अपने एक साबिक़ हमकार की पेशकश और अलीगढ़ यूनीवर्सिटी की इल्मी अहमियत के दर्मियान फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए मेरी राय जानना चाहते हैं। मेरे लिए भी वही उलझन थी लेकिन मैंने कहा कि अगर अब रियासत-ए-जम्मू कश्मीर में उर्दू का ख़ासा मुक़ाम है लेकिन वहाँ की यूनीवर्सिटी को अलीगढ़ की तरह मर्कज़ियत हासिल नहीं है। तारीख़ी और इल्मी अहमियत की बिना पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लाइब्रेरी में ज़्यादा लोग उससे इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने भी अलीगढ़ ही के हक़ में फ़ैसला कर दिया और अब ये नायाब ज़ख़ीरा वहीं मौजूद है। उस ज़ख़ीरे में सिर्फ़ क़दीम ही नहीं बल्कि जदीद मरासी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं।
मर्सिया का दौर-ए-जदीद अनीस-ओ-दबीर से शुरू होता है। इस दौर जदीद की बुनियाद तो मीर ज़मीर ने रखी लेकिन इस की तकमील दौर-ए-अनीस में हुई। मसऊद साहब ने अनीस ही को तहक़ीक़ात का मौज़ू बनाया। मसऊद साहब बीसवीं सदी के “अनीसिए” थे, आपस में लड़ाने के लिए नहीं बल्कि वो अनीस के खुल्लम खुल्ला तरफ़दार थे। और दबीर को इस मर्तबे का शायर नहीं समझते थे। इस मुआमले में वो अल्लामा शिबली के हमनवा थे। किसी बात में भी दबीर की फ़ौक़ियत तस्लीम करने को तैयार नहीं थे, मसलन दबीर के बा’ज़ बेनिया मरसिए अच्छे समझे जाते हैं, बी.ए. की तालिब इल्मी के ज़माने में एक दिन मैं मसऊद साहब के दौलत कदे पर हाज़िर हुआ। ग़ालिबन अली अब्बास हुसैनी भी वहाँ मौजूद थे। बातों बातों में मैंने कहा कि मिर्ज़ा साहब के बा’ज़ सोज़ के मरसिए अच्छे हैं। फ़रमाने लगे “कैसे?” मैंने कहा मसलन ये मर्सिया,
“जब हुई ज़हर तलक क़त्ल सिपाह शब्बीर।” फ़रमाया, “हाँ अच्छा तो है, लेकिन इसका जवाब अनीस ने एक मतला में दे दिया है।” फिर थोड़ी देर के लिए ख़ामोश हो गए। शायद मेरा रद्द-ए-अमल जानना चाहते थे। मैंने ख़ामोशी तोड़ी “तो वो मतला मरहमत फ़रमाइए।” कुछ देर रुक कर गोया हुए,
“आज शब्बीर पे क्या आलम-ए-तन्हाई है?” उनका वो रुक रुक कर तास्सुर भरे लहजे में ये मिसरा दोहराना और एक आह सर्द खींचना आज तक मेरे कानों में गूंज रहा है। मैंने उस वक़्त तक अनीस का ये मर्सिया पढ़ा नहीं था। ख़ामोश हो गया। बाद में ये मर्सिया ढूंढ निकाला। शुरू से आख़िर तक पढ़ गया। अच्छा है लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि एक मिस्रे पर दबीर का सारा मर्सिया निसार कर दिया जाए। इसमें शक नहीं कि मतला में अनीस ने बड़ी मानवियत भर दी है लेकिन मरसिए के मुक़ाबले में एक मिसरे को तो नहीं रखा जा सकता।
मसऊद साहब कुछ ऐसे मूड में आ गए थे जिसमें क़दीम शोअरा किसी के अच्छे शे’र पर अपना पूरा दीवान निछावर कर दिया करते थे। ऐसी रिवायत “साइब” से लेकर “ग़ालिब” तक अक्सर शायरों के बारे में दोहराई गई है।
उन्होंने अनीस के मरासी, सलाम, रुबाइयाँ, ख़ुतूत, मुनाजात सबको यकजा किया। हयात से ताल्लुक़ जहाँ-जहाँ मवाद मिल सका, बड़ी काविश से जमा किया। अस्लाफ़-ओ-अख़्लाफ़ अनीस पर भी काम करते रहे। “अस्लाफ़-ए-अनीस” पर उनकी किताब शाए हो कर अरबाब-ए-नज़र से ख़िराज-ए-तहसीन ले चुकी है। लेकिन ख़ुद अनीस की ज़िन्दगी पर वो कोई सैर-हासिल या तफ़सीली किताब न लिख पाए। सिर्फ़ “रूह-ए-अनीस” में मुख़्तसर हालात हैं। इसके अलावा अनीस सदी के तक़रीबात के सिलसिले में अनीस पर एक मुख़्तसर रिसाला शाए किया था। उसमें भी कुछ हालात दर्ज हैं अलबत्ता मुख़्तलिफ़ पहलुओं पर कई मज़ामीन लिखे हैं। हयात-ए-अनीस पर उनका वो जमा करदा मवाद जो शाए नहीं हुआ है वो बहुत है और क़ाबिल-ए-क़दर है। आख़िर उम्र में, मैंने कई बार अर्ज़ करने की जसारत की, क़िबला ये बिखरा हुआ मवाद किसी तरह भी समेट दीजिए। नोक पलक बाद के एडिशनों में दुरुस्त करते रहिएगा। लेकिन मैं ये जानता था कि ये उनका तरीक़-ए-कार नहीं है और इस पर हरगिज़ राज़ी न होंगे।
मुझे ये डर था (और ग़लत नहीं था) कि उनके ज़ेहन में इतना कुछ महफ़ूज़ है कि उसका समेटना मुश्किल है। यही उनकी मुश्किल थी जैसे कि यही मुश्किल क़ाज़ी अब्दुल वदूद की भी है। ढलती हुई उम्र, गिरती हुई सेहत, जवाब देता हुआ हाफ़िज़ा, घटती हुई ताक़त और काम करने की सलाहियत, ये तो फ़ित्रत के अतियात-ए-पीरी हैं। ये ख़्वाहिशों के फैलाने का नहीं बल्कि काम के समेटने का वक़्त होता है। इतना मसऊद साहब को भी मालूम था और क़ाज़ी अब्दुल वदूद को भी मालूम है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये काम समेटे कैसे जाएं और मुआविन-ए-कार कहाँ से ढूंढे जाएं? आख़िर में इंसान ये सोच कर हाथ पाँव डाल देता है कि,
फ़ुर्सत कहाँ कि तेरी तमन्ना करे कोई! मसऊद साहब फिर भी हिम्मत वाले थे कि उन्होंने क़ुदमा की मर्सिया निगारी पर “अलीगढ़ तारीख़ अदब-ए-उर्दू” के लिए एक बाब लिखा। फिर “तहरीर” दिल्ली में नादिर मवाद शाए कराया और “अस्लाफ़-ए-मीरअनीस” की तकमील की। अब अनीस पर उन्होंने जो कुछ लिखा है उसे यकजा कर देने का काम रह जाता है और यक़ीन है कि नय्यर मसऊद इसे अव्वलियत देकर मुकम्मल करेंगे।
अनीस के सिलसिले में मसऊद साहब का एक और कारनामा मिर्ज़ा अनीस की तकमील है, वो निस्फ़ सदी से उसके पीछे पड़े हुए थे। उस काम में उनके रफ़ीक़-ए-देरीना अली अब्बास हुसैनी ने उनका बहुत कुछ हाथ बटाया और मज़ार-ओ-मकान अनीस की मरम्मत बड़ी हद तक उन्हीं की कोशिश की मरहून-ए-मिन्नत है।
उसके बाद अनीस सदी मनाने का ख़्याल भी उन्हीं को सबसे पहले आया और काफ़ी पहले से इस काम की इब्तिदा की। शुरू में लखनऊ में एक कमेटी बनाई गई जिसने शुदबुद शुरू की। कुल हिंद पैमाने पर काम करना उस कमेटी के बस में न था। ख़ुद मसऊद साहब उम्र की उस मंज़िल में थे जब वो सिर्फ़ तजावीज़ पेश कर सकते थे या तरीक़-ए-कार मुअय्यन कर सकते थे। दौड़ धूप करना उनके बस में न था। दौड़ धूप वैसे भी उनके लिए नहीं बनाई गई थी। इसलिए दिल्ली में एक कुल-हिंद कमेटी की तश्कील करना पड़ी। मसऊद साहब उसके जनरल सेक्रेटरी मुंतख़ब हुए। उस कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि अनीस के कलाम के सदी एडिशन सेहत-ए-मतन के साथ शाए किए जाएं। ये काम मसऊद साहब ने अपने ज़िम्मे लिया और नायब हुसैन नक़वी को अपना नायब तजवीज़ किया, सेहत और उनके अपने बिखरे हुए कामों को देखते हुए उनका ये इसरार कि वो हर एक मुसव्वदा ख़ुद देखेंगे और तसहीह करेंगे नामुमकिन-उल-अमल मालूम होता था। लेकिन उनकी बुजु़र्गी, अनीस से उनकी वाबस्तगी और शेफ़्तगी को देखते हुए कमेटी ने उनकी ख़्वाहिशात के सामने सर-ए-तस्लीम ख़म कर दिया। हुआ वही जिसका डर था। काम में बेहद ताख़ीर होने लगी और चलती हुई गाड़ी रुकने लगी, इस सिलसिले में वो नायब हुसैन नक़वी से कुछ कबीदा भी हो गए और ये कशीदगी बिल-आख़िर कमेटी ही से कबीदगी की शक्ल इख़्तियार कर गई और सेहत का उज़्र कर के वो कमेटी से अलग हो गए। इसके बावजूद कमेटी से उनकी दिलचस्पी बाक़ी रही।
जब मैं आख़िरी बार उनसे मिला तो उन्होंने तदवीन-ए-मरासी के काम की रफ़्तार के बारे में सवालात किए। अगरचे ये काम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक़ नहीं हो रहा था फिर भी इस बात से ख़ुश थे कि जैसा भी होगा पिछले मतून के मुक़ाबले में शायद ये काम अच्छा ही हो जाएगा। ख़ुदा का शुक्र है कि अब काम चल पड़ा है। सलामों और रुबाइयों के मजमुए राक़िम-उल-हुरूफ़ ने मुरत्तब कर दिए हैं, कुछ नए सलामों और रुबाइयों का सुराग़ नायब हुसैन नक़वी ने लगाया था। मैंने उन्हें भी शामिल कर लिया है। नायब हुसैन को बेश्तर सलाम रियासत-ए-महमूदाबाद के नादिर ज़ख़ीरे से जनाब महाराज कुमार साहब की इनायत से मिले थे और ख़ुद रियासत को ये सलाम अख़्लाफ़-ए-अनीस से दस्तियाब हुए थे। इस नए मवाद की फ़राहमी को अनीस सदी की देन समझना चाहिए और बिल-वास्ता इसकी फ़राहमी का सेहरा भी मसऊद साहब ही के सर है।
ये नया मवाद सलाम-ओ-रुबाई तक ही महदूद नहीं है। बहुत से नए मरसिए भी दरियाफ़्त हुए हैं और उन नवादिरात-ए-मरासी की एक जिल्द अलग से मुरत्तब हो रही है। मत्बू’आ मरासी की तर्बियत-ओ-तदवीन का काम सालिहा आबिद हुसैन ने अंजाम दिया है। ये काम भी इब्तिदाई मंज़िलों में मसऊद साहब की रहबरी में अंजाम पाया था बाद में औरों ने भी हाथ बटाया और बेगम साहिबा ने तकमील की। बेगम साहिबा ही ने नागरी रस्म-उल-ख़त में भी मरासी-ए-अनीस की एक जिल्द मुरत्तब कराई है। ग़ैर मत्बू’आ मरासी की दरियाफ़्त बेश्तर नायब हुसैन नक़वी की कोशिशों का समरा है। ये काम तेज़ी से तकमील की तरफ़ बढ़ रहे हैं और बार-बार ये ख़्याल होता है कि वो हयात होते तो उन कामों को देखकर उन्हें कितनी मसर्रत होती।
मैंने इब्तिदा में अपनी शागिर्दी का ज़िक्र ज़रा रवादारी में कर दिया था। इस सिलसिले के चंद क़ाबिल-ए-ज़िक्र वाक़ियात याद आ रहे हैं। मुझे उनकी शागिर्दी के सिर्फ़ दो साल बी.ए. में नसीब हुए। उसकी भी सूरत ये थी कि वो हफ़्ते में सिर्फ़ एक दिन फ़ारसी जदीद का दर्स देते थे। फ़ारसी में दो और उस्ताद थे। सय्यद यूसुफ़ हुसैन मूसवी और अब्दुल क़वी फ़ानी लेकिन उनके दर्जों से मैं अक्सर ग़ायब रहता। ये मेरी ज़िन्दगी का वो दौर था जब सियासत के सिवा मुझे कुछ सूझता ही न था। फ़ारसी के दर्जे से नहीं बल्कि फ़लसफ़े के दर्जे से भी गैर हाज़िर हो जाता था। फ़लसफ़ा-ओ-फ़ारसी दोनों ही जमातों में थोड़े से तालिब इल्म होते थे और ग़ायब हो जाने वाला फ़ौरन पकड़ लिया जाता था लेकिन मेरी सियासी सरगर्मियों की बिना पर अक्सर उस्ताद रिआयत करते और कभी कभी गैर-हाज़िरी बख़्श दिया करते थे। मुझे उस दौर में सर-ओ-पा का होश नहीं था, हाज़िरी वालों में अगर मेरा नंबर पहला नहीं तो पांच सवारों में ज़रूर होता था। उस वक़्त ख़ुद मैं और स्टूडेंट्स फ़ेडरेशन के दूसरे साथी असातिज़ा से लेकर वाइस चांसलर तक दौड़ते और हाज़िरी की कमी किसी न किसी तरह पूरी कराई जाती। कुछ असातिज़ा भी मेहरबानी करके इस आड़े वक़्त में हाज़िर बना देते। लेकिन मसऊद साहब के यहाँ ये नामुमकिन था, बस इतनी रिआयत ज़रूर करते कि अगर देर से भी आता तो हाज़िर बना देते और ये रिआयत भी सिर्फ़ मेरे लिए मख़सूस न थी। ग़रज़ ये उस्तादी और शागिर्दी भी दूरियों का सिलसिला थी जो चीज़ क़रीब लाने वाली थी वो अदब से दिलचस्पी थी।
शागिर्दी भी दर अस्ल कई तरह की होती है, एक तो दर्स लेने की आदत का नाम शागिर्दी रखा गया है। ये शागिर्दी दो बरस की क़लील मुद्दत में ख़त्म हो गई और चूँकि हफ़्ते में सिर्फ़ एक दिन उनके लेक्चर में शरीक होता था, इसलिए ये मुद्दत तातीलात वग़ैरा को निकाल कर बारह महीनों में तब्दील हो जाएगी और उन बारह महीनों में भी सिर्फ़ एक घंटे की शागिर्दी, ज़ाहिर है कि ये मुद्दत बहुत ही क़लील थी। लेकिन दूसरे शागिर्दी की मुद्दत काफ़ी तवील थी, चालीस साल से कुछ ऊपर मसऊद साहब से जितना अदबी ख़ुलूस बढ़ता गया उनकी शख़्सियत उसी क़दर बरफ़्गंदा नक़ाब होती गई। मसलन मैंने उनसे लफ़्ज़ों की परख सीखी। वो एक एक लफ़्ज़ तौल के लिखते थे। इबारत को बार-बार पढ़ते हुए ज़रूरत महसूस करते तो बार-बार तरमीम करते। उन्होंने ये सिखाया कि क़लम बर्दाश्ता लिख लेना ही कमाल नहीं बल्कि नाप तौल के जाँच परख के लिखना भी कमाल है। लिखने से पहले मौज़ू का मुताला ज़रूरी है। जितना ही मुताला फ़ुरूई और सरसरी होगा इबारत उतनी ही नाकाफ़ी और ना-साफ़ होगी। ख़्याल जितना ही आईना होगा, मवाद की सेहत पर जितना ही ख़्याल होगा तहरीर में उतनी ही वज़ाहत होगी और क़तईयत भी होगी।
वो उर्दू नस्र के साहिबान-ए-असालीब में से हैं। उनका तर्ज़-ए-तहरीर क़ुदमा में मुहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली दोनों से बैक वक़्त मुतअस्सिर है। हाली का बयानिया अंदाज़ और रवां इबारत और आज़ाद की शगुफ़्तगी ख़िताबत को मिला कर मसऊद साहब ने एक मुतवाज़िन तर्ज़ अपनाई। ख़िताबत का पहलू बहुत दबा हुआ और दलाइल के सिलसिलों से मरबूत है। शगुफ़्तगी तर्तीब कलिमात से पैदा करते हैं लेकिन इस तरह के इबारत आराई का गुमान न हो और सदाक़त लहजा मजरूह न होने पाए। वो जदीद उर्दू नस्र की तरह जुमलों की शनाख़्त तक में मग़रिबी असालीब की नक़्क़ाली नहीं करते। वो अरबी फ़ारसी अल्फ़ाज़ या असातिज़ा की तरकीबें मुस्तआर लेकर उर्दू के फ़ित्री हुस्न पर मस्नूई आराइशों का ग़ाज़ा नहीं चढ़ाते, उनका संभाला हुआ अंदाज़-ए-बयान, शुस्ता उर्दू का अच्छा नमूना है। उनके इस्तिदलाल में मतानत के अलावा वज़ाहत और मंतक़ी ज़ोर है। इस्तिदलाल को क़वी तर बनाने के लिए वो तफ़सील से गुरेज़ नहीं करते। कोशिश यही होती है कि कोई पहलू तिश्ना न रह जाए। इसके बाइस शाज़-ओ-नादिर उनके यहाँ तूल का एहसास भी हो सकता है लेकिन जब मक़सद की वकालत करना हो तो तूल से बचना नामुमकिन है। अदबी चाशनी उनकी हर तहरीर पर छा जाती है। चाहे उस चाश्नी की तह कितनी ही हल्की क्यों न हो।
उनसे इंसान ये भी सीख सकता है कि अदब और तहक़ीक़ में कोई हर्फ़-ए-आख़िर नहीं है। अदीब के ज़ेहन के दरीचों को हमेशा खुला रहना चाहिए कि ताज़ा हवा और रौशनी बराबर आती रहे। जिन्होंने उनकी तस्नीफ़ “हमारी शायरी” के मुख़्तलिफ़ एडिशन देखे हैं वो महसूस करेंगे कि किस तरह बराबर इज़ाफ़े करते रहे हैं और क़ाबिल-ए-तरमीम अजज़ा में तग़य्युर-ओ-तफ़कीक। मज़ामीन में भी यही अमल जारी रहता। पहले के शाए शुदा मज़ामीन जब बाद में किताबी सूरत में आते तो जगह जगह से पैवंद कारी हो चुकी होती। क़ारी के साथ ये दयानतदाराना रवय्या ज़िन्दा रहने वाले अदीब की पहचान है और उन्होंने ये दयानतदाराना रवय्या कभी तर्क नहीं किया।
वो मुहक़्क़िक़ के लिए ये ज़रूरी समझते थे कि मुतक़द्दिमीन से भरपूर इस्तिफ़ादा करे, उनकी इज़्ज़त करे लेकिन उनसे बेजा तौर पर मरऊब न हो। इसलिए उन्होंने बा’ज़ नज़ाई हस्तियों को अपनी तहक़ीक़ का मैदान क़रार दिया। उनमें मुहम्मद हुसैन आज़ाद भी शामिल थे और वाजिद अली शाह भी। उनका तरीक़ा-ए-कार था कि वो अपने मौज़ू और हुस्न-ए-तहक़ीक़ की तरफ़ हमदर्दी से मुतवज्जा होते, ग़लतियाँ गिनाने से पहले ये मान कर चलते कि ग़लतियाँ किस से नहीं होती। न वो अदीब-ओ-शायर को फ़रिश्ता मानते थे न बादशाह को। उन्होंने वाजिद अली शाह और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नाक़िदीन को पढ़ा था। लेकिन ये महसूस करते थे कि उन दोनों के साथ इन्साफ़ नहीं हुआ है।
“आब-ए-हयात का तन्क़ीदी मुताला” मुख़्तसर होने के बावजूद बहुत ही जचा तुला मुताला है और मसऊद साहब ने वकालत का हक़ अदा कर दिया है। बा’ज़ असहाब ने ये फिज़ा पैदा करना चाही थी कि “आब-ए-हयात”का मुसन्निफ़ हक़ाइक़ से खेलता है बल्कि हक़ाइक़ तसनीफ़ करता है और इस एतिबार से उसका लिखा हुआ सरासर पाया-ए-एतिबार से साक़ित है। इस ग़ैर मोतदिल रवय्ये को देखकर ग़ैर मुहक़्क़िक़ अदीबों ने ग़रीब आज़ाद को बुरी तरह निशाना-ए-मलामत बनाना शुरू किया। मसऊद साहब ने “आब-ए-हयात” का तन्क़ीदी मुताला लिख कर इस ग़लती पर हमको टोका। प्रोफ़ेसर महमूद शीरानी जैसे साहिब-ए-नज़र मुहक़्क़िक़ ने भी इस क़िस्म की बे-एतिदालियों की निशानदेही की। अब आज़ाद की तरफ़ तन्क़ीद का रुख़ उतना मुआनिदाना नहीं रह गया है।
वाजिद अली शाह को फ़रिश्ता कौन कहेगा? वो अपने बा’ज़ गुनाहों के इक़रारी मुजरिम हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सर-ता-पा गुनाह थे या वो रंगरलियों ही के बादशाह थे और रक़्स-ओ-सुरूद-ओ-ऐश के अलावा कुछ और जानते ही न थे। ये सूरत तो अंग्रेज़ों ने इसलिए बनाई कि ग़सब-ए-सल्तनत और बर्बादी-ए-अवध का जवाज़ निकाल सकें। मौलवी नज्म-उल-ग़नी (जिनका वाबस्ता-ए-सरकार इंग्लिशिया होना ढकी छुपी बात नहीं है) जो कुछ लिखते हैं उस पर अक्सर इफ़रात-ओ-तफ़रीत की छाप होती है। कुछ तो बात थी कि वाजिद अली शाह की माज़ूली पर अवाम ने आँसू बहाए, वाजिद अली शाह फ़ुनून-ए-लतीफ़ा के बहुत बड़े सरपरस्त थे, वो ख़ुद भी नस्सार-ओ-शायर थे, उनमें मज़हबियत की तरफ़ मैलान के बावजूद सेक्युलरिज़्म का जज़्बा-ए-हस्सास था। वो फ़ुनून-ए-हर्ब का भी शुऊर रखते थे लेकिन साज़िशों का शिकार थे और तोहमात में मुब्तला। मजमूई तौर पर जो तस्वीर उभरती है वो इतनी बुरी नहीं है। जो बा’ज़ रंग आमेज़ पेश करना चाहते हैं। अगर उन्हें कोई अख़लाक़-ए-आलिया का नमूना बनाकर पेश करना चाहे तो ग़लत होगा। लेकिन अगर उन्हें कोई सर ता पा क़ाबिल-ए-नफ़रत ख़साइस का मजमूआ क़रार दे तो वो और भी ग़लत होगा। मसऊद साहब ने वाजिद अली शाह के अच्छे पहलुओं पर अपनी तहक़ीक़ का रुख़ मोड़ा। इस हमदर्दाना मुताले से बहुत से वो हक़ाइक़ सामने आए जिनसे लोग आम तौर पर वाक़िफ़ न थे। बुराइयों का बड़ा अम्बार पहले ही लगाया जा चुका है। उसको मसऊद साहब ने नहीं छुवा, बज़ाहिर ये ग़ैर मुतवाज़िन तहक़ीक़ समझी जाएगी लेकिन मसऊद साहब का जवाज़ ये था कि वो पहले की ग़ैर मुतवाज़िन तहक़ीक़ में तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
दीवान-ए-फ़ाइज़ देहलवी की तलाश और उसकी तदवीन-ओ-इशाअत मसऊद साहब का एक और ये कारनामा है। शुमाल-ए-हिंद में इससे पहले कोई और साहब-ए-दीवान शायर अभी तक तलाश नहीं किया जा सका है। सिर्फ़ अव्वलियत ही नहीं बल्कि मवाद के एतिबार से भी ये दीवान बहुत अहम है और जो लोग बेसमझे बूझे, लखनऊ स्कूल और दिल्ली स्कूल, की बातें करते रहते हैं उनकी रहनुमाई के लिए भी एक अहम दस्तावेज़ है। यही हाल फ़ैज़ मीर, मजालिस रंगीं और फ़साना-ए-इबरत और तज़्किरा-ए-नादिर और तज़्किरा-ए-मुब्तला का भी है। उन्होंने हर क़दीम तसनीफ़ की बाज़ियाबी में हमें एक अछूता तोहफ़ा दिया है। हज़ारों ही किताबें उनकी नज़र से गुज़री होंगी लेकिन उन्होंने इशाअत के लिए इंतिख़ाब में बड़ी एहतियात से काम लिया है।
मसऊद साहब से मैंने ये भी सीखा कि अपनी राय दूसरों पर लादना नहीं चाहिए। उनसे जब भी बात होती तो वो अपना नुक़्ता-ए-नज़र बड़ी वज़ाहत से पेश करते, दलीलें देते, जवाबात देते लेकिन दूसरे की बात सुनने को भी तैयार रहते। मसऊद साहब पर दूसरों ने बहुत कुछ लिखा है। उनकी तन्क़ीदें भी हुई हैं ख़ुद मैंने ज़माना-ए-तालिब इल्मी ही में एक-बार उनसे इख़्तिलाफ़-ए-राय किया। इस पर मुझे मौलाना तिलहरी और हुसैनी साहब दोनों ने टोका कि तुम्हें पहले उनसे रुजू कर के शुबहात का अज़ाला कर लेना चाहिए था। मैंने अर्ज़ किया कि जब किताब छप गई या मज़मून शाए हो गया तो वो सबकी मिल्कियत हो गया और यारान-ए-नुक्तादां के लिए सिला-ए-आम, अब हर शख़्स इज़हार-ए-ख़्याल में आज़ाद है। ख़ुद मसऊद साहब ने इस बारे में एक लफ़्ज़ भी ज़बान से न निकाला, अगरचे मज़मून उस वक़्त शाए हुआ जब वो मेरे उस्ताद हो चुके थे। उनकी शागिर्दी इख़्तियार करने के बाद भी मैंने “ज़माना” कानपुर में एक मज़मून लिखा जिसमें दबे लफ़्ज़ों में कहीं मसऊद साहब के बा’ज़ ख़्यालात पर ईराद था। अल्लामा तिलहरी की अचूक नज़र उस हिस्से तक आकर रुक गई। उन्होंने कहा कि हक़-ए-उस्तादी उसका मुतक़ाज़ी न था। मैंने जवाब दिया कि जब शागिर्द बया क़लम संभाल ले तो कुछ हक़-ए-शागिर्दी भी हो जाता है। मुझे यक़ीन था कि मसऊद साहब तहक़ीक़ के आदमी हैं। बुरा न मानेंगे और अगर बुरा भी माना तो मुझे कभी महसूस न होने देंगे। हुआ भी ऐसा ही। वो हमेशा उसी शफ़क़त-ओ-मुहब्बत से मिलते रहे। अक्सर ख़त लिखते और मुझे “अज़ीज़-ए-गिरामी-ए-क़द्र” कह कर मुख़ातब करते। अदब के पर्दों से भी ऐसे इंसान रोज़ नहीं निकलते।
वो सब काम नपे तुले अंदाज़ में करते थे। वो शेरवानी, अलीगढ़ कट का पाजामा, सर पर कभी बालदार और कभी किश्ती नुमा टोपी पहनते थे। घर पर सिर्फ़ कुर्ते और पाजामे में रहते और उसी लिबास में अमलन मिलते भी थे। कभी कभी सूट भी पहन लिया करते थे। लेकिन मैंने उन्हें अंग्रेज़ी टोपी पहने हुए कभी नहीं देखा उसके बर-अक्स अंग्रेज़ी सूट पर मशरिक़ी टोपी ज़रूर देखी है। मुक़दिरत के बावजूद कार कभी नहीं रखी। तांगा रखते थे जिसमें जुते हुए घोड़े की बागडोर उनके भाई आफ़ाक़ के हाथ में रहती थी। बाद में उस तांगे से भी नजात पाली।
क़द लांबा और बदन गुदाज़ था। दाढ़ी मुंडाते और मूँछें छोटी रखते थे लेकिन कभी नीची न होने देते थे। मैंने “आपसे मिलिए” सिलसिला-ए-मज़ामीन में जो बाद में किताबी शक्ल में भी शाए हो गए, उन पर भी एक मज़मून लिखा। उसमें मूँछों के बारे में मेरे क़लम से ये निकल गया कि वो “तितली मार्का” मूँछें रखते हैं। इशाअत के बाद एक रोज़ मौलाना अख़्तर अली ने उस मज़मून का ज़िक्र छेड़ा। मसऊद साहब कहने लगे कि लिखा तो अच्छा है लेकिन सचमुच बताइए क्या आपको भी मेरी मूँछें तितली मार्का लगती हैं? अख़्तर अली साहब ने नफ़ी में सर हिलाया तो मसऊद साहब ख़ामोश हो गए। बाद में अख़्तर अली साहब ने मुझे बताया कि मूँछों की तौसीफ़ मसऊद साहब को पसंद न आई। कमान से छूटे हुए तीर की तरह फ़िक़रा क़लम से निकल चुका था। अब तो आइन्दा इशाअत ही में तरमीम मुम्किन थी। इसकी नौबत उनकी ज़िन्दगी में न आ सकी। मैंने उस मौज़ू पर उनसे कुछ कहना मुनासिब न समझा और ख़ुद मसऊद साहब ने इशारतन और किनाएतन उसका ज़िक्र नहीं किया।
मसऊद साहब हुसैनी और तिलहरी के दोस्त थे, लेकिन उन तीनों के माबैन एहतिराम भरी दोस्ती थी, तू को कौन कहे, कभी ‘आप’ से ‘तुम’ तक गुफ़्तगू न पहुँच पाई। आपस में मज़ाह-उल-मोमिनीन भी होता, संजीदा जुमले भी चुस्त होते लेकिन लँगोटिया यार वाली कैफ़ियत कभी पैदा न हो पाती। हुसैनी और तिलहरी मसऊद साहब को एक सीनियर अदीब तो नहीं मानते थे क्योंकि सनों में तफ़ावुत बहुत कम था लेकिन उनकी इज़्ज़त करते थे और उनकी बुराई क्या, तन्क़ीद भी सुनने को आमादा न होते थे। ये पुराने इक़दार के परस्तार, उसको भी शान-ए-दोस्ती के ख़िलाफ़ जानते थे, यही वजह है कि दोनों मौक़ों पर जब मैंने कुछ लिखा, तो मैं टोका गया। लेकिन हुसैनी और तिलहरी के बरअक्स मसऊद साहब ने दोस्ती, अदब, क़ौमी का जम सब के अलग ख़ाने से बना रखे थे और वो किसी एक शो’बे की दूसरे शो’बे में मुदाख़लत गवारा नहीं करते थे।
जब मैंने दिल्ली मर्सिया गोयों पर “आंध्रा प्रदेश”में एक मुख़्तसर सा मज़मून लिखा तो बहुत ख़ुश हुए और मेरी तलाश की दाद दी। फिर अपने यहाँ बाज़ क़दीम मख़्तूतात की निशानदही की। मैं वहाँ हाज़िर हुआ तो मुझे नादिर बयाज़ें दिखाईं, हाशिम और करम अली के मरासी की ज़ियारत कराई। कहने लगे कि “मेरे पास मिस्कीन के मरासी का बड़ा ज़ख़ीरा है। फिर मैंने नोट लेना चाहे। फ़रमाया कि आप शौक़ से नोट लें लेकिन ये मेरी ज़िंदगी भर की तलाश का नतीजा हैं इसलिए उन पर पहले मैं लिखूँगा।” ये उनकी साफ़गोई मुझे पसंद आई। फिर मेरी मालूमात में ये इज़ाफ़ा किया कि इसी तरह मरासी-ए-मीर और बा’ज़ दूसरे मरासी पहले मैंने तलाश किए लेकिन दूसरों ने उन पर मुझसे पहले लिख डाला और लुत्फ़ ये कि वो मरासी उन्हें मैंने ही दिए थे। मैंने इज़हार-ए-हमदर्दी करते हुए कहा कि आप तहक़ीक़ में लग जाते हैं और दूसरे कात के लिए दौड़ते हैं। मुस्कुराकर ख़ामोश हो रहे। ग़रज़ इस मसले में मसऊद साहब के नज़दीक दोस्ती अदब पर हावी नहीं हो सकती थी।
क़ौमी कामों में भी सूरत-ए-हाल यही थी। अनीस कमेटी बनाई गई, ख़ुद ख़ज़ानची और अली अब्बास हुसैनी सेक्रेट्री बने। मसऊद साहब गोशा नशीन और अली अब्बास हुसैनी बेहद फ़आल। उन्होंने दौड़ धूप कर पच्चीस तीस हज़ार की रक़म मुहय्या कर ली। इसमें मो’तद ब हिस्सा हुकूमत-ए-हिन्द की इमदाद का था। फिर काम शुरू हुआ। हुसैनी साहब ने ये फ़र्ज़ करने में ग़लती की थी कि मसऊद साहब तामीर के काम में मुदाख़लत न करेंगे। इस सिलसिले में तफ़सीलात का इल्म नहीं कि क्या हुआ लेकिन इतना मालूम है कि हुसैनी साहब ने सेक्रेट्रीशिप से बददिल हो कर इस्तीफ़ा दे दिया।
किताबों का बेहतरीन ज़ख़ीरा मसऊद साहब के ज़ाती कुतुबख़ाने में था। घर पर अगर कोई आता तो वो उसकी इजाज़त दे देते कि वहीं बैठ कर देख ले, लेकिन वो किसी को भी किताब आरियत नहीं देते थे। इसमें अंदुरूनी और बेरूनी की भी तफ़रीक़ नहीं थी। एक-बार मुझसे उनके दामाद मसीह-उज़्ज़मां मरहूम ने भी दबे लफ़्ज़ों में तक़रीबन शिकायत आमेज़ लहजे में इसकी तस्दीक़ की। अपनी कई नादिर किताबें खो देने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि तकल्लुफ़-बरतरफ़, किताबें आरियत देना कोई बहुत बड़ी ख़िदमत नहीं है। मालिक राम साहब का मुआमला इसके बरअक्स है। अगर किसी ने दयानत का सबूत बहम पहुँचा दिया और वो किताबों से सही काम लेने के क़ाबिल भी हुआ तो वो बे-पस-ओ-पेश किताब दे देते हैं। मैंने उनके ज़ख़ीरे से अक्सर इस्तिफ़ादा किया है।
मसऊद साहब का शुमार सिक़्क़ा लोगों में था। वो अवामिर व नवाही पर सख़्ती से आमिल रहा किए हैं। रोज़ों का हाल मालूम नहीं लेकिन नमाज़ें पाबंदी से पढ़ते थे। जवानी के ज़माने में उन्होंने ड्रामे भी देखे हैं। जवानी जवानी ही होती है। उन्हें इब्तिदा से ड्रामों से शग़फ़ था और ये शग़फ़ बिलआख़िर उनकी इस तसनीफ़ का सबब बना जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी से इनाम मिला। ये तसनीफ़ दर-अस्ल दो तसानीफ़ “लखनऊ का शाही स्टेज”और “लखनऊ का अवामी स्टेज”का मजमूआ है। इस में शक नहीं कि इस मौज़ू पर मसऊद साहब ने जी खोल कर दाद-ए-तहक़ीक़ दी है।
मसऊद साहब ने ऐसे तो फ़ाइज़ और मीर जैसे क़ुदमा पर भी लिखा है लेकिन अगर बहैसियत मजमूई देखिए तो नवाबीन-ए-अवध का आख़िरी दौर और लखनऊ ही बेश्तर उनके तसानीफ़ और तहक़ीक़ात का महवर रहे हैं। ये तरीक़-ए-कार मुनासिब भी है। अगर किसी ज़माने या ख़ास इलाक़े को तहक़ीक़ के लिए चुना जाए तो इस पर सैर-ए-हासिल और हश्त-पहलू काम हो सकता है। अगर तवज्जो चहार जानिब होगी तो हर तरफ़ तिश्नगी का एहसास होता रहेगा। उन्होंने वक़्त और माहौल मुंतख़ब कर लिया और एक ख़त-ए-मुस्तक़ीम पर चलते रहे। उस ख़त से फूटने वाली तमाम शाख़ों पर भी नज़र रखी और उससे एक तनव्वो पैदा हुआ, वर्ना कहाँ मर्सिया और कहाँ स्टेज?
उर्दू में तहक़ीक़ के लिए इतने गोशे पड़े हुए हैं कि जिस तरफ़ भी नज़र उठाई जाती है वहाँ कुछ न कुछ ज़रूर मिल जाता है और इसी लिए बैक वक़्त कई तरफ़ मुतवज्जे होना मुम्किन हो जाता है। हमारे यहाँ क़ाज़ी अब्दुल वदूद की मिसाल सामने है। अगरचे ग़ालिबियात और सतवातियात पर उन्होंने ज़्यादा तवज्जो की लेकिन वो जिस तरफ़ भी झुक जाते हैं वुसअत-ए-मुताला के बलबूते पर वहाँ से कुछ न कुछ निकाल ही लेते हैं। उस वुसअत की वजह से उन्होंने अब तक जो कुछ किया है उसका समेटना नामुमकिन हो रहा है। मसऊद साहब ने कारोबार-ए-शौक़ को इतना फैलाया नहीं था, फिर भी उन्होंने अनीस और वाजिद अली शाह पर इतना मवाद यकजा कर लिया था कि उसी का समेटना उनके लिए मुश्किल हो गया था। ये सदमा शायद मसऊद साहब को आख़िर वक़्त तक रहा हो।
अंग्रेज़ों के ज़माना-ए-हुकूमत की यूनीवर्सिटियों में उर्दू और फ़ारसी ही क्या हिन्दी संस्कृत और अरबी भी दूसरे दर्जे के मज़ामीन समझे जाते थे और उनके पढ़ाने वाले आम ज़ेहनों में दूसरे दर्जे के उस्ताद शुमार होते थे। मगर मसऊद साहब का रख-रखाव ऐसा था कि वो जिस तरफ़ भी जाते उनकी इज़्ज़त दूसरों ही की तरह बल्कि बा’ज़ औक़ात दूसरों से भी ज़्यादा होती थी। वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और ख़ज़ानची (मुद्दतों चन्द्रभान गुप्ता ख़ज़ानची रहे) भी अहम उमूर में उनसे मश्वरे लेते थे। साल के शुरू में दाख़िले के बाद फ़ीस की माफ़ी की दौड़ धूप शुरू होती। उर्दू शो’बे के एक रीडर डाक्टर सय्यद मोहम्मद हुसैन साहब हर तालिब इल्म की दरख़ास्त पर सिफ़ारिश कर दिया करते, चाहे वो किसी शो’बे का तालिब इल्म क्यों न हो। हिन्दी और संस्कृत के तल्बा भी अपने उस्तादों से मायूस हो कर उनसे सिफ़ारिश करा ले जाते थे लेकिन मसऊद साहब सिफ़ारिश ही न करते। नतीजा ये था कि मोहम्मद हुसैन साहब की सिफ़ारिश तो सिफ़ारिश ही न समझी जाती थी और मसऊद साहब की सिफ़ारिश वाले आम तौर से मुस्तहिक़-ए-वज़ीफ़ा क़रार पाते थे।
मसऊद साहब को बहुत से अच्छे शागिर्द मिले जिन्होंने उर्दू अदब की दुनिया में ख़ुद अपने लिए एक जगह बना ली। मसऊद साहब को इससे बड़ी ख़ुशी होती कि उनके शागिर्द मुफ़ीद अदबी ख़िदमतें अंजाम दे रहे हैं। वो उनकी तहरीरों पर नज़र रखते और कभी कभी मश्वरे भी दिया करते थे। हिम्मत अफ़्ज़ाई भी करते थे। उनके साहबज़ादे हिंदुस्तान-ओ-पाकिस्तान की दो यूनीवर्सिटियों में उनकी अदबी जानशीनी कर रहे हैं। उनमें नय्यर मसऊद से ख़ुसूसियत के साथ बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। सबसे बड़ा काम फ़ौरी तौर पर ये है कि उनके तहक़ीक़ी मज़ामीन और ग़ैर मुरत्तब मवाद को तर्तीब के साथ शाए कर दिया जाए।
तन्क़ीद में मसऊद साहब का ख़ास मक़ाम है। लेकिन तहक़ीक़ में उसका मक़ाम यक़ीनन बुलंदतर है। वो अच्छे शहरी और अच्छे इंसान थे, बड़े वज़ादार, कुशादा नज़र, कम-आमेज़, वसी उल ख़्याल, मोहतात, मुतदय्यन। नस्र के रसिया तो थे ही, लेकिन इब्तिदा में शायरी भी की थी और उनके नाम के साथ अदीब का इज़ाफ़ा उसी दौर का यादगार था। उनके बा’ज़ इब्तिदाई अशआर मैंने उन्हीं से सुने थे और दो एक “आपसे मिलिए”में महफ़ूज़ भी कर दिए थे। ग़ालिबन जवानी में उन्हें सोज़-ख़्वानी से भी शग़फ़ था और कभी कभी ख़ल्वत में शे’र गुनगुनाया भी करते थे। रंगारंगी में यक रंगी ही उनकी ज़िन्दगी का तुर्रा-ए-इम्तियाज़ थी और उसे मुद्दतों आँखें ढूंढती रहेंगी।
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.