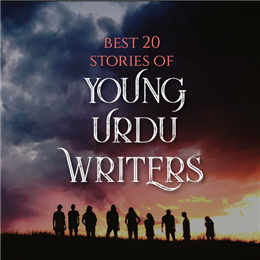कहानियों से परे
तस्वीर के ’अक़ब में तहरीर-शुदा ’इबारत पढ़ने के बा’द मेरे औसान-ख़ता हो गए। तारीख़ पर नज़र पड़ी तो हवास मु’अत्तल हो गए, गोया पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। मुझे किसी भी हाल में पहुँचना था लेकिन मैं ये तय नहीं कर पा रहा था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। नई-नई मुलाज़िमत, वसाइल की कमी और वालिदा की बीमारी ने मुझे शदीद कश्मकश में मुब्तिला कर दिया था, किसी एक नतीजे पर पहुँचने की सूरत नज़र नहीं आ रही थी और इस ग़म को ग़लत करने की कोशिश में सिगरेट निकाला, गहरा कश लगाया और धुएँ का दबीज़ मर्ग़ूला फ़िज़ा में तहलील होता हुआ देखकर कुछ मुतमइन होने की सई’-ए-नाकाम करने लगा कि कल... और फिर मेरी परेशानी बढ़ने लगी।
हैरत-ओ-बे-यक़ीनी, उलझन और बेचैनी का साया दराज़ होते-होते मेरे वजूद पर मुहीत होने लगा, वजूद घुटने लगा था, घुट कर एक कैफ़ियत में तबदील हो चुका था... बे-हिस-ओ-हरकत, जामिद और साकित... अचानक कोई एक ख़याल मेरे ज़मीर को झिंझोड़ने लगा, मुझे जाना है और मुझे जाना ही होगा और इसके लिए मुझे अभी निकलना होगा, अभी और इसी वक़्त। एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर मा’लूम हुआ कि मतलूबा पते पर पहुँचने के लिए मज़ीद पाँच घंटे लगेंगे, टेढ़ी-मेढ़ी ख़स्ता-हाल सड़क और ऊबड़-खाबड़ पगडंडियों से गुज़र कर जाना पड़ेगा। एक नीम-मरई ख़ौफ़, एक मुबहम तजस्सुस, एक दिल-गुदाज़ उदासी दरून-ए-ज़ात ख़ेमा-ज़न थी, शाम क़रीब होती जा रही थी, सूरज की बलग़मी शु’आ’एँ, तेज़ी से पीछे की तरफ़ दौड़ते पेड़ों की सब्ज़ पत्तियों में रू-पोश हो रही थीं। शाम होते-होते मतलूबा जगह पर पहुँच गया था। डायरी के पन्ने पलटता हुआ... वरक़-दर-वरक़, काग़ज़ों की लकीरों में उलझी-बिखरी ज़िंदगी के धागों को एक तार में जोड़ता हुआ...
मुझसे बेहतर कौन जा सकता है कि तुम चंद मौहूम नुक़्तों, साकिन हर्फ़ों, ख़ामोश लफ़्ज़ों नीज़ गुंजलक सत्रों के ‘इलावा भी बहुत कुछ हो, मैं जानता हूँ कि तुम एक ठोस हक़ीक़त हो, वाहिमा भी, नक़्श-बर-आब, सराब और मुग़ालता भी।
मैं जानता हूँ कि तुम एक ख़ब्त हो, ख़लल हो और हुस्न-ए-ख़याल भी, तुम कायनात की तकमील का इस्ति’आरा हो। तुम्हारे जिस्म के नशेब-ओ-फ़राज़ मैंने देखे हैं... जैसे खड़ी दोपहरिया की लू से ज़ेर-ओ-ज़बर होती ज़मीन... लहर-दार, सब्ज़ा-ज़ार, शरर-बार, ख़्वाबशार... तुमसे क़ब्ल कोई चीज़ मुकम्मल वजूद नहीं रखती थी, मैं भी नहीं। सब कुछ तिश्ना-तिश्ना, निस्फ़ और सोख़्ता... मैं ये ए’तिराफ़ करता हूँ कि मैंने एक ना-क़ाबिल-ए-मुआ’फ़ी जुर्म किया है। मैंने तुम्हारी रूह को मजरूह किया है, मैं जज़्बात के कमज़ोर लम्हों में बहक गया था... पिघल गया था... मुकम्मल हो गया था... जो लम्हे हम मुहब्बत में अमर कर सकते हैं वो लड़ झगड़ कर बर्बाद क्यों कर रहे हैं, ये रोज़-रोज़ की अज़ीयत क्यों।
ये बै’अत, ये ’अहद-ओ-पैमाँ। कुछ तो यक़ीन करो।
कितने साल हो गए, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है? बहर-हाल में अपने इक़्दाम पर पशेमाँ हूँ। क्या तुम इन्फ़िआ’ल के वो क़तरे नुक़्तों की शक्ल में हुरूफ़ के रुख़्सार पर महसूस नहीं कर रही हो? लफ़्ज़ तो तुम्हारे ख़ामोश थे मेरे नहीं। तुम्हारे अल्फ़ाज़ ख़ामोश नहीं थे तुमसे रूठे हुए थे क्योंकि तुमने उनको जज़्बों की रोशनाई से शबनमी करना बंद कर दिया था इसलिए वो सूख-सूख कर कमज़ोर और रूठ-रूठ कर सरकश हो गए थे...
बे-मा’नी, मुजर्रद और बे-नुक़त... मेरे भी अल्फ़ाज़ ख़ामोश हो गए क्या? तुमने ही कहा था मेरे लफ़्ज़ों में ज़िंदगी है, रूह है, हुस्न-ए-कायनात मौज-ज़न है। तो फिर ये तुमको ज़िंदा करने में नाकाम क्यों रहे? तुमने ही कहा था कि मेरे अल्फ़ाज़ दर-अस्ल मेरे ही वजूद का जुज़ हैं जो मुकम्मल कैफ़ियत के साथ तुम्हारी ज़ात में तज्सीम होते हैं, तुम्हें एहसास-ए-लतीफ़ के रेशमी धागों से बुनते-उधेड़ते तकमील के नए पैरहन में मलबूस करते हैं। तो फिर तुम मुहब्बत का ये नया पैरहन क्यों उतार फेंकना चाहती हो? फिट नहीं बैठ रहे? रास नहीं आ रहा है? ‘आदत है? तुम जहन्नुम हो और उस वक़्त तक तुम्हारा पेट नहीं भरेगा जब तक कि ख़ुदा अपना बायाँ पैर...
हाँ मैंने ठीक सुना है कि मैं एक जहन्नुम हूँ, जो हमेशा तिश्ना रहेगा... हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद...
जो एक पैर रखे जाने का मुंतज़िर है लेकिन उस एक पैर से क़ब्ल पता नहीं कितने पैरों की वहशत, थकन और मैल उसे पीना है, मैं एक जहन्नुम हूँ जिससे हज़ारों जहन्नुम-पसंद आतिश-ए-नफ़्सानी को बुझाने की ख़्वाहिश रखते हैं, एक पैर तुम्हारा भी पड़ा हुआ है। मैं एक जहन्नुम हूँ लेकिन ये बात भला कैसे समझूँगी कि मैं ज़मीन-ज़ादी नहीं हूँ, परी हूँ, ख़ुद-सर हूँ, सरकश-ओ-पुर-कशिश हूँ... मुसाम-दर-मुसाम तिश्ना, प्यासी और उदास हूँ... मैं देवदासी हूँ... मैं हालत-ए-तरदीद में जी रही थी, जीना है और जियूँगी कि ख़ानदानी विरसे के नाम पर बस यही एक फ़ितरी इख़्तियार मुझे मिला हुआ है, तुमसे बेहतर भला कौन जान सकता है। ज़िंदगी शमशीर-ओ-सिनाँ के दरमियान किसी एक नोक से पैवस्ता हो जाती है, कभी भी नश्तर-ए-फ़िशार रग-ए-जाँ का फ़स्द खोल सकता है, मैं जहन्नुम, कभी भी जहन्नुम-रसीद हो सकती हूँ। ये बात भला तुम ज़मीन-ज़ादे कैसे समझोगे। मेरा ख़याल था कि मैं बाग़-ए-अ’दन के ख़याबाँ से आई हुई कोई हूर हूँ और हर परी-शमाइल को ये क़िस्मत नहीं मिलती, लाला-ओ-गुल में नुमायाँ होना सब का मुक़द्दर नहीं जब कि तुम ज़मीन-ज़ादे जब तक ये तस्लीम नहीं कर लेते कि ये दुनिया एक जहन्नुम है और ये ज़िंदगी इसकी एक सज़ा है।
तब तक तुम्हारे अन्दर हयात-बख़्श मुक़व्वी कीड़े नुमू और तक़वियत नहीं पाते, तब तक तुम ज़िंदगी जीने के क़ाबिल नहीं हो पाते, ये कीड़े मरने लगते हैं और साथ में तुम भी। तुम ख़ाक-ज़ादे इसी तसव्वुर की पूजा करते आए हो कि ये ज़िंदगी जहन्नुम के हशरात में से एक कीड़ा है और तुम उस कीड़े के मालिक हो, यही कुल तुम्हारी औक़ात है लेकिन मैं परी-ज़ादा थी, ज़िद और हुसूल-ए-आन-ए-वाहिद में पूरे होने चाहिएँ यही मेरी सरिश्त का लाज़िमी तक़ाज़ा था सो मैं ज़िद करती रही।
एक पल के लिए भी मैंने ये नहीं सोचा कि ये ज़मीन-ज़ादा सिर्फ़ एक कीड़े का मालिक है... कुबड़ा, ठिठुरा, सिकुड़ा, पज़मुर्दा... कुन-फ़-यकून उसके इख़्तियार में नहीं है। किसने कहा कि मैं मुहब्बत के उस पैरहन को उतार फेंकना चाहती हूँ, महज़ मफ़रूज़ों की बुनियाद पर हतमी राय क़ायम करना तुम्हारा शुरू’ से वतीरा रहा है। तुमने कहा था ज़िंदगी के मुख़्तलिफ़ रंग होते हैं, उस रंग का इंतिज़ार करो जो तुम्हारा अपना होगा, ख़ालिस... आलाईशों, आमेज़िशों और फुज़लात से पाक... मुझको यक़ीन नहीं आ रहा था। इत्मीनान-ए-क़ल्ब के लिए वापिस पूछा तहय्युर, इस्तिजाब और इस्तिफ़हाम से पुर लहजे में, कब चढ़ेगा वो रंग। तुमने कोई जवाब नहीं दिया, बीवी का फ़ोन आ गया, बेटे की तबी’अत ख़राब, तुम्हारे पास पैसे नहीं, पर्स साफ़ किए और चल दिए और मैं उस रंग का इंतिज़ार करती रही...
नहीं, तुमने इंतिज़ार नहीं किया, वही किया जो नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे ज़हनी इर्तिक़ा और ज़ौक़-ए-जमाल के इर्तिफ़ा के लिए जो दलीलें और फ़लसफ़े मैंने इस्ति’माल किए वही अब तुम मेरे ख़िलाफ़ इस्ति’माल कर रही हो। मान तो तुमने भी तोड़ा फिर फ़र्द-ए-जुर्म सिर्फ़ मुझ पर ही क्यों? आख़िर, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी, तुमने मेरे बारे में एक-बार भी नहीं सोचा, आख़िर क्यों?
फ़िक्र मत करो जहाँ तुम इतने बुरे मर्ग-ज़दा इक़्दाम के बावुजूद इसी समाज में और उन्हीं अपनों के दरमियान चल फिर सकती हो जो तुम्हें एक बार पैदा करते हैं और बार-बार दफ़्न करते हैं तो फिर हम जैसे क्या मा’नी रखते हैं। तुमने मुझे भी तख़य्युल बना के रख दिया लेकिन इत्मीनान इस बात का है कि मुकम्मल वजूद में आने से क़ब्ल ही मर गया... कोई मुवाख़िज़ा नहीं, कोई मुहासिबा नहीं...
तुम्हें ज़िंदगी गुज़ारने के लिए जवाज़ की नहीं जुरअत की ज़रूरत है। जुरअत जो सिर्फ़ जहन्नुम-ज़ादों से मिल सकती थी। तुमने कहा था कि तुम शाइ’रा हो, सूरत-गर हो, फ़साना-नवीस हो, ज़ूद-हिस हो, तुम्हारी ख़्वाहिशों की तितली के पर नोच कर फेंक दिए गए हैं इसलिए तुम बाग़ी हो गई हो। तुम झूट बोलती हो। ज़ात के निहा-ख़ानों में महबूस परी बाग़ी कैसे हो सकती है।
ख़्वाहिशों और ना-रसाइयों की कर्ब-अंगेज़ पुर-अफ़्शाँ किर्चियों की कराह पीने वाली लड़की रिवायत-शिकन कैसे हो सकती है। भला समझौतों को कहीं बग़ावत का नाम दिया गया है? तुमने समझौते किए हैं, क़दम-क़दम पर सौ। एक और समझौता क्यों नहीं किया। एक और मुआ’हिदा सुल्ह-ए-हदीबिया जैसा। मुझे तुमसे मुहब्बत है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए जियो, मैं ख़ुद-ग़रज़ हूँ। ये एहसास कि तुम ज़िंदा हो मेरे ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी है। तुम्हारे बग़ैर ज़िंदगी, ज़िंदगी नहीं ला-हासिली का अ’ज़ाब है, कर्ब का नापैदा कनार है, नाकाम हसरतों का वसी’ रेगज़ार है। वो वक़्त जो हम चोरों की तरह साथ गुज़ारते हैं, कहीं किसी रेस्तोराँ के कोने में, किसी ख़स्ता होटल के बदबूदार कमरे में डर-डर कर। उन हज़ार साअ’तों से बेहतर है जो बग़ैर किसी कैफ़ियत, मुहब्बत और विसाल के यूँही गुज़र जाते हैं। ये ज़िंदगी तुमने मुंतख़ब की है, तुम शादी से गुरेज़ाँ हो लेकिन मौत से ख़ाइफ़ नहीं। मुझे अफ़सोस है कि तुम अच्छी ता’लीम, तमकीन और आसाइशें हासिल करने के बावुजूद, अशराफ़िया की सारी नज़ाकतों का पैरहन ओढ़ लेने के बावुजूद इस राज़ को नहीं समझ सकीं कि ज़िंदगी अपने फ़ितरी अ’नासिर में ख़ुद जीने का एक मुकम्मल जवाज़ है। ज़िंदगी ख़्वाह वो तुम्हारी हो या किसी रंडी की...
काश मैं रंडी होती, इ’ज़्ज़त-ए-नफ़स और ख़ानदानी शराफ़तों के तक़द्दुस और कसाफ़त से मुबर्रा होती, वजूद की ये लताफ़त क़ाबिल-ए-बरदाश्त तो होती। तो क्या रंडियाँ आज़ाद होती हैं? तुमने ग़ौर नहीं किया था किस तरह तुमने ये लफ़्ज़ अदा किया था, तुम्हारे अंदर की सारी कराहियत बाहर आ गई थी, और किस तरह मैं कैफे से उठकर चली आई थी, ज़ात का सारा कर्ब, ख़स्तगी, थकन और ज़िल्लत-ओ-मस्कनत वहीं कोल्ड काफ़ी के मग में उंडेल कर... मुझे यक़ीन था कि वो तुम पी जाओगे लेकिन तुमने ग़ुस्से से यूँ मेज़ उलट दी थी कि सब कुछ उलट-पलट गया, कोल्ड काफ़ी में मौजूद मेरा वजूद यूँ फ़र्श पर बिखरा पड़ा था कि मुझे मुंतहा-ए-विसाल में फ़ना होने का मंज़र याद आ गया जब तुम अब्ना-ए-शर्म-ओ-हया में क़तरा-फ़िशार उंडेल कर ग़ुस्ल-ख़ाने में चले गए और मैं यूँ चित लेटी रही, शर्मिंदा सी, सोचती रही कि ये कैसा विसाल है जो आसूदगी के साथ ख़त्म हो जाता है, ये विसाल नहीं महज़ नुक़्ता-ए-इत्तिसाल था, मैं चाहती थी कि तुम मेरे ऊपर यूँही पड़े रहो, सारी थकन, दर्द, कर्ब और महरूमियाँ साँसों की धूँकनी के साथ बाहर निकल जाने दो लेकिन आसूदा होने के बा’द तुम एक लाश में तबदील हो चुके थे और मैं भी, सो एक तिश्ना लाश पर एक आसूदा लाश का पड़े रहना क्या मा’नी?
लेकिन तुम मसीहा-नफ़स लाशों में रूह फूंकना जानते हो सो अंजाम-ए-कार मैं वापिस जी उठी। बुलबुले की सूरत बार-बार फ़ना होने के लिए, मैं फ़ना होती रही, तुम वजूद बख़्शते रहे। मैं मरती रही, तुम ज़िंदा करते रहे, ये सिलसिला चलता रहा फिर एक दिन तुमने मुझे चाक से उठा दिया, मेरी लताफ़त भी ना-क़ाबिल-ए-बर्दाश्त हो गई। तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि तुमसे मिलने के लिए कितने जोखम उठाने पड़ते हैं, कितने झूट बोलने पड़ते हैं, हर एक की नज़रों से बचने के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं। तुमने ही कहा था कि जब हम लम्हों में जीने लगते हैं तो ज़िंदगी मुख़्तसर हो जाती है। मुझे मुख़्तसर कर दिया गया है, लम्हों में जी रही हूँ... उधार मुस्त’आर लम्हे... अब घर से बाहर क़दम रखना मुश्किल हो गया है। मैं मौत से ख़ाइफ़ नहीं हूँ लेकिन शादी से गुरेज़ाँ ज़रूर हूँ कि ऐसी सूरत में हम दोनों को मार देंगे, एक न एक दिन उन्हें पता चल जाएगा, तुम्हारा बेटा यतीम हो जाएगा, तुम्हारी बे-क़सूर बीवी बेवा हो जाएगी, इसलिए जब तक ये खेल चल रहा है, चलने दो, मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई भी ’उम्र मरने के लिए अच्छी ’उम्र नहीं, लेकिन तुम मरने पर ब-ज़िद थे, तुम्हारा ख़याल था कि तुम्हारे मरने से तुम्हारा ख़ुदा नहीं मर जाता, तुम ठीक कहते थे लेकिन उस ख़ुदा को कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा है, ये हमें गुनाह करता हुआ क्यों देखता है, ये उन लोगों के दिलों को बदलता क्यों नहीं जो हमारे इस मुक़द्दस गुनाह का सबब हैं।
तुम ठीक कहते हो कि मैं कम-ज़र्फ़ हूँ, मैं कम-ज़र्फ़ हूँ कि तुम मुझे नहीं मिले, तुम्हारे ’इलावा हर चीज़ ज़र्फ़ से सिवा मिली... तरका, तहफ़्फ़ुज़, मीरास और महरूमी... उस दिन से जब तुम बड़े भाई के साथ घर तशरीफ़ लाए थे दिल-ओ-दिमाग़ के तार झनझना रहे हैं। रात के किसी पहर घुँघरुओं की छन-छन तेज़ हो जाती है। ये तार ख़ामोश होने के लिए तुम्हारी उँगलियों के मोहताज हैं। घुंघरू कभी भी उतारे जा सकते हैं, शादी की तारीख़ मुत’अय्यन हो गई है, हम सब आबाई गाँव जा रहे हैं, पुरखों को ख़िराज पेश करने। वहाँ भी कई गलियाँ हैं जो रोक-रोक कर तुम्हारा पता पूछेंगी। मौत मेरे क़रीब खड़ी है और उससे आँखें मिलाने की हिम्मत नहीं कि मौत किसी एक शक्ल में नहीं बाप, भाई, बहन और शौहर हर रूप में नज़र आ रही है। मुझे मा’लूम है मैं कैसे मारी जाऊँगी। काश “गुनाहों का पसीना” पोछने का मौक़ा’ मिलता। जो भी हो जाम-ए-फ़ना-ओ-बे-ख़ुदी।
शाम होते-होते मतलूबा जगह पर पहुँच गया था। डायरी की वरक़-गर्दानी भी जारी थी... मसाफ़त की गर्द ने थकन से निढाल कर दिया था लेकिन धूल थी कि तवानाई बन कर पैरों में दौड़ने लगी... यादों की, मुहब्बत की, वसीयत और हिर्मां-नसीबी की धूल... गोरकन के हाथ गर्म किए, बे-निशाँ हमवार क़ब्रों से बचता-बचाता, पतली क्यारियों से गुज़ारता हुआ वो मुझे एक क़ब्र के पास ले गया। क़ब्र ज़मीन के बराबर मौज़ून हो गई थी, आस-पास ख़ुद-रौ घास उगी हुई थी, साँप और बिच्छू का ख़ौफ़ बदन में सरायत करने लगा, मैंने दहशत की इसी पुर-असरार फ़िज़ा में सलाम किया जो सलाम कम ख़ौफ़ की लर्ज़िशों का इज़हार ज़ियादा था। मैंने महसूस किया कि जैसे कोई मुझसे हम-कलाम है।
“बशीर तुम क्यों नहीं आए?”
फूल चढ़ाने और दुआ’एँ मांगने के बा’द वहाँ से बसरात वापिस आना चाहता था लेकिन कोई एक ना-मा’लूम ताक़त मुझे रोक रही थी और मैं रुक गया। कोई आवाज़ मेरा तआ’क़ुब कर रही थी... ऐसे मत जाओ, आए हो तो कुछ बताकर जाओ, वो दुनिया कैसी है जो मुझसे छीन ली गई, कुछ बदला या नहीं, क्या अब भी बे-वफ़ाई, बद-चलनी, ग़ैरत और ज़मीन जायदाद के नाम पर बेटियाँ क़त्ल की जाती हैं? तुम मत करना, उस बच्ची के बारे में सोचना जिसका बाप उसकी क़ब्र खोद रहा था और वो बाप के कपड़े पर से मिट्टी साफ़ कर रही थी, पसीना पोछ रही थी, तुम ज़रूर सूचना कि ‘औरत का दिल वैजाइना में नहीं होता और न ही मर्द की मर्दानगी उसके उ’ज़्व-ए-मख़्सूस में होती है...
दिल चाहता था कि कुछ देर और रुकूँ लेकिन शाम के मुहीब साये और सन्नाटों का लर्ज़ा-ख़ेज़ शोर दरून-ए-ज़ात मुझे तोड़ फोड़ रहे थे। मैं रंजूर, महज़ून और फ़सुर्दा-दिल, बे-जान क़दमों के साथ वापिस आ गया कि कल अ’लल-सुब्ह दुबारा हाज़िरी दूँगा। एक आवाज़ मुसलसल तआ’क़ुब करती रही... बशीर तुम क्यों नहीं आए? क्या अब भी, क्या अब भी?
आज दर-ओ-दीवार गिर्या-कुनाँ होंगे, हर चीज़ कुछ बोलना चाहती होगी, हर एक के पास कहानियाँ होंगी, दीवारों के पास हसरत-ओ-लम्स की, अलमारी के पास डायरी की, बाथरूम के पास सिगरेट की, बाक़ियात में रोशनाई की एक शीशी पड़ी हुई है, इन लिखा हुआ है। अम्मी के पास भी कुछ कहानियाँ होंगी, मेरे पास भी हैं। मुझे याद है डैड हम लोगों में जीते थे, हँसते थे, बहुत भरपूर और फिर ख़ामोश हो जाते थे। बहुत ख़ामोश जिसे हम लोग भाँप नहीं पाते थे, वो हमारे दरमियान होते हुए भी नहीं होते थे। हमें लगता था कि वो कोई काम अधूरा छोड़ कर आए हैं इसलिए ज़हन उस तरफ़ चला गया है।
मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, उन्हें बाप होने का एहसास मुझसे मिला था। मैंने उनकी जवानी के दिन देखे थे, वो साल भर पहले भी जवान थे और सौ साल बा’द भी जवान ही होते... ज़िंदगी से भरपूर लेकिन अंदर से कहीं दीमक-ज़दा जिसका एहसास अब मुझे हो रहा है... मुझे याद है एक दिन वो हम भाई बहन को गार्डन में लेकर गए, हम लोग खेलने लगे और वो गार्डन में एक किनारे बेंच पर बैठ गए, कोई किताब उनके हाथ में थी, कुछ देर बा’द हमने देखा कि वो सर झुकाए दोनों हाथ अपने मुँह पर रखे किसी ख़याल में मुस्तग़रक़ हैं। हमें लगा कि वो कुछ सोच रहे हैं... घर में कई दिनों से बिजली नहीं है, अम्मी की तबी’अत ख़राब है, हमें खाने की कोई चीज़ नहीं दिलाई है... लेकिन जब पास पहुँचे तो देखा कि वो ज़ार-ओ-क़तार रो रहे थे, उन्होंने हम दोनों को भींच लिया और देर तक उसी आ’लम में बैठे रहे, आँसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हम कुछ पूछ नहीं सके... बुरा हो उस ‘औरत का जो कल ऑफ़िस आई और मुझसे मिले बग़ैर एक मुहर-बंद लिफ़ाफ़ा छोड़कर चली गई, लिफ़ाफ़े में एक डायरी थी, कुछ तस्वीरें, कुछ ख़ुतूत और एक नोट। एक तस्वीर जानी-पहचानी सी थी, डैड कई बार मुझे उनसे मिलवा चुके थे, मुझे याद है वो मेरे गाल पकड़ते हुए डैड से मुख़ातिब होतीं।
“बशीर ये बिलकुल तुम पर गया है। कितना क्यूट है! काश...”
और फिर डैड ख़ामोश हो जाते थे। तस्वीर को पलट कर देखता हूँ शायद वहाँ कोई नाम लिखा हो, लेकिन वहाँ जो कुछ लिखा था वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था... नाहीद जिसे मेरी वजह से दस साल क़ब्ल बद-चलन होने के नाम पर ज़िंदा-दर-गोर कर दिया गया... बाप ने बेटों की मुख़ालिफ़त के बावुजूद ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा उसके नाम कर दिया था। उनके मरते ही उसे अज़ीयत देने का सिलसिला शुरू’ कर दिया गया, उसने मुझसे अ’हद किया था कि वो हर हाल में ज़िंदा रहेगी इस लिए उसने ख़ुदकुशी नहीं की, बद-चलन, बे-ग़ैरत और बेवफ़ा होने का इल्ज़ाम बर्दाश्त करती रही ताँ-आँकि उसे मारने की कोशिश की गई, उसने मुज़ाहमत की और फिर जाँ-ब-हक़ हो गई, वो जाने से क़ब्ल मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन आख़िरी दिनों में मिज़ाजन बहुत मुतशद्दिद हो गई थी इसलिए मैंने नज़र-अंदाज़ कर दिया कि शादी के बा’द शायद ठीक हो जाएगी, मुझे यक़ीन था कि हम वापिस ज़रूर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे लेकिन फिर वो वक़्त नहीं आया। मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना था लेकिन मरना पड़ा, मैंने जीने की बहुत कोशिश की है लेकिन आगही का अ’ज़ाब क़तरा-क़तरा ख़ाक करता गया और फिर वो दिन आ गया... ज़िंदगी रायगाँ थी रायगाँ ही गई... मुझे नहीं याद मैं किस दिन मरा हूँ लेकिन फ़ुलाँ तारीख़ को उसकी बरसी है, हर साल बिला-नाग़ा मैं उसकी क़ब्र पर हाज़िरी देता आया हूँ इस बार तुम चले जाना... कह देना कि मुझे मु’आफ़ कर दे, शायद वो तुम्हारी बात सुन ले...
“डियर आंटी, अस्सामु-‘अलैकुम!”
“बशीर तुम क्यों नहीं आए?”
“डियर आंटी आज डैड की पहली बरसी है, उन्होंने आपको सलाम भेजा है!”
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.