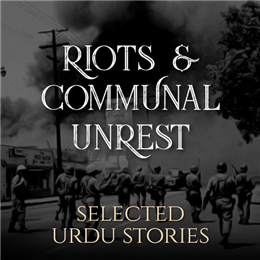मेरी मौत
स्टोरीलाइन
एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इसका मुख्य किरदार एक साम्प्रदायिक मुसलमान है। वह मुसलमान सरदारों से डरता भी है और उनसे नफरत भी करता है। वह अपने पड़ोसी सरदार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। लेकिन विभाजन के दौरान जब दंगे भड़क उठते हैं तब यही पड़ोसी सरदार उस मुसलमान को बचाता है।
लोग समझते हैं कि सरदार-जी मारे गए। नहीं। यह मेरी मौत है। पुराने ‘मैं’ की मौत। मेरे तअ'स्सुबात की मौत। उस मुनाफ़रत की मौत जो मेरे दिल में थी। मेरी यह मौत कैसे हुई? यह बताने के लिए मुझे अपने पुराने मुर्दा ‘मैं’ को ज़िंदा करना पड़ेगा। मेरा नाम शैख़ बुरहान-उद्दीन है।
जब दिल्ली और नई दिल्ली में फ़िर्का-वाराना क़त्ल-ओ-ग़ारत का बाज़ार गर्म और मुसलमानों का ख़ून सस्ता हो गया तो मैंने सोचा वाह-री क़िस्मत, पड़ोसी भी मिला तो सिख। हक़-ए-हम-साएगी अदा करना और जान बचाना तो कुजा, न जाने कब किरपाण भौंक दे।
बात यह है कि उस वक़्त तक मैं सिखों पर हँसता भी था, उनसे डरता भी था और काफ़ी नफ़रत भी करता था। आज से नहीं बचपन से। मैं शायद छः बरस का था जब पहली बार मैंने एक सिख को देखा था, जो धूप में बैठा अपने बालों में कंघी कर रहा था। मैं चिल्ला पड़ा, “अरे वो देखो, औरत के मुँह पर कितनी लंबी दाढ़ी!” जैसे-जैसे उ'म्र गुज़रती गई, ये इस्ते'जाब एक नस्ली नफ़रत में तबदील होता गया।
घर की बड़ी बूढ़ियाँ जब किसी बच्चे के बारे में ना-मुबारक बात का ज़िक्र करतीं। मसलन यह कि उसे निमोनिया हो गया था, या उसकी टांग टूट गई थी तो कहतीं, “अब से दूर किसी सिख फ़िरंगी को निमोनिया हो गया था या अब से दूर किसी सिख फ़रंगी की टांग टूट गई थी।” बा'द को मा'लूम हुआ कि यह कोसना 1857 ई. की यादगार था।
जब हिंदू मुसलमानों की जंग-ए-आज़ादी को दबाने में पंजाब के सिख राजों और उनकी फ़ौजों ने फ़िरंगियों का साथ दिया था। मगर उस वक़्त तारीख़ी हक़ाएक़ पर नज़र नहीं थी, सिर्फ़ एक मुबहम-सा ख़ौफ़, एक अ'जीब सी नफ़रत और एक अमीक़ तअ'स्सुफ़। डर अंग्रेज़ से भी लगता था और सिख से भी, मगर अंग्रेज़ से ज़्यादा।
मसलन जब मैं कोई दस बरस का था, एक रोज़ दिल्ली से अ'लीगढ़ जा रहा था। हमेशा थर्ड या इंटर में सफ़र होता था। सोचा कि अब की बार सेकेंण्ड क्लास में सफ़र करके देखा जाए। टिकट ख़रीद लिया और एक ख़ाली डिब्बे में बैठ कर गद्दों पर ख़ूब कूदा, बाथरूम के आईने में उचक-उचक कर अपना अक्स देखा। सब पंखों को एक साथ चला दिया। रौशनियों को कभी जलाया कभी बुझाया। मगर अभी गाड़ी के चलने में दो-तीन मिनट बाक़ी थे कि लाल-लाल मुँह वाले चार फ़ौजी गोरे आपस में डैम-ब्लडी क़िस्म की गुफ़्तगू करते हुए दर्जे में घुस आए।
उनको देखना था कि सेकेण्ड क्लास में सफ़र करने का शौक़ रफ़ू-चक्कर हो गया और अपना सूटकेस घसीटता में भागा और एक निहायत खचा-खच भरे हुए थर्ड क्लास के डिब्बे में आकर दम लिया। यहाँ देखा कोकई सिख दाढ़ियाँ खोले, कच्छे पहने बैठे थे मगर मैं उनसे डर कर दर्जा छोड़कर नहीं भागा। सिर्फ़ उनसे ज़रा फ़ासले पर बैठ गया।
हाँ, तो डर सिखों से भी लगता था और अंग्रेज़ों से उनसे ज़्यादा। मगर अंग्रेज़ अंग्रेज़ थे और कोट पतलून पहनते थे जो मैं भी पहनना चाहता था और डैम-ब्लडीफ़ूल वाली ज़बान बोलते थे जो मैं भी सीखना चाहता था। इसके अ'लावा वे हाकिम थे और मैं भी छोटा-मोटा हाकिम बनना चाहता था। वे काँटे छुरी से खाना खाते थे और मैं भी काँटे छुरी से खाना खाने का ख़्वाहाँ था ताकि दुनिया मुझे भी मुहज़्ज़ब और मुतमद्दिन समझे मगर सिखों से जो डर लगता था, वो हिक़ारत-आमेज़।
कितने अ'जीब-उल-ख़िलक़त थे ये सिख जो मर्द हो कर भी सिर के बाल औरतों की तरह लंबे-लंबे रखते थे। यह और बात है कि अंग्रेज़ी फ़ैशन की नक़ल में सिर के बाल मुंडाना कुछ मुझे भी पसंद नहीं था। अब्बा के इस हुक्म के बा-वजूद कि हर जुमा को सर के बाल ख़शख़शी कराए जाएँ, मैंने बाल ख़ूब बढ़ा रखे थे, ताकि हॉकी और फूटबॉल खेलते वक़्त बाल हवा में उड़ें जैसे अंग्रेज़ी खिलाड़ियों के।
अब्बा कहते, “यह क्या औरतों की तरह पट्टे बढ़ा रखे हैं मगर अब्बा तो थे ही पुराने दक़्यानूसी ख़याल के। उनकी बात कौन सुनता था। उनका बस चलता तो सिर पर उस्तरा चलवा कर बचपन में भी हमारे चेहरों पर दाढ़ियाँ बंधवा देते...” हाँ इस पर याद आया कि सिखों के अ'जीब-अल-ख़िलक़त होने की दूसरी निशानी उनकी दाढ़ियाँ थीं और फिर दाढ़ी, दाढ़ी में भी फ़र्क़ होता है।
मसलन अब्बा की दाढ़ी जिसको निहायत एहतिमाम से नाई फ़्रेंच कट बनाया करता था या ताया अब्बा की जो नुकीली और चोंचदार थी। मगर यह भी क्या कि दाढ़ी को कभी क़ैंची लगे ही नहीं, झाड़-झंकार की तरह बढ़ती ही रहे बल्कि तेल और दही और न जाने क्या-क्या मलकर बढ़ाई जाए और जब कई फुट लंबी हो जाएगी तो इसमें कंघी की जाए जैसे औरतें सर के बालों में करती हैं... औरतें या मुझ जैसे स्कूल के फ़ैशने-बल लड़के। इसके अ'लावा दादा जान की दाढ़ी भी कई फुट लंबी थी और वह भी उसमें कंघी करते थे। मगर दादा जान की बात और थी। आख़िर वह... मेरे दादा जान ठहरे और सिख फिर सिख थे।
मैट्रिक करने के बा'द मुझे पढ़ने लिखने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ भेजा गया। कॉलेज में जो पंजाबी लड़के पढ़ते थे, उनको हम दिल्ली और यू.पी. वाले नीच, जाहिल और उज्जड़ समझते थे। न बात करने का सलीक़ा न खाने पीने की तमीज़। तहज़ीब-ओ-तमद्दुन छू नहीं गए थे। गँवार, लठ। ये बड़े-बड़े लस्सी के गिलास पीने वाले भला केवड़ेदार फ़ालूदे और लिप्टन की चाय की लज़्ज़त क्या जानें। ज़बान निहायत ना-शाइस्ता। बात करें तो मा'लूम हो लड़ रहे हैं।
अस्सी, तुस्सी, साडे, तुहाडे... लाहौल-वला-क़ुव्वत। मैं तो हमेशा उन पंजाबियों से कतराता था मगर ख़ुदा भला करे हमारे वार्डन साहब का कि उन्होंने एक पंजाबी को मेरे कमरे में जगह दे दी। मैंने सोचा चलो जब साथ ही रहना है तो थोड़ी बहुत हद तक दोस्ती ही कर ली जाए। कुछ दिनों में काफ़ी गाढ़ी छनने लगी। उसका नाम ग़ुलाम रसूल था। रावलपिंडी का रहने वाला था। काफ़ी मज़ेदार आदमी था और लतीफ़े ख़ूब सुनाया करता था।
अब आप कहेंगे ज़िक्र शुरू' हुआ था सरदार साहब का। यह ग़ुलाम रसूल कहाँ से टपक पड़ा। मगर अस्ल में ग़ुलाम रसूल का इस क़िस्से से क़रीबी तअ'ल्लुक़ है। बात यह है कि वो जो लतीफ़े सुनाता था वो आम तौर से सिखों के बारे में होते थे जिनको सुन-सुन कर मुझे पूरी सिख क़ौम की आ'दात-ओ-ख़साइ'स, उनकी नस्ली ख़ुसूसिआ'त और इज्तिमाई कैरेक्टर का ब-ख़ूबी इ'ल्म हो गया था। ब-क़ौल ग़ुलाम रसूल,
“सिख तमाम बे-वक़ूफ़ और बुद्धू होते हैं। बारह बजे तो उनकी अ'क़्ल बिल्कुल ख़ब्त हो जाती है।” इसके सुबूत में कितने ही वाक़िआ'त बयान किए जा सकते हैं। मसलन एक सरदार-जी दिन के बारह बजे साईकिल पर सवार अमृतसर के हॉल बाज़ार से गुज़र रहे थे। चौराहे पर एक सिख कांस्टेबल ने रोका और पूछा, “तुम्हारी साईकल की लाईट कहाँ है?” साईकिल सवार सरदार-जी गिड़गिड़ा कर बोले, “जमादार साहब अभी-अभी बुझ गई है। घर से जलाकर तो चला था।”
इस पर सिपाही ने चालान करने की धमकी दी। एक राह चलते सफ़ेद दाढ़ी वाले सरदार-जी ने बीच-बचाव कराया, “चलो भई कोई बात नहीं। लाईट बुझ गई है तो अब जला लो।” और इसी क़िस्म के सैंकड़ों क़िस्से ग़ुलाम रसूल को याद थे और उन्हें जब वो पंजाबी मुकालमों के साथ सुनाता था तो सुनने वालों के पेट में बल पड़ जाते थे। अस्ल में उनको सुनने का मज़ा पंजाबी ही में था क्योंकि उजड्ड सिखों की अ'जीब-ओ-ग़रीब हरकतों के बयान करने का हक़ कुछ पंजाबी जैसी उजड्ड ज़बान ही में हो सकता है।
सिख न सिर्फ़ बे-वक़ूफ़ और बुद्धू थे बल्कि गंदे थे जैसा कि एक सुबूत तो ग़ुलाम रसूल का (जिसने सैकड़ों सिखों को देखा था) यह था कि वे बाल नहीं मुंडाते थे। इसके अ'लावा बर-ख़िलाफ़ हम साफ़-सुथरे नमाज़ी मुसलमानों के जौहर अठवारे जुमा के जुमा ग़ुस्ल करते हैं, ये सिख कच्छा बाँध सबके सामने नल के नीचे बैठ कर नहाते तो रोज़ हैं मगर अपने बालों और दाढ़ी में न जाने क्या-क्या गंदी और ग़लीज़ चीज़ें मलते हैं। मसलन दही। वैसे तो मैं भी सिर में लाइम जूस ग्लिसरीन लगाता हूँ जो किसी क़दर गाढ़े गाढ़े दूध से मुशाबह होती है मगर उसकी बात और है। वो विलायत की मशहूर परफ़्यूमर फ़ैक्ट्री से निहायत ख़ूबसूरत शीशी में आती है और दही किसी गंदे-संदे हलवाई की दुकान से।
ख़ैर जी हमें दूसरों के रहने-सहने के तरीक़ों से क्या लेना। मगर सिखों का सबसे बड़ा क़ुसूर यह था कि ये लोग अक्खड़पन, बद-तमीज़ी और मार-धाड़ में मुसलमानों का मुक़ाबला करने की जुरअत करते थे। अब दुनिया जानती है कि एक अकेला मुसलमान दस हिंदुओं या सिखों पर भारी होता है। मगर फ़िर ये सिख मुसलमानों के रौ'ब को नहीं मानते थे। किरपाणें लटकाए, अकड़-अकड़ कर मूँछों बल्कि दाढ़ी पर भी ताव देते चलते थे। ग़ुलाम रसूल कहता उनकी हेकड़ी एक दिन हम ऐसी निकालेंगे कि ख़ालसा जी याद ही तो करेंगे।
कॉलेज छोड़े कई साल गुज़र गए। तालिब-ए-इ'ल्म से मैं क्लर्क और क्लर्क से हैड क्लर्क बन गया। अलीगढ़ का हॉस्टल छोड़ नई दिल्ली में एक सरकारी क्वार्टर में रहना-सहना इख़्तियार कर लिया। शादी हो गई बच्चे हो गए, मगर कितनी ही मुद्दत के बा'द मुझे ग़ुलाम रसूल का वह कहना याद आया जब एक सरदार साहब मेरे बराबर के क्वार्टर में रहने को आए... ये रावलपिंडी से बदली करा कर आए थे क्योंकि रावलपिंडी के ज़िला में ग़ुलाम रसूल की पेशिन-गोई के ब-मूजिब सरदारों की हेकड़ी अच्छी तरह से निकाली गई थी। मुजाहिदों ने उनका सफ़ाया कर दिया था। बड़े सूरमा बनते थे, किरपाणें लिए फिरते थे। बहादुर मुसलमानों के सामने उनकी एक न बनी।
उनकी दाढ़ियाँ मूंड कर उनको मुसलमान बनाया गया था। ज़बरदस्ती उनका खतना किया गया था। हिंदू प्रेस हस्ब-ए-आ'दत मुसलमानों को बदनाम करने के लिए यह लिख रहा था कि सिख औरतों और बच्चों को भी मुसलमानों ने क़त्ल किया है। हालाँकि यह इस्लामी रिवायात के ख़िलाफ़ है। कोई मुसलमान मुजाहिद कभी औरत या बच्चे पर हाथ नहीं उठाता। रहीं औरतों और बच्चों की लाशों की तस्वीरें जो छापी जा रही थीं, वो या तो जाली थीं और या सिखों ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ख़ुद अपनी औरतों और बच्चों को क़त्ल किया होगा।
रावलपिंडी और मग़रिबी पंजाब के मुसलमानों पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने हिंदू और सिख लड़कियों को भगाया था, हालाँकि वाक़िआ' सिर्फ़ इतना है कि मुसलमानों की जवाँ-मर्दी की धाक बैठी है और अगर नौजवान मुसलमानों पर हिंदू और सिख लड़कियाँ ख़ुद ही लट्टू हो जाएँ तो उनका क्या क़ुसूर है कि वे तब्लीग़-ए-इस्लाम के सिलसिले में इन लड़कियों को अपनी पनाह में ले लें। हाँ तो सिखों की नाम-निहाद बहादुरी का भांडा फूट गया था। भला अब तो मास्टर तारा सिंह लाहौर में किरपाण निकाल कर मुसलमानों को धमकियाँ दे। पिंडी से भागे हुए सरदार और उसकी ख़स्ता-हाली को देखकर मेरा सीना अ'ज़मत-ए-इस्लाम की रूह से भर गया।
हमारे पड़ोसी सरदार-जी की उ'म्र कोई साठ बरस की होगी। दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी, हालाँकि मौत के मुँह से बच कर आए थे। मगर ये हज़रत हर वक़्त दाँत निकाले हँसते रहते थे, जिससे साफ़ ज़ाहिर होता था कि वह दरअस्ल कितना बे-वक़ूफ़ और बे-हिस है। शुरू' शुरू' में उन्होंने मुझे अपनी दोस्ती के जाल में फँसाना चाहा। आते-जाते ज़बरदस्ती बातें करना शुरू' कर दीं। न जाने सिखों का कौन सा त्यौहार था, उस दिन प्रसाद की मिठाई भी भेजी (जो मेरी बीवी ने फ़ौरन महतरानी को दे दी) पर मैंने ज़्यादा मुँह न लगाया। कोई बात हुई सूखा-सा जवाब दे दिया और बस। मैं जानता था कि सीधे मुँह दो-चार बातें कर लीं तो ये पीछे ही पड़ जाएगा। आज बातें तो कल गालम-गुफ़्तार।
गालियाँ तो आप जानते ही हैं, सिखों की दाल रोटी होती हैं। कौन अपनी ज़बान गंदी करे ऐसे लोगों से तअ'ल्लुक़ात बढ़ा कर। हाँ एक इतवार की दोपहर को मैं अपनी बीवी को सिखों की हिमाक़त के क़िस्से सुना रहा था। उसका अ'मली सुबूत देने के लिए ऐ'न बारह बजे मैंने अपने नौकर को सरदार-जी के यहाँ भेजा कि पूछ कर आए क्या बजा है?
उन्होंने कहलवा दिया, “बारह बज कर दो मिनट हुए हैं।” मैंने कहा, “बारह बजे का नाम लेते घबराते हैं ये।” और हम ख़ूब हँसे। इसके बा'द मैंने कई बार बे-वक़ूफ़ बनाने के लिए सरदार-जी से पूछा, “क्यों सरदार-जी बारह बज गए?” और वो बे-शर्मी से दाँत फाड़ कर जवाब देते, “जी असाँ दे ताँ चौबीस घंटे बारह बजे रहते हैं।” और यह कह कर ख़ूब हँसे। गोया ये बड़ा मज़ाक़ हुआ।
मुझे सबसे ज़्यादा डर बच्चों की तरफ़ से था। अव्वल तो किसी सिख का ए'तिबार नहीं। कब बच्चे ही के गले पर किरपाण चला दे। फिर ये लोग रावलपिंडी से आए थे। ज़रूर दिल में मुसलमानों की तरफ़ से कीना रखते होंगे और इंतिक़ाम लेने की ताक में होंगे। मैंने बीवी को ताकीद कर दी थी कि बच्चे हरगिज़ सरदार-जी के क्वार्टर की तरफ़ न जाने दिए जाएँ। पर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। चंद रोज़ बाद मैंने देखा कि सरदार की छोटी लड़की मोहिनी और उनके पोतों के साथ खेल रहे हैं।
यह बच्ची जिसकी उम्र मुश्किल से दस बरस की होगी, सच-मुच मोहिनी ही थी। गोरी चिट्टी, अच्छा नाक नक़्शा, बड़ी ख़ूबसूरत। कम-बख़्तों की औरतें काफ़ी ख़ूबसूरत होती हैं। मुझे याद आया कि ग़ुलाम रसूल कहा करता था कि अगर पंजाब से सिख मर्द चले जाएँ और अपनी औरतों को छोड़ जाएँ तो फिर हूरों की तलाश की ज़रूरत नहीं। हाँ तो जब मैंने बच्चों को सरदार-जी के बच्चों के साथ खेलते देखा तो मैं उनको घसीटता हुआ अंदर ले आया और ख़ूब पिटाई की। फिर मेरे सामने कम से कम उनकी हिम्मत न हुई कि उधर का रुख़ करें।
बहुत जल्द सिखों की असलियत पूरी तरह ज़ाहिर हो गई। रावलपिंडी से तो डरपोकों की तरह पिट कर भाग कर आए थे। पर मशरिक़ी पंजाब में मुसलमानों को अक़ल्लियत में पाकर उन पर ज़ुल्म ढाना शुरू' कर दिया... हज़ारों बल्कि लाखों मुसलमानों को जाम-ए-शहादत पीना पड़ा। इस्लामी ख़ून की नदियाँ बह गईं। हज़ारों औरतों को बरहना कर के जुलूस निकाला गया। जब से मग़रिबी पंजाब से भागे हुए सिख इतनी बड़ी ता'दाद में दिल्ली में आने शुरू' हुए थे, इस वबा का यहाँ तक पहुँचना यक़ीनी हो गया था। मेरे पाकिस्तान जाने में अभी चंद हफ़्ते की देर थी। इसलिए मैंने अपने बड़े भाई के साथ अपने बीवी बच्चों को हवाई जहाज़ से कराची भेज दिया और ख़ुद ख़ुदा पर भरोसा कर के ठहर रहा।
हवाई जहाज़ में सामान तो ज़्यादा नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने पूरी एक वैगन बुक करा ली मगर जिस दिन सामान चढ़ाने वाले थे, उस दिन सुना कि पाकिस्तान जाने वाली गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं। इसलिए सामान घर में ही पड़ा रहा।
15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाया गया मगर मुझे इस आज़ादी में क्या दिलचस्पी थी। मैंने छुट्टी मनाई, और दिन-भर लेटा डॉन और पाकिस्तान टाईम्स का मुताला' करता रहा। दोनों में नाम निहाद... आज़ादी के चीथड़े उड़ाए गए थे और साबित किया गया था कि किस तरह हिंदूओं और अंग्रेज़ों ने मिलकर मुसलमानों का ख़ात्मा करने की साज़िश की थी। वो तो हमारे क़ाइद-ए-आज़म का ए'जाज़ था कि पाकिस्तान लेकर ही रहे।
अगरचे अंग्रेज़ों ने हिंदुओं और सिखों के दबाव में आकर अमृतसर को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया। हालाँकि दुनिया जानती है, अमृतसर ख़ालिस इस्लामी शहर है और यहाँ की सुनहरी मस्जिद जो (GOLDEN MOSQUE) के नाम से दुनिया में मशहूर है... नहीं वह तो गुरूद्वारा है और (GOLDEN TEMPLE) कहलाता है।
सुनहरी मस्जिद तो दिल्ली में है। सुनहरी मस्जिद ही नहीं, जामा मस्जिद भी। लाल क़िला है, निज़ामउद्दीन औलिया का मज़ार, हुमायूँ का मक़बरा, सफ़दरजंग का मदरसा। ग़रज़ कि चप्पे-चप्पे पर इस्लामी हुकूमत के निशान पाए जाते हैं। फिर भी आज उसी दिल्ली बल्कि कहना चाहिए कि शाहजहानाबाद पर हिंदू साम्राज्य का झंडा बुलंद किया जा रहा था... रो ले अब दिल खोल ऐ दीदा-ए-ख़ूँ-बार... और यह सोच कर मेरा दिल भर आया कि दिल्ली जो कभी मुसलमानों का पाया-ए-तख़्त था, तहज़ीब-ओ-तमद्दुन का गहवारा था, हमसे छीन लिया गया था और हमें मग़रिबी पंजाब और सिंध, ब्लूचिस्तान जैसे उजड्ड और ग़ैर-मुतमद्दिम इलाक़े में ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है।
जहाँ किसी को शुस्ता उर्दू ज़बान भी बोलनी नहीं आती। जहाँ शलवार जैसा मज़हका-ख़ेज़ लिबास पहना जाता है। जहाँ हल्की फुल्की पाव भर में बीस चपातियों की बजाए दो-दो सैर की नानें खाई जाती हैं।
फिर मैंने अपने दिल को मज़बूत कर के, क़ाइद-ए-आज़म और पाकिस्तान की ख़ातिर यह क़ुर्बानी तो हमें देनी ही होगी, मगर फिर भी दिल्ली छोड़ने के ख़याल से दिल मुरझाया ही रहा... शाम को जब मैं बाहर निकला और सरदार-जी ने दाँत निकाल कर कहा, “क्यों बाबू जी तुमने आज कुछ ख़ुशी नहीं मनाई?” तो मेरे जी में आई कि उसकी दाढ़ी में आग लगा दूँ। हिंदुस्तान की आज़ादी और दिल में सिखा शाही आख़िर रंग ला कर ही रही। अब मग़रिबी पंजाब से आए हुए रिफ्यूजीज़ (REFUGEES) की ता'दाद हज़ारों से लाखों तक पहुँच गई। ये लोग दरअस्ल पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अपने घर-बार छोड़कर, वहाँ से भागे थे।
यहाँ आकर गली कूचों में अपना रोना-रोते फिरते थे। कांग्रेसी प्रोपेगैंडा मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़ोरों पर चल रहा था और इस बार कांग्रेसियों ने चाल यह चली कि बजाए कांग्रेस के नाम लेने के, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और शहीदी दल के नाम से काम कर रहे थे। हालाँकि दुनिया जानती है कि ये हिंदू चाहे कांग्रेसी हो या महासभाई, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। चाहे दुनिया को दिखाने की ख़ातिर वे ब-ज़ाहिर गांधी और जवाहर लाल नेहरू को गालियाँ ही क्यों न देते हों।
एक दिन सुब्ह को ख़बर आई कि दिल्ली में क़त्ल-ए-आ'म शुरू' हो गया। क़रोल बाग़ में मुसलमानों के सैकड़ों घर फूँक दिए गए। चाँदनी चौक के मुसलमानों की दूकानें लूट ली गईं और हज़ारों का सफ़ाया हो गया। ये था कांग्रेस के हिंदू राज का नमूना। ख़ैर मैंने सोचा नई दिल्ली तो मुद्दत से अंग्रेज़ों का शहर रहा है। लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ रहते हैं। कमांडर-इन-चीफ़ यहाँ रहता है।
कम से कम यहाँ वे मुसलमानों के साथ ऐसा ज़ुल्म न होने देंगे। यह सोच कर मैं दफ़्तर की तरफ़ चला। क्योंकि उस दिन मुझे प्रोविडेंट फ़ंड का हिसाब करना था और दरअस्ल इसीलिए मैंने पाकिस्तान जाने में देर की थी। अभी गोल मार्किट के पास पहुँचा ही था कि दफ़्तर का एक हिंदू बाबू मिला। उसने कहा, “ये क्या कर रहे हो। जाओ वापस जाओ। बाहर न निकलना। कनॉट प्लेस में बलवाई मुसलमानों को मार रहे हैं।” मैं वापस भाग आया।
अपने स्कावयर में पहुँचा ही था कि सरदार-जी से मुड़भेड़ हो गई। कहने लगे, “शैख़-जी फ़िक्र न करना। जब तक हम सलामत हैं तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता।” मैंने सोचा उसकी दाढ़ी के पीछे कितना मक्र छुपा हुआ है। दिल में तो ख़ुश है। चलो अच्छा हुआ मुसलमानों का सफ़ाया हो रहा है... मगर ज़बानी हम-दर्दी जता कर मुझ पर एहसान कर रहा है बल्कि शायद मुझे चिढ़ाने के लिए यह कह रहा है।
क्योंकि सारे स्कवायर में बल्कि तमाम सड़क पर मैं तन-ए-तन्हा मुसलमान था। पर मुझे उन काफ़िरों का रहम-ओ-करम नहीं चाहिए। मैं सोच कर अपने क्वार्टर में आ गया। मैं मारा भी जाऊँगा तो दस बीस को मार कर। सीधा अपने कमरे में गया जहाँ पलंग के नीचे, मेरी दोनाली शिकारी बंदूक़ रखी थी। जब से फ़सादात शुरू' हुए थे, मैंने कारतूस और गोलियों का भी काफ़ी ज़ख़ीरा जमा कर रखा था। पर वहाँ बंदूक़ न मिली। सारा घर छान मारा। उसका कहीं पता न चला।
“क्यों हुज़ूर क्या ढूँढ रहे हैं आप?”
यह मेरा वफ़ादार मुलाज़िम ममदू था।
“मेरी बंदूक़ क्या हुई?” मैंने पूछा। उसने कोई जवाब न दिया। मगर उसके चेहरे से साफ़ ज़ाहिर था कि उसे मा'लूम है। शायद उसने छुपाई है, या चुराई है।
“बोलता क्यों नहीं?” मैंने डाँट कर कहा। तब हक़ीक़त मा'लूम हुई कि ममदू ने मेरी बंदूक़ चुरा कर अपने चंद दोस्तों को दे दी थी, जो दरियागंज में मुसलमानों की हिफ़ाज़त के लिए हथियारों का ज़ख़ीरा जमा कर रहे थे।
“कई सौ बंदूक़ें हैं सरकार हमारे पास। सात मशीन गनें, दस रिवॉल्वर और एक तोप। काफ़िरों को भून कर रख देंगे, भून कर।”
मैंने कहा, “दरियागंज में मेरी बंदूक़ से काफ़िरों को भून दिया गया तो इसमें मेरी हिफ़ाज़त कैसे होगी। मैं तो यहाँ निहत्ता काफ़िरों के नर्ग़े में फँसा हुआ हूँ। यहाँ मुझे भून दिया गया तो कौन ज़िम्मेदार होगा?” मैंने ममदू से कहा वो किसी तरह छुपता-छुपाता दरियागंज तक जाए और वहाँ से मेरी बंदूक़ और सौ दो सौ कारतूस लेकर आए।
वो चला तो गया मगर मुझे यक़ीन था कि अब वो लौट कर नहीं आएगा। अब मैं घर में बिल्कुल अकेला रह गया था। सामने कॉर्निस पर मेरी बीवी और बच्चों की तस्वीरें ख़ामोशी से मुझे घूर रही थीं। यह सोच कर मेरी आँखों में आँसू आ गए कि अब उनसे कभी मुलाक़ात होगी भी या नहीं लेकिन फिर यह ख़याल करके इत्मिनान भी हुआ कि कम से कम वे तो ख़ैरियत से पाकिस्तान पहुँच गए थे। काश मैंने प्रोविडेंट फ़ंड का लालच न किया होता और पहले ही चला गया होता। पर अब पछताने से क्या होता है।
“सत शिरी अकाल... हर हर महादेव।” दूर से आवाज़ें क़रीब आ रही थीं। ये बलवाई थे। ये मेरी मौत के हरकारे थे। मैंने ज़ख़्मी हिरन की तरह इधर-उधर देखा, जो गोली खा चुका हो और जिसके पीछे शिकारी कुत्ते लगे हों। बचाव की कोई सूरत न थी। क्वार्टर के किवाड़ पतली लकड़ी के थे और उनमें शीशे लगे हुए थे। अगर मैं बंद हो कर बैठ भी रहा तो दो मिनट में बलवाई किवाड़ तोड़ कर अंदर आ सकते थे।
“सत शिरी अकाल। हर हर महादेव।” आवाज़ें और क़रीब आ रही थीं। मेरी मौत क़रीब आ रही थी। इतने में दरवाज़े पर दस्तक हुई। सरदार-जी दाख़िल हुए, “शैख़-जी तुम हमारे क्वार्टर में आ जाओ। जल्दी करो।” ब-ग़ैर सोचे समझे अगले लम्हे में सरदार-जी के बरामदे की चक्कों के पीछे था। मौत की गोली सन से मेरे सर पर से गुज़र गई। क्योंकि मैं वहाँ दाख़िल ही हुआ था कि एक लारी आकर रुकी और उसमें से दस पंद्रह नौजवान उतरे। उनके लीडर के हाथ में एक टाइप की हुई फ़हरिस्त थी। क्वार्टर 8 शैख़ बुरहान-उद्दीन। उसने काग़ज़ पर नज़र डालते हुए हुक्म दिया और यह ग़ोल का ग़ोल मेरे क्वार्टर पर टूट पड़ा। मेरी गृहस्थी की दुनिया मेरी आँखों के सामने उजड़ गई। लुट गई। कुर्सियाँ, मेज़ें, संदूक़, तस्वीर, किताबें, दरियाँ, क़ालीन, यहाँ तक कि मैले कपड़े हर चीज़ लारी पर पहुँचा दी गई।
डाकू!
लुटेरे!
क़ज़्ज़ाक़!
और ये सरदार-जी जो ब-ज़ाहिर हम-दर्दी जता कर मुझे यहाँ ले आए थे। ये कौन से कम लुटेरे थे? बाहर जा कर बलवाइयों से कहने लगे, “ठहरिए साहब। इस घर पर हमारा हक़ ज़्यादा है। हमें भी इस लूट में हिस्सा मिलना चाहिए”, और यह कह कर उन्होंने अपने बेटे और बेटी को इशारा किया और वो भी लूट में शामिल हो गए। कोई मेरी पतलून उठाए चला आ रहा है। कोट सूटकेस, कोई मेरी बीवी बच्चों की तस्वीरें भी ला रहा है और ये सब माल-ए-ग़नीमत सीधा अंदर के कमरे में जा रहा था।
अच्छा रे सरदार ज़िंदा रहा तो तुझसे भी समझूँगा। पर उस वक़्त तो मैं चूँ भी नहीं कर सकता था क्योंकि फ़सादी जो सबके सब मुसल्लह थे, मुझसे चंद गज़ के फ़ासले पर थे। अगर उन्हें कहीं मा'लूम हो गया कि मैं यहाँ हूँ।
“अरे अन्दर आओ तूसी!” दफ़अ'तन मैंने देखा कि सरदार-जी नंगी किरपाण हाथ में लिए मुझे अंदर बुला रहे हैं। मैंने एक बार उस दढ़ियल चेहरे को देखा जो लूट मार की भाग दौड़ से और भी ख़ौफ़नाक हो गया था, और फिर किरपाण को जिसकी चमकीली धार मुझे दावत-ए-मौत दे रही थी, बहस करने का मौक़ा नहीं था। अगर मैं कुछ भी बोला और बलवाइयों ने सुन लिया तो एक गोली मेरे सीने के पार होगी। किरपाण और बंदूक़ में से एक को पसंद करना था। मैंने सोचा इन दस बंदूक़-बाज़ बलवाइयों से किरपाण वाला बूढ्ढा बेहतर है। मैं कमरे में चला गया... झिजकता हुआ ख़ामोश।
“उत्थे नहीं। और अन्दर आओ।” मैं और अंदर के कमरे में चला गया, जैसे बकरा क़साई के साथ ज़िब्ह-ख़ाने में दाख़िल होता है। मेरी आँखें किरपाण की धार से चौंधियाती जा रही थीं।
“ये लो जी। अपनी चीज़ें सँभाल लो।” यह कह कर सरदार-जी ने वो तमाम सामान मेरे सामने रख दिया जो उन्होंने और उनके बच्चों ने झूठ-मूठ की लूट में हासिल किया था। सरदारनी बोली, “बेटा हम तो तेरा कुछ भी सामान न बचा सके।” मैं कोई जवाब न दे सका। इतने में बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। बलवाई मेरी लोहे की अलमारी को बाहर निकाल रहे थे और उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसकी चाबियाँ मिल जातीं तो सब मुआमला आसान हो जाता।
“चाबियाँ तो इसकी पाकिस्तान में मिलेंगी। भाग गया न डरपोक कहीं का। मुसलमान का बच्चा था तो मुक़ाबला करता...”
नन्ही मोहिनी मेरी बीवी के चंद रेशमी क़मीस और ग़रारे न जाने किस से छीन कर ला रही थी कि उसने ये सुना। वो बोली, “तुम बड़े बहादुर हो शैख़-जी डरपोक क्यों होने लगे। वो तो पाकिस्तान नहीं गए।”
“नहीं गया तो यहाँ से कहीं मुँह काला कर गया।”
“मुँह काला क्यों करते वो तो हमारे यहाँ...”
मेरे दिल की हरकत एक लम्हे के लिए बंद हो गई। बच्ची अपनी ग़लती का एहसास करते ही ख़ामोश हो गई। मगर उन बलवाइयों के लिए यही काफ़ी था। सरदार-जी पर जैसे ख़ून सवार हो गया। उन्होंने मुझे अंदर के कमरे में बंद कर के कुंडी लगा दी। अपने बेटे के हाथ में किरपाण दी और ख़ुद बाहर निकल गए। बाहर क्या हुआ ये मुझे ठीक तरह मा'लूम न हुआ।
थप्पड़ों की आवाज़... फिर मोहिनी के रोने की आवाज़ और उसके बा'द सरदार-जी की आवाज़। पंजाबी गालियाँ कुछ समझ में न आया कि किसे गालियाँ दे रहे हैं और क्यों। मैं चारों तरफ़ से बंद था। इसलिए ठीक सुनाई न देता था। और फिर... गोली चलने की आवाज़... सरदारनी की चीख़... लारी रवाना होने की गड़-गड़ाहट और फिर तमाम स्कवायर पर जैसे सन्नाटा छा गया। जब मुझे कमरे की क़ैद से निकाला गया तो सरदार-जी पलंग पर पड़े थे और उनके सीने के क़रीब, सफ़ेद क़मीस ख़ून से सुर्ख़ हो रही थी। उनका लड़का हम-साए के घर से डॉक्टर को टेलीफ़ोन कर रहा था।
“सरदार-जी ये तुमने क्या किया?” मेरी ज़बान से न जाने ये अल्फ़ाज़ कैसे निकले। मैं मबहूत था... मेरी बरसों की दुनिया, ख़यालात, महसूसात, तअ'स्सुबात की दुनिया खंडर हो गई थी।
“सरदार-जी यह तुमने क्या किया?”
“मुझे क़र्ज़ा उतारना था बेटा!”
“क़र्ज़ा?”
“हाँ रावलपिंडी में तुम्हारे जैसे ही एक मुसलमान ने अपनी जान देकर मेरी और मेरे घर वालों की जान और इज़्ज़त बचाई थी।”
“क्या नाम था उसका सरदार-जी?”
“ग़ुलाम रसूल!”
“ग़ुलाम रसूल!”
और मुझे ऐसा मा'लूम हुआ जैसे मेरे साथ क़िस्मत ने धोका किया हो। दीवार पर लटके हुए घंटे ने बारह बजाने शुरू' किए। एक... दो... तीन... चार... पाँच... सरदार-जी की निगाहें घंटे की तरफ़ फिर गईं जैसे मुस्कुरा रहे हों और मुझे अपने दादा याद आ गए जिनकी कई फुट लंबी दाढ़ी थी। सरदार-जी की शक्ल उनसे कितनी मिलती थी। छः... सात... आठ... नौ... जैसे वो हँस रहे हों, उनकी सफ़ेद दाढ़ी और सिर के खुले हुए बालों ने चेहरे के गिर्द एक नूरानी हाला-सा बनाया हुआ था... दस... ग्यारह... बारह... जैसे वो कह रहे हों, “जी असाँ दे हाँ तो चौबीस घंटे बारह बजे रहते हैं।” फिर वो निगाहें हमेशा के लिए बंद हो गईं।
और मेरे कानों में ग़ुलाम रसूल की आवाज़ दूर से, बहुत दूर से आई। मैं कहता न था कि बारह बजे इन सिखों की अ'क़्ल ग़ाइब हो जाती है और ये कोई न कोई हिमाक़त कर बैठते हैं। अब इन सरदार-जी ही को देखो... एक मुसलमान की ख़ातिर अपनी जान दे दी।
पर ये सरदार-जी नहीं मरे थे। मैं मरा था।
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.