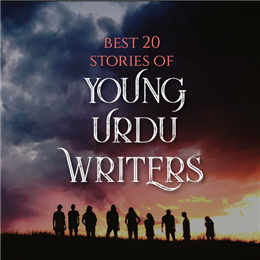नौहा-गर
एक बोसीदा मकान में हम चार “जानदार” इक्ट्ठे रहा करते थे। अब्बा, अम्माँ, मैं और एक सफ़ेद बकरी।
मैं चारपाई से बंधा हर रोज़...
बकरी को मिमियाते, माँ को बड़बड़ाते और अब्बा के माथे पर मौजूद लकीरों को सिकुड़ते-फैलते देखा करता।
मेरी माँ ज़ेर-ए-लब क्या बड़बड़ाया करती थी...? कभी सुन न पाया।
बकरी दर्द-भरी आवाज़ में चिल्ला-चिल्ला कर क्या बताना चाहती थी...? उस पर कभी ध्यान नहीं दिया।
अब्बा, होंटों से बीड़ी दबाए किन सोचों में गुम रहता और उसके माथे की तह-दार लकीरें क्यों सिकुड़ा-फैला करती थीं ...? मैं ये समझने से क़ासिर रहा।
मैं, अपने और बकरी के गले में बंधी रस्सी तो ब-ख़ूबी देख सकता था लेकिन अम्माँ और अब्बा की गर्दन से कसा हुआ चमड़े का पट्टा मुझे कभी नज़र न आया। वो दोनों भी शायद इससे बे-ख़बर थे। बिल्कुल वैसे ही कि जब दो आँखों वाली मछली अपना पेट भरने के लिए शिकार तो ढूँढ लेती है लेकिन नायलान के तार से बंधा कांटा उसे दिखाई नहीं देता।
साथ वाले मकान में ख़ाला सुग़रा रहा करती थीं। उनका एक बेटा भी था, जिसकी ‘उम्र लगभग-सात आठ बरस होगी, सब उसे काची कह कर बुलाया करते। ख़ाला मेरी अम्माँ को अक्सर बताया करती हैं कि काची पैदाइश के वक़्त सफ़ेद ऊन के गोले की तरह था लेकिन मुसलसल धूप में खेलते रहने की वज्ह से काची की रंगत अब सियाह हो गई है।
“अपने काली रंगत वाले बच्चे के लिए ऐसा सफ़ेद झूट, सिर्फ़ एक माँ ही बोल सकती है।”
काची का बाप हर दूसरे महीने उसके सर पर उस्तरा फिरवा दिया करता। चावल के दाने जितने बाल अब काची की शख़्सियत का मुस्तक़िल हिस्सा बन चुके थे। मैंने उसे हमेशा से अधनंगा ही देखा। कभी उसे लंबी क़मीज़ पहना दी जाती कि जिसका दामन घुटनों तक आया होता या फिर कभी सुर्ख़-रंग का जांगिया।
चावल के दाने बराबर बालों वाला... अधनंगा काची, जब कभी ख़ाला के हम-राह घर में दाख़िल होता तो मेरी जान पर बन आती। उसे देखते ही मुझ पर एक ख़ौफ़ की सी कैफ़ियत तारी होने लगती।
ख़ौफ़... और नफ़रत की मिली जुली कैफ़ियत
वो घर का दरवाज़ा पार करते ही मुझे ललचाई हुई नज़रों से देखने लगता। उसे जब मौक़ा’ मिलता तो वो मुझे दबोच लेने की कोशिश करता। मैं बचने के लिए जब चारपाई की दूसरी जानिब छलांग लगाता तो वो घूम कर मेरे सामने आ खड़ा होता। उसे सामने खड़ा पाकर मैं उल्टे पाँव दौड़ लगाता लेकिन मेरी दौड़ कभी ढाई मीटर से आगे न जा सकी। मेरी गर्दन में बंधी हुई रस्सी तन जाती और वो एका-एकी किसी पहलवान की तरह मुझ पर झपट पड़ता और मेरी गर्दन को अपनी बदबू-दार बग़ल में दाब लेता। मेरा साँस रुक जाता और तकलीफ़ की शिद्दत से मेरे हल्क़ से घुटी हुई चीख़ें बरामद होने लगतीं। इस हड़बोंग और चीख़-ओ-पुकार में साथ बैठी ख़ाला का ध्यान हमारी जानिब हो जाता और वो काची को मुझसे यूँ दस्त-ओ-गरेबाँ होते देखकर करख़्त आवाज़ में चिल्लाते कहतीं...
“अरे ओ कम-’अक़्ल काची, क्यों छिनाल के लौंडों की तरह इस बे-ज़बान से धींगा-मुश्ती में लगा है।
अगर तुझे उसकी हाय लगी... तो सच कहती हूँ, तू कहीं का नहीं रहेगा।
अरे ओ बद-बख़्त तू उसे छोड़ता है कि मैं चप्पल धरूँ तेरे सर पर।”
ख़ाला को यूँ ग़ुस्से में सांडनी की तरह बिफरता देखकर काची की गिरफ़्त मेरी गर्दन पर ढीली पड़ने लगती, और मैं अपने जिस्म को एक ज़ोरदार झटका देकर उसकी क़ैद से आज़ाद हो जाता। मैं लपक कर ख़ाला की ओट ले लेता और काची मुझे ललचाई हुई नज़रों से ऐसे देखता, मानो जैसे उसका मन-पसंद खिलौना उससे छीन लिया गया हो। मार पड़ने के ख़ौफ़ से वो मुझे दुबारा दबोचने का इरादा तर्क कर देता और आम के दरख़्त से बंधी बकरी की तरफ़ बढ़ जाता कि जहाँ वो सर झुकाए सुकून से चारा खा रही होती। वो कभी बकरी को सींग से पकड़ कर उसकी गर्दन को दाएँ-बाएँ घुमाता या फिर कान को इस ज़ोर से मरोड़ा करता कि बकरी दर्द से बिलबिला उठती। उसे बकरी से छेड़-छाड़ करते देख कर ख़ाला बग़ैर कुछ कहे ज़मीन पर पड़ी अपनी चप्पल उठाती और बैठे-बैठे ताक कर ऐसा निशाना साधा करतीं कि चप्पल ठीक काची की कमर से जा लगती। काची बकरी का कान छोड़कर अपनी कमर सहलाता हुआ घर से बाहर की जानिब भाग खड़ा होता। बकरी इस अचानक सर पर पड़ी उफ़्ताद से छुटकारा पाते ही दुबारा चारा खाने में जुत जाती, ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही न हो।
सफ़ेद बकरी लम्हे भर में सब कुछ कैसे भूल जाया करती मुझे नहीं मा’लूम। काची चले जाने के बा’द मेरे दिल से उसका ख़ौफ़ तो ज़ाइल हो जाता लेकिन नफ़रत फिर भी बाक़ी बच रह जाती।
ये एक-बार का क़िस्सा नहीं, हर दफ़ा’ ऐसा ही होता है। और मैंने हमेशा यूँही होते देखा...
काची के चले जाने के बा’द ख़ाला सुग़रा ग़ीबत में लिथड़े हुए मोहल्ले-भर के क़िस्से कहानियाँ नए सिरे से कहना शुरू’ करतीं और मेरी माँ बग़ैर कुछ बोले उन्हें चुप-चाप सुनती रहती। मैंने ख़ाला को अक्सर ये कहते सुना...
“अरी ओ नेक-बख़्त कुछ अपने मुँह से भी कह-सुन लिया कर, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ऐसे ख़ामोश बैठी रहेगी तो किसी दिन, ख़ुदा न करे तेरा दिल फट जाएगा... लेकिन हाय, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे तुझ करम-जली के मुँह में ज़बान है ही नहीं। मैंने लाख समझाया था तेरी माँ को कि अपनी इस चाँद सी बेटी को शो’बदा-बाज़ों के घर मत दे लेकिन तेरे घरवाले ने ऐसा नज़र-बंद किया कि उनकी ‘अक़्ल पर पर्दा पड़ गया। और वो शो’बदा-बाज़ तुझे ले उड़ा...”
ख़ाला सुग़रा अपने सीने पर हाथ मारते हुए जुमले मुकम्मल करतीं और सर पर ओढ़नी जमा कर बाहर निकल जातीं।
मैं सच कह रहा हूँ ये सब एक-बार का क़िस्सा नहीं, हर दफ़ा’ ऐसा ही होता। और मैंने हमेशा यूँही होते देखा।
कभी-कभी मुझे शक होता था कि अब्बा कि मुँह में भी ज़बान नहीं है। मैंने उसे भी कभी... हुँह... हाँ से ज़ियादा कहते कुछ नहीं सुना। लेकिन ख़ाला ने कभी उसे बे-ज़बान नहीं कहा।
बस यूँ समझ लीजिए कि!
इस बोसीदा मकान में हम चार... “बे-ज़बान” इकट्ठे रहा करते थे।
मैं, अब्बा, मेरी माँ और एक सफ़ेद बकरी।
अब्बा जब कभी मुझे नज़र भर के देखता, तो उस की आँख की पुतलियाँ आसूदगी के चराग़ बन कर जल उठतीं। वो हर-रोज़ शाम वापसी पर मेरी रगों में अपना हुनर उंडेलता। दिन-भर मुझे कई-कई घंटे मश्क़ कराते हुए न थकता। ज़िंदगी की आख़िरी जंग की तैयारी करते हुए बूढ़ा जिस्म हांप जाता। लेकिन उस नातवाँ जिस्म ने कभी हिम्मत नहीं हारी। ज़िंदगी की बिसात पर मैं उसका वाहिद पियादा था, जिसे आगे चल कर अपने बूढ़े और कमज़ोर बादशाह का दिफ़ा’ करना था।
जब कभी मुझसे कोई ग़लती सरज़द हो जाती। तो वो मेरे सर पर एक हल्की सी चपत रसीद कर दिया करता। लेकिन मेरी ग़लती की सज़ा बेचारी बकरी को भुगतना पड़ती। अब्बा का बे-रहमी से बरसता डंडा, और खूंटे से बंधी दर्द से मिमियाती हुई सफ़ेद बकरी को देखकर मैं सहम जाता।
अब्बा की ये ना-इंसाफ़ी मुझे कभी समझ न आई।
आख़िर मेरी ग़लती की सज़ा बकरी को क्यों?
न जाने वो ऐसा क्यों करता था...? मुझे नहीं मा’लूम।
बस उसके बा’द मेरी यही कोशिश होती कि मैं वो ग़लती दुबारा न दोहराऊँ कि जिसकी सज़ा मेरी प्यारी दोस्त को मिले।
अब्बा जब बकरी को मारते-मारते थक जाता तो डंडा ज़मीन पर फेंक देता और अपनी दोनों बाँहें फैला कर मुझे अपने क़रीब आने का इशारा करता। मैं दौड़ता हुआ अब्बा की गोद में चढ़ जाता और वो मुझे प्यार से चुमकारने लगता... मैं अब्बा से नज़रें बचा कर दर्द से हाँफती, मिमियाती बकरी को कन-अँखियों से देखता और दिल ही दिल में दुबारा ग़लती न करने का ‘अहद कर लेता। हर गुज़रता दिन मेरी ग़लतियों को सुधारता चला गया, अब्बा का हुनर मेरे सीने पर तमग़ा बन कर चमकने लगा और मेरी दुख की साथी, सुख की जुगाली करने लगी।
एक शाम अब्बा ने बकरी के गले से बंधी रस्सी खोली और उसे मेरे सामने पछाड़ दिया। बकरी घुटी हुई आवाज़ में चिल्लाई लेकिन अब्बा ने बड़ी ही बे-दर्दी से उसके गले पर छुरी फेर दी। कटे हुए नर्ख़रे से ख़ून का फ़व्वारा बुलंद हुआ और मेरा पूरा चेहरा ख़ून से रंग गया। मैं बद-हवासी के ‘आलम में इधर-उधर भागने लगा। अब्बा ने मेरी हवास-बाख़्तगी पर ज़रा भी ध्यान नहीं किया। मेरे सामने बैठ कर सालिम बकरी को गोश्त की छोटी-छोटी बोटियों में काट लेने के बा’द उसे आग पर चढ़ी देग में पकाने लगा... शाम ढलते ही आस पड़ोस के बुज़ुर्ग और ख़ानदान के कुछ अफ़राद घर में मदऊ’ किए गए... वो सब बहुत देर तक मेरी मोहसिन को अपने हरीस जबड़ों से चबाते और न निगली जाने वाली हड्डियों को हवा में उछाल देते। मैं हवा में क़ला-बाज़ी लगाता और उन हड्डियों को ज़मीन पर गिरने से पहले ही दबोच लेता, फिर तो जैसे लोगों ने इसे खेल ही बना लिया और देग में बची आख़िरी बोटी तक ये सिलसिला चलता रहा। रात हो जाने पर लोग भरे पेट अपने घरों को लौट गए। घर ख़ाली होते ही अब्बा ने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर वो सोने चला गया... मैंने जमा’ की हुई तमाम हड्डियों को इकट्ठा किया और उसे एक तर्तीब के साथ ख़ून-आलूद रस्सी और खूंटे के गिर्द जमा’ किया... सुपीदा-ए-सहरी तक मेरी समा’अत क़ुम-बि-इज़निल्लाह सुनने को तरसती रही।
मेरा अब्बा एक मदारी था।
गली-गली करतब दिखाने वाला एक मदारी।
दा’वत के अगले रोज़ से मैं अब्बा के साथ काम पर जाने लगा। घर से बाहर की दुनिया बड़ी तेज़-गाम थी। वो भरी दोपहर गली-गली सदा लगाता, करतब दिखाता। जब थक जाता तो किसी दरख़्त के साये में बैठ कर बीड़ी सुलगा लिया करता। बीड़ी अब्बा की ‘अय्याशी का वाहिद सामान थी। वो बीड़ी के एक सिरे से अधूरी ख़्वाहिशों को कशीद कर लिया करता और ताज़ा-दम हो कर रोटी की तलाश में उठ खड़ा होता।
“अब्बा! ख़ुदा के नज़दीक मेरी सफ़ेद बकरी से कम न था।”
वो ख़ानदान का दुख अपने बदन पर झेलता। हमारी ज़रूरतों के ‘इवज़ उसके जिस्म पर रोज़ाना डंडे बरसाए जाते। डंडे बरसाने वाला हाथ, और अब्बा के जिस्म पर पड़े नील मुझे कभी दिखाई न दिए... लेकिन अब्बा के हमवार माथे पर फैलती सिकुड़ती-लकीरों और बीड़ी के हर कश के बा’द उतरते-चढ़ते तअस्सुरात का भेद अब मैं जानने लगा था।
ख़ुदा जाने अब्बा तमाशा दिखाया करता था या वो ख़ुद एक तमाशा था कि जिसे आसमान की खिड़की से कोई और भी देखा करता होगा।
अब तमाशबीन अब्बा की आवाज़ और डुगडुगी की डुग-डुग सुनकर इकट्ठे हो जाते, तमाशाइयों का हुजूम अब्बा के अंदर एक नया जोश भर देता। अब्बा के नहीफ़ बदन से गरज-दार आवाज़ एक मो’जिज़ा बन कर निकलती। डुगडुगी की ताल पर सदा लगा कर वो तमाशे का आग़ाज़ करता। तमाश-बीनों की नज़र शुरू’ होने वाले तमाशे पर टिकी होतीं और अब्बा की आँखें तमाश-बीनों की रुपये पैसे से ठुँसी हुई जेबों पर। वो तरसी हुई निगाहों से जेबों की जानिब रेंगते हुए हाथों को बड़ी आस लग कर देखा करता, इस ख़याल से... कि न जाने कब कोई हाथ उसकी जानिब पैसा उछाल दे।
अब्बा और तमाश-बीनों की नज़रें क्या देखा करतीं, मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह न थी। लेकिन मेरी नज़र अब्बा के डुगडुगी बजाते हाथ और डंडे की मानूस सफ़्फ़ाकियत पर होती। और फिर मुझे अपनी प्यारी बकरी याद आ जाया करती। आज ना-इंसाफ़ी और दर्द झेलने के लिए मेरी बकरी तो मौजूद न थी लेकिन फिर भी मैं डंडे को देख कर दिल ही दिल में कोई ग़लती न करने का ‘अहद दोहरा कर अपनी दोस्त को याद कर लिया करता। मैं सारे दिन ज़मीन पर पड़े सिक्के जमा’ करता और उन्हें अब्बा के आगे रखे बर्तन में डाल देता। रुपया देखकर डुगडुगी की... डुग... डुग... और अब्बा की आवाज़ इस क़दर बुलंद हो जाती कि आसमाँ पर सोए हुए फ़रिश्ते तक जाग जाते...
लेकिन ख़ुदा की आँख फिर भी नम न होती।
“ख़ुदा को यूँ ख़ामोश और मसरूफ़ पा कर डुगडुगी के शोर से जाग जाने वाले फ़रिश्ते, फ़ुरात के उजले पानियों और सुर्ख़ रेत को याद करते हुए दुबारा सो जाते।”
नीम-ख़्वाबीदा हालत में एक फ़रिश्ता ज़मीन पर उतर कर मेरे पास आया और मेरे कान में से कहा,
“तुम्हारा बाप घर वालों के पेट का दोज़ख़ अपनी कमाई से बुझाया करता है, तुम पर एहसान नहीं करता। ये उसकी ज़िम्मेदारी है।”
फ़रिश्ते की बात सुनकर मैं अफ़्सुर्दा हो गया और सोचने लगा कि, “वाक़ई’ ज़िम्मेदारियाँ मुहब्बत के ज़ैल नहीं आतीं। शायद इसीलिए मेरे अब्बा के पैरों तले जन्नत नहीं है बस ख़ुदा ने उसके पैरों तले पहिए लगा दिए हैं जो हमेशा उसे घुमाए रखते हैं।”
घर में एक नन्हे फ़रिश्ते की आमद मुतवक़्क़े’ है। सच कहूँ तो घर में एक और नौहा-गर माँ की कोख में अपनी बारी के इंतिज़ार में था।
“वाह-रे मौला तो भी फ़रिश्ते के जिस्म में पेट टाँक कर उसे इंसान बना देता है और भूक... उसे हैवान।”
ज़िम्मेदारियाँ आकास बेल बन कर अब्बा के जिस्म से लिपटी हुई थीं। एक दिन, अब्बा सूरज से जंग हार गया, वो अपनी शिकस्त-ख़ुर्दा सूखी हुई जड़ों के सहारे ज़ियादा देर खड़ा न रह सका। और एक जानिब ढह गया। नए मदारी की आँख खुलने से पहले ही पुराने मदारी की आँख बंद हो गई। इस बार हवा में ख़ून का फ़व्वारा बुलंद नहीं हुआ। हाँ अलबत्ता अब्बा के हल्क़ से घुटी हुई आवाज़ ज़रूर निकली थी।
तमाशा वक़्त से पहले अपने अंजाम को पहुँचा लेकिन रुका नहीं।
अब डुगडुगी माँ के हाथ में थी और नया मदारी माँ के पेट में। मेरी प्यारी माँ अब गली-गली डुगडुगी बजा कर अब्बा का नौहा दोहराने लगी। तमाशा वही पुराना था और तमाशबीन भी, लेकिन पैसा... अब पहले से कहीं ज़ियादा बरसता था, मेरी ‘अक़्ल छोटी थी इसलिए देर से समझ आया कि अब तमाशबीन की आँखों में हैरत और दिलचस्पी के साथ “हवस” भी शामिल है।
फिर एक दिन अचानक डुगडुगी बजते-बजते दुबारा ख़ामोश हो गई, जब मैंने पलट कर देखा तो माँ अपना पेट पकड़े ज़मीन पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी। मैं उस दर्द को समझने से क़ासिर था। एक दफ़ा’ डुगडुगी बजना बंद हुई थी तो मेरा बाप मुझसे जुदा हो गया। और फिर जब आज दुबारा डुगडुगी खेल ख़त्म होने से पहले ख़ामोश हुई तो दिल में ख़याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी माँ भी मुझसे बिछड़ने वाली है...
मैं दौड़ता हुआ माँ के क़रीब पहुँचा, वो दर्द से कराह रही थी। मुझ बे-’अक़्ल को कुछ सुझाई नहीं दिया सिवाए इसके कि मैंने माँ के हाथों में डुगडुगी और डंडा थमाया और अपनी पहली वाली हालत में खड़ा हो गया। इस इंतिज़ार में कि डुगडुगी दुबारा बजे... और इस बार मैं वो शानदार कलाबाज़ी लगाऊँ के पैसा पहले से ज़ियादा मिले... दिल में सोचा। इस बार ऊँची छलांग लगा कर आसमान के उस पार से अब्बा को ज़मीन पर खींच लाऊँगा, वो इतना ग़ैर-ज़िम्मेदार नहीं कि हमें इस हाल में अकेला छोड़ दे। बस वो थक गया होगा और किसी दरख़्त के नीचे बीड़ी सुलगाए बैठा होगा...”
लेकिन डुगडुगी फिर भी न बजी। पलट कर देखा तो डंडा और डुगडुगी एक बार फिर ज़मीन पर थीं...
बे-हिसी चारों जानिब रक़्साँ थी। लोगों के लिए एक नया तमाशा शुरू’ हो चुका था। चीख़ती-चिंघाड़ती एम्बूलैंस मजमे’ को चीरती हुई आगे बढ़ी और उसने मेरी माँ को ज़िंदा निगल लिया। बस उस दिन के बा’द से में अपनी माँ का चेहरा दुबारा कभी न देख सका...
मेरे पास वो डुगडुगी आज भी मौजूद है, जब कभी मुझे अपने अम्माँ-अब्बा की याद आती है तो मैं अपने गले से बंधी हुई रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ कर बाज़ार की जानिब निकल आता हूँ। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे अब्बा मेरी रस्सी थाम कर बड़ी शान से चला करता था। मैं बाज़ार के वस्त में खड़ा हो कर ज़ोर-ज़ोर से डुगडुगी बजाता हूँ और अपने दोनों हाथ ऊपर किए दीवाना-वार नाचने लगता हूँ... पुराने तमाशबीन मुझे पहचान कर मेरी जानिब रोटी उछाल देते हैं मगर कुछ लोग अब भी ख़ुदाई-सिफ़त का भरम क़ाएम रखते हैं और मुझ पर निगाह किए बग़ैर ही गुज़र जाते हैं लेकिन मैं इन बातों की परवाह किए बग़ैर नाचता ही चला जाता हूँ।
अकेला देखकर चंद शरारती बच्चे मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैं नज़दीकी दरख़्त पर चढ़ कर उसकी शाख़ों को इस ज़ोर से हिलाता हूँ कि उसके सारे पत्ते झड़ने लग जाते हैं... जब मैं उनके हाथ नहीं आता तो वो सब मिलकर मुझे पत्थर मारने लगते हैं। मैं दरख़्त की नंगी शाख़ पर बैठा आसमान की जानिब सर उठा कर एक-बार फिर डुगडुगी बजा कर अपने अब्बा का नौहा दोहराने लगता हूँ...
डुग, डुग, डुग... डरप... डुग, डुग, डरप, डरप, डुग-डुग...
ना-मा’लूम सिम्त से अचानक काची नुमूदार हो कर मेरे और पत्थर मारने वाले बच्चों के दरमियान एक दीवार बन कर खड़ा हो जाता है। सियाह माइल रंगत वाला काची कि जिसके बाल चावल के दाने के बराबर थे वो दौड़ कर बच्चों की गर्दनें अपनी बदबू-दार बग़ल में सख़्ती से दाब लेता और उन्हें चिल्लाते हुए कहता है...
“कम-‘अक़्लों अगर इस बे-ज़बान की हाय लगी तो कहीं के नहीं रहोगे। अगर आइंदा ऐसा किया तो इससे भी ज़ियादा बुरा हश्र करूँगा।”
सुग़रा ख़ाला झूट कहा करती थीं कि बे-ज़बान की आह लग जाया करती है। वो कभी मुझे मिलें तो मैं उनकी ये ग़लत-फ़हमी ज़रूर दूर कर दूँगा... और उनसे कहूँगा कि,
“बे-ज़बान की आह... सातवें आसमान से ज़रा पहले ही दम तोड़ दिया करती है। अगर ऐसा होता... तो काची कब का मर चुका होता।”
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.