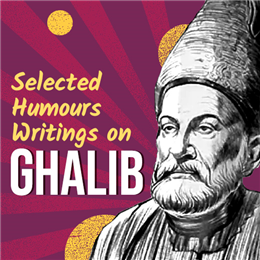असद-उल-अल्लाह खाँ तमाम हुआ
ग़ालिब की ज़िंदगी अपने आग़ाज़-ओ-अंजाम और दरमियानी वाक़िआत की तर्तीब-ओ-इर्तिक़ा के लिहाज़ से एक ड्रामाई कैफ़ियत रखती है। दुनियाए शे’र में तो मिर्ज़ा ग़ालिब ख़ल्लाक़-ए-मआनी और फ़नकार थे ही, लेकिन उनकी शख़्सी ज़िंदगी के मुरक़्क़ा को भी रंग और रोशनी और साये की आमेज़िश ने एक मुस्तक़िल फ़न्नी कारनामा बना दिया है। ग़ालिब की ज़िंदगी का पूरा ड्रामा, तख़य्युल की ज़रा सी कोशिश से, हम पर ख़ुद बख़ुद मुनकशिफ़ हो जाता है। ये ड्रामा सल्तनतों के हुबूत-ओ-ज़वाल,अज़ीमुश्शान अख़लाक़ी-ओ-दीनी कुव्वतों की पैकार, और मशरिक़-ओ-मग़रिब की फ़ैसलाकुन आवेज़िश के पस मंज़र पर नमूदार होता है। ग़ालिब के सवानिह हयात का क़ारी सिर्फ़ ये करता है कि निस्फ़ सदी के वाक़िआत के फैलाव को समेट कर अपने फ़न्नी शऊर के दायरे के अंदर ले आता है और फिर ये हैरत अंगेज़ ड्रामा ख़ुद बख़ुद हरकत करने लगता है।
मिर्ज़ा ग़ालिब ने इकहत्तर बरस की उम्र पाई। उनका ज़माना-ए-हयात मुसलमानान-ए-हिंद के सियासी ज़वाल का ज़माना था। जुनूब से मरहटों, मग़रिब से सिख्खों, मशरिक़ से अंग्रेज़ों ने मुग़लों की सियासी ताक़त पर पै दर पै हमले किए लेकिन मुसलमानों की तहज़ीब-ओ-तमद्दुन का एक नन्हा सा नुक़्ता फिर भी हिंदुस्तान के क़ल्ब में रोशन रहा। उस रोशन नुक़्ते का नाम था... दिल्ली।
उन्नीसवीं सदी की दिल्ली में अह्ल-ए-कमाल का एक ऐसा मजमा नज़र आता है जिससे अकबरी और शाहजहानी अह्द के इल्म-ओ-फ़ज़ल की याद ताज़ा हो जाती है। अह्ल-ए-कमाल की उस जमात पर नज़र डालिए तो बुज़ुर्गों में शाह अब्दुल अज़ीज़ और शाह इस्माईल, मौलाना फ़ज़ल हक़ ख़ैराबादी और मुफ़्ती सदर उद्दीन ख़ां आज़ुर्दा, नवाब मुस्तफ़ा ख़ां शेफ़्ता और मौलवी इमाम बख़्श सहबाई, शेख़ मुहम्मद इब्राहीम ज़ौक़ और हकीम मोमिन ख़ां मोमिन और नौजवानों में सय्यद अहमद ख़ां और हाली, ज़का-उल्लाह और नज़ीर अहमद के पाए के लोग दिखाई देते हैं।
उसी दिल्ली में 1830 के मौसम-ए-गर्मा का ज़िक्र है कि एक दिन सह पहर के वक़्त मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ां ग़ालिब के मकान के बाहर...
एक ख़ुशइलहान फ़क़ीर: कंकर चुन-चुन महल बनाया मूर्ख कहे घर मेरा है,
ना घर मेरा, ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा है
ना घर मेरा, ना घर तेरा...
(आवाज़ दूर होती जाती है)
(घर के अंदर बेगम ग़ालिब तख़्त पर बैठी हैं। सेहन में बैरी के दरख़्त से तोते का पिंजरा टंगा है)
बेगम ग़ालिब: दवा, ऐ दवा, ज़रा उठियो जल्दी से, लीजियो ये अधन्ना, दरवाज़े तक जाकर बिचारे को दे आइयो। (दवा जाती है)
(एक आह-ए-सर्द के साथ तास्सुफ़ आमेज़ लहजे में आहिस्ता) चिड़िया रैन-बसेरा चिड़िया के भाग फिर अच्छे कि अपने घोंसले में तो बैठी है। और मैं नवाब इलाही बख़्श ख़ां की बेटी... ग़रीब के सर पर भी अपना झोंपड़ा होता है, लेकिन मेरे लिए दिल्ली में किराए के मकानों के सिवा, अब कोई ठिकाना नहीं रहा। अब्बा जान ने आँखें क्या बंद कीं, मेरे नसीब सो गए। चार साल से चूल्हा उठाए घर-घर फिरती हूँ। अब बरसों के रखे हुए, ज़रबफ़्त और किम-ख़्वाब के जोड़े भी एक एक करके बिकने लगे। कलकत्ते का सफ़र मुझे तो बहुत महंगा पड़ा। क्या-क्या उम्मीदें लेकर मिर्ज़ा साहिब रवाना हुए थे और फिर किस हाल में वापस हुए, अब छः महीने बाद भी कोई एक नेक ख़बर कलकत्ते से नहीं आई (ज़रा बुलंद आवाज़ से) दवा, मदार ख़ां से कहियो मिर्ज़ा साहिब से पूछे कि ठंडा पानी दीवानख़ाने में पिएँगे या... क्या कहा? आरहे हैं, तो बस ठीक है।
(तोता बोलता है)
लो अब मियां मिट्ठू को थोड़ी सी चूरी दे दो।
(मिर्ज़ा ग़ालिब आते हैं)
ग़ालिब: चिड़िया रैन बसेरा। आपने भी ये वा’ज़ सुना? लेकिन ज़िंदगी कितनी ही बे सबात हो, उसका ये मर्तबा तो देखिए कि उस पर वा’ज़ कहने की ज़रूरत होती है (तोता फिर बोलता है) कहो मियां मिट्ठू अब क्या फ़र्याद है? आज चूरी नहीं मिली? अरे मियां ख़ुश रहो। न तुम्हारे बच्चे न जोरू, चूरी खाओ और मज़े करो, यही ज़िंदगी है।
बेगम: इन बातों से क्या फ़ायदा? देखना ये है कि हमारी अपनी ज़िंदगी कैसी है?
ग़ालिब: अच्छी... और बुरी... और अच्छी।
बेगम: अब ये पहेलियां भला कौन बूझे?
ग़ालिब: बात तो साफ़ कहता हूँ। सबसे पहले अच्छी इसलिए कह रहा हूँ कि शुरू में बरसों तक ज़िंदगी ख़ूब गुज़री। फिर बुरी इसलिए कहा कि चार पाँच बरस से हम लोग चक्कर में हैं और फिर दुबारा अच्छी इसलिए कि मुक़द्दमे का फ़ैसला होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
बेगम: मैं तो पाँच साल से इन्हीं उम्मीदों पर जी रही हूँ।
ग़ालिब: तो मायूस होने की कोई वजह भी हो? सरकार अंग्रेज़ी ने पच्चीस बरस पहले हम दोनों भाईयों के लिए दस हज़ार सालाना की जागीर मुक़र्रर की। शम्सुद्दीन ख़ां नवाब हैं तो फ़िरोज़पुर झिरका के हैं, मेरे सरकारी वज़ीफ़ा के नवाब नहीं हैं। न इस में तसर्रुफ़ करने के मजाज़ हैं। हमारे उस दस हज़ार को पंद्रह सौ कौन बना सकता है? सरकारी शक्क़े किसी की जालसाज़ी से बदल नहीं जाते। ये रक़म मिलकर रहेगी, बल्कि अगर इन्साफ़ हुआ तो अब तक जिस क़दर कम रक़म मिलती रही है, उस की वासलात इब्तिदा से आज तक दिलवाई जाएगी।
बेगम: (ज़हरखंद से) इन्साफ़, मैंने सिर्फ़ उसका नाम सुना है। इन्साफ़ करने वाले हाकिम बदलते हैं, माज़ूल होते हैं, मरते हैं, मगर इन्साफ़ नहीं होता।
ग़ालिब: इन्साफ़ होगा।
बेगम: नहीं होगा, ऐसे इन्साफ़ को मैं क्या करूँ जिसके इंतज़ार में एक भाई पागल हो गया और दूसरा...
ग़ालिब: और दूसरा?
बेगम: और दूसरा मिट गया। चक्की के दो पाटों तले पिस कर रह गया।
ग़ालिब: मेरा पिस जाना कुछ ऐसा आसान नहीं है। चक्की के पाट अलबत्ता घिस गए हैं। अभी और घिसेंगे।
(बाहर के दरवाज़े पर दस्तक, मदार ख़ां मुलाज़िम आता है)
मदार ख़ां: सरकार, मौलाना फ़ज़ल हक़ साहिब का आदमी ये रुक्क़ा छोड़ गया है।
ग़ालिब: मौलाना को आज ख़ुद यहां आना था... ख़ैर, लाओ। (रुक्क़ा खोलते हुए) , किरोड़ी मल महाजन को मेरे ख़िलाफ़ डिग्री मिल गई। हूँ, किरोड़ी मल भी क्या करे, कलकत्ते जाने से पहले उससे क़र्ज़ा लिया था। अब किरोड़ी मल और दीवानी अदालत का प्यादा मेरी तलाश में मंडला रहे हैं।
बेगम: अब क्या होगा?
ग़ालिब: होगा क्या, घर में बैठूँगा (तोता बोलता है) मियां मिट्ठू से बातें करूँगा। आपकी नमाज़ में हारिज हूँगा। दस्तूर के मुताबिक़ शुरफ़ा को दीवानी अदालत के डिग्रीदार घर के अंदर तो गिरफ़्तार कर नहीं सकते, और दिन के वक़्त मैं बाहर निकलने से रहा। (ज़रा हंसकर) दोनों वक़्त मिलते जब चराग़ में बत्ती पड़ती है, मैं भी चमगादड़ों के साथ थोड़ी देर के लिए निकला करूँगा, और बाहर का काम धंदा कर आया करूँगा। मदार ख़ां, देखो सरस की गली जाओ, जो छींट आज मैंने फ़र्ग़ुल के लिए ख़रीदी थी वो अज़ीज़ उन्निसा ख़ानम, मेरी भतीजी को दे आओ। (बेगम से ज़रा धीमे लहजे में) वो बच्ची नए कपड़े को तरस गई है... और देखो यूसुफ़ बेग ख़ां का हाल पूछना और कह आना कि मैं आज हकीम साहिब को नहीं लाऊँगा। हाँ, कल मग़रिब के बाद उन्हें साथ लिए आऊँगा। (मदार ख़ां जाता है) बेचारा यूसुफ़, हमारे लड़कपन में लोग कहा करते थे कि दोनों भाईयों में वही कमाऊ होगा। क्या बदन था, जैसे लोहे की लाठ और जब हैदराबाद से अपने रिसाले को छोड़कर आया तो देखकर दिल काँप जाता था... मज्ज़ूब, मख़्बूत, टूटी हुई कमान की तरह बेहाल, अगर उसका हाल ठीक होता तो मैं इस मुक़द्दमे के लिए शायद उसी को कलकत्ते भेजता।
बेगम: उफ़, कलकत्ते का नाम सुनकर मेरे सीने में एक तीर लगता है। इस कलकत्ते की उम्मीद ने हमें वीरान कर दिया, वर्ना लखनऊ के दरबार से कुछ न कुछ मिल गया होता।
ग़ालिब: (ज़रा तल्ख़ी से) तुम्हें लखनऊ के दरबार का हाल क्या मालूम? रोशन उद्दौला के हाथ दो-चार हज़ार के एवज़ अपनी आबरू बेच डालता? वो अगर नायब-उल-सल्तनत था तो मैं भी ख़ानदानी शरीफ़ ज़ादा था। वो मेरी ताज़ीम देने पर क्यों आमादा न हुआ? क्या उसके लिए ये काफ़ी न था कि मैंने उसकी मदह में एक नस्र तैयार की? उसके साथ ये शर्त क्यों लगाई गई कि गदागरों की तरह नज़र भी पेश करूँ? मैंने फ़ौरन कहा कि मैं ऐसी हुज़ूरी से माफ़ी चाहता हूँ।
बेगम: अच्छा, हमारा मुक़द्दर।
ग़ालिब: जो कुछ मुक़द्दर में लिखा है, वो तो हो कर रहेगा। हम अगर शिकवा करें भी तो क्या हासिल?
बेगम: हाँ, तुम्हारे लिए सब कुछ आसान है और नहीं तो शे’र लिख कर दिल की भड़ास निकाल ली।
ग़ालिब: आपके आँसूओं से भी तो दिल की भड़ास ख़ूब निकल जाती है।
बेगम: (दर्दनाक आवाज़ में) तो क्यों न रोऊँ बाप मर गया। भाई से तुम्हारी अनबन हो गई, मकान बिक गया। घर में जो ज़ेवर या कपड़ा था वो भी ये जागीर का मुक़द्दमा खा गया। अब तुम्हारे पीछे अदालत के प्यादे क़ैद करने को फिरते हैं। बच्चे थे (भराई हुई आवाज़ में) वो मरकर मुझे जिस सन्नाटे में छोड़ गए, मेरा ही दिल जानता है (सिसकियाँ लेकर रोते हुए) कैसे प्यारे बच्चे थे, जैसे चांद के टुकड़े, अभी तुतलाना ही शुरू किया था कि अल्लाह को प्यारे हो गए (रोते हुए) एक एक करके सब गए। पहला... और दूसरा, फिर तीसरा भी... चौथा भी।
(मुख़्तसर वक़फ़ा)
ग़ालिब: (आहिस्ता से) दवा, क्या ज़ैन उल आबदीन ख़ां आज इधर नहीं आया? मैंने सुबह उससे कहा तो था कि घड़ी दो घड़ी के लिए अपनी ख़ाला के पास होजाया करो... बड़ा नेक बख़्त लड़का है। किसी काम की वजह से रुक गया होगा, देखो, सुबह उनके हाँ जाना और कहना, मियां भूल क्यों गए? तुम्हारी ख़ाला तन्हाई में कुढ़ती रहती हैं। यहां आओगे, कुछ मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। कुछ तुम्हारी ख़ाला तुमसे बातें करेंगी, उनका जी बहल जाएगा... और बेगम अब जल्द ही हमारे दिन फिरेंगे। मेरे काग़ज़ात गवर्नर जनरल के सामने अनक़रीब पेश होंगे। अंग्रेज़ सेक्रेटरी मेरा दोस्त है...
बेगम: हाँ, मगर साल भर पहले वो भी तो तुम्हारा दोस्त था। दिल्ली का अंग्रेज़ एजेंट...
ग़ालिब: कोल बुर्क?
बेगम: जो माज़ूल हो गया। ख़ैर, फिर तुमने दिल को यूं तसल्ली दी कि उसकी जगह दूसरा अंग्रेज़ दोस्त आ गया।
ग़ालिब: हाँ हाँ फ्रेज़र।
बेगम: लेकिन फ्रेज़र छः हफ़्ते के अंदर बदल गया और उसकी जगह नया रेजिडेंट आया जो तुम्हारा नहीं, शम्सुद्दीन ख़ां का दोस्त है।
ग़ालिब: तो क्या हुआ, हर बार ऐसे ही इत्तिफ़ाक़ तो पेश नहीं आएँगे। न हाकिंज़ की रूदाद पर आख़िरी फ़ैसला हो जाएगा। कलकत्ते में लाट साहिब का सेक्रेटरी स्टर्लिंग साहिब मेरा मुख़लिस और बही ख़्वाह है। क्या ख़ूब आदमी है, पहली मुलाक़ात पर शरीफ़ों की तरह उठकर मुझे ताज़ीम दी। अपने हाथ से इतर और इलायची पेश की और बाद में भी हमेशा तकरीम से पेश आता रहा। मेरे काग़ज़ात उसी के हाथ से निकलेंगे। फिर अभी चंद साल वो अपनी जगह से टल भी नहीं सकता। इसलिए मुझे कोई ख़तरा नहीं है। स्टर्लिंग कलकत्ते में है तो सब ठीक है।
(बाहर के दरवाज़े पर दस्तक)
बेगम: या इलाही ख़ैर, अब ये कौन आया?
ग़ालिब: कोई नहीं, मदार ख़ां वापस आया होगा।
(मदार ख़ां आता है)
मदार ख़ां: सरकार सदरुस्सूदूर साहिब का आदमी मेरे साथ ही पहुंचा और ये पर्चा दे गया।
ग़ालिब: आज सब दोस्तों की तरफ़ से एक एक रुक्क़ा ज़रूर आएगा। लाओ देखें क्या कहते हैं, मुफ़्ती सदर उद्दीन ख़ां साहिब। (काग़ज़ खोलते हैं)
बेगम: ख़ुदाया कोई ख़ैर की ख़बर दीजो।
ग़ालिब: कलकत्ते से... ख़बर आई है... स्टर्लिंग साहिब 23 मई को मर गए... हाए जवाँ मर्ग।
(ये मिर्ज़ा ग़ालिब की ज़िंदगी का एक रुख़ था। लेकिन इस ज़ाती और ख़ानगी परेशानी के अलावा उनकी ज़िंदगी के कुछ और पहलू भी थे। उन पहलूओं का ताल्लुक़ उनके रोशन ज़मीर दोस्तों की सोहबत और उनकी बढ़ती हुई शायराना शोहरत से था। लार्ड विलियम बेंटिंक, गवर्नर जनरल ने मुक़द्दमे का फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ किया। कुछ पुरानी परेशानियों में कमी हुई, कुछ नई परेशानियों का इज़ाफ़ा हुआ, इसी तरह और बारह साल गुज़र गए। उस ज़माने में एक सुबह का ज़िक्र है कि मौलाना फ़ज़ल हक़ ख़ैराबादी मिर्ज़ा ग़ालिब के मकान पर पहुंचे।)
मौलाना: अरे भई मिर्ज़ा, अब उठो और ख़ुदा का नाम लो। मर्द-ए-ख़ुदा यह भुला सोने का वक़्त है। मैं दो घड़ी तुमसे बात करने आया था और तुम हो कि शराबियों की तरह सुबह के वक़्त ग़ाफ़िल पड़े हो।
ग़ालिब: ये जो आपने मुझे शराबी से तशबीह दी, उसे इस्तिलाह में तश्बीह-ए-ताम कहते हैं।
मौलाना: अब आप इल्म मआनी पर अपना दर्स रहने दीजिए और ज़रा उठकर हाथ मुँह धो लीजिए।
ग़ालिब: भई मौलाना, मुझे इतनी मोहलत तो दो कि तुम्हारी तशरीफ़ आवरी पर ज़रा ख़ुश हो लूं। मैं ख़्वाब देख रहा था कि क़िला-ए-मुअल्ला से चोबदार ने आकर ख़बर दी कि जहांपनाह ने याद फ़रमाया है, सो उसी ख़्वाब की ताबीर तुम्हारी मुलाक़ात है।
जहाने मुख़्तसर ख़्वाहम कि दर्दे
हमें जाये मन वजाए तू बाशद
कल्लू: आफ़ताबे में पानी लाओ। ज़रा मुँह भी धोलें और बातें भी करते जाएं और देखो मौलाना के लिए शर्बत भी लाओ। मौलाना, ये पेशगाह-ए-हुज़ूर में तलबी का ख़्वाब कुछ और मअनी भी रखता है। हकीम अहसन उल्लाह ख़ां कभी कभी मेरा ज़िक्र करते हैं। मियां इब्राहीम खाकानी-ए-हिंद हस्ब-ए-मामूल उस पर जुज़ बुज़ होते हैं। लेकिन बादशाह सलामत को इस तरफ़ तवज्जो ज़रूरी हो गई है। ख़ैर, ये क़िस्सा तो फिर सुनाऊँगा। आप कहिए कि सुबह सुबह कैसे आना हुआ?
मौलाना: भई, पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ, ये ग़ैर मुक़ल्लिदीन का फ़ित्ना किसी तरह फ़िरो होने में नहीं आता।
ग़ालिब: मैं तो आपके मुक़ल्लिदीन में से हूँ। यूं कि मुँह धोए बग़ैर दीन की बात नहीं करता। लीजिए ये शर्बत नोश फ़रमाईए और फिर इतमीनान से बैठ कर बात करते हैं।
मौलाना: मिर्ज़ा, इस प्याले में से दो एक घूँट पहले तुम पियो।
ग़ालिब: ये क्यों?
मौलाना: इसलिए कि तुम्हारी ज़बान का असर मेरी ज़बान में आजाए।
ग़ालिब: मौलाना, अगर एक रिंद गुनाहगार को यूं कांटों में घसीटोगे तो मैं उठकर तुम्हारे क़दमों को छुलूंगा। मेरे लिए यही सआदत कम नहीं कि मैं और तुम एक ही साल पैदा हुए और तुमने जवानी से लेकर इस उम्र तक जिस तरह मेरी रहनुमाई की है...
मौलाना: तो भई मिर्ज़ा, इस रहनुमाई के बदले, अब कुछ मेरी रहनुमाई करो। वही मसला इम्तिना-ए-नज़ीर ख़ातिम-उन-नबीयीन... इस पर अपना और वहाबी जमात का इख़्तिलाफ़ मुझे परेशान कर रहा है। तुम मेरा ये अक़ीदा जानते हो कि ख़ातिम-उन-नबीयीन का मिस्ल मुम्तना बिलज़ात है यानी जिस तरह ख़ुदा अपना मिस्ल पैदा नहीं कर सकता, उसी तरह ख़ातिम-उन-नबीयीन का मिस्ल भी पैदा नहीं कर सकता। उनको इसरार है कि ख़ातिम -उन-नबीयीन का मुम्तना बिलग़ैर है, मुम्तना बिलज़ात नहीं है यानी आँ हज़रत का मिस्ल इसलिए पैदा नहीं हो सकता कि उसका पैदा होना आपकी ख़ात्मियत के मुनाफ़ी है, न इसलिए कि ख़ुदा उसके पैदा करने पर क़ादिर नहीं है। मिर्ज़ा तुम ज़रा ग़ौर करो कि क्या ये बिलवास्ता ख़त्म-ए-नबुव्वत से इनकार नहीं है?
ग़ालिब: है, मगर मौलाना अगर ख़ुदा लगती सुनो तो मैं ये कहूं कि जो कुछ तुम कहते हो वो ज़ात बारी की क़ुदरत-ए-कामिला से इनकार है। शाह इस्माईल के पैरू इस पर चराग़-ए-पा न हूँ तो क्यों?
मौलाना: अरे मियां ये क्या कुफ़्र बकने लगे हो? कौन ख़ुदा की क़ुदरत-ए-कामिला का मुनकिर है। तुम्हारे नज़दीक तो अल्लाह ताला की क़ुदरत का इज़हार सिर्फ़ उसी सूरत में हो सकता है कि वो अपनी फ़ित्रत के क़वानीन को ख़ुद ही तोड़े, हालाँकि इस तरह उस की क़ुदरत महदूद होजाती है। मेरे रिसाला बहस “कातेग़ोरयास” में ये ज़िक्र मौजूद है। हाँ जिसकी तबीयत माक़ूल के बजाय ग़ैर माक़ूल की तरफ़ राग़िब हो, उसका रास्ता मुझसे जुदा है (ज़रा ठहर कर) तो मैं आज इसलिए तुम्हारे पास आया था कि तुमसे एक मबसूत और मुदल्लिल मसनवी लिखने को कहूं जिससे नज़ीर ख़ातिम -उन-नबीयीन का इम्तिना साबित हो। काश, मुझे भी बयान पर वही क़ुदरत हासिल होती, जो तुम्हें है तो मैं ये ख़िदमत ख़ुद अंजाम देता।
ग़ालिब: मौलाना ये मुआमला नाज़ुक है और शे’र-ओ-हुज्जत को जमा करना भी कुछ आसान नहीं, ताहम आपके इरशाद की तामील नागुज़ीर है। मैं इस बाब में ज़रूर फ़िक्र करूँगा। अब कहो तो मुस्तफ़ा ख़ां के हाँ चलें। वहां आज सदरुस्सूदूर साहिब से भी मुलाक़ात हो जाएगी। शायद मोमिन ख़ां भी हों।
मौलाना: तो आओ चलें, मेरी पालकी बाहर मौजूद है।
ग़ालिब: बस मैं ज़रा कान में दवा डाल लूं।
मौलाना: क्यों ख़ैरियत तो है?
ग़ालिब: कुछ दिनों से ऊंचा सुनने लगा हूँ। इससे घबराता हूँ। हकीम साहिब ने मुस्हिल पिलाकर तनक़िया किया। उसके बाद हफ़्ता भर अर्क़ अनार तुर्श और रोग़न गुल मुसावी मिलाकर चंद क़तरे नीम गर्म... कान में टपकाता रहा। कल से आब-ए-बर्ग शफ़तालू नीम गर्म टपका रहा हूँ। अभी तक कुछ इफ़ाक़ा नहीं हुआ।
मौलाना: ये तशवीश की बात है। तुम्हारी तमाम दुनिया तो बस यही चश्म-ओ-गोश की दुनिया है।
ग़ालिब: कई बरस हुए, मैंने एक ग़ज़ल कही थी जिसका एक शे’र यूं है;
लुत्फ़-ए-ख़िराम साक़ी-ओ-ज़ौक़-ए-सदाए चंग
ये जन्नत-ए-निगाह वो फ़िरदौस-ए-गोश है
अब इस फ़िरदौस-ए-गोश से निकलने का तसव्वुर मुझे उसी तरह मुज़्तरिब कर देता है जिस तरह आदम-ए-अव्वल को फ़िरदौस-ए-बरीं से निकलने का ख़्याल... लीजिए दवा तो कान में पड़ गई, आईए अब चलें।
(इस तरह ये दोनों हम उम्र, हम मज़ाक़, हम इल्म दोस्त बातें करते हुए नवाब मुस्तफ़ा ख़ां शेफ़्ता के मकान तक पहुंचे। नवाब साहिब के दीवानख़ाने में मजलिस-ए-अहबाब जमी हुई थी। गाना हो रहा था और एक ग़ज़ल अभी ख़त्म हुई थी। मिर्ज़ा ग़ालिब और मौलाना फ़ज़ल हक़ को साज़ों की मूसीक़ी के साथ सिर्फ़ आख़िरी लफ़्ज़ “ऐसी” की गूंज सुनाई देती है।)
शेफ़्ता: (दोनों दोस्तों को देखकर) आइए मिर्ज़ा साहिब, आइए मौलाना, तशरीफ़ लाइए। मेरी आँखें तो दरवाज़े पर लगी हुई थीं, और मौलाना सदर उद्दीन ख़ां आज़ुर्दा भी कई बार पूछ चुके हैं। मुफ़्ती साहिब ये लीजिए आख़िर आ ही पहुंचे मिर्ज़ा नौशा।
आज़ुर्दा: और मिर्ज़ा नौशा के मिर्ज़ा शह बाला भी तो साथ हैं। बहुत ख़ूब, ख़ुश-आमदीद।
शेफ़्ता: अफ़सोस सिर्फ़ इतना है कि आप मुफ़्ती साहिब की एक मुरस्सा ग़ज़ल से महरूम रहे। मुफ़्ती साहिब कमगो हैं और नग्ज़ गो। काश आप आजाते और सुनते।
ग़ालिब: तो आप मेरी मौजूदगी को अदम मौजूदगी से क्यों ताबीर फ़रमाते हैं, मुझे वक़्त की रवानी मुक़र्रर न फ़रमाईए कि अभी हूँ और अभी नहीं हूँ (हंसकर)ऐ हरचंद कहें कि है नहीं है
मौलाना: मुफ़्ती साहिब, ये बड़ा ज़ुल्म होगा अगर हम महरूम रह गए।
आज़ुर्दा: साहिब-ए-ग़ज़ल मुख़्तसर है और इसमें भी काम के शे’र बस दो हैं। आपको इसरार है तो मैं ख़ुद ही सुनाए देता हूँ।
मौलाना: इरशाद।
आज़ुर्दा: मुखड़ा वो बला, ज़ुल्फ़-ए-सियह फ़ाम वो काफ़िर
क्या ख़ाक जिए जिसकी शब ऐसी, सह्र ऐसी
“वाह, वाह, मर्हबा, किया शे’र है” का शोर। आज़ुर्दा दूसरा शे’र पढ़ने से पहले ये मिसरा दोहराते हैं। ऐ क्या ख़ाक जिए जिसकी शब ऐसी सह्र ऐसी, और फिर ये शे’र पढ़ते हैं;
या तंग न कर नासिह नादाँ मुझे इतना
या चल के दिखादे दहन ऐसा कमर ऐसी
(फिर दाद का शोर)
मौलाना: क्या अछूता अंदाज़ है और फिर ये ज़मीन, मुफ़्ती साहिब ये ज़मीन कहां से पाई?
ग़ालिब: कहां से पाई? अरे भाई आसमान से और कहां से।
शेफ़्ता: साहिबो, पान और शर्बत हाज़िर है।
ग़ालिब: मैं तो शर्बत पियूँगा... इस शर्बत का रंग मुझे पुकार पुकार कर बुला रहा है... मौलाना, आप क्यों ललचाई हुई नज़रों से मेरे सदक़े क़ुर्बान हुए जाते हैं। आपको इस शर्बत का एक घूँट नहीं मिलेगा।
(दोस्तों का क़हक़हा)
आज़ुर्दा: हाँ साहिब, मैं ज़िक्र करने वाला था कि अंग्रेज़ी गर्वनमेंट को दिल्ली कॉलेज का इंतज़ाम अज़सर-ए-नौ मंज़ूर है।
मौलाना: मुफ़्ती साहिब, ये दिल्ली कॉलेज का नया इंतज़ाम कहीं वैसा ही न हो जैसा सात आठ बरस पहले ताजमहल के लिए तजवीज़ किया गया था।
शेफ़्ता: क्या कहने हैं। ताजमहल के, आगरा उस वीरानी पर भी एक मुरस्सा ग़ज़ल है मगर बैत-उल-ग़ज़ल ताजमहल है।
मौलाना: ये तो नवाब मुस्तफ़ा ख़ां शेफ़्ता कहते हैं ना। अंग्रेज़ों की क़द्र दानी मुलाहिज़ा फ़रमाईए कि लार्ड विलियम बेंटिंक ने ताजमहल का तमाम संगमरमर उखड़वाकर फ़रोख़्त कर देने की तजवीज़ की और बचाओ इस तरह हुआ कि पहले उखड़वाई का अंदाज़ा किया गया तो मालूम हुआ कि ख़र्च ज़्यादा होगा और आमदनी कम।
ग़ालिब: मौलाना, ऐब मय जुमला बगफ़ती हुनरिश नीज़ बगो, लेकिन आप तो अंग्रेज़ों की नफ़रत से उबले पड़ते हैं, आप क्या इन्साफ़ करेंगे।
मौलाना: न मानो, मगर मेरी ये बात याद रखो कि अंग्रेज़ों को ख़ुदा इख़्तियार दे तो ताजमहल और लाल क़िला में गधे बंधवा दें। जामा मस्जिद को अपना अस्तबल बना लें।
आज़ुर्दा: तो मौलाना आप ख़ुदा से सिफ़ारिश कीजिए कि अंग्रेज़ों को इख़्तियार न दे। मुझे तो अंग्रेज़ों के इख़्तियार में फ़िलहाल कोई कमी होती नज़र आती नहीं... बहरहाल, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि टामसन साहिब आगरा से दिल्ली आए हैं। दिल्ली कॉलेज के लिए सौ रुपये महीने पर फ़ारसी के उस्ताद का तक़र्रुर हो रहा है। मैंने मिर्ज़ा नौशा से पूछे बग़ैर उनके लिए तहरीक करा दी है। मुशाहिरा निहायत माक़ूल है और ये जगह मिर्ज़ा साहिब के लिए मुनासिब भी मालूम होती है।
ग़ालिब: (हंसकर) शुक्र है मेरी शायरी नहीं तो मेरी ज़बान दानी आपके नज़दीक मुस्लिम हो गई... ये मन्सब वाक़ई मेरे लिए निहायत मुनासिब है और निहायत नामुनासिब भी।
शेफ़्ता: मिर्ज़ा साहिब, लिल्लाह, इस बाब में यूं शायरी न फ़रमाईए, ये तक़र्रुर अगर हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो।
ग़ालिब: लेकिन साहिब मैं क्या करूँ, कल मेरी शायरी इस तक़र्रुर का क़िस्सा पाक कर भी आई।
शेफ़्ता-ओ-आज़ुर्दा: (चौंक कर) यानी?
ग़ालिब: यानी ये कि परसों टामसन साहिब ने मुझे याद फ़रमाया, कल मैं पहुंचा। साहिब को इत्तिला कराई, ख़ुद पालकी से उतर कर ठहरा रहा कि साहिब हस्ब-ए-दसतूर इस्तिक़बाल को निकलेंगे, थोड़ी देर में साहिब का जमादार हमा-तन सवाल बन कर निकला कि आप अंदर क्यों नहीं आते। मैंने कहा, साहिब इस्तिक़बाल को तशरीफ़ नहीं लाए, में क्यूँ-कर अंदर जाऊं? जमादार फिर अंदर गया तो साहिब ख़ुद बाहर निकल आए और बोले जब आप दरबार गवर्नरी में बहैसियत रईस के तशरीफ़ लाएँगे तो आपकी वो ताज़ीम होगी, लेकिन इस वक़्त आप नौकरी के लिए आए हैं। इस वक़्त वो सूरत नहीं है।
आज़ुर्दा: है है मिर्ज़ा, तुमने ग़ज़ब कर दिया।
ग़ालिब: हाँ मैंने उनको साफ़ जवाब दिया कि साहिब मैं सरकारी नौकरी को ज़रिया अफ़्ज़ाइश-ए-इज़्ज़त जानता हूँ। ये नहीं कि बुज़ुर्गों की बख़्शी हुई इज़्ज़त भी खो बैठूँ, बस यहीं बात तमाम हो गई। टामसन साहिब ने अपने दरवाज़े का रुख़ किया और मैंने ग़ालिब अली शाह के तकिए का।
शेफ़्ता: सुब्हान-अल्लाह मिर्ज़ा साहिब, दुनिया कुछ भी कहे, इसमें शक नहीं कि ख़ुद्दारी और आज़ादा रवी को आपने इंतिहा पर पहुंचा दिया।
ग़ालिब: कल शाम एक ग़ज़ल हो गई थी, जिसमें इत्तिफ़ाक़ से यही मज़मून आगया। लीजिए ये पर्चा मुलाहिज़ा फ़रमाईए।
आज़ुर्दा: क्यों साहिब, ये पर्चा वही क्यों मुलाहिज़ा फ़रमाएं। पढ़ कर सुनाइए... महफ़िल को महरूम न कीजिए।
शेफ़्ता: हाँ साहिब, तो फिर इरशाद हो।
ग़ालिब: (दाद-ओ-तहसीन के शोर में ये ग़ज़ल ख़त्म करते हैं)
दर खोर-ए-क़हर-ओ-ग़ज़ब जब कोई हम सा न हुआ
फिर ग़लत क्या है कि हम सा कोई पैदा न हुआ
बंदगी में भी वो आज़ादा-ओ-ख़ुदबीं हैं कि हम
उल्टे फिर आए दर-ए-काबा अगर वा न हुआ
सीने का दाग़ है वो नाला कि लब तक न गया
ख़ाक का रिज़्क़ है वो क़तरा कि दरिया न हुआ
नाम का मेरे है वो दुख कि किसी को न मिला
काम का मेरे है वो फ़ित्ना कि बरपा न हुआ
थी ख़बर गर्म कि ‘ग़ालिब’ के उड़ेंगे पुर्जे़
देखने हम भी गए थे, प तमाशा न हुआ
(इस तरह मिर्ज़ा ग़ालिब की ज़िंदगी के पंद्रह साल और गुज़र गए। इस अर्से में मिर्ज़ा साहिब माने हुए बुज़्रगान-ए-अदब में शुमार होने लगे। एक ख़ानदानी सदमा इस अर्से में उन्हें पहुंचा। ज़ैन उल आबदीन ख़ां आरिफ़ जवान हुए, शायर बने, और मर गए। उनका छोटा बच्चा हुसैन अली ख़ां अब मिर्ज़ा साहिब के घर में रहता था, और मिर्ज़ा साहिब उसे अपने बेटे की मानिंद अज़ीज़ रखते थे। शे’र-ओ-सुख़न, नग़मा-ओ-सुरूर, मुहब्बत-ओ-दोस्ती की ये फ़िज़ा आख़िरकार 1857 में एक दम ब्रहम हुई। पहले मई में अंग्रेज़ क़त्ल हुए लेकिन फिर सितंबर में अंग्रेज़ं की फ़तहमंद फ़ौज दिल्ली में दाख़िल हुई और दिल्ली के मुसलमानों ने वो मुसीबतें देखीं, जिनसे चंगेज़ और हलाकू की याद ताज़ा हो गई। सितंबर 57 ई. में मिर्ज़ा ग़ालिब अपने मकान में बैठे हैं, हुसैन अली ख़ां भी मौजूद हैं।
ग़ालिब: बेटा, बेटा हुसैन अली ख़ां, हकीम साहिब नहीं आए? बहरापन तो जान का रोग बन गया।
हुसैन अली ख़ां: (आवाज़ बुलंद करके) दादा हज़रत, शहर में बलवा हो रहा है।
ग़ालिब: बलवा...? अभी तक।
हुसैन अली ख़ां: (चीख़ कर) आप सुन नहीं रहे हैं। हमारी गली में से लोग भागते हुए जा रहे हैं।
ग़ालिब: हाँ कुछ शोर सा सुनाई तो देता है... हाय दिल्ली, क्या तू इस तरह सिसक सिसक कर मरेगी? मुझे भी अपने साथ ही ले जा (फिर ज़रा धीमी आवाज़ में) अवध की सल्तनत मुझ पर मेहरबान हुई। मेरी क़ज़ा ने उसे दो बरस में ख़त्म कर दिया। दिल्ली की सल्तनत कुछ ज़्यादा सख़्त-जान थी। सात बरस मुझको रोटी देकर बिगड़ी...
हुसैन अली ख़ां: (फिर चिल्ला कर) सुनिए, बादशाह सलामत को गोरों ने पकड़ लिया।
ग़ालिब: (उसी लहजे में) अच्छा, ये शम्मा भी बुझ गई?
हुसैन अली ख़ां: (चीख़ कर) और सुनिए, मीर मयकश और मौलाना सहबाई क़त्ल हो गए।
ग़ालिब: (सर्द आह भर कर) अल्लाह...! अल्लाह।
(हुजूम का शोर... गोली चलने की आवाज़)
हुसैन अली ख़ां: कल्लू कहता है, मौलाना फ़ज़ल हक़ को गोरे पकड़ ले गए।
ग़ालिब: (बेताबाना) हाय।
हुसैन अली ख़ां: और नवाब मुस्तफ़ा ख़ां और मुफ़्ती साहिब को भी।
ग़ालिब: अच्छा है, अच्छा है मैं भी अब कफ़न पहन कर ज़िंदगी के दिन गुज़ारूँगा। जाओ कल्लू से कहो, मेरे कपड़े लाए। मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता हूँ। वो हवालात में मेरे मुंतज़िर हैं।
(हुजूम की चीख़ पुकार)
हुसैन अली ख़ां: (काँपती हुई आवाज़ में) सरस की गली से आदमी आया है... दादा यूसुफ़ बेग ख़ां को गोरों ने मार डाला।
ग़ालिब: मर गया, यूसुफ़ मर गया, उफ़... औफ़, मेरा भाई... (क़हक़हा लगाकर) दीवाने को गोली मार दी, उफ़... (काँपती हुई आवाज़ में) बेटा, लोग यूसुफ़ को मजनून कहते थे।आज मैं मजनूनों से बदतर हूँ।
हुसैन अली ख़ां: दादा हज़रत ख़ुदा के...
(हुसैन अली ख़ां की आवाज़ गोलीयों की बाढ़ में गुम होजाती है)
हुसैन अली ख़ां: दादा हज़रत, हकीम साहिब तशरीफ़ ला रहे हैं।
ग़ालिब: अब क्या फ़ायदा?
मेरे सुनने को अब रह ही क्या गया है।
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.