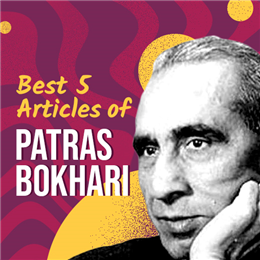सिनेमा का इश्क़
सिनेमा का इश्क़“ उन्वान तो अ’जब हवस ख़ेज़ है। लेकिन अफ़सोस कि इस मज़मून से आप की तमाम तवक़्क़ोआत मजरूह होंगी क्यूँकि मुझे तो इस मज़मून में कुछ दिल के दाग़ दिखाने मक़सूद हैं।
इससे आप ये न समझिए कि मुझे फिल्मों से दिलचस्पी नहीं या सिनेमा की मौसीक़ी और तारीकी में जो रुमान-अंगेज़ी है, मैं उसका क़ायल नहीं। मैं तो सिनेमा के मामले में अवायल उ’म्र ही से बुज़ुर्गों का मौरिद-ए-इ’ताब रह चुका हूँ, लेकिन आज-कल हमारे दोस्त मिर्ज़ा साहब की मेहरबानियों के तुफ़ैल सिनेमा गोया मेरी दुखती रग बन कर रह गया है। जहां उसका नाम सुन पाता हूँ, बा’ज़ दर्द-अंगेज़ वाक़यात की याद ताज़ा हो जाती है जिससे रफ़्ता-रफ़्ता मेरी फ़ितरत ही कज-बीं बन गयी है।
अव्वल तो ख़ुदा के फ़ज़्ल से हम कभी सिनेमा वक़्त पर नहीं पहुंच सके। इसमें मेरी सुस्ती को ज़रा दख़्ल नहीं ये सब क़सूर हमारे दोस्त मिर्ज़ा साहब का है जो कहने को तो हमारे दोस्त हैं लेकिन ख़ुदा शाहिद है कि उनकी दोस्ती से जो नुक़्सान हमें पहुंचे हैं किसी दुश्मन के क़बज़ा-ए-क़ुदरत से भी बाहर होंगे।
जब सिनेमा जाने का इरादा हो, हफ़्ता भर पहले से उन्हें कह रखता हूँ कि क्यूँ भई मिर्ज़ा अगली जुमेरात सिनेमा चलोगे ना! मेरी मुराद ये होती है कि वो पहले से तैयार रहें और अपनी तमाम मस्रूफ़ियतें कुछ इस ढब से तर्तीब दे लें कि जुमेरात के दिन उनके काम में कोई हर्ज वाक़े न हो लेकिन वो जवाब में अ’जब क़द्र ना-शनासी से फ़रमाते हैं,
“अरे भई चलेंगे क्यों नहीं क्या हम इंसान नहीं ? हमें तफ़रीह की ज़रूरत नहीं होती? और फिर कभी हमने तुमसे आज तक ऐसी बे-मुरव्वती भी बरती है कि तुमने चलने को कहा हो और हमने तुम्हारा साथ न दिया हो?”
उनकी तक़रीर सुनकर मैं खिसयाना सा हो जाता हूँ। कुछ देर चुप रहता हूँ और फिर दबी ज़बान से कहता हूँ,
“भई अब के हो सका तो वक़्त पर पहुंचेंगे। ठीक है ना!”
मेरी ये बात आ’म तौर पर टाल दी जाती है क्योंकि इससे उनका ज़मीर कुछ थोड़ा सा बेदार हो जाता है, ख़ैर मैं भी बहुत ज़ोर नहीं देता। सिर्फ़ उनको बात समझाने के लिए इतना कह देता हूँ,
“क्यों भई सिनेमा आज-कल छः बजे शुरू होता है ना ?”
मिर्ज़ा साहिब अ’जब मासूमियत के अंदाज़ में जवाब देते हैं,
“भई हमें ये मालूम नहीं।”
“मेरा ख़्याल है छः ही बजे शुरू होता है।”
“अब तुम्हारे ख़्याल की तो कोई सनद नहीं।”
“नहीं मुझे यक़ीन है। छः बजे शुरू होता है।”
“तुम्हें यक़ीन है तो मेरा दिमाग़ क्यों मुफ़्त में चाट रहे हो ?”
इसके बाद आप ही कहिए मैं क्या बोलूँ?
ख़ैर जनाब जुमेरात के दिन चार बजे ही उनके मकान को रवाना हो जाता हूँ। इस ख़्याल से कि जल्दी-जल्दी उन्हें तैयार करा के वक़्त पर पहुंच जाएँ। दौलत-ख़ाने पर पहुँचता हूँ तो आदम न आदम-जा़द। मर्दाने के सब कमरों में घूम जाता हूँ। हर खिड़की में से झाँकता हूँ, हर शिगाफ़ में से आवाज़ें देता हूँ लेकिन कहीं से रसीद नहीं मिलती। आखिर तंग आकर उन के कमरे में बैठ जाता हूँ। वहां दस-पंद्रह मिनट सीटियां बजाता रहता हूँ। दस-पंद्रह मिनट पैंसिल से ब्लॉटिंग पेपर पर तस्वीरें बनाता रहता हूँ। फिर सिगरेट सुलगा लेता हूँ और बाहर डेवढ़ी में निकल कर इधर-उधर झांकता हूँ। वहां बदस्तूर हू का आलम देखकर कमरे में वापस आ जाता हूँ और अख़बार पढ़ना शुरू कर देता हूँ। हर कॉलम के बाद मिर्ज़ा साहब को एक आवाज़ दे लेता हूँ। इस उम्मीद पर कि शायद साथ के कमरे में या ऐन ऊपर के कमरे में तशरीफ़ ले आये हों। सो रहे थे तो मुमकिन है जाग उठे हों या नहा रहे थे तो शायद ग़ुस्ल-ख़ाने से बाहर निकल आये होँ लेकिन मेरी आवाज़ मकान की वुसअतों में से गूंज कर वापस आ जाती है। आख़िर-कार साढे़ पाँच बजे के क़रीब ज़नाने से तशरीफ़ लाते हैं। मैं अपने खौलते हुए ख़ून को क़ाबू में ला कर मतानत और अख़्लाक़ को बड़ी मुश्किल से मद्द-ए-नज़र रख कर पूछता हूँ,
“क्यों हज़रत! आप अंदर ही थे?”
“हाँ मैं अंदर ही था।”
“मेरी आवाज़ आपने नहीं सुनी?”
“अच्छा, ये तुम थे? मैं समझा कोई और है?”
आँखें बंद करके सर को पीछे डाल लेता हूँ और दाँत पीस कर ग़ुस्से को पी जाता हूँ और फिर काँपते हुए होंटों से पूछता हूँ,
“तो अच्छा अब चलेंगे या नहीं ?”
“वो कहाँ ?”
“अरे बंदा-ए-ख़ुदा आज सिनेमा नहीं जाना?”
“हाँ सिनेमा। सिनेमा (ये कह कर वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं) ठीक है। सिनेमा, मैं भी सोच रहा था कि कोई न कोई बात ज़रूर ऐसी है जो मुझे याद नहीं आ रही है। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया वर्ना मुझे रात भर उलझन रहती।”
“तो चलो फिर अब चलें।”
“हाँ वो तो चलेंगे ही। मैं सोच रहा था आज ज़रा कपड़े बदल लेते। ख़ुदा जाने धोबी कमबख़्त कपड़े भी लाया है या नहीं। यार इन धोबियों का तो कोई इंतज़ाम करो।”
अगर क़त्ल-ए-इंसानी एक संगीन जुर्म न होता तो ऐसे मौक़े पर मुझसे ज़रूर सरज़द हो जाता लेकिन क्या करूं अपनी जवानी पर रहम खाता हूँ। बेबस होता हूँ सिर्फ़ यही कह सकता हूँ कि,
“मिर्ज़ा! भई लिल्लाह मुझपर रहम करो। मैं सिनेमा चलने को आया हूँ, धोबियों का इंतज़ाम करने नहीं आया। यार बड़े बदतमीज़ हो पौने छः बज चुके हैं और तुम जूं के तूं बैठे हो।”
मिर्ज़ा साहब अ’जब मुरब्बियाना तबस्सुम के साथ कुर्सी पर से उठते हैं गोया ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि अच्छा भई तुम्हारी तिफ़लाना ख़्वाहिशात आख़िर हम पूरी कर ही दें। चुनांचे फिर ये कह कर अन्दर तशरीफ़ ले जाते हैं कि अच्छा कपड़े पहन आऊं।
मिर्ज़ा साहब के कपड़े पहनने का अ’मल इस क़दर तवील है कि अगर मेरा इख़्तियार होता तो क़ानून की रौ से उन्हें कभी कपड़े उतारने ही न देता। आध घंटे के बाद वो कपड़े पहने हुए तशरीफ़ लाते हैं। एक पान मुँह में दूसरा हाथ में, मैं भी उठ खड़ा होता हूँ। दरवाज़े तक पहुंच कर मुड़ के जो देखता हूँ तो मिर्ज़ा साहब ग़ायब। फिर अन्दर आ जाता हूँ मिर्ज़ा साहब किसी कोने में खड़े कुछ कुरेद रहे होते हैं।
“अरे भई चलो।”
“चल तो रहा हूँ यार। आख़िर इतनी भी क्या आफ़त है?”
“और ये तुम क्या कर रहे हो?”
“पान के लिए ज़रा तंबाकू ले रहा था।”
तमाम रास्ते मिर्ज़ा साहब चहल-क़दमी फ़रमाते जाते हैं। मैं हर दो तीन लम्हे के बाद अपने आपको उन से चार पांच क़दम आगे पाता हूँ। कुछ देर ठहर जाता हूँ। वो साथ आ मिलते हैं तो फिर चलना शुरू कर देता हूँ। फिर आगे निकल जाता हूँ। फिर ठहर जाता हूँ। ग़रज़ कि गो चलता दुगनी तिगुनी रफ़्तार से हूँ लेकिन पहुँचता उनके साथ ही हूँ।
टिकट लेकर अंदर दाख़िल होते हैं तो अंधेरा घुप। बहुतेरा आँखें झपकता हूँ, कुछ सुझाई नहीं देता। उधर से कोई आवाज़ देता है। “ये दरवाज़ा बंद कर दो जी!” या अलल्लाह अब जाऊं कहाँ? रस्ता, कुर्सी, दीवार, आदमी कुछ भी तो नज़र नहीं आता। एक क़दम बढ़ाता हूँ तो सर उन बाल्टियों से जा टकराता है जो आग बुझाने के लिए दीवार पर लटकी रहती हैं। थोड़ी देर के बाद तारीकी में कुछ धुँदले से नक़्श दिखाई देने लगते हैं। जहां ज़रा तारीक तर सा धब्बा दिखाई दे जाये। वहां समझता हूँ ख़ाली कुर्सी होगी। ख़मीदा पुश्त हो कर उसका रुख़ करता हूँ इसके पावँ को फाँद, उसके टखनों को ठुकरा, ख़वातीन के घुट्नों से दामन बचा कर आख़िरकार किसी की गोद में जा कर बैठता हूँ। वहां से निकाल दिया जाता हूँ और लोगों के धक्कों की मदद से किसी ख़ाली कुर्सी तक जा पहुँचता हूँ। मिर्ज़ा साहब से कहता हूँ, “मैं न बकता था कि जल्दी चलो। ख़्वाह-मख़्वाह में हमको रुसवा करवाया न! गधा कहीं का!” इस शगुफ़्ता बयानी के बाद मा’लूम होता है कि साथ की कुर्सी पर जो हज़रत बैठे हैं और जिनको मुख़ातिब कर रहा हूँ वो मिर्ज़ा नहीं कोई और बुज़ुर्ग हैं।
अब तमाशे की तरफ़ मुतवज्जे होंता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि फ़िल्म कौन सी है? उसकी कहानी क्या है? और कहाँ तक पहुंच चुकी है? और समझ में सिर्फ़ इस क़दर आता है कि एक मर्द और एक औरत जो पर्दे पर बग़ल-गीर नज़र आते हैं, एक दूसरे को चाहते होंगे। इस इंतज़ार में रहता हूँ कि कुछ लिखा हुआ सामने आये, तो मुआ’मला खुले कि इतने में सामने की कुर्सी पर बैठे हुए हज़रत एक वसी-व-फ़र्राख़ अंगड़ाई लेते हैं जिसके दौरान में कम अज़ कम दो तीन सौ फ़ीट फ़िल्म गुज़र जाती है। जब अंगड़ाई को लपेट लेते हैं तो फिर सर खुजाना शुरू कर देते हैं और इस अ’मल के बाद हाथ को सर से नहीं हटाते बल्कि बाज़ू को वैसे ही ख़मीदा रखे रहते हैं। मैं मजबूरन सर को नीचा करके चाय-दानी के उस दस्ते के बीच में से अपनी नज़र के लिए रास्ता निकाल लेता हूँ और अपने बैठने के अंदाज़ से बिल्कुल ऐसा मालूम होता हूँ जैसे टिकट ख़रीदे बगै़र अंदर घुस आया हूँ और चोरों की तरह बैठा हुआ हूँ। थोड़ी देर के बाद उन्हें कुर्सी की नशिस्त पर कोई मच्छर या पिस्सू महसूस होता है। चुनांचे वो दाएं से ज़रा ऊंचे हो कर बाएं तरफ़ को झुक जाते हैं। मैं मुसीबत का मारा दूसरी तरफ़ झुक जाता हूँ। एक दो लम्हे के बाद वही मच्छर दूसरी तरफ़ हिजरत कर जाता है। चुनांचे हम दोनों फिर से पैंतरा बदल लेते हैं। ग़रज़ कि ये दिललगी यूं ही जारी रहती है। वो दाएं तो मैं बाएं और वो बाएं तो मैं दाएं। उनको क्या मा’लूम कि अंधेरे में क्या खेल खेला जा रहा है। दिल यही चाहता है कि अगले दर्जे का टिकट लेकर उन के आगे जा बैठूँ और कहूँ कि ले बेटा! देखूँ तो अब तू कैसे फ़िल्म देखता है।
पीछे से मिर्ज़ा साहब की आवाज़ आती है, “यार तुम से निचला नहीं बैठा जाता। अब जो हमें साथ लाए हो तो फ़िल्म तो देखने दो।”
इसके बाद ग़ुस्से में आकर आँखें बंद कर लेता हूँ और क़तल-ए-अम्द, ख़ुदकुशी, ज़हर-ख़ुरानी वग़ैरा मुआ’मलात पर ग़ौर करने लगता हूँ। दिल में, मैं कहता हूँ कि ऐसी की तैसी इस फ़िल्म की। सौ-सौ क़स्में खाता हूँ कि फिर कभी न आऊँगा और अगर आया भी तो इस कम्बख़्त मिर्ज़ा से ज़िक्र तक न करूँगा। पाँच-छः घंटे पहले से आ जाऊँगा। ऊपर के दर्जे में सबसे अगली क़तार में बैठूंगा। तमाम वक़्त अपनी नशिस्त पर उछलता रहूँगा! बहुत बड़े तुर्रे वाली पगड़ी पहन कर आऊँगा। अपने ओवर-कोट को दो छड़ियों पर फैला कर लटका दूंगा! बहरहाल मिर्ज़ा के पास तक नहीं फटकूँगा!
लेकिन इस कम्बख़्त दिल को क्या करूं? अगले हफ़्ते फिर किसी अच्छे फ़िल्म का इश्तिहार देख पाता हूँ तो सबसे पहले मिर्ज़ा के हाँ जाता हूँ और गुफ़्तुगु फिर वहीं से शुरू होती है कि “क्यों भई मिर्ज़ा! अगली जुमेरात सिनेमा चलोगे ना?”
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.