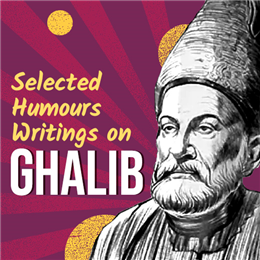ग़ालिब के घर में एक शाम
तारीख़: शब-ए-क़द्र और दीवाली का दिन। क़ब्ल ग़दर दिल्ली में, 1800 ई.
वक़्त: माबैन अस्र-ओ-मग़रिब। साया ढल रहा है।
किरदार:
1-मीरज़ा ग़ालिब
2- बेगम ग़ालिब
(एक मर्दाना कमरा। दीवारों पर ताज़ा सफ़ेदी फिरी हुई, बोसीदा ईरानी क़ालीन जिस पर चीते की खाल का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। तीन तकिए इधर उधर पड़े हुए एक पर कुलाह-ए-पपाख़, एक के पास जाम-ए-सिफ़ाल, एक पर औंधी मीनाए मय। पास ही एक शम्मा ख़ामोश और एक चौसर की बिसात बिछी हुई है, दाएं तरफ़ बाहर का एक दरवाज़ा, कुंडी लगी हुई। वस्त में एक मुक़फ़्फ़ल दरवाज़ा, क़ुफ्ल अबजद वाला, बाएं जानिब एक अफ़्सुर्दा गुलख़न, आधी जली हुई लकड़ियों से भरा हुआ, ऐन छत के क़रीब जाले से ढंपा हुआ रौज़न।)
पर्दा उठने पर मीरज़ा ग़ालिब तन्हा खुला हुआ क़बा पहने इधर उधर टहलते नज़र आते हैं, कुछ गुनगुना रहे हैं। कभी क़लम से काग़ज़ पर कुछ लिख देते हैं।
मीरज़ा ग़ालिब: हफ़्त औरंग, ऐ जहाँदार-ए-आफ़ताब-ए-आसार... आफ़ताब-ए-आसार, इन्क़िलाब-ए-आसार। आफ़ताब को क़ाफ़िया करदूं, बादशाह को ऐसी ही ज़मीन पसंद आती है। इन “लैला आश्ना” और “बेपर्वा नमक” वाली ग़ज़लों पर बहुत ख़ुश हुए थे, जभी वज़ीफ़ा मुक़र्रर कर दिया, मगर ये कुछ इस बदज़ौक़ का अंदाज़ा हो जाता है और फिर ख़्वाह-मख़्वाह की दिमाग़ सोज़ी। “आसार” ठीक है। “अफ़्गार” और “फ़िगार” दोनों तरह के क़ाफ़िए बंध सकेंगे। हाँ तो, “था मैं इक दर्द मंद सीना-फ़िगार” ठीक! “था मैं इक बे नवाए गोशा नशीं” और “था मैं अफ़्सुर्दा दिल शिकस्ता... मगर ये मेरा अपना मर्सिया नहीं उनका क़सीदा है, सीना फ़िगार ही काफ़ी है तो फिर क्या हुआ मुझे? “हो गई मेरी गर्मी-ए-बाज़ार” हाँ, “तुमने जो मुझको आबरू बख़्शी, हो गई मेरी गर्मी-ए-बाज़ार” बड़ी।
मोमिन ख़ां को फ़िक़रा कसने का मौक़ा मिल गया और तो कुछ न हुआ, कहता था, “अब तुम वज़ीफ़ा-ख़्वार हो दो शाह को दुआ।” लेकिन उसकी तअल्लियों से क्या होता है। आप तो रमल फ़ाल से पैसे कमा लेता है, गो ढोंग तबाबत का रचा रखा है। ख़ैर मुझे मिसरा हाथ आ गया। मक़ता नहीं बनता था, न जाने ये मक़ता क्यों ज़रूरी है। मुशायरे की ग़ज़लों में कहना ही पड़ता है। अच्छा भला हो गया था, “ग़ालिब वज़ीफ़ा-ख़्वार हो दो शाह को...” वो दिन गए कि “कहते थे नौकर नहीं हूँ में।” जैसे मुशायरे वैसी ग़ज़लें, अजीब अजीब शे’रों पर दाद मिलती, “ख़ाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ।” हाय, “आख़िर गुनहगार हूँ काफ़िर नहीं हूँ मैं।” इस पर बस मोमिन और मुफ़्ती साहिब (यानी आज़ुर्दा) को जुंबिश हुई बाक़ी तो वो ख़ाक बने रहे।
ये भी ज़िला जगत हो गई। कम्बख़्त दरबारियों की सोहबत मेरा मज़ाक़ बिगाड़ रही है, क़सीदे भी लिखने पड़े। अभी तीन शे’र ही हुए हैं और ये मिसरा “हो गई मेरी...” कुछ सुस्त सा है, क़तआ क्यों न कर डालूं। “हुई मेरी वो गर्मी-ए-बाज़ार” ठीक, “कि हुआ मुझ सा ज़र्रा-ए-नाचीज़” क्या हुआ? ज़र्रा को आफ़ताब बनाना पड़ेगा जभी समझेंगे। हाँ..., “मुझसा ज़र्रा-ए-नाचीज़।” क्या हो गया? मतला अल अनवार...? क़ाफ़िया तो ख़ूब है: रू-कश मेहर मतला-ए-अलानवार? बेमानी मालूम होगा उन्हें। पहले ही मोहमलगो कहने लगते हैं... है आफ़ताब सवाबित सय्यारा? नहीं, नहीं, रूशनास-ए-सवाबित सय्यारा, ये ठीक है। लेकिन ये फिर मेरा अपना क़सीदा होजाता है।
उस कम्बख़्त को कान भरने का मौक़ा मिल जाएगा। क्या करूँ, नाहक़ दरबारी बन गया। उसके लिए तो बाइस-ए-आबरू था ये ओह्दा। उस दिन चोट समझा नहीं: “बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता।” मक़ता काम आगया। सब हंस रहे थे और वो हैरान था... हाँ... तो: “बादशाह का ग़ुलाम कारगुज़ार।” ये ठीक रहेगा। इसमें अपनी कारगुज़ारी भी आ गई... मुसलसल कर डालूं इसे। एक, दो, तीन। ठीक तीनों बैठ गए हैं, गरचे अज़रूए नंग बेहुनरी हूँ ख़ुद अपनी नज़र में इतना ख़्वार, अगर अपने को मैं कहूं ख़ाकी, जानता हूँ कि आए ख़ाक को आर। शाद हूँ लेकिन अपने जी में कि हूं, बादशह का ग़ुलाम कारगुज़ार। बादशाह सलामत को मार्फ़त का भी दावा है। बेचारा सूफ़ी मिज़ाज है। इस दिन: “असल-ए-शुहूद-ओ-शाहिद-ओ-मशहूद एक है” पर ख़ासी दाद दी थी।
उस दिन से कभी कभी ग़ज़ल में एक-आध तसव्वुफ़ का शे’र जोड़ना ही पड़ जाता है, पीर-ओ-मुर्शिद जो हुए: ख़ानाज़ाद और मुरीद और... ख़ुदा जाने क्या? मुरीद और नौकर? नहीं नौकरी का अलग ज़िक्र चाहिए। उस मक़ता पर कहा गया था कि: “वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं” में रऊनत पाई जाती है, गोया मतासन हूँ, और हूँ भी... हाँ तो: ख़ानाज़ाद और मुरीद और... मद्दाह था हमेशा से ये... क्या था मैं पहले? सवानिह निगार था मगर ये लफ़्ज़ बैठता नहीं तो फिर क्या हो?... हाँ, “अरीज़ा निगार” “था हमेशा से ये अरीज़ा निगार।” ठीक! “ख़ानाज़ाद और मुरीद और मद्दाह, था हमेशा से ये अरीज़ा निगार” और बारे नौकर भी हो गया... सद हैफ़! सच तो यही है मगर...
(मुक़फ़्फ़ल दरवाज़े पर ज़नाना दस्तक होती है)
खोलता हूँ, खोलता हूँ, सब्र करो, क्या हर्फ़ थे। क़ुफ्ल अबजद लगा हुआ है। तुम्हारी ही पसंद है, सब्र करो (बड़ी मुश्किल से हुरूफ़ जोड़ कर खोलते हैं और बेगम साहिबा नाक पर रूमाल रखे दाख़िल होती हैं।)
बेगम: ये दरवाज़े बंद करके क्या कर रहे थे? बारे आज ख़लवत है। मीना ख़ाली जो है (नाक से रूमाल हटाकर) मगर बदबू बदस्तूर आरही है। सारा कमरा मुतअफ़्फ़िन है।
मीरज़ा: काम कर रहा हूँ, अब ये पुरानी बहस अज़सर-ए-नौ शुरू करने से क्या हासिल, मेरे खाने पीने के बर्तन तो अलग कर रखे हैं तुमने।
बेगम: तुमने वो बर्तन भी तो बेच डाले, अब मिट्टी के आबखू़रों पर जाम-ए-जम के तसव्वुर में ख़ुश हो रहे हो, न जाने तुम्हारी फ़ाका शिकनी क्या रंग लाएगी। मगर अच्छा हुआ वो सारा शैतानी कारख़ाना भी साथ ही बर्बाद हो गया। शराब सबको ले डूबी। आख़िर तुम्हें ऐसी बदबूदार चीज़ से इतनी मुहब्बत क्यों है?
मीरज़ा: (मुस्कराकर) तुम जैसी नकीरैन को भगाने के लिए, कहा जो है काम कर रहा हूँ। मतलब की बात कहो।
बेगम: काम? क्यों काम का नाम बदनाम कर रहे हो। क्या काम था।
मीरज़ा: काम का नाम बदनाम माशा अल्लाह मुक़फ़्फ़ा इबारत बोलने लगी हो। आख़िर शायर की बीवी ठेरीं।
बेगम: तुम शे’र भी तो काम के नहीं कहते।
मीरज़ा: (बिगड़ कर) क्या हुआ मेरे शे’रों को?
बेगम: यही तो मैं पूछती हूँ। न जाने क्या हुआ है उनको। आग़ा ऐश की बीवी कहती थी किसी की समझ में ही नहीं आते।
मीरज़ा: समझ हो तो आएं, मगर तुम अच्छी बीवी हो, दुश्मनों की हाँ मैं हाँ मिलाती हो।
बेगम: सच बोलती हूँ झूट की आदत नहीं मुझे, तुम्हारा ही कहा किया है।
मीरज़ा: (मुस्कुराकर) बारे मेरे शे’र तो याद होने लगे तुम्हें। आहिस्ता-आहिस्ता समझने भी लगोगी।
बेगम: तुमने कुछ-कुछ मेरी ज़बान सीखनी शुरू की है तो सुलझ गए हो वर्ना वो आग़ाई उर्दू किसे याद हो सकती है, नाख़ुन तैश-ए-मिज़्राब नहीं, न जाने क्या था, हकीम ऐश की बीवी कुछ सुना रही थी।
मीरज़ा: (बिगड़ कर) क्या बेहूदगी है। मेरा शे’र कब है ये, सब उसी बेगमाती आग़ा की तोहमत तराशी है। चाहते हैं मैं भी ज़नानी बोली लिखा करूँ। हम आबाई सुलह बंद ठेरे (तन कर) सौ साल से है पेश-ए-आबा सिपहगरी, कुछ...
बेगम: (बीच में बात काट कर) सच कहते हो। वाक़ई ये तुम्हारी किस्म की शायरी ज़रिया-ए-इज़्ज़त नहीं हो सकती। इसमें तुमसे वो हज्जाम का लड़का ही अच्छा रहा ख़ाक़ानी-ए-हिंद, मलकुश्शुअरा, न जाने क्या-क्या कुछ कहलाया। काश, तुम बुज़ुर्गों की तरह सुलह बंद ही रहते। ये शे’र गोई क्यों शुरू की। बुज़ुर्गों का नाम डुबोना ही था तो कोई और काम करते, जिससे कुछ आमद होती।
मीरज़ा: काम तो कर रहा था। तुम यूंही तज़ी-ए-औक़ात कर रही हो।
बेगम: ख़ाक काम कर रहे थे। क्या काम था जो ताले चढ़ा कर यूं जुते हुए थे?
मीरज़ा: अब तुम्हें तो जब तक कोई घास खोदता नज़र न आए, काम मालूम नहीं होता। क़सीदा लिख रहा हूँ। बादशाह सलामत का और आज रात दरबार में हाज़िरी है, सुनाना है।
बेगम: घास खोद सकते तो यूं दरोदीवार पर सब्ज़ा तो न उग रहा होता, घर सहरा मालूम होता है। इतना सब्ज़ा है कि बाज़ार में बेचने से रात की रोटी का सामान आजाता। इसी लिए आई थी। न लकड़ी है न कोयला, आराम के अस्बाब तो क्या सामान खूर्द-ओ-नोश भी नहीं, महीने भर से रोज़ कहती हूँ ख़त्म हो गया, मगर तुम हर बार मज़ाक़ में टाल देते हो।
मीरज़ा: महीना भर से रोज़ कहती हो और ख़त्म आज हुआ है। तुम औरतों की किसी बात का एतबार क्या हो, और फिर मैं क्या करूँ, मामा को पैसे दो, मंगवा लो।
बेगम: पैसे दो, मंगवा लो, पैसे कहां से दूं? चील के घोंसले में मास कहां? मर्दों की छः माही की तरह तनख़्वाह मिलती है तुम्हें, एक तिहाई साहूकार के नज़र होजाती है, कुछ शराब-ओ-कबाब में उड़ा डालते हो। जायदाद पहले ही से रहन है। ख़ुदा जाने तुम शराब क्यों पीते हो? ख़ुदा और रसूल का ख़्याल नहीं तो जेब ही का फ़िक्र होता। शराब की मुहब्बत है तो अगले जहां में महरूमी के ख़ौफ़ ही से तो रुक जाओ।
मीरज़ा: वहां मिलती रहेगी, फ़िक्र न करो। तुम्हें आदत नहीं है, तुम अपना ख़्याल करो। अच्छू पे अच्छू आएँगे, हमारा क्या है, साक़ी-ए-कौसर की बख़्शिश पर सहारा है, और यहां तो तुम्हारे रवय्ये को बर्दाश्त करने और भुलाने की ख़ातिर पीता हूँ। कल बीमार था, अकेला पड़ा सड़ा किया, तुम्हें इतनी तौफ़ीक़ न हुई कि पूछ लेतीं, शराब न पियूँ तो और क्या करूँ?
बेगम: बीमार? ज़्यादा पी ली थी और क्या और फिर तुमने ख़ुद ही तो कह रखा है,
“पड़िए गर बीमार तो कोई न हो तीमारदार।” मैंने तुम्हारा कहा कर देखा।
मीरज़ा: साथ “हम सुख़न कोई न हो और हम ज़बां कोई न हो” की शर्त भी तो थी। इस रोज़ की चिड़चिड़ से तंग आकर लिखा था। भला इस तू तू मैं मैं में क्या काम हो सके, और रुपया कहां से आये।
बेगम: तो क्या रुपया कमाने का काम कर रहे थे? क्या था वो काम?
मीरज़ा: क़सीदा लिख रहा था बाशाह सलामत का।
बेगम: तुम रुपया कमाने का ज़िक्र कर रहे थे, उन क़सीदों में क्या रखा है, पहले लिख कर क्या मिला? सड़ी हुई मूंग की दाल, अकड़ी हुई बेसनी रोटी, सेम के बीज, जो अब दावे बांध रहे हो। यही ग़नीमत है साल में चंद ठीकरियाँ मिल जाती हैं जैसा काम वैसे दाम। ख़ुदा जाने ये सिलसिला भी किस तरह क़ायम है। तुम्हारे शे’र भी तो इसी क़िस्म के होते हैं।
मीरज़ा: देखो, मज़ाक़ की हद होती है। मैंने तुम्हें नमाज़ पर कुछ हंसी मज़ाक़ में कहा था तो तुम मैके चले जाने की धमकियां देने लगी थीं। मेरे शे’रों के मुताल्लिक़ ये अंदाज़-ए-गुफ़्तगु जारी रखा तो फिर मैं भी खोटे हथियारों पर उतर आऊँगा।
बेगम: लेकिन नमाज़ तो फ़र्मुद-ए-ख़ुदा है तुम्हारे शे’रों से क्या निस्बत?
मीरज़ा: मेरे शे’र भी तो नवा-ए-सरोश हैं, ग़ैब से मज़ामीन आते हैं,
ग़ालिब अगर ईं फ़न-ए-सुख़न दीन बूदे
आँ दीन रा एज़दी किताब एन बूदे
बेगम: ठीक, ख़ुदा की बातें ख़ुदा ही जाने। ग़ैब ही से मज़ामीन आते होंगे जो मअनी यूं ग़ायब रहते हैं और ज़बान तो वाक़ई ऊपर वाली है। इस ज़मीन पर बसने वाले तो नहीं बोलते, कम अज़ कम दिल्ली में तो नहीं बोलते हैं।
मीरज़ा: दिल्ली दिल्ली, दिल्ली को मैं क्या जानता हूँ? ख़ुद उर्दू की क्या हैसियत है? मेरे मआनी आनेवाली नसलें समझेंगी।
बेगम: सही होगा, मगर रोटी तो आज चाहिए। आने वाली नसलें ख़ुदा जाने कब आएं। क़सीदा तो बहादुर शाह, दिल्ली के बादशाह को सुनाना है।
मीरज़ा: और ऐसा लिख रहा हूँ कि बादशाह सुनकर फड़क जाये। सुनो कैसे पुरज़ोर अशआर हैं,
ऐ शहनशाह-ए-आसमां औरंग
ऐ जहाँदार-ए-आफ़ताब-ए-आसार
था...
बेगम: (टोक कर) ये पहला शे’र है क्या? मतला कहां है?
मीरज़ा: मतला मक़ता क्या होता है, तुम शे’र सुनो;
ऐ शंहशाह...
था मैं इक बे नवाए गोशा नशीं
था मैं इक दर्दमंद सीना फ़िगार
तुमने मुझको जो आबरू बख़्शी
हुई मेरी वो गर्मी-ए-बाज़ार
कि हुआ मुझसा ज़र्रा-ए-नाचीज़
रूशनास-ए-सवाबित-ओ-सय्यार
गरचे अज़रूए नंग-ए-बेहुनरी
हूँ ख़ुद अपनी नज़र में इतना ख़्वार
कि गर अपने को मैं कहूं ख़ाकी
जानता हूँ कि आए ख़ाक को आर
शाद हूँ अपने जी में कि हूँ
बादशह का ग़ुलाम-ए-कारगुज़ार
ख़ानाज़ाद और मुरीद और मद्दाह
था हमेशा से ये अरीज़ा निगार
बारे नौकर भी हो गया सद-शुक्र
निस्बतें हो गईं मुशख़्ख़स चार
बेगम: इसमें आधी फ़ारसी है और काम की बात नदारद। ये दास्तान-ए-माज़ी है, आज की हालत बयान करो। मगर तुम्हें सीधा साफ़ लिखना ही नहीं आता। मैं ये था और मैं वो था, अब क्या हो ये कहो। लेकिन अब वक़्त कम है और ऐसी मुश्किल ज़बान में लिखना कोह-ए-कुन्दन के बराबर है।
मीरज़ा: कोह-ए-कुन्दन क्या। लिखना क्यों नहीं आता। मैं क्या हूँ, ये लिखूँ। लो अभी लो। (फ़िललबदीह कहने लगते हैं)
आज मुझसा नहीं ज़माने में
शायर नग़ज़ गो-ए-ख़ुश गुफ़्तार
रज़्म की दास्तान गर सुनिए
है ज़बां मेरी तेग़-ए-जौहरदार
बज़्म का इल्तिज़ाम गर कीजे
है क़लम मेरा अब्र-ए-गौहर बार
बेगम: (टोक कर) ये अपना क़सीदा कह रहे हो कि बादशाह का, मतलब की बात कहो, साफ़ साफ़ कहो तनख़्वाह माहवार चाहिए, ऊपर सर्दियां आरही हैं, कपड़े नहीं हैं, आख़िर तुम दरबारी हो, तुम्हारी बे आबरूई दरबार की बे आबरूई है, क़र्ज़ा बढ़ रहा है।
मीरज़ा: तो ये भट्ट गिरी हुई।
बेगम: तो क़सीदा और क्या होता है। मेरी मानो, सीधी सीधी बातें लिक्खो, मगर वही आग़ा ऐश की बीवी की बात, तुम उस तरह लिख ही नहीं सकते।
मीरज़ा: लिख नहीं सकता? यूं वाहियात बकना क्या मुश्किल है, सन लो;
न कहूं आपसे तो किससे कहूं
मुद्दआ-ए-ज़रूरी अल इज़हार
पीर-ओ-मुर्शिद अगरचे मुझको नहीं
ज़ौक़-ए-आराइश-ए-सरोद-ओ-तार
कुछ तो जाड़े में चाहिए आख़िर
ताना दे बाद-ए-ज़महरीर आज़ार
क्यों न दरकार हो मुझे पोशिश
जिस्म रखता हूँ, है अगरचे नज़ार
कुछ ख़रीदा नहीं है अब के साल
कुछ बनाया नहीं है अब के बार
आग तापे कहां तलक इंसान
धूप खाए कहां तलक जानदार
धूप की ताबिश आग की गर्मी
वक़िना रब्बना अज़ाबन्नार
बेगम: (बीच में) बात हुई न? और वो क़र्ज़ और तनख़्वाह का मुआमला?
मीरज़ा: (कान से क़लम उतार कर फिर लिखने लगते हैं और साथ ही साथ पढ़ते जाते हैं)
मेरी तनख़्वाह जो मुक़र्रर है
ऊस के मिलने का है अजब हंजार
रस्म है मुर्दे की छः माही एक
ख़ल्क़ का है उसी चलन पे मदार
मुझको देखो तो हूँ ब-क़ैद-ए-हयात
और छः माही हो साल में दोबार
बस कि लेता हूँ हर महीने क़र्ज़
और रहती है सूद की तकरार
मेरी तनख़्वाह में तिहाई का
हो गया है शरीक साहूकार
ज़ुल्म है गर न दो सुख़न की दाद
क़ह्र है गर करो न मुझको प्यार
आपका बंदा और फिरूँ नंगा
आपका नौकर और खाऊँ उधार
मेरी तनख्वाह कीजिए माह ब माह
ता न हो मुझको ज़िंदगी दुशवार
बेगम: बात हुई न? जब तुम यूं लिख सकते हो तो फिर हमेशा इसी तरह क्यों नहीं लिखते। देख लेना दाद भी ख़ूब मिलेगी और बादशाह सलामत को हक़ीक़त-ए-हाल भी मालूम हो जाएगी।
मीरज़ा: ख़ैर दाद तो जो मिलेगी, मालूम। अलबत्ता क़सीदा गया। छत्तीस के क़रीब अशआर हो गए हैं, एक दो दुआइया रास्ते में लगा दूंगा। तर्तीब भी बदल दूँगा, मुकम्मल काम हो गया, चलो तुम्हारा कहा भी कर देखता हूँ।
(इतने में मग़रिब की अज़ान सुनाई देती है, बेगम नमाज़ के लिए ज़नाने में चली जाती हैं और ग़ालिब कपड़े बदलने लगते हैं। कुलाह पपाख़ का तिर्छा ज़ाविया बना रहे थे कि बेगम लौट आती हैं)
बेगम: खाना अभी खाओगे या वापस लौट कर।
मीरज़ा: खाना? कहाँ से आगया? और तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आईं? नमाज़ तो ख़ुदा के दरबार में हुज़ूरी होती है मगर तुम करो भी क्या। आख़िर तुम्हें नमाज़ों से क्या हासिल? जन्नत में हम जाएं तो हमें हूरें मिलेंगी, तुम्हें क्या मिलेगा? कोई मस्जिद का मुल्ला, नीला तहमद, खद्दर का कुर्ता, कांधे पर रूमाल, रूमाल में हुजरे की कुंजी, सर पर पग्गड़, और हम... जनाब दाएं तरफ़...
बेगम: (बिगड़ कर) देखिए ये तमस्खुर अब छोड़िए, मैं कह चुकी हूँ ख़ुदा और रसूल के अहकाम पर फब्तियां न किया करो, ये उसी का वबाल है कि मेरे बच्चे ज़िंदा नहीं रहते। आरिफ़ को पाला था वो भी...(बेगम की आँखें नमनाक होजाती हैं। ग़ालिब भी नमनाक हो जाते हैं, इतने में बाहर से कहारों की आवाज़ आती है, “पीनस हाज़िर।”)
बेगम: नवाब ख़ैर से सवार हो जाइए और कोई अच्छी ख़बर लाइए।
मिर्ज़ा: (ज़ेर-ए-लब) “बेमाया चूमाई कि मिर्ज़ा रिन्दही।” कहते हुए बाहर चले जाते हैं, बेगम ज़नाने में लौट आती हैं।
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.