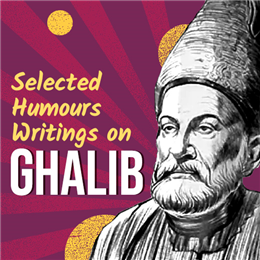मिर्ज़ा ग़ालिब से इंटरव्यू
मैं: क्या ये वाक़िया है कि आपके वालिद मोहतरम अबदुल्लाह बेग आपकी तरह अह्ल-ए-क़लम या अह्ल-ए-ख़राबात में से नहीं बल्कि अह्ल-ए-सैफ़ में से थे और उनका इंतक़ाल भी एक मुहिम में बंदूक़ की गोली खाकर हुआ था। नीज़ आपका सिलसिला-ए-नसब शाहान-ए-तूराँ अफ़सरासियाब और पशंग से मिलता है।
ग़ालिब: सौ पुश्त से है पेशा-ए-आबा सिपहगरी
कुछ शायरी ज़रीया-ए-इज़्ज़त नहीं मुझे
मैं: माफ़ कीजिएगा क़िबला, मैंने महज़ इंटरव्यू के शुरूआत की ग़रज़ से ये बात पूछ ली वर्ना आपकी शायरी ही के बारे में आपसे कुछ दरयाफ़्त करना मक़सूद है। हक़ीक़त में आपका पूरा उर्दू कलाम मोतियों में तौलने के क़ाबिल है। रशीद अहमद सिद्दीक़ी ने सच कहा है कि अगर मुझसे पूछा जाये कि हिन्दोस्तान को मुग़लिया सल्तनत ने क्या दिया तो मैं बेतकल्लुफ़ तीन नाम लूँगा, ग़ालिब, उर्दू और ताज महल।
आपके मजमूआ-ए-कलाम की सी ग़ैरमामूली अहमियत और मक़बूलियत आज तक उर्दू के किसी दूसरे शे’री मजमुए को नसीब नहीं हो सकी। उर्दू के अलावा दुनिया की बेशुमार मुतअद्दिद ज़बानों में भी इसके बेशुमार एडिशन शाया हो चुके हैं। आप अपने आपको ‘हज़ार गुलशन-ए-ना-आफ़्रीदा’ का अंदलीब कहें लेकिन हमारे इस दौर के एक मशहूर शायर तिलोक चंद महरूम के बाक़ौल,
गुलज़ार-ए-सुख़न से फूल जो चुनते हैं
बुलबुल की नवा में तेरी लय सुनते हैं।
मफ़हूम तेरा समझ नहीं पाते जो
वो भी तेरे अशआर पे सर धुनते हैं।
ग़ालिबः गर ख़ामुशी से फ़ायदा इख़्फ़ा-ए-हाल है
ख़ुश हूँ कि मेरी बात समझनी मुहाल है।
मैं: आपकी ख़ुशी सर आँखों पर हुज़ूर लेकिन इस तमहीद से मेरा मक़सद आपसे ये दरयाफ़्त करना है कि आपकी अपनी नज़र में आपके चंद ऐसे मुंतख़ब उर्दू अशआर कौन से हैं जो आपके शायराना कमाल की पूरी नुमाइंदगी करते हैं।
ग़ालिबः फ़ारसी बीं ताबबीनी नक़्श-हा-ए-रंग रंग
बुग्ज़र अज़ मजमूआ-ए-उर्दू कि बेरंग-ए-मन अस्त।
मैं: लेकिन आली-जनाब आप जिसे बेरंग कह रहे हैं वो मजमूआ हमारे लिए तो रंगों की एक कान से कम नहीं। इसके मुताल्लिक़ हमारे एक नौजवान नाक़िद ख़लील-उर-रहमान आज़मी ने पेशगोई की है कि इस शायरी के एक से ज़्यादा रंग हैं, जूँ-जूँ ज़माना गुज़रता जाएगा, इसमें रंगों का इज़ाफ़ा होता जाएगा। हद तो ये है कि मुल्हिद हों, सूफ़ी हों या फ़लसफ़ी, मार्क्स के पुजारी हों या फ्राएड के पैरोकार, सभी को आपके अशआर के पैमानों में अपने-अपने अक़ाइद के रंग झलकते दिखाई दे जाते हैं।
ग़ालिबः दिल-ए-हसरत ज़दा था माइदा-ए-लज़्ज़त-ए-दर्द
काम यारों का बक़द्र-ए-लब-ओ-दंदाँ निकला।
मैं: लेकिन गुस्ताख़ी माफ़, चंद ऐसे शारेहीन-ए-किराम भी हैं जो आपके बा’ज़ अशआर को बेमानी क़रार देते हैं।
ग़ालिबः न सताइश की तमन्ना न सिले की पर्वा
न सही गर मेरे अशआर में मअनी न सही।
मैं: आपने ठीक कहा है कि आपके अशआर गंजीना-ए-मअनी के तिलिस्म हैं। उन्हें समझना कार-ए-तिफ़लाना नहीं। आप इसे ख़ुद मेरी शोख़ी-ए-तिफ़लाना पर ही महमूल कीजिए लेकिन ये कहने की जसारत तो मैं भी करूँगा कि आपके इस क़िस्म के अशआर...
ग़ुन्चा ता शगुफ़्तन हा बर्ग-ए-आफ़ियत मालूम
बावजूद-ए-दिलजमई ख़्वाब-ए-गुल परेशां है।
या
ब-हसरत गाह नाज़-ए-कुश्ता जान बख़्शी ख़ूबाँ
ख़िज़्र को चश्म-ए-आब-ए-बक़ा से तर जबीं पाया।
मुझे भी कुछ मुबहम से नज़र आते हैं और मेरे ख़्याल में आपके चंद शे’रों का मफ़हूम इजमाली इशारों की वजह से गुंजलक हो गया है जैसे...
मैकदा गर चश्म-ए-मस्त-ए-नाज़ से पावे शिकस्त
मू-ए-शीशा दीदा-ए-साग़र की मिज़्गानी करे।
या
नक़्श-ए-नाज़-ए-बुत-ए-तन्नाज़ ब आग़ोश-ए-रक़ीब
पा-ए-ताऊस प-ए-ख़ामा-ए-मानी माँगे।
ग़ालिबः मेरे इबहाम पे होती है तसद्दुक़ तौज़ीह
मेरे इजमाल से करती है तराविश तफ़सील।
मैं: इसमें क्या शक है क़िबला-ओ-का’बा,
सब कहाँ कुछ लाला-ओ-गुल में नुमायाँ हो गईं
ख़ाक में क्या सूरतें होंगी कि पिनहाँ हो गईं।
और
महरम नहीं है तू ही नवा-हा-ए-राज़ का
याँ वर्ना जो हिजाब है पर्दा है साज़ का।
जैसे सदाबहार और हकीमाना शे’र कह कर आपने उर्दू शायरी के खज़ाने में जो बेश-बहा इज़ाफ़ा किया है, उसकी वजह से अगर आपकी शख़्सियत को ‘गुल-ए-नग़मा’ और ‘पर्दा-ए-साज़’ से ताबीर किया जाये तो ना-मुनासिब न होगा।
ग़ालिबः न गुल-ए-नग़्मा हूँ न पर्दा-ए-साज़
मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़।
मैं: अल्लाह-अल्लाह इतनी दिल शिकस्तगी और मायूसी! जोश मलीहाबादी ने आपके बारे में वाक़ई सच कहा है कि आज ग़ालिब को पूजा जा रहा है। कल जब वो ज़िंदा था तो उसी दिल्ली में अक्सर-ओ-बेशतर आधा पाव गोश्त और एक पाव शराब के लिए तरसता रहा। आज मुल्क के बड़े-बड़े दौलतमंद उसके मज़ार की ज़यारत के लिए आते हैं। कल जब वो ज़िंदा था तो उसे ख़ुद उमरा के दरवाज़ों पर जाना पड़ता था।
ग़ालिबः ज़िंदगी अपनी जो इस तौर पे गुज़री ग़ालिब
हम भी क्या याद करेंगे कि ख़ुदा रखते थे।
मैं: ग़ालिबन इस तौर पर ज़िंदगी गुज़ारने का नतीजा है कि ग़म आपकी शायरी का ग़ालिब रुझान बन गया है, जैसे...
मुनहसिर मरने पर हो जिसकी उम्मीद
ना-उमीदी उसकी देखा चाहिए।
और
कहते हैं जीते हैं उम्मीद पे लोग
हमको जीने की भी उम्मीद नहीं।
और
जिसे नसीब हो रोज़-ए-सियाह मेरा सा
वो शख़्स दिन न कहे रात को तो क्यों कर हो।
ग़ालिबः ग़म-ए-हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज
शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक।
मैं: चलिए मौत ग़म-ए-हस्ती का इलाज सही लेकिन जनाब-ए-मन, मौत कितनी भी ख़ूबसूरत हो ज़िंदगी का कोई जवाब नहीं।
ग़ालिबः हवस को है निशात-ए-कार क्या-क्या
न हो मरना तो जीने का मज़ा क्या।
मैं: ख़ूब! तो मरकर आपने जीने का मज़ा हासिल कर लिया, लेकिन जीते-जी क्या सूरत रही?
ग़ालिब: था ज़िंदगी में मौत का खटका लगा हुआ
उड़ने से पेशतर भी मेरा रंग ज़र्द था।
मैं: खटके का सवाल मिर्ज़ा साहिब, मौत तो आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी महरूमी थी और आप जीते जी यही कहते रहे कि...
मरते हैं आरज़ू में मरने की
मौत आती है पर नहीं आती।
और
किस से महरूमी-ए-क़िस्मत की शिकायत कीजे
हमने चाहा था कि मर जाएँ सो वो भी न हुआ।
ये फ़रमाईए कि अब आपकी ये शिकायत रफ़ा हो चुकी है। आप क्या महसूस करते हैं?
ग़ालिब: ढाँपा कफ़न ने दाग़-ए-उयूब-ए-बरहनगी
मैं वर्ना हर लिबास में नंग-ए-वुजूद था।
मैं: आपने फ़रमाया…
तुझे हम वली समझते जो न बादा-ख़्वार होता।
हमारे नज़दीक बादाख़्वारी के बावुजूद आपकी हक़ीक़त किसी वली से कम नहीं। लेकिन ये तो बताईए, क्या शराब से आपकी इतनी गहरी वाबस्तगी महज़ ग़म का रद्द-ए-अमल है।
ग़ालिबः मय से ग़रज़ निशात है किस रू-सियाह को
यक गू ना बेख़ुदी मुझे दिन रात चाहिए।
मैं: गुस्ताख़ी माफ़, खू-ए-बद रा बहाना बिस्यार वाली बात है। ख़ैर, इस ख़ाना-ख़राब के जवाज़ में आप कुछ भी कहिए लेकिन ये फ़रमाईए, अब मुल्क-ए-अदम में इस देरीना मश्ग़ले की क्या सूरत है?
ग़ालिब: ग़ालिब छुटी शराब पर अब भी कभी-कभी
पीता हूँ रोज़-ए-अब्र-ओ-शब-ए-माहताब में।
मैं: लेकिन एक रिंद-ए-बला नोश होने के बावजूद और इस क़िस्म की बातें कहने के बाद कि...
पिला दे ओक से साक़ी जो हम से नफ़रत है
पी जिस क़दर मिले शब-ए-महताब में शराब।
सर्फ़-ए-बहा-ए-मय हुए आलात-ए-मयकशी
बेमय किसे है ताकत-ए-आशोब-ए-आगही।
क़र्ज़ की पीते थे मय
आपने ये शे’र क्योंकर कह दिया...
सोहबत-ए-रिंदाँ से लाज़िम है हज़र
जा-ए-मय अपने को खींचा चाहिए।
ग़ालिबः तर्क-ए-लज़्ज़त भी नहीं लज़्ज़त से कम
कुछ मज़ा इसका भी चखना चाहिए।
मैं: आपने हुस्न-ओ-इश्क़ की निहायत नाज़ुक कैफ़ियतों के मुताल्लिक़ अक्सर निहायत शगुफ़्ता शे’र कहे हैं, लेकिन इस शगुफ़्तगी में हिज्र का एक गहरा एहसास भी कारफ़र्मा है जैसे...
कब से हूँ क्या बताऊँ जहान-ए-ख़राब में
शब हाए-हिज्र को भी रखूँ गर हिसाब में।
क्या महबूब के वस्ल से महरूम ही रहे?
ग़ालिबः ये न थी हमारी क़िस्मत कि विसाल-ए-यार होता
अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता।
मैं: तो गोया वस्ल-ए-यार से महरूम रहने के बावजूद आप ज़िंदगी-भर इश्क़ में मुबतला रहे और आपको ये एहसास भी होता रहा कि आपके ऐसे काम के आदमी को इश्क़ ने “निकम्मा” करके रख दिया है। आख़िर ऐसे इश्क़ से हासिल...
ग़ालिबः इश्क़ से तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया
दर्द की दवा पाई दर्द-ए-ला-दवा पाया।
मैं: लेकिन अब भी आपको महबूब के वस्ल की तमन्ना है या नहीं? क्योंकि हमने जिगर मुरादाबादी की ज़बान से यही सुना है,
इश्क़ मरने पे भी नहीं मिटता
ये ताल्लुक़ ज़रूर रहता है।
ग़ालिब: दिल में ज़ौक़-ए-वस्ल-ओ-याद-ए-यार तक बाक़ी नहीं
आग इस घर में लगी ऐसी कि जो था जल गया।
मैं: आपकी काफ़ी समअ ख़राशी की क़िबला, माफ़ कीजिएगा। आख़िर में एक छोटी सी बात और पूछना चाहता हूँ, वो ये कि अपनी शायरी को ज़्यादा से ज़्यादा मुअस्सर और ताबनाक बनाने के लिए एक शायर को किस चीज़ की ज़रूरत होती है?
ग़ालिबः हुस्न फ़रोग़ शम्म-ए-सुख़न दूर है असद
पहले दिल-ए-गुदाख़्ता पैदा करे कोई।
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.