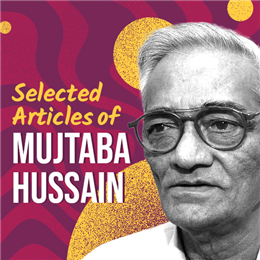मुशायरे और मुजरे का फ़र्क़
दिल्ली के एक हफ़तावार रिसाले ने उर्दू मुशायरों के ज़वाल पर मुख़्तलिफ़ शायरों और दानिशवरों के बयानात को शाए करने का सिलसिला शुरू किया है। उसके ताज़ा शुमारे में उर्दू के बुज़ुर्ग शायर हज़रत ख़ुमार बाराबंकवी का एक बयान शाया हुआ है जिसमें उन्होंने मुशायरे के ज़वाल के दीगर अस्बाब पर रौशनी डालते हुए “आज के दौर की शायरात के बारे में भी इज़हार-ए-ख़याल किया है। उनका कहना है कि आज की शायरात ने मुशायरे को मुजरा बना दिया है। पहले मैं मुशायरे में जाता था तो उम्र बढ़ती थी। मगर अब मुशायरों में जाने से उम्र घटने लगी है।”
हज़रत ख़ुमार बाराबंकवी माशा-अल्लाह अब अस्सी (80) के पेटे में हैं और पिछले साठ बरसों से मुल्क के मुशायरों में हिस्सा ले रहे हैं। ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि जितने मुशायरे उन्होंने पढ़े हैं, उतनी तो किताबें भी हमने न पढ़ी होंगी। अपनी उम्र, तजुर्बा और इ'ल्म के ऐ'तबार से उनका शुमार हमारे बुज़ुर्गों में होता है और वो हमारे पसंदीदा शायरों में से हैं। लेकिन कभी-कभी हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि बुज़ुर्गों से इख़्तिलाफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने एक बार पतरस बुख़ारी से पूछा, “बताइए के तंबूरे और तानपुरे में क्या फ़र्क़ होता है?” इस पर पतरस बुख़ारी ने सर ज़फ़रुल्लाह ख़ाँ से पूछा, “हुज़ूर! ये बताइए कि अब आपकी उम्र क्या है?” सर ज़फ़रुल्लाह ख़ाँ बोले, “पचहत्तर (75) बरस का हो चुका हूँ।” ये सुनकर पतरस बुख़ारी ने निहायत इत्मिनान से कहा, “हुज़ूर! जब आपने अपनी ज़िंदगी के पचहत्तर बरस तंबूरे और तानपुरे का फ़र्क़ जाने बगै़र गुज़ार दिए तो पाँच दस बरस और सब्र कर लीजिए। ऐसी भी क्या जल्दी है।” ख़ुमार बाराबंकवी ने अब जो ये कहा है कि मौजूदा दौर की शायरात ने मुशायरे और मुजरे के फ़र्क़ को ख़त्म कर दिया है और ये कि मुशायरों में शिरकत करने से अब उनकी उम्र घटने लगी है तो इस सिलसिले में हमारी दस्त-बस्ता अ'र्ज़ ये है कि वो ऐसी ग़ैर ज़रूरी बातों पर ग़ौर करके अपनी उम्र को मज़ीद घटने न दें। ये क्या ज़रूरी है कि वो अपनी उम्र को बढ़ाने की आस में मुशायरों में शिरकत करते रहें। माना कि ख़ुमार बाराबंकवी हमारे बुज़ुर्ग हैं लेकिन हम उनके इस बयान से इत्तिफ़ाक़ नहीं करते कि आजकी शायरात ने मुशायरे और मुजरे के फ़र्क़ को ख़त्म कर दिया है क्योंकि हमारा ख़याल है कि मुशायरे और मुजरे में अब भी एक वाज़ेह फ़र्क़ मौजूद है।वो इस तरह कि मुजरे में तवाइफ़ें इस तरह बन-संवर कर और सज-धज कर पेश नहीं होतीं जैसी हमारी ख़ातून शाएरा मुशायरों में जलवागर होती हैं।
माशा अल्लाह हमने भी दुनिया देखी है और हम उम्र की इस मंज़िल में हैं जहाँ हम अपनी उम्र के हिंदसे काग़ज़ पर लिखते हैं तो ये हिंदसे तक एक दूसरे से मुंह मोड़े हुए नज़र आते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी उम्र अब ख़ुदा के फ़ज़ल से 62 बरस की हो चुकी है और ज़रा मुलाहिज़ा फ़रमाएं कि 2 और 6 के हिंदसों में कैसी अन बन पैदा हो चुकी है कि एक का मुंह मग़रिब की तरफ़ तो दूसरे का मश्रिक़ की तरफ़। उम्र की ये वो मंज़िल होती है जहाँ आदमी न सिर्फ़ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगता है बल्कि अपने गुनाहों का ए'तिराफ़ भी कर लेता है। ख़ुमार साहब ने हो सकता सिर्फ़ मुशायरों में शिरकत की हो लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में (जो ख़ुमार साहब की उम्र के लिहाज़ से मुख़्तसर ही कहलाएगी) मुशायरों और मुजरों दोनों में शिरकत की है बल्कि एक मुजरे वाली के घर पर मुशायरों की सदारत भी की है। जवानी में आदमी क्या नहीं करता। ये 1968 ई. की बात है। अब आपसे क्या छुपाएं कि उस मुजरे वाली के हाँ, जो अदब का बहुत अच्छा ज़ौक़ रखती थी मुशायरा रात में दस बजे मुक़र्रर होता था तो हम आठ बजे ही मुशायरा की सदारत करने के लिए पहुंच जाते थे। मुशायरा तो रात के बारह बजे बरख़ास्त हो जाता था लेकिन हमारी सदारत बसा-औक़ात रात में दो बजे तक जारी रहती थी। सामईन के लिए शतरंजियाँ बाद में बिछती थीं, पहले मस्नद-ए-सदारत बिछाई जाती थी जो सबसे आख़िर में उठाई जाती थी। ख़ुदा झूट न बुलवाए उन मुशायरों में भी हमने हमेशा शे'र ही सुने। कभी मुजरा नहीं देखा जबकि आज के मुशायरों में हम बा'ज़ ख़ातून शो'रा की इ'नायत से मुशायरा कम सुनते हैं और मुजरा ज़्यादा देखते हैं। दूसरी बात ये कि हमने मुजरे वालियों को कभी इतना बे-बाक (बल्कि बे-बाक़), बे-हया, बे-शर्म मगर साथ ही साथ ऐसा बे-पनाह नहीं पाया जैसा कि मुशायरों में हमारी बा'ज़ शायरात नज़र आती हैं। ख़ुदा की क़सम मुजरे वालियाँ तो बेहद शरीफ़, पाक-बाज़ और हयादार होती हैं। उन बेचारी शरीफ़ बीबियों को तो अपने गाने बजाने से मतलब होता है जबकि बा'ज़ शायरात की शायरी में शायरी की इतनी अहमियत नहीं होती जितनी कि “मावरा-ए-शायरी” की होती है। उनका सारा दारोमदार “मावरा-ए-शायरी” पर ही होता है। हमारे एक नदीदे दोस्त हैं जिन्होंने पाँच-छः बरस पहले एक मुशायरे में ऐसी ही किसी “मावरा-ए-शायरी शायरा” को सुनने के बाद आँखें फाड़-फाड़ कर हम से कहा था,“ब-ख़ुदा क्या शे'र कहती है कि बस देखते रह जाइए।” हमने कहा, “मगर शे'र का तअ'ल्लुक़ देखने से नहीं सुनने से होता है।” बोले, “मगर उस शायरा का यही तो कमाल है कि उसके शे'र सुनने के नहीं देखने के होते हैं। बिल्कुल हाथी के दाँतों वाला मुआ'मला है। बहरा आदमी भी उसके कलाम को आसानी से समझ सकता है। शायरी हो तो ऐसी बा'ज़ शे'र तो ऐसे निकालती है कि बिला मुबालिग़ा शे'रों से लिपट जाने और उन्हें अपनी बाँहों में समेट लेने को जी चाहे। उर्दू में आज तक किसी ने ऐसे शे'र नहीं कहे थे। यही वजह है कि उसके शे'रों से कमा हक़्क़हु लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आँखों का ज़्यादा से ज़्यादा और कानों का कम से कम इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर उसकी शायरी कानों से सुनी जाए तो हो सकता है कि बा'ज़ मिस्रे बह्र से ख़ारिज नज़र आएं, वज़न भी कहीं-कहीं गिर रहा हो। लेकिन अगर आप अपनी आँखों से उसे देखें तो वल्लाह वो सरापा बंद बह्र नज़र आती है। वज़न में ऐसी जकड़ी हुई और तनी हुई है कि ख़ुद देखने वाले का वज़न गिर-गिर जाए और संभाले न संभले। वो तरन्नुम से कलाम नहीं सुनाती बल्कि कलाम से तरन्नुम सुनाती है। सिर्फ़ वो ही नहीं बोलती बल्कि उसका अंग-अंग बोलता है।शे'र उसके सालिम बदन में मचलने और थिरकने, ठुमकने और हुमकने लगता है और शे'र का मतलब उसके पूरे सियाक़-व-सबाक के साथ उसकी ख़ुमार आलूदा आँखों में यूँ छलकने लगता है कि देखने वाला आँख मारे बिना नहीं रह सकता। हाय-हाय ज़ालिम शे'र सुनाती है तो लगता है कि ख़ुद सरापा ग़ज़ल बन गई है।”
अल-ग़रज़ हमारे नदीदे दोस्त ने उस शायरा के बारे में और भी बहुत सी बातें कही थीं लेकिन हम उन्हें यहाँ मज़ीद इसलिए बयान नहीं करेंगे कि उन्हें लिखने में बैठे हैं तो ख़ुद हमारी तबीयत के मचलने और बहकने के आसार नमूदार होने लगे हैं। इसलिए अपने नदीदे दोस्त के बयान को हम यहाँ ख़त्म करते हैं।
अभी पिछले महीना हमारे दोस्त और उर्दू के बही-ख़्वाह प्रोफ़ेसर सत्य पाल आनंद ने हमें अमरीका से ख़त लिखा था, जिसमें एक मुशायरे की रूदाद बयान की गई थी। उन्होंने बताया था कि अमरीका के एक मुशायरे में ऐसी ही एक शायरा जब कलाम सुनाने लगी तो एक सामेअ' को जो हाज़िरीन में बैठा हुआ था उसका कोई शे'र इतना पसंद आया कि उसने इज़हार-ए-पसंदीदगी के तौर पर महफ़िल में बैठे-बैठे ही शायरा को दूर ही से दस डालर का करंसी नोट दिखाया। इस पर शायरा डायस से उतर कर ख़रामाँ-ख़रामाँ दस डालर को हासिल करने की ग़रज़ से करंसी नोट के पास गई। उसे हासिल किया और करंसी नोट को सीने के ऐ'न ऊपर मगर बलाउज़ के अंदर रखते हुए फिर से वही शे'र सुनाना शुरू कर दिया। ज़रा ग़ौर कीजिए कि सामेअ' ने “मुक़र्रर इरशाद” का क्या ख़ूबसूरत नेम-उल-बदल दरयाफ़्त किया है। सच है अमरीकी डालर में बड़ी ताक़त होती है।
हमें उस वक़्त अपनी जवानी के दिनों के एक सहाफ़ी दोस्त याद आ गए जो इन दिनों सऊदी अरब में निहायत कामयाब और शरीफ़ाना ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। बिल्कुल इस्म-ए-बा-मुसम्मा बन गए हैं। जवानी के दिनों में उन्हें हमेशा कोई न कोई नई बात सूझती थी। आज से तीस-पैंतीस बरस पहले उन्होंने हैदराबाद के रवींद्र भारती थियेटर में एक ऐसा मुशायरा मुनअ'क़िद किया था जिसमें सिर्फ़ ख़ातून शो'रा ने शिरकत की थी और जिसमें उनके कहने के मुताबिक़ मुल्क भर की मुमताज़ ख़ातून शो'रा शरीक हुई थीं। हमें अब भी उन ख़ातून शो'रा के कुछ नाम याद हैं जैसे नाज़ कानपूरी, पूनम कलकत्तवी, सुलताना बाराबंकवी, ज़ेबा मुरादाबादी, नजमा नागपुरी, चित्रा भोपाली वग़ैरा। मुशायरा से पहले अख़बारों में बतौर-ए-तशहीर इन शायरात की जान लेवा तस्वीरें (जिन के तराशे पिछले साल तक हमारे पास महफ़ूज़ थे) कुछ ऐसे एहतिमाम से शाए हुईं कि कई सिक़्क़ा और संजीदा हज़रात ने भी इस मुशायरे में शिरकत को ज़रूरी समझा। ऐसे हज़रात में हम भी शामिल थे। मुशायरा कुछ इतना कामयाब रहा कि रवींद्र भारती थियेटर की छतों का उड़ना बाक़ी रह गया था। (छतें इसलिए भी नहीं उड़ीं कि उन दिनों ये थियेटर नया नया बना था और मज़बूत भी था।) मुशायरे के बाद हम किसी वजह से कुछ देर रुक गए और जब बाहर निकले तो देखा कि मुशायरागाह के बाहर ज़ेबा मुरादाबादी, नजमा नागपुरी और पूनम कलकत्तवी एक रिक्शा वाले से हैदराबाद के एक मख़सूस मोहल्ले तक चलने के लिए किराए के मसले पर तकरार कर रही हैं। सच पूछिए तो उस मुशायरे में हमें मुशायरे का ही लुत्फ़ आया था, मुजरे का नहीं। तीस-पैंतीस बरस में हमारे हाँ मुशायरे की रिवायत उस मुक़ाम पर पहुंच गई है जहाँ मुजरा पीछे रह गया है और मुशायरा आगे को निकल गया है। इसलिए कि मुजरे के कुछ आदाब होते हैं जिनका अब तक भी पास-व-लिहाज़ रखा जाता है लेकिन मुशायरा के आदाब जो कभी हुआ करते थे अब बाक़ी नहीं रहे। हज़रत ख़ुमार बाराबंकवी से हमें दिली हमदर्दी है कि ऐसे मुशायरों में जाकर उनकी उम्र बढ़ने के बजाए कम होने लगी है। हम तो ख़ैर कभी भी किसी मुशायरे में ये सोचकर नहीं गए कि यहाँ जाने से हमारी उम्र बढ़ेगी। अगर मुशायरों में जाने से उम्र बढ़ सकती तो इ'ल्म-ए-तिब ने आज इतनी तरक़्क़ी न की होती। हर कोई हस्पताल जाने के बजाए मुशायरा में भर्ती हो जाता। हम तो ख़ैर ख़ुद भी शायर नहीं हैं और न ही शायरी से कोई दिलचस्पी रखते हैं। बस कभी कभार बा'ज़ मख़सूस शायरात को देखने के लिए मुशायरों में चले जाते हैं। हमें नहीं पता कि इससे हमारी उम्र बढ़ती है या घटती है। लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि हम अपने आप को फिर से जवान महसूस करने लगते हैं। अब भला बताइए इस उम्र में ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है।
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.