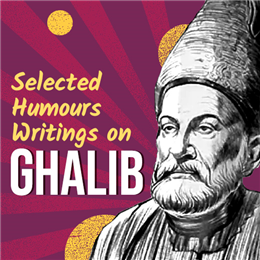आए है बे-कसी-ए-इश्क़ पे रोना ग़ालिब
इस गर्दिश-ए-अय्याम ने किसी और को बिगाड़ा हो या न बिगाड़ा हो मगर इश्क़ को अ'र्श से फ़र्श पर वो पटख़नी दी है कि अगर उस दौर में आँसुओं पर इतना शदीद पहरा न होता तो यक़ीनन उसकी बे-कसी पर रोना आ जाता। यूँ दुहाई देते तो फिर भी लोग नज़र आ ही जाते हैं।
फिरते हैं दश्त दश्त दिवाने किधर गए
वो आ'शिक़ी के हाय ज़माने किधर गए
हाय-हाय। कैसे-कैसे ज़माने देखे हैं इश्क़ ने...! जिधर नज़र डालिए बस इश्क़ ही इश्क़ का राज था। अंदाज़ा होता है कि उस ज़माने में क्या अ'वाम क्या ख़वास, क्या शायर, क्या तबीब सबका पेशा इश्क़ था। तूल-व-अर्ज़ में फैली हुई इस वसीअ' काइनात में किसी और चीज़ से दिलचस्पी नहीं। किसी काम से मतलब नहीं। किसी बात की फ़िक्र नहीं। दिल पर ख़ूँ की एक गुलाबी से उम्र भर शराबी-शराबी रहते हैं और प्राहिबेशन ऐक्ट के तहत पकड़े भी नहीं जाते...!
दर पर बिन कहे घर बना लेते हैं और न महबूब उन्हें वहाँ से कान पकड़ कर लटकाता है, न स्टेट ऑफिसर दा'वा दाएर करता है! तेग़-ओ-कफ़न बांधे हुए जाते हैं और ख़ुदकुशी का इल्ज़ाम भी आइद नहीं होता!
और उस दौर के आ'शिक़ को ख़ुद को आ'शिक़ साबित करने के लिए कुछ कहने सुनने की तो ख़ैर ज़रूरत ही नहीं थी... हुलिया देख कर ही लोग समझ जाते थे। जनाब नहीफ़-व-निज़ार इतने कि अअ'ज़ा दीदा-ए-ज़ंजीर की मुज़गानी करें... किसी महफ़िल में बिठा दिए जाएँ तो दूरबीन ख़ुर्दबीन की मदद के बगै़र नज़र न आएँ। बिस्तर पर लेटें तो उसकी शिकन में गुम हो जाएँ... अव्वल तो बे लिबासी तुर्रा-ए-इम्तियाज़! जो बिलफ़र्ज़ लिबास हो भी तो गिरेबान चाक-चाक और दामन तार-तार... चेहरे पर हवाइयाँ...पाँव में छाले... एक हाथ में दिल, दूसरे में जिगर... आँखों से जू-ए-ख़ून बह रही हैं तो मुँह से आहों के साथ शोले निकल रहे हैं... अब इस हुलिये के बाद भला इज़हार-ए-इश्क़ की ज़रूरत ही बाक़ी कहाँ रह जाती है! ये तो चलता फिरता इश्तिहार हुआ... आँख के अंधे और कान के बहरे और गांठ के पूरे को भी आपके मजनूँ के भाई-बंद होने में ज़रा शुबहा नहीं रहता... (वैसे रिवायत यही है कि आज तक दुनिया का कोई महबूब अंधा बहरा या गाँठ का पूरा नहीं हुआ!)
जो ज़रा सलीक़ामंद आशिक़ हुआ... और जिसने दामन-ओ-गिरेबान से बग़ावत न की और न ही बू-ए-ख़ूँ और आह-ए-आतिशीं से कुछ ज़्यादा वास्ता रखा तो फिर उसका कुछ इस क़िस्म का हुलिया होता था,
कहता था कसू से कुछ तकता था कसू का मुँह
कल मीर खड़ा था याँ सच है कि दीवाना था
आज यूँ अगर कोई सर झाड़ मुँह पहाड़ खड़ा जिस तिस का मुँह तका करे तो लोग बजाए कूचा-ए-महबूब के चंदा करके सीधे रांची पहुंचा आएँ। अब तो ये आलम-ए-होश-ओ-हवास और बसद चैन-ओ-सुकून इश्क़ करना पड़ता है और आशिक़ ग़रीब की आधी ज़िंदगी इसी उलझन की नज़्र हो जाती है कि वो अपने आशिक़ होने का ऐलान कैसे करे, महबूब के जोर-ओ-सितम उसे घुलाते हों या न घुलाते हों, मगर ये उलझन उसे ज़रूर आधा कर देती है (दुनिया में हर क़िस्म के कामों में मशविरा देने वाली कंपनियाँ और ब्यूरो खुल चुके हों, काश कोई साहब-ए-ज़ौक़ और हमदर्द मुल्क-ओ-क़ौम इस तरफ़ भी तवज्जो दे!)
जाने ख़ून सफ़ेद हो गए हैं या बनास्पती चीज़ें खाते-खाते और बनास्पती बातें करते-करते जिस्म में ख़ून रहा ही नहीं। बहरहाल आज का आशिक़ ख़ून के आँसू नहीं रोता। बल्कि वो सिरे से आँसू बहाने के फ़न से ही नावाक़िफ़ होता है। मौक़ा बे-मौक़ा क़हक़हे अलबत्ता लगा लेता है और क़हक़हों को इज़हार इश्क़ का ज़रिया अब तक तस्लीम नहीं किया गया!
वो बतौर रसीद ग़श खाकर गिर पड़ने वाली ख़ास अदा हुआ करती थी वो आज न जाने क्यों रिवायती सींगों की हैसियत इख़्तियार कर चुकी है! ग़ालिबन इसलिए कि सड़कें आज कल पक्की होने लगी हैं! अगर इब्तिदा-ए-इश्क़ में ही उसे यूँ सर पकड़ कर रोना पड़े(बल्कि बहुत मुम्किन है कि मरहम पट्टी भी करवानी पड़े!)तो आगे-आगे जो कुछ भी होगा उसे देखने की हिम्मत उसमें कहाँ बाक़ी रह जाएगी...!
तो आशिक़ आज न रो सकता है न ग़श खा कर गिर सकता है। न पाँव में आबले होते हैं। न आहें बाल-ए-अ'न्क़ा को जला देने वाली! और दामन-ओ-गिरेबान को तार-तार करना क्या मा'नी एक ज़रा सी खोंच कपड़ों में लग जाए तो क़ीमत का ख़याल आते ही आशिक़ के टूटे टुटाए दिल पर एक बाल और पड़ जाता है। इसीलिए तो आज का शायर कहता है,
वो जो अब चाक गिरेबाँ भी नहीं करते हैं
देखने वालो कभी उनका जिगर तो देखो
अब ज़ाहिर है जिगर डॉक्टर के सिवा कोई नहीं देख सकता। और हर एक का महबूब डॉक्टर तो होता नहीं। लीजिए, हज़रत-ए-इश्क़ अपना सा मुँह लेकर रह गए!
आ'शिक़-ए-क़दीम को खाने कमाने की तो कोई फ़िक्र होती नहीं। ग़ालिबन वो ग़म ही को मन-ओ-सल्वा समझ कर खा लिया करता था और ख़ून-ए-जिगर को शरबत-ए-रूह-अफ़्ज़ा समझ कर पी लेता था। लिहाज़ा जब देखे वो हज़रत कूचा-ए-दिलदार ही में पाए जाते थे।
जीते जी कूचा-ए-दिलदार से जाया न गया
उसकी दीवार का सर से मेरे साया न गया
आज का आशिक़ दिन भर तो कूचा-ए-अफ़्सुर्दा दफ़्तर में जान गँवाता है, शाम को जो ज़रा बन संवर कर कूचा-ए-दिलदार की नियत बांध के दरवाज़े के बाहर क़दम रखा और घर के सब ख़ुर्द-ओ-कलाँ ने शक-ओ-शुबहा की नज़्रों से देखा और मा'ना-ख़ेज़ अंदाज़ में मुस्कराने लगे।
बावा जान ने कड़कदार आवाज़ में पूछा, “हुज़ूर की सवारी इस वक़्त कहाँ तशरीफ़ ले जा रही है।”
लीजिए अब कोई फ़िलबदीह बहाना गढ़िए! जिसमें ये शायराना सलाहियत और तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी न हुई वो हकलाते नज़र आने लगे,
“वो-वो इमरान के पास जा रहा हूँ।”
“मियाँ साहबज़ादे, इमरान ख़ुद आप की इत्तिला के मुताबिक़ आज सुबह जबलपुर गया है।”
“जी हाँ, जी हाँ, तो ज़रा सेंट्रल लाइब्रेरी ही चला जाऊँगा।”
“ये तुम्हारी लायब्रेरी पीर को कब से खुलने लगी?”
और अब आशिक़ बेचारा बाल बिगड़ जाने के डर से सर तक नहीं पीट सकता!
जाने पुराने ज़माने के आशिकों पर ये रोक-टोक क्यों नहीं थी। शायद उस ज़माने में आशिक़ का कोई रिश्तेदार कोई वली वारिस होता ही नहीं होगा। बस आज़ादी ही आज़ादी थी। आशिक़ी पर एक का पैदाइशी हक़ था। बल्कि कार-ए-सवाब और तर्क-ए-आशिक़ी गुमराही समझी जाती थी।
अल्लाह री गुमरही बुत-ओ-बुतख़ाना छोड़ कर
मोमिन चला है का'बा को इक पारसा के साथ
लेकिन आज ये बड़ी हिम्मत का काम है। ग़ैरों के नाविक-ए-दुशनाम। अपनों की तर्ज़-ए-मलामत। ता'ने तिशने कानाफूसी और रुसवाई सर-ए-बाज़ार... इश्क़ से पहले आशिक़ का ख़ात्मा यक़ीनी!
उम्र-ए-रफ़्ता के महबूब इस क़दर क़त्ल-ओ-ग़ारत और फ़ित्ना-ओ-शर बरपा करने के बावजूद भी बेचारे बुरे-भले और ख़ुदातरस बंदे हुआ करते थे। घर हमेशा ऐसे तंग-व-तारीक कूचों में बस्ते थे कि जिस में धूप का कहीं ज़िक्र नहीं। हमेशा दीवार का साया ही रहा करता था और तारीकी ऐसी कि सारी ज़िंदगी दीवार के साए के तले गुज़ार दीजिए क्या मजाल जो किसी राहगीर तक की नज़र पड़ जाए!
ख़ुदा जाने आज कल वो तंग-ओ-तारीक कूचे कहाँ जा बसे। ये मलबे चौड़े रास्ते और जलती हुई तारकोलों की सड़कें आ गईं कि इतना भी तो साया नहीं होता कि आशिक़ दरिया के सामने दम भर को सुस्ता ले। और जो वो ज़रा किसी दरख़्त के साये में या दीवार की आड़ में उम्मीद-ओ-बीम की हालत में दिल की तेज़ होती हुई धड़कनों को गिनता। दरवाज़े पर नज़रें गाड़े खड़ा हो गया। या उचक-उचक कर अंदर के हालात का जाएज़ा लेने की कोशिश की। या सड़क के दो-चार चक्कर लगाए तो पुलिस चोर उचक्का समझ कर पीछे लग गई और दरिया के बजाए हज़रत-ए-आशिक़ दर-ए-कोतवाली पर नज़र आने लगे! वो ये तक नहीं कह सकता,
दैर नहीं दम नहीं दर नहीं आस्ताँ नहीं
बैठे हैं राहगुज़र पे हम कोई हमें उठाए क्यों
और अगर पुलिस के दस्त-ए-रसा से बच भी गए तो हर आन दनदनाती हुई गुज़रने वाली मोटरों की ज़द में आ जाना यक़ीनी है!
चार-छः चक्कर लगाने के बाद ज़रा जाँबाज़ क़िस्म के आशिक़ अंदर दाख़िल होने या सदा देने का इरादा भी कर लें तो सियासत-ए-दरबाँ तो नहीं अलबत्ता दिल नारा-ए-दरबाँ से ज़रूर डर जाता है! जब दरबान अशरफ़-उल-मख़लूक़ात में से हुआ करते थे, आशिक़ कभी तो उनके क़दम ले लिया करते थे और कभी उसकी गालियों के जवाब में दुआएँ देकर उसे ख़ुश करते थे... मगर इन फ़ील-ए-तन बर्क़ रफ़तार। राद-ए-गुफ़्तार कुत्तों के क़दम कोई किस तरह ले!
चलिए... ये मजनूँ के रिश्तेदार मुँह लटकाए बे-नील-ओ-मराम कूचा-ए-जानाँ से लौट आए।
इतना ये नाज़ुक कि आशिक़ कूचा-ए-जानाँ के दो एक फेरों में ही घबरा जाता है। मगर ज़रा पुराने आशिक़ की हिम्मत तो मुलाहिज़ा फ़रमाइए,
उस नक़्श-ए-पा के सज्दे ने क्या-क्या किया ज़लील
मैं कूचा-ए-रक़ीब में भी सर के बल गया
कूचा-ए-रक़ीब और फिर सर के बल? दाद नहीं दी जा सकती इस बे-जिगरी की! आशिक़ी काहे को हुई अच्छी ख़ासी नट गिरी हो गई। (वैसे आशिक़ के लिए उस फ़न का माहिर होना यूँ भी ज़रूरी है!) आज सर के बल किसी कूचे में चलने से महबूब तो नहीं सर्कस में नौकरी ज़रूर मिल सकती है!
बड़ी आसानी की बात तो उस दौर में ये थी कि शहर में बस एक ही हसीन और एक ही महबूब हुआ करता था क्योंकि ख़याल ये था कि,
जो शहर में तुम से एक दो हों तो क्यों कर हो
लीजिए साहब... इंतिख़ाब की सारी उलझनें ख़त्म... आज कल तो शहर के जिस कोने में चाहे हसीनों को एक पुरा क़हक़हे लगाता रंग-ओ-नूर का तूफ़ान लिये आँखों को चकाचौंद करता गुज़र जाएगा और आप ट्रैफ़िक के उसूलों की इस तरह ख़िलाफ़ वर्ज़ी करने की रिपोर्ट भी किसी कोतवाली में दर्ज नहीं करा सकेंगे!
तो शहर भरा है हसीनों से और हर आशिक़ का अपना एक महबूब है बल्कि बैयक वक़्त कई-कई महबूब हुआ करते हैं। इज़हार-ए-इश्क़ का मसला और टेढ़ा हो गया!
इस तरक़्क़ी पसंदी, तहज़ीब-ओ-तमद्दुन और इस एडिकेट ने तो इश्क़ को और डुबो दिया... इशारे कनाए, ज़बान बे-ज़बानी सब ख़त्म हो गए... जब तक आप अपना मक़सद फ़ुट नोटस के साथ बयान न करें तब तक आपको क्या या ख़ुद आप समझ लीजिए या अगर ख़ुदा को हंगामा हाए-शश जह्त से फ़ुर्सत मिल गई तो वो समझ लेगा मगर इस बीसवीं सदी का पढ़ा लिखा अक़लमंद महबूब तो नहीं समझ सकता!
आपने एक लंबी सी ठंडी आह भरी और वो ये समझकर कि आपको साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है फ़ौरन आपकी ख़िदमत में पानी पेश कर देगा। (ख़्वाह मारे झुंझलाहट के आप उसमें डुबकियाँ ही क्यों न लगाने का तहय्या कर लें!)
आपने दिल के दर्द की शिकायत की वो आपको शहर के बेहतरीन डॉक्टर के पास ले जाकर दिल का कार्डियोग्राम करवा देगा! शिकस्तगी का इज़हार कीजिए, सर्जीकल डिपार्टमेंट से रुजू करने का मशवरा मिलेगा!
बीमारी में अगर उन को देखकर चेहरे पे रौनक़ आ जाए तो उस डाक्टर का तफ़सीली पता और शिजरा-ए-नस्ब पूछा जाएगा जिसका इलाज आप करवा रहे हैं... और वो तमाम दवाएं देखी और चखी जाएँगी जो इस्तेमाल की जा रही हैं!
इत्तिफ़ाक़ीया तौर पर कहीं मुलाक़ात हो जाने पर अगर आपकी आँखों से ख़ुशी दमकने लगी और होंटों पर मुस्कुराहट नाचने लगी तो इसे रस्मी अख़लाक़ पर मह्मूल किया जाएगा! कुछ वज़ाहत के ख़याल से आपने क़हक़हा लगाया और आप पर हतक-ए-इज़्ज़त का दावा!
उनकी पैरवी में ब्लैक काफ़ी, कोल्ड काफ़ी, मेंढक का अचार, कछुवे का मुरब्बा जैसी वाहियात चीज़ें ज़हर-मार कीजिए... आपके ज़ौक़ का इर्तिक़ा और नख़रे की दाद दी जाएगी!
हिज्र में तारे गिनिए... वो समझेंगे हिसाब की क़ाबिलियत बढ़ाई जा रही है। घर के आगे मुझे चक्कर लगाइए। ख़याल होगा कि सड़कें नाप कर इंजीनियरिंग में किसी नए बाब के इज़ाफ़े की तैयारी है।
ज़ुल्फ़ें परेशाँ कीजिए... फ़लसफ़ी का ख़िताब मिलेगा।
खाना-पीना छोड़ दीजिए, गुमान गुज़रेगा कुछ और नाज़ुक और स्मार्ट बनने की कोशिश की जा रही है।
और जो तंग आकर सचमुच मर जाइए... तो दुआ-ए-मग़्फ़िरत के बाद कहा जाएगा, ख़लल था दिमाग़ का।
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.