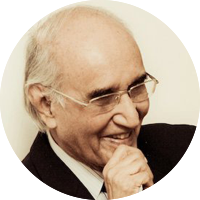बारे आलू का कुछ बयाँ हो जाए
दूसरों को क्या नाम रखें, हम ख़ुद बीसियों चीज़ों से चिड़ते हैं। करम कल्ला, पनीर, कम्बल, काफ़ी और काफ्का, औरत का गाना, मर्द का नाच, गेंदे का फूल, इतवार का मुलाक़ाती, मुर्ग़ी का गोश्त, पानदान, ग़रारा, ख़ूबसूरत औरत का शौहर...
ज़्यादा हद्द-ए-अदब कि मुकम्मल फ़ेहरिस्त हमारे फ़र्द-ए-गुनाह से भी ज़्यादा तवील और हरी-भरी निकलेगी। गुनहगार सही लेकिन मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग की तरह ये हमसे आज तक नहीं हुआ कि अपने तअस्सुबात पर माक़ूलात का नीम चढ़ा कर दूसरों को अपनी बेलुत्फ़ी में बराबर का शरीक बनाने की कोशिश की हो। मिर्ज़ा तो बक़ौल कसे, ग़लत इस्तिदलाल के बादशाह हैं। उनकी हिमायत-ओ-वकालत से माक़ूल से माक़ूल “काज़” निहायत लच्चर मालूम होने लगता है। इसलिए हम सब उन्हें तब्लीग़-ए-दीन और हुकूमत की हिमायत से बड़ी सख़्ती से बाज़ रखते हैं। उनकी एक चिड़ हो तो बताएं। फ़ेहरिस्त रंगा-रंग ही नहीं, इतनी ग़रीबपरवर भी है कि उसमें इस फ़क़ीर बे-तक़सीर का नाम भी ख़ासी ऊंची पोज़ीशन पर शामिल रह चुका है। बाद में हमसे ये पोज़ीशन बैंगन के भरते ने छीन ली और उसकी जैकी कैनेडी के दूल्हा ओनासिस ने हथिया ली। मिर्ज़ा को आज जो चीज़ पसंद है कल वो दिल से उतर जाएगी और परसों तक यक़ीनन चिड़ बन जाएगी।
लोग हमें मिज़्रा का हमदम-ओ-हमराज़ ही नहीं, हमज़ाद भी कहते हैं। लेकिन इस यगानगत और तक़र्रुब के बावजूद हम वसूक़ से नहीं कह सकते कि मिर्ज़ा ने आलू और अबुल कलाम आज़ाद को अव्वल अव्वल अपनी चिड़ कैसे बनाया। नीज़ दोनों को तिहाई सदी से एक ही ब्रैकट में क्यों बंद कर है?बुए या सुमन बा क़ेस्त मौलाना के बाब में मिर्ज़ा को जितना खुरचा, तास्सुब के मुलम्मा के नीचे ख़ालिस मंतिक़ की ये मोटी मोटी तहें निकलती चली गईं। एक दिन कई वार ख़ाली जाने के बाद इरशाद फ़रमाया, “एक साहब-ए-तर्ज़ इंशा पर्दाज़ ने बानी-ए-नदवतुल उलमा के बारे में लिखा है कि शिबली पहला यूनानी था जो मुसलमानों में पैदा हुआ। इस पर मुझे ये गिरह लगाने की इजाज़त दीजिए कि यूनानियों की इस इस्लामी शाख़ में अबुल कलाम आख़िरी अह्ल-ए-क़लम था जिसने उर्दू रस्म-उल-ख़त में अरबी लिखी।”
हमने कहा, “उनकी शिफ़ाअत के लिए यही काफ़ी है कि उन्होंने मज़हब में फ़लसफ़े का रस घोला। उर्दू को अरबी का सोज़-ओ-आहंग बख़्शा।”
फ़रमाया, “उनकी नस्र का मुताला ऐसा है जैसे दलदल में तैरना, इसीलिए मौलवी अब्दुल हक़ ऐलानिया उन्हें उर्दू का दुश्मन कहते थे। इल्म-ओ-दानिश अपनी जगह मगर उसको क्या कीजिए कि वो अपनी अना और उर्दू पर आख़िरी दम तक क़ाबू न पा सके।
कभी-कभार रमज़ान में उनका तर्जुमान-उल-क़ुरआन पढ़ता हूँ तो (अपने दोनों गालों पर थप्पड़ मारते हुए) नऊज़-बिल्लाह महसूस होता है गोया कलाम-अल्लाह के पर्दे में अबुल कलाम बोल रहा है!”
हमने कहा, “लाहौल वला क़ुव! उस बुज़ुर्ग की तमाम करदा-ओ-नाकरदा ख़ताएँ तुम्हें सिर्फ़ इस बिना पर माफ़ कर देनी चाहिऐं कि तुम्हारी तरह वो भी चाय के रसिया थे। क्या नाम था उनकी पसंदीदा चाय का? अच्छा सा नाम था, हाँ याद आया। व्हाइट जैसमीन! यासमीन सफ़ेद!”शगुफ़्ता हुए। फ़रमाया, “मौलाना का मशरूब भी उनके मशरब की मानिंद था। टूटे हुए बुतों को जोड़ जोड़ कर इमाम उल-हिंद ने ऐसा माबूद तराशने की कोशिश की जो अह्ल-ए-सोमनात को भी काबिल-ए-क़बूल हो। यूनानी फ़लसफ़े की ऐनक से जब उन्हें दीन में दुनिया और ख़ुदा में ना-ख़ुदा का जलवा नज़र आने लगा तो वो मुसलमान हो गए और सच्चे दिल से अपने आप पर ईमान ले आए।
उसी तरह ये चीनी चाय महज़ इसलिए उनके दिल को भा गई कि उसमें चाय के बजाय चम्बेली के गजरे की लपट आती है। हालाँकि कोई शख़्स जो चाय पीने का ज़रा भी सलीक़ा रखता है, इसलिए चाय पीता है कि उसमें चाय की, फ़क़त चाय की, महक आती है, न कि चम्बेली के तेल का भबका!” हमने कहा, “ताज्जुब है तुम इस बाज़ारी ज़बान में इस आब-ए-निशात अंगेज़ का मज़हका उड़ा रहे हो, जो बक़ौल मौलाना, तबा शोरिश पसंद को सरमस्तियों की और फ़िक्र-ए-आलम आशोब को आसूदगीयों की दावत दिया करती थी।”
इस जुमले से ऐसे भड़के कि भड़कते चले गए। लाल-पीले हो कर बोले, “तुमने लिप्टन कंपनी का क़दीम इश्तिहार ‘चाय सर्दीयों में गर्मी और गर्मियों में ठंडक पहुंचाती है’, देखा होगा। मौलाना ने यहां इसी जुमले का तर्जुमा अपने मद्दाहों की आसानी के लिए अपनी ज़बान में किया है!”
बहस और दिल-शिकनी का ये सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा। लेकिन मज़ीद नक़ल कुफ़्र कर के हम अपनी दुनिया-ओ-आक़िबत ख़राब करना नहीं चाहते। लिहाज़ा इस तश्बीब के बाद मिर्ज़ा की दूसरी चिड़ यानी आलू की तरफ़ गुरेज़ करते हैं।ये दाँत सलामत हैं जब तकमिर्ज़ा का “बॉस” दस साल बाद पहली मर्तबा तीन दिन की रुख़सत पर जा रहा था। और मिर्ज़ा ने अपने मुशीरों और बही ख़्वाहों को जश्न-ए-नजात मनाने के लिए बीच लग्झरी होटल में लंच पर मदऊ किया था।
वहां हमने देखा कि समुंदरी कछुवे का शोरबा सड़ सड़ पीने के बाद मिर्ज़ा मुसल्लम केकड़े(मुसल्लम के मानी ये हैं कि मरहूम की सालिम टांगें, खपरे, आँखें और मूँछें प्लेट पर अपनी क़ुदरती हालत में नज़र आरही थीं) पर टूट पड़े।
हमने कहा, “मिर्ज़ा, हमने तुम्हें चहका मारती ख़मीरी नान खाते देखा है, खुरों के चटपटे सरेश में डुबो डुबो कर, जिसे तुम दिल्ली के निहारी-पाए कहते हो। मुफ़्त की मिल जाये तो सडांदी सारडीन यूं निगलते हो गोया नाक नहीं रखते और तो और रंगा माटी में चकमा क़बीले की एक दोशीज़ा के हाथ से नशीला कसैला जैक फ्रूट लप लप खाते हुए फ़ोटो खिंचवा चुके हो और इसके बाद पेशावर में चिड़ों के पकौड़े खाते हुए भी पकड़े जा चुके हो। तुम्हारे मशरब-ए-अक्ल-ओ-शर्ब में हर “य हलाल है सिवाए आलू के!'खुल गए, फ़रमाया, “हमने आज तक किसी मौलवी, किसी फ़िरक़े के मौलवी की तंदुरुस्ती ख़राब नहीं देखी। न किसी मौलवी का हार्ट फ़ेल होते सुना। जानते हो क्या वजह है? पहली वजह तो ये कि मौलवी कभी वरज़िश नहीं करते। दूसरी ये कि सादा ग़िज़ा और सब्ज़ी से परहेज़ करते हैं!”होटल हज़ा और आलू की अमलदारीसब्ज़ी न खाने के फ़वाइद ज़ेहन नशीन कराने की ग़रज़ से मिर्ज़ा ने अपनी ज़ेर-ए- तजुर्बा ज़िंदगी के इन गोशों को बेनक़ाब की जो आलू से कीमियाई तौर पर मुतास्सिर हुए थे। ज़िक्र आलू का है। इन्ही की ज़बान-ए-ग़ीबत बयान से अच्छा मालूम होगा। तुम्हें क्या याद होगा, मैं दिसंबर 1951 में मुंटगुमरी गया था। पहली दफ़ा कराची से बाहर जाने की मजबूरी लाहक़ हुई थी। मुंटगुमरी के प्लेटफार्म पर उतरते ही महसूस हुआ गोया सर्दी से ख़ून रगों में जम गया है। उधर चाय के स्टाल के पास एक बड़े मियां गर्म चाय के बजाय माल्टे का रस पिए चले जा हरे थे। उस बंदा-ए- ख़ुदा को देख देखकर और दाँत बजने लगे। कराची का दाइमी हब्स और बग़ैर खिड़कियों वाला कमरा बेतरह याद आए। क़ुली और ताँगे वाले से सलाह-ओ-मश्वरे के बाद एक होटल में बिस्तरा लगा दिया। जिसका असली नाम आज तक मालूम ना हो सका लेकिन मैनेजर से लेकर मेहतर तक सभी उसे होटल हज़ा कहते थे।
कमरा सिर्फ़ एक ही था जिसके दरवाज़े पर कोयले से बहरूफ़ अंग्रेज़ी वार “कमरा नम्बर1” लिखा था। होटल हज़ा में न सिर्फ़ ये कि कोई दूसरा कमरा नहीं था, बल्कि मुस्तक़बिल क़रीब या बईद में इसकी तामीर का इमकान भी नज़र नहीं आता था क्योंकि होटल के तीन तरफ़ म्यूंसिपल्टी की सड़क थी और चौथी तरफ़ उसी इदारे की मर्कज़ी नाली जो शहर की गंदगी को शहर ही में रखती थी, जंगल तक नहीं फैलने देती थी।
जज़ीरा नुमा कमरा नंबर1 में “अटैच्ड बाथरूम” तो नहीं था, अलबत्ता एक अटैच्ड तनूर ज़रूर था, जिससे कमरा इस कड़ाके की सर्दी में ऐसा गर्म रहता था कि बड़े बड़े “सेंट्रली हीटेड” (Centrally heated) होटलों को मात करता था।
पहली रात हम बनियान पहने सो रहे थे की तीन बजे सुबह जो तपिश से एका एकी आँख खुली तो देखा कि इमाम दीन बैरा हमारे सिरहाने हाथ में ख़ून आलूद छुरी लिए खड़ा है। हमने फ़ौरन अपनी गर्दन पर हाथ फेर कर देखा। फिर चुपके से बनियान में हाथ डाल कर पेट पर चुटकी ली और फिर कलमा पढ़के इतनी ज़ोर से चीख़ मारी कि इमाम दीन उछल पड़ा और छुरी छोड़कर भाग गया।
थोड़ी देर बाद तीन बैरे समझा-बुझा कर उसे वापस लाए। उसके औसान बजा हुए तो मालूम हुआ कि छुरी से वो नन्ही नन्ही बटेरें ज़बह कर रहा था।
हमने एक वक़ार के साथ कहा, “अक़लमंद आदमी, ये पहले क्यों न बताया?” उसने फ़ौरन अपनी भूल की माफ़ी मांगी और वादा किया कि आइन्दा वो पहले ही बता दिया करेगा कि छुरी से बटेर ही ज़बह करना चाहता है। नीज़ उसने आसान पंजाबी में ये भी यक़ीन दिलाया कि आइन्दा वो चीख़ सुनकर डरपोकों की तरह ख़ौफ़ज़दा नहीं हुआ करेगा।”हमने रसान से पूछा, “तुम उन्हें क्यों ज़बह कर रहे थे?”
बोला, “जनाब, ज़िला मुंटगुमरी में जानवर को हलाल कर के खाते हैं! आप भी खाएँगे?”
हमने क़दरे तुर्श रवी से जवाब दिया, “नहीं!”
और रेलवे टाइम टेबल से पंखा झलते हुए सोचने लगे कि जो लोग दूध पीते बच्चों की तरह जल्दी सोते और जल्दी उठते हैं वो इस रम्ज़ को क्या जानें कि नींद का असल मज़ा और सोने का लुत्फ़ आता ही उस वक़्त है जब आदमी उठने के मुक़र्ररा वक़्त पर सोता रहे कि उस साअत दुज़-दीदा में नींद की लज़्ज़तों का नुज़ूल होता है।
इसीलिए किसी जानवर को सुबह देर तक सोने की सलाहियत नहीं बख़शी गई। अपने अशरफ़-उल-मख़लूक़ात होने पर ख़ुद को मुबारकबाद देते-देते सुबह हो गई और हम पूरी और आलू छोले का नाशता करके अपने काम पर चले गए। थोड़ी देर बाद मेदे में गिरानी महसूस हुई। लिहाज़ा दोपहर को आलू पुलाव और रात को आलू और पनीर का कोरमा खा कर तनूर की गरमाई में ऐसे सोए कि सुबह चार बजे बैरे ने अपने मख़सूस तरीक़े से हमें जगाया, जिसकी तफ़सील आगे आएगी।नाशते से पहले हम सर झुकाए क़मीज़ का बटन नोच कर पतलून में टाँकने की कोशिश कर रहे थे कि सूई खिच से उंगली में भुक गई। बिल्कुल इज़तिरारी तौर पर हमने उंगली अपनी क़मीज़ की जेब पर रखकर ज़ोर से दबाई, मगर जैसे ही दूसरी ग़लती का एहसास हुआ तो ख़ून के गीले धब्बे पर सफ़ेद पाउडर छिड़क कर छुपाने लगे और दिल में सोचने लगे कि अल्लाह ताला ने बीवी भी क्या चीज़ बनाई है लेकिन इंसान बड़ा ही ना शुकरा है। अपनी बीवी की क़दर नहीं करता।
इतने में बैरा मक़ामी ख़ालिस घी में तली हुई पूरियां ले आया। मुंटगुमरी का असली घी पाकिस्तान भर में सबसे अच्छा होता है। उसमें चार फ़ीसद घी होता है बैरे ने हस्ब-ए-मामूल अपने अबरूए तसाहुल से हमें कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और जब हम उस पर चार के हिन्दसे की तरह तिहरे हो कर बैठ गए तो हमारे ज़ानू पर गीला तौलिया बिछाया और उसपर नाशते के ट्रे जमा कर रख दी।(मुम्किन है बाज़ शक्की मिज़ाज क़ारईन के ज़ेहन में ये सवाल पैदा हो कि अगर कमरे में मेज़ या स्टूल नहीं था तो बान की चारपाई पर नाशता क्यों न कर लिया। शिकायतन नहीं, इत्तिलाअन अर्ज़ है कि जैसे ही मुंटगुमरी का पहला मुर्ग़ पहली बाँग देता, बैरा हमारी पीठ और चारपाई के दरमियान से बिस्तर एक ही झटके में घसीट लेता।
अपने ज़ोर-ए-बाज़ू और रोज़मर्रा की मश्क़ से इस काम में इतनी सफ़ाई और महारत पैदा कर ली थी कि एक दफ़ा सिरहाने खड़े हो कर जो बिस्तर घसीटा तो हमारा बनियान तक उतर कर बिस्तर के साथ लिपट कर चला गया और हम खरी चारपाई पर केले की तरह छिले हुए पड़े रह गए। फिर चारपाई को पांयती से उठा कर हमें सर के बल फिसलाते हुए कहने लगा, साब फ़र्नीचर ख़ाली करो वजह ये कि इस फ़र्नीचर पर सारे दिन “परोप्राइटर एंड मैनेजर होटल हज़ा” का दरबार लगा रहता था।
एक दिन हमने इस बे आरामी पर पुरज़ोर एहतिजाज किया तो होटल के क़वाइद-ओ-ज़वाबित का पैंसिल से लिखा हुआ एक नुस्ख़ा हमें दिखाया गया, जिसके सर-ए- वर्क़ पर 'ज़ाब्ता फ़ौजदारी होटल हज़ा' तहरीर था।
उसकी दफ़ा नौ की रू से फ़ज्र की अज़ान के बाद ‘पसैंजर’ को चारपाई पर सोने का हक़ नहीं था। अलबत्ता क़रीब-उल-मर्ग मरीज़, ज़च्चा और यहूद-ओ-नसारा, इससे मुस्तसना थे। लेकिन आगे चल कर दफ़ा 28 (ब) ने उनसे भी ये मुराआत छीन ली थीं। उसकी रू से ज़च्चा और क़रीब-उल-मर्ग मरीज़ को ज़च्चगी और मौत से तीन दिन पहले तक होटल में आने की इजाज़त नहीं थी। “ख़िलाफ़वरज़ी करने वालों को बैरों के हवाले कर दिया जाएगा।”हमने निगाह उठा कर देखा तो उसे झाड़न मुँह में ठूंसे बड़े अदब से हंसते हुए पाया। हमने पूछा, “हंस क्यों रहे हो?” कहने लगा, “वो तो मैनेजर साब हंस रहे थे, बोलते थे, हमको लगता है कि कराची का पसैंजर बटेर को तलेर समझ के नहीं खाता!”हर चीज़ के दो पहलू हुआ करते हैं। एक तारीक, दूसरी ज़्यादा तारीक। लेकिन ईमान की बात है इस पहलू पर हमारी नज़र भी नहीं गई थी और अब इस ग़लतफ़हमी का अज़ाला हम पर वाजिब हो गया था। फूली हुई पूरी का लुक़मा प्लेट में वापस रखते हुए हमने रुँधी हुई आवाज़ में उस जालसाज़ परिंद की क़ीमत दरयाफ़्त की।
बोला, “ज़िंदा या मुर्दा?” हमने जवाब दिया कि हम तो इस शहर में अजनबी हैं। फ़िलहाल मुर्दा को ही तर्जीह देंगे। कहने लगा, “दस आने प्लेट मिलती है। एक प्लेट में तीन बटेरें होती हैं। मगर जनाब के लिए तो एक ही रास काफ़ी होगी!”क़ीमत सुनकर हमारे मुँह में भी पानी भर आया। फिर ये भी था कि कराची में मवेशीयों का गोश्त खाते खाते तबीयत उकता गई थी। लिहाज़ा दिल ही दिल में अह्द कर लिया कि जब तक मुंटगुमरी का आब-ओ-दाना है, तुयूर के इलावा किसी चीज़ के हाथ नहीं लगाएँगे। लंच पर भुनी हुई बटेर या चाय के साथ बटेर का नूरी चर्ग़ा, सोने से पहले बटेर का आब-ए-जोश।
इस रिहायशी तंवर में फ़िरोकश हुए हमें चौथा दिन था, और तीन दिन से यही अलल्ले तल़्ले थे। चौथी सुबह हम ज़ानू पे तौलिया और तौलिये पर ट्रे रखे तली हुई बटेर से नाशता कर रहे थे कि बैरे ने झाड़न फिर मुँह में ठूंस ली। हमने चमक कर पूछा, “अब क्या बात है?”
कहने लगा, “कुछ नहीं, मैनेजर साब हंस रहे थे। बोलते थे कमरा नंबर एक के हाथ बटेर लग गई है!” हमने तंज़न अटैच्ड तनूर की तरफ़ इशारा करते हुए पूछा, “तुम्हारे होटल हज़ा में और कौन सा मन-ओ-सिल्वा उतरता है?”
बोला, “हराम गोश्त के इलावा दुनिया-भर की डिश मिलती है, जो चाहें आर्डर करें,जनाब आलू-मटर, आलू-गोभी, आलू-मेथी, आलू-गोश, आलू-मच्छी, आलू-बिरयानी और ख़ुदा तुम्हारा भला करे, आलू-कोफ़्ता, आलू-बड़िया, आलू समोसा, आलू का रायता, आलू का भरता, आलू क़ीमा...”
हमने रोक कर पूछा, “और स्वीट डिश?”
बोला, “आलू की खीर।” हमने कहा, “भले आदमी, तुमने तो आलू का पहाड़ा सुना दिया। तुम्हारे होटल में कोई ऐसी डिश भी है जिसमें आलू का नाम न आए।” फ़ातिहाना तबस्सुम के साथ फ़रमाया, “क्यों नहीं! पोटेटो कटलेट! हाज़िर करूँ जनाब?”क़िस्सा दर असल ये था कि एक साल पहले मालिक होटल हज़ा ने हेड कांस्टेबल के ओहदे से सुबुकदोश हो कर ज़राअत की तरफ़ तवज्जो फ़रमाई और ज़मीन से भी उन्ही हथकंडों से सोना उगलवाना चाहा। मगर हुआ ये कि आलू की काश्त में पच्चीस साल की ज़हानत से जमा की हुई रिश्वत ही नहीं बल्कि पेंशन और प्रावीडेंट फ़ंड भी डूब गए।ज़मीं खा गई बे ईमां कैसे कैसेपस-अंदाज़ किए हुए आलूओं से होटल के धंदे का डोल डाला। जिन्हें अब उसके बेहतरीन दोस्त भी ताज़ा नहीं कह सकते थे। सुना है बटेर भी उसी ज़माने में पास पड़ोस के खेतों से पकड़ थे।मुकालमा दर मज़म्मत आलू“मिर्ज़ा ये बटेर नामा अपनी जगह, मगर ये सवाल अभी तिश्ना है कि तुम आलू क्यों नहीं खाते।” हमने फिर वही सवाल किया।“नहीं साहिब, आलू खाने से आदमी आलू जैसा हो जाता है। कोई अंग्रेज़ औरत (मिर्ज़ा की आदत है कि तमाम सफ़ेद फ़ाम ग़ैर मुल्कियों को अंग्रेज़ कहते हैं। मसलन अमरीका के अंग्रेज़, जर्मनी के अंग्रेज़, हद ये कि इंग्लिस्तान के अंग्रेज़) जिसे अपना ‘फिगर’ और मुस्तक़बिल ज़रा भी अज़ीज़ है, आलू को छूती तक नहीं। सामने स्वीमिंग पूल में पैर लटकाए ये मेम जो मिस्र का बाज़ार खोले बैठी है, उसे तुम आलू की एक हवाई भी खिला दो तो बंदा इसी हौज़ में डूब मरने को तैयार है। अगर ये काफ़ी में चीनी के चार दाने भी डालती है, या कोई उसे मीठी नज़र से भी देख ले तो इसकी कैलोरीज़ का हिसाब अपनी धोबी की कापी में रखती है।” उन्होंने जवाब दिया। “मिर्ज़ा क्या मेमें भी धोबी की कापी रखती हैं?”“हाँ उनमें की जो कपड़े पहनती हैं, वो रखती हैं।” हमारी तिश्नगी, इल्म बढ़ती देखकर मिर्ज़ा ने आलू की हजो में दलायल-ओ-नज़ाइर का तूमार बांध दिया। जहां कहीं मंतिक़ के टाट में ज़रा सुराख़ भी नज़र आया, वहां मख़मली मिसाल का बड़ा सा पैवंद इस तरह लगाया कि जी चाहता था कुछ और सुराख़ होते।
कहने लगे कर्नल शेख़ कल रात ही यूरोप से लौटे हैं। कह रहे थे यूरोप की और हमारी ख़वातीन में बड़ा फ़र्क़ है। यूरोप में जो लड़की दूर से सत्रह बरस की मालूम होती है वो क़रीब पहुंच कर सत्तर बरस की निकलती है और हमारे हाँ जो ख़ातून दूर से सत्तर बरस की दिखलाई पड़ती है वो नज़दीक आने पर सत्रह बरस की निकलती है! मगर ये वज़ादारी इंग्लिस्तान में ही देखी कि जो उम्र दूर से नज़र आती है वही पास से। चुनांचे कमर कमर तक बालों वाली जो लड़की दूर से उन्नीस साल की नज़र आती है वो पास जाने पर भी उन्नीस ही साल का ‘हिप्पी’ निकलता है, ख़ैर सुनी सुनाई बातों को छोड़ो।
उस मेम का मुक़ाबला अपने हाँ की आलू खोर ख़वातीन से करो। उधर फ़ानुस के नीचे, सुर्ख़ सारी में जो मुहतरमा लेटरबाक्स बनी अकेले अकेले गपा गप बीफ़ स्टिक और आलू उड़ा रही, अमां! गँवारों की तरह उंगली से इशारा मत करो। हाँ हाँ वही, अरे साहिब क्या चीज़ थी, लगता था एक अप्सरा सीधी अजंता के ग़ारों से चली आ रही है और क्या फिगर था। कहते हुए ज़बान सौ-सौ बल खाती है। चलती तो क़दम यूं रखती थी दिन जैसे किसी के फिरते हैं।पहले-पहल मार्च 1951 में देखा था। वो सुबह याद आती है तो कोई दिल पर दस्तक सी देने लगता है और अब? अब तुम्हारी आँखों के सामने है। बारह साल की Go Go Girl गोश्त के अंबार में कहीं खो गई है। इश्क़ और आलू ने इन हॉलों को पहुंचा दिया।हमने कहा, “मारों घुटना फूटे आँख!”
बोले, “अह्ल-ए-ज़बान के मुहावरे उन्ही के ख़िलाफ़ अंधा धुंद इस्तेमाल करने से पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। हुमैरा वो आईडीयल औरत थी जिसके ख़्वाब हर सेहतमंद आदमी देखता है यानी शरीफ़ ख़ानदान, ख़ूबसूरत और आवारा! उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़्रेंच और जर्मन फ़र्राटे से बोलती थी, मगर किसी भी ज़बान में ‘न’ कहने की क़ुदरत नहीं रखती थी। हुस्न और जवानी की बशिर्कत ग़ैरे मालिक थी। ये दोनों अश्या-ए-लतीफ़ जब तबर्रुक हो गईं और पलकों के साये गहरे हो चले तो मारे बाँधे एक अक़द शरई भी किया। मगर एक महीने के अंदर ही दूल्हे ने उरूसी कमरबंद का फंदा गले में डाल कर ख़ुदकुशी कर ली। जा तुझे कश्मकश-ए-अक़द से आज़ाद किया। फिर तो ऐसे कान हुए कि इस बेचारी ने शरई तकल्लुफ़ात से ख़ुद को कभी मुकल्लफ़ नहीं किया। साहिब मर्द का क्या बने, आजकल मर्द ज़िंदगी से उकता जाता है तो शादी कर लेता है और अगर शादीशुदा है तो तलाक़ दे देता है लेकिन औरत ज़ात की बात और है। बदी पे आई हुई औरत जब परेशान या पशेमान होती है तो टी.एस.इलियट के बक़ौल ग्रामोफोन रिकार्ड लगा कर अपने जोड़े को मेकानिकी अंदाज़ से थपथपाते हुए ख़्वाबगाह में बोलाई बोलाई नहीं फिरती बल्कि ग़िज़ा से ग़म ग़लत करती है। हुमैरा ने भी मर्द की बेवफ़ाई का मुक़ाबला अपने मेदे से किया। तुम ख़ुद देख लो। किस रफ़्तार से आलू के क़त्ले क़ाब से प्लेट और प्लेट से पेट में मुंतक़िल कर रही है। बस उसी ने सूरत से बे सूरत कर दिया।हमने उनका वक़्त और अपनी रही सही इज़्ज़त बचाने की ख़ातिर उनकी इस ‘थ्योरी’ से झट इत्तफ़ाक़ कर लिया कि ज़नाना आवारगी की रोक-थाम के लिए अक़द और आलू से बेहतर कोई आला नहीं कि दोनों से बदसूरती और बदसूरती से नेकचलनी ज़ोर पकड़ती है।
उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए हमने कहा, “लेकिन अगर आलू से वाक़ई मोटापा पैदा होता है तो तुम्हारे हक़ में तो उल्टा मुफ़ीद होगा क्योंकि अगर तुम्हारा वज़न सही मान लिया जाये तो मेयारी हिसाब से तुम्हारा क़द तीन फुट होना चाहिए। एक दिन तुम्हीं ने बताया था कि आस्तीन के लिहाज़ से 17 नंबर की क़मीज़ तुम्हें फ़िट आती है और कालर के लिहाज़ से 13 नंबर!”करिश्मे कार्बो हाइड्रेट केउसी साल जून में मिर्ज़ा अपने दफ़्तर में अगाता क्रिस्टी का ताज़ा नॉवेल पढ़ते पढ़ते अचानक बेहोश हो गए। होश आया तो ख़ुद को एक आरामदेह क्लीनिक (Clinic) कंपनी के ख़र्च पर साहिब-ए-फ़राश पाया। उन्हें इस बात से सख़्त मायूसी हुई कि जिस मक़ाम पर उन्हें दिल का शदीद दर्द महसूस हुआ था, दिन उससे बालिश्त भर दूर निकला। डाक्टर ने वहम दूर करने की ग़रज़ से उंगली रखकर बताया कि दिल यहां नहीं, यहां होता है। उसके बाद उन्हें दिल का दर्द दिल ही में महसूस होने लगा।जैसे ही उनके कमरे से ‘मरीज़ से मुलाक़ात मना है’ की तख़्ती हटी, हम ज़िनिया का गुलदस्ता लेकर अयादत को पहुंचे। दोनों एक दूसरे की शक्ल देख देखकर ख़ूब रोए। नर्स ने आकर दोनों को चुप कराया और हमें अलाहदा ले जा कर मुतनब्बा किया कि इस अस्पताल में बीमारपुर्सी करने वालों को रोना और कराहना मना है। हमने फ़ौरन ख़ुद पर फ़र्माइशी बशाशत तारी कर के मिर्ज़ा को हिरासाँ होने से मना किया और तलक़ीन की कि मरीज़ को अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, वो चाहे तो तिनके में जान डाल दे। हमारी नसीहत का ख़ातिर-ख़्वाह बल्कि उससे भी ज़्यादा असर हुआ।
“तुम क्यों रोते हो पगले?” हमने उनकी पेशानी पर हाथ रखते हुए कहा।“यूंही ख़्याल आ गया कि अगर तुम मर गए तो मेरी अयादत को कौन आया करेगा!” मिर्ज़ा ने अपने आँसू नर्स के रूमाल में महफ़ूज़ करते हुए वजह रिक़्क़त बयान की।मर्ज़ की असल वजह डाक्टरों के नज़दीक कसरत-ए-अफ़्क़ार थी, जिसे मिर्ज़ा की ज़बान में क़ादिर-उल-बयान ने कसरत कार बना दिया। ख़ैर, इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं थी। ताज्जुब की बात तो ये थी कि मिर्ज़ा चाय के साथ आलू के ‘चिप्स’ उड़ा रहे थे।
हमने कहा, “मिर्ज़ा, आज तुम रंगे हाथों पकड़े गए।”
बोले (और ऐसी आवाज़ में बोले गोया किसी अंधे कुँवें के पेंदे से बोल रहे हैं।) डाक्टर कहते हैं, तुम्हारा वज़न बहुत कम है। तुम्हें आलू और ऐसी चीज़ें ख़ूब खानी चाहिऐं जिनमें ‘स्टार्च” और कार्बो हाइड्रेट की इफ़रात हो। साहिब आलू एक नेअमत है, कम अज़ कम साईंस की रू से!”
हमने कहा, “तो फिर दबा दब आलू खा कर ही सेहतयाब हो जाओ।”
फ़रमाया, “सेहतयाब तो मुझे वैसे भी होना ही पड़ेगा। इसलिए कि ये नर्सें इस क़दर बदसूरत हैं कि कोई आदमी जो अपने मुँह पर आँखें रखता है, यहां ज़्यादा अर्से पड़ा नहीं रह सकता!”वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतेंक्लीनिक से निकलते ही मिर्ज़ा ने अपनी तोपों का रुख़ फेर दिया। ख़ूगर हजो के शब-ओ-रोज़ अब आलू की तारीफ़-ओ-तौसीफ़ में बसर होने लगे। एक वक़्त था कि वियतनाम पर अमरीकी बमबारी की ख़बरें पढ़ कर मिर्ज़ा पछतावा करते कि कोलंबस ने अमरीका दरयाफ़्त कर के बड़ी नादानी की। मगर अब प्यार में आते तो आलू की गदराई हुई गोलाइयों पर हाथ फेरते हुए फ़रमाते, “साहिब! कोलंबस जहन्नुम में नहीं जाएगा। उसे वापस अमरीका भेज दिया जाएगा। मुहज़्ज़ब दुनिया पर अमरीका के दो एहसान हैं:तंबाकू और आलू। सो तंबाकू का बेड़ा तो सरतान ने ग़र्क़ कर दिया।मगर आलू का मुस्तक़बिल निहायत शानदार है। जो मुल़्क जितना ग़ुर्बत ज़दा होगा, उतना ही आलू और मज़हब का चलन ज़्यादा होगा।” और कभी ऐसा भी होता कि हरीफ़ ज़रीफ़ साईंसी हथियारों से ज़ेर नहीं हुआ तो शायरी के मार से वहीं ढेर कर देते। “साहिब, जूँ-जूँ वक़्त गुज़रता है याददाश्त कमज़ोर होती जाती है। पहले अपनी पैदाइश के दिन ज़ेहन से उतरा। फिर महीना और अब तो सन् भी याद नहीं रहता, बेगम या किसी बद-ख़्वाह से पूछना पड़ता है। अक्सर तुम्हारे लतीफ़े तुम्हें ही सुनाने बैठ जाता हूँ। वो तो जब तुम पेट पकड़ पकड़ कर हँसने लगते हो तो शक गुज़रता है कि लतीफ़ा तुम्हारा ही होगा।
बेगम अक्सर कहती हैं कि कॉकटेल पार्टीयों और डांस में तुम्हें ये तक याद नहीं रहता कि तुम्हारी शादी हो चुकी है ग़रज़ कि हाफ़िज़ा बिल्कुल चौपट है। अब ये आलू का एजाज़ नहीं तो और क्या है कि आज भी किसी बच्चे के हाथ में भू बल में सेंका हुआ आलू नज़र आजाए तो उसकी मानूस महक से बचपन का एक एक वाक़िया ज़ेहन में ताज़ा हो जाता है। मैं टकटकी बांध कर उसे देखता हूँ। उससे फूटती हुई सोंधी भाप के परे एक भूली-बिसरी सूरत उभरती है।
गर्द-आलूद बालों के पीछे शरारत से रोशन आँखें। कुरता बटनों से बेनयाज़, गले में गुलेल, नाख़ुन दाँतों से कुतरे हुए। पतंग उड़ाने वाली उंगली पर डोर की ख़ूनआलूद लकीर, बैरी समय हौले हौले अपनी केंचुलियां उतारता चला जाता है और मैं नंगे-पाँव तितलियों के पीछे दौड़ता, रंग बिरंगे बादलों में रेज़गारी के पहाड़, परीयों और आग उगलते अज़दहों को बनते बिगड़ते देखता, खड़ा रह जाता हूँ।” “यहां तक कि आलू ख़त्म हो जाता है।” हमने साबुन के बुलबुले पर फूंक मारी, सँभले। गर्दिश-ए-अय्याम को अपने बचपन के पीछे दौड़ाते दौड़ाते लगाम खींची। और गाली देने के लिए गला साफ़ करते हुए फ़रमाया, “ख़ुदा जाने हुकूमत आलू को बज़ोर-ए-क़ानून क़ौमी ग़िज़ा बनाने से क्यों डरती है। सस्ता इतना कि आज तक किसी सेठ को इसमें मिलावट करने का ख़्याल नहीं आया। स्केंडल की तरह लज़ीज़ और ज़ूद-हज़्म, विटामिन से भरपूर, ख़ुश-ज़ाएक़ा, सूफ़ियाना रंग, छिलका ज़नाना लिबास की तरह, यानी बरा-ए-नाम।”“साफ़ इधर से नज़र आता है उधर का पहलू।”दस्त ख़ुद दहान ख़ुदमिर्ज़ा पर अब ये झक सवार थी कि अगर संदल का घिसना और लगाना दर्द-ए-सर के लिए मुफ़ीद है तो उसे उगाना कहीं ज़्यादा मुफ़ीद होना चाहिए। हिक्मत-ओ-ज़राअत की जिन पुरख़ार राहों को मस्ताना तय कर के वो इस नतीजे पर पहुंचे, उनका इआदा किया जाये तो तिब्ब पर एक पूरी किताब मुरत्तब हो सकती है। अज़ बस कि हम हकीमों की लगी लगाई रोज़ी पे हाथ डालना नहीं चाहते, इसलिए दो तीन चिनगारियां छोड़कर दूर खड़े हो जाऐंगे।एक दिन हमसे पूछा, ”बचपन में खट मिट्ठे बेर, मेरा मतलब है झरबेरी के बेर खाए हैं?”
अर्ज़ किया, “जी हाँ, हज़ार दफ़ा। और उतनी ही दफ़ा खांसी में मुब्तला हुआ हूँ।”
फ़रमाया, “बस यही फ़र्क़ है, ख़रीद के खाने में और अपने हाथ से तोड़ के खाने में। तजुर्बे की बात बताता हूँ। बेर तोड़ते वक़्त उंगली में कांटा लग जाये और ख़ून की बूँद पर पर थरथराने लगे तो आस-पास की झाड़ियों के तमाम बेर मीठे हो जाते हैं!”“साइंटिफिक दिमाग़ में ये बात नहीं आती।” हमने कहा।हमारा ये कहना था कि ज़्यादा उबले हुए आलू की तरह तड़खते बिखरते चले गए। कहने लगे, “साहिब, बाज़े हकीम ये करते हैं कि जिसका मेदा कमज़ोर हो उसे ओझड़ी खिलाते हैं। जिसके गुर्दों का फे़अल दुरुस्त न हो उसे गुर्दे और जो ज़ोफ़-ए- जिगर में मुब्तला हो उसे कलेजी। अगर मैं हकीम होता तो तुम्हें मग़ज़ ही मग़ज़ खिलाता।” राक़िम उल-हरूफ़ के उज़ू ज़ईफ़ की निशानदेही करने के बाद इरशाद हुआ, “अब आलू ख़ुद काश्त करने की साइंटिफिक वजह भी सुन लो। पिछले साल उतरती बरसात की बात है, मैं टोबा टेक सिंह में काले तीतर की तलाश में कच्चे में बहुत दूर निकल गया, मगर एक तीतर नज़र न आया, जिसकी वजह गाईड ने ये बताई कि शिकार के लिए आपके पास डिप्टी कमिश्नर का परमिट नहीं है। वापसी में रात हो गई और हमारी1945 मॉडल जीप पर दमे का दौरा पड़ा।
चंद लम्हों बाद वो ज़ईफ़ा तो एक गढ़े में आख़री हिचकी लेकर ख़ामोश हो गई मगर क़फ़स-ए-उंसरी में हमारे ताएर-ए-रूह को परवाज़ करता छोड़ गई। हम स्टेयरिंग पर हाथ रखे दिल ही दिल में ख़ुदा का शुक्र अदा कर रहे थे कि रहमत-ए-एज़दी से जीप गढ़े में गिरी वर्ना गढ़े की जगह कुँआं होता तो उस वक़्त ख़ुदा का शुक्र कौन अदा करता?
ना कभी जनाज़ा उठता, ना कहीं मज़ार होता हमारे क़र्ज़-ख़्वाहों पर क्या गुज़रती? हमारे साथ रक़म के डूबने पर उन्हें कैसे सब्र आता कि अभी तो हमारे तमस्सुक की रोशनाई भी ख़ुश्क नहीं हुई थी? हम अभी उनके और उनके छोटे बच्चों के सरों पर हाथ फेर ही रहे थे कि एक किसान बकरी का नौज़ाईदा बच्चा गर्दन पर मफ़लर की तरह डाले उधर से गुज़रा। हमने आवाज़ देकर बुलाया।
अभी हम इतनी ही तमहीद बाँधने पाए थे कि हम कराची से आए हैं और काले तीतर की तलाश में थे कि वो गढ़े की तरफ़ इशारा करके कहने लगा कि तहसील टोबा टेक सिंह में तीतर पानी में नहीं रहते। हमारे गाईड ने हमारी फ़ौरी ज़रूरियात की तर्जुमानी की तो वो ऐसा पसीजा कि अपनी बैलगाड़ी लाने और उसे जीप में जोत कर अपने घर ले जाने के लिए इसरार करने लगा और वो भी बिला मुआवज़ा, साहिब अंधा क्या चाहे?” “दो आँखें!” हमने झट लुक़मा दिया।“ग़लत बिल्कुल ग़लत, अगर उसकी अक़ल भी बीनाई के साथ ज़ाइल नहीं हुई है तो अंधा दो आँखें नहीं चाहता, एक लाठी चाहता है!” मिर्ज़ा ने मुहावरे की भी इस्लाह फ़रमा दी।हम हुँकारा भरते रहे, कहानी जारी रही, “थोड़ी देर बाद वो बैलगाड़ी ले आया जिसके बैल अपनी जवानी को बहुत पीछे छोड़ आए थे। अदवान की रस्सी से जीप बाँधते हुए उसने हमें बैलगाड़ी में अपने पहलू में अगली सेट की पेशकश की और डेढ़ दो मील दूर किसी मौहूम नुक़्ते की तरफ़ इशारा करते हुए तसल्ली देने लगा, “ओ जेड़ी, नवीं लालटेन बलदी पई ए ना, ओही मेरा घार वे।” (वो जहां नई लालटेन जल रही है ना वही मेरा घर है।)घर पहुंचते ही उसने अपनी पगड़ी उतार कर चारपाई के सीरवे वाले पाए को पहना दी। मुँह पर पानी के छपके दिए और गीले हाथ सफ़ेद बकरी की पीठ से पोंछे। बरसात की चांदनी में उसके कुरते पर बड़ा सा पैवंद दूर से नज़र आ रहा था और जब थूनी पर लटकी हुई नई लालतेन की लौ भड़की तो उस पैवंद में लगा हुआ एक और पैवंद भी नज़र आने लगा जिसके टाँके अभी उसकी मुस्कुराहट की तरह उजले थे।
उसकी घर वाली ने खड़ी चारपाई पर खाना चुन कर ठंडे मीठे पानी के दो धात के गिलास पट्टी पर बान छिदरा कर के जमा दिए। मेज़बान के शदीद इसरार और भूक के शदीद तर तक़ाज़े से मजबूर हो कर जो हमने ख़ुश्क चिनाई शुरू की है तो यक़ीन मानो पेट भर गया मगर जी नहीं भरा। राल निगलते हुए हमने पूछा, “चौधरी! इससे मज़ेदार आलू का साग हमने आज तक नहीं खाया, क्या तरकीब है पकाने की?”बोला, “बादशाहो, पहले ते इक कल्ले ज़मीन विच पंच मन अमरीका दी खाद पाओ। फिर... (पहले एक एकड़ ज़मीन में पाँच मन अमरीकी खाद डालो फिर (उस ज़माने में कीमियाई खाद अमरीका से आती थी)क़िस्सा आलू काश्त काबात अगर अब भी गले से नहीं उतरी तो “ख़ुद उगाओ ख़ुद खाओ” सिलसिले की तीसरे दास्तान सुनिए जिसका अज़ाब-सवाब मिर्ज़ा की गर्दन पर है कि वही उसके फ़िरदौसी हैं और वही रुस्तम। दास्तान का आग़ाज़ यूं होता है,“साहिब, बाज़ार से सडे-बुसे आलू ख़रीद कर खाने से तो ये बेहतर है कि आदमी चने भसकता फिरे। परसों हम ख़ुद आलू ख़रीदने गए, शबराती की दुकान से। अरे साहिब! वही अपना शबराती, जिसने चौदह-पंद्रह साल से वो साइनबोर्ड लगा रखा है,मालिक ईं दुकान शबराती मुहाजिरीनअगर कोई दावा कुंद बातिल शुदबमुक़ाम मौज़ा काठ, अक़ब जामा मस्जिद कलांपोस्ट ऑफ़िस क़स्बा बागपत, ज़िला मेरठहाल मुक़ीम करांचीहमने एक आलू दिखाते हुए कहा, “मियां शबराती हाल मुक़ीम करांची, तुम्हारे आलू तो पिलपिले हैं, ख़राब लगते हैं।”
बोला, “बाऊ जी! ख़राब निकलें तो काला नाग(उसके गधे का नाम) के मूत से मूंछ मुंडवा देना। दर-हक़ीक़त में ये पहाड़ी आलू हैं।”
हमने कहा, “हमें तो कराची से पाँच सौ मील तक कोई पहाड़ नक़्शे में नज़र नहीं आता।”
बोला, “बाऊजी, तुम्हारे नक़्शे में और कौन सी फल फलारी करांची में नजर आवे है? ये रुपये छटांक का सांची पान जो तुम्हारे ग़ुलाम के कल्ले में बताशे की तरियों घुल रहा है, मक़ाम बंगाल से आ रिया है। यहां क्या दम दुरूद रखा है। हालीयत तो ये है जी! करांची में मिट्टी तलक मलेर से आवे है। किस वास्ते कि उसमें ढाका से मंगा के घांस लगावेंगे। जवानी क़सम बाऊ जी, पिशावर के चौक यादगार में मुर्ग़ा अज़ान देवे है तो कहीं जा के करांची वालों को सुबह अंडा नसीब होवे है!”और एक मर्द ग़ैरत मंद ने चमन-ज़ार कराची के दिल यानी हाऊसिंग सोसाइटी में आलू की काश्त शुरू कर दी। अगरचे सर-ए-दस्त पाँच मन अमरीकी खाद का इंतज़ाम न हो सका, लेकिन मिर्ज़ा का जोश-ए-जुनूँ उन्हें इस मुक़ाम पर पहुंचा चुका था जहां खाद तो खाद, वो बग़ैर ज़मीन के भी काश्त करने का जिगरा रखते थे!मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग और खेती बाड़ी। हमारा ख़्याल है कि सारा खेत एयर कंडीशन कर दिया जाये और ट्रैक्टर में एक रॉकिंग चेयर(झूला कुर्सी) डाल दी जाये तो मिर्ज़ा शायद दो-चार घंटे के लिए काश्तकारी का पेशा इख़्तियार करलें, जिसके बारे में उनका मब्लग़-ए-इल्म बस इस क़दर है कि उन्होंने सिनेमा के पर्दे पर क्लीन शेव एक्टरों को छाती पर मस्नूई बाल चिपकाए, स्टूडियो के सूरज की धूप में, सिगरेट की पुनी चढ़ी हुई दरांतियों से बाजरे के खेत में से मक्का के भुट्टे काटते देखा है। यहां ये बताना ग़ालिबन बेमहल न होगा कि इससे चंद साल पेशतर मिर्ज़ा बाग़बानी का एक इंतहाई नादिर और उतना ही नाकाम तजुर्बा करके हमें एक मज़मून का ख़ाम मवाद मुहय्या कर चुके थे। उन्हें एक दिन अपने कोट का नंगा कालर देखकर दफ़अतन इलक़ा हुआ कि होने को तो घर में अल्लाह का दिया सब कुछ है सिवाए रुपये के। लेकिन अगर बाग़ में गुलाब के गमले नहीं तो जीना फ़ुज़ूल है। उन्हें ज़िंदगी में अचानक एक ज़बरदस्त ख़ला महसूस होने लगा जिसे सिर्फ़ अमरीकी खाद से पुर किया जा सकता था।अब जो आलू की काश्त का सौदा सर में समाया तो डेढ़ दो हफ़्ते फ़क़त इस मौज़ू पर रिसर्च होती रही कि आलू बुख़ारे की तरह आलू के भी बीज होते हैं, या क्वेटा के गुलाब की तरह आलू की भी टहनी काट कर साफ़ सुथरे गमले में गाड़ दी जाती है। नीज़ आलू पटसन की मानिंद घुटनों घुटनों पानी मांगता है या अखरोट की तरह बग़ैर मेहनत के पुश्तहा पुश्त तक फल देता रहेगा।
दौरान-ए-तहक़ीक़ एक शक कहीं से ये भी निकल आई कि बैंगन की तरह आलू भी डला डाल पे लटकेंगे या तुरई की बेल की तरह पड़ोसी की दीवार पर पड़े रहेंगे। प्रोफ़ेसर अबदुल क़ुद्दूस ने तो ये शोशा भी उठाया कि अगर रफ़ा शर की ख़ातिर ये मान लिया जाये कि आलू वाक़ई ज़मीन से उगते हैं तो डंठल का निशान कैसे मिटाया जाता है?छुपा दस्त हिम्मत में दस्त-ए-क़ज़ा हैफिर क्या था। क्वेटा से बज़रिये पी आई ए सफ़ेद गुलाब की क़लमें मँगाई गईं। गमलों को खौलते पानी और फिनाइल से “डिस इन्फेक्ट” किया गया। फिर क्वेटा के नाज़ुक-ओ-नायाब गुलाब को कराची के दीमक और कीड़ों से महफ़ूज़ रखने के लिए ओबाश बकरी की मेंगनी की गर्म खाद में इतनी अमरीकी खाद और अमरीकी खाद में हम वज़न डी डी टी पाउडर मिलाया गया। उबले हुए पानी से सुबह-ओ-शाम सिंचाई की गई और ये वाक़िया है कि उन गमलों में कभी कोई कीड़ा नज़र नहीं आया और न गुलाब!प्रोफ़ेसर क़ाज़ी अब्दुल क़ुद्दूस कुछ ग़लत तो नहीं कहते कि मिर्ज़ा हमाक़त भी करते हैं तो इस क़दर “ओरीजनल” कि बख़ुदा बिल्कुल इल्हामी मालूम होती है।पायानेकार मिर्ज़ा ने आलू की काश्त के लिए ज़मीन यानी अपना “लॉन”(जिसकी अफ़्रीक़ी घास की हरियाली ऐसी थी कि सिगरेट की राख झाड़ते हुए दिल दुखता था) तैयार किया। उस ज़राअती तजुर्बे के दौरान जहां-जहां अक़ल महव-ए-तमाशाए लब-ए-बाम रही, वहां जोश-ए-नमरूद बेख़तर गुलज़ार-ए-ख़लील में कूद पड़ा। दफ़्तर के चपरासियों, अपने पालतू ख़रगोश और महल्ले के लौंडे लाड़ियों की मदद से दो ही दिन में सारा लॉन खोद फेंका। बल्कि उसके बाद भी ये अमल जारी रखा। यहां तक कि दूसरी मंज़िल के किरायादारों ने हाथ-पांव जोड़ के खुदाई रुकवाई, इसलिए कि मकान की नींव नज़र आने लगी थी।इस की शबों का गुदाज़हमें डेढ़ महीने के लिए काम से ढाका जाना पड़ा और मिर्ज़ा से मुलाक़ातों का सिलसिला मौक़ूफ़ हो गया। ख़त-ओ-किताबत का मिर्ज़ा को दिमाग़ नहीं। जैसे ही हम वापस आए, अनन्नास और मुंशी गंज के केलों से लदे-फंदे मिर्ज़ा के हाँ पहुंचे। हमने कहा, “अस्सलामु अलैकुम!”
जवाब मिला, “फल अंदर पहुँचवा दो। वाअलैकुम अस्सलाम!” ग़ौर से उनकी सूरत देखी तो दिल पे चोट सी लगी।“ये क्या हाल बना लिया तुमने?”“हमें जी भर के देख लो। फिर इस सूरत को तरसोगे। इशतिहा ख़त्म, दवाओं पर गुज़ारा है। दिन-भर में तीन अंगूर खा पाता हूँ, वो भी छिलका उतार के। खाने के नाम से हौल उठता है, दिल बैठा जाता है। हर वक़्त एक बे कली सी रहती है। हर चेहरा उदास उदास, हर शय धुआँ धुआँ, ये हो नुक्ता सन्नाटा, ये चैत की उदास चांदनी,ये...” “मिर्ज़ा हम तुम्हें रोमैंटिक होने से रोक तो नहीं सकते लेकिन ये महीना चैत का नहीं है।” “चैत न सही, चैत जैसा ज़रूर है, ज़ालिम। तुम तो एक हिंदू लड़की से दिल भी लगा चुके हो, तुम्हीं बताओ, ये कौन से महीने का चांद है?” मिर्ज़ा ने सवाल किया।“इसी महीने का मालूम होता है।” हमने झिजकते हुए जवाब दिया।“हमें भी ऐसा ही लगता है। साहिब अजीब आलम है, काम में ज़रा जी नहीं लगता और बेकारी से भी वहशत होती है। ज़ेहन परागंदा बल्कि सच पूछो तो महज़ गंदा। तारों भरे आसमान के नीचे रात रात-भर आँखें फाड़े तुम्हारी हिमाक़तें गिनता रहता हूँ। तन्हाई से दिल घबराता है और लोगों से मिलता हूँ तो जी चाहता है मुँह नोच लूं, और साहिब!एक दो का ज़िक्र किया, सारे के सारे नोच लूं।”“मिर्ज़ा हो न हो,ये इश्क़ के आसार हैं।” “बजा, लेकिन अगर साहिब मुआमले पर चालीस महावटें पड़ चुकी हों, तो ये आसार इश्क़ के नहीं ‘अल्सर’ के हैं। खाना खाते ही महसूस होता है गोया किसी ने हलक़ से लेकर मेदे तक तेज़ाब की फुरेरी फेर दी है। इधर खाया, उधर पेट फूल कर मशकीज़ा हुआ, हंसी का रुख़ भी अंदर की तरफ़ हो गया है। सारा फ़ुतूर आलू का है। मेदे में एसिड बहुत बनने लगा है ‘पेप्टिक अल्स’र हो गया है।” उनकी आँखें डबडबाईं। “इसमें हिरासाँ होने की क्या बात है। आजकल किसी को 'हार्ट-अटैक,या अल्सर’ न हो तो लोग उस पर तरस खाने लगते हैं कि शायद बेचारा किसी ज़िम्मेदार ओहदे पर फ़ाइज़ नहीं है! मगर तुम तो मुलाज़मत को जूते की नोक पर रखते हो। अपने ‘बॉस’ से टांग पर टांग रखकर बात करते हो। फिर ये कैसे हुआ?
वक़्त पर सोते हो,वक़्त पर उठते हो। दादा के वक़्तों की चांदी की पतीली में उबाले बग़ैर पानी नहीं पीते। वुज़ू भी पानी में ‘लिस्ट्रीन’ मिला कर करते हो, जिसमें 26 फ़ीसद अलकोहल होता है। हालात हाज़रा से ख़ुद को बे-ख़बर रखते हो। बातों के इलावा किसी चीज़ में तुरशी को रवा नहीं रखते। तेल भी तुम नहीं खाते। दस साल से तो हम ख़ुद देख रहे हैं, मुंटगुमरी का ख़ालिस दानेदार घी खा रहे हो।” हमने कहा।“तुम्हें यक़ीन नहीं आएगा, ये सब उसी मनहूस का फ़ुतूर है। अब की दफ़ा जो सोने के कुश्ता से ज़्यादा ताक़त बख़्श घी, का सर बमुहर कनस्तर अपने हाथ से अँगेठी पर तपाया तो मालूम है तह में क्या निकला? तीन तीन उंगल आलू की दानेदार लुगदी, जभी तो मैं कहूं कि मेरा बनियान तो तंग हो गया, मगर वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा!” मिर्ज़ा ने आख़िर अपने दस साला मरज़ की जड़ पकड़ ली, जो ज़िला मुंटगुमरी तक फैली हुई थी।क्या असीरी है, क्या रिहाई हैपहले मिर्ज़ा को दर्द ज़रा बर्दाश्त नहीं थी। हमारे सामने की बात है, पहली दफ़ा पेट में दर्द हुआ तो डाक्टर ने मार्फिया का इंजेक्शन तैयार किया। मगर मिर्ज़ा ने घिगिया कर मिन्नतें कीं कि उन्हें पहले क्लोरोफ़ार्म सुंघा दिया जाये ताकि इंजेक्शन की तकलीफ़ महसूस न हो लेकिन अब अपनी बीमारी पर इस तरह इतराने लगे थे जैसे अक्सर ओछे अपनी तंदुरुस्ती पर अकड़ते हैं।
हमें उनकी बीमारी से इतनी तशवीश नहीं हुई जितनी इस बात से कि उन्हें अपने ही नहीं पराए मरज़ में भी उतनी ही लज़्ज़त महसूस होने लगी थी। भांत भांत की बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों से इस तरह कुरेद कुरेद कर मुतअद्दी तफ़सीलात पूछते कि रात तक उनके सारे मरज़ अपना लेते।
इस हद तक बुख़ार किसी को चढ़ता, सर सामी बातें वो करते। इस हमदर्दाना तर्ज़-ए-अयादत से मिर्ज़ा ने ख़ुद को ज़च्चगी के सिवा हर क़िस्म की तकलीफ़ में मुब्तला कर लिया। घर या दफ़्तर की क़ैद नहीं, न अपने-बेगाने की तख़सीस, हर मुलाक़ाती को अपनी आंतों के नाक़िस फे़’ल से आगाह करते और इस सीमाब-सिफ़त रियाही दर्द का लफ़्ज़ी ग्राफ़ बनाते जो मुसाफ़ा करते वक़्त नफ़ख़-ओ-क़राक़िर का मुहर्रिक था। फिर दाएं आँख के पपोटे में ‘करंट’ मारता, मुतवर्रम जिगरह को छेदता, टली हुई नाफ़ की तरफ़ बढ़ने लगा था कि पिछले-पहर अचानक पल्टा और पलट कर दिल में बुरे बुरे ख़्याल पैदा करने लगा और फिर मिर्ज़ा हर बुरे ख़्याल को इस तरह खोल कर बयान करते किमैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है।जिन लोगों ने मिर्ज़ा को पहले नहीं देखा था वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि ये मर्द बीमार जो फ़ाइलों पर सर झुकाए, ‘अल्सर’ की टपक मिटाने के लिए हर दूसरे घंटे एक गिलास दूध मुँह बना कर पी लेता है, ये चार महीने क़ब्ल कोफ़्ते में हरी मिर्च भरवा कर खाता था और उससे भी जी नहीं भरता तो शाम को यही कोफ़्ता हरी मिर्च में भरवा देता था।
ये नीम जाँ जो बे मिर्च मसाले के रातिब को ‘इंग्लिश फ़ूड’ कह कर सब्र-ओ-शुक्र के साथ खा रहा है, ये वही चटोरा है जो चार महीने पहले ये बता सकता था कि सुबह सात बजे से लेकर रात के नौ बजे तक कराची में किस ‘स्वीट मर्चेंट’ की कढ़ाई से उतरती गर्म जलेबी मिल सकती है। हाऊसिंग सोसाइटी के कौन से चीनी रेस्तोरां में तले हुए झींगे खाने चाहिऐं जिनका चौगुना बिल बनाते वक़्त मालिक रेस्तोरां की बेटी इस तरह मुस्कुराती है कि बख़ुदा रुपया हाथ का मैल मालूम होता है।
उन्हें न सिर्फ़ ये पता था कि लाहौर में जे़वरात की कौन सी दुकान में निहायत सुबुक ‘हीरा-तराश’ कलाइयाँ देखने को मिलती हैं, बल्कि ये भी मालूम था कि मज़ंग में तिक्का कबाब की वो कौन सी दुकान है जिसका हेड ऑफ़िस गुजरांवाला में है और ये भी कि कड़कड़ाते जाड़ों में रात के दो बजे लाल कुरती की किस पान की दुकान पर पिंडी के मनचले तरह तरह के पानों से ज़्यादा उनके रसीले नामों के मज़े लूटने आते हैं।
क़िस्सा-ख़्वानी के किस मुछ्छैल हलवाई की दुकान से काली गुलाब जामुन और नाज़िम आबाद की कौन सी चौरंगी के क़रीब गुलाब में बसा हुआ क़ला क़ंद क़र्ज़ पर मिल सकता है। (ये मुफ़ीद मतलब मालूमात मिर्ज़ा के मुल्कगीर चटोरपन का निचोड़ हैं। उन्होंने सारी उम्र किया ही क्या है। अपने दाँतों से अपनी क़ब्र खोदी है। इत्तिलाअन अर्ज़ है कि मिर्ज़ा नक़द पैसे दे कर मिठाई ख़रीदना फुज़ूलखर्ची समझते हैं) ।
भला कोई कैसे यक़ीन कर लेता कि ये आलू और ‘कार्बो हाइड्रेट’ का शिकार वही है जिसने कल तक मन भाते खानों के कैसे कैसे अलबेले जोड़े बना रखे थे।खड़े मसाले के पसंदे और बेसनी रोटी, क़ीमा भरे करेले और घी में तर तराते पराठे, मद्रासी बिरयानी और पारसी कोफ़्ते (वो भी एक लखनवी पड़ोसन के हाथ के) चुपड़ी रोटी और उरद की फुरेरी दाल, भिंडी और भिंडी!(भिंडी के साथ मिर्ज़ा किसी और चीज़ को शामिल करने के रवादार नहीं।)मिर्ज़ा को खाने का ऐसा हौका है कि एक मुँह उन्हें हमेशा नाकाफ़ी मालूम होता है उनके नदीदे पन को देखकर एक दफ़ा प्रोफ़ेसर क़ाज़ी अब्दुल क़ुद्दूस ने कहा था, “मिर्ज़ा तुम्हारा हाल गिरगिट जैसा है। उसकी ज़बान की लंबाई उसके जिस्म की आधी होती है!” मिर्ज़ा की उदास आँखें एक दम मुस्कुरा उठीं।
कहने लगे, “साहिब, ख़ुदा ने एक पार-ए-गोश्त को जाने किस लज़्ज़त से हमकनार कर दिया। अगर सारा बदन उस लज़्ज़त से आश्ना हो जाता तो इंसान उसकी ताब न लाता। ज़मीन की छाती फट जाती!”मिर्ज़ा पाँच छः हफ़्ते में पलंग को लात मार कर खड़े हो गए। हम तो उसे उनकी क़ुव्वत-ए-इरादी की करामात ही कहेंगे, हालाँकि वो ख़ुद कुछ और वजह बताते थे। एक दिन उनके मेदे से ख़ून कट कट कर आने लगा। हमें चश्म-ए-पुरआब देखा तो ढारस देने लगे, “में मुसलमान हूँ। जन्नत का भी क़ाइल हूँ, मगर मुझे वहां जाने की जल्दी नहीं है। मैं मौत से नहीं डरता, मगर मैं अभी मर नहीं सकता। मैं अभी मरना नहीं चाहता। इसलिए कि अव्वल तो तुम मेरी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। दोम, मैं पहले मर गया तो तुम मुझ पर मज़मून लिख दोगे!”
ख़ुदा बेहतर जानता है कि वो ख़ौफ़-ए-ख़ाका से सेहतयाब हुए या बक़ौल शख़से मुर्ग़ी के ग़ुस्ल-ए-मय्यत के पानी से जिसे वो चिकन सूप कह कर नोश-ए-जान फ़रमा रहे थे।
बहरहाल, बीमारी जैसे आई थी, उसी तरह चली गई। फ़ायदा ये हुआ कि आलू से जो बेज़ारी पहले बिला वजह थी, अब उसकी निहायत माक़ूल वजह हाथ आ गई और ये सरासर मिर्ज़ा की अख़लाक़ी फ़तह थी।मरज़ अलहमदु लिल्लाह दूर हो चुका था। परहेज़ अलबत्ता जारी था। वो इस तरह कि पहले मिर्ज़ा दोपहर के खाने के बाद आध सेर जलेबी अकेले खा जाते थे लेकिन अब डाक्टरों ने मीठा बंद कर दिया था। लिहाज़ा आध सेर इमरती पर इकतिफ़ा करते थे।आलू का मुँह काला, भिंडी बोल बालाजैसे ही मिर्ज़ा की सेहत और तबीयत मामूल पर आई, बग़दादी जिमखाना में यार लोगों ने शायान-ए-शान पैमाने पर ग़ुस्ल-ए-सेहत के जश्न का एहतिमाम किया। इस्तिक़बालिया कमेटी ने फ़ैसला किया कि घिसे पिटे डिनर-डांस के बजाय फैंसी ड्रैस बाल का एहतिमाम किया जाये ताकि एक दूसरे पर हँसने का मौक़ा मिले।
मेहमान-ए-खुसूसी तक ये भनक पहुंची तो उन्होंने हमारी ज़बानी कहला भेजा कि नए मज़हकाख़ेज़ लिबास सिलवाने की चंदाँ ज़रूरत नहीं। मेंबरान और उनकी बेगमात अगर ईमानदारी से वही कपड़े पहने पहने जिमखाना चले आएं, जो वो उमूमन घर में पहने बैठे रहते हैं तो मंशा पूरा हो जाएगा।रक़्स के लिए अलबत्ता एक कड़ी शर्त मिर्ज़ा ने ये लगा दी कि हर मेंबर सिर्फ़ अपनी बीवी के साथ रक़्स करेगा, मगर इस लपक और हुमक से गोया वो उसकी बीवी नहीं है।
जश्न की रात जिमखाना को झंडियों और भिंडियों से दुल्हन बनाया गया। सात कोर्स के डिनर से पहले रूई और काग़ज़ से बने हुए एक क़द-ए-आदम आलू की अर्थी निकाली गई, जिस पर मिर्ज़ा ने अपने हाथ से ब्रांडी छिड़क कर माचिस दिखाई और सरगबाशी के 'डिम्पल' पर गल्फ़ क्लब मार के क्रिया करम किया। डिनर के बाद मिर्ज़ा पर टायलट पेपर के फूल बरसाए गए और कच्ची कच्ची भिंडियों में तौला गया जिन पर अभी ठीक से सुनहरी रोवां भी नहीं निकला था। फिर ये भिंडियां मुस्तहक़्क़ीन यानी मेदे के लखपती मरीज़ों में तक़सीम कर दी गईं।
शेम्पेन से महकते हुए बाल रुम में गुब्बारे छोड़े गए। ख़ाली बोतलों की क़ीमत का अतीया एक यतीमख़ाने को देने का एलान किया गया और ग़ुस्ल-ए-सेहत की ख़ुशी में कार्ड रुम वालों ने जुए के अगले-पिछले सारे कर्जे़ माफ़ कर दिए।मिर्ज़ा बात बे बात पर मुस्कुरा रहे थे। तीसरा रक़्स ख़त्म होते ही हम अपनी कोहनियों से रास्ता बनाते हुए हम उन तक पहुंचे। वो उस लम्हे एक बड़े गुब्बारे में जलते हुए सिगरेट से सुराख़ करने चले थे कि हमने उसका ज़िक्र छेड़ दिया जिसकी जनाब में कल तक गुस्ताख़ि-ए-फ़रिश्ता पसंद न थी।
“मिर्ज़ा, आलू अगर इतना ही मुज़िर है तो इंगलैंड में इस क़दर मक़बूल क्यों है? एक अंग्रेज़ औसतन दस औंस आलू यौमिया खा जाता है। यानी साल में साढे़ पाँच मन, सुन रहे हो, साढे़ पाँच मन!”
बोले, “साहिब, अंग्रेज़ की क्या बात है, उसकी मुफ़लिसी से भी एक शान टपकती है। वो पिटता भी है तो एक हेकड़ी के साथ लन युतांग ने कहीं लिखा है कि हम चीनियों के बारे में लोगों ने ये मशहूर कर रखा है कि क़हत पड़ता है तो हम अपने बच्चे तक खा जाते हैं। लेकिन ख़ुदा का शुक्र है कि हम उन्हें इस तरह नहीं खाते जिस तरह अंग्रेज़ 'बीफ’ खाते हैं यानी कच्चा!”
हम भी जवाबन कुछ कहना चाहते थे कि एक नुकीली एड़ी जो एक हसीन बोझ सहारे हुए थी, हमारे पंजे में बरमे की तरह उतरती चली गई। हमारी मर्दाना चीख़FOR HE IS A JOLLY GOOD FELLOW के कोरस में दब गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने का बर्मी सागवान का डांस फ़्लोर बहके बहके क़दमों तले फिर चरचराने लगा।
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.