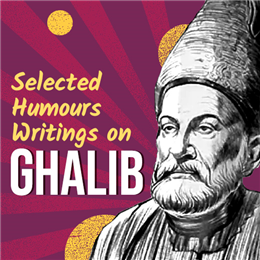ग़ालिब के साथ आराफ़ में
अलिफ़: आदाब अर्ज़ करता हूँ क़िबला।
ग़ालिब: जीते रहो, जीते रहो... आलम-ए-ख़ाकी से आरहे शायद... कैसे आना हुआ?
अलिफ़: बस शौक़-ए-ज़ियारत खींच लाया, फ़रमाईए, इस आलम-ए-लाहूत में कैसे बसर हो रही है?
ग़ालिब: अजी, यहां धरा क्या है?
अलिफ़: अच्छा, तो फिर वही कुछ सुनाइए जो आप पर आलम-ए-ख़ाकी में बीती।
ग़ालिब: अरे मियां! क्यों भरे ज़ख़्म कुरेदते हो... अच्छा हुआ क़ैद-ए-हयात-ओ-बंद-ए-ग़म से रिहाई पाई। दुख है तो ये कि फ़रिश्तों के लिखे पर नाहक़ पकड़ा गया हूँ। दम-ए-तहरीर कोई आदमी तो था नहीं कि बुरे-भले पर निगाह रखता... बहर कैफ़ नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत रहा हूँ।
अलिफ़: बहरहाल, कुछ तो कहिए कि इस ख़ाक-दाँ में दिन कैसे कटे?
ग़ालिब: सुनना चाहते हो? अच्छा तो कान धरो... मगर बीच में बोलना मत।
अलिफ़: इरशाद।
ग़ालिब: आलम दो हैं, एक आलम-ए-अर्वाह और एक आलम-ए-आब-ओ-गिल। क़ायदा ये है कि आलम-ए-आब-ओ-गिल के मुजरिम आलम-ए-अर्वाह में सज़ा पाते हैं लेकिन यूं भी हुआ है कि आलम-ए-अर्वाह के गुनहगार को दुनिया में भेज कर सज़ा देते हैं। चुनांचे मैं आठवीं रजब 1212 हि. मुताबिक़ 1717 ई. में रू-बकारी के वास्ते आलम-ए-आब-ओ-गिल में भेजा गया।
मैं क़ौम का तुर्क सलजूक़ी हूँ। दादा मेरा मावराउन्नहर से शाह आलम के वक़्त में हिंदुस्तान आया... बाप मेरा अबदुल्लाह बेग ख़ां बहादुर लखनऊ जाकर आसिफ़ उद्दौला का नौकर हुआ, फिर हैदराबाद में नवाब निज़ाम अली ख़ां का मुलाज़िम हुआ। वो नौकरी एक ख़ाना-जंगी के बखेड़े में जाती रही। अलवर का क़सद किया... महाराजा बख़्तियार सिंह की रिफ़ाक़त में मारा गया। मेरा चचा हक़ीक़ी मरहटों की तरफ़ से अकबराबाद का सूबेदार था। उसने मुझे पाला, मेरा हक़ीक़ी भाई बस एक था, वो तीस बरस दीवाना रह कर मर गया।
मैंने अय्याम दबिस्ताँ नशीनी में शरह मातह आमिल तक पढ़ा, बाद उसके लहू व लोब और आगे बढ़कर फ़िस्क़-ओ-फ़ुजूर और ऐश-ओ-इशरत में मुनहमिक हो गया। फ़ारसी ज़बान से लगाव और शे’र-ओ-सुख़न का जौक़ फ़ित्री-ओ-तब्ई था। नागाह एक शख़्स कि सासान पंजुम की नस्ल में माहज़ा मंतिक़-ओ-फ़लसफ़ा में मौलवी फ़ज़ल हक़ मरहूम का नज़ीर और मोमिन मुवह्हिद-ओ-सूफ़ी साफ़ी था, मेरे शहर में वारिद हुआ... उस्ताद बे मुबालग़ा जामा सिप अह्द-ओ-बज़र जमहर अस्र था।
मेरा क़द दराज़ी में अंगुश्तनुमा है। जब मैं जीता था तो मेरा रंग चम्पई था और दीदावर लोग उसकी सताइश किया करते थे। अब जब कभी मुझको वो अपना रंग याद आता है तो छाती पर साँप सा लोट जाता है, जब दाढ़ी मूंछ में बाल सफ़ेद आगए, तीसरे दिन चियूंटी के अंडे गालों पर नज़र आने लगे। इससे बढ़कर ये हुआ कि आगे के दो दाँत टूट गए। नाचार मिस्सी भी छोड़ दी और दाढ़ी भी, मगर ये भी याद रखिए कि इस शहर में एक वर्दी आम है। मुल्ला, हाफ़िज़, बिसाती नेचा बंद, धोबी, सक्क़े, भटियारा, जोलाहा, कुंजड़ा मुँह पर दाढ़ी रखता है सर पर बाल। फ़क़ीर ने जिस दिन दाढ़ी रखी उसी दिन सर मुंडाया।
मुग़ल बच्चे ग़ज़ब होते हैं जिस पर मरते हैं उसको मार रखते हैं। मैं भी मुग़ल बच्चा हूँ। उम्र भर में एक बड़ी सितम पेशा डोमनी को मैंने भी मार रखा था। मैं जब बहिश्त का तसव्वुर करता हूँ और सोचता हूँ कि अगर मग़फ़िरत होगी और एक हूर और क़स्र मिलेगा। उसी में इक़ामत जाविदानी और उसी एक नेक-बख़्त के साथ ज़िंदगानी होगी तो इस तसव्वुर से जी घबराता है, कलेजा मुँह को आता है। वो हूर अजीरन हो जाएगी। तबीयत क्यों न घबराएगी वो ज़मुर्रदीं काख़ और तूबी की एक शाख़ चशम-ए-बद्दूर वही एक हूर...
तेरह बरस हवालात में रहा, 7 रजब 1228 हि. को मेरे वास्ते हुक्म दवाम हब्स सादर हुआ, एक बेड़ी मेरे पांव में डाल दी और दिल्ली शहर को ज़िंदाँ मुक़र्रर किया... मगर नज़्म-ओ-नस्र को मशक़्क़त ठहराया। बरसों के बाद उस जेलख़ाने से भागा। तीन बरस बिलाद-ए-शिरकिया में फिरता रहा। पायानेकार मुझे कलकत्ते से पकड़ लाए और फिर उसी मजलिस में बिठा दिया। जब देखा कि क़ैदी गुरेज़पा है दो हथकड़ीयां और बढ़ा दीं।
न जज़ा न सज़ा, न नफ़रीं न आफ़रीं, न अदल न ज़ुल्म, न लुत्फ़ न क़हर, एक ज़माने में दिन को रोटी रात को शराब मिलती थी। फिर सिर्फ़ रोटी मिले जाती थी शराब नहीं। कपड़ा अय्याम तनाम का बना हुआ था। उसकी कुछ फ़िक्र नहीं की, नादारी के ज़माने में जिस क़दर ओढ़ना बिछौना घर में था सब बेच बेच कर ख़ा लिया, गोया और लोग रोटी खाते थे और मैं कपड़ा खाता था। बे रिज़्क़ जीने का ढब मुझको इसीलिए आगया है। रमज़ान का महीना रोज़ा खा खाकर काटा करता था। आइन्दा ख़ुदा राज़िक़ है, कुछ और खाने को न मिलता तो ग़म तो था। बस एक चीज़ खाने को हो चाहे ग़म ही हो तो क्या ग़म है?
एक-बार में बीमार हो गया था। बीमार क्या हुआ तवक़्क़ो ज़ीस्त की न रही। क़ूलिंज और फिर क्या शदीद कि पाँच पहर मुर्ग़-ए-बिस्मिल की तरह तड़पा किया। आख़िर एस्सार-ए-रियो नद और अरंडी का तेल पिया। उस वक़्त तो पच गया मगर क़िस्सा क़ता न हुआ। दस दिन में दोबार आधी आधी ग़िज़ा खाई, गोया दस दिन में एक-बार ग़िज़ा तनावुल फ़रमाई। गुलाब और इमली का पन्ना और आलूबुख़ारे का अफ़्शुर्दा उस पर मदार रहा।
एक बरस तक अवारिज़ फ़साद-ए-ख़ून में मुबतला रहा। बदन फोड़ों की कसरत से सरो चराग़ाँ हो गया। ताक़त ने जवाब दे दिया। दिन रात लेटा रहता था... सर से पांव तक बारह फोड़े, हर फोड़े पर एक ज़ख़्म, हर ज़ख़्म पर एक ग़ार। हर-रोज़ बिला मुबालग़ा बारह तेरह फाए और पाव भर मरहम दरकार... और शब-ओ-रोज़ बेताब। अगर कभी आँख लग गई दो-घड़ी ग़ाफ़िल रहा हूँगा कि एक-आध फोड़े में टीस उठी। जाग उठा, तड़पा किया फिर सो गया फिर होशयार हो गया। 1277 हि. में मेरा न मरना सिर्फ़ मेरी तक़ज़ीब के वास्ते था, मगर इन तीन बरस में हर रोज़ मर्ग-ए-नौ का मज़ा चखता था... किताब से नफ़रत, शे’र से नफ़रत, जिस्म से नफ़रत, रूह से नफ़रत... जितना ख़ून बदन में था बे मुबालग़ा आधा उसमें से पीप बन कर निकल गया। सन कहाँ थी जो फिर तौलीद सालिह होती। बहरहाल ज़िंदा था,मियां 1277 हि. की बात ग़लत न थी मगर मैंने वबाए आम में मरना अपने लायक़ न समझा। वाक़ई उसमें मेरी कसर-ए-शान थी।
सतरा बहतरा उर्दू में तर्जुमा पैर-ए-ख़ज़फ़ मेरी तिहत्तर बरस की उम्र हुई, पस मैं अख़रफ़ हुआ। हाफ़िज़ा गोया कभी था ही नहीं, सामिआ बातिल बहुत दिन से था। रफ़्ता-रफ़्ता वो भी हाफ़िज़ा के मानिंद मादूम हो गया। फिर ये हाल था कि जो दोस्त आते रस्मी पुर्सिश-ए-मिज़ाज से बढ़कर जो बात होती वो काग़ज़ पर लिख देते। ग़िज़ा मफ़क़ूद थी, सुबह को क़ंद और शीरा बादाम मुक़श्शर। दोपहर को गोश्त का पानी, सर-ए-शाम तले हुए चार कबाब, सोते वक़्त पाँच रुपये भर शराब, उसी क़दर गुलाब... अख़रफ़ हूँ, पोच हूँ, आसी हूँ, फ़ासिक़ हूँ, रू सियाह हूँ। ये शे’र मीर तक़ी मीर का मेरे हस्ब-ए-हाल है;
मशहूर हैं आलम में मगर हों भी कहीं हम
अल-क़िस्सा न दरपे हो हमारे कि नहीं हम
मैं इंतिहाए उम्र नापायदार को पहुंच कर आफ़ताब लब-ए-बाम और हुजूम-ए-अमराज़ जिस्मानी और आलाम रुहानी से ज़िंदा दरगोर था। कुछ याद-ए-ख़ुदा भी चाहिए थी। नज़्म-ओ-नस्र की क़लमरू का इंतज़ाम एज़द दाना-ओ-तवाना की इनायत-ओ-इआनत से ख़ूब हो चुका, अगर उसने चाहा तो क़ियामत तक मेरा नाम-ओ-निशान बाक़ी और क़ायम रहेगा;
ग़ालिब बक़ौल हज़रत-ए-हाफ़िज़ ज़ फैज़-ए-इश्क़
सब्त अस्त बर जरीद-ए-आलम दवाम मा
(ठंडी सांस)
और ये था मेरा मरना जीना
अलिफ़: हक़ मग़फ़िरत करे।
ग़ालिब: कुछ और भी पूछना चाहते हो?
अलिफ़: इजाज़त हो तो...
ग़ालिब: अच्छा तो पूछ लो, मगर जल्दी करना, क्योंकि अभी तक यक-जान बे नवाए असद को हज़ारों आफ़तें झेलनी हैं... मैं दश्त-ए-ग़म में आहूए सय्याद दीदा हूँ।
अलिफ़: हाँ, तो ये बताइए अगर ज़हमत न हो कि ये क़ैद वैद का क्या क़िस्सा था।
ग़ालिब: कोतवाल दुश्मन था और मजिस्ट्रेट नावाक़िफ़, फ़ित्ना घात में था और सितारा गर्दिश में, बावजूद ये कि मजिस्ट्रेट कोतवाल का हाकिम है, मेरे बाब में वो कोतवाल का मह्कूम बन गया और मेरी क़ैद का हुक्म सादर कर दिया। सेशन जज बावजूद ये कि मेरा दोस्त था, उसने भी इग़्माज़ और तग़ाफ़ुल इख़्तियार किया। सदर में अपील किया गया मगर किसी ने न सुना और वही हुक्म बहाल रहा। फिर मालूम नहीं क्या बाइस हुआ कि जब आधी मीयाद गुज़र गई तो मजिस्ट्रेट को रहम आया और सदर में मेरी रिपोर्ट और वहां से हुक्म रिहाई का आ गया। और हुक्काम सदर ने ऐसी रिपोर्ट भेजने पर उसकी बहुत तारीफ़ की... सुना था कि रहम दिल हाकिमों ने मजिस्ट्रेट को बहुत नफ़रीन की थी और मेरी ख़ाकसारी और आज़ादा रवी से उसको मुत्तला किया था, यहां तक कि उसने मेरी रिहाई की रिपोर्ट भेज दी, अगरचे मैं हर काम को ख़ुदा की तरफ़ से समझता हूँ और ख़ुदा से लड़ा नहीं जा सकता।
अलिफ़: (ठंडी आह भर कर) हुंह कैसे दुख की बात है... आप ऐसा शायर और क़ैदख़ाने की ज़िल्लत।
ग़ालिब: भला दुख कैसे न होता, सरकार अंग्रेज़ी में बड़ा पाया रखता था, रईस ज़ादों में गिना जाता था। पूरा ख़िलअत पाता था, फिर बदनाम हो गया और एक बड़ा धब्बा लग गया। किसी रियासत में दख़ल कर नहीं सकता था, मगर हाँ, उस्ताद या पीरर मद्दाह बन कर रस्म-ओ-राह पैदा करता... मेरी ये आरज़ू थी कि दुनिया में न रहूं। रोम है, मिस्र है, ईरान है, बग़दाद है। ये भी जाने दो काअबा आज़ादों की जाएपनाह है और आस्ताना-ए-रहमत-उल-लिलआलमीन दिलदादों की तकियागाह है... ये है जो कुछ कि मुझ पर गुज़रा है... और ये है जिसका मैं आरज़ूमंद हूँ;
राज़ दाना ग़म रुस्वाई जावेद बलासत
बहर-ए-आज़ार ग़म अज़ क़ैद फ़िरंगम न बूद
जू राअदा-ए-दो अज़दल् ब रिहाई लेकिन
तान-ए-अहबाब कम अज़ ज़ख़्म ख़दंगम न बूद
अलिफ़: आपने ग़दर के मुताल्लिक़ कुछ न कहा... हंगामा तो ऐसा न था कि आप उसे भूल गए हों।
ग़ालिब: ग़दर की बातें क्या पूछते हो, लो सुनो, मई 1857 ई.में मुल्क ने ये फ़ित्ना उठाया। 11 मई को पहर दिन चढ़े वो बाग़ी फ़ौज मेरठ से दिल्ली आई थी या ख़ुद क़हर-ए-इलाही का पै दर पै नुज़ूल हुआ था। बक़दर-ए-ख़ुसूसियत दिल्ली मुमताज़ थी वर्ना सरता सर क़लमरू हिंद फ़ित्ना-ओ-बला का दरवाज़ा बाज़ था (लेकिन दिल्ली कब तक महफ़ूज़ रहती) फिर जो अहकाम दिल्ली में सादर हुए वो अहकाम क़ज़ा-ओ-क़दर थे, उनका मुराफ़ा कहीं नहीं, अब यूं समझ लो कि न हम कभी कहीं के रईस थे न जाह-ओ-हशम रखते थे न पेंशन रखते थे।
अलिफ़: ग़दर में आपका भी कुछ लुटा?
ग़ालिब: ग़दर में मेरा घर नहीं लुटा मगर मेरा कलाम मेरे पास कब था कि न लुटा। भाई ज़िया उद्दीन अहमद साहिब और नाज़िर हुसैन मिर्ज़ा साहिब हिन्दी-ओ-फ़ारसी नज़्म-ओ-नस्र के मुसव्विदात मुझसे लेकर अपने पास जमा कर लिया करते थे सो उन दोनों घरों पर झाड़ू फिर गई। न किताब रही न अस्बाब रहा, फिर मैं अपना कलाम कहाँ से लाता। इस हंगामे में कुछ गोरे मेरे मकान में भी घुस आए थे। मगर उन्होंने अपनी नेक खूई से घर के अस्बाब को बिल्कुल नहीं छेड़ा। मगर मुझे और मेरे दोनों बच्चों को और दो तीन नौकरों को मा चंद हमसायों के कर्नल ब्राउन के रूबरू जो मेरे मकान के क़रीब हाजी क़ुतुब उद्दीन सौदागर के घर में मुक़ीम थे, ले गए। कर्नल ब्राउन ने बहुत नरमी और इन्सानियत से सारा हाल पूछा और रुख़सत कर दिया।
1858 ई. में अमन हुआ... हुक्म हुआ कि अय्याम-ए-ग़दर में तुम बाग़ीयों से इख़लास रखते थे,अब गर्वनमेंट से क्यों मिलना चाहते हो... दूसरे दिन मैंने अंग्रेज़ी ख़त उनके नाम लिखवाकर उनको भेजा। मज़मून ये कि बाग़ीयों से मेरा इख़लास मज़िन्न-ए-महज़ है... तहक़ीक़ात फ़रमाई जाये ताकि मेरी सफ़ाई और बेगुनाही साबित हो। फरवरी 1860 ई. में पंजाब के मुल्क से जवाब आया कि लार्ड साहिब फ़रमाते हैं हम तहक़ीक़ात न करेंगे, बस ये मुक़द्दमा तै हुआ और बार और ख़िलअत मौक़ूफ़, पेंशन मस्दूद... वजह ला मालूम... दो शंबा 2 मार्च 1863 ई. को सवाद-ए-शहर मख़ेम ख़य्याम-ए-गवर्नरी हुआ। आख़िर रोज़ मैं अपने शफ़ीक़-ए-क़दीम जनाब मौलवी इज़हार हुसैन ख़ां बहादुर के पास गया। असनाए गुफ़्तगु में फ़रमाया कि तुम्हारा दरबार और ख़िलअत बदस्तूर बहाल और बरक़रार है।
कारसाज़ मा बफ़िक्र-ए-कार मा
फ़िक्र-ए-मादर कार्मा आज़ार मा
शंबा 3 मार्च को 12 बजे नवाब लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर ने मुझको बुलाया। ख़िलअत अता किया और फ़रमाया कि लार्ड साहिब बहादुर के यहां का दरबार और ख़िलअत भी बहाल है।
अलिफ़: अल्हम्दुलिल्लाह! लेकिन ग़दर के बाद दिल्ली का क्या नक़्शा था?
ग़ालिब: भाई क्या पूछते हो... दिल्ली की हस्ती मुनहसिर कई हंगामों पर है। क़िला, चाँदनी चौक, हर रोज़ मजमा जामा मस्जिद का, हर हफ़्ते सैर जमुना पुल की, हर साल मेला फूल वालों का... ये पांचों बातें नहीं रहीं थीं, फिर कहो दिल्ली कहाँ। एक दिन में सवार हो कर कुंओं का हाल दरयाफ़्त करने गया था, मस्जिद जामे से राजघाट दरवाज़े तक बिला मोमबालग़ा एक सहरा लक़-ओ-दक़ था। ईंटों के ढेर जो पड़े थे वो अगर उठ जाते तो हू का मकान हो जाता। याद करो मिर्ज़ा गौहर के बाग़ीचे के उस जानिब को कई बाँस नशेब था, फिर वो बाग़ीचा सेहन के बराबर हो गया यहाँ तक कि राजघाट का दरवाज़ा बंद हो गया, फ़सील के कंगूरे खिले हुए थे बाक़ी सब अट गया...पंजाबी कटरा, धोबी वाड़ा, राम जी गंज, सआदत ख़ां का कटरा, जरनैल की बीबी की हवेली, राम जी दास गोदाम वाले के मकानात, साहिब राम का बाग़-ओ-हवेली उनमें से किसी का पता नहीं मिलता।
ज़िन्हार कभी ये गुमान न कीजिएगा कि दिल्ली की अमलदारी मेरठ और आगरा और बिलाद-ए-शिरकिया की मिसल है। ये पंजाब अहाता में शामिल है न क़ानून न आईन, जिस हाकिम की जो राय में आए वो वैसा करे।
7 नवंबर 14 जमादी उल अव्वल, साल हाल जुमा के दिन अबुल ज़फ़र सिराज उद्दीन बहादुर शाह क़ैद-ए-फिरंग-ओ-क़ैद जिस्म से रिहा हो गए... इन्ना लिल्लाह-ए-व इन्ना इलैहे राजेऊन... फिर कहो दिल्ली कहाँ... क़िस्सा मुख़्तसर शहर सहरा हो गया और अब जो कुँवें जाते रहे और पानी गौहर-ए-नायाब हो गया तो ये सहरा सहराए कर्बला हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह दिल्ली वाले वहाँ की ज़बान को अच्छा कहते थे। वाह-रे हुस्न-ए-एतिक़ाद बंदा-ए-ख़ुदा, उर्दू बाज़ार न रहा उर्दू कहाँ? दिल्ली कहाँ? वल्लाह शहर नहीं कैंप रह गया था छावनी थी, न क़िला न शहर न बाज़ार न नहर...
अलिफ़: अदालती कार्यवाहियां उस ज़माने में कैसी रहीं?
ग़ालिब: कह तो दिया न क़ानून न आईन, जिस हाकिम की जो राय में आए वो वैसा करे। सुनो हाफ़िज़ मम्मू बेगुनाह साबित हुए। रिहाई पाई, हाकिम के सामने हाज़िर हुआ करते थे, इमलाक अपनी मांगते थे। क़ब्ज़-ओ-तसर्रुफ़ उनका साबित हो चुका था सिर्फ़ हुक्म की देर थी। एक दिन जो हाज़िर हुए मिसल पेश हुई, हाकिम ने पूछा, “हाफ़िज़ मुहम्मद बख़्श कौन?” अर्ज़ किया कि “में!” फिर पूछा कि “हाफ़िज़ मम्मू कौन?” अर्ज़ किया, “मैं... असल नाम मोहम्मद बख़्श है, मम्मू करके मशहूर हूँ।” फ़रमाया, “ये कुछ बात नहीं हाफ़िज़ मुहम्मद बख़्श भी तुम, हाफ़िज़ मम्मू भी तुम, सारा जहान भी तुम, जो दुनिया में है वो भी तुम, हम मकान किस को दें।” मिसल दाख़िल दफ़्तर हुई। मियां मम्मू अपने घर चले आए... फिर कहो दिल्ली कहाँ... दिल्ली कहाँ... दुख-दर्द की बरसात थी।
बरसात का नाम आ गया... लो पहले तो मुजमिलन सुनो एक ग़दर कालों का, एक हंगामा गोरों का। एक फ़ित्ना इन्हिदाम मकानात का, एक आफ़त वबा की। एक मुसीबत काल की, फिर बरसात जमी हालात की जामा है, इक्कीसवां दिन था आफ़ताब इस तरह गाह गाह नज़र आजाता था जिस तरह बिजली चमक जाती है। रात को कभी कभी तारे अगर दिखाई देते तो लोग जुगनू समझ लेते। अँधेरी रातों में चोरों की बन आई, कोई दिन नहीं होता कि दो-चार जगह किसी चोरी का हाल न सुना जाता। मुबालग़ा न समझना हज़ारहा मकान गिर गए, सैकड़ों आदमी जाबजा दब कर मर गए, गली गली नदी बह रही थी, क़िस्सा मुख़्तसर वो अनकाल था कि मेंह न बरसा, अनाज न पैदा हुआ। ये पन काल था कि पानी ऐसा बरसा कि बोए दाने बह गए, जिन्होंने नहीं बोया था वो बोने से रह गए सुन लिया दिल्ली का हाल?
अलिफ़: अच्छा जाने दीजिए इन बातों को, जब दिल्ली वाले न रहे तो दिल्ली कहाँ रहती, सुनकर कलेजा कटता है... हाँ, ये तो फ़रमाईए कि आपके मज़हबी अक़ाइद क्या थे क्योंकि उसके मुताल्लिक़ लोगों में गूना-गूं चे मिगोइयाँ हो रही हैं। आपको आलम-ए-आब-ओ-गिल के कुछ लोग मुशरिक कहते हैं।
ग़ालिब: मेरा क्या बिगड़ा... मुशरिक वो हैं जो वुजूद को वाजिब-ओ-मुम्किन में मुश्तर्क जानते हैं। मुशरिक वो हैं जो मुस्लिमा को नबुव्वत में ख़ातिम-उल-मुरसलीन का शरीक गरदानते हैं, मुशरिक वो हैं जो नौ मुस्लिमों को अबू लाइमा का हमसर मानते हैं। दोज़ख़ उन लोगों के वास्ते है... मैं मुवह्हिद ख़ालिस और मोमिन कामिल हूँ। ज़बान से ला-इलाहा इल-लल्लाह कहता हूँ और दिल में लामौजूद इल-लल्लाह लामुवस्सर फ़ी वुजूद अल्लाह समझे हुए हूँ। अंबिया सब वाजिब-उल-ताज़ीम और अपने वक़्त में सब मुफ़्तरिज़-उल-अताअत थे। मुहम्मद सल्ल अल्लाह अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत ख़त्म हुई। ये ख़ातिम-उल-मुरसलीन और रहमतुल लिल आलमीन हैं। मक़ता नबुव्वत का मतला, इमामत न इजमाई बल्कि मिन अल्लाह है और इमाम मिन अल्लाह अली अलैहिस्सलाम हैं सुम्मा हसन सुम्मा हुसैन इसी तरह ता मेहदी अलैहिस्सलाम।
बरीं ज़ीस्तम हम बरीं बगुज़रम
हाँ इतनी बात और है कि अबायत और ज़ंदिक़ा को मर्दूद, शराब को हराम और अपने को आसी समझता हूँ। अगर मुझको दोज़ख़ में डालेंगे तो मुझको जलाना मक़सूद न होगा बल्कि दोज़ख़ का ईंधन हूँगा और दोज़ख़ की आँच को तेज़ करूँगा ताकि मुशरिकीन और मुनकरीन नबुव्वत ए मुस्तफ़वी और इमामत ए मुर्तज़वी उसमें जलें।
मुझमें कोई बात मुसलमानी की नहीं है फिर मैं नहीं जानता कि मुसलमानों की ज़िल्लत पर मुझको क्यों इस क़दर रंज और तास्सुफ़ होता है... सूफ़ी साफ़ी हूँ और हज़रात सूफ़िया हिफ़्ज़-ए-मरातिब मलहूज़ रखते हैं।
गर हिफ़्ज़-ए-मरातिब न कनी ज़िंदीक़ी
शाह मुहम्मद आज़म ख़लीफ़ा थे मौलाना फ़ख़्र उद्दीन साहिब के और मैं मुरीद हूँ उस ख़ानदान का...
बंदा परवर! मैं तो बनी आदम को, मुसलमान हो या हिंदू या नसरानी, अज़ीज़ रखता हूँ। और अपना भाई गिनता हूँ, दूसरा माने या न माने। बाक़ी रही अज़ीज़दारी जिसको अहल-ए-दुनिया क़राबत कहते हैं, उसको क़ौम और ज़ात और मज़हब और तरीक़ शर्त है और उसके मुरातिब-ओ-मदारिज हैं... मियां किस क़िस्से में फंसा है... ख़ुदा के बाद नबी और नबी के बाद इमाम यही है मज़हब-ए-हक़ और अस्सलाम-ओ-वलइकराम, अली अली किया कर और फ़ारिगुलबाल रहा कर।
ग़ालिब नदीम-ए-दोस्त से आती है बू-ए-दोस्त
अलिफ़: ख़ूब! सुनते हैं कि आप मय-ए-नाब के बड़े रसिया थे?
ग़ालिब: आसूदा बाद ख़ातिर ग़ालिब... क्या ज़िक्र छेड़ा वल्लाह।
इक तीर मेरे सीने पर मारा कि हाय हाय
जब दो जुरए पी लिए फ़ौरन रग-ओ-पै में दौड़ गई। दिल तवाना, दिमाग़ रोशन हो गया। चार बोतल शराब तीन शीशे गुलाब के तोशा ख़ाने में मौजूद हैं, लेकिन अपना तो ये ख़्याल है कि;
मय से ग़रज़ निशात है किस रू सियाह को
इक-गो न बे-ख़ुदी मुझे दिन रात चाहिए
अलिफ़: वाह वाह... मज़ा आ गया... ख़ैर... और ये आम वाम की बात क्या थी, आपकी दो बातें तो आम से चिपक कर रह गईं कि मीठा हो और बहुत हो।
ग़ालिब: मुझसे पूछो तुम्हें ख़बर क्या है
आम के आगे नीशकर क्या है
न गुल इसमें न शाख़-ओ-बर्ग न बार
जब ख़िज़ां आए तब हो इसकी बिहार
और दौड़ाइए क़ियास कहाँ
जान-ए-शीरीं में ये मिठास कहाँ
नज़र आता है यूं मुझे ये समर
कि दवाख़ान-ए-अज़ल में मगर
आतिश-ए-गुल पे क़ंद का है क़िवाम
शीरा के तार का है रेशा नाम
साहिब-ए-शाख़-ओ-बर्ग-ओ-बार है आम
नाज़ पर्वर्द-ए-बहार है आम
एक दिन मैं पलंग पर लेटा हूँ कि नागाह चराग़ दूदमान इल्म-ओ-यक़ीन सय्यद नसीरउद्दीन आया तो एक कोड़ा हाथ में और एक आदमी साथ उसके, सर पर टोकरा धरा, उस पर घास हरी बिछी। मैंने कहा अहा, सुलतान उल उलमा मौलाना सरफ़राज़ हुसैन देहलवी दुबारा रसद... बारे मालूम हुआ कि वो नहीं हैं, ये कुछ और है, फ़ैज़-ए-ख़ास नहीं लुत्फ़-ए-आम है, यानी शराब नहीं आम है। ख़ैर, ये अतीया भी बे ख़लल है बल्कि नेम-उल-बदल है, एक एक को सरबमुहर गिलास समझा। लकोर से भरा मगर वाह, कैसी हिक्मत से भरा हुआ है कि 65 गिलास में से एक क़तरा नहीं गिरा है।
अच्छा अब चलता हूँ, देर हो गई। कहीं गैरहाज़िरी न लिख दें और भगोड़ों में शामिल न कर दें। आख़िर फ़रिश्ते हैं, उन्होंने पहले क्या किया कि अब ख़ैर की तवक़्क़ो करूँ।
अलिफ़: बस एक आख़िरी सवाल?
ग़ालिब: कहो कहो... जल्दी से कह डालो...
अलिफ़: आपने अपनी शायरी और तस्नीफ़ के मुताल्लिक़ कुछ इरशाद नहीं फ़रमाया।
ग़ालिब: हुंह, अच्छा ये भी सन लो... ख़ाकसार ने इब्तदाए सन तमीज़ में उर्दू ज़बान में सुख़न सराई की थी फिर औसत उम्र में बादशाह दिल्ली का नौकर हो कर चंद रोज़ इसी रविश पर ख़ामाफ़रसाई की... नज़्म-ओ-नस्र का आशिक़-ओ-माइल हूँ। हिन्दोस्तान में रहता था मगर तेग़ इस्फ़हानी का घायल था। जहां तक ज़ोर चल सका फ़ारसी ज़बान में बहुत बका। एक उर्दू का दीवान हज़ार बारह सौ बैत का,एक फ़ारसी का दीवान दस हज़ार कई सौ बैत का, तीन रिसाले नस्र के, ये पाँच नुस्खे़ मुरत्तिब हो गए फिर सोचा अब और क्या कहूँगा। मदह का सिला न मिला। ग़ज़ल की दाद न पाई। हर्ज़ागोई में सारी उम्र गँवाई। ग्यारहवीं मई 1855 ई. से 31 जुलाई 1857 ई. तक की रूदाद नस्र में ब इबारत फ़ारसी ना आमेख़्ता ब अरबी लिखी और वो 15 सतर के मेस्तर से चार जुज़ की किताब आगरा के मतबा मुफ़ीद-ए-ख़लायक में छपी। दस्तंबू उसका नाम रखा और उसमें सिर्फ़ अपनी सरगुज़श्त और अपने मुशाहिदे के बयान से काम रखा।
ज़बान फ़ारसी में ख़तों का लिखना पहले ही मतरूक कर दिया था। पीराना साली और ज़ोफ़ के सदमों से मेहनत पर वही और जिगर कावी की क़ुव्वत मुझमें न रही। हरारत-ए-ग़रीज़ी का ज़वाल था और ये हालत;
मुज़्महिल हो गए क़ुवा ग़ालिब
अब अनासिर में एतिदाल कहाँ
(एक आवाज़ दूर से सुनाई देती है)
आवाज़: मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ां देहलवी हाज़िर होवे।
ग़ालिब: अच्छा ख़ुदाहाफ़िज़... आलम-ए-आब-ओ-गिल के रहने वालों को सलाम पहुंचा देना।
अलिफ़: ज़रूर ज़रूर... इंशाअल्लाह... मगर ज़हमत हुई आपको।
आवाज़: मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ां ग़ालिब हाज़िर होवे।
ग़ालिब: हाज़िर... हाज़िर (चलते चलते) ख़ुदा-हाफ़िज़... ख़ुदा-हाफ़िज़...
अब कहाँ वो लोग... चाट गई ये ज़मीन
मक़दूर हो तो ख़ाक से पूछूँ कि ऐ लईम
तूने वो गंज हाए गिरांमाया क्या किए
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.