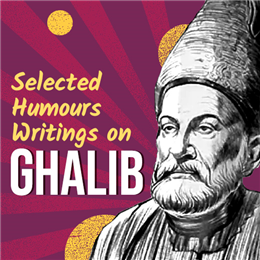ग़ालिब जन्नत में
ग़ालिब की मौत
पस-मंज़र: एक सेह-दरा दालान है जिसके सामने एक बड़ा सेहन है। दालान के दरूँ में अंदरूनी जानिब पर्दे आधी मेहराब तक बंधे हुए हैं। दालान के वस्त में एक पलंग है जिसका सिराहना शुमाल की सिम्त है, पलंग पर गद्दा बिछा हुआ है और सफ़ेद चादर चारों तरफ़ कल्ला बत्तूं की डोरियों से पायों में बंधी हुई है। पलंग से मिला हुआ तख़्तों का चौका है जिस पर दरी बिछी हुई है और उस पर साफ़ फ़र्श है जो चारों कोनों पर मीर फ़रोशों से दबा है। सदर में बड़ा गाव तकिया क़रीने से रखा है। सामने साफ़ उगालदान रखा है, उगालदान से कुछ ऊपर पलंग से नज़दीक ख़ासदान रखा है जिसके ऊपर बहुत नफ़ीस तार का काम किया हुआ है। एक काग़ज़गीर में ख़त लिखने का काग़ज़ दबा हुआ पास ही रखा है।
पलंग के दाहिने जानिब कुछ पुराने क़िस्म के मोंढे रखे हुए हैं जिन पर हाली, शेफ़्ता, हकीम अहसन उल्लाह ख़ां साक़िब और नवाब ज़िया उद्दीन अहमद ख़ां बैठे हुए हैं। ग़ालिब पलंग पर उम्दा छींट की रज़ाई ओढ़े लेटे हैं, दोनों घुटने खड़े हैं, पूरा जिस्म ढका है सिर्फ़ चेहरा खुला है आँखें नीम-वा हैं। बेहोशी की सी कैफ़ियत है। हलक़ से ख़र-ख़र की आवाज़ बराबर आरही है। सिरहाने एक नौकर चारखाने का बड़ा रूमाल लिए मक्खियां झल रहा है।
यकायक ज़ोर की ख़र-ख़र के साथ ग़ालिब चौंकते हैं और आँखें खोल देते हैं। हाली ने आगे बढ़कर एक पर्चा पेश किया। नवाब अलाउद्दीन ख़ां लोहारू का ख़त इस्तिफ़सार हाल व तलब ख़ैरियत का था। काग़ज़ कुछ देर सामने किए रहे, बेनूर आँखों ने सफ़ा को देखा, होंटों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, ज़ोर से खँकारा, ज़रा गर्दन उठाई, अहसन उल्लाह ख़ां की तरफ़ देखा। वो उठकर तख़्त पर आए, काग़ज़गीर से काग़ज़ निकाला, क़लम-दान से क्लिक का क़लम निकाला, अंगूठे पर उसका क़त जाँचा और घुटने पर काग़ज़ रखकर लिखने को तैयार हो गए। ग़ालिब नहीफ़ आवाज़ में बोले, लिक्खो:
“मिर्ज़ा अलाई... गुमान ज़ीस्त बूद बरमन्नत ज़ुबैदरदी
बद अस्त मर्ग वले बदतर अज़ गुमान तो नीस्त
मेरा हाल मुझसे क्या पूछते हो, एक-आध रोज़ में हमसायों से पूछना...
न करदह हिज्र मदारा ब मन सर तो सलामत।
अज़्कार-ए-रफ़्ता-ओ-दरमांदा हूँ (रुक कर) ये मिसरा चुपके चुपके पढ़ता हूँ,
“ए मर्ग-ए-नागहां तुझे क्या इंतज़ार है?”
“मर्ग का तालिब ग़ालिब (रुक कर) मुहर करके भेज दो।”
फिर ग़फ़लत तारी हो जाती है, सब लोग ख़ामोश हो जाते हैं। अहसन उल्लाह ख़ां क़लम-दान से मुहर निकाल कर सब्त करते हैं लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता।(एक फ़रिश्ता बाएं जानिब आ खड़ा होता है जिसे सिर्फ़ ग़ालिब देख रहे हैं)
फ़रिश्त-ए-अजल: क्या वाक़ई आपको मेरा इंतज़ार है?
ग़ालिब: हाँ, क्या तुम मुझे लेने आए हो?
फ़रिश्ता: (सुनी को अनसुनी करते हुए) मगर आप जीने से इस क़दर बेज़ार क्यों हैं?
ग़ालिब: मेरी तमाम उम्र हसरत-ओ-नाकामी में गुज़री। हमेशा अपने हम-चश्मों की सैर चश्मी पर गुज़ारा होता रहा। मेरे तमाम हौसले दिल के दिल ही में रह गए। न कमाल की क़दर हुई, न हुनर की पज़ीराई, फिर भी तुम कहते हो कि जीने से क्यों बेज़ार हूँ।
फ़रिश्ता: तो आप चलने के लिए तैयार हैं? मगर क्या आपको अपनी नई ज़िंदगी में कुछ बेहतरी की उम्मीद है?
ग़ालिब: (आह करके)
उम्र-भर देखा किए मरने की राह
मर गए पर देखिए दिखलाएँ क्या
मेरी बेचैनी का यही तो बाइस है, मैं चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ।
फ़रिश्ता: बहुत अच्छा, चलिए।
(फ़रिश्ता आहिस्ता से ग़ालिब के क़ल्ब पर अनगुश्त-ए-शहादत रखता है। ग़ालिब एक आह के साथ आँखें खोल देते हैं, हाली आगे बढ़कर इशारों में मिज़ाजपुर्सी करते हैं।)
ग़ालिब: (नहीफ़ आवाज़ में)
दम-ए-वापसीं बरसर-ए-राह है
अज़ीज़ो बस अल्लाह ही अल्लाह है (हिचकी)
(पेशानी पर पसीने की बूँदें नज़र आने लगती हैं। चेहरे पर मुर्दनी छा जाती है। शेफ़्ता जल्दी से उठकर शर्बत-ए-अनार का चमचा हलक़ में टपकाते हैं। रूह परवाज़ कर जाती है। सब लोगों पर सुकूत तारी होजाता है। नौकर आँखें और मुँह बंद करके चादर उढ़ा देता है।)
ग़ालिब क़ब्र में
पस-ए-मंज़र: एक फ़राख़ बग़ली क़ब्र में ग़ालिब कफ़न में लिपटे पड़े हैं, हर तरफ़ तारीकी छाई हुई है। यकायक एक सुराख़ से बारीक तेज़ रोशनी की शुआ दाख़िल होती है जिससे पूरी क़ब्र में उजाला हो जाता है। रोशनी में दो फ़रिश्ते ग़ालिब के सिरहाने एक दाएं एक बाएं जानिब दोज़ानू बैठे नज़र आते हैं और ग़ालिब के चेहरे से कफ़न हटाकर उन्हें बग़ौर देखते हैं, दोनों फ़रिश्ते आहिस्ता-आहिस्ता बातचीत करते हैं।)
मुनकिर: अब इन्हें जगाना चाहिए।
नकीर: हाँ हाँ, इस मंज़िल में इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए।
मुनकिर: मगर ये हैं कौन?
नकीर: ईं, इन्हें नहीं जानते, ये दिल्ली के मशहूर-ओ-मारूफ़ फ़ारसी और रेख़्ता के शायर व इंशा पर्दाज़ मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ां ग़ालिब हैं।
मुनकिर: कौन ग़ालिब? वही तो नहीं जो (हंसकर) अपने ख़्याल में हम लोगों को दूर रखने के लिए उम्र-भर शुग़ल मयख़्वारी फ़रमाते रहे।
नकीर: मैं समझा नहीं।
मुनकिर: तुमको याद नहीं, उन्होंने एक शे’र कहा था जिसके किरामन कातबीन अक्सर चर्चे किया करते थे।
ज़ाहिर है कि घबरा के न भागेंगे नकीरें
हाँ मुँह से मगर बादा-ए-दोशीना की बू आए
नकीर: अख़ाह, यही वो ग़ालिब हैं (मुतफ़क्किर लहजे में) देखिए बारगाह क़ुद्स से इनके लिए क्या हुक्म होता है।
मुनकिर: ये तो कोई ऐसी संगीन तक़सीर नहीं है। शायराना शोख़ी से ज़्यादा इसकी क्या अहमियत है।
नकीर: बात ये है कि गुमराही क़रीब क़रीब तमाम शोअरा का तुर्रा-ए-इम्तियाज़ है। वो तो ख़ैर हमारे साथ ठिटोल थी। देखना ये अभी और क्या-क्या ऊटपटांग जवाब देते हैं।
मुनकिर: जो कुछ हो अब इन्हें जगाना चाहिए।
नकीर: अच्छा जगाता हूँ।
(ग़ालिब के कान के पास मुँह ले जाता है और गरजती हुई आवाज़ में “क़ुम बेइज़्नल्लाह” कहता है, ग़ालिब के पलकों में हल्की हल्की हरकत पैदा होती है फिर झुरझुरी सी आती है। एक दम से उठकर बैठ जाते हैं और आँखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगते हैं।)
ग़ालिब: (फ़रिश्तों को देखकर) मैं कहाँ हूँ?
मुनकिर: क़ब्र में।
ग़ालिब: तुम कौन लोग हो?
मुनकिर: नकीर हम मुनकिर नकीर हैं।
ग़ालिब: (चीं ब जबीं हो कर) यहां भी आराम से सोना नहीं मिलेगा।
मुनकिर-नकीर: हम बहुक्म-ए-ख़ुदा आए हैं, आपसे चंद सवाल करके चले जाऐंगे।
ग़ालिब: बिसमिल्लाह फ़रमाईए।
(कहते हुए सँभल कर बैठ जाते हैं मगर चेहरे से बराबर नागवारी के असरात नुमायां हैं)
मुनकिर: (अरबी में) मिन रब्बिक
ग़ालिब: मैं अरबी से ज़रा कम वाक़िफ़ हूँ, तूरानी उल असल हूँ और पारसी ज़बान का शायर और कभी कभी अहबाब की ख़ातिर रेख़्ता में भी फ़िक्र कर लिया करता था।
नकीर: दादार तवे कीस्त?
मुनकिर: कुदाम रसूल रा पीरो बूदी?
नकीर: ईमान चीस्त, नूर राज़ ज़ुल्मत चूँ शनाख़्ती?
(सवालात की बोछाड़ से घबरा उठे और बोले)
ग़ालिब: ठहरो ठहरो, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मैंने ज़िंदगी में एक शे’र कहा था जिस पर मेरा अक़ीदा है जो चाहो समझ लो:
हम मुवह्हिद हैं हमारा कैश है तर्क-ए-रूसूम
मिल्लतें जब मिट गईं अज्ज़ा-ए-ईमाँ हो गईं
(मुनकिर नकीर दोनों अंगुश्त बदनदाँ रह गए और सोचने लगे। कई मिनट गुज़र गए, यकायक फ़िज़ा में हल्का हल्का लहन दौड़ने लगा। ग़ालिब भौंचक्के हो कर इधर उधर देखने लगे लेकिन मुनकिर नकीर मोअद्दब और नमाज़ की सी नीयत बांध कर सर झुकाकर खड़े हो गए, लहन लहज़ा बह लहज़ा बढ़ता गया। यकायक साज़ ख़ामोश हो गया और एक बा रोब लेकिन बारीक आवाज़ सुनाई दी।)
मुनकिर नकीर: तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। इस बंदे का जवाब तुम्हारे कानों के लिए बिल्कुल नया है लेकिन बात उसने बड़े पते की कही है, इस पर अज़ाब-ए-क़ब्र की ज़रूरत नहीं। किरामन कातबीन से कहो इसकी फ़र्द-ए-आमाल इसे सुना दें ताकि ये अपने गुनाहों की जवाबदेही के लिए तैयार हो जाए।
(मुनकिर नकीर हैरत से ग़ालिब को देखते हुए फ़िज़ा में तहलील होजाते हैं।)
ग़ालिब मिला-ए-आला की अदालत में
पस-ए-मंज़र: एक बहुत ही वसीअ कमरा, चारों तरफ़ बड़े बड़े तारे नज़र आरहे हैं, शुमाल-ओ-जुनूब में दो-रूया सफ़ेद साये नज़र आरहे हैं, उन सायों के इख़्तिताम पर मशरिक़ी किनारे पर एक 75-80 बरस का बूढ़ा पुश्त ख़म, बदन में रअशा लेकिन इस उम्र में भी सुर्ख़ सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ सर झुकाए खड़ा है। उसके यमीन-ओ-यसार एक एक परदार फ़रिश्ता काग़ज़ के पुलिंदे हाथ में लिए खड़ा है। उनके चेहरों से बेबाकी, ख़ुदएतिमादी और तमानियत ज़ाहिर हो रही है। दोनों ख़ामोश जैसे किसी इंतज़ार में खड़े हों। दफ़अतन हल्की हल्की लहन की आवाज़ पैदा होती है, तमाम साये सर झुका देते हैं फ़रिश्ते ज़्यादा करख़्त अंदाज़ में खड़े होजाते हैं। उनके परों की सरसराहाट से ग़ालिब चौंक कर सर उठाते हैं और फ़रिश्तों को दाएं-बाएं देखकर कुछ मुतहय्यर से हुए और बोले अभी अभी तो दोनों से नजात हासिल की। आप फ़रमाईए आप कौन हैं?)
किरामन हम किरामन कातबीन हैं। ये मिला-ए-आला है, हमें हुक्म मिला है कि तुम्हें तुम्हारे उन जुर्मों की तफ़सील सुना दें जो तुमने दुनिया में किए हैं।
ग़ालिब: बहुत ख़ूब, आप भी अपने हौसले निकाल लीजिए।
कातबीन: (अदालत को मुख़ातिब करते हुए) ये मुल्ज़िम एशिया के मशहूर-ओ-मारूफ़ ख़ित्ता-ए-हिंद का नामवर शायर-ओ-अदीब मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ां अल-मुतख़ल्लुस ब ग़ालिब मारूफ़ ब नौशा है। आज ही इसने दार उल-अमल को छोड़ा है, हम इसकी फ़र्द-ए- आमाल लेकर हाज़िर हुए हैं कि बारगाह-ए-जलालत में पेश करें।
निदा-ए-ग़ैबी: तुम को जो कुछ कहना हो कहो और मुजरिम को जवाबदेही का मौक़ा दो।
किरामन: अह्कमुल हाकिमीन इसकी फ़र्द-ए-आमाल इस्याँ से बिल्लकुल स्याह है।
निदा-ए-ग़ैबी: इसके ख़िलाफ़ ख़ास ख़ास इल्ज़ामात क्या हैं?
(किरामन कातबीन ने अपने अपने पुलिंदे खोले और यूं गोया हुए)
किरामन: रब उल अरबाब, ये मुजरिम आलम-ए-अर्वाह 1212 हि. को रू-बकारी के लिए आलम-ए-आब-ओ-गिल में भेजा गया। 13 बरस हवालात में रहा। 17 रजब 1225हि. को इसके लिए हुक्म दवाम-ए-हब्स सादर हुआ। पांव में बेड़ी डाल दी गई और दिल्ली शहर को ज़िंदाँ मुक़र्रर किया गया। नज़्म-ओ-नस्र मशक़्क़त ठेराई गई मगर ये गुरेज़ पा क़ैदी जेलख़ाने से भाग कर तीन साल तक बिलाद-ए-शिरकिया में फिरता रहा, पायानेकार कलकत्ता से पकड़ लाया गया और दो हथकड़ियां और बढ़ा दी गईं। बावजूद पांव बेड़ी से फ़िगार और हाथ हथकड़ियों से ज़ख़्मदार और मशक़्क़त मुक़र्रर होने के उसने आज 1285 ई. तक क़लील मुद्दत में अपने जराइम में इज़ाफ़ा करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। चुनांचे इसका सबसे संगीन जुर्म ये है कि इसने बार गाह-ए-क़ुद्स में उम्र-भर सर-ए-नियाज़ नहीं झुकाया और न कभी रोज़ा रखा।
निदा-ए-ग़ैबी: इस इल्ज़ाम का कोई सबूत?
कातबीन: ऐ दादार-ए-जहां, इसने ख़ुद अपने मुँह से ग़दर के बाद जब इसकी पेंशन बंद हुई थी और दरबार में शिरकत से रोक दिया गया था, पंजाब की लेफ़टनटी के मीर-ए-मुंशी से ये कहा था कि तमाम उम्र में एक दिन शराब न पी हो तो काफ़िर और एक दफ़ा नमाज़ पढ़ी हो तो गुनहगार, फिर मैं नहीं जानता कि सरकार ने मुझे बाग़ी मुसलमानों में क्यों शुमार किया है।
किरामन: ताला शानक यही नहीं, उम्र-भर क़िमारबाज़ी करता रहा। दुनिया में इसके लिए भी सज़ा भुगती मगर इस फे़अल से बाज़ नहीं आया। रोज़ा इसने कभी न रखा। माह-ए-सियाम में कोठरी में दिन भर बंद रहता और शतरंज खेला करता। कभी रोटी का टुकड़ा मुँह में डाल लिया, कभी दो घूँट पानी पी लिया और इसे रोज़ा बहलाने से ताबीर किया करता था।
कातबीन: जल जलालक, एक मर्तबा जब बहादुर शाह ज़फ़र ने इस मसले में इससे बाज़पुर्स की तो उसने इस्तिहज़ा के साथ ये जवाब देकर उसे ख़ामोश कर दिया;
सामान ख़ौर-ओ-ख़्वाब कहाँ से लाऊँ
आराम के अस्बाब कहाँ से लाऊँ
रोज़ा मिरा ईमान है ग़ालिब लेकिन
ख़स-ख़ाना-ओ-बर्फ़-ए-आब कहाँ से लाऊँ
(कातबीन ये कह कर रुके ही थे कि ग़ालिब ने कराह कर आह की और गिड़गिड़ाकर बोले)
ग़ालिब: बार-ए-इलाहा, इन फ़रिश्तों की फ़र्द-ए-जुर्म तवील और मैं साल भर से बिस्तर पर पड़े पड़े नहीफ़-ओ-नज़ार हो गया हूँ। तमाम जिस्म ज़ख़महाए बिस्तर से फ़िगार है। इतनी ताक़त नहीं कि खड़े खड़े उनकी दास्तानें सुनूँ। शाहा, मुझे इजाज़त मर्हमत हो कि कहीं पीठ टेक कर उनका इस्तिग़ासा सुनूँ।
निदा-ए-ग़ैबी: अच्छा तेरे साथ ये रिआयत की जाती है कि फ़र्श पर बैठ जा।
(साथ ही सायों में हरकत हुई और एक नर्म क़ालीन ग़ालिब के नीचे बिछा दिया गया और एक गाव तकिया रख दिया गया। ग़ालिब एक आह के साथ तकिया का सहारा लेते उस पर नीम दराज़ हो गए।)
किरामन कातबीन: इसके फ़र्द-ए-जुर्म में कुछ और बयान करना बाक़ी है या इल्ज़ामात ख़त्म हो गए।
किरामन: आक़ाए दो-जहाँ, ये तो समुंदर से एक क़तरा था, इसके स्याह कारनामों का सिलसिला तो लामतनाही है।
निदा-ए-ग़ैबी: अच्छा आगे बढ़ो।
किरामन: इसने बारगाह-ए-जलालत में बारहा गुस्ताख़ी की है और निहायत बेबाकी से पेश आया है।
निदा-ए-ग़ैबी: इस इल्ज़ाम का कोई सबूत?
कातबीन: इस शे’र सेबढ़ कर इसकी दरीदा दहनी का और क्या सबूत हो सकता है;
ज़िंदगी अपनी जो इस तौर से गुज़री ग़ालिब
हम भी क्या याद करेंगे कि ख़ुदा रखते थे
किरामन: इसने क़ज़ा-ओ-क़दर के इंतज़ामात पर भी अक्सर तमस्खुर किया है।
निदा-ए-ग़ैबी: वो क्योंकर?
कातबीन: एक दफ़ा रात को पलंग पर लेटे हुए तारों की ज़ाहिरी बे नज़्मी और इंतिशार देखकर बोले जो काम ख़ुद-राई और लापरवाही से किया जाता है अक्सर बेढंगा होता है। सितारों को देखो किस अबतरी से बिखरे हुए हैं न तनासुब न इंतज़ाम है न बेल न बूटा, मगर बादशाह ख़ुद मुख़्तार है कोई दम नहीं मार सकता।
किरामन: और या बारी-ए-ताला, इसने क़ियामत से भी इनकार किया है।
(इतना सुनते ही ग़ालिब ज़रा चौंके और सँभल कर बैठ गए)
इसने एक शे’र कहा था जिससे क़ियामत का इनकार लाज़िम आता है;
नहीं कि मुझको क़ियामत का एतिक़ाद नहीं
शब-ए-फ़िराक़ से रोज़-ए-जज़ा ज़ियाद नहीं
(ग़ालिब जो ज़रा चौकन्ने हो गए थे शे’र सुनते ही फिर इत्मीनान से गाव तकिए से लग कर बैठ गए और चुपके से “सुख़न-फ़हमी आलम-ए-बाला मालूम शुद” कह के ख़ामोश हो गए।)
कातबीन: इसके फ़र्द-ए-जुर्म में दूसरा संगीन जुर्म इसकी शराब से वालिहाना मुहब्बत है। इसने तमाम उम्र मयख़्वारी की। किसी रोज़ नाग़ा नहीं किया। अक्सर रात को सरख़ुशी के आलम में इसकी तलब-ए-शराब बढ़ जाती थी।
किरामन: शराब की अहमियत में इसे इतना ग़ुलू था कि इसके एक दोस्त ने इससे तंबीहन कहा कि शराबखोर की दुआ क़बूल नहीं होती तो उसने निहायत दरीदा दहनी से जवाब दिया कि भाई जिसे शराब मयस्सर हो उसको और क्या चाहिए जिसके लिए दुआ करे।
कातबीन: ख़ुदावंद, यही नहीं बल्कि इसने बड़ी बड़ी बुज़ुर्ग हस्तीयों को अपनी शराबनोशी का ठेकेदार क़रार दिया था, मसलन एक मर्तबा इसने साक़ी को धौंसने की नई तरकीब निकाली, जब उसने मज़ीद शराब देने से इनकार कर दिया तो इसने कहा;
कल के लिए कर आज न ख़िस्त शराब में
ये सोर ज़न है साक़ी-ए-कौसर के बाब में
और तो और इसे मुतबर्रिक अश्या रहन रखकर और बेच कर शराब ख़रीदने में भी कोई बाक न था, एक मर्तबा ये कह कर;
रखता फिरूँ हूँ ख़िरक़ा-ओ-सज्जादा रहन-ए-मय
मुद्दत हुई है दावत-ए-आब-ओ-हवा किए
इसने बुज़ुर्गों की ये मीरास भी बनिए की नज़र कर दी।
किरामन: इसने ग़ज़ब ये किया कि हज़रत साक़ी-ए-कौसर को उम उल ख़बाइस का साक़ी क़रार देकर उनके एतिमाद पर धड़ल्ले से पिया करता था। इसने इस यक़ीन का किस बुलंद आहंगी से ऐलान किया है;
बहुत सही ग़म-ए-गेती शराब कम क्या है
ग़ुलाम साक़ी-ए-कौसर हूँ मुझको ग़म क्या है
इसने दुनिया की शर्म-ओ-हया भी बालाए ताक़ रख दी थी, मदहोशी में इसका भी ख़्याल नहीं रहता था कि किस जगह पी रहा है और ज़ाहिरी रख-रखाव को तोड़ने पर फ़ख़्र करता था;
जब मयकदा छुटा तो फिर अब क्या जगह की क़ैद
मस्जिद हो मदरसा हो कोई ख़ानक़ाह हो
कातबीन: या इल्लाहुल आलमीन, इसकी मय-नोशी की लत का अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि जब मय-नोशी के बाइस इसके आज़ा-ओ-जवारेह ने बिल्कुल जवाब दे दिया और इसके रअशादार हाथों ने जाम उठाने से इनकार कर दिया तो इसने सिर्फ़ बूए मय पर इक्तिफ़ा की और अपने मुलाज़िमों को हुक्म दिया कि;
गो हाथ में जुंबिश नहीं आँखों में तो दम है
रहने दो अभी सागर-ओ-मीना मिरे आगे
किरामन: इसने जाम नोशी की वो हवा बांध रखी थी कि जब कभी किसी फ़र्ज़ की अदाई के सिलसिले में सरज़मीन दिल्ली से गुज़रा तो मुझे ऐसा महसूस होने लगता था कि जैसे शराब से मतकीफ़ हुआ जा रहा हूँ। इस ज़ालिम शायर ने ये कह कर;
है हवा में शराब की तासीर
बादानोशी है बादा पैमाई
ख़्याल को हक़ीक़त बना दिया था।
(ग़ालिब इस तमाम रूएदाद-ए-जराइम के दौरान बिल्कुल ख़ामोश तकिया के सहारे आँखें बंद किए लेटे रहे और सिवाए एक बार कराहने के उन्होंने एक लफ़्ज़ भी नहीं कहा। किरामन की फ़हरिस्त इल्ज़ामात ख़त्म हुई तो निदा आई।)
निदा-ए-ग़ैबी: इसकी फ़र्द-ए-जुर्म ख़त्म हुई या अभी कुछ बाक़ी है?
किरामन कातबीन: ख़ुदा वन्द-ए-जहाँ, इसकी फ़र्द-ए-जुर्म बहुत तवील है, जिसका सिर्फ़ एक हिस्सा बारगाह आली-ओ-मुताली में हमने पेश किया। हमने अपनी उम्र में ऐसा फ़र्द नहीं पाया जिसे इस्याँ कोशी में लुत्फ़ आता हो और जिसका हौसला गुनाह हमेशा बढ़ा हुआ हो। इसने अपने मआसी को कभी अहमियत नहीं दी और उन्हें मामूली दर्जा का समझता रहा। इसकी जुर्रत-ए-बेबाकाना मुलाहिज़ा फ़रमाएं, कहता है;
दरिया-ए-मआसी तुनुक-आबी से हुआ ख़ुश्क
मिरा सर-ए-दामन भी अभी तर न हुआ था
ग़ालिब का जवाब
पस-ए-मंज़र: मंज़र में ज़रा सा तग़य्युर हो जाता है, सिम्त मग़रिब में एक निहायत ठंडी हल्की मावराए नीलगूं रोशनी उफ़ुक़ पर नुमायां हो जाती है। लहन ज़रा तेज़ होजाता है। तमाम साये मा किरामन कातबीन के बाअदब सर झुकाकर खड़े होजाते हैं। एक शीरीं मगर पुरअसर लहजे में आवाज़ आती है।
निदा-ए-ग़ैबी: ग़ालिब सुनता है, तेरे ख़िलाफ़ तेरे हर दम के साथियों ने क्या-क्या ज़हर उगला है। तेरे पास इन इल्ज़ामात का क्या जवाब है?
(ग़ालिब इस बराह-ए-रास्त तख़ातुब से कुछ घबरा से गए और खाँसते कराहते उठकर दोज़ानू बैठ गए। कुछ लम्हे ख़ामोश रहने के बाद बोले)
ग़ालिब: तू दाना है, तू बीना है, तुझसे कुछ पिनहां नहीं है। इन इल्ज़ामात की सेहत-ओ-अदम सेहत के मुताल्लिक़ में कुछ अर्ज़ नहीं कर सकता, लेकिन उनके बाअज़ एतराज़ात के मुताल्लिक़ अगर इजाज़त मर्हमत हो तो कुछ अर्ज़ करूँ।
निदा-ए-ग़ैबी: हमारे हुज़ूर में तुझे हर तरह की आज़ादी है, तुझे अपनी बरीयत के मुताल्लिक़ जो कुछ कहना हो कह।
ग़ालिब: आसी नवाज़, तेरे रहम-ओ-अलताफ़ बेपायाँ के सदक़े, मुझे सबसे पहले तो इस इल्ज़ाम शराबनोशी के बारे में ये अर्ज़ करना है कि इन्हें मेरे शे’रों से सख़्त मुग़ालता हुआ। मैंने जो कुछ कहा, ज़रह्-ए-इम्तिसाल अमर कहा। मेरी नीयत हमेशा बख़ैर रही। मैंने दुनियाए आब-ओ-गिल में हमेशा साफ़ गोई से काम लिया और इस वक़्त तेरे हुज़ूर में जहां सिदक़-ओ-किज़्ब आश्कारा हैं, मैं कहता हूँ कि;
मय से ग़रज़ निशात है किस रू सियाह को
इक-गू न बेख़ुदी मुझे दिन रात चाहिए
मैंने हमेशा मय को अफ़्क़ार से नजात का ज़रिया समझा और अगर इस दार उलजज़ा में भी मेरी क़िस्मत में अफ़्क़ार से रिहाई नामुमकिन है तो मुझे इस मय अंदाज़ा रुबा” के दो जुरए पीने से गुरेज़ नहीं।
(किरामन-कातबीन इस जुरअत-ए-रिंदाना पर अपनी जगह मुतहय्यर रह गए।)
निदा-ए-ग़ैबी: हमें तेरी साफ़ गोई बहुत पसंद आई, लेकिन इसके ये मअनी नहीं कि तू बकिया इल्ज़ामात से बरी उल-ज़िम्मा हो गया। लेकिन इतनी रिआयत तेरी मंज़ूर है कि तू ख़ुद बता कि तू ने कौन कौन से गुनाह किए हैं।
ग़ालिब: करीमा वाए पर्दापोश आसियाँ, मुझ ज़र्रा-ए-बेमिक़दार की क्या मजाल कि हुक्मउदूली का ख़्याल तक भी दिल में लाऊँ, लेकिन इस यक़ीन के साथ कि तेरी रहमत तेरे ग़ज़ब से बढ़ी हुई है और मैं इसी रहमत के दामन में पनाह लेकर बारगाह अक़्दस में बसद इल्तिजा अर्ज़ करना चाहता हूँ कि;
आता है दाग़-ए-हसरत दिल का शुमार याद
मुझसे मिरे गुनाह का हिसाब ऐ ख़ुदा न मांग
(ये बेबाक तर्ज़ जवाब सुनकर किरामन-कातबीन के चेहरे ज़र्द पड़ गए और वो सर से पैर तक काँपने लगे। कुछ सायों में भी हल्की जुंबिश हुई लेकिन मिला-ए-आला की इस ख़ुनुक रोशनी में तबदीली नहीं हुई।)
निदा-ए-ग़ैबी: इसके मअनी ये हुए कि तुम्हें अपने गुनाहों का इक़रार है जिन्हें तुम बयान नहीं करना चाहते, इसलिए अपने गुनाहों की पादाश के लिए तैयार होजाओ। (ग़ालिब ये सुनकर सन से हो गए। सारी ताक़त ग़ायब हो गई लेकिन उसने फिर जुर्रत करके रहमत-ए-तमाम को अपील की।)
ग़ालिब: या अर्हम उलराहमीन, तेरा फ़रमाना बरहक़, इस ज़र्रा-ए-बेमिक़दार को ताब चूँ-ओ-चरा कहाँ, अगर बारगाह-ए-जलालत से मेरे हक़ में फ़ैसला हो गया है तो मुझे जाये गुफ़्तगु कुजा लेकिन (ज़रा ज़ोर से)
नाकर्दा गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद
या रब अगर इन करदा गुनाहों की सज़ा है
(किरामन-कातबीन तो ये बेअदबी देखकर ''सुब्बूहन क़ुद्दूसन रब्बना-ओ-रब उलमलायक व अलरूह” पढ़ते हुए ख़ौफ़ के मारे सज्दे में गिर पड़े। सायों में भी यहां से वहां तक एक लर्ज़िश पैदा हो गई। कुछ निगाहें ग़ालिब के चेहरे पर गड़ी हुई थीं, कुछ नज़रें अर्श की तरफ़ थीं कि कब इस गुस्ताख ख़ाकी पर साइक़ा गिरती है लेकिन नूर पुरसुकून में कोई जुंबिश नहीं हुई। कुछ देर बाद फिर आवाज़ आई।)
निदा-ए-ग़ैबी: ग़ालिब ख़ाकी नज़ाद, हरचंद तेरी गुस्ताख़ियाँ नाक़ाबिल-ए-अफ़व हैं और उनका तक़ाज़ा ये है कि तुझे चशमज़दन में तेरे कैफ़र-ए-किरदार को पहुंचा दिया जाये ताकि दूसरों को इबरत हो लेकिन हमारी बारगाह में तेरी अदाए तुरकाना पसंद आगई है। इसलिए तू अब तक यहां नज़र आरहा है, बजुज़ यादा गोई के तूने अपने गुनाहों से बरीयत के सिलसिले में एक लफ़्ज़ भी नहीं कहा। इससे यह नतीजा निकलता है कि किरामन-कातबीन की मर्तबा फ़र्द-ए-जुर्म बिल्कुल सही-ओ-दरुस्त है।
(ग़ालिब फिर सिटपिटाए। कुछ देर सोचते रहे। आख़िर अपनी तरकश का आख़िरी तीर चलाने के लिए तैयार हो गए।)
ग़ालिब: या आफ़ी उल आफ़ईन, मुश्त-ए-ख़ाक ग़ालिब की जुर्रत कहाँ कि अहकाम-ए- ख़ुदावंदी के ख़िलाफ़ कुछ कह सके लेकिन इतना ज़रूर अर्ज़ करने की रुख़सत चाहता है कि इस अदालत रब्बानी और सलातीन अर्ज़ की अदालत में कुछ फ़र्क़ होना चाहिए।
निदा-ए-ग़ैबी: क्या मतलब है तेरा?
ग़ालिब: (गिड़गिड़ाकर) ऐ बेआसराओं के पनाह देने वाले, ये कहाँ का इन्साफ़ है कि;
पकड़े जाते हैं फ़रिश्तों के लिखे पर नाहक़
आदमी कोई हमारा दम-ए-तहरीर भी था
(किरामन-कातबीन ये सुनते ही ग़ुस्से से लाल-पीले हो गए। ऐसा मालूम होता था कि अनक़रीब ग़ालिब पर टूट पड़ेंगे। लेकिन अदालत का रोब दाब उन्हें रोके हुए है।)
निदा-ए-ग़ैबी: ग़ालिब तेरी जुर्रत-ओ-बेबाकी की हद हो गई है। होश में आ, तू किससे मुख़ातिब है।
ग़ालिब: (ख़जालत के अंदाज़ में) करम गुस्तरा;
रहमत अगर क़बूल करे क्या बईद है
शर्मिंदगी से उज़्र न करना गुनाह का
निदा-ए-ग़ैबी: गुनहगार बंदे, तेरी अदाए शर्मसारी भी हमें भा गई। तेरी कोताहियां माफ़ की गईं, जा और हमारी रहमत-ए-बेपायाँ के समरात से लुत्फ़ अंदोज़ हो, फ़ीक़ाईल और अनकाईल इसे रिज़वान के सपुर्द कर दो।
(रोशनी ग़ायब होजाती है। दो साये ग़ालिब की तरफ़ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। कहीं कहीं कोई तारा झिलमिलाता नज़र आता है और तमाम साये और किरामन-कातबीन फ़िज़ा में तहलील होजाते हैं)
ग़ालिब और रिज़वान
पस-ए-मंज़र: एक बहुत बड़ा सफ़ेद फाटक है जो नक़्श-ओ-निगार से बिल्कुल मुअर्रा है, सिर्फ़ उसके ऊपर जगमगाते हुए तारों में “दार अस्सलाम” लिखा हुआ है। फाटक के क़रीब एक नूरानी सूरत बुज़ुर्ग तस्बीह लिए मुसल्ले पर बैठे हुए हैं। एक जरीब ज़ैतूनी बाएं तरफ़ रखी हुई है। ये बुज़ुर्ग आँखें बंद किए तहलील-ओ-तस्बीह में मसरूफ़ हैं। दाने खट खट हाथ की हरकत से नीचे गिर रहे हैं।
ग़ालिब जिनमें सिरे से काया पलट हो गई है, न झुर्रियाँ हैं न रअशा, न बदन पर ज़ख़्म हैं। एक तनोमंद और सुर्ख़-ओ-सपैद जवान राना की शक्ल में फ़ीक़ाईल और अनकाईल की मय्यत में दरवाज़े की तरफ़ आरहे हैं। दोनों फ़रिश्ते मुसल्ले से ज़रा दूर रुक जाते हैं और अस्सलामु अलैकुम या रिज़वान कह कर उन पासबान दर को अपनी तरफ़ मुतवज्जा करते हैं। ग़ालिब ने रिज़वान का नाम सुनकर ज़रा तन्क़ीदी निगाह से उन्हें सर से पैर तक देखा और ज़ेर-ए-लब मुस्कुराए। रिज़वान ने आवाज़ सुनकर आँखें खोलीं और पुर रोब आवाज़ में वाअलैकुम अस्सलाम या अख़ी, कह कर जवाब दिया और कनखियों से ग़ालिब की तरफ़ देखते हुए पूछा, ये नावक़्त कैसे आना हुआ और ये तुम्हारे साथ कौन है?
अनकाईल: ये ग़ालिब हैं।
रिज़वान: ग़ालिब कौन?
(इससे पहले कि फ़रिश्ते कुछ जवाब दें ग़ालिब ने सर को झटका देते हुए निहायत सूखे मुँह से कहा)
ग़ालिब: पूछते हैं वो कि ग़ालिब कौन है
कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या
(रिज़वान ने शे’र सुनकर तीखे चितवनों से ग़ालिब को देखा लेकिन हाथ के इशारे से फिर फ़रिश्तों से पूछा कि कौन हैं?)
फ़ीक़ाईल: ये दिल्ली के मशहूर-ओ-मुस्तनद शायर रेख़्ता-ओ-फ़ारसी मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ां ग़ालिब हैं। आज ही दार उल-अमल से दार उल-जज़ा में आए हैं और अभी अभी इन्हें बारगाह-ए-इलाही से आमुर्ज़िश का परवाना इनायत हुआ है। बहुक्म रब उल-आलमीन हम इन्हें आपके सपुर्द करने आए हैं।
रिज़वान: (उछल कर) कौन असदुल्लाह ख़ां मिर्ज़ा नौशा मुनकिर जन्नत और इसकी आमुर्ज़िश... जन्नत का परवाना (अर्श की तरफ़ सर उठाकर) ख़ुदावंद तेरे इसरार से हम सब नावाक़िफ़ हैं (कुछ धीमे पड़कर और ग़ालिब की तरफ़ मुड़ते हुए) मगर तुम को ये ताक़-ए-निस्याँ का गुलदस्ता कैसे याद आया?
ग़ालिब: (तेवरियाँ बदल कर) क्या मतलब?
रिज़वान: क्या तुमने दुनिया में ये शे’र नहीं कहा था;
सताइश-गर है ज़ाहिद इस क़दर जिस बाग़-ए-रिज़वाँ का
वो इक गुलदस्ता है हम बे-ख़ुदों के ताक़-ए-निस्याँ का
ग़ालिब: याद किस मसखरे को आई और तलब किस मुँह से करता। मेरा मक़ूला तो ये है कि;
बेतलब दें तो मज़ा इसमें सवा मिलता है
वो गदा जिसको न हो ख़ू-ए-सवाल अच्छा है
रिज़वान: तो फिर इरादा क्या है?
ग़ालिब: ख़ूब! ये आपका तजाहुल-ए-आरिफ़ाना है। आपके पास भेजा किस लिए गया हूँ कि आप मुझे जन्नत की सैर कराएं।
रिज़वान: मगर तुम तो दुनिया में जन्नत को दोज़ख़ में झोंक देने पर आमादा थे।
ग़ालिब: हाय हाय जो रोना मुझे दुनिया में था वही यहां भी है। वाह री क़िस्मत।
रिज़वान: (पेच-ओ-ताब खाकर) इस जुमले के क्या मअनी?
ग़ालिब: जब तक दुनिया में रहा इस ग़म में ख़ून-ए-जिगर खाया किया कि मेरा कलाम न लोगों की समझ में आया और न उन्होंने समझने की कोशिश की। इस ख़्याल से कुछ कुछ तसल्ली हो जाया करती थी कि ख़ैर यहां न सही आलम-ए-अर्वाह में क़ुदसियों से दाद-ए-कलाम पाऊँगा, मगर देखता हूँ तो यहां भी ईं ख़ाना तमाम आफ़ताब अस्त का मज़मून नज़र आता है।
रिज़वान: (इस जवाब से कुछ जिज़बिज़ हुए और ज़रा रुक कर बोले) ख़ैर, तुम्हें जन्नत में तो लिए चलता हूँ मगर जिस फ़िक्र में आप जा रहे हैं वो कहीं नाम को भी नहीं मिलेगी, इससे जमा ख़ातिर रखिए।
ग़ालिब: आपकी ये चीसतानी तक़रीर तो मेरी समझ में आई नहीं। इस मुअम्मा को आप ही हल फ़रमाएं।
रिज़वान: (भन्नाकर) ये शे’र तुम्हारा नहीं है?
ग़ालिब: कौन सा शे’र?
रिज़वान: यही कि;
वो चीज़ जिसके लिए हमको हो बहिश्त अज़ीज़
सिवाए बादा-ए-गुलफ़ाम मुश्क-बू क्या है
ग़ालिब: जी शे’र तो मेरा है लेकिन मैंने आपसे बादा-ए-गुलफ़ाम की दरख़्वास्त की होती तब आप कहते। इस क़ब्ल अज़ मर्ग वावेला के क्या मअनी?
रिज़वान: (लाजवाब हो कर) अच्छा ख़ैर, चलो मगर एक बात का वादा करो कि सैर-ए-बाग़ के बाद कोई आएं बाएं शाएं राय नहीं दोगे।
ग़ालिब: आपको ये शुबहा कैसे पैदा हुआ?
रिज़वान: बात ये है कि तुम्हारे इस शे’र से मुतरश्शेह होता है;
कोई दुनिया में मगर बाग़ नहीं है वाइज़
ख़ुल्द भी बाग़ है ख़ैर आब-ओ-हवा और सही
कि तुम उसे भी अर्ज़ी बाग़ों का सा समझते हो।
ग़ालिब: (झल्लाकर) मैं सैर जन्नत से दर-गुज़रा, आप तो निकाह की सी शर्तें क़बूलवा रहे हैं। (एक तिलाई कार्ड बढ़ाते हुए) लीजिए परवाना जन्नत में इन पाबंदियों के साथ जन्नत में दाख़िल होने से दर-गुज़रा।
(ये कह कर चलने के लिए मुड़ते हैं)
रिज़वान: ठहरो ठहरो! बात सिर्फ़ इतनी है कि तुम आदमी ज़रा मख़दूश हो। इसलिए मुझे इतनी हिफ़ाज़ती तदाबीर इख़्तियार करना पड़ीं। वर्ना मैं तो बिला एक लफ़्ज़ कहे लोगों को जन्नत में दाख़िल कर दिया करता हूँ। मेरा बस चले तो मैं तुमको हरगिज़ बहिश्त के अंदर क़दम न रखने दूं मगर हुक्म-ए-हाकिम मर्ग-ए-मुफ़ाजात और हुक्म भी रब उल- आलमीन का, सरताबी की मजाल नहीं... अच्छा चलो।
(ग़ालिब और रिज़वान साथ साथ दरवाज़े में दाख़िल होते हैं। ग़ालिब ने महाकमाना नज़र से हर चीज़ को देखना शुरू किया और रिज़वान के साथ इधर उधर घूमते रहे। बशरे से ये मालूम होता है कि जन्नत ज़्यादा पसंद नहीं आई। उनकी नज़र टहलते टहलते दूर पर चमकते तुंद-ओ-तेज़ शोलों पर पड़ती है)
ग़ालिब: ये तेज़ रोशनी कैसी है?
रिज़वान: नार-ए-दोज़ख़ का इलतिहाब है।
ग़ालिब: (बग़ैर सोचे समझे अर्श की तरफ़ सर उठाकर) बार-ए-इलाहा, तूने अपने करम बेपायाँ और रहमत-ए-लामतनाही के सदक़े मुझ गुनहगार को वो कुछ अता किया जिसका मैं किसी तरह अह्ल नहीं था, एक आख़िरी आरज़ू मेरी और पूरी हो जाए।
निदा-ए-ग़ैबी: अब क्या चाहता है?
ग़ालिब: क्यों न फ़िरदौस में दोज़ख़ को मिला लूँ या-रब
सैर के वास्ते थोड़ी सी फ़िज़ा और सही
निदा-ए-ग़ैबी: नादान तेरी जो बात है निराली है। तेरी ये आरज़ू पूरी होने से क्यों रह जाये, जा और अपनी अहमक़ाना ख़्वाहिश का तमाशा देख।
(दोज़ख़ के शोले आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते हैं। पहले तो ग़ालिब निहायत ज़ौक़-ओ-शौक़ से उनके रक़्स-ओ-तमूज का तमाशा देखते रहे मगर जब शोले क़रीब होते गए तो ग़ालिब तपिश और इलतिहाब से परेशान होने लगे। शोले और क़रीब आए, ग़ालिब हिद्दत से घबराकर सज्दे में गिर पड़े और गिड़गिड़ाकर चीख़ने लगे।)
ग़ालिब: बार-ए-इलाहा, बस मुझमें इन शोलों से खेलने की ताब नहीं। मैं अपनी अहमक़ाना ख़्वाहिश से भर पाया। जान आफ़रीना, मुझे इस अतीए से माफ़ रख। (गर्मी से ग़ालिब बेहोश होजाते हैं और शोले आहिस्ता-आहिस्ता पीछे हट जाते हैं।)
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.