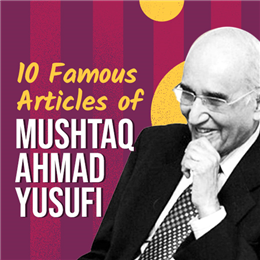हवेली
वह आदमी है मगर देखने की ताब नहीं
यादश बख़ैर! मैंने 1945 में जब क़िबला को पहले पहल देखा तो उनका हुलिया ऐसा हो गया था जैसा अब मेरा है। लेकिन ज़िक्र हमारे यार-ए-तरहदार बशारत अली फ़ारूक़ी के ख़ुस्र का है, लिहाज़ा तआ'रुफ़ कुछ उन्हीं की ज़बान से अच्छा मा'लूम होगा, हमने बारहा सुना,आप भी सुनिए।
“वह हमेशा से मेरे कुछ न कुछ लगते थे। जिस ज़माने में मेरे ख़ुस्र नहीं बने थे तो फूपा हुआ करते थे और फूपा बनने से पहले मैं उन्हें चचा हुज़ूर कहा करता था। उससे पहले यक़ीनन वह और भी कुछ लगते होंगे, मगर उस वक़्त मैंने बोलना शुरू नहीं किया था। हमारे हाँ मुरादाबाद और कानपुर में रिश्ते-नाते उबली हुई सेवइयों की तरह उलझे और पेच दर पेच गुथे होते हैं। ऐसा जलाली ऐसा मग़लूब-उल-ग़ज़ब आदमी ज़िंदगी में नहीं देखा।
बारे उनका इंतक़ाल हुआ तो मेरी उम्र आधी इधर, आधी उधर, चालीस के लगभग तो होगी। लेकिन साहब! जैसी दहशत उनकी आंखें देख कर छुट्पन में होती थी, वैसी ही न सिर्फ़ उनके आख़िरी दम तक रही, बल्कि मेरे आख़िरी दम तक भी रहेगी। बड़ी-बड़ी आंखें अपने सॉकेट से निकली पड़ती थीं। लाल सुर्ख़, ऐसी वैसी? बिल्कुल ख़ून-ए-कबूतर! लगता था बड़ी-बड़ी पुतलियों के गिर्द लाल डोरों से अभी ख़ून के फ़व्वारे छूटने लगेंगे और मेरा मुंह ख़ूनम ख़ून हो जाएगा।
हर वक़्त गुस्से में भरे रहते थे, जाने क्यों। गाली उनका तकिया कलाम थी और जो रंग तक़रीर का था वही तहरीर का। रख हाथ निकलता है धुआं मग़्ज़-ए-क़लम से। ज़ाहिर है कुछ ऐसे लोगों से भी पाला पड़ता था जिन्हें बवजूह गाली नहीं दे सकते थे। ऐसे मौक़ों पर ज़बान से तो कुछ न कहते, लेकिन चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन लाते कि क़द-ए-आदम गाली नज़र आते।
किस की शामत आई थी कि उनकी किसी भी राय से इख़्तिलाफ़ करता। इख़्तिलाफ़ तो दर-किनार, अगर कोई शख़्स महज़ डर के मारे उनकी राय से इत्तफ़ाक़ कर लेता तो फ़ौरन अपनी राय तब्दील करके उल्टे उसके सर हो जाते।
अरे साहब! बात और गुफ़तगू तो बाद की बात है। बा'ज़ औक़ात महज़ सलाम से मुश्तइल हो जाते थे! आप कुछ भी कहें, कैसी ही सच्ची और सामने की बात कहें, वह उसकी तर्दीद ज़रूर करेंगें। किसी की राय से इत्तफ़ाक़ करने में सुब्की समझते थे। उनका हर जुमला ‘नहीं’ से शुरू होता था। एक दिन कानपुर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मेरे मुंह से निकल गया कि “आज बड़ी सर्दी है, बोले नहीं, कल इससे ज़्यादा पड़ेगी।”
“वह चचा से फूपा बने और फूपा से ख़ुसर-उल-ख़द्र, लेकिन मुझे आख़िर वक़्त तक निगाह उठाकर बात करने की जसारत न हुई। निकाह के वक़्त वो क़ाज़ी के पहलू में बैठे थे।
क़ाज़ी ने मुझसे पूछा, क़ुबूल है? उनके सामने मुंह से हाँ कहने की जुर्अत न हुई। बस अपनी ठोड़ी से दो मोअद्दबाना ठोंगें मार दीं जिन्हें क़ाज़ी और क़िबला ने रिश्ता-ए-मुनाकिहत के लिए नाकाफ़ी समझा।
क़िबला कड़क कर बोले, लौन्डे! बोलता क्यों नहीं? डांट से मैं नर्वस हो गया। अभी क़ाज़ी का सवाल भी पूरा नहीं हुआ था कि मैं ने जी हां! क़ुबूल है कह दिया।
आवाज़ यकलख़्त इतने ज़ोर से निकली कि मैं ख़ुद चौंक पड़ा। क़ाज़ी उछल कर सेहरे में घुस गया। हाज़रीन खिल-खिला के हंसने लगे। अब क़िबला इस पर भन्ना रहे हैं कि इतने ज़ोर की ‘हाँ’ से कि बेटी वालों की हेटी होती है। बस, तमाम उम्र उनका यही हाल रहा और तमाम उम्र मैं कर्ब-ए-क़राबतदारी व क़ुर्बत-ए-क़हरी दोनों में मुब्तिला रहा।
‘हालाँकि इकलौती बेटी, बल्कि इक्लौती औलाद थी और बीवी को शादी के बड़े अरमान थे, लेकिन क़िबला ने माइयों के दिन ऐ'न उस वक़्त जब मेरा रंग निखारने के लिए उबटन मिलाया जा रहा था, कहला भेजा कि दूल्हा मेरी मौजूदगी में अपना मुंह सेहरे से बाहर नहीं निकालेगा। दो सौ क़दम पहले सवारी से उतर जाएगा और पैदल चल कर अक़्द गाह तक आएगा।
अक़्द गाह उन्होंने इस तरह कहा कि जैसे अपने फैज़ साहब क़त्ल गाह का ज़िक्र करते हैं और सच तो यह है कि क़िबला की दहशत दिल में ऐसी बैठ गई थी कि मुझे तो उ'रूसी छपर खट भी फांसी घाट लग रहा था। उन्होंने यह शर्त भी लगाई कि बराती पुलाव-ज़र्दा ठूंसने के बाद यह हर्गिज़ नहीं कहेंगे कि गोश्त कम डाला और शक्कर ड्योढ़ी नहीं पड़ी। ख़ूब समझ लो, मेरी हवेली के सामने बैंड-बाजा हरगिज़ नहीं बजेगा और तुम्हें रंडी नचवानी है तो Over my dead body अपने कोठे पर नचवाओ।
किसी ज़माने में राजपूतों और अरबों में लड़की की पैदाईश नहूसत और क़हर-ए-इलाही की निशानी तसव्वुर की जाती थी। उनकी ग़ैरत यह कैसे गवारा कर सकती थी कि उनके घर बरात चढ़े। दामाद के ख़ौफ़ से वह नौज़ाईदा लड़की को ज़िन्दा गाड़ आते थे। क़िबला इस वहशियाना रस्म के ख़िलाफ़ थे। वह दामाद को ज़िन्दा गाड़ देने के हक़ में थे।
‘चेहरे, चाल और तेवर से कोतवाल-ए-शहर लगते थे। कौन कह सकता था कि बांसमंडी में उनकी इमारती लकड़ी की एक मामूली सी दुकान है। निकलता हुआ क़द। चलते तो क़द, सीना और आंखें, तीनों ब यक-वक़्त निकाल कर चलते थे। अरे साहब! क्या पूछते हैं, अव्वल तो उनके चेहरे की तरफ़ देखने की हिम्मत नहीं होती थी, और कभी जी कड़ा कर के देख भी लिया तो बस लाल भभूका आंखें ही आंखें नज़र आती थीं, निगह-ए-गर्म से इक आग टपकती है असद।
रंग गंदुमी, आप जैसा, जिसे आप उस गंदुम जैसा बताते हैं जिसे खाते ही हज़रत आदम, ब-यक बीवी व दो गोश जन्नत से निकाल दिए गए। जब देखो झल्लाते तनतनाते रहते। मिज़ाज, ज़बान और हाथ किसी पर क़ाबू न था।
दायमी तैश से लर्ज़ा बर अंदाम रहने के सबब ईंट, पत्थर, लाठी, गोली, गाली किसी का भी निशाना ठीक नहीं लगता था। गुछी-गुछी मूंछें जिन्हें गाली देने से पहले और बाद में ताव देते। आख़िरी ज़माने में भवों को भी बल देने लगे। गठा हुआ कसरती बदन मलमल के कुर्ते से झलकता था। चुनी हुई आस्तीन और उससे भी महीन चुनी हुई दो पल्ली टोपी।
गर्मियों में ख़स का इत्र लगाते। केकरी की सिलाई का चूड़ीदार पाजामा। चूड़ियों की ये कसरत कि पाजामा नज़र नहीं आता था। धोबी अलगनी पर नहीं सुखाता था। अलाहदा बांस पर दस्ताने की तरह चढ़ा देता था। आप रात के दो बजे भी दरवाज़ा खटखटा कर बुलाएँ तो चूड़ीदार ही में बरामद होंगे।
“वल्लाह! मैं तो यह तसव्वुर करने की भी जुर्अत नहीं कर सकता कि दाई ने उन्हें चूड़ीदार के बग़ैर देखा होगा। भरी-भरी पिंड्लियों पर ख़ूब खब्ता था। हाथ के बुने रेश्मी ईज़ारबंद में चाबियोँ का गुच्छा छनछनाता रहता। जो ताले बरसों पहले बेकार हो गए थे उनकी चाबियाँ भी उस गुच्छे में महफ़ूज़ थीं। हद ये कि उस ताले की भी चाबी थी जो पाँच साल पहले चोरी हो गया था। महल्ले में उस चोर का बरसों चर्चा रहा, इसलिए कि चोर सिर्फ़ ताला, पहरा देने वाला कुत्ता और उनका शजरा-ए-नस्ब चुरा कर ले गया था।
फ़रमाते थे कि इतनी ज़लील चोरी कोई अ'ज़ीज़ रिश्तेदार ही कर सकता है। आख़िरी ज़माने में यह ईज़ारबंदी गुच्छा बहुत वज़नी हो गया था और मौक़ा बे मौक़ा फ़िल्मी गीत के बाज़ूबंद की तरह खुल खुल जाता। कभी झुक कर गर्मजोशी से मुसाफ़ा करते तो दूसरे हाथ से ईज़ारबंद थामते। मई-जून में टेम्प्रेचर 110 हो जाता और मुंह पर लू के थप्पड़ से पड़ने लगते तो पाजामे से एयर-कंडिशिनिंग कर लेते। मतलब ये कि चूड़ियों को घुट्नों-घुट्नों पानी में भिगो कर, सर पर अंगोछा डाले, तर्बूज़ खाते।
ख़स-ख़ाना व बर्फाब कहाँ से लाते। उसके मोहताज भी न थे। कितनी ही गर्मी पड़े, दुकान बंद नहीं करते थे। कहते थे, मियाँ! ये तो बिज़नेस, पेट का धंधा है। जब चमड़े की झोंपड़ी (पेट) में आग लग रही हो तो क्या गर्मी क्या सर्दी। लेकिन ऐसे में कोई शामत का मारा गाहक आ निकले तो बुरा भला कहके भगा देते थे। इसके बावजूद वह खिंचा-खिंचा दोबारा उन्हीं के पास आता था, इसलिए कि जैसी उम्दा लकड़ी वो बेचते थे, वैसी सारे कानपुर में कहीं नहीं मिलती थी।
फ़रमाते थे, दाग़ी लकड़ी बंदे ने आज तक नहीं बेची। लकड़ी और दाग़दार? दाग़ तो दो ही चीज़ो पर सजता है दिल और जवानी।
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.