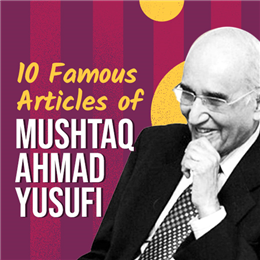हुए मर के हम जो रुस्वा
अब तो मा'मूल सा बन गया है कि कहीं ता'ज़ियत या तज्हीज़-व-तकफ़ीन में शरीक होना पड़े तो मिर्ज़ा को ज़रूर साथ ले लेता हूँ। ऐसे मौक़ों पर हर शख़्स इज़्हार-ए-हम-दर्दी के तौर पर कुछ न कुछ ज़रूर कहता है।
क़तअ'-ए-तारीख़-ए-वफ़ात ही सही। मगर मुझे न जाने क्यूँ चुप लग जाती है, जिससे बा'ज़ औक़ात न सिर्फ़ पसमांदिगान को बल्कि ख़ुद मुझे भी बड़ा दुख होता है। लेकिन मिर्ज़ा ने चुप होना सीखा ही नहीं। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि सही बात को ग़लत मौक़े पर बे-दग़दगा कहने की जो खुदा दाद सलाहियत उन्हें वदीअ'त हुई है वह कुछ ऐसी तक़रीब में गुल खिलाती है। वह घुप्प अंधेरे में सर-ए-रहगुज़र चराग़ नहीं जलाते, फुलझड़ी छोड़ते हैं, जिससे बस उनका अपना चेहरा रात के सियाह फ़्रेम में जगमग-जगमग करने लगता है और फुलझड़ी का लफ्ज़ तो यूँ ही मरव्वत में क़लम से निकल गया वर्ना होता ये है कि,
जिस जगह बैठ गए आग लगा कर उठ्ठे
इसके बा-वस्फ़ वह ख़ुदा के उन हाज़िर-व-नाज़िर बंदों में से हैं जो महल्ले की हर छोटी-बड़ी तक़रीब में, शादी हो या ग़मी, मौजूद होते हैं। बिल्खुसूस दा'वतों में सबसे पहले पहुंचते और सबके बा'द उठते हैं। इस अंदाज़-ए-नशिस्त-ओ-बर्ख़ास्त में एक खुला फ़ायदा ये देखा कि वह बारी-बारी सबकी ग़ीबत कर डालते हैं। उनकी कोई नहीं कर पाता है।
चुनांचे इस सनीचर की शाम को भी मेवा शाह क़ब्रिस्तान में मेरे साथ थे। सूरज इस शहर-ए-ख़मोशां को जिसे हज़ारों बंदगान-ए-ख़ुदा ने मर-मर के बसाया था, लाल अंगारा सी आँख से देखता–देखता अंग्रेज़ो के इक़बाल की तरह गूरूब हो रहा था। सामने बेरी के दरख़्त के नीचे एक ढांचा क़ब्र-बदर पड़ा था। चारों तरफ मौत की अ'मलदारी थी और सारा क़ब्रिस्तान ऐसा उदास और उजाड़ था जैसे किसी बड़े शहर का बाज़ार इतवार को।
सभी रंजीदा थे। (बक़ौल मिर्ज़ा,दफ़न के वक़्त मैय्यत के सिवा सब रंजीदा होते हैं।) मगर मिर्ज़ा सबसे अलग-थलग एक पुराने कत्बे पर नज़रें गाड़े मुस्कुरा रहे थे।
चंद लम्हों बाद मेरे पास आए और मेरी पसलियों में अपनी कोहनी से आंकस लगाते हुए उस कत्बे तक ले गए, जिस पर मिन्जुम्ला तारीख़-ए-पैदाइश-व-पेन्शन, मुअल्लिद-ओ-मस्कन, वल्दियत व ओ'ह्दा (ए'ज़ाज़ी मजिस्ट्रेट दर्जा सोम) आसूद-ए-लहद की तमाम डिग्रियाँ मअ'-डिवीज़न और यूनीवर्सिटी के नाम कुंदा थीं और आख़िर में, निहायत जली हुरूफ़ में, मुंह फेरकर जाने वाले को बज़रिय-ए-क़तअ' बशारत दी गई थी कि अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द उसका भी यही हश्र होने वाला है।
मैंने मिर्ज़ा से कहा, “ये लौह-ए-मज़ार है या मुलाज़िमत की दर्ख़वास्त? भला डिग्रियाँ, ओ'ह्दा और वल्दियत वग़ैरा लिखने का क्या तुक था?”
उन्होंने हस्ब-ए-आ'दत बस एक लफ़्ज़ पकड़ लिया। कहने लगे, “ठीक कहते हो, जिस तरह आजकल किसी की उम्र या तनख़्वाह दरयाफ़्त करना बुरी बात समझी जाती है, उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह बीस साल बाद किसी की वल्दियत पूछना बदअख़लाक़ी समझी जाएगी!”
अब मुझे मिर्ज़ा की चूंचाल तबीयत से ख़तरा महसूस होने लगा। लिहाज़ा उन्हें वल्दियत के मुसतक़्बिल पर मुस्कुराता छोड़ कर मैं आठ-दस क़ब्र दूर एक टुकड़ी में शामिल हो गया, जहाँ एक साहब जन्नत मकानी के हालात-ए-ज़िंदगी मज़े ले-ले कर बयान कर रहे थे।
वह कह रहे थे कि ख़ुदा ग़रीक़-ए-रहमत करे, मरहूम ने इतनी लम्बी उम्र पाई कि उनके क़रीबी अइ'ज़्ज़ा दस-पंद्रह साल से उनकी इंशोरेंस पालिसी की उम्मीद में जी रहे थे। उन उम्मीदवारों में बेश्तर को मरहूम ख़ुद अपने हाथ से मिट्टी दे चुके थे। बक़िया को यक़ीन हो गया था कि मरहूम ने आब-ए-हयात न सिर्फ़ चखा है बल्कि डुगडुगा के पी चुके हैं।
रावी ने तो यहाँ तक बयान किया कि अज़-बस कि मरहूम शुरू से रख रखाव के हद दर्जा क़ाएल थे, लिहाज़ा आख़िर तक इस सेहत बख़्श अ'क़ीदे पर क़ायम रहे कि छोटों को ता'ज़ीमन पहले मरना चाहिए। अल्बत्ता इधर चंद बर्सों से उनको फ़लक-ए-कज रफ़्तार से ये शिकायत हो चला थी कि अफ़सोस अब कोई दुश्मन ऐसा बाक़ी नहीं रहा, जिसे वह मरने की बददुआ दे सकें।
उनसे कटकर मैं एक दूसरी टोली में जा मिला। यहाँ मरहूम के एक शनासा और मेरे पड़ोसी उनके गिल्र्ड़ लड़के को सब्र-ए-जमील की तल्क़ीन और गोल मोल अलफ़ाज़ में नाएम-उल-बदल की दुआ देते हुए फ़रमा रहे थे कि बर्ख़ुर्दार! ये मरहूम के मरने के दिन नहीं थे।
हालाँकि पाँच मिनट पहले यही साहब, जी हाँ, यही साहब मुझसे कह रहे थे कि मरहूम ने पाँच साल क़ब्ल दोनों बीवियों को अपने तीसरे सेहरे की बहारें दिखाई थी और ये उनके मरने के नहीं, डूब मरने के दिन थे।
मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने उँगलियों पर हिसाब लगा कर कानाफूसी के अंदाज़ में ये तक बताया कि तीसरी बीवी की उम्र मरहूम की पेंशन के बराबर है। मगर है बिल्कुल सीधी और बेज़बान। उस अल्लाह की बंदी ने कभी पलट कर नहीं पूछा था कि तुम्हारे मुंह के दाँत नहीं हैं, मगर मरहूम इस ख़ुश फ़हमी में मुब्तिला थे कि उन्होंने महज़ अपनी दुआ'ओं के ज़ोर से मौसूफ़ा का चाल चलन क़ाबू में रखा है।
अल्बत्ता बियाहता बीवी से उनकी कभी नहीं बनी। भरी जवानी में भी मियाँ-बीवी 62 के हिंदसे की तरह एक दूसरे से मुंह फेरे रहे और जब तक जिये, एक दूसरे के अअ'साब पर सवार रहे। मम्दूहा ने मशहूर कर रखा था कि (ख़ुदा उनकी रूह को न शरमाए) मरहूम शुरू से ही ऐसे ज़ालिम थे कि वलीमे का खाना भी मुझ नई नवेली दुल्हन से पकवाया।
मैंने गुफ़्तगू का रुख़ मोड़ने के ख़ातिर गुंजान क़ब्रिस्तान की तरफ़ इशारा करते हुए कहा कि देखते ही देखते चप्पा-चप्पा आबाद हो गया। मिर्ज़ा हस्ब-ए-मा'मूल फिर बीच में कूद पड़े। कहने लगे, देख लेना वह दिन ज़्यादा दूर नहीं जब कराची में मुर्दे को खड़ा गाड़ना पड़ेगा और नायलोन के रेडीमेड कफ़न में ऊपर ज़िप (zip) लगेगी ताकि मुंह देखने दिखाने में आसानी रहे।
मेरी तबीअ'त इन बातों से ऊबने लगी तो एक दूसरे गोल में चला गया, जहाँ दो नौजवान सितारे के ग़िलाफ़ जैसी पतलूने चढ़ाए चहक रहे थे। पहले “टेडी बॉय” की पीली क़मीज़ पर लड़कियों की ऐसी वाहियात तस्वीरें बनी हुई थीं कि नज़र पड़ते ही सिक़्क़ा आदमी लाहौल पढ़ने लगते थे और हमने देखा कि हर सिक़्क़ा आदमी बार-बार लाहौल पढ़ रहा था। दूसरे नौजवान को मरहूम की बेवक़्त मौत से वाक़ई दिली सदमा पहुँचा था, क्योंकि उसका सारा “वीक-एन्ड”चौपट हो गया था।
चोंचों और चुहलों का ये सिलसिला शायद कुछ देर और जारी रहता कि इतने में एक साहब ने हिम्मत करके मरहूम के हक़ में पहला कल्मा-ए-ख़ैर कहा और मेरी जान में जान आई। उन्होंने सही फ़रमाया, “यूँ आंख बंद होने के बाद लोग कीड़े निकालने लगें, ये और बात है, मगर ख़ुदा उनकी क़ब्र को अम्बरी करे, मरहूम बिला शुबहा साफ दिल, नेक नियत इंसान थे और नेक नाम भी। ये बड़ी बात है।”
“नेक नामी क्या कलाम है। मरहूम अगर यूँ ही मुंह हाथ धोने बैठ जाते तो सब यही समझते कि वुज़ू कर रहे...” जुम्ला ख़त्म होने से पहले मद्दाह की चमकती चंदिया यका-यक एक धंसी हुई क़ब्र में ग़ुरूब हो गई।
इस मक़ाम पर एक तीसरे साहब ने (जिन से मैं वाक़िफ़ नहीं) “रूए-सुख़न किसी तरफ़ हो तो रू-सियाह”वाले लहजे में नेक नियती और साफ़ दिली का तजज़िया करते हुए फ़रमाया कि बा'ज़ लोग अपनी पैदाइशी बुज़्दिली के सबब तमाम उम्र गुनाहों से बचते रहते हैं। इसके बरअ'क्स बा'ज़ों के दिल-ओ-दिमाग़ वाक़ई आईने की तरह साफ़ होते हैं...या'नी नेक ख़याल आते हैं और गुज़र जाते हैं।
शामत-ए-आ'माल कि मेरे मुंह से निकल गया, “नियत का हाल सिर्फ़ ख़ुदा पर रोशन है मगर अपनी जगह यही क्या कम है कि मरहूम सबके दुख-सुख में शरीक और अदना से अदना पड़ोसी से भी झुक कर मिलते थे।”
अरे साहब! ये सुनते ही वह साहब तो लाल भभूका हो गए। बोले, “हज़रत! मुझे ख़ुदाई का दा'वा तो नहीं, ता-हम इतना ज़रूर जानता हूँ कि अक्सर बूढ़े ख़ुर्रांट अपने पड़ोसियों से महज़ इस ख़याल से झुक कर मिलते है कि अगर वह ख़फ़ा हो गए तो कंधा कौन देगा।”
ख़ुशक़िस्मती से एक खुदा तरस ने मेरी हिमायत की। मेरा मतलब है मरहूम की हिमायत की। उन्होंने कहा कि मरहूम ने, माशा-अल्लाह, इतनी लम्बी उम्र पाई, मगर सूरत पर ज़रा नहीं बरसती थी। चुनांचे सिवाए कंपटियों के और बाल सफ़ेद नहीं हुए। चाहते तो ख़िज़ाब लगा के खुर्दों में शामिल हो सकते थे मगर तबियत ऐसी क़लंदराना पायी थी कि ख़िज़ाब का कभी झूटों भी ख़याल नहीं आया।
वह साहब सचमुच फट पड़े, “आपको ख़बर भी है, मरहूम का सारा सर पहले निकाह के बाद ही सफ़ेद काला हो गया था। मगर कंपटियों को वह क़स्दन सफ़ेद रहने देते थे ताकि किसी को शुबहा न गुज़रे कि ख़िज़ाब लगाते हैं। सिल्वर ग्रे क़ल्में! ये तो उनके मेकअप में एक नेचुरल टच था!”
“अरे साहब! इसी मस्लेहत से उन्होंने अपना एक मस्नूई दाँत भी तोड़ रखा था”, एक दूसरे बदगो ने ताबूत में आख़िरी कील ठोंकी।
“कुछ भी सही, वह उन खूसटों से हज़ार दर्जे बेहतर थे जो अपने पोपले मुंह और सफ़ेद बालों की दाद छोटों से यूँ तलब करते हैं, गोया ये उनकी ज़ाती जद्दोजहद का सम्रा है।” मिर्ज़ा ने बिगड़ी बात बनाई।
उनसे पीछा छुड़ा कर कच्ची-पक्की क़ब्रें फांदता मैं मुंशी सनाउल्लाह के पास जा पहुँचा, जो एक कत्बे से टेक लगाए बेरी के हरे-हरे पत्ते कचर-कचर चबा रहे थे और इस अम्र पर बार-बार अपनी हैरानी का इज़्हार फ़रमा रहे थे कि अभी पर्सों तक तो मरहूम बातें कर रहे थे। गोया उनके अपने आदाब-ए-जान की रू से मरहूम को मरने से तीन चार साल पहले चुप होना चाहिए था।
भला मिर्ज़ा ऐसा मौक़ा कहाँ ख़ाली जाने देते थे। मुझे मुख़ातिब करके कहने लगे, याद रखो! याद रखो कि मर्द की आँख और औरत की ज़बान का दम सबसे आख़िर में निकलता है।
यूँ तो मिर्ज़ा के बयान के मुताबिक़ मरहूम की बेवाएँ भी एक दूसरे के छाती पर दोहत्तड़ मार-मार कर बैन कर रही थीं, लेकिन मरहूम के बड़े नवासे ने जो पांच साल से बे-रोज़गार था, चीख़-चीख़ कर अपना गला बिठा लिया था। मुंशी जी बेरी के पत्तों का रस चूस-चूस कर जितना उसे समझाते पुचकारते, उतना ही वह मरहूम की पेंशन को याद करके धाड़े मार-मार कर रोता।
उसे अगर एक तरफ़ हज़रत इज़राईल से गिला था कि उन्होंने तीस तारीख़ तक इंतज़ार क्यूँ न किया तो दूसरी तरफ़ ख़ुद मरहूम से भी सख़्त शिकवा था,
क्या तेरा बिगड़ता जो न मरता कोई दिन और?
इधर मुंशी जी का सारा ज़ोर इस फ़लसफ़े पर था कि बरख़ुर्दार! ये सब नज़र का धोका है। दर हक़ीक़त ज़िंदगी और मौत में कोई फ़र्क़ नहीं। कम-अज़-कम एशिया में। नीज़ मरहूम बड़े नसीबावर निकले कि दुनिया के बखेड़ों से इतनी जल्दी आज़ाद हो गए। मगर तुम हो कि नाहक़ अपनी जवान जान को हल्कान किए जा रहे हो। यूनानी मिस्ल है कि,
वही मरता है जो महबूब-ए-ख़ुदा होता है
हाज़्रीन अभी दिल ही दिल में हसद से जले जा रहे थे कि हाय, मरहूम की आई हमें क्यूँ न आ गई कि दम भर को बादल के एक फ़ाल्सई टुकड़े ने सूरज को ढक लिया और हल्की-हल्की फुवार पड़ने लगी।
मुंशी जी ने यकबारगी बेरी के पत्तों का फूंक निगलते हुए उसको मरहूम के बहिश्ती होने का ग़ैबी शगुन क़रार दिया, लेकिन मिर्ज़ा ने भरे मजमे में सर हिला-हिलाकर उस पेशगोई से इख़्तिलाफ़ किया।
मैंने अलग ले जाकर वजह पूछी तो इरशाद हुआ, “मरने के लिए सनीचर का दिन बहुत मन्हूस होता है।”
लेकिन सबसे ज़्यादा पतला हाल मरहूम के एक दोस्त का था, जिनके आंसू किसी तरह थमने का नाम नहीं लेते थे कि उन्हें मरहूम से देरीना रब्त-व-रफ़ाक़त का दावा था। इसलिए रूहानी यकजहती के सुबूत में अक्सर इस वाक़ए का ज़िक्र करते कि बग़दादी क़ाएदा ख़त्म होने से एक दिन पहले हम दोनों ने एक साथ सिगरेट पीना सीखा था।
चुनांचे उस वक़्त से भी साहिब-ए-मौसूफ़ के बैन से साफ़ टपकता था कि मरहूम किसी सोचे समझे मन्सूबे के तहत दाग़ बल्कि दग़ा दे गए और बग़ैर कहे-सुने पीछा छुड़ा के चुप चुपाते जन्नत-उल-फ़िर्दौस को रवाना हो गए... अकेले ही अकेले!
बाद में मिर्ज़ा ने सराहतन बताया कि बाहमी इख़्लास-व-यगानगत का ये आ'लम था कि मरहूम ने अपनी मौत से तीन माह पेश्तर मौसूफ़ से दस हज़ार रूपये सिक्क-ए-राइज-उल-वक़्त बतौर-ए-क़र्ज़े-ए-हस्ना लिये और वह तो कहिए, बड़ी ख़ैरियत हुई कि इसी रक़म से तीसरी बीवी का मेह्र-ए-मुअ'ज्जल बेबाक़ कर गए वर्ना क़यामत में अपने सास-ससुर को क्या मुंह दिखाते।
(2)
आप ने अक्सर देखा होगा कि गुन्जान महल्लों में मुख़्तलिफ़ बल्कि मुतज़ाद तक़रीबें एक दूसरे में बड़ी ख़ूबी से ज़म हो जाती हैं, गोया दोनों वक़्त मिल रहे हों। चुनांचे अक्सर हज़रात दा’वत-ए-वलीमा में हाथ धोते वक़्त चेहल्लुम की बिर्यानी की डकार लेते, या सोयम में शबीना फ़तूहात की लज़ीज़ दास्तान सुनाते पकड़े जाते हैं।
लज़्ज़त-ए-हमसायगी का नक़्शा भी अक्सर देखने में आया है कि एक क्वाटर में हनीमून मनाया जा रहा है तो रत जग्गा दीवार के उस तरफ़ हो रहा है और यूँ भी होता है कि दाएँ तरफ वाले घर में आधी रात को क़व्वाल बिल्लियाँ लड़ा रहे हैं, तो हाल बाएँ तरफ वाले घर में आ रहा है।
आमदनी हमसाए की बढ़ती है तो इस ख़ुशी में नाजाएज़ ख़र्च हमारे घर का बढ़ता है और ये सानिहा भी बारहा गुज़रा कि मछली तरहदार पड़ोसन ने पकाई और
मुद्दतों अपने बदन से तेरी ख़ुश्बू आई।
इस तक़रीबी घपले का सही अंदाज़ा मुझे दूसरे दिन हुआ जब एक शादी की तक़रीब में तमाम वक़्त मरहूम की वफ़ात-ए-हस्रत आयात के तज़्किरे होते रहे। एक बुज़ुर्ग ने, कि सूरत से ख़ुद पा बा रकाब मा'लूम होते थे, तश्वीशनाक लहजे में पूछा, आख़िर हुआ क्या?
जवाब में मरहूम के एक हम-जमाअ'त ने इशारों कनायों में बताया कि मरहूम जवानी में इश्तिहारी अम्राज़ का शिकार हो गए। अधेड़ उम्र में जिन्सी तवन्नुस में मुब्तिला रहे, लेकिन आख़िरी अय्याम में तक़्वा हो गया था।
“फिर भी आख़िर हुआ क्या?” पा ब रकाब मर्द बुज़ुर्ग ने अपना सवाल दोहराया।
“भले चंगे थे, अचानक एक हिच्की आई और जाँ-बहक़ हो गए”, दूसरे बुज़ुर्ग ने अंगोछे से एक फ़र्ज़ी आँसू पोंछते हुए जवाब दिया।
“सुना है चालीस बरस से मर्ज़-उल-मौत में मुब्तिला थे”, एक साहब ने सूखे से मुंह से कहा।
“क्या मतलब?”
“चालीस बरस से खांसी में मुब्तिला थे और आख़िर इसी में इंतिक़ाल फ़रमाया।”
“साहब! जन्नती थे कि किसी अजनबी मर्ज़ में नहीं मरे। वर्ना अब तो मेडिकल साइंस की तरक़्क़ी का ये हाल है कि रोज़ एक नया मर्ज़ ईजाद होता है।”
“आपने गांधी गॉर्डन में उस बोहरी सेठ को कार में चहल क़दमी करते नहीं देखा जो कहता है कि मैं सारी उम्र दमे पर इतनी लागत लगा चुका हूँ कि अब अगर किसी और मर्ज़ में मरना पड़ा तो ख़ुदा की क़सम, ख़ुदकुशी कर लूँगा।” मिर्ज़ा चुटकुलों पर उतर आए।
“वल्लाह! मौत तो ऐसी हो! (सिस्की) मरहूम के होंटो पर आ'लम-ए-सुक्रात में भी मुस्कुराहट खेल रही थी।”
“अपने क़र्ज़ ख़्वाहों का ख़याल आ रहा होगा”, मिर्ज़ा मेरे कान में फुसफुसाए।
“गुनहगारों का मुंह मरते वक़्त सुअर जैसा हो जाता है, मगर चश्म-ए-बद्दूर। मरहूम का चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ था।”
“साहब! सलेटी रंग का गुलाब हमने आज तक नहीं देखा”, मिर्ज़ा की ठंडी-ठंडी नाक मेरे कान को छूने लगी और उनके मुंह से कुछ ऐसी आवाज़ें निकलने लगीं जैसे कोई बच्चा चमकीले फ़र्नीचर पर गीली ऊँगली रगड़ रहा हो।
असली अलफ़ाज़ तो ज़ेह्न से मह्व हो गए, लेकिन इतना अब भी याद है कि अंगोछे वाले बुज़ुर्ग ने एक फ़लसफ़ियना तक़रीर कर डाली, जिसका मफ़हूम कुछ ऐसा ही था कि जीने का क्या है। जीने को तो जानवर भी जी लेते हैं, लेकिन जिसने मरना नहीं सीखा, वह जीना क्या जाने। एक मुतबस्सुम ख़ुद-सुपुर्दगी, एक बे-ताब आमादगी के साथ मरने के लिए एक उम्र का रियाज़ दरकार है। ये बड़े ज़र्फ़ और बड़े हौसले का काम है, बंदा नवाज़!
फिर उन्होंने बेमौत मरने के खानदानी नुस्ख़े और हंस्ते-खेलते अपनी रूह क़ब्ज़ कराने के पैंतरे कुछ ऐसे उस्तादाना तेवर से बयान किए कि हमें अताई मरने वालों से हमेशा-हमेशा के लिए नफ़रत हो गई।
ख़ातम-ए-कलाम इस पर हुआ कि मरहूम ने किसी रूहानी ज़रिए से सुन-गुन पा ली थी कि मैं सनीचर को मर जाऊँगा।
“हर मरने वाले के मुतअ'ल्लिक़ यही कहा जाता है”, बातस्वीर क़मीज़ वाला टेडी बॉय बोला कि, “वह सनीचर को मर जाएगा?” मिर्ज़ा ने उस बदलगाम का मुंह बंद किया।
अंगोछे वाले बुज़ुर्ग ने शय-ए-मज़्कूर से पहले अपने नरी के जूते की गर्द झाड़ी, फिर पेशानी से पसीना पोंछते हुए मरहूम के इरफ़ान-ए-मर्ग की शहादत दी कि जन्नत-मकानी ने विसाल से ठीक चालीस दिन पहले मुझसे फ़रमाया था कि इंसान फ़ानी है!
इंसान के मुतअ'ल्लिक़ ये ताज़ा ख़बर सुनकर मिर्ज़ा मुझे तख़्लिए में ले गए। दरअसल तख़लिए का लफ़्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था, वर्ना जिस जगह वह मुझे धकेलते हुए ले गए, वह ज़नाने और मर्दाने के सरहद पर एक चबूतरा था, जहाँ एक मीरासन घूँघट निकाले ढोलक पर गालियाँ गा रही थी।
वहाँ उन्होंने इस शग़फ़ की जानिब इशारा करते हुए जो मरहूम को अपनी मौत से था, मुझे आगाह किया कि ये ड्रामा तो जन्नत मकानी तो अक्सर खेला करते थे। आधी-आधी रातों को अपनी होने वाली बेवाओं को जगा-जगा कर धमकियाँ देते कि मैं अचानक अपना साया तुम्हारे सर से उठा लूँगा। चश्मे ज़दन में मांग उजाड़ दूँगा।
अपने बे तकल्लुफ़ दोस्तों से भी कहा करते कि वल्लाह! अगर ख़ुदकुशी जुर्म न होती तो कभी का अपने गले में फंदा डाल लेता। कभी यूँ भी होता कि अपने आप को मुर्दा तसव्वुर करके डकारने लगते और चश्म-ए-तसव्वुर से मंझली के सोंटा से हाथ देख कर कहते, बख़ुदा! मैं तुम्हारा रंडापा नहीं देख सकता।
मरने वाले की एक-एक ख़ूबी बयान करके ख़ुश्क सिस्कियाँ भरते और सिस्कियों के दर्मियान सिगरेट की कश लगाते और जब इस अ'मल से अपने ऊपर रिक़्क़त तारी कर लेते तो रूमाल से बार-बार आंख के बजाए अपनी डबडबाई हुई नाक पोंछते जाते, कपकपाते हुए हाथ से तीनों बेवाओं की मांग में यके बाद दीगरे ढेरों अफ़्शाँ भरते।
इससे फ़ारिग़ होकर हर एक को कोहनियों तक महीन-महीन, फंसी-फंसी चूड़ियाँ पहनाते (ब्याहता को चार चूड़ियाँ कम पहनाते थे)।
हालाँकि इससे पहले भी मिर्ज़ा को कई मर्तबा टोक चुका था कि ख़ाक़ानि-ए-हिन्द उस्ताद ज़ौक़ हर क़सीदे के बाद मुंह भर-भर के कुल्लियाँ किया करते थे। तुम पर हर कलमे, हर फ़िक़रे के बाद वाजिब हैं लेकिन इस उक़्त मरहूम के बारे में ये ऊल-जुलूल बातें और ऐसे व अश्गाफ़ लेहजे में सुनकर मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही मुनग़्ग़ज़ हो गई।
मैंने दूसरों पर ढाल कर मिर्ज़ा को सुनाई, “ये कैसे मुसलमान हैं मिर्ज़ा! दुआ-ए-मग़्फ़िरत नहीं करते, न करें। मगर ऐसी बातें क्यों बनाते हैं ये लोग?”
“ख़लक-ए-ख़ुदा की ज़बान किसने पकड़ी है। लोगों का मुंह तो चेहल्लुम के निवाले ही से बंद होता है।”
(3)
मुझे चेहल्लुम में भी शिरकत का इत्तफ़ाक़ हुआ लेकिन सिवाए एक नेक-तीनत मौलवी साहब के जो पुलाव के लिए चावलों की लम्बाई और गिलावट को ठेठ जन्नती होने की निशानी क़रार दे रहे थे, बक़िया, हज़रात की गुल अफ़शानी-ए-गुफ़्तार का वही अंदाज़ था, वही जग-जगे थे, वही चहचहे!
एक बुज़ुर्गवार जो नान-क़ोरमे के हर आतिशीं लुक़्मे के बाद आधा-आधा गिलास पानी पीकर क़ब्ल अज़ वक़्त सैर बल्कि सैराब हो गए थे, मुंह लाल करके बोले कि मरहूम की औलाद निहायत नाख़ल्फ़ निकली। मरहूम-व-मग़फ़ूर शद-ओ-मद से वसियत फ़रमा गए थे कि मेरी मिट्टी बग़दाद ले जाई जाए लेकिन ना-फ़रमान औलाद ने उनकी आख़िरी ख़्वाहिश का ज़रा पास न किया।
इस पर एक मुंह फट पड़ोसी बोल उट्ठे, “साहब! ये मरहूम की सरासर ज़्यादती थी कि उन्होंने ख़ुद तो तादम-ए-मर्ग म्युनिस्पल हुदूद से क़दम बाहर नहीं निकाला। हद ये है कि पास्पोर्ट तक नहीं बनवाया और...”
एक वकील साहब ने क़ानूनी मुशग़ाफ़ी की “बैन-उल-अक़वामी क़ानून के ब-मुजिब पास्पोर्ट के शर्त सिर्फ़ ज़िंदों के लिए है। मुर्दे पास्पोर्ट के बग़ैर भी जहाँ चाहें जा सकते हैं।”
“ले जाए जा सकते हैं”, मिर्ज़ा फिर लुक़्मा दे गए।
“मैं कह रहा था कि यूँ तो हर मरने वाले के दिल में ये ख़्वाहिश सुलगती रहती है कि मेरा कांसी कि मुजस्समा (जिसे क़द-ए-आदम बनाने के लिए बसा औक़ात अपनी तरफ़ से पूरे एक फ़ुट का इज़ाफ़ा करना पड़ता है) म्युनिस्पल पॉर्क के बीचों बीच ईस्तादह किया जाए और...”
“और जुम्ला नाज़नीनान-ए-शहर चार महीने दस दिन तक मेरे लाशे को गोद में लिये, बाल बिखराए बैठी रहीं।” मिर्ज़ा ने दूसरा मिस्रा लगाया।
“मगर साहब! वसियतों की भी एक हद होती है। हमारे छूटपन का क़िस्सा है। पीपल वाली हवेली के पास एक झोंपड़ी में सन् 39 ई. तक एक अफ़ीमी रहता था। हमारे मोहतात अंदाज़े के मुताबिक़ उम्र 66 साल से किसी तरह कम न होगी, इसलिए कि ख़ुद कहता था कि पैंसठ साल से तो अफ़ीम खा रहा हूँ। चौबीस घंटे अंटा ग़फ़ील रहता था। ज़रा नशा टूटता तो मग़मूम हो जाता।
ग़म ये था कि दुनिया से बेऔलादा जा रहा हूँ। अल्लाह ने कोई औलाद-ए-देरीना न दी जो उसकी बान की चार पाई की जाएज़ वारिस बन सके! उसके मुतअ'ल्लिक़ महल्ले में मशहूर था कि पहली जंग-ए-अ'ज़ीम के बाद नहीं नहाया है। उसको इतना तो हमने भी कहते सुना कि ख़ुदा ने पानी सिर्फ़ पीने के लिए बनाया था मगर इंसान बड़ा ज़ालिम है,
राहतें और भी हैं ग़ुस्ल की राहत के सिवा
हाँ तो साहब! जब उसका दम आख़िर होने लगा तो महल्ले की मस्जिद के इमाम का हाथ अपने डूबते दिल पर रख कर ये क़ौल-ओ-क़रार किया कि मेरी मैयत को ग़ुस्ल न दिया जाए। बस पोले-पोले हाथों से तयमुम करा के कफ़्ना दिया जाए वर्ना हश्र में दामनगीर हूँगा।”
वकील साहब ने ताईद करते हुए फ़रमाया, “अक्सर मरने वाले अपने करने के काम पस्मांदगान को सौंप कर ठंडे-ठंडे सिधार जाते हैं। पिछली गर्मियों में दीवानी अ'दालतें बंद होने से चंद यौम क़ब्ल एक मक़ामी शायर का इन्तिक़ाल हुआ। वाक़या है कि उनके जीते जी किसी फ़िल्मी रिसाले ने भी उनकी उरियां नज़्मों को शर्मिंद-ए-तबाअ'त न किया। लेकिन आपको हैरत होगी कि मरहूम अपने ईसाल-ए-सवाब की ये राह समझा गए कि बाद-ए-मूर्दन मेरा कलाम हिनाई काग़ज़ पर छपवा कर साल के साल मेरी बर्सी पर फ़क़ीरों और मुरीदों को बिला हदिया तक़्सीम किया जाए।
पड़ोसी की हिम्मत और बढ़ी, “अब मरहूम ही को देखिए, जिंदगी में ही एक क़तअ'-ए-अराज़ी अपने क़ब्र के लिए ब़ड़े अरमानों से रजिस्ट्री करा लिया था गो कि बेचारे उसका क़ब्ज़ा पूरे बारह साल बाद ले पाए। नसीहतों और वसीयतों का यह आ'लम था कि मौत से दस साल पेश्तर अपने नवासों के एक फ़ेहरिस्त हवाले कर दी थी, जिसमें नाम ब-नाम लिखा था कि फ़लाँ वल्द फ़लाँ को मेरा मुंह न दिखाया जाए।(जिन हज़रात से ज़्यादा आज़ुर्दा ख़ातिर थे, उनके नाम के आगे वल्दियत नहीं लिखी थी।) तीसरी शादी के बाद उन्हें इसका तवील ज़मीमा मुरत्तब करना पड़ा, जिसमें तमाम जवान पड़ोसियों के नाम शामिल थे।”
“हमने तो यहाँ तक सुना है कि मरहूम न सिर्फ़ अपने जनाज़े में शुर्का की ता'दाद मुतअय्यन कर गए बल्कि आज के चेहल्लुम का ‘मिनू’ भी ख़ुद ही तय फ़रमा गए थे।” वकील ने ख़ाके में शोख़ रंग भरा।
इस नाज़ुक मरहले पर ख़शख़शी दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग ने पुलाव से सैर हो कर अपने शिकम पर हाथ फेरा और ‘मिनू’की ताईद-ओ-तौसीफ़ में एक मुसलसल डकार दाग़ी, जिसके इख़्तिताम पर इस मासूम हसरत का इज़हार फ़रमाया कि आज मरहूम ज़िन्दा होते तो ये इंतिज़ामात देख कर कितने ख़ुश होते!
अब पड़ोसी ने तेग़-ए-ज़बान को बेनियाम किया, “मरहूम सदा से सू-ए-हज़्म के मरीज़ थे। ग़िज़ा तो ग़िज़ा, बेचारे पेट में बात तक नहीं ठहरती थी। चटपटी चीज़ों को तरस्ते ही मरे। मेरे घर में से बता रहीं थीं कि एक दफ़ा मलेरिया में सरसाम हो गया और लगे बहकने। बार-बार अपना सर मंझली के रानों पर पटख़्ते और सुहाग की क़सम दिला कर ये वसियत करते थे कि हर जुमेरात को मेरी फ़ातिहा, चाट और कंवारी बकरी के सिरी पर दिलवाई जाए।”
मिर्ज़ा फड़क ही तो गए। होंट पर ज़बान फेरते हुए बोले, “साहब! वसियतों की कोई हद नहीं। हमारे महल्ले में डेढ़ पौने दो साल पहले एक स्कूल मास्टर का इंतिक़ाल हुआ, जिन्हें ईद-बक़रीद पर भी सालिम-व-साबुत पाजामा पहने नहीं देखा। मगर मरने से पहले वह भी अपने लड़के को हिदायत कर गए कि
पुल बना, चाह बना, मस्जिद-ओ-तालाब बना!
लेकिन हुज़ूर अब्बा की आख़िरी वसियत के मुताबिक़ फ़ैज़ के अस्बाब बनाने में लड़के की मुफ़लिसी के इ'लावा मुल्क का क़ानून भी मुज़ाहिम हुआ।”
“या'नी क्या?” वकील साहब के कान खड़े हुए।
“या'नी ये कि आज का पुल बनाने की इजाज़त सिर्फ़ पी.डब्लू.डी. को है और बिल-फ़र्ज़-ए-मोहाल कराची में चार फ़ुट गहरा कुआँ खोद भी लिया तो पुलिस उसका खारी कीचड़ पीने वालों का चालान इक़्दाम-ए-ख़ुदकुशी में कर देगी।
यूँ भी फ़टीचर से फ़टीचर क़स्बे में आजकल कुएँ सिर्फ़ ऐसे वैसे मौक़ों पर डूब मरने के लिए काम आते हैं। रहे तालाब, तो हुज़ूर! ले दे के उनका ये मस्रफ़ रह गया है कि दिन भर उनमें गाँव की भैंसें नहाएँ और सुब्ह जैसी आई थीं, इससे कहीं ज़्यादा गंदी होकर चराग़ जले बाड़े में पहुंचें।”
ख़ुदा-ख़ुदा करके ये मुकालमा ख़त्म हुआ तो पटाख़ों का सिलसिला शुरू हो गया,
“मरहूम ने कुछ छोड़ा भी?”
“बच्चे छोड़े हैं!”
“मगर दूसरा मकान भी तो है”
“उसके किराये को अपने मिर्ज़ा की सालाना मरम्मत सफ़ेदी के लिए वक़्फ कर गए हैं।”
“पड़ोसियों का कहना है कि ब्याहता बीवी के लिए एक अंगूठी भी छोड़ी है। अगर उसका नगीना असली होता तो किसी तरह बीस हज़ार से कम की नहीं थी।”
“तो क्या नगीना झूटा है?”
“जी नहीं, असली इमिटेशन है!”
“और वह पचास हज़ार की इंशोरेंस पॉलिसी क्या हुई?”
“वह पहले ही मंझली के मेहर में लिख चुके थे।”
“उसके बारे में यार लोगों ने लतीफ़ा घड़ रखा है कि मंझली बेवा कहती है कि सरताज के बग़ैर जिंदगी अजीरन है। अगर कोई उनको दोबारा ज़िंदा कर दे तो मैं बख़ुशी दस हज़ार लौटाने पर तैयार हूँ।”
“हमने ख़ॉनगी ज़राए से सुना है कि अल्लाह उन्हें करवट-करवट जन्नत नसीब करे, मरहूम मंझली पर ऐसे लहलोट थे कि अब भी रात-बिरात, ख़्वाबों में आ आकर डराते हैं।”
“मरहूम अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ठीक करते हैं। अभी तो उनका कफ़न भी मैला नहीं हुआ होगा, मगर सुनने में आया है कि मंझली ने रंगे चुने दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर दिया है।”
“अगर मंझली ऐसा करती है तो बिल्कुल ठीक करती है। आपने सुना होगा कि एक ज़माने में लखनऊ के निचले तब्क़े में ये रिवाज था कि चालीसवें पर न सिर्फ़ अन्वा-व-अक़्साम के पुरतकल्लुफ़ खानों का एहतिमाम किया जाता, बल्कि बेवा भी सोलह-सिंगार करके बैठती थी ताकि मरहूम की तरसी हुई रूह कमाहक़ा, मतमत्ता हो सके।” मिर्ज़ा ने ‘हे’ और ‘ऐन’ सही मख़्रज से अदा करते हुए मरे पर आख़िरी दुर्रा लगाया।
वापसी पर रास्ते में मैंने मिर्ज़ा को आड़े हाथों लिया, “जुमा को तुमने वाईज़ नहीं सुना? मौलवी साहब ने कहा था कि मरे हुओं का ज़िक्र करो तो अच्छाई के साथ। मौत को न भूलो कि एक न एक दिन सबको आनी है।”
सड़क पार करते-करते एक दम बीच में अकड़ कर खड़े हो गए। फ़रमाया, “अगर कोई मौलवी ये ज़िम्मा ले ले कि मरने के बाद मेरे नाम के साथ रहमतुल्लाह लिखा जाएगा तो आज ही... इसी वक़्त, इसी जगह मरने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी जान की क़सम!”
आख़िरी फ़िक़रा मिर्ज़ा ने एक बेसब्री कार के बम्पर पर तक़रीबन उकडूं बैठ कर जाते हुए अदा किया।
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.