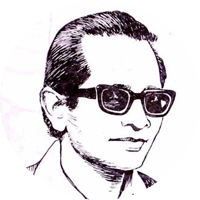दफ़्तर में नौकरी
हमने दफ़्तर में क्यों नौकरी की और छोड़ी, आज भी लोग पूछते हैं मगर पूछने वाले तो नौकरी करने से पहले भी पूछा करते थे।
“भई, आख़िर तुम नौकरी क्यों नहीं करते?”
“नौकरी ढूंडते नहीं हो या मिलती नहीं?”
“हाँ साहब, इन दिनों बड़ी बेरोज़गारी है।”
“भई, हरामख़ोरी की भी हद होती है।”
“आख़िर कब तक घर बैठे माँ बाप की रोटी तोड़ोगे।”
“लो और सुनो, कहते हैं, गु़लामी नहीं करेंगे।”
“मियां साहबज़ादे, बरसों जूतीयां घिसनी पड़ेंगी, तब भी कोई ज़रूरी नहीं कि...”
ग़रज़ कि साहब घर वालों, अज़ीज़ रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों के दिन-रात के तक़ाज़ों से तंग आकर हमने एक अदद नौकरी करली। नौकरी तो क्या की, घर बैठे बिठाए अपनी शामत मोल ले ली। वही बुज़ुर्ग जो उठते बैठते बेरोज़गारी के तानों से सीना छलनी किए देते थे, अब एक बिल्कुल नए अंदाज़ से हम पर हमला आवर हुए।
“अमाँ, नौकरी करली? लाहौल वला क़ुव्वा।”
“अरे, तुम और नौकरी?”
“हाय, अच्छे भले आदमी को कोल्हू के बैल की तरह दफ़्तर की कुर्सी में जोत दिया गया।”
“अगर कुछ काम वाम नहीं करना था तो कोई कारोबार करते इस नौकरी में क्या रखा है।”
लेकिन मुलाज़मत का पुरसा और नौकरी पर जाना दोनों काम जारी थे। ऐसे हज़रात और ख़वातीन की भी कमी न थी जिनकी नज़रों में ख़ैर से हम अब तक बिल्कुल बेरोज़गार थे। लिहाज़ा उन सबकी तरफ़ से नौकरी की कन्वेसिंग भी जारी थी। रोज़गार करने और रोज़गार न करने का बिल्कुल मुफ़्त मशवरा देने वालों से निबट कर हम रोज़ाना दफ़्तर का एक चक्कर लगा आते। यहाँ चक्कर लगाने, का लफ़्ज़ मैंने जान-बूझ कर इस्तेमाल किया है क्योंकि अब तक हमको नौकरी मिल जाने के बावजूद काम नहीं मिला था। बड़े साहब दौरे पर गए हुए थे। उनकी वापसी पर ये तै होना था कि हम किस शोबे में रखे जाएंगे। दफ़्तर हम सिर्फ़ हाज़िरी के रजिस्टर पर दस्तख़त करने की हद तक जाते थे। फ़िक्र इसलिए न थी कि हमारी तनख़्वाह जुड़ रही थी, यानी पैसे दूध पी रहे थे। परेशानी इस बात की थी कि इस ‘बाकार’ ‘बेकारी’ के नतीजे में हम कहीं ‘हरामख़ोर’ न होजाएं।
बेरोज़गारी के तक़ाज़ों से हम इस क़दर तंग आचुके थे कि अब किसी पर ये ज़ाहिर करना न चाहते थे कि बावजूद रोज़गार से लगे होने के हम बिल्कुल बेरोज़गार हैं और बेरोज़गार भी ऐसे कि जिससे कार तो कार, बेगार तक नहीं लिया जा रहा है।
रोज़ाना हम घर से दफ़्तर के लिए तैयार हो कर निकलते और रास्ते में साइकिल आहिस्ता करके दफ़्तर के फाटक पर खड़े चपरासी से पूछते, “अमाँ आया?”
जवाब मिलता, “अभी नहीं आया।”
इसके बाद हम दफ़्तर में जाकर हाज़िरी लगा उल्टे क़दमों बाहर आते, साइकिल उठाते और शहर के बाहर देहात, बाग़ों और खेतों के चक्कर लगा लगा कर दिल बहलाते और वक़्त काटते।
लेकिन दो-चार दिन में, जब देहात की सैर से दिल भर गया, तो शहर के नुक्कड़ पर एक चायख़ाने में अड्डा जमाया। फिर एक-आध हफ़्ते में इससे भी तबीयत घबरा गई। अब सवाल ये कि जाएं तो जाएं कहाँ? एक तरकीब सूझ गई। घर में कह दिया, छुट्टी ले ली है। दो-चार दिन बड़े ठाठ रहे आख़िर झक मारकर वही दफ़्तरी आवारागर्दी शुरू कर दी।
उसके बाद दो एक दिन दफ़्तर में स्वाँग रचाया। एक दिन दफ़्तर में छुट्टी की वजह ये बताई कि हमारे अफ़सर एक मुख़्तसर अलालत के बाद आज वफ़ात पा गए। मगर ये ख़ुश आगीं लम्हात भी मुद्दत-ए-वस्ल की तरह जल्द ख़त्म हो गए। अब क्या करें। स्कूल के ज़माने में हमने छुट्टी हासिल करने के लिए एक एक करके तक़रीबन अपने पूरे ख़ानदान को मौत के घाट उतार दिया था।
गैरहाज़िरी का ये उज़्र पेश करते,
“दादा-जान पर अचानक डबल निमोनिया का हमला हुआ और वो एक ही दिन में अल्लाह को प्यारे हो गए।”
नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि मास्टर साहब ने बेद खड़काते हुए कड़क कर पूछा, “कल कहाँ थे?”
रोनी सूरत बनाकर अर्ज़ किया, “वालिद साहब का इंतक़ाल हो गया।”
दरोग़ गो रा हाफ़िज़ा न बाशद
हम वालिद मरहूम की वफ़ात हसरत-ए-आयात की तफ़सील में जाने के लिए मसाइब पर आने ही वाले थे कि मास्टर साहब गरजे, “तुम्हारे वालिद का तो पिछले महीने इंतक़ाल हो चुका है।”
जल्दी से बात बनाते हुए कहा, “अब्बा से मुराद बड़े अब्बा, जिन्हें हम अब्बा कहते थे। हमारे बड़े अब्बा।”
मास्टर साहब हमारी इस ताज़ा-तरीन यतीमी से बेहद मुतास्सिर हुए। इस मौक़े पर तो ख़ैर हम बिल्कुल बाल बाल बच गए। लेकिन जब हमने अपनी भावज के तीसरी बार इंतक़ाल की ख़बर सुनाई तो मास्टर साहब खटक गए। हमसे बज़ाहिर रस्मी हमदर्दी की मगर शाम को बेद लेकर ताज़ियत के लिए हमारे घर आए, जहाँ हमारे ख़ानदान के हर मरहूम से उन्होंने ज़ाती तौर पर मुलाक़ात करने के बाद हमको हमारे घर नुमा क़ब्रिस्तान में बेद से मारते मारते ज़िंदा दरगोर कर दिया।
चुनांचे अब जो दफ़्तर से बचने के सिलसिले में ज़माना-ए-तालिब इल्मी में छुट्टी के हथकंडों पर नज़र दौड़ाई और तबीयत गुदगुदाई तो बजाय दफ़्तर जाने के घर में ऐलान कर दिया,
“डायरेक्टर साहब का आज इंतक़ाल हो गया।”
रफ़्ता-रफ़्ता वक़्त गुज़ारी से इतने आजिज़ आगए कि एक दिन ये सोच कर कि न रहेगा बाँस और न बजेगी बाँसुरी, इस्तीफ़ा जेब में रखकर दफ़्तर पहुँचे लेकिन हमारी बदक़िस्मती मुलाहिज़ा फ़रमाइए कि क़ब्ल इसके कि हम इस्तीफ़ा पेश करते हमें ये ख़ुशख़बरी सुना दी गई कि फ़ुलां शोबे से हमको वाबस्ता कर दिया गया है, जहाँ हमको फ़ुलां फ़ुलां काम करने होंगे।
अब हम रोज़ाना बड़ी पाबंदी से पूरा वक़्त दफ़्तर में गुज़ारने लगे। दिन दिन भर दफ़्तर की मेज़ पर जमे नॉवलें पढ़ते, चाय पीते और ऊँघते रहते।
जब हम अपने इंचार्ज से काम की फ़र्माइश करते तो वो बड़ी शफ़क़त से कहते ऐसी जल्दी क्या है, अज़ीज़म ज़िंदगी भर काम करना है।
एक दिन हम जैसे ही दफ़्तर पहुँचे तो मालूम हुआ कि जिन डायरेक्टर साहब को हम अपने घर में मरहूम क़रार दे चुके थे, वो हमको तलब फ़रमा रहे हैं, फ़ौरन पहुँचे।
बड़े अख़लाक़ से मिले। देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद बोले, “अच्छा।”
“आपने शायद मुझे किसी काम से याद फ़रमाया था।”
“ओह ठीक है, सेक्रेटरी साहब से मिल लीजिए। वो आपको समझा देंगे।”
सेक्रेटरी साहब से एक हफ़्ते बाद कहीं मुलाक़ात हो सकी। उन्होंने अगले दिन बुलाया और बजाय काम बताने के डिप्टी सेक्रेटरी का पता बता दिया। मौसूफ़ दौरे पर थे। दो हफ़्ते बाद मिले। बहुत देर तक दफ़्तरी नशेब-ओ-फ़राज़ समझाने के बाद हमें हुक्म दिया कि इस मौज़ू पर इस इस क़िस्म का एक मुख़्तसर सा मक़ाला लिख लाइए। आधे घंटे के अंदर तैयार कर दिया।
ख़ुशी के मारे हम फूले न समाए कि हम भी दुनिया में किसी काम आसकते हैं। दो सफ़हे का मक़ाला तैयार करना था जो हमने बड़ी मेहनत के बाद आधे घंटे के अंदर तैयार कर दिया। मौसूफ़ ने मक़ाला बहुत पसंद किया।
मज़ीद काम के लिए हम उनके कमरे का रुख़ करने ही वाले थे कि उस दफ़्तर के एक घाग अफ़सर ने हमारा रास्ता रोकते हुए हमें समझाया, भैया, अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहते हो या हम लोगों की नौकरियां ख़त्म कराना चाहते हो? आख़िर तुम्हारा मतलब क्या है? जो काम तुमको दिया गया था, उसे करते रहो हम लोग दफ़्तर में काम करने नहीं बल्कि अपने आपको मसरूफ़ रखने के लिए आते हैं।”
अगले दिन इतवार की छुट्टी थी। नाशता करते वक़्त अख़बार के मैगज़ीन सेक्शन पर जो नज़र दौड़ाई तो वही मक़ाला हमारे एक साहब के साहब के साहब के साहब के नाम-ए-नामी और इस्म गिरामी के दुम छल्ले के साथ बड़े नुमायां तौर पर छपा हुआ नज़र आ गया।
हमारे हिसाब से अब उगला आध घंटे का काम दो-तीन महीने की दौड़ धूप के बाद दफ़्तर में मिल सकता था, जिस पर लानत भेजते हुए बजाय दफ़्तर जाने के हमने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया, जिसको मंज़ूर होने में इतने दिन लगे जितने दिन हमने दफ़्तर में काम भी नहीं किया था।
शायद आप पूछें कि मुलाज़मत करके हमने क्या खोया और क्या पाया। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि नौकरी खोई और दिन में ऊँघने, सोने और नॉवलें पढ़ने और वक़्त गुज़ारी की आदत पाई। हमें और क्या चाहिए?
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.