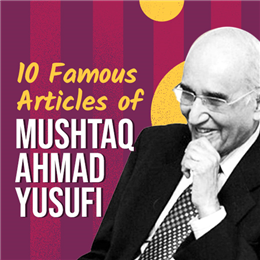जुनून-ए-लतीफ़ा
बड़ा मुबारक होता है वो दिन जब कोई नया ख़ानसामां घर में आए और इससे भी ज़्यादा मुबारक वो दिन जब वो चला जाये! चूँकि ऐसे मुबारक दिन साल में कई बार आते हैं और तल्ख़ी-ए-काम-ओ-दहन की आज़माईश करके गुज़र जाते हैं। इसलिए इत्मिनान का सांस लेना, बक़ौल शायर सिर्फ़ दो ही मौक़ों पर नसीब होता है,
इक तिरे आने से पहले इक तिरे जाने के बाद
आ'म तौर पर ये समझा जाता है कि बदज़ाइक़ा खाना पकाने का हुनर सिर्फ़ ता'लीम याफ़्ता बेगमात को आता है लेकिन हम आ'दाद-ओ-शुमार से साबित कर सकते हैं कि पेशेवर ख़ानसामां इस फ़न में किसी से पीछे नहीं। असल बात ये है कि हमारे हाँ हर शख़्स ये समझता है कि उसे हँसना और खाना आता है। इसी वजह से पिछले सौ बरस से ये फ़न कोई तरक़्क़ी नहीं कर सके।
एक दिन हमने अपने दोस्त मिर्ज़ा अ'ब्दुल वदूद बेग से शिकायतन कहा कि अब वो ख़ानसामां जो सत्तर क़िस्म के पुलाव पका सकते थे, मिन हैस-उ-जमाअ'त रफ़्ता-रफ़्ता नापैद होते जा रहे हैं।
जवाब में उन्होंने बिल्कुल उल्टी बात कही, कहने लगे, ख़ानसामां-वानसामां ग़ायब नहीं हो रहे बल्कि ग़ायब हो रहा है वो सत्तर क़िस्म के पुलाव खाने वाला तब्क़ा जो बटलर और ख़ानसामां रखता था और उड़द की दाल भी डिनर जैकेट पहन कर खाता था। अब इस वज़ा'दार तब्क़े के अफ़राद बावर्ची नौकर रखने के बजाय निकाह सानी करलेते हैं। इसलिए कि गया गुज़रा बावर्ची भी रोटी कपड़ा और तनख़्वाह मांगता है। जबकि मनकूहा फ़क़त रोटी कपड़े पर ही राज़ी होजाती है। बल्कि अक्सर-ओ-बेशतर खाने और पकाने के बर्तन भी साथ लाती है।
मिर्ज़ा अक्सर कहते हैं कि ख़ुद काम करना बहुत आसान है मगर दूसरों से काम लेना निहायत दुश्वार। बिल्कुल उसी तरह जैसे ख़ुद मरने के लिए किसी ख़ास क़ाबीलियत की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन दूसरों को मरने पर आमादा करना बड़ा मुश्किल काम है। मा'मूली सिपाही और जरनैल में यही फ़र्क़ है। अब उसे हमारी सख़्तगिरी कहिए या नाअह्ली या कुछ और, कोई ख़ानसामां एक हफ़्ते से ज़्यादा नहीं टिकता। ऐसा भी हुआ है कि हंडिया अगर शबराती ने चढ़ाई तो बघार रमज़ानी ने दिया और दाल बुलाकी ख़ां ने बाँटी। मुम्किन है मज्कूर-उल-सद्र हज़रात अपनी सफ़ाई में ये कहें कि,
हम वफ़ादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं!
लिहाज़ा हम तफ़सीलात से एह्तिराज़ करेंगे। हालाँकि दिल ज़रूर चाहता है कि ज़रा तफ़सील के साथ मिनजुम्ला दीगर मुश्किलात के इस सरासीमगी को बयान करें जो उस वक़्त महसूस होती है जब हमसे अज़ रूए हिसाब ये दरयाफ़्त करने को कहा जाये कि अगर नौकर की 13 दिन की तनख़्वाह 30 रुपये और खाना है, तो 9 घंटे की तनख़्वाह बग़ैर खाने के क्या होगी?
ऐसे नाज़ुक मवाक़े पर हमने सवाल को आसान करने की नीयत से अक्सर ये मा'क़ूल तजवीज़ पेश की कि इसको पहले खाना खिला दिया जाये। लेकिन अव्वल तो वो इस पर किसी तरह रज़ामंद नहीं होता। दोम खाना तैयार होने में अभी पूरा सवा घंटा बाक़ी है और इससे आपको असुलन इत्तफ़ाक़ होगा कि 9 घंटे की उजरत का हिसाब 10-1/4 घंटे के मुक़ाबले में फिर भी आसान है।
हम दाद के ख़ाहां हैं न इन्साफ़ के तालिब। कुछ तो इस अंदेशे से कि कहीं ऐसा न हो कि जिनसे ख़स्तगी की दाद पाने की तवक़्क़ो है, वो हमसे ज़्यादा ख़स्ता तेग़-ए-सितम निकलें और कुछ इस डर से कि,
हम इल्ज़ाम उनको देते थे क़सूर अपना निकल आया
मक़सद सरेदस्त उन खानसामाओं का तआ'रुफ़ कराना है जिनकी दामे दरमे ख़िदमत करने का शर्फ़ हमें हासिल हो चुका है। अगर हमारे लहजे में कहीं तल्ख़ी की झलक आए तो उसे तल्ख़ी-ए-काम-ओ-दहन पर महमूल करते हुए, ख़ानसामाओं को मा'फ़ फ़रमाएं।
ख़ानसामां से अह्द-ए-वफ़ा उस्तवार करने और उसे हमेशा के लिए अपना ग़ुलाम बनाने का ढंग कोई मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग से सीखे। यूं तो उनकी सूरत ही ऐसी है कि हर कस व नाकस का बेइख़्तियार नसीहत करने को जी चाहता है लेकिन एक दिन हमने देखा कि उनका देरीना बावर्ची भी उनसे अबे-तबे करके बातें कर रहा है।
हमारी हैरत की इंतिहा न रही, क्योंकि शुरफ़ा में अंदाज़-ए-गुफ़्तगू महज़ मुख़्लिस दोस्तों की साथ रवा है। जुह्ला से हमेशा संजीदा गुफ़्तगु की जाती है। हमने मिर्ज़ा की तवज्जो इस अमर की तरफ़ दिलाई तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने जान-बूझ कर इसको इतना मुँह ज़ोरावर बदतमीज़ कर दिया है कि अब मेरे घर के सिवा इसकी कहीं और गुज़र नहीं हो सकती।
कुछ दिन हुए एक मिडल फ़ेल ख़ानसामां मुलाज़मत की तलाश में आ निकला और आते ही हमारा नाम और पेशा पूछा। फिर साबिक़ खानसामाओं के पते दरयाफ़्त किए। नीज़ यह कि आख़िरी ख़ानसामां ने मुलाज़मत क्यों छोड़ी?
बातों बातों में उन्होंने ये इंदिया भी लेने की कोशिश की कि हम हफ़्ते में कितनी दफ़ा बाहर मदऊ' होते हैं और बावर्चीख़ाने में चीनी के बर्तनों के टूटने की आवाज़ से हमारे आ'साब और अख़लाक़ पर क्या असर मुरत्तब होता है। एक शर्त उन्होंने ये भी लगाई कि अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ पर जाएंगे तो पहले ए'वज़ी मालिक पेश करना पड़ेगा।
काफ़ी रद्द-ओ-कद के बाद हमें यूं महसूस होने लगा जैसे वो हममें वही खूबियां तलाश कर रहे हैं जो हम उनमें ढूंढ रहे थे। ये आँख-मिचोली ख़त्म हुई और काम के औक़ात का सवाल आया तो हमने कहा कि असुलन हमें मेहनती आदमी पसंद हैं। ख़ुद बेगम साहिबा सुबह पाँच बजे से रात के दस बजे तक घर के काम काज में जुटी रहती हैं।
कहने लगे, साहिब! उनकी बात छोड़िये, वो घर की मालिक हैं। मैं तो नौकर हूँ! साथ ही साथ उन्होंने ये वज़ाहत भी कर दी कि बर्तन नहीं मांझुँगा, झाड़ू नहीं दूँगा। ऐश ट्रे साफ़ नहीं करूँगा, मेज़ नहीं लगाऊँगा। दा'वतों में हाथ नहीं धुलाऊँगा।
हमने घबराकर पूछा, फिर क्या करोगे?
ये तो आप बताईए, काम आपको लेना है, मैं तो ताबे'दार हूँ।
जब सब बातें हस्ब-ए-मंशा-ए-ज़रूरत (ज़रूरत हमारी, मंशा उनकी) तय हो गईं तव हमने डरते-डरते कहा कि भई सौदा सुल्फ़ लाने के लिए फ़िलहाल कोई अलैहदा नौकर नहीं है। इसलिए कुछ दिन तुम्हें सौदा भी लाना पड़ेगा। तनख़्वाह तय कर लो।
फ़रमाया, जनाब! तनख़्वाह की फ़िक्र न कीजिए। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कम तनख़्वाह में भी ख़ुश रहूँगा।
फिर भी?
कहने लगे, पछत्तर रुपये माहवार होगी। लेकिन अगर सौदा भी मुझी को लाना पड़ा तो चालीस रुपये होगी!
उनके बाद एक ढंग का ख़ानसामां आया मगर बेहद दिमाग़दार मा'लूम होता था। हमने उसका पानी उतारने की ग़रज़ से पूछा, मुग़लई और अंग्रेज़ी खाने आते हैं?
हर क़िस्म का खाना पका सकता हूँ। हुज़ूर का किस इलाक़े से ता'ल्लुक़ था?
हमने सही सही बता दिया, झूम ही तो गए। कहने लगे, मैं भी एक साल उधर काट चुका हूँ। वहां के बाजरे की खिचड़ी की तो दूर दूर तक धूम है।
मज़ीद जिरह की हममें ताब न थी। लिहाज़ा उन्होंने अपने आप को हमारे हाँ मुलाज़िम रख लिया। दूसरे दिन पुडिंग बनाते हुए उन्होंने ये इन्किशाफ़ किया कि मैंने बारह साल अंग्रेज़ों की जूतियां सीधी की हैं, इसलिए बैठ कर चूल्हा नहीं झोंकूँगा। मजबुरन खड़े हो कर पकाने का चूल्हा बनवाया।
उनके बाद जो ख़ानसामां आया, उसने कहा कि मैं चपातियाँ बैठ कर पकाऊँगा, मगर बुरादे की अँगीठी पर। चुनांचे लोहे की अँगीठी बनवाई। तीसरे के लिए चिकनी मिट्टी का चूल्हा बनवाना पड़ा। चौथे के मुताल्बे पर मिट्टी के तेल से जलने वाला चूल्हा ख़रीदा और पांचवां ख़ानसामां इतने सारे चूल्हे देख कर ही भाग गया।
उस ज़ालिम का नाम याद नहीं आ रहा। अलबत्ता सूरत और ख़द्द-ओ-ख़ाल अब तक याद हैं। इब्तिदाए मुलाज़मत से हम देख रहे थे कि वो अपने हाथ का पका हुआ खाना नहीं खाता, बल्कि पाबंदी से मिलागिरी होटल में उकड़ूं बैठ कर दो पैसे की चटपटी दाल और एक आने की तंवरी रोटी खाता है।
आख़िर एक दिन हमसे न रहा गया और हमने ज़रा सख़्ती से टोका कि, घर का खाना क्यों नहीं खाते?
तुनक कर बोला, साहिब! हाथ बेचा है, ज़बान नहीं बेची!
उसने निहायत मुख़्तसर मगर ग़ैर मुब्हम अलफ़ाज़ में ये वाज़ह कर दिया कि अगर उसे अपने हाथ का पका खाना खाने पर मजबूर किया गया तो वो फ़ौरन इस्तिफ़ा दे देगा।
उसके रवैय्ये से हमें भी शुबहा होने लगा कि वो वाक़ई ख़राब खाना पकाता है। नीज़ हम इस मंतक़ी नतीजे पर पहुंचे कि दोज़ख़ में गुनहगार औरतों को उनके अपने पकाए हुए सालन ज़बरदस्ती खिलाए जाऐंगे। उसी तरह रेडियो वालों को फ़रिश्ते आतिशीं गुर्ज़ मार-मार कर बार-बार उन ही के नश्र किए हुए प्रोग्रामों के रिकार्ड सुनाएँगे।
हम खाने के शौक़ीन हैं, ख़ुशामद के भूके नहीं (गोकि इससे इनकार नहीं कि अपनी ता'रीफ़ सुन कर हमें भी अपना बनियान तंग मा'लूम होने लगता है)। हमने कभी ये तवक़्क़ो नहीं की कि बावर्ची खाना पकाने के बजाय हमारे गुन गाता रहे लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि वो चौबीस घंटे अपने मरहूम और साबिक़ आक़ाओं का कलमा पढ़ता रहे। जबकि इस तौसीफ़ का असल मक़सद हमें जलाना और उन ख़ूबियों की तरफ़ तवज्जो दिलाना होता है जो हम में नहीं हैं।
अक्सर औक़ात बेतहाशा जी चाहता है कि काश हम भी मरहूम होते ताकि हमारा ज़िक्र भी इतने ही प्यार से होता। बा'ज़ निहायत क़ाबिल खानसामाओं को महज़ इस दूरअंदेशी की बिना पर अ'लाहिदा करना पड़ा कि आइन्दा वो किसी और का नमक खा कर हमारे हक़ में प्रोपेगंडा करते रहीं। जो शख़्स भी आता है यही दा'वे करता है कि उसके साबिक़ आक़ा ने उसे स्याह व सफ़ेद का मालिक बना रखा था (यहां ये बताना बेमहल न होगा कि उसूली तौर पर हम ख़ुद भी हमेशा दूसरों पर भरोसा करते हैं लेकिन रेज़गारी ज़रूर गिन लेते हैं)। एक ख़ानसामां ने हमें मुत्तला किया कि उसका पिछ्ला साब इस क़दर शरीफ़ आदमी था कि ठीक से गाली तक नहीं दे सकता था।
हमने जल कर कहा, फिर तुमने नौकरी क्यों छोड़ी?
तड़प कर बोले, कौन कहता है कि ख़ुदाबख़्श ने नौकरी छोड़ी? क़िस्सा दरअसल ये है कि मेरी पाँच महीने की तनख़्वाह चढ़ गई थी और अब आपसे क्या पर्दा? सच तो ये है कि उनके घर का ख़र्च भी मैं रद्दी अख़बार और बियर की ख़ाली बोतलें बेच कर चला रहा था। उन्होंने कभी हिसाब नहीं मांगा। फिर उन्होंने एक दिन मेरी सूरत देख कर कहा कि ख़ुदाबख़्श! तुम बहुत थक गए हो। दो दिन की छुट्टी करो और अपनी सेहत बनाओ।
दो दिन बाद जब मैं सेहत बना कर लौटा तो घर ख़ाली पाया। पड़ोसियों ने बताया कि “तुम्हारा साब तो परसों ही सारा सामान बांध कर कहीं और चला गया।”
ये क़िस्सा सुनाने के बाद उस नमक हलाल ने हमसे पेशगी तनख़्वाह मांगी ताकि अपने साबिक़ आक़ा के मकान का किराया अदा कर सके।
गुज़िश्ता साल हमारे हाल पर रहम खा कर एक करम फ़रमा ने एक तजुर्बेकार ख़ानसामां भेजा, जो हर इ'लाक़े के खाने पकाना जानता था।
हमने कहा, भई और तो सब ठीक है मगर तुम सात महीने में दस मुलाज़मतें छोड़ चुके हो, ये क्या बात है?
कहने लगे, साब! आजकल वफ़ादार मालिक कहाँ मिलता है?
इस सितम ईजाद की बदौलत बर्र-ए-सग़ीर के हर खित्ते बल्कि हर तहसील के खाने की खूबियां इस हीचमदां पुंबा दहां के दस्तरख़्वान पर सिमट कर आ गईं। मसलन दोपहर के खाने पर देखा कि शोरबे में मुसल्लम कैरी हिचकोले ले रही है और सालन इस क़दर तुर्श है कि आँखें बंद हो जाएं और अगर बंद हों तो पट से खुल जाएं। पूछा तो उन्होंने आगाही बख़्शी कि दक्कन में रुअसा खट्टा सालन खाते हैं। और हम ये सोचते ही रह गए कि अल्लाह जाने बक़िया लोग क्या खाते होंगे।
उसी दिन शाम को हमने घबराकर पूछा कि दाल में पुराने जूतों की बू क्यों आरही है?
जवाब में उन्होंने एक धुआँधार तक़रीर की जिसका लुब्ब-ए-लुबाब ये था कि मारवाड़ी सेठों के फलने-फूलने और फैलने का राज़ हींग में मुज़मिर है। और दूसरे दिन जब हमने दरयाफ़्त किया कि बंदा-ए-ख़ुदा ये चपाती है या दस्तर-ख़्वान?
तो हंस कर बोले कि वतन मालूफ़ में रोटी के हदूद अर्बा यही होते हैं।
आख़िर कई फ़ाक़ों के बाद एक दिन हमने ब नज़र हौसला अफ़्ज़ाई कहा, “आज तुमने चावलों का अचार बहुत अच्छा बनाया है।”
दहकते हुए तवे से बीड़ी सुलगाते हुए बोले, “बंदापरवरी है! काठियावाड़ी पुलाव में क़ोर्मे के मसाले पड़ते हैं!”
“ख़ूब! मगर यह क़ोर्मे का मज़ा तो नहीं!”
“वहां क़ोर्मे में अचार का मसाला डालते हैं!”
फिर एक दिन शाम के खाने पर मिर्ज़ा ने नाक सुकेड़ कर कहा, “मियां! क्या खीर में खटमलों का बघार दिया है?”
सफ़ेद दीवार पर कोयले से सौदे का हिसाब लिखते हुए हिक़ारत से बोले, “आपको मा'लूम नहीं? शाहान-ए-अवध लगी हुई फ़ीरनी खाते थे?”
“मगर तुमने देखा क्या अंजाम हुआ अवध की सल्तनत का?”
मुख़्तसर ये कि डेढ़ महीने तक वो सुबह व शाम हमारे नापुख़्त ज़ौक़ व ज़ाइक़ा को सँवारता और मशरूबात-ओ-मा'कूलात से वसीअ'-उल-मशरबी का दर्स देता रहा। आख़िर आख़िर में मिर्ज़ा को शुबहा हो चला था कि वो ग़ैरमुल्की एजेंट है जो सालन के ज़रिये सुबाई ग़लतफ़ह्मियाँ फैला रहा है।
अगर आपको कोई खाना बेहद मर्ग़ूब है जो छुड़ाए नहीं छूटता तो ताज़ा वारदान-ए-बिसात ख़ानसामां इस मुश्किल को फ़ौरन आसान कर देंगे। अश्या-ए-ख़ुर्दनी और इन्सानी मे'दे के साथ भरपूर तजुर्बे करने की जो आज़ादी बावर्चियों को हासिल है वो नित नई कीमियावी ईजादात की ज़ामिन है। मिसाल के तौर पर हमें भिंडी बहुत पसंद है लेकिन दस घंटे क़ब्ल ये मुनकशिफ़ हुआ कि इस नबात ताज़ा को एक ख़ास दर्जा हरारत पर पानी की मुक़र्ररा मिक़दार में (जिसका इ'ल्म सिर्फ़ हमारे ख़ानसामां को है) मीठी आँच पर पकाया जाये तो इस मुरक्कब से दफ़्तरों में लिफ़ाफ़े और बदलगाम अफ़सरों के मुँह हमेशा के लिए बंद किए जा सकते हैं।
इन्ही हज़रत ने गुज़िश्ता जुमे'रात को सारा घर सर पर उठा रखा था। हमने बच्ची को भेजा कि उससे कहो कि मेहमान बैठे हैं। इस वक़्त सिल खूटने की ज़रूरत नहीं।
उसने कहला भेजा कि हम इनही मेहमानों की तवाज़ो के लिए सिल पर कबाबों का क़ीमा पीस रहे हैं। थोड़ी देर बाद हमने कबाब मुँह में रखा तो महसूस हुआ गोया चटपटा रेग माल खा रहे हैं और हमें रह-रह कर मीर साहिब पर रश्क आने लगा कि वो मस्नूई बत्तीसी लगाए बेख़बर बैठे खा रहे थे और हमारी तरह किरकिरा महसूस करके लाल पीले नहीं हुए। सुबह तक सब को पेचिश हो गई। सिर्फ़ हमें नहीं हुई और हमें इसलिए नहीं हुई कि हम पहले ही इसमें मुब्तिला थे।
ये बात नहीं कि ख़ुदा-न-ख़ास्ता हम बीमारी और मौत से डरते हैं। हम तो पुरानी चाल के आदमी हैं। इसलिए नई ज़िंदगी से ज़्यादा ख़ौफ़ खाते हैं। मौत बरहक़ है और एक न एक दिन ज़रूर आएगी। बात सिर्फ़ इतनी है कि बुलाने के लिए हम अपनी नेक कमाई में से पच्चास साठ रुपये माहवार ख़र्च नहीं करना चाहते। हमें किसी मर्ज़ नाशिनास हकीम के हाथों मरने पर भी चंदाँ ए'तराज़ न होगा। लेकिन हम किसी सूरत ख़ानसामां को बिल अक़सात रूह क़ब्ज़ करने का इख़्तियार नहीं देना चाहते कि ये सिर्फ़ हकीम-डाक्टरों का हक़ है।
बीमारी का ज़िक्र चल निकला तो उस क़वी हैकल ख़ानसामां का क़िस्सा भी सुन लीजिए जिसको हम सब आग़ा कहा करते थे (आग़ा इसलिए कहा करते थे कि वो सचमुच आग़ा थे)। उनका ख़्याल आते ही मे'दे में महताबियाँ सी जल उठती हैं। ता दम-ए-विदा उनके खाना पकाने और खिलाने का अंदाज़ वही रहा जो मुलाज़मत से पहले हींग बेचने का होता था...या'नी डरा धमका कर उसकी की खूबियां मनवा लेते थे।
बिलउ'मूम सुबह नाशते के बाद सोकर उठते थे। कुछ दिन हमने सुबह तड़के जगाने की कोशिश की लेकिन जब उन्होंने नींद की आड़ में हाथा पाई करने की कोशिश की तो हमने भी उनकी इस्लाह का ख़्याल तर्क कर दिया। इससे क़त-ए-नज़र, वो काफ़ी ताबे'दार थे।
ताबे'दार से हमारी मुराद ये है कि कभी वो पूछते कि चाय लाऊँ? और हम तकल्लुफ़न कहते कि जी चाहे तो ले आओ वर्ना नहीं। तो कभी वाक़ई ले आते और कभी नहीं भी लाते थे। जिस दिन से उन्होंने बावर्चीख़ाना सँभाला घर में हकीम-डाक्टरों की रेल-पेल होने लगी। यूं भी उनका पकाया हुआ खाना देख कर सर (अपना) पीटने को जी चाहता था। “अपना” इसलिए कि हालाँकि हम सब ही उनके खानों से आ'जिज़ थे, लेकिन किसी की समझ में नहीं आता था कि उनको क्यों कर पुर अमन तरीक़ से रुख़्सत किया जाए।
उनको नौकर रखना ऐसा ही साबित हुआ जैसे कि शेर-बब्बर पर सवार हो तो जाये लेकिन उतरने की हिम्मत न रखता हो।
एक दिन हम इसी उधेड़बुन में लेटे हुए गर्म पानी की बोतल से पेट सेंक रहे थे और दवा पी-पी कर उनको कोस रहे थे कि सर झुकाए आए और ख़िलाफ़-ए-मा'मूल हाथ जोड़ कर बोले, ख़ू! साब! तुम रोज़ रोज़ बीमार ओता ए, इससे अमारा क़बीला में बड़ा रुस्वाई, ख़ू, ख़ाना-ख़राब ओता ए, (साहिब! तुम बार-बार बीमार होते हो। इस से हमारे क़बीले में हमारी रुस्वाई होती है और हमारा ख़ाना-ख़राब होताहै।) इसके बाद उन्होंने कहा-सुना माफ़ कराया, और बग़ैर तनख़्वाह लिए चल दिए।
ऐसी ही एक और दा'वत का ज़िक्र है जिसमें चंद अहबाब और आफ़सरान बाला-ए-दस्त मदऊ' थे। नए ख़ानसामां ने जो क़ोर्मा पकाया, उसमें शोरबे का ये आलम था कि नाक पकड़ के ग़ोते लगाऐं तो शायद कोई बोटी हाथ आजाए। इक्का दुक्का कहीं नज़र आभी जाती तो कुछ इस तरह कि,
साफ़ छुपती भी नहीं सामने आती भी नहीं
और बसा ग़नीमत था क्योंकि मेहमान के मुँह में पहुंचने के बाद, ग़ालिब के अलफ़ाज़ में, ये कैफ़ियत थी कि,
खींचता है जिस क़दर उतनी ही खिंचती जाये है!
दौरान ज़याफ़त अहबाब ने बकमाल संजीदगी मश्वरा दिया कि, “रेफ्रीजरेटर ख़रीद लो। रोज़-रोज़ की झक-झक से नजात मिल जाएगी। बस एक दिन लज़ीज़ खाना पकवालो और हफ़्ते भर ठाट से खाओ और खिलाओ।”
क़िस्तों पर रेफ्रीजरेटर ख़रीदने के बाद हमें वाक़ई बड़ा फ़र्क़ महसूस हुआ और वो फ़र्क़ ये है कि पहले जो बदमज़ा खाना सिर्फ़ एक ही वक़्त खाते थे, अब उसे हफ़्ते भर खाना पड़ता है।
हमने इस अ'ज़ाब मुसलसल की शिकायत की तो वही अहबाब तलक़ीन फ़रमाने लगे कि, “जब ख़र्च किया है, सब्र भी कर, इसमें तो यही कुछ होताहै।”
कल फिर मिर्ज़ा से अपनी गूना-गूं मुश्किलात का ज़िक्र किया तो कहने लगे,
ये उलझनें आपने अपने चटोरपन से ख़्वाह-मख़ाह पैदा कर रखी हैं। वर्ना सादा ग़िज़ा और आ'ला ख़्यालात से ये मसला कभी का ख़ुद बख़ुद हल हो गया होता। यही आईन-ए-क़ुदरत है और यही आज़ाद तहज़ीब की असास भी! आपने मौलवी इस्माईल मेरठी का वो पाकीज़ा शे'र नहीं पढ़ा?
मिले ख़ुश्क रोटी जो आज़ाद रह कर
तो वो ख़ौफ़-ओ-ज़िल्लत के हलवे से बेहतर
अ'र्ज़ किया, “मुझे किसी के आज़ाद रहने पर, ख़्वाह शायर ही क्यों न हो, कोई ए'तराज़ नहीं। लेकिन इस शे'र पर मुझे अ'र्सा से ये ए'तराज़ है कि इसमें आज़ादी से ज़्यादा ख़ुश्क रोटी की ता'रीफ़ की गई है। मुम्किन है उ'म्दा ग़िज़ा आ'ला तहज़ीब को जन्म न दे सके, लेकिन आ'ला तहज़ीब कभी ख़राब ग़िज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकती।
फ़रमाया, बर्दाश्त की एक ही रही! ख़राब खाना खा कर बदमज़ा न होना, यही शराफ़त की दलील है।
गुज़ारिश की, “मर्दानगी तो ये कि आदमी अ'र्सा तक उ'म्दा ग़िज़ा खाए और शराफ़त के जामे से बाहर न हो!”
मुश्तइल हो गए, “बजा! लेकिन ये कहाँ की शराफ़त है कि आदमी उठते-बैठते खाने का ज़िक्र करता रहे। बुरा न मानिएगा, आपके बा'ज़ मज़ामीन किसी बिगड़े हुए शाही रिकाबदार की ख़ानदानी बयाज़ मा'लूम होते हैं। जभी तो कम पढ़ी लिखी औरतें बड़े शौक़ से पढ़ती हैं।”
हमने टोका, “आप भूल रहे हैं कि फ़्रांस में खाना खाने और पकाने का शुमार फ़नून-ए-लतीफ़ा में होता है।”
वो बिगड़ गए, “मगर आपने तो उसे जुनून-ए-लतीफ़ा का दर्जा दे रखा है। अगर आप वाक़ई अपनी बेक़सूर क़ौम की इस्लाह के दरपे हैं तो कोई काम की बात कीजिए और तरक़्क़ी की राहें सुझाइए।”
मज़ा लेने की ख़ातिर छेड़ा, “एक दफ़ा क़ौम को अच्छा पहनने और खाने का चस्का लग गया तो तरक़्क़ी की राहें ख़ुद बख़ुद सूझ जाएँगी। गांधी जी का क़ौल है कि जिस देस में लाखों आदमियों को दो वक़्त का खाना नसीब न होता हो, वहां भगवान की भी हिम्मत नहीं होती कि अन्नदाता के सिवा किसी और रूप में सामने आ सके। भूके के लिए भोजन ही भगवान का अवतार है और...”
क़ता कलामी की माफ़ी मांगे बग़ैर बोले, “मगर वो तो बकरी का दूध और खजूर खाते थे और आप फ़न-ए-ग़िज़ा शनासी को फ़लसफ़ा ख़ुदा शनासी समझ बैठे हैं। ख़ुद आपके महबूब यूनानी फ़लसफ़ी जो भरपूर ज़िंदगी के क़ाइल थे, दिमाग़ से महसूस करते और दिल से सोचते थे। मगर आप तो मे'दे से सोचते हैं और देखा जाये तो आप आज भी वही मश्वरा दे रहे हैं जो मलिका मैरी अनतोनीत ने दिया था। एक दरबारी ने जब उसके गोश-ए-गुज़ार किया कि रोटी न मिलने के सबब हज़ारों इन्सान पैरिस की गलियों में दम तोड़ रहे हैं तो उसने हैरत से पूछा कि “ये अहमक़ केक क्यों नहीं खाते?”
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.