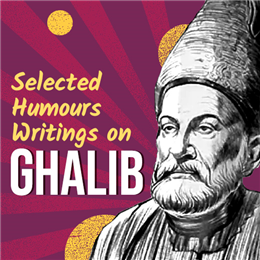नतीजा ग़ालिब शनासी का
मिर्ज़ा ग़ालिब जितने बड़े शायर थे उतने ही बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही दानिशमंद और दूर अंदेश आदमी थे। उन्हें मालूम था कि एक वक़्त ऐसा आएगा जब उनके वतन में उनका कलाम सुख़न फ़ह्मों के हाथों से निकल कर हम जैसे तरफ़दारों के हाथ पड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने ब-कमाल-ए-होशियारी ये मशविरा दिया था कि भाइयो, मेरा फ़ारसी कलाम पढ़ो और उर्दू कलाम से एहतिराज़ करो क्योंकि इसमें मेरा रंग है नहीं। लेकिन उनसे ग़लती ये हुई कि ये मशविरा उन्होंने ब-ज़बान-ए-फ़ारसी दिया और ये शे'र उनके उर्दू दीवान में शामिल नहीं किया जा सका। अदब भी शतरंज का खेल है और कौन सी चाल उल्टी पड़ेगी ये बाद में मालूम होता है। नतीजा ये हुआ कि ग़ालिब क़ैद-ए-हयात से तो छूटे लेकिन बंद-ए-ग़म से नहीं छूट सके। ये बंद-ए-ग़म उनके शारहीन और नाक़िदीन की देन है। अताए तू, लक़ाए तू इसे ही कहते हैं।
हमारे हाँ ग़ालिब शनासी का रिवाज कोई 50 साल पहले शुरू हुआ होगा। शुरू-शुरू में ये बड़ा मुश्किल काम था और सिर्फ़ पढ़े लिखे लोग ग़ालिब की तरफ़ मुतवज्जे हुआ करते थे। जिसे भी अपनी उम्र के बेशतर हिस्से की तबाही और अपनी सेहत की बर्बादी मक़सूद होती वो ग़ालिब के कलाम की शरह लिखने का काम अपने ज़िम्मे लेता। रफ़्ता-रफ़्ता ये फ़न फ़ैशन बन गया और फिर इस फ़न ने मरज़ की सूरत इख़्तियार कर ली। ग़ालिब सदी में तो हर शख़्स ग़ालिब के अशआ'र गुनगुनाने लगा। बेरोज़गार नौजवान अपनी मुलाज़िमत की दरख़ास्तों में ये लिखने लगे कि वो कबड्डी और कैरम के अलावा ग़ालिब भी जानते हैं। मुअ'ज़्ज़िज़ लोगों ने महफ़िलों में ऐलान करना शुरू किया कि उनकी हॉबी ग़ालिब हैं और एक ऊंचे दर्जे के क्लब की सदारत के उम्मीदवार के हक़ में ये कहकर वोट हासिल किए गए कि मौसूफ़ गोल्फ और ग़ालिब दोनों के माहिर हैं। कहा जाता है एक ज़माने में ऐसा कड़ा वक़्त फ़्रांस पर भी आया था जब हर शख़्स को पिकासो(असली या जाली)पेंटिंग अपने दीवानख़ाने में लटकानी पड़ी थी और आर्ट की दिल-दादा ख़वातीन में से चंद ने अपने शौहरों से सिर्फ़ इसलिए तलाक़ हासिल कर ली थी कि उनके शौहर पिकासो के फ़न पर बहस नहीं कर सकते थे।(हालाँकि ये बहस सिर्फ़ दो मिनट की होती थी।)
ग़नीमत है कि हमारे हाँ ग़ालिब ने लोगों की इज़दवाजी ज़िंदगी में कोई रख़्ना नहीं डाला। वो सिर्फ़ मर्दाने में रहे। मुम्किन है कि उसकी ये वजह भी रही हो कि हमारे हाँ ख़वातीन का ज़ौक़ अभी इतना बिगड़ा नहीं है कि वो ग़ालिब पर बातचीत कर के ज़ेवर, लिबास और ग़ैर हाज़िर ख़वातीन के अयूब जैसे अहम मसाइल को नजर अंदाज़ कर दें।
ज़ौक़ के लफ़्ज़ पर याद आया कि ज़ौक़ भी ग़ालिब ही के अ'ह्द में शायरी करते थे और दरबार शाही से ख़िलअ'त के अलावा उन्हें हाथी भी इनाम में मिला करते थे। उस ज़माने में हाथी ही सबसे ज़्यादा मुअ'ज्ज़िज़ सवारी थी। इसमें शक नहीं कि नादिर शाह जब हिंदोस्तान आए तो उन्हें ये सवारी पसंद नहीं आई लेकिन नादिर शाह बज़ात-ए-ख़ुद आमियाना ज़ौक़ के आदमी थे। उनमें बुलंद ख़याली का फ़ुक़दान था इसलिए हर मुआमले में और खासतौर पर हाथी जैसी मोअतबर और मुनफ़रिद शख़्सियत के बारे में उनकी राय क़ाबिल-ए-क़ुबूल नहीं हो सकती। शायरी का सही ज़माना वाक़ई वही ज़माना था। एक क़सीदा कहो हाथी ले लो, एक ग़ज़ल कहो दो-चार घोड़े लिखवा लो। क्या ज़माना था। शे'र कहने पर गाँव मिला करते थे, आज शे'र कहो तो लोग गाँव से बाहर कर देते हैं।
ग़ालिब बहुत मक़बूल शायर हैं और उनके कितने ही मिस्रे लोगों को अज़बर हैं। बहुतों को तो पूरे-पूरे शे'र भी याद हैं। ये और बात है कि वो दूसरे मिस्रे को पहले मिस्रे से पहले पढ़ते हैं। लेकिन इसमें कोई क़बाहत नहीं है क्योंकि शायरी कोई क्रिकेट का खेल नहीं है कि दूसरी इनिंग पहली इनिंग के बाद ही खेली जाए। यूँ भी ग़ालिब मिस्रों में ज़्यादा पसंद किए जाने के लायक़ शायर हैं। उन्होंने दस बीस मिस्रे तो इस ग़ज़ब के कहे हैं कि हर ज़रूरत को पूरा करते हैं और अगर वो सिर्फ़ मिस्रे ही कहते, तब भी इतने ही बड़े शायर होते जितने कि वो मुकम्मल शे'र कहने की वजह से हैं। उनकी शायरी का ये पहलू ग़ालिब सदी के दौरान हम सबके सामने आया। जश्न-ए-ग़ालिब के सिलसिले में जितने भी जलसे हुए उन सब जलसों के अनाउंसर ग़ालिब के मिस्रों से पूरी तरह लैस थे जो भी जलसा या मुशायरा हुआ इस मिस्रे से शुरू हुआ,
हुई ताख़ीर तो कुछ बाइ'स-ए-ताख़ीर भी था
सद्र-ए-जलसा के तआ'रुफ़ के सिलसिले में कहा गया,
वो आएं घर में हमारे ख़ुदा की क़ुदरत है
पता नहीं इस मिस्रे से अनाउंसर साहब की क्या मुराद थी। मुम्किन है वो सद्र-ए-जलसा को ख़ुदा की क़ुदरत का नमूना कहना चाह रहे हों। मेहमान-ए-ख़ुसूसी की ता'रीफ़ के पुल के लिए इस मिस्रे को संग-ए-बुनियाद क़रार दिया गया,
कहता हूँ सच कि झूट की आ'दत नहीं मुझे
इन जलसों में मेहमान-ए-ख़ुसूसी का इंतिख़ाब उ'मूमन तबका-ए-इनास ही से किया जाता था और ग़ालिब के कई मिस्रे उन पर सर्फ़ किए जाते थे।
ग़ालिब सदी की वजह से कुछ दिलदोज़ वाक़ियात भी हुए। कुछ लोग ग़ालिब की मोहब्बत में इतने आगे निकल गए कि वापस आने का रास्ता भूल गए। एक साहब ने उन्ही दिनों अपना सर-नेम ग़ालिबी मुक़र्रर कर लिया और वो मिर्ज़ा अहमदुल्लाह बेग ग़ालिबी कहलाने लगे। (कुछ लोग तो उन्हें ग़ालिबन भी कहते थे) इस साल उन्होंने बाज़ाब्ता हलफ़ उठाया था कि वो कोई काम ग़ालिब के दीवान से मदद लिए बगै़र नहीं करेंगे। इत्तिफ़ाक़ से उसी साल उनके हाँ एक फ़र्ज़न्द की विलादत अ'मल में आई। दोस्तों ने घर आकर मुबारकबाद दी तो उन्होंने मुबारकबाद के जवाब में इरशाद फ़रमाया,
मुझे दिमाग़ नहीं ख़ंदा हाय-बेजा का
दोस्तों में से किसी ने पूछा मिर्ज़ा साहब: इस मिस्रे का यहाँ क्या मौक़ा था। बोले मैं सब जानता हूँ,
हथकंडे हैं चर्ख़ नीली फ़ाम के
मिर्ज़ा साहब पेशे से डाक्टर हैं। डाक्टरी ठीक-ठाक चल रही थी लेकिन ग़ालिब का कुछ ऐसा जुनून उन पर सवार हुआ कि फिर ये कहीं के नहीं रहे, एक मुअ'ज्ज़िज़ घराने की ख़ातून उनसे फ़ोन पर अपने मर्ज़ की कैफ़ियत बयान कर रही थीं। मरीज़ा ने जब उनसे कहा कि मिर्ज़ा साहब मेरी कमर में भी दर्द होता है तो मिर्ज़ा साहब ने फ़ोन पर ही झूम कर कहा हाँ-हाँ यक़ीनन होता होगा,
क्या जानता नहीं हूँ तुम्हारी कमर को मैं
एक और मरीज़ा के साथ भी तक़रीबन ऐसा ही वाक़िआ हुआ। डाक्टर साहब अपने मतब में मरीज़ा का मुआईना फ़रमा रहे थे और साथ ही साथ ज़ेर-ए-लब गुनगुना रहे थे, आ तुझे किस तमन्ना से हम देखते हैं। उस दिन न सिर्फ़ इस मरीज़ा का नक़्श-ए-क़दम उनके सर पर पड़ा बल्कि उन दोनों ख़वातीन के शौहरों ने उन्हें अदालत में भी घसीट लिया और बजाए इसके कि मिर्ज़ा साहब राह-ए-रास्त पर क़दम रंजा फ़रमाने की कोशिश करते, फ़ख़्रिया फ़रमाते रहे इन मुक़दमों से क्या होता है।
रंग खुलता जाए है जितना कि उड़ता जाए है
उन पर ग़ालिबी रंग चढ़ता ही गया और एक मेटरनिटी होम के संग-ए-बुनियाद रखने के लिए जब शहर की ख़ातून-ए-अव्वल ने अपने हिना आलूदा हाथों से मख़सूस पत्थर को छुआ तो मिर्ज़ा साहब ने ब आवाज़ बुलंद अपने महबूब शायर का मिस्रा पढ़ दिया,
ख़ाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं
उसी वक़्त उनका नाम दर्ज रजिस्टर कर लिया गया और इसके बाद कुछ ऐसे वाक़िआत हुए कि इश्क़ के बाद ही उनके दिमाग़ में ख़लल आ गया।
ग़ालिब शनासी के ऐसे मोहलिक हादिसे और भी हुए हैं लेकिन ग़ालिब के नाम का फ़ैज़ भी जारी है और कभी-कभी जी चाहता है कि काश ग़ालिब आज हमारे दरमियान मौजूद होते। हम उन्हें बड़े एहतिमाम से किसी कुल-हिंद मुशायरे में बुलवाते और उन्हीं के मेयार के किसी अच्छे अनाउंसर का इंतिख़ाब करते। मुशायरे के डायस पर उन्हें किसी डाइमंड जुब्ली करने वाली फ़िल्म की हीरोइन के बिल्कुल मुत्तसिल न सही, उसके क़ुर्ब-ओ-जवार में जगह देते। किसी हीरो से उनकी गुल पोशी करवाते और थोड़ा बहुत उनका कलाम भी सुनते। ग़ालिब यक़ीनन ख़ुश होते और उन्हें ये शिकायत न होती कि शायरी में इज़्ज़त नहीं हुआ करती।
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.