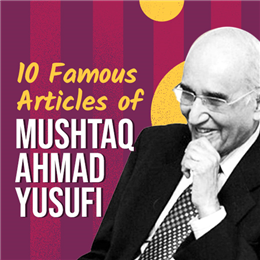पड़िए गर बीमार
तो कोई न हो तीमारदार? जी नहीं! भला कोई तीमारदार न हो तो बीमार पड़ने से फ़ायदा? और अगर मर जाईए तो नौहा-ख़्वाँ कोई न हो? तौबा कीजिए मरने का ये अकल खरा दक़ियानूसी अंदाज़ मुझे कभी पसंद न आया। हो सकता है ग़ालिब के तरफ़दार ये कहें कि मग़रिब को महज़ जीने का क़रीना आता है, मरने का सलीक़ा नहीं आता। और सच पूछिए तो मरने का सलीक़ा कुछ मशरिक़ ही का हिस्सा है।
इसी बिना पर ग़ालिब की नफ़ासत पसंद तबीयत ने 1277 हि. में वबाए आम में मरना अपने लायक़ न समझा कि इसमें उनकी कस्र-ए-शान थी। हालाँकि अपनी पेशेनगोई को सही साबित करने की ग़रज़ से वो उसी साल मरने के आर्ज़ूमंद थे।
इसमें शक नहीं कि हमारे हाँ बाइज़्ज़त तरीक़े से मरना एक हादिसा नहीं, हुनर है जिसके लिए उम्र-भर रियाज़ करना पड़ता है और अल्लाह अगर तौफ़ीक़ न दे तो ये हर एक के बस का रोग भी नहीं। बिलखुसूस पेशेवर सियासतदान उसके फ़न्नी आदाब से वाक़िफ़ नहीं होते। बहुत कम लीडर ऐसे गुज़रे हैं जिन्हें सही वक़्त पर मरने की सआदत नसीब हुई।
मेरा ख़्याल है कि हर लीडर की ज़िंदगी में ख़ाह वो कितना ही गया गुज़रा क्यों न हो, एक वक़्त ज़रूर आता है जब वो ज़रा जी कड़ा कर के मर जाये या अपने सियासी दुश्मनों को रिश्वत देकर अपने आपको शहीद करा ले तो वो लोग साल के साल न सही हर इलेक्शन पर ज़रूर धूम धाम से उसका उर्स मनाया करें। अलबत्ता दिक़्क़त ये है कि इस क़िस्म की सआदत दूसरे के ज़ोर-ए-बाज़ू पर मुनहसिर है और सादी कह गए हैं कि दूसरे के बलबूते पर जन्नत में जाना अक़ूबत दोज़ख़ के बराबर है। फिर उसका क्या ईलाज कि इंसान को मौत हमेशा क़ब्ल अज़ वक़्त और शादी बाद अज़ वक़्त मालूम होती है।
बात कहाँ से कहाँ जा पहुंची। वर्ना सर-ए-दस्त मुझे उन ख़ुशनसीब जवाँ मर्गों से सरोकार नहीं जो जीने के क़रीने और मरने के आदाब से वाक़िफ़ हैं। मेरा ताल्लुक़ तो उस मज़लूम अक्सरियत से है जिसको बक़ौल शायर,
जीने की अदा याद, न मरने की अदा याद
चुनांचे इस वक़्त मैं उस बेज़बान तबक़े की तर्जुमानी करना चाहता हूँ जो इस दरमियानी कैफ़ियत से गुज़र रहा है जो मौत और ज़िंदगी दोनों से ज़्यादा तकलीफ़देह और सब्र-आज़मा है, या’नी बीमारी। मेरा इशारा उस तबक़े की तरफ़ है जिसे सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है सेहत के सिवा।
मैं उस जिस्मानी तकलीफ़ से बिल्कुल नहीं घबराता जो लाज़िमा अलालत है। एस्प्रीन की सिर्फ़ एक गोली या मार्फिया का एक इंजेक्शन उससे नजात दिलाने के लिए काफ़ी है लेकिन इस रुहानी अज़ीयत का कोई ईलाज नहीं जो अयादत करने वालों से मुसलसल पहुँचती रहती है।
एक दाइम-उल-मर्ज़ की हैसियत से जो इस दर्द ला-दवा की लज़्ज़त से आश्ना है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मार्फिया के इंजेक्शन मरीज़ के बजाय मिज़ाजपुर्सी करने वालों के लगाए जाएं तो मरीज़ को बहुत जल्द सुकून आ जाए।
उर्दू शायरों के बयान को बावर किया जाये तो पिछले ज़माने में अलालत की ग़ायत 'तक़रीब बह्र-ए-मुलाक़ात’ के सिवा कुछ न थी। महबूब अयादत के बहाने ग़ैर के घर जाता था और हर समझदार आदमी इसी उम्मीद में बीमार पड़ता था कि शायद कोई भूला भटका मिज़ाजपुर्सी को आ निकले,
अलालत बे अयादत जलवा पैदा कर नहीं सकती
उस ज़माने के अंदाज़-ए-अयादत में कोई दिल नवाज़ी होतो हो मैं तो उन लोगों में से हूँ जो महज़ अयादत के ख़ौफ़ से तंदुरुस्त रहना चाहते हैं। एक हस्सास दाइम-उल-मर्ज़ के लिए मिज़ाज अच्छा है? एक रस्मी या दुआइया जुमला नहीं बल्कि ज़ाती हमला है जो हर बार उसे कमतरी में मुब्तला कर देता है। मैं तो आए दिन की पुरसिश-ए-हाल से इस क़दर बेज़ार हो चुका हूँ कि अहबाब को आगाह कर दिया है कि जब तक मैं बक़लम ख़ुद ये इत्तिला न दूं कि आज अच्छा हूँ, मुझे हस्ब-ए-मामूल बीमार ही समझें और मिज़ाजपुर्सी करके शर्मिंदा होने का मौक़ा न दें।
सुना है शाइस्ता आदमी की ये पहचान है कि अगर आप उससे कहें कि मुझे फ़ुलां बीमारी है तो वो कोई आज़मूदा दवा न बताए। शाइस्तगी का ये सख़्त मेयार सही तस्लीम कर लिया जाये तो हमारे मुल्क में सिवाए डाक्टरों के कोई अल्लाह का बंदा शाइस्ता कहलाने का मुस्तहिक़ न निकलने।
यक़ीन न आए तो झूट-मूट किसी से कह दीजिए कि मुझे ज़ुकाम हो गया है। फिर देखिए कैसे कैसे मुजर्रिब नुस्खे़, ख़ानदानी चुटकुले और फ़क़ीरी टोटके आपको बताए जाते हैं। मैं आज तक ये फ़ैसला न कर सका कि इसकी असली वजह तिब्बी मालूमात की ज़्यादती है या मज़ाक़-ए-सलीम की कमी। बहरहाल बीमार को मश्वरा देना हर तंदुरुस्त आदमी अपना ख़ुशगवार फ़र्ज़ समझता है और इन्साफ़ की बात ये है कि हमारे यहां निन्नानवे फ़ीसद लोग एक दूसरे को मश्वरे के इलावा और दे भी क्या सकते हैं।
बाज़औक़ात अहबाब इस बात से बहुत आज़ुर्दा हैं कि मैं उनके मश्वरों पर अमल नहीं करता। हालाँकि उन पर अमल पैरा न होने का वाहिद सबब ये है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा ख़ून किसी अज़ीज़ दोस्त की गर्दन पर हो। इस वक़्त मेरा मंशा सलाह-ओ-मश्वरा के नुक़्सानात गिनवाना नहीं (इसलिए कि मैं दिमाग़ी सेहत के लिए ये ज़रूरी समझता हूँ कि इंसान को पाबंदी से सही ग़िज़ा और ग़लत मश्वरा मिलता रहे। इसी से ज़ेहनी तवाज़ुन क़ायम रहता है न यहां सितमहाए अज़ीज़ाँ का शिकवा मक़सूद है।
मुद्दआ सिर्फ़ अपने उन बही ख़्वाहों को मुतआरिफ़ कराना है जो मेरे मुज़मिन अमराज़ के अस्बाब-ओ-अलल पर ग़ौर करते और अपने मश्वरे से वक़तन फ़वक़तन मुझे मुस्तफ़ीद फ़रमाते रहते हैं। अगर इस ग़ोल में आपको कुछ जानी-पहचानी सूरतें नज़र आएं तो मेरी ख़स्तगी की दाद देने की कोशिश न कीजिए, आप ख़ुद लायक़-ए-हमदर्दी हैं।
सर-ए-फ़हरिस्त उन मिज़ाजपुर्सी करने वालों के नाम हैं जो मर्ज़ तशख़ीस करते हैं न दवा तजवीज़ करते हैं। मगर उसका ये मतलब नहीं कि वो मुन्कसिर मिज़ाज हैं। दरअसल उनका ताल्लुक़ उस मदरसा-ए-फ़िक्र से है जिसके नज़दीक परहेज़ ईलाज से बेहतर है। ये इस शिकम आज़ार अक़ीदे के मोबल्लिग़-ओ-मुअय्यिद हैं कि खाना जितना फीका सीठा होगा सेहत के लिए उतना ही मुफ़ीद होगा।
यहां ये बताना बेमहल न होगा कि हमारे मुल्क में दवाओं के ख़वास दरयाफ़्त करने का भी यही मेयार है जिस तरह बा’ज़ ख़ुश एतिक़ाद लोगों को अभी तक ये ख़्याल है कि हर बदसूरत औरत नेक-चलन होती है। उसी तरह तिब्ब क़दीम में हर कड़वी चीज़ को मुसफ़्फ़ा-ए-ख़ून तसव्वुर किया जाता है। चुनांचे हमारे हाँ अंग्रेज़ी खाने और कड़वे कदहे इसी उम्मीद में नोश-ए-जान किए जाते हैं।
इस क़बील के हमदर्दान-ए-सेहत दो गिरोहों में बट जाते हैं। एक वो ग़िज़ा रसीदा बुज़ुर्ग जो खाने से ईलाज करते हैं। दूसरे वो जो ईलाज और खाने दोनों से परहेज़ तजवीज़ फ़रमाते हैं। पिछली गर्मियों का वाक़िया है कि मेरी बाएं आँख में गोहान्जनी निकली तो एक नीम जान जो ख़ुद को पूरा हकीम समझते हैं, छूटते ही बोले, ''फ़म मेदा पर वर्म मालूम होता है। दोनों वक़्त मूंग की दाल खाइए। दाफ़े नफ़ख़-ओ-मुहल्लि वर्म है।”
मैंने पूछा, “आख़िर आपको मेरी ज़ात से कौन सी तकलीफ़ पहुंची जो ये मश्वरा दे रहे हैं?”
फ़रमाया, “क्या मतलब?”
अर्ज़ किया, “दो-चार दिन मूंग की दाल खा लेता हूँ तो उर्दू शायरी समझ में नहीं आती और तबीयत बेतहाशा तिजारत की तरफ़ माइल होती है। इस सूरत में ख़ुदा-न-ख़्वास्ता तंदुरुस्त हो भी गया तो जी के क्या करूँगा?”
बोले, “आप तिजारत को इतना हक़ीर क्यों समझते हैं? अंग्रेज़ हिंदुस्तान में दाख़िल हुआ तो उसके एक हाथ में तलवार और दूसरे में तराज़ू थी।”
गुज़ारिश की, “और जब वो गया तो एक हाथ में यूनीयन जैक था और दूसरी आस्तीन ख़ाली लटक रही थी।”
बात उन्हें बहुत बुरी लगी। इसलिए मुझे यक़ीन हो गया कि सच थी। उसके बाद ताल्लुक़ात इतने कशीदा हो गए कि हमने एक दूसरे के लतीफों पर हँसना छोड़ दिया। इस्तिआरा-ओ-किनाया बरतरफ़, मेरा अपना अक़ीदा तो ये है कि जब तक आदमी को ख़वास की ग़िज़ा मिलती रहे, उसे ग़िज़ा के ख़वास के बखेड़े में पड़ने की मुतलक़ ज़रूरत नहीं। सच पूछिए तो उम्दा ग़िज़ा के बाद कम-अज़-कम मुझे तो बड़ा इंशिराह महसूस होता है और बेइख़्तियार जी चाहता है कि बढ़ के हर राहगीर को सीने से लगा लूं।
दूसरा गिरोह क़ुव्वत-ए-इरादी से दवा और ग़िज़ा का काम लेना चाहता है और जिस्मानी अवारिज़ के ईलाज-मुआलिजा से पहले दिमाग़ की इस्लाह करना ज़रूरी समझता है। ये हज़रात इब्तदाए मर्ज़ ही से दवा के बजाय दुआ के क़ाइल हैं और उनमें भारी अक्सरियत उन सत्रे-बहत्रे बुज़ुर्गों की है जो घिगिया घिगिया कर अपनी दराज़ी-ए-उम्र की दुआ मांगते हैं और उसी को ऐन इबादत समझते हैं।
इस रुहानी ग़िज़ा के लिए मैं फ़िलहाल अपने आपको तैयार नहीं पाता। मुझे इस पर क़तअन ताज्जुब नहीं होता कि हमारे मुल्क में पढ़े लिखे लोग ख़ूनी पेचिश का ईलाज गंडे-तावीज़ों से करते हैं। ग़ुस्सा इस बात पर आता है कि वो वाक़ई अच्छे हो जाते हैं।
कुछ ऐसे अयादत करने वाले भी हैं जिनके अंदाज़-ए-पुर्सिश से ज़ाहिर होता है कि बीमारी एक संगीन जुर्म है और किसी आसमानी हिदायत के बमूजब उसकी तफ़तीश पर मामूर किए गए हैं।
पिछले साल जब इंफ्लुएंज़ा की वबा फैली और मैं भी साहिब-ए-फ़राश हो गया तो एक हमसाये जो कभी फटकते भी न थे, कमरा-ए- अलालत में ब नफ़स-ए-नफ़ीस तशरीफ़ लाए और ख़ूब कुरेद कुरेद कर जिरह करते रहे। बिलआख़िर अपना मुँह मेरे कान के क़रीब करके राज़दाराना अंदाज़ में कुछ ऐसे निजी सवालात किए जिनके पूछने का हक़ मेरी नाचीज़ राय में बीवी और मुनकिर नकीर के इलावा किसी को नहीं पहुंचता।
एक बुजु़र्गवार हैं जिनसे सिर्फ़ दौरान-ए-अलालत में मुलाक़ात होती है, इसलिए अक्सर होती रहती है। मौसूफ़ आते ही बरस पड़ते हैं और गरजते हुए रुख़सत होते हैं। पिछले हफ़्ते का ज़िक्र है, हलहला कर बुख़ार चढ़ रहा था कि वो आ धमके, कपकपा कर कहने लगे, बीमारी आज़ारी में भी बड़ी ग़ैरियत बरतते हो, बारख़ुरदार, दो घंटे से मलेरिया में चुपचाप मुब्तला हो और मुझे ख़बर तक ना की।”
बहतेरा जी चाहा कि इस दफ़ा उनसे पूछ ही लूं कि क़िबला कुनैन अगर आपको बरवक़्त इत्तिला करा देता तो आप मेरे मलेरिया का क्या बिगाड़ लेते?”
उनकी ज़बान इस क़ैंची की तरह है जो चलती ज़्यादा है और काटती कम। डाँटने का अंदाज़ ऐसा है जैसे कोई कौदन लड़का ज़ोर ज़ोर से पहाड़े याद कर रहा हो। मुझे उनकी डाँट पर ज़रा ग़ुस्सा नहीं आता। क्योंकि अब उसका मज़मून अज़बर हो गया है। यूं भी उस केंडे के बुज़ुर्गों की नसीहत में से डाँट और डाढ़ी को अलैहदा कर दिया जाये या बसूरत नुक़्स अमन डाँट में डंक निकाल दिया जाये तो बक़ीया बात (अगर कोई चीज़ बाक़ी रहती है निहायत लगो मालूम होगी।
उनका आना फ़रिश्ता-ए-मौत का आना है। मगर मुझे यक़ीन है कि हज़रत इज़राईल अलैहिस-सलाम रूह क़ब्ज़ करते वक़्त इतनी डाँट-डपट नहीं करते होंगे। ज़ुकाम उन्हें निमोनिया का पेश-ख़ेमा दिखाई देता है और ख़सरा में टाईफ़ाइड के आसार नज़र आते हैं।
उनकी आदत है कि जहां महज़ सीटी से काम चल सकता है वहां बेधड़क बिगुल बजा देते हैं। मुख़्तसर ये कि एक ही सांस में ख़ुदा-न-ख़्वास्ता से इन्नल्लाह तक की तमाम मंज़िलें तय करलेते हैं। उनकी मंज़ूम डाँट की तमहीद कुछ इस क़िस्म की होती है,
“मियां ये भी कोई अंदाज़ है कि घर के रईसों की तरह नब्ज़ पर हाथ धरे मुंतज़िर-ए-फ़र्दा हो। बेकारी बीमारी का घर है। शायर ने क्या ख़ूब कहा है,
बीमार मबाश कुछ किया कर
मिसरे का जवाब शे’र से देता हूँ,
कमज़ोरी मेरी सेहत भी, कमज़ोर मिरी बीमारी भी
अच्छा जो हुआ कुछ कर न सका, बीमार हुआ तो मर न सका
ये सुनकर वो बिफर जाते हैं और अपने सिन-ओ-साल की आड़ लेकर कौसर-ओ-तसनीम में धुली हुई ज़बान में वो बेनुक़त सुनाते हैं कि ज़िंदा तो दर किनार मुर्दा भी एक दफ़ा कफ़न फाड़ कर सवाल-ओ-जवाब के लिए उठ बैठे।
तक़रीर का लुब्ब-ए-लुबाब ये होता है कि राक़िम-उल-हरूफ़ जान-बूझ कर अपनी तंदुरुस्ती के पीछे हाथ धो कर पड़ा है। मैं उन्हें यक़ीन दिलाता हूँ कि अगर ख़ुदकुशी मेरा मंशा होता तो यूं एड़ियां रगड़ रगड़ कर नहीं जीता, बल्कि आँख बंद कर के उनकी तजवीज़ करदा दवाएं खा लेता।
आईए, एक और मेहरबान से आपको मिलाऊं। उनकी तकनीक क़दरे मुख़्तलिफ़ है। मेरी सूरत देखते ही ऐसे हिरासाँ होते हैं कि कलेजा मुँह को आता है। उनका मामूल है कि कमरे में बग़ैर खटखटाए दाख़िल होते हैं और मेरे सलाम का जवाब दिए बग़ैर तीमारदारों के पास पंजों के बल जाते हैं। फिर खुसर फुसर होती है। अलबत्ता कभी कभी कोई उचटता हुआ फ़िक़रा मुझे भी सुनाई दे जाता है। मसलन,
“सदक़ा दीजिए, जुमेरात की रात भारी होती है।”
“पानी हलक़ से उतर जाता है?”
“आदमी पहचान लेते हैं?”
यक़ीन जानिए। ये सुनकर पानी सर से गुज़र जाता है और मैं तो रहा एक तरफ़, ख़ुद तीमारदार मेरी सूरत नहीं पहचान सकते।
सरगोशियों के दौरान एक-दो दफ़ा मैंने ख़ुद दख़ल देकर बकायमी होश-ओ-हवास अर्ज़ करना चाहा कि मैं बफ़ज़्ल-ए-तआला चाक़-ओ-चौबंद हूँ। सिर्फ़ पेचीदा दवाओं में मुब्तला हूँ। मगर वो इस मसले को क़ाबिल-ए-दस्त अंदाज़ी-ए-मरीज़ नहीं समझते और अपनी शहादत की उंगली होंटों पर रखकर मुझे ख़ामोश रहने का इशारा करते हैं।
मेरे ऐलान सेहत और उनकी पुरज़ोर तरदीद से तीमारदारों को मेरी दिमाग़ी सेहत पर शुबहा होने लगता है। यूं भी अगर बुख़ार सौ डिग्री से ऊपर हो जाये तो मैं हिज़यान बकने लगता हूँ जिसे बेगम, इक़बाल-ए-गुनाह और रिश्तेदार वसीयत समझ कर डाँटते हैं और बच्चे डाँट समझ कर सहम जाते हैं। मैं अभी तक फ़ैसला नहीं कर सकता कि ये हज़रत मिज़ाजपुर्सी करने आते हैं या पुर्सा देने।
उनके जाने के बाद मैं वाक़ई महसूस करता हूँ कि बस अब चल-चलाव लग रहा है। सांस लेते हुए धड़का लगा रहता है कि रिवायती हिचकी न आजाए। ज़रा गर्मी लगती है तो ख़्याल होता है कि शायद आख़िरी पसीना है और तबीयत थोड़ी बहाल होती है तो हड़बड़ाकर उठ बैठता हूँ कि कहीं सँभाला न हो।
लेकिन मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग का अंदाज़ सबसे निराला है। मैं नहीं कह सकता कि उन्हें मेरी दिलजोई मक़सूद होती है या इसमें उनके फ़लसफ़ा-ए-हयात-ओ-ममात का दख़ल है। बीमारी के फ़ज़ाइल ऐसे दिलनशीन पैराए में बयान करते हैं कि सेहत याब होने को दिल नहीं चाहता, तंदुरुस्ती वबाल मालूम होती है और ग़ुस्ल-ए-सेहत में वो तमाम क़बाहतें नज़र आती हैं, जिनसे ग़ालिब को फ़िक्र-ए-विसाल में दो-चार होना पड़ा कि
गर न हो तो कहाँ जाएं, हो तो क्यूँ-कर हो
अक्सर फ़रमाते हैं कि बीमारी जान का सदक़ा है। अर्ज़ करता हूँ कि मेरे हक़ में तो ये सदक़ा जारीया हो कर रह गई है। इरशाद होता है ख़ाली बीमार पड़ जाने से काम नहीं चलता। इसलिए कि पसमांदा ममालिक में
फ़ैज़ान-ए-अलालत आम सही, इर्फ़ान-ए-अलालत आम नहीं
एक दिन मैं कान के दर्द में तड़प रहा था कि वो आ निकले। इस अफ़रातफ़री के ज़माने में ज़िंदा रहने के शदाएद और मौत के फ़यूज़-ओ-बरकात पर ऐसी मुअस्सर तक़रीर की कि बेइख़्तियार जी चाहा कि उन्ही के क़दमों पर फड़फड़ा कर अपनी जान आफ़रीन के सपुर्द कर दूं और इंशोरंस कंपनी वालों को रोता-धोता छोड़ जाऊं। उनके देखे से मेरे तीमारदारों की मुँह की रही सही रौनक़ जाती रहती है। मगर मैं सच्चे दिल से उनकी इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि मेरा अक़ीदा है कि महज़ जीने के लिए किसी फ़लसफ़ा की ज़रूरत नहीं। लेकिन अपने फ़लसफ़ा की ख़ातिर दूसरों को जान देने पर आमादा करने के लिए सलीक़ा चाहिए।
चूँकि ये मौक़ा ज़ाती तास्सुरात के इज़हार का नहीं, इसलिए मैं मिर्ज़ा के अंदाज़-ए- अयादत की तरफ़ लोटता हूँ। वो जब तंदुरुस्ती को उम्मुल ख़्बाइस और तमाम जराइम की जड़ क़रार देते हैं तो मुझे रह-रह कर अपनी ख़ुशनसीबी पर रश्क आता है। अपने दावे के सबूत में ये दलील ज़रूर पेश करते हैं कि जिन तरक़्क़ी याफ़्ता ममालिक में तंदुरुस्ती की वबा आम है वहां पर जिन्सी जराइम की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है।
मैं कान के दर्द से निढाल होने लगा तो उन्होंने मसलले-मसाइल बयान कर के मेरी ढारस बंधाई, “मियां हिम्मत से काम लो। बड़े बड़े नबियों पर ये वक़्त पड़ा है।”
मैं दर्द से हलकान हो चुका था वर्ना हाथ जोड़ कर अर्ज़ करता कि ख़ुदा मारे या छोड़े, मैं बग़ैर दावा-ए-नबूवत ये अज़ाब झेलने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। इलावा अज़ीं, क़सस-उल-अंबिया मैंने बचपन में पढ़ी थी और ये याद नहीं आ रहा था कि कौन से पैग़ंबर कान के दर्द के बावजूद फ़राइज़-ए-नबवी अंजाम देते रहे।
इस वाक़िया के कुछ दिन बाद मैंने अज़ राह-ए-तफ़न्नुन मिर्ज़ा से कहा, “फेरेंक हैरिस के ज़माने में कोई साहिब-ए-इस्तिताअत मर्द उस वक़्त तक 'जैंटलमैन’ होने का दावा नहीं करसकता था जब तक वो कम अज़ कम एक मर्तबा ना-गुफ़्ता ब जिन्सी अमराज़ में मुब्तला न हुआ हो। ये ख़्याल आम था कि इससे शख़्सियत में लोच और रचाओ पैदा होता है।”
तंबाकू के पान का पहला घूँट पी कर कहने लगे, “ख़ैर ये तो एक अख़लाक़ी कमज़ोरी की फ़लसफ़ियाना तावील है, मगर इसमें शुबहा नहीं कि दर्द अख़लाक़ को सँवारता है।”
वो ठेरे एक झक्की। इसलिए मैंने फ़ौरन ये इक़रार कर के अपना पिंड छुड़ाया कि मुझे इस कुल्लिया से इत्तफ़ाक़ है। बशर्तिकि दर्द शदीद हो और किसी दूसरे के उठ रहा हो।”
पिछले जाड़ों का ज़िक्र है। मैं गर्म पानी की बोतल से सेंक कर रहा था कि एक बुज़ुर्ग जो अस्सी साल के लपेटे में हैं, ख़ैर-ओ-आफ़ियत पूछने आए और देर तक क़ब्र-ओ-आक़िबत की बातें करते रहे जो मेरे तीमारदारों को ज़रा क़ब्ल अज़ वक़्त- मालूम हुईं।
आते ही बहुत सी दुआएं दीं, जिनका ख़ुलासा ये था कि ख़ुदा मुझे हज़ारी उम्र दे ताकि अपने और उनके फ़र्ज़ी दुश्मनों की छाती पर रिवायती मूंग दलने के लिए ज़िंदा रहूं। उसके बाद जांकनी और फ़िशार-ए-गोर का इस क़दर मुफ़स्सिल हाल बयान किया कि मुझे ग़रीबख़ाने पर गोर-ए-ग़रीबाँ का गुमान होने लगा। अयादत में इबादत का सवाब लूट चुके तो मेरी जलती हुई पेशानी पर अपना हाथ रखा जिसमें शफ़क़त कम और रअशा ज़्यादा था और अपने बड़े भाई को (जिनका इंतक़ाल तीन माह क़ब्ल इसी मर्ज़ में हुआ था, जिसमें मैं मुब्तला था, याद कर के कुछ इस तरह आब-दीदा हुए कि मेरी भी हिचकी बंध गई।
मेरे लिए जो तीन अदद सेब लाए थे वो खा चुकने के बाद जब उन्हें कुछ क़रार आया तो वो मशहूर ताज़ियती शे’र पढ़ा जिसमें उन ग़ुंचों पर हसरत का इज़हार किया गया है जो बन खिले मुरझा गए।
मैं फ़ित्रतन रक़ीक़-उल-क़ल्ब वाक़े हुआ हूँ और तबीयत में ऐसी बातों की सहार बिल्कुल नहीं है। उनके जाने के बाद जब लाद चले बंजारा वाला मूड तारी हो जाता है और हालत ये होती है कि हर परछाईं भूत और हर सफ़द चीज़ फ़रिश्ता दिखाई देती है। ज़रा आँख लगती है तो बेरब्त ख़्वाब देखने लगता हूँ।
गोया कोई ‘कामिक’ या बातस्वीर नफ़सियाती अफ़साना सामने खुला हुआ है। क्या देखता हूँ कि डाक्टर मेरी लाश पर इंजेक्शन की पिचकारियों से लड़ रहे हैं और लहूलुहान हो रहे हैं। उधर कुछ मरीज़ अपनी अपनी नर्स को क्लोरोफ़ार्म सुंघा रहे हैं। ज़रा दूर एक लाइलाज मरीज़ अपने डाक्टर को यासीन हिफ़्ज़ करा रहा है।
हर तरफ़ सागूदाने और मूंग की दाल की खिचड़ी के ढेर लगे हैं। आसमान बनफ़्शी हो रहा है और उन्नाब के दरख़्तों की छांव में, सना की झाड़ियों की ओट लेकर बहुत से ग़िल्माँ एक मौलवी को ग़िज़ा बिलजब्र के तौर पर माजूनें खिला रहे हैं। ता हद-ए-नज़र काफ़ूर में बसे हुए कफ़न हवा में लहरा रहे हैं। जा-ब-जा लोबान सुलग रहा है और मेरा सर संगमरमर की लौह-ए-मज़ार के नीचे दबा हुआ है और उसकी ठंडक नस-नस में घुसी जा रही है। मेरे मुँह में सिगरेट और डाक्टर के मुँह में थर्मामीटर है।
आँख खुलती है तो क्या देखता हूँ कि सर पर बर्फ़ की थैली रखी है। मेरे मुँह में थर्मामीटर ठुंसा हुआ है और डाक्टर के होंटों में सिगरेट दबा है।
लगे हाथों, अयादत करने वालों की एक और क़िस्म का तआरुफ़ करा दूं। ये हज़रात जदीद तरीक़-ए-कार बरतते और नफ़सियात का हर उसूल दांव पर लगा देते हैं। हर पाँच मिनट बाद पूछते हैं कि इफ़ाक़ा हुआ या नहीं? गोया मरीज़ से ये तवक़्क़ो रखते हैं कि आलम-ए-नज़अ में भी उनकी मालूमात आम्मा में इज़ाफ़ा करने की ग़रज़ से RUNNING COMMENTARY करता रहेगा।
उनकी ये कोशिश होती है कि किस तरह मरीज़ पर साबित कर दें कि महज़ इंतक़ामन बीमार है या वहम में मुतब्ला है और किसी संगीन ग़लतफ़हमी की बिना पर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। उनकी मिसाल उस रोज़ा खोर की सी है जो इंतहाई नेक नीयती से किसी रोज़ादार का रोज़ा लतीफों से बहलाना चाहता हो। मुकालमा नमूना मुलाहिज़ा हो,
मुलाक़ाती, माशाअल्लाह आज मुँह पर बड़ी रौनक़ है।
मरीज़, जी हाँ आज शेव नहीं किया है।
मुलाक़ाती, आवाज़ में भी करारा पन है।
मरीज़ की बीवी, डाक्टर ने सुबह से सागूदाना भी बंद कर दिया है।
मुलाक़ाती (अपनी बीवी से मुख़ातिब हो कर, बेगमा, ये सेहतयाब हो जाएं तो ज़रा उन्हें मेरी पथरी दिखाना जो तुमने चार साल से स्प्रिट की बोतल में रख छोड़ी है।
(मरीज़ से मुख़ातिब हो कर) साहिब यूं तो हर मरीज़ को अपनी आँख का तिनका भी शहतीर मालूम होता है। मगर यक़ीन जानिए, आपका शिगाफ़ तो बस दो तीन उंगल लंबा होगा, मेरा तो पूरा एक बालिश्त है। बिल्कुल कनखजुरा मालूम होता है।
मरीज़ (कराहते हुए), मगर मैं टाईफ़ाइड में मुब्तला हूँ।
मुलाक़ाती (एका एकी पैंतरा बदल कर) ये सब आपका वहम है। आपको सिर्फ़ मलेरिया है।
मरीज़, ये पास वाली चारपाई, जो अब ख़ाली पड़ी है, उसका मरीज़ भी इसी वहम में मुब्तला था।
मुलाक़ाती, अरे साहिब! मानिए तो आप बिल्कुल ठीक हैं। उठकर मुँह हाथ धोईए।
मरीज़ की बीवी (रुहांसी हो कर), दो दफ़ा धो चुके हैं, सूरत ही ऐसी है।
इस वक़्त एक देरीना करम फ़र्मा याद आ रहे हैं, जिनका तर्ज़-ए-अयादत ही और है। ऐसा हुलिया बना कर आते हैं कि ख़ुद उनकी अयादत फ़र्ज़ हो जाती है,
“मिज़ाज शरीफ़” को वह रस्मी फ़िक़रा नहीं, बल्कि सालाना इम्तिहान का सवाल समझते हैं और सचमुच अपने मिज़ाज की जुमला तफ़सीलात बताना शुरू कर देते हैं।
एक दिन मुँह का मज़ा बदलने की ख़ातिर मैंने “मिज़ाज शरीफ़” के बजाय “सब ख़ैरीयत है?” से पुर्सिश-ए-अहवाल की।
पलट बोले, “इस जहान-ए-शरियत में ख़ैरीयत कहाँ?” इस माबाद-उल-तबैयाती तमहीद के बाद कराची के मौसम की ख़राबी का ज़िक्र आँखों में आँसू भरकर ऐसे अंदाज़ से किया, गोया उन पर सरासर ज़ाती ज़ुल्म हो रहा है, और उसकी तमाम-तर ज़िम्मेदारी म्यूनसिपल कारपोरेशन पर आइद होती है।
आपने देखा होगा कि बा’ज़ औरतें शायर की नसीहत के मुताबिक़ वक़्त को पैमाना-ए-इमरोज़-ओ-फ़र्दा से नहीं नापतीं बल्कि तारीख़-ओ-सन और वाक़ियात का हिसाब अपनी यादगार ज़च्चगियों से लगाती हैं। मज़कूर-उल-सदर दोस्त भी अपनी बीमारियों से कैलेंडर का काम लेते हैं। मसलन शहज़ादी मारग्रेट की उम्र वो अपने दम्मे के बराबर बताते हैं। स्वेज़ से अंग्रेज़ों के नहर बदर किए जाने की तारीख़ वही है जो उनका पित्ता निकाले जाने की।
मेरा क़ायदा है कि जब वो अपनी और जुमला मुताल्लिक़ीन की अदम ख़ैरियत की तफ़सीलात बता कर उठने लगते तो इत्तिलाअन अपनी ख़ैरियत से आगाह कर देता हूँ।
बीमार पड़ने के सदहा नुक़्सानात हैं। मगर एक फ़ायदा भी है, वो ये कि इस बहाने अपने बारे में दूसरों की राय मालूम हो जाती है। बहुत सी कड़वी-कसैली बातें जो आम तौर पर होंटों पर लरज़ कर रह जाती हैं, बेशुमार दिल-आज़ार फ़िक़रे जो ख़ौफ़-ए-फ़साद-ए-ख़ल्क़ से हलक़ में अटक कर रह जाते हैं, उस ज़माने में यार लोग नसीहत की आड़ में “हो-अल-शाफ़ी” कह कर बड़ी बेतकल्लुफ़ी से दाग़ देते हैं।
पिछले सनीचर की बात है। मेरी अक़ल डाढ़ में शदीद दर्द था कि एक रूठे हुए अज़ीज़ जिनके मकान पर हाल ही में क़र्ज़ के रुपया से छत पड़ी थी, लुक्क़ा कबूतर की मानिंद सीना ताने आए और फ़रमाने लगे, “हैं आप भी ज़िद्दी आदमी, लाख समझाया कि अपना ज़ाती मकान बनवा लीजिए मगर आपके कान पर जूं नहीं रेंगती।”
ताने की काट दर्द की शिद्दत पर ग़ालिब आई और मैंने डरते डरते पूछा, “भाई! मेरी अक़ल तो इस वक़्त काम नहीं करती। ख़ुदारा आप ही बताईए, क्या ये तकलीफ़ सिर्फ़ किरायादारों को होती है?”
हंसकर फ़रमाया, “भला ये भी कोई पूछने की बात है। किराए के मकान में तंदूरुस्ती क्यूँकर ठीक रह सकती है?”
कुछ दिन बाद जब उन्ही हज़रत ने मेरे घुटने के दर्द को बे दूध की चाय पीने और रमी खेलने का शाख़साना क़रार दिया तो बेइख़्तियार उनका सर पीटने को जी चाहा।
अब कुछ जग-बीती भी सुन लीजिए।
झूट-सच का हाल ख़ुदा जाने, लेकिन एक दोस्त अपना तजुर्बा बयान करते हैं कि दो माह क़ब्ल उनके गले में ख़राश हो गई, जो उनके नज़दीक बद-मज़ा खाने और घर वालों के ख़्याल में सिगरेट की ज़्यादती का नतीजा थी। शुरू में तो उन्हें अपनी बैठी हुई आवाज़ बहुत भली मालूम हुई और क्यों न होती? सुनते चले आए हैं कि बैठी हुई (HUSKY) आवाज़ में बेपनाह जिन्सी कशिश होती है।
ख़ुदा की देन थी कि घर बैठे आवाज़ बैठ गई। वर्ना अमरीका में तो लोग कोकाकोला की तरह डालर बहाते हैं जब कहीं आवाज़ में ये मुस्तक़िल ज़ुकाम की सी कैफ़ियत पैदा होती है। लिहाज़ा जब ज़रा इफ़ाक़ा महसूस हुआ तो उन्होंने रातों को गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर, बल्कि खंखुना खंखुना कर दुआएं मांगीं,
“बारे इलाही, तेरी शान-ए-करीमी के सदक़े, ये सोज़िश भले ही कम हो जाये, मगर भर्राहट यूंही क़ायम रहे!”
लेकिन चंद दिन बाद जब उनका गला ख़ाली नल की तरह भक् भक् करने लगा तो उन्हें भी तशवीश हुई।
किसी ने कहा, “लुक़्मान का क़ौल है कि पानी पीते वक़्त एक हाथ से नाक बंद कर लेने से गला कभी ख़राब नहीं होता।”
एक साहिब ने इरशाद फ़रमाया, “सारा फ़ुतूर फल न खाने के सबब है। मैं तो रोज़ाना निहार मुँह पंद्रह फुट गन्ना खाता हूँ। मेदा और दाँत दोनों साफ़ रहते हैं।” और सबूत में उन्होंने अपने मस्नूई दाँत दिखाए जो वाक़ई बहुत साफ़ थे।
एक और ख़ैरख़ाह ने इत्तिला दी कि ज़ुकाम एक ज़हरीले वाइरस से होता है जो किसी दवा से नहीं मरता। लिहाज़ा जोशांदा पीजिए कि इंसान के इलावा कोई जानदार उसका ज़ायक़ा चख कर ज़िंदा नहीं रह सकता।
बक़ीया रूदाद उन्ही की ज़बान से सुनिए, और जिन करम फ़र्माओं ने अज़ राह-ए- कसर-ए-नफ़सी दवाएं तजवीज़ नहीं कीं, वो हकीमों और डाक्टरों के नाम और पते बता कर अपने फ़राइज़-ए-मंसबी से सुबुकदोश हो गए। किसी ने इसरार किया कि आयुर्वेदिक ईलाज कराओ। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि मैं तिब्बी मौत मरना चाहता हूँ।
किसी ने मश्वरा दिया कि हकीम नब्बाज़ मिल्लत से रुजू कीजिए। नब्ज़ पर उंगली रखते ही मरीज़ का शिजरा-ए-नसब बता देते हैं (इसी वजह से कराची में उनकी तबाबत ठप है) क़ारुरे पर नज़र डालते ही मरीज़ की आमदनी का अंदाज़ा कर लेते हैं। आवाज़ अगर साथ देती तो मैं ज़रूर अर्ज़ करता कि ऐसे काम के आदमी को तो इन्कम टैक्स के महिकमा में होना चाहिए।
ग़रज़ कि जितने मुँह उनसे कहीं ज़्यादा बातें! और तो और सामने के फ़्लैट में रहने वाली स्टेनोग्राफ़र (जो चुस्त स्वेटर और जीन्स पहन कर, बक़ौल मिर्ज़ा अब्दुल बेग, अंग्रेज़ी का s मालूम होती है) भी मिज़ाजपुर्सी को आई और कहने लगी, हकीमों के चक्कर में न पड़िये। आँख बंद कर के डाक्टर दिलावर के पास जाईए। तीन महीने हुए, आवाज़ बनाने की ख़ातिर मैंने इमली खा खा कर गले का नास मार लिया था। मेरी ख़ुशनसीबी कहिए कि एक सहेली ने उनका पता बता दिया। अब बहुत इफ़ाक़ा है।
इस बयान की ताईद कुछ दिन बाद मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग ने भी की। उन्होंने तसदीक़ की डाक्टर साहिब अमरीकी तरीक़े से ईलाज करते हैं और हर केस को बड़ी तवज्जो से देखते हैं। चुनांचे सैंडिल के इलावा हर चीज़ उतरवा कर उन्होंने स्टेनोग्राफ़र के हलक़ का बग़ौर मुआइना किया। ईलाज से वाक़ई काफ़ी इफ़ाक़ा हुआ और वो इस सिलसिले में अभी तक पीठ पर बनफ़्शी शुआओं से सेंक कराने जाती है।
मुझे यक़ीन है कि इस तरीक़ा-ए-इलाज से डाक्टर मौसूफ़ को काफ़ी इफ़ाक़ा हुआ होगा।
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.